| Mansoor hasan | ||||
| Ramesh Saini | Eric Chopra |
 Sneha Richariya
Sneha Richariya
स्नेहा रिछारिया
जो मैंने लिखे हैं तीन हज़ार शब्द उनको कितने लोग पढ़ेंगे, कितने लोग समझेंगे ?:— स्नेहा
परिचय
स्नेहा रिछारिया नई दिल्ली में एक मल्टीमीडिया पत्रकार हैं। इनका काम स्वास्थ्य, पर्यावरण और लिंगभेद समस्या पर प्रमुख रूप से केंद्रित है। स्नेहा जी ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं, “शब्द संवाद” में अरमान नदीम से बात करते हुए बताया की किस तरह ऑनलाइन मीडिया प्लेटफार्म अपने पत्रकारो को प्रताड़ित करते है। उनके हिसाब से आज के वक्त में सोशल मीडिया ने जो फ़िल्टर हटा दिया है वो नई पीढ़ी के लिए बेहद ख़तरनाक है, स्नेहा बताती है की पॉडकास्टिंग को किस तरह से कंपनीज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है । एक सवाल के जवाब में बताया कि “लोग इसे एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं लेंगे लोग समझते हैं कि यह 30 मिनट का एपिसोड है जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा” लेकिन जब उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है तो वो हाथ खड़े कर देते है।
बातचीत के प्रमुख अंश
अरमान नदीम:- आपने अलग-अलग न्यूज एजेंसियों के लिए काम किया है। आपका काम सबसे ग्राउंड पर दिखता भी है लेकिन मैं यही जानना चाहूंगा कि अपने पत्रकारिता को ही क्यों चुना ?
स्नेहा रिछारिया :- अच्छा, क्यों चुना जब हम बचपन में पढ़ाई कर रहे थे उस समय टीवी देखते थे तो यह काम अच्छा लगता था आमतौर पर उस वक्त पत्रकारिता को एंकरिंग समझते थे। जो टीवी में दिखते हैं वह शायद पत्रकार हैं। लेकिन जब हम पत्रकारिता की असल दुनिया में आए तो पता चला जैसा सोचते है वैसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की उस वक्त भी उतना समझ नहीं आता था। लेकिन जब जामिया में आए तो एक्टिव होकर देखना शुरू किया अपने से आगे वालों को देखा कि कैसे लिखते हैं और कैसे बात की जाती है। तो उस समय समझ आया कि पत्रकारिता वैसी नहीं है । और समझ आया कि एक एंकर जरूरी नहीं वह पत्रकार हो लेकिन एक पत्रकार एंकर हो सकता है। फिर रिपोर्टिंग के बारे में भी मालूम हुआ कैसे होती है। मुझे लगता है कि मीडिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन हो गया है। और मुश्किल भी हो गई है आज की पत्रकारिता क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है और पहचान करना भी मुश्किल हो गया है की कौन पत्रकार है कौन कंटेंट क्रिएटर है, कौन किस मीडिया के लिए काम करता है। और आम लोगों को तो समझ ही नहीं आता है। आप कहते हैं पत्रकार हैं छोटे शहरों में कुछ समझते हैं बड़े शहरों में कुछ और समझते हैं। ये भी एक चैलेंज है आपने आप में है। लेकिन मैं क्या करती हूं यह मैं आपको बता सकती हूं । मैं डिजिटल स्पेस में काम करती हूं टीवी से मेरा कोई वास्ता नहीं है जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता है वह मैंने कभी नहीं की , ना मैंने कभी किसी न्यूज़ चैनल में काम किया है। अखबार में भी मैं नहीं लिखा है। लेकिन डिजिटल स्पेस में ऑनलाइन पोर्टल है उनसे मैं काफी अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। और मैं जानती हूं कि वह कैसे काम करते हैं और मैं कोशिश करती हूं जो भी मैं लिखती हूं वह तो तीन चीजों से जुड़ा रहता है एनवायरमेंट पर्यावरण संबंधित हेल्थ, हंगर से जुड़ा रहता है कभी-कभी कुछ स्टोरी हो सकती है कि तीनों से जुड़ी होती है। या दो मुद्दे हो। तो इस तरह की स्टोरी में लिखती रहती हूं और उनके कंबाइंड करने से फायदा भी रहता है जो स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग भी रहती है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हां आप कुछ क्रिएटिव लिख रहे हैं कलेक्टिव लिख रहे हैं तो एक जो स्पेस है एनवायरनमेंट का तो मैं इसमें लिखती हूं। और अपने सवाल किया था कि क्यों चुनी पत्रकारिता तो मुझे लगता है कि अगर मैं यह नहीं करती तो शायद किसी कारपोरेट सेक्टर में होती, कोई जॉब कर रही होती। मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट जब आप काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काम करते हैं। लोगों की कहानी बताते हैं तो उसका एक अलग रोमांच होता है। हालांकि उसमें अपने ड्रॉबैक्स भी हैं बहुत सारे। आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके नाम से जाता है। वो सिर्फ इन्हीं चीजों में होता है ना कि किसी और में।
अरमान नदीम :- आपने कहा कि आपका टीवी से कोई वास्ता नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक सवाल उसीसे संबंधित पूछना चाहूंगा आज के वक्त को देखकर क्या आपको मीडिया में निष्पक्षता खतरे में नजर आ रही है?
स्नेहा रिछारिया :- यह जो अपने सवाल पूछा है मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो अभी भी काफी लोग टीवी न्यूज़ चैनल देखते हैं।
अरमान नदीम :- टीवी देखते हैं लेकिन उनका नजरिया बदल चुका है। एक वक्त था जब हम न्यूज़ चैनल देखते थे खबरों के लिए लेकिन अगर अब टिपिकल टीवी न्यूज़ चैनल की बात करें तो अब लगता है कि वह सिर्फ वहां एक मुद्दे को लेकर ग्लोरिफाई करते है। यह सिर्फ एक एजेंडा बेस खबरें चलाई जाती है सीधे-सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वह खबरें बिकी हुई है।
स्नेहा रिछारिया :- हां, मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से समझाना चाहूंगी। जैसे न्यूज़ चैनल की हम बात करें तो पत्रकार होने के नाते महसूस करते हैं कि कैसे पत्रकारिता चल रही है। टीवी में किस तरह से न्यूज़ कवरेज हो रहा है। तो निश्चित ही इसमें बदलाव तो आया है या ऐसा कहें कि उनकी भाषा अभद्र भी हो गई है। उसकी जो शैली है पहले के न्यूज़ चैनल हम देखते थे और यह अब देखते है। बहुत पुरानी बात भी नहीं है मुझे लगता है 2014 से पहले या उसके आसपास का देख लीजिए जब तक पूरा टेकओवर नहीं हुआ था उस समय तक भी थोड़ी भाषा थी , टी वी देखने लायक था कुछ-कुछ जब मैं ही बड़ी हो रही थी. लेकिन अब आज से हम तुलना करते हैं तो एक दम गाली गलौज पर आ गए हैं. अब उसमें देखने लायक सीखने लायक तो कुछ नहीं है. लेकिन आज भी आप देखेंगे तो हमसे पहले की जो जनरेशन है या गांव देख लीजिए छोटे शहरों में देख लीजिए तो। जैसे कि आप बीकानेर में रहते हैं आप शहर में जाएंगे बाजार से जब गाड़ी चलाते निकलेंगे तो कई बार आपको दुकानों में टीवी चलती हुई दिख जाएगी उसमें लोग अभी भी “आज तक” और यह “ज़ी न्यूज़” चैनल देखते हैं। तो उनको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी तक के यह न्यूज़ बिकी हुई कैसे होती है पेड न्यूज़ कैसी होती है। उनको यह सब इतने अच्छे से नहीं मालूम वह आज भी उसी वैल्यू से ही लेते हैं और वो उसे ऐसे देखते हैं कि अरे फलां न्यूज़ वाले तो यही दिखा रहे थे। आप अगर उनसे बात भी करेंगे ना या आर्गुमेंट करेंगे तो उनके आर्गुमेंट में भी उसी की रेफरेंस होती है। तो उनका अभी तक वही सोर्स है न्यूज़ का लेकिन मुझे लगता है हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते उनकी जितनी समझ है वह उसी हिसाब से देखते हैं । लेकिन अगर आपके सवाल का जवाब दूं तो काफी कुछ बदल गया है। मेरे हिसाब से अभी हालात खराब हैं। जो मैं जर्नलिज्म कर रही हूं देख रही हूं काफी खराब हो चुका है और काम करने लायक नहीं रहा है नई जनरेशन के लिए।
अरमान नदीम :- पहले के मुकाबले दर्शकों में गिरावट तो आई है?
स्नेहा रिछारिया :- हां, बिल्कुल आई है बहुत से लोग शिफ्ट कर चुके हैं। मैं खुद ही जानती हूं मैंने खुद ही कितने सालों से टीवी नहीं देखा है क्योंकि एक यह भी है कि फोंस आ गए हैं। और मान के चलिए कोई नये घर में शिफ्ट होता है तो उसे अब टीवी की जरूरत ही नहीं लगती के देखेंगे भी तो क्या? तो अब फोन से ही चल रहा है सब कुछ।
अरमान नदीम :- आपकी नजर में एक पत्रकार की क्या परिभाषा है ।
स्नेहा रिछारिया :- मुझे लगता है अब पत्रकारिता बहुत बदल गई है। डेफिनेशन लोगों के हिसाब से भी चेंज हो गई है पहले लोग न्यूज़ गैदरिंग को ही पत्रकारिता समझते थे। आप न्यूज़ इकट्ठा कर रहे हैं समझिए एक्सीडेंट हो गया कहीं कुछ हो गया तो आप इसे अपने संपादक को दे रहे हैं डेस्क वाले लिख रहे हैं तो उस तरीके से देखते थे। लेकिन आज देखें तो मुझे लगता है वह डेफिनेशन बहुत हद तक बदल सी गई है खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद क्योंकि अब कोई फिक्स नहीं है कि जिसने पत्रिका की डिग्री ली है वही पत्रकार है। पत्रकार बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे फॉर्मल तरीके से पढ़ा नहीं है लेकिन वह उनसे बेहतर कर रहे हैं जो डिग्री होल्डर हैं। तो सोशल मीडिया ने यह भी दिया है लोगों को। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की पत्रकारिता में करती हूं या जिसमें विश्वास रखती हूं वह पढ़ने लिखने वालों के लिए होती है अगर आपके सवाल का जवाब दूं तो ऐसा लगता है कि जब भी किसी इशू के बारे में बात करते हैं लिखते हैं या उसकी कवरेज करते हैं उसका वहीं ढंग सही होता है। आप सबसे बात करें सभी को स्पेस दीजिए आईडेंटिफाई करें इस स्टोरी में कौन-कौन स्टेज होल्डर हैं। तो उसमें यह भी है आपको काटना छांटना नहीं है। सबसे बात करके इसके बाद आपको अपना एक वर्जन देकर फिर उसे सभी के पर्सपेक्टिव पर छोड़ दीजिए। कौन इसे कैसे देखता है । तो यह तरीका है हालांकि यह मैं अपनी कार्यशैली के हिसाब से बता रही हूं लेकिन जर्नलिज्म सोशल मीडिया पर भी हो रही है ।जैसे मैं बता रही थी वीडियो के जरिए, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कंटेंट क्रिएटर तो कंटेंट बनाते हैं वह भी अपने आप को जर्नलिस्ट बोल रहे हैं उनको लगता है कि यही पत्रकारिता है तो वह भी बहुत चेंज हो रहा है I लेकिन जो लोग इसमें एडजस्ट नहीं कर रहे हैं वह खत्म भी हो जाएंगे ।कुछ टाइम में मुझे ऐसा लगता है। सभी को सीखना भी होगा कि कैसे बदलना है। अपने कम्युनिकेशन के, मीडियम को, अपने कहानी बताने के अंदाज को।
अरमान नदीम :- आपने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है और जो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वह खत्म भी हो जाएंगे लेकिन फिर भी असर रहेगा।
स्नेहा रिछारिया :- बिल्कुल रहेगा क्योंकि उनका भी कंजप्शन हुआ है जैसे कि मैं बता रही हूं मैं जर्नलिज्म करती हूं उनकी एक निश ऑडियंस है उनको बहुत कम लोग पढ़ते हैं उनके कोई मिलियन व्यूज नहीं आते हैं लेकिन वह सरवाइव करेगा ऐसा नहीं है कि वह खत्म हो जाएगा लेकिन उसे स्पेस में काम करने वाले लोग स्ट्रगल करते हैं जैसे मैं भी कई बार सोचती हूं की जो मैंने इतना पढ़ लिखकर, इतना मुश्किल से ट्रैवल करने के बाद जो लिखा है तीन हज़ार शब्दों का ,उसको कितने लोग पढ़ेंगे उसको कितने लोग समझेंगे तो मैं भी सोचती हूं यार एक्चुअली शोल्ड ई दो थिस या मैं एक कमरे में बैठकर एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख एक अच्छा सा कैमरा के साथ और अच्छे से तैयार होकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ दूं और उसे वीडियो को अच्छे से एडिट कर कर सोशल मीडिया पर डाल दूं या ट्रेडीशनअल ट्रांजैक्शन पर लगा दूं तो रेल तो उसमें ज्यादा व्यूज आएंगे क्योंकि कंजप्शन ऐसा हो रहा है ,हो गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो मैंने तीन हज़ार शब्द लिखे हैं उनका कोई मायने नहीं है या उसका कोई उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है ।
अरमान नदीम :- अच्छा ऐसा कभी किसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लिया बाद में उनकी कथनी और करनी में फर्क नजर आया ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस?
स्नेहा रिछारिया :- ऐसा हुआ है मेरे साथ एक्चुअली में एक बार इसमें पहले में एक पॉडकास्ट प्लेटफार्म के लिए काम करती थी। तो उसमें पॉडकास्टिंग में बहुत होता है। उनको ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट ऐसा प्लेट फार्म है जहां आप अपनी बात कह सकते हैं आप अपने काम के बारे में बताइए और लोग इसे एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं लेंगे लोग समझते हैं कि यह 30 मिनट का एपिसोड है जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा तो उसी के चलते हुआ बेंगलुरु में एक इनीशिएटिव है उन्होंने अप्रोच किया हमें एडिटर थ्रू बेंगलुरु में जो वॉटर क्राइसिस है इसके बारे में आप इससे इससे बात करिए तो मैंने किया इंटरव्यू रिलीज भी हो गया उसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात है जब बेंगलुरु में वॉटर क्राइसिस आया बहुत भयानक पानी की कमी हो गई थी तो उसे वक्त लगा कि यहां से एक स्टोरी करती हूं तो सोचा कि उन्हें से बात करते हैं जिन्होंने जिसे लास्ट ईयर इंटरव्यू किया था तो मैंने उन्हें लिखा कि बताइए कभी अब बताइए अभी जो क्राइसिस चल रहा है वह उसे वक्त उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें करी थी तो अब उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ग्राउंड पर जंग जो लोग काम कर रहे हैं उसे मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है इस हालत में तो उसे वक्त उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो इस तरह की चीज होती है फिर पता चला कि वह कुछ खास करते भी नहीं थे काम उनके इस रवैया के बाद हमने उनका वह इंटरव्यू भी हटा दिया था और एक मैसेज थ्रू भी दिया था कि यह बिल्कुल अनप्रोफेशनल बिहेवियर है
अरमान नदीम:- संस्था के साथ ऐसा कभी अनुभव रहा कि उनकी वजह से अपनी आईडियोलॉजी से समझौता करना पड़े या ऐसा दबाव डाला हो कि नहीं इसी तरह से काम करना है?
स्नेहा रिछारिया :- मैंने जहां काम किया वहां ऐसा नहीं हुआ, काफी ठीक था. उन्होंने मुझे काफी स्पेस दिया था। डेफिनेटली होता है और मैं बिना नाम लिए ही आपको बता सकती हूं मैंने जितना देखा है जितना भी मैं मीडिया स्पेस को समझती हूँ बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया में लोग हैं नए प्लेटफार्म है जो बहुत ही खुद को रिवॉल्यूशनरी दिखाने की कोशिश करते हैं। कि हम तो लेबर राइट्स पर काम करते हैं हम लोग बंधुआ मजदूरी के ऊपर स्टोरी करते हैं। लेकिन जब आप उनके लिए स्टोरी करने वाले पत्रकारों को देखेंगे बात करेंगे तो पता चलेगा कि उन्हें 25-30 हज़ार में लगा रखा है दिन भर काम कर रहे हैं वीकेंड्स पर बुला रहे हैं एकदम एक्सप्लोइट कर रखा है। मतलब उन्होंने मास्टर्स किया है उन्हें आप 20-25 हज़ार में रखना चाहते हैं तो उनको बाहर दुनिया को सरकार को क्रिटिसाइज करने का जो जोश है जब बात अपने पर आता है तो खत्म हो जाता है। लेकिन बाहर वो दिखाने की कोशिश में रहेंगे की कुछ भी इंजस्टिस हो रहा है तो उस पर लिखते हैं और हम ही पत्रकारिता के कर्ताधर्ता है लेकिन जो उनके अंदर का सिस्टम होता है वहीं उन्हें सबसे ज्यादा एक्सप्लोइट करता है।
Dr. Gaurav Bissa
डॉक्टर गौरव बिस्सा
दुनिया में कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, सारी प्रेरणा आंतरिक है। - डॉक्टर गौरव बिस्सा
पाँच सौ से ज्यादा मैनेजमेंट कार्यशालाओं का आयोजन कर लगभग दो लाख से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, बैंक कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों, वैज्ञानिकों, कॉर्पोरेट कार्मिकों को प्रत्यक्ष मैनेजमेंट प्रशिक्षण देने का राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करने वाले मैनेजमेंट ट्रेनर डॉक्टर गौरव बिस्सा से शब्द संवाद के लिए अरमान नदीम की खास बातचीत ।
परिचय डॉक्टर गौरव बिस्सा
• विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) प्रोजेक्ट हेतु दूरदर्शन के ज्ञान दर्शन, व्यास चैनल के लिए अब तक 90 (नब्बे) से ज्यादा मैनेजमेंट फिल्मों का निर्माण और विषय विशेषज्ञ की भूमिका का निर्वहन किया। ये फि़ल्में मार्केटिंग मैनेजमेंट, संगठनात्मक व्यवहार और सामान्य प्रबन्ध अध्ययन के विषयों पर आधारित हैं।
• मानव संसाधन प्रबंध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट(ISTD) द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट ट्रेनर का आई एस टी डी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुरस्कार, पच्चीस हज़ार रूपए नकद और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित, पूरे भारत में प्रथम स्थान।
• मैनेजमेंट शिक्षा की सर्वोच्च संस्था ऑल इण्डियन मैनेजमेंट एसोसिअशन (AIMA) नई दिल्ली द्वारा जुलाई 2015 में एक वर्ष की चयन प्रक्रिया के उपरान्त भारत के “सर्वश्रेष्ठ सर्टिफाइड मैनेजमेंट ट्रेनर” का प्रमाण पत्र।
• नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क, यूनाइटेड किंगडम और ऑलइण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा “सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट ट्रेनर” का प्रमाण पत्र प्राप्त।
• मानव व्यवहार और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में नेशनल एक्रेडिटेड मैनेजमेंट टीचर अवार्ड से सम्मानित, राजस्थान में एकमात्र।
• जैसलमेर स्थापना दिवस पर जैसलमेर फोर्ट म्यूजियम ट्रस्ट(जैसलमेर महारावल) द्वारा सर्वोच्च महारावल जैसल सम्मान से सम्मानित।
• बीकानेर स्थापना दिवस पर राव बीकाजी संस्थान, जिला प्रशासन और नगर विकास न्यास द्वारा आयोजित समारोह में मैनेजमेंट शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर प्रतिष्ठित “अमर कीर्ति पुरस्कार” से सम्मानित।
• गणतंत्र दिवस 2012 में जिला प्रशासन बीकानेर, गणतंत्र दिवस 2005 में जिला प्रशासन जोधपुर तथा स्वतंत्रता दिवस 2014 को नगर निगम बीकानेर द्वारा पर सम्मानित।
• आईआईएम राजस्थान उदयपुर के संस्थापक विशेषाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी।
• मैनेजमेंट की 15 (पन्द्रह) पुस्तकों का लेखन।
• 70 (सत्तर) से ज्यादा शोध पत्र रेफ्रीेड जर्नल्स में प्रकाशित।
• 200 से अधिक शोध पत्र अनेकानेक कॉनफ्रेंसेज़, सेमीनार में प्रस्तुत और प्रकाशित।
• रोजगारपरक शिक्षा के क्षेत्र में 11 (ग्यारह) विशेष कोर्सेज़ का लेखन और सम्पादन।
• अखबारों में नियमित कॉलम लेखन, नेशनल राजस्थान में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट पर आधारित “गुरुमंत्र” स्तम्भ में 1200 (बारह सौ) से ज्यादा लेख प्रकाशित।
• मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में 10 (दस) मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स का सफल क्रियान्वयन।
• तीन सौ से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में केरियर गाइडेंस, प्रबन्ध प्रशिक्षण, रोजगारपरक प्रशिक्षण देने का कीर्तिमान।
• दस विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ़ स्टडीज़ सदस्य, कन्वीनर या चेयरपर्सन के रूप में कार्यानुभव।
• रामायण, महाभारत, भगवद गीता पर विशेष शोध करने पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित।
• चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट प्रोफ़ेसर अवार्ड, पांच अन्तरराष्ट्रीय और बीस राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। नगर निगम, चुरू जिला प्रशासन, अस्थमा केयर सोसाइटी, ब्राह्मण महासभा, जोधपुर कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट, लायंस क्लब, सीमा सुरक्षा बल, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस बल इत्यादि सहित अब तक सत्तर से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा सम्मानित।
• सात विद्यार्थियों को पी एच डी और 150 विद्यार्थियों को डेज़रटेशन हेतु गाइडेंस।
• रेडियों में नियमित रूप से वार्ताओं का प्रसारण, रेडियों पर सुभाष चन्द्र बोस के जीवन पर आधारित तेरह खंडीय नाट्य“कदमों के निशां” का लेखन और निर्देशन। अब तक पचास से ज्यादा रेडियो कार्यक्रमों में भूमिका।
• जयपुर दूरदर्शन पर “देखो-देखो”, “सोने की चिडकली” और“लल्ला को ब्याह” में अभिनय। विद्यार्थियों हेतु पर्सनैलिटी डेवेलपमेंट शो “आओ हम बदलें वर्तमान” कार्यक्रम में बीस वार्ताएं प्रसारित। विद्यार्थियों में बढते तनाव को दूर करने हेतु टीवी शो “एक्ज़ाम्स - टेक इट ईज़ी” में बतौर मुख्य वक्ता और निर्देशक के रूप में कार्य।
• विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर विद्यार्थी के रूप में वाद विवाद और आशु भाषण में कॉलेज हेतु अस्सी से ज्यादा पुरस्कार जीतने का विशेष कीर्तिमान।
दैनिक युगपक्ष में नियमित कॉलम ।
अरमान नदीम :- आप साइंस से ग्रेजुएट हैं और उसके बाद एमबीए किया है और आज की तारीख में लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, साहित्य की तरफ रुझान कैसे हुआ?
डॉ. गौरव बिस्सा :-बिल्कुल आपने सही कहा की मैं साइंस ग्रेजुएट हूं और उसके बाद मैंने एमबीए किया । एम ए हिस्ट्री। पत्रकारिता में मास्टर्स , इन सब के बाद तकरीबन एक साल कॉरपोरेट सेक्टर में रहने के बाद मैंने शिक्षा को चुना बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तभी से मैं यही काम कर रहा हूं । साहित्य लेखन की जहां तक बात है कि कैसे जुड़ना हुआ तो घर में शुरू से ही पढ़ाई का एनवायरमेंट आभामंडल बना रहा । मेरे पिताजी एक अच्छी लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं । प्रेस कटिंग मेंटेन करते हैं। शुरुआत से ही क्योंकि घर में लाइब्रेरी थी तो पिताजी मुझसे कहा करते थे कि यह मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फाइल है इसकी तुम मुझे इंडेक्सिंग करके बताओ लेख नंबर एक जुपिटर पर क्या दिक्कत आ रही है या फिर मार्स पर क्या चल रहा है एक लाइन में लिखकर बताओ तो पढ़ना ही पड़ता था।यहां से मेरी धीरे-धीरे पढ़ने की रूचि विकसित हो गई। और मेरे लेखन की अगर आप स्थिति देखेंगे तो वह सरलतम भाषा में है। अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे समझ सकता है। मेरा तो उद्देश्य यही रहता है। यहीं से मेरी साहित्य के प्रति दिलचस्पी और अधिक जागी।
अरमान नदीम :- मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं इससे जुड़े हुए, इसे हम कह सकते हैं आसान होता है उपदेश देना। सवाल है कि व्यक्ति उसे अपने जीवन में कैसे उतारते है ?
डॉ. गौरव बिस्सा - अरमान जी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आज तक दो लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दे चुका हूं। मैं प्रेरणा की बात कहता हूं और मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कम से कम हजार जगह कहां होगा कि टाइम लॉक बनाओ 9:00 क्या करते हो 8:00 क्या करते हो 10:00 क्या करते हो तीन दिन बनाओ आपको आपकी प्रोडक्टिविटी समझ में आ जाएगी कितने उत्पादक हैं । बार-बार कहने से मुझे खुद में एक बदलाव यह महसूस हुआ कि आप जब भी मेरे पास में आएंगे तो आपको मेरे पास एक प्लान मिलेगा । किस वक्त और किस दिन मुझे क्या-क्या काम करने हैं यह पहले से मेरे फिक्स्ड रहते हैं । आपको कहा कि कोई भी चीज असंभव नहीं है और मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता जब मैं यह बात सौ बार कहूंगा या बार-बार लोगों को खुद की तरफ से समझाऊंगा और जब मेरे पास में ऐसा कोई कार्य आएगा जो मुझे कठिन लगे तब यह चीज मेरे दिमाग में भी आएगी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता । और मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है । उदाहरण जिसे मैं अपने शिष्यों को समझता हूं तो वह उदाहरण कहीं ना कहीं मेरे सामने या तो पहले घटित हो चुके होते हैं और आगे भी होते रहेंगे । दिमाग में कहीं ना कहीं यही चीज घूमती है कि अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। एक चीज में जोड़ना चाहूंगा इसमें कि दुनिया के अंदर कोई भी किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकता , सारी प्रेरणा आंतरिक है । मैं सिर्फ आपको ऊपरी तौर पर समझा सकता हूं कि आपको किस तरीके से क्या चीज करनी चाहिए। आप तो साहित्य जगत से जुड़े हैं और अपने मारवाड़ी में कहते हैं "अक्ल सरीरा उपजे दिया लागे डाम "यानी की अक्ल की प्रेरणा होती है वह अंदर से आती है। आप हजार बार कह दीजिए कि यह आपको पढ़ना है इस वक्त आपको करना है अगर वह नहीं करना चाहता उसके अंदर से वह ऊर्जा नहीं मिल पा रही है उसे तो वह नहीं करेगा।
अरमान नदीम :- ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति अपने सामाजिक मूल्यों से भटकता जा रहा है, और अगर हम इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें फिर चाहे वह हिंदू धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो या इस्लाम धर्म को मानने वाला नौजवान, कहीं ना कहीं वह अपने सामाजिक और धार्मिक दोनों ही मूल्यों से दूर होता जा रहा है।
डॉ. गौरव बिस्सा :-मैं इस सवाल का जवाब आपको रिसर्च बेस मामले को देखते हुए दूंगा क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर हूं तो मैं आपको इस तरीके से इस चीज का जवाब देना चाहूंगा । बहुत ही साफ-साफ दो कारण है इस चीज के पहले होता है भ्रष्टाचार की औकात बहुत खरी बात कहना चाह रहा हूं पहले भ्रष्टाचार की औकात पति अपने भ्रष्टाचार की औकात के अनुसार आनंद ले रहा है स्टूडेंट एक शिष्य की भ्रष्टाचार की औकात है कि वह अपनी क्लास को छोड़ दे और बाहर जाकर मौज मस्ती करें। थोड़ा अगर आगे बढ़े और एक सरकारी कर्मचारी की औकात है कि वह देर से जाए और जल्दी घर वापस आ जाइए उसकी औकात है। व्यापारी है तो वह कुछ मिलावट करके अपना काम निकल रहा है। आप अगर एक बच्चे से पूछेंगे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे चलिए हम इसे थोड़ा और आसान करते हैं अगर आप एक अच्छे खासे स्कूल अध्यापक से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं आगे और क्या करना चाहते हैं और क्या सोचते हो तो वह यह रहेगा कि मैं शिक्षक तो हूं लेकिन मेरा पटवारी में सलेक्शन हो गया , देश की सेवा करूंगा । मैंने उसे कहा कि तुम उससे अधिक वेतन श्रृंखला पर इस वक्त मौजूद हो जवाब आता है कि देश की सेवा करूंगा। देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार करने की जो हैसियत होती है वह पटवारी में ज्यादा है शिक्षक में इतनी नहीं होती।और कितनी बार उसे दोहराया जाता है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है यह सब होने की साल में एक बार 3 महीने में एक बार दिन में एक बार। एक बार एक व्यक्ति को नींद नहीं आई कहता है कि आज रिश्वत ली है ,दूसरे व्यक्ति को नींद नहीं आती कहता है क्यों क्योंकि आज मैंने रिश्वत नहीं ली है। और इन सब गतिविधियों को व्यक्तियों ने व्यक्ति ने सामान्य मूल्य मान लिया है कोई उसकी बांह पकड़कर यह नहीं पूछता अरमान जी की तुम्हारा वेतन तो पचास हज़ार है और तुमने घर पांच करोड़ का कैसे बना लिया। उल्टा उस व्यक्ति की प्रशंसा होती है। तो यही एकमात्र मूल्य बन चुका है कि किसी भी माध्यम से मुझे धन कमाना है फिर उसकी कोई भी वजह कारण और मध्यम क्यों ना हो। और जब पैसा कमाना पहली प्राथमिकता हो जाए और घर परिवार की मर्यादा दूसरे दर्जे पर आ जाए। तब यह सब होता है।
अरमान नदीम :- जैसा कि आपने कहा लोगों ने इन्हें अपना लिया है ,बड़े लोगों को या फिर नेताओं को भ्रष्टाचार करते हुए कि यह बड़ा है तो यह बड़ा भ्रष्टाचार करेगा तो यह इसमें सफल कैसे हुए लोगों की मानसिकता को इस तरीके से बनाने में ?
डॉ. गौरव बिस्सा :- नहीं यह सफल नहीं हुए हैं इसके अंदर अब जैसे कि युवा है या हम लोग हैं तो हम आसान मार्ग को चुनना पसंद करते हैं जो मेहनतकश जो चीज हैं उसमें हम अपने आपको देखना ही नहीं चाहते ,लोग चुनाव में वोटिंग तक करने नहीं जाते हैं । अगर आपको किसी राजनेता से परेशानी है तो आप उसके खिलाफ वोट डालिए आप अगर वह इलेक्ट भी हो चुका है तो आप उसके सामने जाकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए लेकिन यह लोग नहीं करते हैं इस तरीके की चीजों को और अगर जाते भी हैं समस्याएं लेकर तो वह अपनी निजी कामों के लिए राजनेताओं के पास हो जाते हैं सामाजिक कार्यों के लिए आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे जो नेताओं के पास जाते हैं । यह उन्हें कहते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए नेताओं से बात क्यों नहीं करते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि राजनेताओं ने काम नहीं किया होगा आज हमें आजाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं नेताओं ने काम किया है लेकिन जिस तरीके से उन्हें ट्वीट करना चाहिए उसे तरीके से ना तो जनता उनके साथ व्यवहार करती है ना वह जनता के साथ। और यह गलती उनसे ज्यादा मैं समाज की मानता हूं।
अरमान नदीम :- आगे अगर हम बात करें तो वह भी एक सामाजिक समस्या ही है, अकेलापन मैं इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था जिसका शीर्षक मैंने रखा था तन्हाई और अकेलापन। और यही समस्या मुझे लगता है समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है और इसी पर मैं आपके विचार लेना चाहता हूं।
डॉ. गौरव बिस्सा :- तन्हाई और अकेलापन क्या बात है बहुत ही बढ़िया विषय आपने छेड़ा है। आपने जो बात कही है काबिले तारीफ है और मैं इसलिए ऐसा कहूंगा क्योंकि मौजूदा वक्त की जो स्थिति है वह बहुत ही पीड़ादायक है । मैं सबसे पहले आपको अगर बात कहूं तो शोध के विषय में ही आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक शोध में बताया गया है कि 2026 जो हमारा आने वाला साल है उसमें 17 करोड़ आदमी और 2036 तक। और महिलाओं की स्थिति और भी खराब है जिसमें 50 फ़ीसदी तक महिलाएं अकेलेपन से परेशान हैं। और क्योंकि लोग एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं इस वजह से जो दिल में और अंदर ही अंदर जो कुंठा पनपती है उसे जिस तरीके से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सदियों तक नहीं की जा पाएगी। और जिस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है लोगों का यह हैरान करने वाली चीज है। अब इसका यही है समाधान के आपको लोगों से मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। ह्यूमन लाइब्रेरी जैसी चीजों की जरूरत पड़ी है हमें यानी कि सामान्य पुस्तकालय में आप क्या करते हैं आप जाते हैं अपनी पसंद की या अपनी रुचि अनुसार पुस्तक लेते हैं उसे पढ़ते हैं और वापस दे देते हैं और उसी तरीके से डेनमार्क में ह्यूमन लाइब्रेरी का चलन हुआ जिसके अंदर आप जाएंगे और आधे घंटा एक घंटा के लिए वहां व्यक्ति को हायर करेंगे अपनी बात करने के लिए तो आज हम इस मुकाम तक आ चुके हैं। तो अकेलेपन से दूर होने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता उसके लिए जुड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है बात करनी पड़ती है और मनोविज्ञान तो बहुत ही एक शानदार बात कहता है कि जितना नुकसान आपको नशे से होता है उससे कहीं गुना अधिक अकेलेपन से होता है। अकेलापन तो बहुत घातक है।
अरमान नदीम :- बिल्कुल आपने बहुत गहरी और शानदार बात कही है अकेलेपन को लेकर के और जिस तरीके से मैंने आपको अपने आर्टिकल के बारे में बताया तन्हाई और अकेलेपन जिसका शीर्षक था उसमें मैं भी यह साफ-साफ लिखा कि अकेला और अकेलापन दोनों में फर्क है अब मैं अकेला अगर बैठा हूं तो अपनी लाइब्रेरी में मैं कुछ काम कर सकता हूं मैं उसे अकेलापन नहीं मानूंगा लेकिन अकेलेपन का जो व्यक्ति शिकार है वह दस लोगों के बीच बैठा भी खुद को अकेला महसूस करेगा तो इन चीजों को समझने की समझने की और जो इसके शिकार हो चुके हैं उनके मां को बाप की आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरत महसूस है। एक और चीज पर मैं कहना चाहूंगा मेरी बातें से लोगों को लग सकता है कि मैं ज्यादातर आलोचना करता हूं लेकिन मैं इसे आलोचनात्मक नहीं विचारात्मक समझता हूं और कुछ चीज हैं जो समाज को लेकर चिंतित करती है क्योंकि मैं जिस उम्र में हूं और मैं जब अपने साथ के लोगों को देखता हूं तो मेरी चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि आज के युवा के आदर्श वह हैं जो कानून की नजर में गुनहगार हैं।
डॉ. गौरव बिस्सा :- समाज जिनका सम्मान करता है समूचा समाज वैसा ही बांटा जाता है आपने गलत लोगों को हीरो के रूप में अगर प्रेजेंट किया तो निश्चित ही आपकी आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी। फिर चाहे वह फिल्मी जगत से जुड़े ही लोग क्यों ना हो वह कहीं केसों में सामने आते हैं लेकिन उसके बाद में भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट या मैं कहूं भीड़ है जो उन्हें मानती है तो जब इस तरीके की चीज होती है तो हम देखते हैं कि उन्हें प्रेजेंट किस तरीके से किया गया है समाज के सामने बात तो यही है कि सवाल समाज को खुद से पूछना चाहिए कि हमने यह किस तरीके से अपने आने वाले लोगों को तैयार किया है। बच्चों में युवाओं में संदेश ऐसा जाता है कि अच्छा बदमाशी करने पर अखबार में फोटो आती है यही करेंगे। तो बात यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है अगर मीडिया को ऐसा लग रहा है कि एक गलत दिशा में समाज के युवा जा रहे हैं तो उनके पैरेलल ही उन लोगों को आप आगे बढ़ाओ जो अच्छे काम कर रहे हैं । फिल्मी जगत में भी अच्छा काम करने अपने सामाजिक जीवन में भी अच्छा काम कर रहे हैं वह राजनेता के रूप में एक अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं तो इन लोगों को आगे लाना चाहिए ना कि ऐसे लोगों को जिनके बारे में केसेज हैं ,जो हत्यारे हैं। आप यह देखिए की सेना में नहीं जुड़ना चाहते बच्चे। जानकारी नहीं है राष्ट्रभक्तों के बारे में तात्या टोपे के बारे में विदेशियों ने यह कहा था के वह इतना खतरनाक शत्रु है कि मैं उसे दो बार मारना चाहता हूं। टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेजो से लोहा लिया जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया उनके बारे में आज का युवा जानता कितना है। म्यूजियम के अंदर टीपू सुल्तान की तलवार देख रहा था तो मुझे पीछे से बुलाने के लिए कहा गया कि तलवार साथ में लेकर चलनी है क्या। मतलब यह है कि हम लोगों ने हमारी मीडिया ने हमारे समाज ने गड़बड़ लोगों को आगे रखा और आगे इन लोगों की प्रेजेंटेशन। ।
अरमान नदीम :- आपने सही कहा कि लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे सलाह भी असल में इसी तरह की दी जाती है कि तुम पैसा कमाओ अब मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण अपना ही देना चाहूंगा इस बीच में शब्द संवाद लगातार जारी है और इसके माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि मैं अलग-अलग लोगों से अलग-अलग शख्सियत से बातचीत करूं और जब मेरे आस-पास के लोग इसे पढ़ते हैं तो वह सवाल यही करते हैं कि तुम्हें अखबार कितना पैसा देता है इसका इससे बढ़िया इसे लिखकर ब्लॉग में डाल दो और इतना लंबा पढ़ेगा कौन यह इस तरह की चीज आती है तो जब लोगों को समझ नहीं होती तो वह इस तरीके की बात करते हैं अब उन्हें कौन बताएं कि जिससे बातचीत हो रही है वह अगर सेमिनार हॉल में यह बात कहें तो तुम हजारों रुपए देकर उनकी बात सुनोगे लेकिन वह जो तुम्हारे घर आ रहा है पांच रुपए का अखबार उसमें लाखों की बात है ,करोड़ों की बात है जो लोग लाइनर लगाकर समझते हैं वह चीज तुम्हारे घर में आ रही है।
डॉ. गौरव बिस्सा :- इस चीज का हम किसे दोष दें क्योंकि यह मानसिकता ही है कि अगर व्यक्ति संपूर्ण निशुल्क हो जाए तो लोग उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। और लोगों को यह लगने लगता है कि इसके पास कंटेंट डिलीवर करने को नहीं है। आपने यह कहिएगा कि आज मैं जो आपके आगे पचास लाइन बोल रहा हूं मक्खन की भांति है जो मैंने पचास हजार लाइन जो शब्द मैंने पढ़ें उनके सार है यह समय की कीमत कौन देगा। एक कटोरी बनाने की भांति है । आदमी 8 घंटे में 400 कटोरी बनाता है बेचने में उसे 2 घंटे लगे ,आप कहेंगे कि दो घंटे के तो दो रुपए ही होंगे अब वह आठ घंटे कौन चुकाएगा। शिक्षक के पेशे की सबसे बड़ी त्रासदी यही है उसकी मेहनत को देखने के लिए तैयार ही नहीं । यही तो सबसे बड़ी दुखद बात है कि जो चीज फ्री में मिल जाती है उसे लोग बेकार समझने लगते हैं । और उसका मूल्य जानते ही नहीं और उसे कहते हैं इसका कोई मोल ही नहीं। फिल्में बनती है अभिनय होता है और उसमें कलाकार तीन-तीन सो चार-चार सौ करोड रुपए लिया करते हैं ।अब जो उस कलाकार को पैसा मिला है वह उसकी ब्रांड वैल्यू है। यही बात है कि अगर आप हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे तो आपको लोग इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। आप मान कर चलिए आपने गाना सुना और आपको वह बहुत पसंद आया और आप उसे मन ही मन हजार बार गुनगुनाएंगे लोगों के सामने । अगर बैठे हैं तब भी आप गुनगुना रहे हैं लेकिन अगर मैंने कहीं पर कोई चीज बोली है ,अपनी स्पीच के अंदर कोई चीज सुना दी, कथा सुना दी और उसे मैं कहीं और रिपीट कर दिया वहां वो पांच फ़ीसदी जो कॉमन ऑडियंस होगी। बड़ी शातिर मुस्कान के साथ दिखेंगे और कहेंगे वहां पर भी इसने वही बोला था मैं तो कोई बात दोहरा नहीं सकता। हर बार के लिए कुछ नया तैयार करना होगा। यह कोई आसान चीज थोड़ी है। आज आपने कुछ लिखा है तो इसकी रायल्टी आपको क्यों नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए। चार लाइन की लघु कथा लिखने के अंदर चार घंटे लग जाएंगे। सिर्फ चार लाइन नहीं है वह चार घंटे की मेहनत है । वह चार घंटे का श्रम है। आपने कहा कि कई लोग कह देते हैं कि इतना बड़ा जो आप लिख रहे हैं इसे पढ़ेगा pकौन तो आप यह कहिए कि शब्द संवाद को अगर कोई एक व्यक्ति भी पढ़ रहा है तो शब्द संवाद मेरा सार्थक है। शब्द संवाद की एक लाइन पढ़कर भी अपने जीवन में कुछ बदलाव ले आए तो वह सार्थक है।
अरमान नदीम :- कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचने की क्षमता को खो देते हैं । ऐसा महसूस होता है कहूं कि कुएं के मेंढक यह जो एक शख्सियत होती है यह क्या है यह उसके आभामंडल का कारण है या यह उसी के मूल का हिस्सा है?
डॉ. गौरव बिस्सा :- यह उनके मूल का हिस्सा नहीं है। हर मनुष्य के मन में एक अनिश्चित आचरण होता है वह किसी भी व्यक्ति की प्रगति को देख को पचा नहीं पाता । बहुत ही अच्छा शोध कार्य हुआ था जिसमें पूछा गया की तनख्वाह हम डबल कर देते हैं आपके साथ वाले हैं उनकी भी डबल कर देते हैं यह तो रही पहली घटना और दूसरे के अंदर कहा गया कि आपकी तनख्वाह आधी कर देते हैं और उनकी भी तनख्वाह आधी कर देते हैं उत्तर लोगों में कहा जो दूसरा ऑप्शन है वह कि मेरी आधी कर दो भले से लेकिन सामने वाले की डबल मत करना । जैसा कि आपने कहा कि जो नेगेटिव सोच होती है एक एकदम संकुचित सोच है यही होता है और मुझे तो लगता है कि व्यक्ति को कई बार खुद से सवाल करने चाहिए कि मैं आखिर चाहता क्या हूं जीवन के लक्ष्य क्या है। हमें क्या करना है। मेरा मौलिक समर्थ क्या है। मैं दिशा में सर्वश्रेष्ठ हूं। उस दिशा में अगर हम काम करें तो हमारी शख्सियत में बेहतरीन तब्दीली आएगी ।
अरमान नदीम - शब्द संवाद के कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार।
डॉक्टर गौरव बिस्सा - आपका धन्यवाद ।
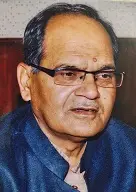 Chitranjan Mishra
Chitranjan Mishra
चित्तरंजन मिश्र
साहित्य में आलोचना की विश्वसनीयता ख़त्म हो रही है - चित्तरंजन मिश्र
साहित्य अकादेमी दिल्ली में हिन्दी परामर्शक मंडल के संयोजक और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे वरिष्ठ साहित्यकार चित्तरंजन मिश्र से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
परिचय
जन्म 29 दिसंबर 1956 उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भागलपुर कस्बे के एक सुशिक्षित ,कुलीन ,प्रतिष्ठित किसान परिवार में. प्रारंभिक शिक्षा गाँव और आसपास के विद्यालयों में । उच्च शिक्षा स्नातक स्नातकोत्तर एवं पीएचडी गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया है। शोध विषय निर्गुण भक्ति काव्य में रामकथा 1982 मे उपाधि प्राप्त की । जनवरी 1983 से इसी विश्वविद्यालय में प्रवक्ता, 1993 से उप आचार्य और 2001 से आचार्य पद पर दायित्व निर्वहन.2016 जनवरी से 2018 दिसंबर तक विभागाध्यक्ष. अगस्त 2014 से दिसम्बर 2015 तक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर एवं संयोजक हिंदी परामर्श मण्डल केंद्रीय साहित्य अकादेमी दिल्ली के पद पर दायित्वों का निर्वहन । गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री के रूप में 15 वर्षों तक शिक्षकों एवं विश्वविद्यालयों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष पूर्ण नेतृत्व. संपादित कृतियां... साहित्य के दृष्टिकोण, कथा भूमि, गद्य की रेखाएँ ,भारतीय साहित्य प्रतिनिधि रचना संचयन, भोजपुरी साहित्य संचयन अन्य प्रकाशन.... कबीर और तुलसी का आंतरिक साम्य ,निर्गुण भक्त कवियों का रामकाव्य, भाषा संस्कृति और समाज. महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में समकालीन साहित्य पर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित. सम्मान.... भगवत शरण उपाध्याय आलोचना सम्मान,. विशिष्ट हिंदी सेवी सम्मान ,प्रेस्टिज सारस्वत साहित्य सम्मान, श्रमवीर साहित्यकार सम्मान. आदि. विदेश यात्राएँ सन् 2012 मे नवें विश्व हिंदी सम्मेलन में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में व्याख्यान । 2014 में मारीशस के महात्मा गांधी संस्थान में व्याख्यान और सत्र की अध्यक्षता । 2015 में भारतीय लेखक प्रतिनिधि मंडल में चीन की यात्रा और चीनी लेखकों से विचार विमर्श, भारतीय दूतावास मे व्याख्यान और सम्मान.
अरमान :- आज की तारीख में आप साहित्य जगत में जाना माना नाम है लेकिन मैं यह सबसे पहले जानना चाहूंगा कि साहित्य में आपकी शुरुआत कैसे हुई?
चित्तरंजन मिश्र :- साहित्य में रुचि की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से ही रूचि रही । गांव के परिवेश में ही में पला , बड़ा हुआ और मेरे बड़े भाई साहब घनश्याम नंद मिश्रा जी ,उन्होंने हिंदी में बहुत काम किया था और उनकी किताबें जब मैं पढ़ता था तो मुझे काफी आनंद आता था । उन किताबों को पढ़कर मेरी दिलचस्पी साहित्य की तरफ बढ़ी। और जब मैंने स्नातक स्तर सब्जेक्ट चुने वे हिंदी, संस्कृत और साहित्य से जुड़े थे । क्योंकि शुरुआत से ही मुझे पढ़ने का जो शौक़ लगा था भाई साहब की किताबों से तो वह शुरुआत मेरी अब तक बनी हुई है। और घर में भी मैं अपने परिवार के लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाया करता था। और एक शौक यह भी रहा कि लगातार अपने वक्त के लेखकों को, विचारकों को पढ़ना उनको समझने की कोशिश करना। राजनीतिक दिलचस्पी भी बनी रही।
अरमान :- हमें देखने को मिल रहा है ना सिर्फ आज से एक लंबे वक्त से लेखक आलोचना से कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखते हैं असहज हो जाते हैं।
चित्तरंजन मिश्र :- आज के वक्त में साहित्य में आलोचना मुंह देखी हो गई है । एक बात आपने सही कही कि रचनाकारों ने आलोचना को स्वस्थ भाव से लेना कम कर दिया है। रचनाकार भी व्यक्तिगत खुन्नस रखने लगते हैं । अगर कोई आलोचना करे अगर उसके काम में कोई सुझाव दे दे तो लेखक नाराज हो जाते हैं कहा जा सकता है कि एक तरह की असहिष्णुता बढ़ी है। कह सकते हैं कि असहिष्णुता पूरे माहौल में बढ़ी है। इसका असर हमें लेखन पर देखने को मिल रहा है। और हमें यह चीज को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बात करें तो दोनों पक्षों को मध्य नजर रखते हुए न्याय संगत बात करें क्योंकि यह भी कह सकते हैं कि आलोचना ने भी अपनी विश्वसनीयता को खोया है। और जो विश्वसनीयता खत्म हो रही है उसमें हम देख सकते हैं कि गुटबाजी भी एक बड़ा कारण हमें नजर आता है। लेखक अपने संघ बना लेते हैं। कुछ-कुछ के अपने-अपने समूह हैं तो इस तरीके से तो न्याय संगत बात हो इसकी उम्मीद भी थोड़ी कम नजर आती है। इसमें यह भी हम देख रहे हैं कि एक समूह के लोग दूसरे समूह के लेखकों की चर्चा नहीं करते हैं दूरी बनाने की कोशिश रहती है। अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं तो वहां भी यही नजर आएगा कि दूसरे संगठन के लेखक के बारे में बात नहीं की जाती। इन्ही कारणों से आलोचना की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।
अरमान :- आपको लगता है आज की तारीख में चाहे वह युवा हो या साहित्यकार वह साहित्य के मूल से दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक आसान रास्ते की तलाश में रहते हैं।
मिश्र :- देखने को मिल रहा है और उनके बहुत गंभीर कारण है। जो सबसे शुरुआती कारण मुझे लगता है वह समाज का वातावरण है। पूरे समाज के वातावरण में एक हड़बड़ी सी फैली हुई महसूस होती है। साहित्य हड़बड़ी का काम नहीं है। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इसने भी लोगों के दिमाग पर खासा असर किया है। मान के चलिए आपका , मेरा फोन कुछ देर के लिए बंद हो गया तो हम परेशान हो जाएंगे। किन्ही कारण से अगर नेट बंद हो चुका है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह जो जल्दबाजी तुरंत रेडीमेड का जो यह कलर आया है इसने साहित्य के ऊपर समाज पर एक खराब असर किया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम जो विज्ञापन देखते हैं इनका भी एक बहुत भयंकर असर देखने को मिलता है कि जिस तरीके से वह आम जनता को समाज को यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि यह कर देने से यह काम हो जाएगा या फिर जो दुनिया को मुट्ठी में लेने की लालसा भी एक वजह बनती है। इन सब चीजों की जो कि असल हकीकत दूर होती है। और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश में वह खुद किसकी मुट्ठी में जा रहा है यह उसको एहसास तक नहीं है। मेरी नजर में पढ़ना चेतना के आंतरिक विकास का प्रकरण है। इन्हीं कारण से चेतना के आंतरिक विकास जो रुचि है वह लोगों में कम हुई है। तुरंत वह चीज चाहिए एक हड़बड़ी है जिसे हम कह सकते हैं कि पेशेंस लेवल लोगों में कम हुआ है। यह बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी है कि धीरे-धीरे विद्या अर्जित की जाती है। और एक दृश्य इसका यह भी है कि समाज कहीं ना कहीं लगातार पूंजीवादी होता जा रहा है। सामाजिक समस्याओं से ध्यान कम हों रहा है लोगों का। जो बाजार है उसमें किताबों की उपलब्धता में भी कमी आई है शहर गोरखपुर खाने को बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन उसमें बेहतर और अच्छी किताबों की कोई बड़ी दुकान देखने को नहीं मिलती। यह सब बातें मिलकर वातावरण का निर्माण करती है और देखने को मिल रहा है यही सब कहीं ना कहीं दूषित हो रही है। जिला पुस्तकालय गांव प्रधान पुस्तकालय इन सब में एक खासी गिरावट आई है और यह कहना बेहतर होगा कि वह खत्म हो चुके हैं। जो चीज नजर नहीं आएगी जिनकी उपलब्धता नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है उनमें दिलचस्पी भी लोगों की धीरे-धीरे कम होती जाएगी कि हम देख रहे हैं उसके आवाज में उसकी जगह पर बहुत सी चीज आ रही है और लोगों को जैसा मैंने आपको बताया जल्दबाजी है, एक हड़बड़ी है तो जल्दी-जल्दी जो चीज हो जाया करें उन्हें वह लोग अपना रहे हैं । जिससे साहित्य में भी लोग जल्दबाजी चाह रहे हैं । लगातार माहौल यह भी बनाया जाता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा या साहित्य जगत में रुचि रखने वालों में कुछ नहीं होगा बिजनेस कीजिए ,व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, तो कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह की चीजों से प्रभावित होते हैं तो वहां से भी एक दूरी बनती है क्योंकि जिस वक्त हम पढ़ रहे थे तो हमारे दिमाग में यह चीज नहीं हुआ करती थी कि इससे कुछ होगा हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा । हम सिर्फ उसे पढ़ रहे थे, हम सिर्फ ज्ञान ले रहे थे ,हमें सिर्फ एक विचार समझने की ललक थी लेकिन आज इस तरह की चीज देखने को नहीं मिलती है। उन्हें वह अगर कोई काम कर रहे हैं तो तत्काल कुछ चाहिए क्योंकि यहां जल्दी से कुछ नहीं मिलता है । तो बस वही बात है कि यह दूरी बन रही है। हमारे वक्त में जो हमारी पूरी पीढ़ी पढ़ने में लगी थी। तो जैसा कि मैंने कहा क्यों नहीं कोई लालच नहीं था कि कुछ मिलेगा लेकिन बात यह भी सत्य है कि जो पढ़ते थे अच्छा पढ़ाते थे उन्हें मिलता भी था। जब कुछ बनते थे और कुछ होते थे तो वह सिर्फ अपने-अपने आपके लिए नहीं हुआ करते थे वह पूरे समाज के लिए बनते थे। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि जो लोग चाहते हैं कुछ काम करना वह सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं उन्हें समाज से और सामाजिक समस्याओं से कुछ खासी दिलचस्पी नहीं है उन्हें समझाने की या उन्हें सुलझाने की। जैसा कि मैं आपको कहा यही लोगों को समझाया जा रहा है यही उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि पढ़ने से कुछ होगा नहीं और जो तुम्हारा एक तरह का जो सिलेबस है जिससे तुम एक नौकरी लग सको या फिर कोई बिजनेस कर सको उतना ही पर्याप्त है उससे आगे सामाजिक समस्याओं के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कह सकते हैं कि यह जो पूरा परिवेश का निर्माण हो रहा है यह पढ़ने के माहौल को खत्म करने का काम कर रहा है। आज की व्यवस्था चाहती ही नहीं है कोई सोच उन्हें विचारकों से एक तरह की समस्या है। तो आज का जो माहौल है वह सोने की फुरसत ही नहीं देना चाहता है कि तुम्हें सोचना नहीं है सिर्फ काम करना है एक तरीके से जो तुम्हें टारगेट दिया जाए उसे पूरा करो उसके आसपास क्या वातावरण है क्या घटित हो रहा है उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
अरमान :- बहुत गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखी और मैं जानना चाहूंगा यह जो समय जिसमें हम हैं इसकी शुरुआत इन समस्याओं की कहां से होती है क्या जब हमारा समाज मॉडर्न होने की राह पर चल रहा है क्या यह वही से इसकी शुरुआत होती है यह कोई एक लंबा काल इसने देखा है? हम कहेंगे एक लंबे वक्त से बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी।
मिश्रा:- मेरी नजर में बदलाव की शुरुआत नई अर्थ नीति से देखने को मिलती है। जिसे हम कह सकते हैं तत्काल परिवर्तन अचानक जो हुआ वह नब्बे के दशक के बाद हमें देखने को मिलता है। हम साफ लफ्जों में अगर कहें कि जब अमेरिका का वर्चस्व बड़ा जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वहीं से एक तरीके से बदलाव ने गति ली। और भारत में जब नई अर्थनीति का हल्ला शुरू हुआ आप याद कर सकते हैं की नई अर्थव्यवस्था का हल्ला बोल और सांप्रदायिकता का उभार लगभग एक साथ ही शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि इसने बहुत हद तक लोगों को बिगाड़ा है। जिसे विकास कहा जाता है। जिसे मैं अक्सर एक फर्जी अवधारणा कहता हूं। विकास की अवधारणा लोगों के साथ एक तरह का फ्रॉड है। विकास का मतलब समझदारी होती है। तुम जो समझना और समझदारी वाली बातें हैं वह कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। और पूंजीवाद का जो एक मॉडल समाज ने अपनाया है वह सिर्फ इस वजह से या इस यहां तक ही सीमित नहीं रहता कि उसने शासन को अपने अधीन कर लिया है। और वह समझ में लोगों के मन दिमाग में यह चीज भर देता है कि जो हो रहा है यही सही है और यही होना चाहिए इसका सबसे बेहतर तरीका काम का यही है तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठाने के जो चीज हुआ करती थी वह खत्म हो जाती है । क्योंकि जब सारे ही प्रश्न एक जगह हैं और अब आप लोगों के मनों में यह भर दिन की जो हो रहा है वह सही है तो जब सब कुछ सही है तो उसे पर सवाल कैसा पड़ेगा। तो यह समाज की हकीकत है और हम इसी गफलत में हैं की जो हो रहा है वह सब सही है और लोग उसे पर सवाल उठाना बंद कर चुके हैं। बार-बार यह एहसास दिलाया जाता है या फिर एक नरेटिव बनाया जाता है कि जो हो रहा है उसका कोई विकल्प भी नहीं है। जब विकल्पहीन समाज की आप भूमिका तैयार करने लगे तो हमें इस तरह की परेशानियों को तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन यह सच नहीं है हर एक चीज का विकल्प होता है और हर समय विकल्प तैयार रहता है। सत्य यह भी है कि जब आप विकल्प की तलाश में रहते हैं तो आपको परेशानी भी झेलनी होती है और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। एक समाजवादी चिंतक थे जिन्होंने समाजवादी जन परिषद की स्थापना की किशन पटनायक डॉक्टर लोहिया के अनुयायी थे। पटनायक साहब की किताब है विकल्प हीन नहीं है दुनिया। मतलब यह जो दुनिया है इसमें जो चीज हैं उसमें विकल्प है। लेकिन जो मौजूदा वक्त में या फिर किसी भी कालखंड में लोगों के दिलों में मनों में दिमाग में जो प्रचारित किया जा रहा है वह इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि जिस तरह उसका कोई विकल्प न हो। यह देखेंगे जो महान मूल्य बीसवीं सदी में थे पंथनिरपेक्षता ,लोकतंत्र ,समानता यह सब लोगों की प्राथमिकता से दूर हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो लोकतंत्र पर एक गहरा संकट है और चर्चा इस पर होती है कि एक साथ चुनाव करवाने से खर्च कम होगा। अब वह मूल्य महत्वपूर्ण नहीं रहे खर्चा महत्वपूर्ण बन चुका है। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा वह महत्वपूर्ण नहीं है। और आप इसे इस तरीके से भी देखेंगे कि यह जो चीज सामने आई है यह सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगी इसमें यह भी होगा यह भी नजर में आ सकता है कि बार-बार चुनाव कराने की क्या जरूरत है, हर पांच साल में जरूरत महसूस नहीं है । एक बार चुनाव हुआ और अब रहने दीजिए। और इन चीजों का जिन्हें विरोध करना चाहिए था देखने को मिल रहा है कि वह भी कहीं ना कहीं इस चंगुल में फंस रहे हैं। बीसवीं शताब्दी में जो हमारे देश में आंदोलन हुए जिसे जनता के मन में न्याय की भूख पैदा की थी जो समानता की भूख पैदा की थी, भाईचारे की भूख पैदा की थी नई व्यवस्था ने इन सभी अप्रासंगिक कर दिया।
अरमान :- सभी का व्यवसायीकरण फिर वह चाहे कोई भी संस्था क्यों ना हो पत्रकारिता या फिर दूसरी दीगर एक नजर से देखा जाए तो हो रहा है और यह बात सच भी है कि खतरनाक है । किस तरीके से इसका सामना कर सकते हैं?
मिश्र - लेकिन आप देखेंगे कि व्यवसाय के भी कुछ मूल्य होते हैं और मीडिया उसके एथिक्स जो कह सकते हैं उससे भी नीचे उतर चुका है। और कुछ सिद्धांत जो बनाए गए थे वह भुलाए जा रहे हैं । और बाजार का कोई सिद्धांत नहीं होता है सिवाय मुनाफे के, उसे मुनाफे से मतलब है फिर वह रास्ता कुछ भी हो सकता है। और जो बाजारवाद है उसने हर एक चीज को बाजारू बना दिया है सबकी कीमत लगाई जा सकती है। सभ्यता के विकास के साथ तो बाजार होगा लेकिन हर व्यक्ति बाजारू हो जाए यह तो सही नहीं है ना। बाजारू हो जाने का मतलब वह केवल और केवल अपना लाभ देखें सामाजिक समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि वह व्यक्ति बड़ा ही प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल होने से आप क्या समझते हैं व्यवहारवाद ही तो है वह कि जिस चीज से आपका काम निकल रहा है वह आप करते रहिए कोई मूल्य नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिकल है। एक जो आइडियल कैरेक्टर होता है वह संघर्ष करेगा वह सड़क पर निकलेगा वह काम करेगा। और जो प्रैक्टिकल होगा वह शांत रहेगा और जहां उसे अपना लाभ नजर आएगा वह बस वहां से अपना काम लेकर शांत हो जाएगा। जो वर्चस्ववाद जिसे कहा जाता है पूंजी का जो वर्चस्व है सामने आया है। इस पूंजी के वर्चस्व ने नागरिक के विवेक को प्रभावित किया है।
अरमान:- और एक जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है सांप्रदायिकता जिस तरीके से हावी हुई। एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत सामने आई। एक चीज जो साफ तौर पर हमें देखने को मिलती है वह दो ही पक्षों की तरफ से महात्मा गांधी के जो विचार थे उन्हें पूरी तरीके से खराब करने की एक मुहिम सी चली।
मिश्र:- बिल्कुल सही कहा और ना सिर्फ महात्मा गांधी के विचार बल्कि पूरे स्वाधीनता संग्राम को बदनाम करने का प्रयास हुआ। स्वाधीनता आंदोलन ने जो देश में विचार का माहौल बनाया था उसे विचार को ही प्रश्नाकित करने का प्रयास हुआ है।
अरमान :- और समाज को इस अवस्था तक लाने के लिए भी एक लम्बा वक्त लगा ।
चित्तरंजन मिश्र :- बिल्कुल सही का कोई भी चीज एक दिन में बदली नहीं जा सकती । देश के बुद्धिजीवियों को भी खास ढंग से प्रभावित किया है ।जैसा मैंने शुरू में ही कहा इस तरीके का माहौल बन गया कि दूसरा विकल्प लोगों ने तलाश ही छोड़ दिया और वहां से लोगों को यह लगने लगा कि जो हो रहा है वही सही है लेकिन हमें आज भी कोशिश में लगे रहना है कि एक दिन हम इसे सब पहले जैसा बना सकेंगे। और जो सबसे बड़ा कारण इनके फलने फूलने का रहा ऐसी विचारधाराओं का वह मेरी नजर में नई अर्थ नीति बनी जिसने इन्हें पूरा मौका दिया अपने विचार को बढ़ाने का प्रचार करने का क्योंकि पूंजीवाद प्रचार को ही सबसे महत्व प्रदान करता है । और वही हमें आज देखने को मिल रहा है जितना जिस चीज का प्रचार करेंगे चाहे वह कितनी ही हानिकारक क्यों ना हो । लेकिन एक वक्त आएगा जब लोग उसे अपनाने लग जाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब लोग उसे अपना रहे। ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे हैं आप हम जैसे लोग आज भी समझ में अपना प्रयास जारी रखे हुए और हमें निरंतर के साथ में ऐसा ही करना। और नई शिक्षा नीति मुझे लगता है पूरी तरीके से शिक्षा के खिलाफ है जिस तरीके से यूजीसी नए-नए नियम बना रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा अरमान साहब रोज एक ऐसा काम करते हैं यह जब तक आप सोचेंगे इसका विरोध करना है तब तक वह दूसरी कोई नई चीज लेकर आ जाएंगे। आप दूसरी चीज को देखेंगे वह जब तक तीसरी चीज लेकर आ जाए तो लगातार एक साइकिल बना दिया है। खतरे को समझना चाहिए उन लोगों को जिनका विश्वास लोकतंत्र में है। जिनका विश्वास स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों में है। जिनका विश्वास वाकई में राष्ट्रीय एकीकरण में है। जो लोग पूरे देश को एक मानते हैं अपना समझते हैं यह उन लोगों को देखना चाहिए। खुलकर कहूं जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लगता है वह पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार नहीं है तो क्या आप वहां के प्रधानमंत्री नहीं हैं किस तरह की सोच है आज के माहौल में? जहा उनकी सरकार है वह सिर्फ वही के प्रधानमंत्री हैं। और जिस राज्य उनकी सरकार नहीं है वह वहां के प्रधानमंत्री नहीं है। इस तरीके की नीति इतने खराब नीति है यह जिसने हमारे पूरे संघीय ढांचे का अपमान किया है। प्रधानमंत्री तो सभी के हैं। क्योंकि आप देखेंगे जिस वक्त राजस्थान में उनकी सरकार नहीं बनी उसे वक्त यह वहां के प्रधानमंत्री नहीं थे और आज की तारीख में जब राजस्थान में सरकार आ गई तो यह वहां के प्रधानमंत्री हो गए। आज के वक्त में हम लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी।
अरमान:- जिस तरीके से कुछ चीजों को सामने रखा गया जैसे धर्म और संस्कृति को एक आमने-सामने खड़ा कर दिया गया जबकि यह दोनों अपने आप में एक अलग चीज है । दूसरा जो पत्रकारिता के ऊपर दबाव बना है ,यह भी एक बड़ा कारण है।
चित्तरंजन मिश्र :- प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है की सांप्रदायिकता को अपने असली रूप में लाज लगती है इसलिए वह संस्कृति का लबादा ओढ़ कर आती है। और इस वक्त यही चल रहा है।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय दिया, आपका बहुत आभार।
चित्तरंजन मिश्र - बहुत बहुत शुक्रिया।
Professor Rawail Singh
प्रोफेसर रवैल सिंह
पंजाबी के वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद् और दीर्घकालीन प्रशासनिक अनुभव रखने वाले प्रोफेसर रवैल सिंह से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
पूंजीवाद ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रभावित किया है - रवैल सिंह ।
परिचय
प्रोफेसर रवैल सिंह
वर्तमान में महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय सिख अध्ययन केंद्र। • 9 मई, 2014 से 28 फरवरी, 2021 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पंजाबी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया (12 फरवरी, 2015-18 तक विभागाध्यक्ष रहे) • 2 मार्च, 2000 से 29 जनवरी, 2014 तक पंजाबी अकादमी, दिल्ली सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया • पंजाबी अकादमी, दिल्ली सरकार के सहायक सचिव के रूप में कार्य किया • ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़रीडर (पंजाबी) के रूप में कार्य किया । प्रशासनिक अनुभव अनुसंधान, शिक्षा के साथ-साथ प्रशासन में 35 वर्षों का विशाल अनुभव है। . दिसंबर, 2022 से पांच वर्षों के लिए साहित्य अकादमी (अकादमी ऑफ लेटर्स) के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित। 2. दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय सिख अध्ययन और मल्टीमीडिया सभागार के महासचिव के रूप में नामित। 3. पंजाब के सचिव के रूप में नामित साहित्य अकादमी, पंजाब सरकार।
4. सदस्य, गवर्निंग काउंसिल (कुलपति द्वारा नामित), एसजीएनडी खालसा कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय
5. सदस्य, गवर्निंग काउंसिल (कुलपति द्वारा नामित), माता सुंदरी कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय
6. सदस्य< गवर्निंग काउंसिल (कुलपति द्वारा नामित)
प्रकाशित पुस्तकें
1. पंजाब दी लोक नट परंपरा ते पंजाबी नाटक, शिलालेख प्रकाशन (2000)
2. पंजाब की लोक नाट्य परंपरा एवं पंजाबी नाटक, पंजाबी अकादमी, दिल्ली 3. बलवंत गार्गी भारतीय साहित्य के निर्माता, साहित्य अकादमी, सरकार। भारत का (2012)
4. मीडिया: विहारिक अध्ययन, ग्रेसियस बुक्स, पटियाला (2012)
5. मीडिया: सभ्याचारक साम्राज्यवाद, अर्सी पब्लिशर्स, दिल्ली (2013)
6. शबद सहज धुन, आर्सी पब्लिशर्स, दिल्ली-2021
7. मार्जानियां (नाटक), अर्से पब्लिशर्स, दिल्ली-2021
8. द वर्च्ड ओन्स (अंग्रेजी में नाटक), हर आनंद बुक्स इंटरनेशनल, दिल्ली, 2022।
अनुवादित पुस्तकें
. भारत दे पंछी, प्रकाशन विभाग, सरकार। भारत का (1999)
भारत दी संसद, की, कियों अते किवेन, नेशनल बुक ट्रस्ट (2001)
भारत दे लोक नाच, प्रकाशन प्रभाग, सरकार। भारत का (2008)
मुनिया रानी, नेशनल बुक ट्रस्ट (2009)
सुनो कहानी, साहित्य अकादमी, सरकार। भारत का (2010)
बच्चों ने फाड़िया चोर, साहित्य अकादमी, सरकार। भारत का (2012)
मोरां वाला बाग, साहित्य अकादमी, सरकार। भारत का (2012)
स्वच्छता दी कहानी, दादी दी ज़ुबानी, (4 खंड), प्रकाशन विभाग, सरकार। भारत का (2017)
संस्थाओं , संगठनों से जुड़ाव
1. विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव।
2. विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव।
3. उत्तराखंड सरकार की भाषा परिषद के सदस्य।
4. साहित्य अकादमी के क्षेत्रीय बोर्ड के पूर्व संयोजक।
5. साहित्य अकादमी के पंजाबी सलाहकार बोर्ड के पूर्व संयोजक।
6. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के पंजाबी बोर्ड के पूर्व संयोजक।
7. पटियाला के विश्व पंजाबी केंद्र के कार्यकारी सदस्य।
8. पंजाब कला परिषद के शासी बोर्ड के सदस्य।
9. पंजाब भाषा विभाग के राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य।
10. ललित कला एवं साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के कार्यकारी सदस्य।
11. पंजाबी साहित्य अकादमी, लुधियाना के कार्यकारी सदस्य।
12. पंजाब सरकार के संस्कृति, पर्यटन एवं विरासत के विकास के लिए उच्चस्तरीय समिति के सदस्य।
13. पंजाबी विकास पर स्थायी समिति के सदस्य, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।
14. महासचिव, पंजाबी संस्कृति केंद्र।
15. उपाध्यक्ष, सलाहकार परिषद, नवी मुंबई सांस्कृतिक संघ, नवी मुंबई।
16. मानद सलाहकार, पंजाबी अकादमी, दिल्ली सरकार।
17. सदस्य, शोध अध्ययन बोर्ड, खालसा कॉलेज, पटियाला
18. सदस्य, शोध अध्ययन बोर्ड, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला
पुरस्कार और विशिष्टताएँ
. पंजाबी भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी साहित्य सभा, दिल्ली द्वारा पुरस्कृत-
2014
पंजाबी साहित्य सभा कनाडा-2017 द्वारा सम्मानित
पंजाब भवन, सर्री, कनाडा-2017 द्वारा सम्मानित
सिरजना केंद्र, कपूरथला-2021 द्वारा करतार सिंह दुग्गल पुरस्कार से सम्मानित
अरमान :- साहित्य लेखन में आपकी शुरुआत कैसे हुई वह कौन से शुरुआती पल थे जिन्होंने आपको साहित्य के प्रति प्रेरित किया?
रवैल सिंह :- पंजाब के छोटे गांव से आता हूं जहां पर लोक नाटक की टोलियां आया करती थी। इस वक्त हम बहुत ज्यादा नाटक देखा करते थे इसमें काफी दिलचस्प बनने लगी मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मेरा शुरुआत ही रुझान था वह लोक नाट्य की तरफ ही था फिर धीरे-धीरे उसमें कुछ जगह भी मिलने शुरू हुई नाटक में रोल करने शुरू किया। लेकिन जो साहित्य की बात करूं तो उसमें मेरा काफी देर बाद से दिलचस्पी शुरू हुई फिर मैं अपने स्कूलिंग और बैचलर्स के बाद में जब मास्टर्स किया पंजाबी के अंदर उस वक्त मेरा साहित्य की तरफ रुझान काफी बड़ा। फिर उसके बाद कविताएं लिखनी शुरू की। फिर उसके बाद आलोचनात्मक आलेख लिखने शुरू किया । और एक वक्त के बाद वापस नाटक की तरफ आया क्योंकि वह शुरुआती प्रेम मेरा वही था । मैंने कुछ मुद्दे उठाए और जो सबसे ज्यादा परेशानियां महिलाओं के लिए थी उसे वक्त उन पर मैंने ध्यान दिया और रेप बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तो उन चीजों के ऊपर भी लिखना शुरू किया। और उसके बाद में ऑल इंडिया रेडियो में मेरी नौकरी लगी। और उसके बाद में मेरा रुझान पत्रकारिता की तरफ बढ़ गया और पत्रकारिता पर भी मैंने किताब लिखी। और उसके बाद में दिल्ली सरकार में पंजाबी अकादमी का सचिव बना। और इसी सब के चलते भाषा, साहित्य ,संस्कृति इन सब के साथ में मेरा रुझान बढ़ता ही गया। और संगीत और नाटक में मेरा दिल पहले से ही था। और उसके बाद पंजाबी अकादमी के सचिव रहते रहते ही मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ। और पंजाबी का हेड भी बना दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
अरमान :- आपने बात की आलोचना की की ,आपने काफी क्रिटिकल क्रिटिक्स के रूप में भी काम किया लेकिन ऐसा महसूस होता है कि लोगों ने आलोचना को कभी समझ ही नहीं ना सिर्फ आम व्यक्ति साहित्य से जुड़ा हुआ भी उसे महसूस नहीं कर पाता और सिर्फ एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपने मन में बना कर रखता है इस पर आपके क्या विचार हैं?
रवैल सिंह :- अगर हम आलोचना का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब विरोध करना होता है। लेकिन जब हम उसको साहित्यिक दृष्टिकोण से देखते हैं। और साहित्यिक आलोचना का मतलब ही होता है कि जब आप किसी रचना को पढ़ते हो जब उसे रचना को तोलते हो कि इसमें अच्छी चीज कौन सी है और कौन सी खामियां नजर आती है और उसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है और यह किस तरीके से और ज्यादा बेहतर हो सकती थी और सही मायने में यही एक आलोचक का काम होता है । उसका काम यह नहीं कि वह उसका खंडन करें और सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को यह मिलती है और यह चीज सभी भाषाओं में हो सकती है क्योंकि मैं दूसरी भाषाओं को भी देखता हूं और थोड़ा कुछ जानता भी हूं क्योंकि मैं आर्ट्स फैकल्टी में रहा हूं और दूसरी भाषाओं के लेखक साहित्यकार ,रचनाकारों से संवाद बना रहता है। और जो हमारे जीवन में 1990 के बाद में जिस तरीके से बदलाव आए हैं तो जिसमें लोग इस तरीके की सोच में डूब चुके हैं कि हम सब कुछ जल्दी-जल्दी हासिल कर ले। फास्ट फूड की तरह वह ज्ञान भी फास्ट हासिल करना चाहते हैं। एक तो यह सबसे बड़ी समस्या आज के लोगों में देखने को मिलती है कि वह सब्र को त्याग रहे हैं उन्हें ठहरता नहीं आता। जिस तरह की जल्दबाजी और हड़बड़ाहट हमें देखने को मिल रही है यह भी एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देती है। इसमें हां यह है कि बंदा रातों-रात ही विद्वान बन जाना चाहता है। जिसमें उसे संघर्ष बिल्कुल करना गवारा नहीं है। और एक और मुझे समस्या देखने को मिलती है सभी भाषाओं में कि उन्होंने वेस्टर्न पॉइंट्स को अपना आधार बना लिया। वहां पर मार्क्सवाद आया तो हमने मार्क्सवाद की बात करनी शुरू कर दी या जैसे-जैसे वहां परिवर्तन हुए उसकी धुरी पर हमने अपना कार्य करना शुरू किया। और हमारी जो अपनी पद्धतियां हैं हमने उनको पीछे कर दिया और वेस्टर्न थिअरीज को हमने अपनाना शुरू कर दिया । हमारा जो थॉट प्रोसेस है वह हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से आता है। और उसे कल्चरल बैकग्राउंड से ही हमारी आलोचना बनानी चाहिए थी यह समस्या असल में नजर आई है। जिस प्रकार फास्ट फूड वेस्ट से आया है उसी तरीके से जल्दी-जल्दी सफल होने का क्या यह हम आंखें बंद करके वेस्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे जीवन में पूरी तरीके से आ गया फिर चाहे वह खाने में कपड़ों में तो विचारों में क्यों नहीं आएगा। और ज्ञानवर्धन भी इस धुरी पर हो रहा है। लगता है यही समस्या है कि लोग आलोचना को क्यों पसंद नहीं करते हैं और खासकर के लेखकों को तो आलोचक बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। और यहां लेखन के साथ भी समस्या आती है मैं वैसे बहुत से लेखकों को जानता हूं। वह लिखते तो है लेकिन वह दूसरे लेखकों की रचना पढ़ते नहीं है। अभी यह विचार आने लग जाए कि जो मैं लिख रहा हूं वैसा कोई और नहीं जानता। एक भ्रम बन जाता है मन में। समाज में जो लिखा जा रहा है जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं उसे खंगालेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि आप नई रचना नहीं लिख सकते। यह भी होता है कि जब आलोचक जवाब देता है तो वह भी बुरा लगता है। और लेखक यह सोचने लग जाता है कि जो मैंने लिखा है वह सही है और इसमें आलोचक की कोई जगह नहीं। और अगर वेस्ट का ही मॉडल अपनाना है तो वेस्ट का मॉडल तो यह भी कहता है कि लेखक के रचना करने के बाद में रचना के लिए लेखक मर जाता है अब वह रचना पाठक की अब वह उसे कैसे देखा है। अब जो रचना के अर्थ है वह पाठक को करने हैं उसे लेखक का कोई मतलब नहीं।
अरमान :- दिल्ली सरकार में काम किया ,प्रोफेसर रहे साहित्य से जुड़ाव है और सामाजिक समस्याओं को काफी नजदीक से आपने देखा और महसूस किया है। और जो सामाजिक बदलाव अगर हमने देखा है तो वह वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है लेकिन जब जो गति पकड़ी है वह पिछले बीस साल में सबसे ज्यादा हुई है आप सामाजिक दृष्टि से पिछले बीस साल के बदलाव को भारतीय समाज पर कैसे देखते हैं?
रवैल सिंह :- 1990 के बाद यू एस एस आर का विघटन होता है। बाद में दुनिया एक की तरफ शिफ्ट होने लगी। कोई तरीके से दुनिया अमेरिका ओरियेंटेड होने लगी। मार्क्स ने कहा था सभी संसाधन बराबर बांटे जाएंगे वह भी नहीं हो सका । लेकिन जो समाजवादी भाव था वह सभी का उद्धार करने वाला था। और पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट हम सभी समझते हैं और जब वह हावी हुआ। और जब पूंजीवाद बढ़ता है तो उसी के साथ-साथ बाजारवाद आता हैं तो लोगों का स्वभाव इसमें परिवर्तन होता है। बाजार बाद में खासकर की जो मीडिया का रोल है। मैं खुद भी पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं। पूंजीवाद ने बाजारवाद ने मीडिया का जो रोल है वह काफी हद तक बदल दिया। किसी वक्त में जब हम कहा करते थे कि समाज का और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता उसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदलने का काम किया है पूंजीवाद बाजारवाद के हावी होने के बाद कि जब लोगों को यह चीज समझ आने लगी कि हम मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं तो उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुए जो कानून बने के दुनिया की साड़ी मार्केट खोल दी जाए सभी के लिए उसे स्थिति में उसे कल के अंदर मीडिया ने अपना ऐसा रोल अदा किया तो उसे स्थिति में जो थर्ड वाल्ड है उसके सभी देश काफी प्रभावित होते हैं। फिर वह एक ऐसा निजाम बना देते हैं कि जहां आपको अपने हाथ में फैसला लेने की ताकत नहीं होती है आपको वही करना होता है जो कहीं ना कहीं बाकी लोग कर रहे हैं यानी कि आपकी जो मर्जी है आपके जो स्थिति है वह इतनी निर्भर नहीं करती जितनी कि सामने वाली की मर्जी और परिस्थिति आप पर हावी होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें लगता है कि आप खुद के फैसले कर रहे हैं लेकिन हकीकत यह नहीं है और ऐसा नहीं होता है कि आप फैसला खुद कर रहे हैं। यही चीज होती है कि आपको लगता है कि आप खुद से वोट कर रहे हैं लेकिन यह भी आधी सच्चाई है। यह भी आपका खुद का फैसला नहीं होता। आपको ऐसे उलझा दिया जाता है खबरों के माध्यम से कि आप मजबूर हो जाते हैं उस एक नॉरेटिव की तरफ जाने के लिए। आपके मन दिमाग में इस तरीके से बातें और गलतफहमियां भर दी जाती है कि जो झूठी खबरें हैं वह भी आपको सच लगने लगती है। उसके कई सारे उदाहरण है मैं इसको समझने के लिए अपने विद्यार्थियों को भी कुछ उदाहरण दिया करता था। जैसे कि क्या हिंदुस्तान की लड़कियां 1990 के बाद ही खूबसूरत हुई या उससे पहले भी वह खूबसूरत थी। यानी कि जब ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन विश्व सुंदरी बनी तो क्या उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर महिलाएं नहीं थी खूबसूरत। तो सवाल यह आता है उसे दौर में ही क्यों इनको विश्व सुंदरियों का खिताब दिया गया। इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेचने थे। तो यह कहा गया कि आपकी औरतें बहुत खूबसूरत है तो वह फलां साबुन का इस्तेमाल करती है। इस तरह के विज्ञापन बड़े पैमाने पर बनाए गए। और अपना वह प्रॉडक्ट बेचने के लिए हिंदुस्तान की लड़कियों को मॉडल बना दिया गया। विज्ञापनों में आप देखते हैं कि अगर आप यह इस्तेमाल करेंगे तभी आप इनकी तरह बन पाएंगे। और सवाल फिर से वही होता है कि जो पैमाना हमने तय किया या जो हमारा पैमाना है खूबसूरती का हम उसे कितना अलग दूर होते जा रहे हैं। इस त्योहार की हम बात करते हैं तो क्या उसमें सच्चाई होती है नहीं भी होती है यह लोगों तक कैसे पहुंचा जाए क्योंकि अगर हम बात करें यह तो एक सामान्य से साबुन की थी लेकिन अगर हम तंबाकू की बात करते हैं और हानिकारक सामग्रियों के भी बड़े पैमाने पर इश्तहार बनाए जाते हैं तो जो एक्टर गुटके का ऐड कर रहा है तो क्या सच में वह खुद भी उसका इस्तेमाल करता है जी बिल्कुल नहीं करता वह सिर्फ अपने पैसे के लिए कर रहा है लेकिन देखने वाले को ऐसा महसूस होता है कैसे अलग सी खुशी होती है कि यह भी उसी का इस्तेमाल कर रहा है जिसको मैं पसंद करता हूं तो यह जो एक वहम जहन के अंदर बन जाता है यही समस्या का सबसे बड़ा कारण बनता है।
अरमान :- मेरा यह सवाल सिर्फ भारतीय समाज पर ही रहेगा हिंदुस्तान के दो प्रमुख धर्म है सनातन और इस्लाम उनके कंजरवेटिव रूढ़िवादी अपनी बहन बेटियों को पर्दे, बुर्के में रखना पसंद करते हैं लेकिन आखिरकार हमें यह भी तो देखना होगा जो दुष्कर्म कर रहे हैं वह भी समाज में से हैं हम में से ही लोग इस तरह की चीजों को करते हैं। तो बात कपड़ों की है या नीयत की क्योंकि हम अक्सर सुना करते हैं की लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। लेकिन हमने यह भी देखा है कि जो मृतक शरीर है महिलाओं के उनके साथ भी बलात्कार हुए हैं
आखिर हम इसे कहां तक जाकर समझ सकते हैं बात कपड़ों की है या नीयत की?
रवैल सिंह :- देखिए कपड़ों की बात तो बिल्कुल भी नहीं है यह तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा वहम बनाया हुआ है कि कपड़ों की वजह से बलात्कार होते हैं। नीयत से पहले भी हमें अपने समाज की कुछ और चीजों के बारे में भी देखना होगा जैसे लड़की पैदा हुई और उसे मार दिया भ्रूण हत्या होती है यानी पैदा होने से पहले ही उसकी जान ले ली गई। और अगर पैदा हो गई तो उसे चार दिवारी में रखा गया जितना हो सके उतना उसे अपने दबाव प्रभाव के अंदर बनाए रखने की कोशिश रही। और जो अनुपात है उसे इतना काम कर दिया 1000 लड़कों के बराबर 700 लड़कियां हुई। दो ढाई सौ का जो गैप बन जाता है यह भी एक बड़ी समस्या बनता है। लड़कियों की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है शादियों में भी। के लड़के हैं और लड़कियां ही नहीं मिल पाती शादी के लिए । वह चीज कब तक होगी जब तक वह उसे बंदिश के अंदर है लेकिन जब उसके बाद में उसको थोड़ी सी भी आजादी मिलेगी तो वह सबसे पहले वही काम करने की इच्छा रखेगा जिसकी उसे पर सबसे ज्यादा बंदिश थी। यही चीज हमने लड़कियों के साथ भी की और उन पर इतनी ज्यादा बंदिश लगा दी और कड़ी निगरानी कर दी कि तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी तो घर के किसी मर्द के साथ बाहर निकलोगे और दूसरे से बात नहीं करोगी ,घर जरूरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाओगी तो इस तरह की चीज यानी कि बाहर समाज में क्या हो रहा है उसकी बात एक अलग है लेकिन हमने उसे घर में ही बंद कर रख दिया। तो इस तरीके की चीज महिलाओं में भी होती है कि जब उन्हें थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो वह अपने उन काम को करना पसंद करती है जो एक सामान्य स्थिति के अंदर किया जा सकता है। ह्यूमन माइंड की ही संरचना है कि जब साइकोलॉजिकल किसी के ऊपर दबाव इतना ज्यादा बनाया जाता है तो वह अपनी थोड़ी सी आजादी को भी सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है और कई बार इन्हीं चीजों में परेशानियां भी लोगों को सामना करती है क्योंकि उन्होंने वह चीज कभी पहले महसूस ही नहीं की थी तो जब इस तरीके की बंदिश है और पहले लगते हैं तो समाज के अंदर काफी परेशानियों का भी जन्म होता है। लगता है नियत से ज्यादा परेशानियां यहां पर भी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यह चीज आपको वेस्टर्न कंट्रीज में पश्चिमी समाज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी मैं जब अमेरिका में गया तो वहां पर लड़कियां लड़के आराम से घूमते भी है थे उसे वक्त और उनके कोई कपड़ों में या उसे तरीके की चीजों के अंदर बंदिशे नहीं है तो जब पहली बार यहां से कोई मर्द औरत देखते है तो उसको वहां एक अलग ही नजर आती है लेकिन कुछ टाइम बाद में वह भी वहां के माहौल में ढल जाता है उसके लिए वह एक सामान्य दर्शन हो जाता है।
अरमान :- आपकी लेखनी वाकई में समाज की उन चीजों की तरफ हमें देख पाने के लिए मजबूर करती है जिसके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते हैं और सही मायने में इसी तरह का लेखन समाज को मिलना चाहिए लेकिन कभी कोई गजल यह कहानी कविता आलेख लिखते हुए मुश्किलों का सामना करना पड़ा या फिर ऐसी कोई आपकी रचना जिसमें आपको सबसे ज्यादा कठिनाई हुई हो? या फिर कभी यह महसूस हुआ कि कि मैंने जो लिखा है मैं इसकी भाषा को और ज्यादा आसान कर देता हूं ताकि जो विचार मेरे हैं वह पाठक आसानी से समझ पाए।
रवैल सिंह :- बिल्कुल यह बात आपने काफी अच्छी कही और मेरे जो गुरु हैं जिनसे लिखना पढ़ना सीखा है , उन्होंने भी मुझे यह एक चीज बताई कि तुम अपने लेखनी अपनी भाषा को जितना हो सके सरल बना ताकि पढ़ने वाला चाहे व्यक्ति दार्शनिक हो या एक आम वह उसे एक बार में समझ पाए। और जब मैं लिखता हूं कोशिश करता हूं कि बहुत लंबे-लंबे सेंटेंस ना बनाऊं। मैं बहुत ज्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। लोगों के पास होकर उनसे कनेक्ट कर लिखना पसंद करता हूं कि जो मैं लिख रहा हूं क्योंकि वह भी तो समाज का ही एक हिस्सा है । अगर मैं किसी गांव की कहानी लिख रहा हूं तो मैं खुद को उस गांव में बैठा हुआ पाता हूं कि मैं खुद भी उस पेड़ की छांव में हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं और आसपास वही वातावरण बनना शुरू हो जाता है। और जब मैं कोशिश करता हूं औरतों के बारे में लिखने की तो मैं यह महसूस सकता हूं कि मैं उन्हीं के बीच में रहकर काम कर रहा हूं। कि उनकी जो परेशानियां है जो उन्होंने महसूस किया है मैं वह लिखूं उनका रूप का काम करूं। जब मैं बच्चों के बारे में लिखता हूं तो मैं बच्चा बन कर लिखता हूं क्योंकि वह चीज आप तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसमें खुद नहीं डूबेंगे। और जब आप इस तरीके से लिखते हैं और अपना काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और आप खुद भी अपनी बात को बेहतर तरीके से सामने वाले को समझ सकते हैं ।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार।
रवैल सिंह - आपका भी बहुत धन्यवाद ।
Vinod Joshi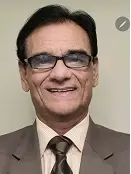
विनोद जोशी
सुप्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक, गुजराती भाषा के विद्वान और साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त विनोद जोशी से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
कवि केवल भाषा रचना करता है और भाषा के माध्यम से अगर हम कविता के सौंदर्य को प्राप्त करें तो इससे आगे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। - विनोद जोशी
विनोद जोशी (जन्म 13 अगस्त 1955) गुजरात, भारत के गुजराती भाषा के एक भारतीय कवि, लेखक और साहित्यिक आलोचक हैं। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में परंतु, गीत (गीतात्मक कविता) का एक संग्रह, शिखंडी, महाभारत के एक पात्र शिखंडी पर आधारित एक लंबी कथात्मक कविता, रेडियो नाटक: स्वरूप एने सिद्धांत (रेडियो नाटक: रूप और सिद्धांत, एक संक्षिप्त पीएच.डी. थीसिस), टुंडिल-टुंडिका, पद्यवर्त का एक रूप, एक गुजराती मध्ययुगीन साहित्यिक शैली, और ज़ालर वागे ज़ूथडी, कविताओं का एक संग्रह शामिल हैं। वह जयंत पाठक पुरस्कार (1985), आलोचक पुरस्कार (1986), कवीश्वर दलपतराम पुरस्कार (2013), साहित्य गौरव पुरस्कार (2015), नरसिंह मेहता पुरस्कार (2018), कलापी पुरस्कार (2018), दर्शक साहित्य सम्मान पुरस्कार (2021), नर्मद सुवर्ण चंद्रक (2022) और साहित्य अकादमी पुरस्कार (2023) के प्राप्तकर्ता हैं।
अरमान :- आज ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश में आपका नाम साहित्यिक जगत में विख्यात है आपकी शुरुआत कैसे हुई ?
विनोद जोशी:- मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं साहित्यकार बनूंगा लेकिन जो मेरी प्राथमिक शिक्षा थी जब मैं अपनी शुरुआती तालीम हासिल कर रहा था उस दौरान मुझे कुछ लिखने का मन होता था । अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन वह छठी सातवीं क्लास होगी जब मेरे मन में पहली बार कुछ लिखने को आया। और जब लिखना शुरू किया और वह चीज जब मुकम्मल हुई तब मैंने वह अपनी रचना किसी को दिखाई तो उन्होंने पढ़कर कहा कि यह तो कविता जैसी मालूम होती है। लेकिन उसे वक्त में इतना छोटा था कि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि कविता क्या होती है। लेकिन जब धीरे-धीरे में बड़ी क्लासों में आया और जब मैं दसवीं क्लास में आया उस वक्त स्कूल की टेक्सबुक पढ़नी शुरू की और उन किताबों में जब मुझे कविताएं पढ़ने को मिली तब कुछ हद तक इसके बारे में मैं समझने लगा था । और जो कि छंद में थी। जब वह कविताएं मैंने पढ़ी और उन्हें समझने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इस तरह की रचनाएं तो मैं भी कर सकता हूं। अगर मैं आपको अपनी कविताओं के बारे में बताऊं तो मेरी जो पहली कविता थी वह मैंने शिखरिणी छंद में लिखी थी वह भी सोनेट के स्वरूप में। और गुजरात में एक सम्मानित और प्रतिष्ठित पत्रिका है कुमार नाम से वहां मैंने अपनी रचना भेजी और वह छप भी गई। और लोगों ने जब मेरी रचना पढ़ी उन्हें काफी पसंद भी आई और वे काफी खुशी के साथ में यह कहते कि कुमार में रचना छपना वाकई बड़ी बात है । कहते कि तुम्हारी कविता शिखरिणी छंद में लिखी हुई है और सोनेट के स्वरूप में छपी है । इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई तब मुझे और प्रोत्साहन मिलता है कि हां मैं लिख सकता हूं। निश्चित ही वह समय लिखते रहने के लिहाज से मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक था । और फिर इन सब के बाद में तो लिखना चालू ही रखा और मैं लिखता रहा । जब मैं कॉलेज में आया और उसे वक्त तक तो मेरी बहुत सारी रचनाए प्रकाशित हो चुकी थी और लगातार हो रही थी । मेरी कविताएं गाई जाती थी मुझे कवि सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता था और दीगर साहित्यिक कार्यक्रमों में भी मुझे आमंत्रण मिलते। और फिर धीरे-धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि शब्द के साथ मेरा जो यह संग है काफी गहरा है और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ सकूंगा । इसी दिशा में निरंतर कार्यरत रहा ।
अरमान :- जब भी कोई लेखक साहित्य सृजन करता है तो उसके दिमाग में काफी चीज रहती है वह काफी मुद्दों को अपने ध्यान में रखता है लेकिन साहित्यिक समाज पर जो राजनीतिक प्रभाव है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं?
विनोद जोशी:- मैं बहुत ही अलग सोच का कवि हूं, मैं कवि की कोई सामाजिक जिम्मेदारी या राजनीतिक दायित्व या फिर अपने इर्द-गिर्द का जो समाज है, उसके जो प्रश्न होते हैं इन सबको कविता का केंद्र नहीं मानता मैं भाव को कविता का केंद्र मानता हूं । जो कि निसर्ग है जो कि सभी में है और यही कविता की कुंजी है मेरी नजर में। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कविता कमिटेड नहीं होनी चाहिए वह भाषा में लिखी जाती है यही उसका सबसे प्रभावशाली कमिटमेंट है जिससे कभी बच नहीं पाता। तो फिर इस कमिटमेंट में और दूसरे कमिटमेंट कैसे जोड़ सकता है। तो मैं कहता हूं कि मुझे यह चीज नहीं भाती। मैं समझता हूं की कविता अपने आप में एक भाव पिंड है और कवि का सामाजिक दायित्व मेरे लिए प्रमुख नहीं है।
अरमान:- आपने कहा कविता का भाव ही उसका केंद्र होना चाहिए लेकिन एक चीज में मैं आपके विचार लेना चाहूंगा कई बार ऐसा महसूस होता है कि लेखक एक रेस का हिस्सा बन चुके हैं जो सिर्फ साहित्य की चकाचौंध देख रहा हैं । आपको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब भी लेखक का साहित्य सृजन अपने उन्हें सामाजिक मूल्यों के लिए काम कर रहा है।
विनोद जोशी:- इस बात पर जो मेरा दृढ़ विश्वास है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं इंसान जब पैदा होता है उस वक्त वह भाषा लेकर पैदा नहीं होता । भाषा उसे अपने परिवेश से बाद में मिलती है वह भाव लिए इस धरती पर आता है । उनको दर्द होता है उनको खुशी होती है और इन सब चीजों के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। मैं यह समझता हूं कि जब भाव सर्वोपरि है, नैसर्गिक हैं और इसके लिए कोई भाषा को उपयोग में लेकर कुछ लिखता है तो यह सेकेंडरी चीज हो गई। और भाषा में मुझे लगता है कि वह पूरा भाव जगत नहीं लिख पाएगा और इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि वह ऐसी भाषा लिखें जो भाषा के रूप में पिघल जाए और भाव के रूप में प्रकट हो जाए ,अनुभूत हो जाए ,जब कोई कविता अपने मन को भाती है तो उस कविता के शब्द उधर नहीं रहते । वह अर्थ से भी आगे जाकर उसका जो सौंदर्य है भाव पिंड है उसकी अनुभूति करते हैं । मेरी नजर में भावों की तो कोई रेस नहीं हो सकती। अगर हंसने की बात है तो मुझे भी उसी प्रकार की हंसी आती है जैसी जापानी और चाइनीज को आती है। मुझे भी दुख होता है, कोई जर्मन है या फ्रांस से है उसे भी दुख का भाव महसूस होता है तो मेरी नजर में इसमें तो रस की कोई बात ही नहीं यह तो निसर्ग तत्व भाव को साथ लिए जीना है और सभी को साथ लिए मरना है।
अरमान :- अपने अपने साहित्य सृजन के बारे में बताया कि जब आप छठी सातवीं कक्षा में थे तब से आपने लिखना शुरू किया मगर अगर हम आज स्कूलों में पढ़ाने के तरीके की बात करें जाहिर तौर से बच्चों को शुरुआत से ही कविताओं की जानकारी दी जाती है और स्कूलों में उनका पाठन कराया जाता है लेकिन मौजूदा वक्त में उसका तरीका हमें काफी अलग देखने को मिलता है क्या आपको लगता है कि पढ़ने के तरीके में बदलाव की जरूरत है जहां हम साहित्य की बात करें।
विनोद जोशी:- जी बिल्कुल मैं प्रोफेसर रहा हूं खुद चालीस साल से भी अधिक समय तक पढ़ाया है और कविताएं भी पढ़ाई हैं और मेरे अपने अनुभव से मैं यह बात कह सकता हूं अगर आप कविता को पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप उसका अर्थ देकर समाप्त कर देना यह उचित नहीं है। कविता के बहुत सारे पहलू होते हैं कविता के जो शब्द होते हैं वह स्वयं में संगीत भी हैं, यह शब्द स्वयं अर्थ की छाया भी हैं यह शब्दों के सम्मेलन का अनोखा रूप भी हैं । इन सभी को लेकर अगर हम बच्चों से बात करें तो उनको यह प्रतीत होता की भाषा की क्या शक्ति होती है, भाषा क्या-क्या काम कर सकती है, भाषा के गुण क्या है, भाषा में जो छुपा हुआ संगीत है वह क्या है कोई भी शब्द अगर हम बोलते हैं तो सबसे पहले तो यह ध्वनि है और इस ध्वनि की अपनी श्रुति में जो आकर हम रचते हैं उसकी महिमा होती है यह सब पढ़ना चाहिए और हम क्या करते हैं कि क्लास रूम के अंदर केवल इसका मतलब और अर्थ बता देते हैं कहते हैं कि इस काव्य में कवि क्या कहना चाहता है कवि कुछ नहीं कहना चाहता कवि केवल कविता करता है और कविता के माध्यम से अगर हम कविता के सौंदर्य को प्राप्त करें तो इससे आगे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती।
अरमान:- आपने आलोचना पर काफी काम किया है और अगर आज के दौर में हम देखें चाहे फिर वह सामाजिक राजनीतिक या साहित्यिक आलोचना हो क्या वह उतनी ही ईमानदारी से की जा रही है जो एक वक्त में उसकी इमानदारी मानी जाती थी? या आपको लगता है कि इन चीजों में लोग कहीं पर बायस्ड हो जाते हैं
विनोद जोशी :- साहित्य में जो आलोचना होती है उसे कभी भी अंतिम नहीं मानता । मैं मानता हूं की आलोचना व्यक्तिगत होती है । जिसकी आलोचना होती है उसका भी संदर्भ जुड़ा हुआ रहता है । अपना जो ज्ञान है उसका भी संदर्भ जुड़ा हुआ होता है । इंटरप्रिटेशन वह भी संदर्भ इसमें जुड़े हुए होते हैं मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी आलोचना अंतिम नहीं होती है और अगर कोई व्यक्ति पक्षकार होकर आलोचना कर रहा है तब भी मैं मानता हूं कि कोई भी साहित्य रचना समय के पड़ाव में खरी न उतारे तब वह सच्ची रचना नहीं है। महाकवि भवभूति ने कहा था “कालो ह्यं निर्वधिर्विपुला च पृथ्वी” काल अनंत है और पृथ्वी विशाल है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई भाव प्राप्त होता है जो किसी रचना को प्रमाणित करता है ऐसा होता है कि कोई रचनाएं इस काल में संभव ना हो कि वह सभी को स्वीकार्य बने तो हो सकता है कि वह दूसरे काल में स्वीकार्य बने ऐसा हम देखते हैं बहुत बार।
अरमान :- एक लेखक आपको कितने मोर्चों पर खड़ा नजर आता है फिर चाहे वह आर्थिक सामाजिक या फिर साहित्यिक नजर से आप देखें। आप उसे कैसे परिभाषित करते हैं?
विनोद जोशी:- जी बिल्कुल लेखक एक सामाजिक व्यक्ति है समाज के जितने भी दायरे होंगे उस पर सभी का असर होगा लेकिन लेखक की अपनी अपने आप में खुद में एक और हस्ती होती है । मैं समझता हूं कि लेखक को दूसरे लोग जानते हैं, वो वैसा होता नहीं लेखक अपने आप में खुद से संवाद करता है और इसके साथ उनका टकराव सदा ही चलता रहता है । कोई लेखक कोई साहित्य सृजक अपने आप में बहुत ही व्यथित हो सकता है लेकिन अपने बाहरी व्यवहार आनंदित भी दिख सकता है। उनका जो दायित्व है वह सामाजिक संदर्भ में और साहित्यिक संदर्भ में अलग-अलग है। कोई एक लेखक अकेला अपना प्रतिनिधित्व नहीं करता वह पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है और अपने साथ संवाद करके फिर ही कोई आकृति पाता है।
अरमान :-जिस वक्त आपने अपना साहित्य सृजन शुरू किया था आप युवा थे या फिर यूं कहूं उससे भी आपकी उम्र कम थी लेकिन आज एक लंबा वक्त हो चुका है आपको लिखते हुए और साहित्य समाज को देखते हुए आज युवा लेखन है कैसे देखते हैं अपने समय से आज तक जो आपने देखा।
विनोद जोशी:- जी बिल्कुल यह मुझे काफी आशा वाद लगता है और आज की जो युवा पीढ़ी लिख रही है इसे देखकर उन्हें जो उपलब्धियां प्राप्त हैं जैसे कि वह सोशल मीडिया पर लिख पाते हैं । कितनी सारी सुविधाएं हैं उनके पास में अपनी प्रस्तुति देने के लिए उन्हें ज्यादा ऑपच्यरुनिटीज मिल रही है । मुझे लगता है कि युवा काफी अच्छा काम कर रहा है। कह सकता हूं कि काम हो रहा है काफी अच्छा हो रहा है। भाषा को पहचानने के लिए आज की युवा पीढ़ी बहुत ही सक्षम दिख रही है। आज की युवा पीढ़ी की समझ और परिपक्वता के साथ तालमेल के साथ अपनी काबिलियत के साथ श्रेष्ठ देने का भरपूर प्रयास कर रही है ।
अरमान:- आपकी परिकल्पना में लेखनी कैसी होनी चाहिए?
विनोद जोशी:- जो भाव को परिष्कृत करें जो अपने आप को प्रतीत करवाएं कि जो लिखा गया वहीं अंतिम नहीं है। किसी भी लेखक को अपनी आखिरी रचना जो उन्होंने लिखी से भी आगे जाना है। ऐसा अगर वह सोचे तो मैं समझता हूं कि उसका जल्दी अंत नहीं आएगा और वह आगे से आगे बढ़ता रहेगा ।
और मैं यही कहना चाहता हूं भाषा एक ऐसी चीज है की अगर हम भाषा को इस तरह से अभिव्यक्त करें जिसमें सार्थकता समाहित हो और भाषा के माध्यम से हम भाव तक पहुंच पाए, और इंसान को ,प्रकृति को और सभी जो हमारे आसपास हैं उनको समझ पाए तो मुझे लगता है यह हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी । भाषा को जिस तरह से हम समझते हैं एक औजार के रूप में वैसी ना रहे इनमें से कुछ भाव प्रतीत हो जैसे कि दीया हम देखते हैं तो आप यह देखिए की दीया जो है वह महत्व नहीं रखता, उजाला महत्व रखता है। इसी तरह से हमें हमारा जो भाव भाव जगत उसके प्रति यही सर्वोपरि कामना होनी चाहिए प्रत्येक साहित्यकार की ।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार ।
विनोद जोशी - धन्यवाद
Dr.Vanita Manchanda
डॉ. वनिता मनचंदा
डॉ. वनिता एक कवियत्री , शिक्षाविद, अनुवादक और आलोचक हैं। उनके पास संगीत और पंजाबी में स्नातकोत्तर उपाधियाँ हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पंजाबी में अपना डॉक्टरेट शोध पूरा किया है। उन्होंने पंजाबी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ-साथ पंजाबी में एम.फिल. में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एम.ए. (पंजाबी) में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के लिए भाई वीर सिंह स्वर्ण पदक प्राप्त किया, और पंजाबी अकादमी से एम.ए. और पंजाबी अकादमी से एम.फिल. में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति तक दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में पंजाबी विभाग में व्याख्याता के रूप में काम किया। उन्होंने पीएचडी की उपाधि के लिए शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने भारत सरकार के संस्कृति विभाग और पंजाबी अकादमी, दिल्ली द्वारा वित्त पोषित दो शोध परियोजनाएँ पूरी की हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। उनके पास बड़ी संख्या में प्रकाशन भी हैं, जिनमें अनुवाद से लेकर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख, संपादित पुस्तकें और पत्रिकाएँ शामिल हैं। उनकी आलोचनात्मक और रचनात्मक दोनों तरह की पुस्तकों का प्रकाशन भी बड़ी संख्या में हुआ है। इसके अलावा, उन्होंने अखिल भारतीय रेडियो पर लगभग सत्तर रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, साथ ही जालन्धर और दिल्ली दूरदर्शन के लिए लगभग साठ टेलीविजन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। वे कई प्रतिष्ठित निकायों की सदस्य हैं जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब अनुसंधान केंद्र, भाई वीर सिंह साहित्य सदन नई दिल्ली, भाषा समिति और पंजाबी भाषा समिति, केके बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली, श्री गुरु ग्रंथ अनुसंधान केंद्र, गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब, नई दिल्ली, पंजाबी भाषा सलाहकार बोर्ड की संयोजक, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, गवर्निंग काउंसिल की सदस्य, पंजाबी अकादमी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बहुसांस्कृतिक और सिख अध्ययन संस्थान, पटियाला, पंजाबी साहित्य अकादमी, लुधियाना, पंजाबी भाषा के लिए पुस्तक सलाहकार समिति, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, आदि। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय द्वारा पंजाबी साहित्य में पुरस्कार के चयन के लिए विभिन्न समितियों में एक विशेषज्ञ के रूप में काम किया है। भारत सरकार ने उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर, पाकिस्तान में पंजाबी के एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विदेशी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया है। वह पंजाबी में युवा पुरस्कार का चयन करने के लिए साहित्य अकादमी की जूरी सदस्य भी रही हैं। पंजाबी में प्रकाशित सर्वाधिक उत्कृष्ट पुस्तक आदि। अकादमिक पुरस्कारों के अलावा, उन्हें 1998-99 में पंजाबी अकादमी द्वारा 'आलोचना पुरस्कार', 2003 में एबीआई (अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट इंक, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए) द्वारा वूमन ऑफ द ईयर अवार्ड, सीआईआईएल (केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान) द्वारा उड़िया पुस्तक, कविता फिर एकवर के अनुवाद के लिए भाषा भारती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। 2003-04 में मैसूर, 2006 में भाषा विभाग, पंजाब सरकार द्वारा पंजाबी शिरोमणि साहित्यकार सम्मान। 2007 में IAPAA (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पंजाबी ऑथर्स एंड आर्टिस्ट्स, इंक. कनाडा) द्वारा प्रोफेसर पियारा सिंह गिल और करम सिंह संधू मेमोरियल अंतर राष्ट्रीय शिरोमणि साहित्यकार पुरस्कार, वर्ष 2007-08 के लिए पंजाबी अकादमी, दिल्ली द्वारा "काल पहर घरियाँ" के लिए कविता पुरस्कार। ब्रैम्पटन में विश्व पंजाबी सम्मेलन के दौरान पंजाबी भाषा, साहित्य और संस्कृति में योगदान के लिए ब्रैमलिया गोर माल्टन को संसद द्वारा मान्यता (2009), साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार (2009), साहित्य अकादमी द्वारा काल पहर घरियाँ (कविता) के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। नई दिल्ली, वर्ष 2010 के लिए istejIndia, सुतिंदर सिंह
पंजाब साहित्य कला परिषद, मलेरकोटला, पंजाब द्वारा नूर यादगारी सम्मान (2011) ई
अरमान:- आपका एकेडमिक्स युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और बड़े ही जिम्मेदार पदों पर आपने अपनी सेवाएं दी और अब भी जारी है। साहित्य में आपकी रुचि किस तरह बनी शुरुआत कैसे हुई?
वनिता मनचंदा :- अगर मैं अपने साहित्य में रुचि की शुरुआत की बात करूं तो मुझे याद है कि जब मैं दसवीं पास की थी तो उसे दौरान में अपनी बुआ जी के पास में जाया करती थी उनसे बात हुआ करती थी और मेरी बुआ जी लेखिका थी अब तो फोत हो चुकी है। वह पंजाबी में लिखा करती थी कवित्री और कथा लेखिका थी। और उनकी भी इच्छा थी कि मैं लिखना शुरू करूं तो उसे छोटी सी उम्र में ही फिर धीरे-धीरे रुचि बनी शुरू हुई और मेरा जो लेखन है वह समाज को समर्पित है मैं जो देखती हूं वही लिखती हूं। और उसे छोटी सी उम्र में नहीं जब मैं कभी कोई ऐसी घटना देखी जिससे लोगों को तकलीफ होती तो वह कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ पहुंचा दी क्योंकि मेरे मन में यह था कि यह दुनिया काफी ज्यादा पीसफुल होनी चाहिए। तो उसके बाद में मैं कविता लिखनी शुरू की और वह छपी भी लेकिन मेरे जो परिवार के जो लोग थे वह काफी रूढ़िवादी थे। उनका यह मानना था कि सीधा साफ आप अपना सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए और यह जो कविताएं हैं या दूसरी चीज हैं उसमें ध्यान नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं था जब मैं मां को देखा करती तो यह था कि उन्होंने कभी इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं कि वह दिखने में काफी अच्छी हैं पैसे की किसी तरह की कोई कमी नहीं है लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बस वह एक चार दिवारी में कैद है और मैं वैसा होना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं बाबा जी के सामने हमेशा यही अरदास किया करती थी कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसी के चलते मैं मास्टर्स भी की और उसके अंदर मैंने संगीत क्लासिकल म्यूजिक फाइन आर्ट्स इस तरह की चीज मैंने अपने मास्टर्स में की और उसके अंदर मैंने अपना एकेडमिक्स पूरा किया। लेकिन घर में इस तरह की चीज पसंद नहीं की जाती थी तो वह कहते तो मैं सुन लिया करती थी ऊपर से मैं काफी कोमल थी लेकिन अंदर से मैं अपने आर्दश के लिए उतनी ही स्ट्रांग हूं। इन्हीं आदर्श की वजह से मैं अपने एकेडमिक्स में टॉप रहे और इसके बाद में मुझे इस घटना ने अपने वजूद का एहसास कराया कि तुम खुद भी बहुत कुछ कर सकते हो उसके बाद में मुझे इनविटेशन भी मिल गया कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज में ही जॉब कर सकती हो म्यूजिक प्रोफेसर के तौर पर। और यही चीज शादी के बाद बरकरार रही मैं अपने हस्बैंड से कहा कि मैं हर चीज को छोड़ सकती हूं लेकिन संगीत और सितार को नहीं उन्होंने भी सहयोग किया। लेकिन मेरी जो सासू मां थी उन्हें यह चीज कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी वह कहा करती थी कि यह जो सीटर है उसमें रुमाल बांधकर अपना बजाया करो और सिर्फ बाबा जी के कमरे में इसे किया करो तो उसके बाद में जब रुमाल बंदा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी ने तारों को रुमाल नहीं बांधा है मेरे गले में रुमाल बंदा है। इसी तरह से कला साहित्य संस्कृति के साथ मेरा रिश्ता बन रहा मैं काफी ज्यादा चीज जाली भी लेकिन कभी ने छोड़ा नहीं और इसी का नतीजा आज है कि मैं इसमें अपना काम कर रही हूं और लगातार करती रहूंगी।
अरमान:- आप खुद कथक और संगीत को समझते हैं पसंद करने वाले हैं और जहां तक मैं जानता हूं मैने खुद भी यह महसूस किया है अमृतसर चंडीगढ़ की तरफ की लड़कियों को कत्थक से एक अलग प्रेम है लेकिन जैसा आपके साथ भी हुआ रूढ़िवादी परिवार होने के कारण उन्हें वह स्पेस नहीं मिल पाता जिस कारण उनकी कला पर अंकुश लगता है इसे आप कैसे देखते हैं?
वनिता मनचंदा :- इस चीज के बारे में मैं आपको बता सकती हूं क्योंकि मैं इस पर अभी कुछ रिसर्च भी कर रही हूं की गुरु ग्रंथ साहिब की बात करो तब भी बुरा मानते हैं कीर्तन की प्रथम है क्लासिकल लेकिन नृत्य की नहीं। तो इस विषय के ऊपर मेरा रिसर्च वर्क अभी चल रहा है। इंडियन क्लासिकल के मां के चलिए जिस तरीके से हमारे देश के साउथ रीजन जो है भरतनाट्यम और उड़ीसा के ओडीसी मणिपुरी। जो नॉर्थ इंडिया है उसमें कत्थक ही लोग पसंद किया करते थे ज्यादातर यही वजह रही कि जो नॉर्थ इंडिया की लड़कियां उन्हें भी कत्थक से प्रेम था और वह यही सीखा करती थी। यह चीज हमें भी बहुत बाद में पता चली कि हम जो क्लासिकल सीखते हैं उसके अंदर सिर्फ कत्थक ही बड़े पैमाने पर क्यों सिखाया जाता है।
अरमान:- आपका कत्थक को लेकर यह विवरण वाकई में काफी सटीक बैठता है क्योंकि अगर हम आजादी से पहले पंजाब की बात करें तो वह जो संस्कृति हमें देखने को मिलती थी जिसमें गजल शायरी खैर वह आज भी हमें बड़े पैमाने पर वही चीज पंजाब में देखने को मिलती है।
वनिता मनचंदा :- जो उंडिवाइडेड पंजाब था उसके अंदर मुगल कलर भी बहुत ज्यादा था और जो म्यूजिक था वह हम उसे कह सकते हैं सांझ ही था बड़े गुलाम अली यहां भी गाए जाते थे और वहां भी। कि उसे वक्त भी अगर आप देखेंगे तो डिवीजन का तो कुछ ख्याल ही नहीं आया था आजादी से पहले एक आखिर तक हमें यह नहीं मालूम था कि बटवारा क्या इस तरीके से होगा। तो अगर आप उधर के पंजाब को भी देखेंगे तो कल्चरल बाउंड्रीज तो आपको आज भी नजर नहीं आएगी। से हम ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज कह सकते हैं।
अरमान : - यही चीज हमें बंगाल के साथ में भी देखने को मिलती है कि लोगों ने धर्म और संस्कृति को एक ही मान लिया था एक वक्त में जो कि बहुत गलत है।
अरमान :- आपके साहित्यिक लेखन की अगर बात करें तो वह ज्यादातर कविताओं और आलोचना पर है। और अगर हम आलोचना की बात करें तो इसे आज तक भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें यह एक नकारात्मक दृष्टिकोण ही महसूस होता।
वनिता मनचंदा :- इस विषय पर आपने बहुत अच्छी बात कही और जब हम भी सुना करते थे ज्यादातर जो आलोचक को तो उनकी जो शब्दावली हुआ करती थी वह इतनी ज्यादा कठोर हुआ करती थी कि समझ ही नहीं आता था। कहां से मैंने यह चीज भी समझी कि जिन लोगों को हमें अवेयर करना है समझता है अगर उन्हें हमारी भाषा ही समझ नहीं आएगी तो वह उसे चीज को ना तो समझ पाएंगे और ना ही कोई उन्हें बदलाव आएगा। तू ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसी चीज को क्रिएट करो कि यह जो सुनने वाले बैठे हैं वह आलोचना के जो तथ्य हैं उन्हें समझे उन्हें लगना चाहिए कि जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म वर्क किया जा रहा है या जो बात की जा रही है वह वाकई में उतनी मूल्यवान है क्योंकि अगर उन्हें वह बात समझ ना आए वह उसे खुद को जोड़ ही ना पाए तो वह किसी भी तरीके से उसे आलोचना को सकारात्मक रूप से नहीं लेंगे। आप आईडियोलॉजिकली स्ट्रांग रहिए लेकिन आपकी बात का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी बात सुनने के लिए बैठे उन्हें बीच में से उठकर जाने का मन ना हो उनका ध्यान आपके शब्दों पर रहे और आपके शब्दों के साथ जो आपका भाव है वह भी उन्हें समझ आना चाहिए। जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो जब क्लास टीचर आता है तो उसे क्लास खाली मिलती है। प्रोफेसर के आने से पहले ही बच्चे क्लास छोड़ देते हैं। लेकिन मैं अगर अपना अनुभव आपको बताऊं तो मेरे साथ में ऐसा नहीं होता था मेरे आने से पहले बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाया करते थे। स्टाइल मैंने क्रिएट किया कि बच्चे खुद ब खुद बैठा करते थे और बात सुन करते थे क्योंकि इस चीज में उन्हें भी एक लालसा रहती थी नई चीज जानने की समझने की जो कि आज के वक्त में खत्म होती जा रही है। और इस चीज के अंदर हम बच्चों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते या फिर हम यह कहें कि हमारे पास में ऑडियंस नहीं है। जब कोई कॉलेज के अंदर फेस्ट होता है कोई प्रोग्राम है तो वहां जब हजारों की संख्या में ऑडियंस जा सकती है तो आपके पास में क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक से बाहर आकर नया क्रिएटिव स्टाइल अपनाना होगा। इसी तरीके से हमें अपनी आलोचना का स्टाइल भी बदलना पड़ेगा यह मेरा मानना है। आज की तारीख में भी मैं अगर कोई हार्डकोर आलोचना कहीं पड़ी तो मैं यह समझता हूं कि अगर वह चीज मुझे समझ नहीं आ रही है तो वह एक आम व्यक्ति को कैसे समझ जाएगी। वहां से मैंने अपना स्टाइल बदल मैंने उसे वक्त भी यह देखा कि अगर एक मैंने अपनी उम्र ली है कि मुझे 40 साल की उम्र में उनके शब्द समझ नहीं आ रहे हैं तो 20 साल का नौजवानों उसे कैसे समझेगा। मेरा मानना इस तरह से है कि क्रिटिसिज्म भी हो जाए अगर कहीं जगह पर अप्रिशिएट करने की जरूरत होती है तो वहां उससे भी पीछे ना हटे। गुरुजी यह कहां करते थे कि जो नए लोग आते हैं उन्हें अप्रिशिएट करो नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा और जो बड़ा मेच्योर लेखक है वह अगर कोई बात बोलता है तो आप उसकी निंदा कीजिए उसको बताओ कि तू कहां गलत है। तो जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन्हें उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए मेरा भी ऐसा मानना है।
अरमान:- साहित्य अकादमी में भी आपने अपनी सेवाएं दी कन्वीनर के रूप में। साहित्य अकादमी के पुरस्कारों के लिए लेखक कहां तक जा सकता है?
वनिता मनचंदा :- पुरस्कारों की तो बात अलग है जिसमें लेखक अपना जोड़-तोड़ करता है लेकिन जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड मेंबर थे नहीं तक यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक महिला कन्वीनर कैसे बनी क्योंकि उनकी एगो इस मामले में इतनी हार्ड थी और इस बात को मधु जी भी अच्छे तरीके से जानते हैं। बात-बात पर वह लोग की एक कोशिश रहती थी तो वह कहते हैं ना कि हर बात पर रहते हो कि तू क्या है तो इस तरह का माहौल भी हमने झेला। और अपने सवाल किया इनमो के ऊपर तो फिर तो हर कोई यह चाहता है कि हमें इनाम मिले साहित्य अकादमी से चीज यह भी हमें मालूम है कि कई लोग इस तरह की चीज चलते हैं चलते आज भी हैं कि अपने लोगों को वह अवार्ड दे लेकिन मैं अपनी तरफ से यह साफ कर देना चाहती हूं कि मेरे रहते हुए कभी भी इस तरह की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। लोगों की शिकायत भी ऐसी रही कि अंडरसर्विंग लोगों को पुरस्कार मिल जाया करते हैं लेकिन मैं जब संभाला तो मेरी पूरी कोशिश यह रही कि ना तो मैं किसी भी तरह की सिफारिश को स्वीकार करूं और ना ही ऐसे लोगों को पुरस्कार दूं जो इसके लायक नहीं कोशिश यही थी कि लायक लोगों को आगे लाया जाए और उन्हें प्रोत्साहन किया जाए। मुझे लोग बताते भी हैं कि इन चीजों के चलते काफी अप्रिशिएट किया गया ग्राउंड पर भी मेरे काम को लोगों ने यह कहा की हमेशा मैडम ने सही लोगों को इनाम दिए। क्योंकि मेरे काम करने का तरीका इसमें यही था कि मैं सही लोगों तक इस चीज को पहुंचाओ और जब फैसला किया जाता था तब भी मेरी तरफ से सीनियर्स हो जाए युवा हो इस तरह के लोगों का नाम आगे दिया जाता तब जूरी मेंबर्स फैसला करते थे। और मैं कह सकती हूं कि मेरा टेन्योर पूरा इसी तरीके से गया और जितने भी इनाम साहित्य अकादमी द्वारा दिए गए वह बिल्कुल जायज थे। ना तो आपने बिल्कुल सही कहा अपने सवाल में अपने की लेखक कहां तक चला जाता है इन इनाम को पाने के लिए एक टैग अपने नाम के आगे लगाने के लिए साहित्य अकादमी का जो की बहुत ही ज्यादा गलत है वह लोग कुछ भी करने को तैयार हैं अकादमी अवार्ड के लिए।
अरमान:- बिल्कुल आपने एक ईमानदारी के साथ में अपना टेन्योर पूरा किया और यह जानकर और यह बात सुनकर खुशी भी होती है लेकिन सवाल यूं ही होते हैं अकादमियों के ऊपर की जो एक आम पाठक है वह भी कहीं ना कहीं यह बोल देता है की विज्ञप्ति निकालने से पहले ही इन लोगों में फैसला हो जाया करता है मैंने काफी लोगों से इस बारे में सवाल किया और लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द प्रदर्शित बने और सिर्फ लायक लोगों को इन अवॉर्ड के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए।
वनिता मनचंदा :- साहित्य अकादमी हो या फिर और कोई भी संस्था वहां रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं और यह देखने वाली बात है कि उन्हें वायलेट कौन कर रहा है और किस तरीके से काम किया जा रहा है जिम्मेदारी की बात है यह हर एक के ऊपर होती है। क्योंकि संस्था जो है वह रूल बनाकर आपको कॉन्फिडेंशियल मोड पर डाल सकती है। मुझे लगता है यह तो लोगों में सेंसिबिलिटी होनी चाहिए यह दोनों तरफ काम है कि लेखक जो है वह भी इस चीज की जिम्मेदारी के साथ काम करें और जो अकादमी के लोग हैं उन्हें भी इसी तरीके से काम करना चाहिए और करते भी हैं जैसे मैंने आपको अपना उदाहरण दिया और भी बहुत से निष्ठावान लोग हैं जो अपने काम को लग्न के साथ करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ निभाते भी हैं। इसीलिए मैं तो आपको कहती हूं कि मेरे जो ग्रुप के लोग थे वह मुझे इसी वजह से नाराज थे कि वह कई बार मुझे यह पूछा करते थे कि किसका नाम दिया है तो मैं उसे यही कहा करती थी क्या यह कॉन्फिडेंशियल है इसे जब ऑफीशियली रिलीज किया जाएगा तो यह आपको भी पता लग जाएगा तो यह चीज ऑफीशियली भी इसी तरीके से होने चाहिए और अनऑफिशियली भी इसी तरीके से होनी चाहिए। तो जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो लोगों की इगो भी हर्ट होती है। हम सारी बातें सरकार या समाज के ऊपर नहीं डाल सकते। व्यक्ति को सबसे पहले खुद के अंदर इन चीजों को देखना होगा और आंतरिक रूप से ताकतवर होना होगा।
अरमान:- और यह चीज लोगों के दिमाग में घर कर चुकी है इत्तेफाकन में अगर आपको अपना खुद का उदाहरण दूं तो 22 और 23 का जो सेशन था उसके अंदर इत्तेफाक से तीनों अकादमी की तरफ से मुझे यह सौभाग्य मिला तो वहां पर भी अंदर खेमे में कई जगह से सुनने को मिला कि लोगों को संदेह था इस चीज पर भी तो यह जो मानसिकता बन चुकी है सबसे बड़ी बात आपने सही कही कैसे व्यक्ति को खुद को अंदर से बदलाव करने की जरूरत है।
वनिता मनचंदा :- जब कभी भी किसी को इनाम मिलता है यह इस तरह की कोई खुशी होती है तो वाकई में ईमानदारी से अगर बात की जाए तो चांद घर के लोगों और करीबी ही होंगे जिन्हें आंतरिक खुशी होगी से बाकी सब इस तरह का दिखावा ही करते हैं। जब मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था तो मुझसे पूछा गया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है तब मेरा जवाब " किसी होकर कहा मुबारक और किसी के होके ने कहा मुबारक" खाने का मतलब यह है कि क्यों ने सिर्फ ऊपर ऊपरी मुबारकबाद दी भारी दिल के साथ में तो यह सब तो होता ही है यह हमने भी चीज महसूस की हुई है। असली खुशी की बात करें तो वह तो बहुत काम सिर्फ अपनों को ही होती है। के तो दिमाग में यह रहता है कि मुझे क्यों नहीं मिला। अभी से देखें तो साइकोलॉजी के लिए सही है कि हर किसी को खुद की चिंता खुद के बारे में ज्यादा पड़ी होती है और दूसरे को खुश देखकर व्यक्ति खुद ज्यादा खुश नहीं होता। लो प्रोफाइल को तो हर कोई देखता है लेकिन हाई प्रोफाइल जिसे हम कहें उसके दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं।
अरमान:- अनुवादक के तौर पर भी आपने अपना काम किया है और मेरे दोस्त हैं मौजूदा वक्त में यूके में रहते हैं और वह खुद भी अनुवादक हैं उनका मानना यह है कि लेखक से कम हम अनुवादक को नहीं कह सकते वह अपने आप में जब अनुवाद करता है तो वह अदीब के बराबर हो जाता है यह महत्व बताते हैं वह अनुवादक का। आपकी नजर में अनुवादक की क्या भूमिका रहती है?
वनिता मनचंदा :- से पहले तो यह बात है मैं कहूंगी सही है क्योंकि क्रिएटिविटी जितना ही यह काम हम देखने को मिलता है कि जब अनुवाद किया जाता है तो हम उसके मूल को ना भूल जाए। क्योंकि सबसे पहले जब आप किसी चीज का अनुवाद करते हैं तो आपको पहले खुद को वह अपने दिल में उतरना पड़ता है अब तो है बहुत ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे एकदम कम वक्त के अंदर हम ट्रांसलेट चीजों को कर सकते हैं लेकिन आज भी जब हम मैन्युअल इसको करते हैं तो हमें एक-एक चीज की बारीकी को देखना पड़ता है और उसके क्या मायने हैं और जब हम दूसरी भाषा में उसे अनुवाद कर रहे हैं उसे चीज का तो वहां उसे चीज को किस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं यह सबसे बड़ी चीज़ इसमें रहती है और जब हम उसे अनुवाद करें समझो कि खून में डूब कर ही कलम को स्याही भरनी होती है। बहुत है जिम्मेदारी का काम होता है अनुवादक का। उड़िया के लेखक रमाकांत जी जिनका कुछ वक्त पहले ही इंतकाल हुआ उनकी जो सबसे प्रसिद्ध और लंबी पोयम रचना है उसका मैं पंजाबी में अनुवाद किया। को पाठक ने इतना पसंद किया और एक लेखक का मेरे पास में फोन आया और वह कहते हैं कि मैं "श्री राधा" पढ़ी जो की कविता का शीर्षक है। वह कहते हैं कि उसके बाद में उसका प्रभाव से मैं पूरी एक नई किताब श्री कृष्णा पर लिख रहा हूं। तो यह एक अच्छे अनुवाद का प्रभाव होता है की लोग उसे इंस्पिरेशन लेते हैं। और मेरे दिमाग में यही चीज थी कि जो पंजाबी लेखक हैं और जब उनके पास में किसी दूसरी भाषा का काम आता है मलयालम बंगाली गुजराती राजस्थानी तो यह चीज देखने को मिली कि हम लोगों में कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज है जो हम शब्द भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी बहुत सी चीज एक सी मिलती है। तो जब हमारा पैनल बैठा तो उसमें कहीं हमने यह भी कहा कि हम तो राजस्थान को रेगिस्तान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमें यह समंदर की तरह खूबसूरत लगता है और कैमल को हम शिप मानते हैं। इस तरीके से जो एक्सचेंज आफ आईडियाज होते हैं शायरी के और जब हमारे मेटाफोर और कल्पना एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं तो मुझे लगता है यही हमारी असली देन होती है हमें हमारे साहित्य को। एक बार को हम कह सकते हैं कि विचार एक जैसे हो सकते हैं लेकिन साहित्य में जब हम इस्तेमाल करते हैं मेटाफोर्स उसके काम करने का तरीका वह जो काल्पनिक था जो हम इस्तेमाल करते हैं वह जब एक जैसी होने लगे जो अंदाज है बयानी है तब वह और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता ह।
अरमान :- यही खूबसूरती है भाषा और साहित्य संस्कृति की कि हम इन चीजों को जब एक दूसरे से साझा करते हैं तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम अलग-अलग हैं एक उदाहरण स और ह का भी हमें देखने को मिलता है। कि अगर हम इस तरफ की बात करें तो जो लोग हैं वह "स" की जगह "ह" का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं।
वनिता मनचंदा :- आपने यह बहुत सही बात कही की और पंजाब के तरफ भी को ऐसा देखने को मिलेगा कि "स" की जगह "ह" इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कि हम अगर पंजाब की बात करें तो एक वक्त में कितना बड़ा था पंजाब तो हमारी जो परंपरा है वह राजस्थान के साथ में भी काफी मिलती है। क्योंकि रफ एंड टू एनवायरमेंट में पहले बड़े हैं राजस्थान और पंजाब की अगर हम बात करें तो। दोनों ही रीजंस के लोगों ने एक्सट्रीम वेदर और बिहेवियर को महसूस किया है। राजस्थान के साथ में भी पंजाब का बहुत सिमिलर कलर देखने को मिलता है।
Madhu Acharya Ashawadi
मधु आचार्य आशावादी
राजनीति के कारण राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल पाई:- मधु आचार्य आशावादी
अरमान नदीम :- आज की तारीख में आप यानी मधु आचार्य आशावादी साहित्यिक दुनिया में बतौर रंगकर्मी ,कथाकार ,साहित्यकार एक जाना माना नाम है, पत्रकारिता में दिलचस्पी कैसे बनी ?
मधु आचार्य आशावादी :- जब मैंने ग्रेजुएशन करके आर ए एस की प्रारंभिक परीक्षा पास की तो उस पिताजी ने बुलाकर मुझसे कहा कि सरकारी नौकरी नहीं करनी और सरकारी नौकरी नहीं करने के पीछे उनका तर्क था कि सरकार का जो कर्मचारी होता है उसका दिमाग संकुचित हो जाता है । उनके पास साहित्य और शिक्षा का अनुभव था इसी के चलते उस दौर में मुझे भवानी शंकर शर्मा जी जैसे व्यक्ति मिले और वह मेरी अभिव्यक्ति की क्षमता को जानते थे , उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पत्रकारिता में आओ हालांकि पत्रकारिता करने के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं था लेकिन मैं शर्मा जी का बहुत सम्मान करता था तो उनके कहने पर मैंने पत्रकारिता चुनी । “राष्ट्रदूत”अखबार में काम शुरू किया उन्होंने वहां मुझसे कॉलम लिखवाए ।जब मैंने कॉलम लिखना शुरू किया , लिखते लिखते मेरी शब्दावली की बहुत समृद्ध हो गई तब उन्होंने मुझसे रिपोर्टिंग भी करवाई । मुझे पत्रकारिता में आनंद आने लगा क्योंकि मुझे लगने लगा कि इस माध्यम के जरिए में अपने मन की बात को लोगों तक पहुंचा सकता हू क्योंकि मेरी सोच का दायरा शुरू से ही प्रगतिशील रहा है और समाज के प्रति में शुरू से ही एक अलग जुड़ाव महसूस करता था । इसीलिए सामाजिक समस्याओं को उकेर कर उसे अभिव्यक्ति देकर लोगों तक पहुंचाने का माध्यम मुझे पत्रकारिता सबसे सर्वश्रेष्ठ लगा । मेरा मन उसमें रमता गया । उसके बाद दूसरे अखबारों के लिए काम किया, भास्कर में एडिटर तक पहुंचा बाद में मुझे धीरे-धीरे यह महसूस होने लगा कि अखबारों की दुनिया बदल सी गई है क्योंकि पहले अखबार एक मिशन हुआ करता था आजादी से पहले और उसके बाद तक लेकिन बाद में यह दुनिया पूरी तरीके से व्यावसायिक हो गई तब मुझे लगा केवल न्यूज़ देना पर्याप्त नहीं है। एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक लड़की जिसका आई आई टी में चयन हुआ बीकानेर की ही थी वह दिल्ली गई और हॉस्टल में तीसरे दिन ही उसने सुसाइड कर लिया। खबर तो इतनी भर ही थी की एक बच्ची थी जिसने दिल्ली में जाकर सुसाइड की लेकिन मेरा इंटरेस्ट जगा की सुसाइड करने का कारण क्या था जबकि वह एक संपन्न घर की बच्ची थी । तब मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड पता किया तो पता चला कि उसका किसी लड़के से प्रेम था वह लड़का शेड्यूल कास्ट का था । समाज की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी जाति थी और उसके घर वाले किसी भी सूरत में उस संबंध को स्वीकार नहीं करते । वह लड़का भी आईआईटी में सिलेक्ट हुआ था , लड़की ने कहा कि आप भी मेरे साथ दिल्ली आइए लेकिन उस बच्चे ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह समाज के यथार्थ को जानता था फिर उसने बेंगलुरु को चुना उसके साथ दिल्ली नहीं आया तो इस कारण से उसने आत्महत्या की थी। अब यह बात अखबार का हिस्सा तो हो नहीं सकती थी तब मैंने उसे लेकर एक कहानी लिखी वहां से मुझे लगा न्यूज़ के पीछे की जो कथा होती है उसको अखबार में नहीं दिखाया जा सकता उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम केवल और केवल साहित्य हो सकता है फिर मेरी रुचि धीरे-धीरे साहित्य की तरफ भी बढ़ गई तो यूं मैं पत्रकारिता और पत्रकारिता से साहित्य का तरफ हुआ।
अरमान नदीम :- वाकई यह किस्सा बहुत मार्मिक है जो बाद में आपकी पहली रचना भी बना । पहली किताब कैसे आई?
आशावादी :- सद्दीक साहब जो बीकानेर के कवि थे मैं उनकी कविताओं से बहुत प्रभावित था मैं नाटक किया करता था रंगकर्मी था और डायरेक्शन भी किया करता था उनकी कविताओं में मुझे गजब का ड्रामा लगता था जैसे उनकी बड़ी पॉपुलर कविता है “ “
"सामने है ढाल थारे लारली हवा, बेगा चालो जीमो बेटा चिकना कवा "
यह उस वक्त सत्ता के तंत्र पर एकदम फिट। उनकी कविताओं की एक किताब थी जो कि उनकी पहली कृति थी अंतसतास उनकी जिसके लोकार्पण में भी मैं था इस शब्द का मतलब होता है भीतर की बड़त ,भीतर की ज्योत तो मैंने उन कविताओं को नाटकीय मोड़ दिया उनकी कई कविताओं को सेलेक्ट किया। मैंने उसे नाम दिया अंतस उजास - आदमी के भीतर का उजास जो राजस्थानी में पहली किताब छपी थी मेरी अंतस उजास ।
अरमान नदीम :- हम लगातार देखते हैं वक्त वक्त पर राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर आवाज उठती है लेकिन मुझे लगता है कि यह केवल फाइलों तक ही सीमित है वह इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही ?
आशावादी :- दरअसल यह पूरा का पूरा गेम पॉलिटिक्स का है राजनीति के कारण राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल पाई जब भाषाओं की बात हो रही थी देश में संविधान बन रहा था उस समय हर प्रदेश में एक भाषा की मांग थी जिसे वहां की लोकल लैंग्वेज बनाया जाए। क्योंकि उस वक्त हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित किया जाना था तो यह सहमति हुई कि हम हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और राजस्थानी की बात उसमें पिछड़ सी गई और उसके बाद राजस्थानी भाषा को लेकर लोगों ने जब-जब भी आवाज उठाई तो हिंदी हावी रही । हालांकि कई लोग इसे राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है यह राज्य भाषा है । लेकिन राजस्थानी अपने हक के लिए लड़ना शुरू हुए आज से लगभग छह दशक पहले। लेकिन सत्ता झुकती है वोटो के वजन से किसी भी दल की सत्ता हो जब तक उसमें वोट का दबाव नहीं पड़ता वह काम नहीं करती और आज भी राजस्थानी भाषा का आंदोलन कमजोर इसलिए है कि लोग सोचते हैं कि यह कोई साहित्यकारों का आंदोलन होगा लेकिन अगर भाषा को मान्यता मिलती है तो जनता को फायदा है ये जन आंदोलन होना चाहिए जैसे कोई आज पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो परीक्षा में 20% सवाल पंजाबी और पंजाब से रिलेटेड आते हैं और उसका जवाब केवल और केवल पंजाबी दे सकता है और अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलती है तो यहां भी ऐसा ही होगा और उन सवालों के जवाब केवल राजस्थानी ही दे सकता है लेकिन यह बात लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। जबकि साहित्यकारो को पुरस्कार भी मिल रहे हैं किताबें भी छप रही है उनको क्या मिलेगा मिलना तो जनता को है। यहां के युवाओं का हक है यह। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सर्वे है जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक हैं वह इतने बड़े आविष्कार क्यों कर पाए क्योंकि उनकी प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में हुई थी कि उनका दिमाग के विकास की गति बड़ी तीव्र गति से होती है अगर देखा जाए तो आज राजस्थान दूसरे राज्यों के लिए चारागाह बन गया है हिंदी प्रदेश के लोग यहां आते हैं नौकरी करते हैं।
अरमान नदीम :- आपने कहा कि यह एक जन आंदोलन होना चाहिए क्योंकि इससे सीधा जनता का फायदा है। आपने देखा होगा कि 1960 के दशक में ऐसे आंदोलन देखे गए जिसमें लोगों की जान तक चली गई अपनी भाषा के लिए लेकिन मैं किसी की भी जान की क्षति और उग्रवाद का समर्थन नहीं करता हूं लेकिन एक जो जोश होना चाहिए जनता में वह दिखाई नहीं पड़ता है भाषा को लेकर खास करके राजस्थान के युवाओं में।
आशावादी :- सबसे बड़ी बात यही है कि साहित्यकार इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वह जनता को समझा ही नहीं पाए कि यह आंदोलन जनता का आंदोलन है यह हमारा आंदोलन नहीं है यह आपके हित के लिए है और बीच-बीच में राजनीतिक दल जिस तरह का व्यवहार करते हैं उससे जनता और भटक जाती है। आपने देखा होगा कि बीच में एक आंदोलन चला कि राजस्थानी भाषा को दूसरी राजभाषा बना दिया जाए उससे हक तो मिलेगा नहीं नौकरी का। क्योंकि पहली भाषा तो हिंदी ही रहेगी। तो यूं भटकाते हैं ।एक यह भी कारण है राजनीतिक भटकाव से जनता इससे जुड़ नहीं पाई। बड़ा अफसोस होता है कि 25 तो लोकसभा के सांसद 10 सदस्य सभा के सांसद और 200 विधायक जब वोट मांगने जाते हैं तो वह मातृभाषा में बात करते हैं राजस्थानी में बात करते हैं और उनके भाषण की शुरुआत ही राम-राम सा के साथ होती है लेकिन जब यह लोग संसद, विधानसभा, राज्यसभा में पहुंचते हैं तो वहां राजस्थानी भाषा की वकालत नहीं करते।
अरमान नदीम :- एक बात और भी है जब बच्चा अपने शुरुआती दिनों में होता है जिस परिवेश में होता है आप जो उसे सिखाओगे वह सीखेगा कई प्राइवेट स्कूलों में तो पनिशमेंट भी दी गई थी कि अगर तुम राजस्थानी बोलते हो तो हम तुम्हें पनिश करेंगे ।तुम हिंदी बोलो या अंग्रेजी में बात करो और छोटे बच्चों के दिमाग में शुरू से यही भरा जाता है।
आशावादी :- मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता हूं लेकिन मेरी मातृभाषा तो राजस्थानी है इसे मैं नकार भी नहीं सकता क्योंकि और बच्चों को कन्फ्यूजन यूं पैदा होता है कि घर में तो उसे कहा जाता है कि राजस्थानी में बात करो और स्कूल में उसे हिंदी या अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। मैं ग्रीक का उदाहरण बताता हूं वहां के लोगों ने एक बार यह तय किया कि हम यहां से स्वर्ग तक एक मार्ग बनाएंगे जिससे हम सीधा स्वर्ग तक पहुंच सके । मीनार बनानी शुरू की तो ऊपर बैठे ईश्वर ने देखा कि यह क्या हो रहा है अगर इन्होंने स्वर्ग तक मीनार बना ली तो यह तो बहुत बड़ा हाहाकार हो जाएगा तो देखा की इन्हें विभाजित कैसे किया जाए और विभाजित करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई थी वह यह थी कि इनकी भाषा छीन लिया जाए तो यह आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे और अगर बात नहीं कर पाएंगे तो एकजुट नहीं रह पाएंगे इनकी कल्चर विकसित नहीं होगी और यही बात यहां पर अंग्रेजों ने किया है भारत को जितना नुकसान अंग्रेजों ने पहुंचाया उतना किसी ने नहीं । उन्होंने ही भाषा के आधार पर भारत को विभाजित किया था । हम कहते हैं हमारी अनेक भाषाएं हैं अनेक संस्कृति है लेकिन उसके बावजूद भी हम एक हैं वह राष्ट्रीयता की भावना हमें एक रखी हुई है लेकिन भाषा के बूते पर उन्होंने हमें विभाजित कर दिया। इसीलिए भाषा होती है तो किसी भी प्रदेश की संस्कृति है। इसीलिए मान्यता की डिमांड आपकी अस्मिता से जुड़ी है। जैसा की तुमने कहा कि बच्चों के दिमाग में प्रेशर होता है लेकिन अब नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में की जाए। यही तो है साहित्यकारों का डर भी यही है अगर भाषा के साथ इसी तरह का बर्ताव होता गया तो कहीं एक दिन अनेक भाषाओं की तरह राजस्थानी भाषा भी विलुप्त ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा कल्चर खराब हो जाएगा।
अरमान नदीम :- जी बिल्कुल अपने न्याय संगत बात कही है लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अपनी भाषा का सम्मान करना सही है बहुत ही बेहतर बात है लेकिन क्या उसके लिए दूसरी भाषा का अपमान करना सही है क्योंकि अंततोगत्वा भाषा भाव प्रकट करने का एक माध्यम ही तो है जैसा कि आपने ग्रीक का उदाहरण देते हुए कहा।
आशावादी :- किसी दूसरी भाषा का विरोध नहीं हो रहा है मेरी दादी मेरी मां जिस जुबान में बोलते हैं मैं उसका सम्मान ना करूं तो यह तो खुद के अस्तित्व पे सवाल करने की बात हो गई अपनी भाषा पर गर्व करो दूसरी भाषाओं का सम्मान करो और दूसरी भाषाओं का अपमान करना तो अपनी भाषा का अपमान करने जैसा ही है।
अरमान नदीम : जी सही कहा आपने लेकिन हमने खुले मंचों से ऐसे दृश्य देखे है कि कि जहां कुछ टेंशन का माहौल बन जाता है अकादमी के प्रोग्रामों में भी - उसे आप कैसे देखते हैं?
आशावादी:- बिल्कुल ही गलत है और मैं तथ्य परख बात कह रहा हूं जिसके डॉक्यूमेंट मौजूद है आप मुझे बता दो हिंदी अगर किसी प्रदेश की भाषा हो तो हिंदी का कोई प्रदेश नहीं है अगर लोक नहीं है प्रदेश नहीं है अगर उसका कोई कल्चर नहीं है इसका मतलब होता है कि वह भाषा होती है कृत्रिम भाषा। हिंदी को तो बनाया गया है हिंदी ओरिजिनल भाषा नहीं है तो उसका अपमान नहीं है। लेकिन वह भाषा यह कहे कि राजस्थानी भोजपुरी या बुंदेलखंडी हमारी बोलियां है आप इसे एक भाषा के रूप में मान्यता तो दो यह हिंदी इन सबसे मिलकर बनी है इन सब भाषाओं से। लेकिन मंचों पर क्या होता है वह कहते हैं कि इससे हिंदी कमजोर होगी लेकिन इससे हिंदी कमजोर नहीं होगी इससे हिंदी सबल होगी अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दोगे तो उससे हिंदी को मजबूती मिलेगी और यह कहना की हिंदी का विरोध करती है क्षेत्रीय भाषाएं तो यह अनुचित है। और अगर ऐसा कोई करता है तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। हम तो हमारी भाषा की बात करते हैं हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए जो हमारी अस्मिता की जरूरत है जो हमारी संस्कृति को बचाने की जरूरत है इसमें दूसरी किसी भाषा का अपमान नहीं है हम तो कहते हैं भोजपुरी को भी मान्यता मिले ,हमें कोई दिक्कत नहीं है और आप यह देखिए की राजस्थानी को नेपाल जैसे देश में मान्यता है लेकिन हमारे राजस्थान में नहीं है।
अरमान नदीम :- जी बिल्कुल यह बात यह भी कहना चाहूंगा कि जब मैंने लोगों से बातचीत की तो उनमें एक गुस्सा भी नजर आया उनका कहना है कि जो लोग इन चीजों का फेस बने हुए हैं उन्हें असल में कोई मतलब नहीं और वह खुले शब्दों में यह कहते हैं कि यह लोग ढोंग कर रहे हैं यह सिर्फ अखबार में आना चाहते हैं और इससे ज्यादा इनका कोई उद्देश्य नहीं है तो कई लोगों के दिमाग में यह चीज भी है।
आशावादी:- अगर भाषा के नाम पर कोई व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहा है तो वह तो पूरी तरीके से निंदनीय हैं उसकी आलोचना होनी चाहिए और भाषा का प्रेम खुद का प्रेम है मेरी नजर में अगर उसे भाषा के साथ हम कोई छद्दम रूप रखकर और इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हम बहुत बड़ा मानवीय अपराध करते हैं इसीलिए जो भी इस तरह की की चीज करते हैं मैं तो खुले शब्दों में उनकी निंदा करता हूं।
अरमान नदीम : अपने जैसा कहा की राजस्थानी को राजनीति के कारण मान्यता नहीं मिल पाए यानी कि एक राजनीतिक दखल रहा शुरू से ही तो यह हम देखते हैं कि यह तो हर एक संस्था के ऊपर है । हर एक संस्था का राजनीतिक करण हो रहा है ।आज की तारीख में अगर हम देखें साहित्य अकादमियों के अध्यक्ष किस तरीके से बदले जाते हैं यह किसी से छुपा नहीं है और यह तो राजस्थान में चलान है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस की सरकार आती है 5 साल में और वह उसी हिसाब से साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बदलते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ही आती है कि इसका सीधा-सीधा असर हमें लेखन पर देखने को मिलता है
आशावादी - यह बिल्कुल व्यावहारिक और सही बात कही है प्रैक्टिकल यही है। भारत में राज्यों की अकादमी पूरी की पूरी तरह सरकार की गिरफ्त में है इस देश में केवल साहित्य अकादमी नई दिल्ली स्वतंत्र बॉडी है जिसमें सरकार की तरफ से मनोनीत नहीं होता। वहां पर साहित्यकार ही अपना अध्यक्ष खुद चुनते हैं पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जब वह साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की सीट पर बैठते थे, तो कहते की भारत के किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि वह साहित्य अकादमी के प्रस्ताव को रोक दे। यह बोल्डनेस जवाहरलाल नेहरू में थी जिस कारण से अकादमी की स्वायत्तता अब तक बची हुई है। आपने गौर से देखा हो तो मैं अपने राजस्थान की ही बात करता हूं अभी भाजपा का शासन है 1 साल बीत चुका है अध्यक्ष नहीं है पहले शासन कांग्रेस का था उसने डेढ़ साल के लिए अध्यक्ष बनाया उससे पहले जो भाजपा का शासन था तो 5 साल तक कोई अध्यक्ष नहीं था राज्यों की अकादमियों पर सरकार का कब्जा होना साहित्य का अहित होना है क्योंकि इससे सीधे-सीधे साहित्यकार दो फाड़ में बट जाते हैं। अगर कोई साहित्य लिखने के लिए आता है तो उससे पहले यह तय करना होता है कि वह अमीर के साथ है या गरीब के साथ है ,वह सत्ता के साथ है या जनता के साथ है वह सही के साथ है या गलत के साथ है यही तय करके कोई साहित्यकार लिखना शुरू करते हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर कोई प्रगतिशील सोच नहीं रखता तो वह साहित्यकार है ही नहीं क्योंकि हमेशा से ही साहित्य तो सत्ता के विपक्ष में खड़ा होता है क्योंकि सत्ता का विपक्ष होता है साहित्य और सत्ता से मेरा मतलब है राज सत्ता से होता है किसी एक दल की सत्ता से नहीं क्योंकि सत्ता का मूल व्यवहार शोषण होता है शोषण का प्रतिकार अपने लिटरेचर के माध्यम से करना होता है धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति पिछले 10-15 साल में ज्यादा बढ़ी है जैसे ही जिस दल का शासन आता है लोग उस दल की विचारधारा को अडॉप्ट करने लगते हैं खुद को उनके जैसे हिसाब से दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं जो सत्ता की चाटुकारिता के लिए सत्ता के विचारों के लिए अपने साहित्य का सृजन करता है मैं उसे किसी सूरत साहित्य मानता ही नहीं।
अरमान नदीम :- आपने कहा लोग बदल रहे हैं और नजर में भी आ रहा है और यह हकीकत है कि लोग चाटुकारिता में अपना संपूर्ण देने की कोशिश में लगे हैं और जिसमें आज की पत्रकारिता अछूती नहीं रही तो फर्क किस तरीके से आपको दिख रहा है।
आशावादी:- मुझे इतने साल हुए पत्रकारिता करते हुए और मैंने आरंभ में ही कहा भाई आपको कि आज की पत्रकारिता व्यवसाय से ग्रसित हो चुकी है। और ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो आज से पहले कभी सुनने को ना मिले। गोदी मीडिया क्या होता है पहले होती थी पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता अभी एक नया फार्मूला आ गया गोदी मीडिया और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है मैंने खुद ने 28 साल पत्रकारिता है ,पत्रकारिता के भी मायने बदल गए पत्रकारिता मिशन नहीं रहा पत्रकारिता व्यवसाय हो गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जिस तरीके से आज देख रहे हैं वह व्यवसाय के भी कुछ सिद्धांत होते हैं और कई लोग उन सिद्धांतों का भी पालन नहीं कर रहे हैं तभी तो गोदी मीडिया जैसे शब्दों का जन्म होता है।
अरमान नदीम:- युवा लेखन को आप कैसे देखते हैं ?
आशावादी:- युवा लेखन की स्थिति में बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं मानता संतोषजनक इसलिए नहीं मानता क्योंकि हम जब साहित्य का सृजन करते हैं तो हमारे पास एक प्रक्रिया है साहित्य की हमारे कंधे पर तो अतीत होना चाहिए और जी हम वर्तमान में होने चाहिए और नजर भविष्य पर होनी चाहिए लेकिन आज का जो हमारा युवा है उसने वर्तमान ही जीवन मान लिया है तो इसलिए ना तो उसकी नजर भूत पर है ना भविष्य पर। साहित्य तो भूत के बिना वर्तमान को जिंदा रख नहीं सकता और अगर उसकी नजर भविष्य पर नहीं होगी तो वर्तमान में लिखा हुआ वर्तमान में ही मर जाएगा ।
अरमान नदीम :- आज के दौर में देखा जाता है कि दिखावा बहुत हो चुका है तो क्या अदबी दुनिया में भी दिखावा बड़ा है?
आशावादी:- अदबी दुनिया तो पूरी की पूरी दिखावे की बन गई है। लोग साहित्यकार बनना नहीं चाहते साहित्यकार दिखाना चाहते हैं क्योंकि साहित्य को भी उन्होंने ग्लैमर बना दिया । क्योंकि इससे उनके बुद्धिजीवी होने का आभास होता है समाज बुद्धिजीवी का सम्मान करता है। उन्हें लगता है कि यह हमसे कुछ ज्यादा जानता है और आत्म प्रशंसा और खुद की तारीफ सुनना तो सबको अच्छा लगता है और इसी के चलते साहित्य में भी एक शब्द पैदा हुआ घोस्ट राइटिंग आपने देखा होगा कि आजकल बड़े-बड़े अधिकारी लेखक बन गए बड़े-बड़े नेता लेखक बन गए उनको लेखक बनने का यह काम घोस्ट राइटिंग ने किया है। साहित्य में दिखावा मेरी नजर में सबसे बड़ी बुराई है क्योंकि दिखावे में साहित्यकार दिखता है साहित्य नहीं दिखता। जबकि मूल रूप से समाज को साहित्य दिखना चाहिए साहित्यकार उसके बाद।
अरमान नदीम :- आज के वक्त में आप साहित्यकारों को या फिर जो नई जनरेशन है उसको क्या सलाह देंगे। यूं कहें कि आशावादी के साहित्यिक अरमान क्या है?
मधु आचार्य आशावादी :- मेरी नजर में हर व्यक्ति संवेदनशील होता है संवेदना किसी भी साहित्यकार की पहली अनिवार्यता होती है. इसकी भी एक यात्रा है अगर आप संवेदनशील हो तो संवेदनशील होने से आपके भीतर भाव पैदा होते हैं आपके पास शब्द का संस्कार आता है और जब शब्द का संस्कार आता है तो आपका एक विचार बनता है और वही विचार साहित्य के रूप में समाज के सामने आता। मैं एक उदाहरण और देता हूं कि मैं और मेरा व्यापारी मित्र हम जा रहे हैं और हमें रास्ते में एक बच्ची मिलती है भीख मांगते हुए , हाथ फैलती है , मेरा व्यापारी मित्र उसे देखकर 20-50 रुपए दे देता है लेकिन एक साहित्यकार उसे देखता रहेगा वह देगा कुछ नहीं लेकिन वह जाकर उसे पर या तो कविता लिख देगा या उस पर कहानी लिखेगा।
अरमान नदीम - "शब्द संवाद" के लिए कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार ।
Dr.Diksha Tiwari
डॉ. दीक्षा तिवारी
बदलाव की शुरुआत खुद से कीजिए । डॉ. दीक्षा तिवारी
छत्तीसगढ़ की समाजसेविका और इतिहास विज्ञ डॉक्टर दीक्षा तिवारी से खास बातचीत ।
परिचय
छत्तीसगढ़ की रहने वाली डॉ. दीक्षा तिवारी आम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने की कोशिश में एक एनजीओ अर्पण एम्पावरिंग से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दीक्षा ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे स्वास्थ्य की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में महिलाओं को जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर ब्लॉग्स लिखती हैं।
अरमान नदीम :- अपने बारे में कुछ बताइए
डॉ. दीक्षा तिवारी :- मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा तिवारी है हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं । मैं एक डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन। मैं पब्लिक हेल्थ में काम कर रही हूं । मैं हेल्थ टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने में मदद कर रही हूं और साथ ही में एक एनजीओ चलाती हूं अर्पण इंपायरिंग । इतिहास में काफी रुचि है जिसके चलते सोशल मीडिया पर हिस्ट्री छत्तीसगढ़ नाम से एक पेज भी है जिसमे कोशिश रहती है की छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में लोगों जानकारी दी जाये ।
अरमान नदीम :- सिर्फ़ आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में रुचि है या बाकी कालखंड में भी आप सक्रिय तौर अध्ययन करते हैं?
डॉ. दीक्षा तिवारी :- ऐसा नहीं है ,मुझे सभी पीरियड की हिस्ट्री पढ़ना काफी पसंद है लेकिन छत्तीसगढ़ का इतिहास सबसे ज्यादा , स्वाभाविक रूप से इसलिए पसंद है क्योंकि मैं यहां की रहने वाली हूं और छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में नॉर्मल कन्वर्सेशन में कभी बात नहीं होती जिसे हम मेन स्ट्रीम इतिहास का हिस्सा कह सकें उस तरीके से इस पर चर्चा नहीं की जाती इसलिए मेरी रुचि इसमें ज्यादा रहती है कि मैं अपने स्टेट के इतिहास के बारे में जानू और लोगों को भी इसके बारे में बताऊं तो यही सबसे बड़ा कारण है की छत्तीसगढ़ के इतिहास पर शोध कार्य करती हूं
अरमान नदीम :- छत्तीसगढ़ के इतिहास पर इतनी खास चर्चा नहीं की जाती और किताबों में ,पाठ्यक्रम में उल्लेख कम है ।और मैंने पढ़ा है की पहले इसका नाम दक्षिण कौशल हुआ करता था
तो दक्षिण कौशल के बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए की इसकी शुरुआत कैसे हुई और छत्तीसगढ़ नाम तक का सफर कैसे तय हुआ?
डॉ. दीक्षा तिवारी :- दक्षिण कौशल असल में सेंट्रल इंडिया का ऐतिहासिक हिस्सा है जिसमें आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा और उड़ीसा का भी शामिल था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब आप इसे देखेंगे तो इसका उल्लेख पौराणिक काल, महाभारत में इसका जिक्र आपको मिलता है ।इसे भगवान श्री राम का ननिहाल भी कहा जाता हैं शिवाकू वंश उन्होंने काफी वक्त तक इस क्षेत्र में राज किया उसके बाद में छेदि राजवंश यहां एक बड़े राजवंश के तौर पर उभरा सातवाहन साम्राज्य ने यहां अपना विस्तार किया गुप्ता एंपायर यहां बहुत फला फूला मौर्य साम्राज्य यहां शक्तिशाली साम्राज्य में से एक रहा और इसी कालखंड के बाद धीरे-धीरे इसका नाम बदला और यह दक्षिण कौशल से छत्तीसगढ़ बन गया।
अरमान नदीम :- बहुत ही संक्षिप्त में गहरी जानकारी दी आपने । आप डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य संबंधी चीजों से जुड़े हुए हैं एक सबसे बड़ी समस्या जो आज के युवा पीढ़ी में हमें नजर आती है अवसाद की समस्या - आप इसे कैसे देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरीके से असर पड़ता है और वह गंभीर रूप किस प्रकार ले लेता है इससे बचने के लिए आप क्या सुझाव देंगे और जागरूकता हम इस माहौल में कैसे फैला सकते हैं?
डॉ. दीक्षा तिवारी :- मैं इस बारे में आपको बेहतर तरीके से बता सकती हूं क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ और इन्हीं चीजों से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हूं मेंटल हेल्थ के मसलों से यानी की जो समस्या आम जन में सबसे ज़्यादा नज़र आती है। आज के दौर में आमतौर पर जो जनरेशन जेड , उसमें यह सबसे ज्यादा देखने को मिलती है । बिल्कुल यह एक गंभीर बीमारी है और यह असल में होती है डिप्रेशन लेकिन इसका मिसयूज भी किया जाता है । लोग कुछ से परेशान होते हैं या लो फील करते हैं तो उसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं । काम की बेचैनी या फिर कोई रिजल्ट आने से पहले की बेचैनी वह उसे भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं । आपने सुना होगा कि हमें साफ-सफाई का शौक है तो हमें ओसीडी है की इतनी आसानी से आज के दौर में लोग मेडिकल टर्म को अपने आम जीवन में इस्तेमाल करने लगे हैं कि वह उसे बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज कर चुके हैं की डिप्रेशन का मरीज हर चौथा व्यक्ति मिल ही जाएगा । मुझे लगता है की सबसे पहले तो इन सब चीजों को लेकर बात करने की जरूरत है। इनमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है । कहने का मतलब यह है कि लोगों को पता ही नहीं कि वह डिप्रेशन में है या नहीं । जितने लोगों से हम सुनते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है तो हो सकता है असल में इतने लोगों को डिप्रेशन हो भी नहीं । लोग इस पर काम कर रहे हैं लगातार काम कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है मैं फिर यही कहूंगी की लोगों को जागरूकता करने की जरूरत है और उन्हें असल मतलब इसका समझने की जरूरत है जिसे आप डिप्रेशन समझ रहे हैं वह डिप्रेशन नहीं । सिंपल स्टेज आफ स्ट्रेस है यानी की कुछ ज्यादा काम कर लेने से या फिर ज्यादा सोचने से भी हो जाता है।
अरमान नदीम - जी बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों को मतलब ही पता नहीं है कि डिप्रेशन असल में चीज क्या होती है लेकिन हम इसे किस तरीके से शुरू करते हैं या इसे सही ढंग से समझाने का तरीका क्या है?
डॉ. दीक्षा तिवारी :- देखिए यह शुरू कैसे होता है एक यह भी जानने की हमें जरूरत है मैं आपको उदाहरण दूंगी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का। मान के चलिए कोई व्यक्ति उसे कंज्यूम कर रहा है और उसका एल्गोरिदम बन गया है मेंटल हेल्थ को लेकर या डिप्रेशन को लेकर तो एक चीज वह भी वहां से शुरू होती है कि उसे सजेशन जिस तरीके के लगातार मिल रहे हैं तो उसकी सोच भी वही डाइवर्ट होती चली जाती है। अगर आपको लगता है क्या आपको वाकई में मेजर प्रॉब्लम्स है तो आप सर्टिफाइड मनोवैज्ञानिक के पास में जाइए जो वाकई में आपकी प्रॉब्लम को समझ कर उसे हिसाब से आपके साथ ट्रीटमेंट करेगा ।
अरमान नदीम- आपको आज की तारीख में सबसे बेहतरीन नीति क्या लगती है स्वास्थ्य को लेकर फिर चाहे हम राज्य सरकार की बात कर सकते हैं या केंद्र सरकार की बात कर सकते हैं सबसे उम्दा जिसे आपकी नजर में एक डॉक्टर की नजर में कहा जा सके।
जैसे अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इससे बड़े-बड़े ऑपरेशंस होते हैं तो वह उसके अंदर कुछ हद तक काम करते हैं और या फिर पूरी तरीके से गरीबों को फ्री में इलाज देते हैं तो इस तरीके की कोई स्कीम जो आपको लगता है कि यह है बेहतर है और इसे दूसरे राज्यों को भी अपनानी चाहिए।
डॉ. दीक्षा तिवारी :- बिल्कुल आपने सही कहा कि सरकारों की नीति वेलफेयर पर होती है और हम वेलफेयर एक सिस्टम से ही जुड़े हुए हैं। हमारा इकोनॉमिक्स पूरा वेलफेयर पर है एक नीति जो हमारी नजर में छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर है , छत्तीसगढ़ में बहुत कम था अस्पताल में जाकर डिलीवरी करवाने वाला तो इसके चलते डेथ हो जाया करती थी जिसे मेडिकल थ्रू बचाया जा सकता था । लेकिन वह जान का नुकसान हुआ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमें लगातार देखने को मिला तो इसी के चलते छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक नीति लॉन्च की महतारी एक्सप्रेस महतारी का मतलब छत्तीसगढ़ में मन से रिलेट होता है तो महतारी एक्सप्रेस शुरू हुआ था इसमें फ्री में महिला को अस्पताल तक ले जाया जाता था उसके द्वारा डिलीवरी कराई जाती थी तो इस तरह की छोटी-छोटी पहल है जो हमें देखने को मिली और इससे काफी फर्क भी हमें देखने को मिला और काफी अच्छी भी लगी हमें स्टेट गवर्नमेंट की।
अरमान नदीम - जी हो सकता है की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन नीति को जनता से इंट्रोड्यूस करवाया जाए लेकिन कई बार ऐसा लगता है वह सिर्फ इंट्रोड्यूस ही हुई है उन तक पहुंच नहीं पाती या फिर लोग उससे जुड़ नहीं पाते हैं तो इसे सबसे ज्यादा और इंप्लीमेंट कैसे कराया जा सकता है और लोगों को इस नीतियों से कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सकता है।
डॉ. दीक्षा तिवारी :- आपने कहा कि हम सभी बच्चों को आंगनबाड़ी में खाना खिलाएंगे जो सभी बच्चों को कुपोषण जैसी समस्याओं से दूर करेगा। लेकिन एक बात यह है कि जो खाना छत्तीसगढ़ के बच्चों को हजम होता है जरूरी या नहीं कि वह दिल्ली के स्लम्स वाले बच्चों को भी हजम हो फिर उनका डायट केरल के बच्चों के साथ मैच करेगा तो सबसे पहले तो यह है कि ब्लैंकेट पॉलिसी को हटाना जाना चाहिए के जो जिस जगह का क्लाइमेट है वातावरण है उसी के हिसाब से वहां तक उन चीजों को सीमित रखा जाए तो यह इस तरह की की चीजों के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं । मान के चलिए जो चीज आदिवासियों की जरूरत है वह मुझे नहीं लगता कि वही महाराष्ट्रीयन को महसूस हो । हमारे यहां चावल ज्यादा खाते हैं आटा कम खाते हैं कहीं पर आटा ज्यादा खाते हैं और चावल को कम खाया जाता है। हम सभी को एक जैसा खाना देंगे तो यह बड़ा ही मुश्किल हो जाता है । उन्हें संभालना भी मुझे लगता है काफी स्पेसिफिक पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ सके और लोग खुद व खुद इसे अपना आपको रिलेट कर सके। तब तो लोगों को फायदा होगा वरना जो पैसा टैक्स पेयर का इन पॉलिसीज में लगता है वह सिर्फ बर्बाद होगा और उसका आम जनता को कोई फायदा नहीं मिलेगा मैं इसे एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगी एक पाउच आता है आंगनबाड़ी में वो बांट दिया जाता है की आप अपने बच्चों को खिलाएं लेकिन असल में ऐसा होता है कि जैसे वह घर लेकर जाती है तो पूरा घर उसे खा लेता है ।जैसे लड्डू बना खा लिया जाता है या हलवा बनाकर खा लेता है पूरा परिवार तो बात आती है कि जो इसके जरूरतमंद होते हैं उन तक वह चीज नहीं पहुंच पाती है। बच्चा या गर्भवती महिला के लिए जो चीज़ पहुंचाई जा रही है वह पूर्ण रूप से उन तक नहीं पहुंच रही , बेनिफिट नहीं मिल पाता उसका भी और जब यह चीज सरकार को और पॉलिसी मेकर्स को समझ आई तो उन्होंने एक इसमें बदलाव किया जिससे हमें फर्क भी नजर आया तो उन्होंने कहा कि हम आपको खाना पैक करके नहीं देंगे यानी ड्राई डाइट है वह आपको नहीं दी जाएगी आपको यही खिलाया जाएगा । तब इस छोटी सी चीज से देखिए आप कितना बदलाव आया है । पोषण पूरा हो पा रहा है इस चीज से तो मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर आपको वाकई में लोगों की मदद करनी है और अपनी पॉलिसीज को उन तक पहुंचना है तो आपको पहले उन्हें समझना भी पड़ेगा और उसे हिसाब से कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे आप सिर्फ कागजों पर काम नहीं कर सकते आपको ग्राउंड पर जो चीज हैं उन्हें भी समझ नहीं जरूरी है की समस्या की जड़ क्या है यह जब तक समस्या नहीं जान जाएगा तब तक किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा।
अरमान नदीम - बिल्कुल यह समस्याएं जब तक जड़ से समझी नहीं जाएगी तब तक इन पर ना तो काम होगा ना इनका लाभ मिल पाएगा और रही बात करप्शन की तो वह हर जगह है जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि जब मैं ₹1 भेजता हूं तो एक पैसा मिलता है यानी की जिस तरीके का करप्शन सिस्टम में हो रखा है यह सब को मालूम है और जब हमें यह हेल्थ यानी कि अस्पताल और इन सब संबंधी चीजों में करप्शन देखने को मिलता है जिसे लोगों की जान जा सकती है उसे पर आप क्या कहना चाहेंगे
डॉ. दीक्षा तिवारी :- अगर आपको इसे सुधारना है या फिर इसे समझना है तो इसकी जड़ तक आपको पहुंचना पड़ेगा और इसकी जड़ से शुरुआत करनी पड़ेगी। कोशिश आपको पर्सनल लेवल पर करनी पड़ेगी । स्वास्थ्य के फील्ड में करप्शन है लेकिन बाकियों में हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो यह भी नहीं होना चाहिए।
अरमान नदीम - हम मनोविज्ञान की बात कर रहे थे जिसमें आपने भी इस बात पर समर्थन जताया कि अवसाद की समस्या आज के नई पीढ़ी में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है ।
डॉ. दीक्षा तिवारी :- इसे आप एक्स्पोज़र से देख सकते हैं बहुत कम उम्र में बहुत सारी चीज एक्स्पोज़र करना एक कम उम्र के व्यक्ति का हो रहा है और मुझे लगता है कि इसमें पैरेंट्स भी जिम्मेदार हैं आपके जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं टीचर्स होते हैं वह भी जिम्मेदार होते हैं इस चीज में हम जब बड़े हो रहे थे हमारा इतना एक्सेस सोशल मीडिया का नहीं था । हम एक सर्टेन आगे तक पहुंचे और उसके बाद में हमने इसे इस्तेमाल किया था कि समझ हुई तो उसे वक्त हमें यह पता था कि क्या चीज मैटर करती है और क्या नहीं । आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया जॉइन करता है तो कितना प्रेशर होता है कोई बहुत सिंपल जीवन जी रहा है ट्रोलिंग होती है लेकिन बात ही आती है क्या आप मेंटली उसे चीज के लिए तैयार है या नहीं क्या आपकी वह उम्र है वह चीज देखने की वह चीज समझने की सहन करने की ।आप सही गलत समझ सके या फिर आप सिर्फ उसमें भेद कर सके यह सिर्फ एक रोलिंग है जिसका आपके वास्तविक जीवन से कोई लेना-देना नहीं है कितना एक्स्पोज़र किस उम्र में होना चाहिए वह आज हमें देखने को नहीं मिलता है । जिम्मेदारी सबसे बड़ी पेरेंट्स की होती है यह उन पर है कि वह कम उम्र में बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखें का जन्म देती है।
अरमान नदीम - अगर हम बात कर रहे हैं एलजीबीटी कम्युनिटी कि ,हम बात करें तो हम कहेंगे बहुत नहीं होना चाहिए । वह भी समाज का हिस्सा है ।
डॉ. दीक्षा तिवारी :- जी बिल्कुल मैं यही बात की की यह हर चीज हमसे ही शुरू हो रही है अगर आप बदलाव करना चाहते हैं समाज में तो आप सबसे पहले खुद में बदलाव कीजिए । महात्मा गांधी ने कहा था आपको खुद से बदलाव की शुरुआत करनी होगी लेकिन यह चीज आसान तो नहीं हो सकती कि हम खुद एक दूसरे को मिम्स शेयर करते हैं और उसमें कितने डार्क ह्यूमर के जोक्स होते हैं। लेकिन हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं जिस वक्त हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे बारे में मेरे ख्याल से सोते भी नहीं है ।बहुत रेगुलर बेस में इस्तेमाल करने लगते हैं उसका एल्गोरिदम बढ़ा देते हैं तब वह एक असर छोड़ता है आपके दिमाग पर भी वह एक निरेटिव बना देता है जो हकीकत जिंदगी में भी दखल देता हैतो यह देखने वाली बात है कि हम खुद को इसमें कितना सजग महसूस करते हैं कि हम सिर्फ इसे इस्तेमाल करें एंटरटेनमेंट के लिए अगर वाकई में इसलिए आपके जीवन पर प्रभाव दे रहा है तो इसे आपको समझने की जरूरत है और मैं एक बार फिर यही बात कहूं कि किसी भी चीज पर बात करनी है अच्छी है लेकिन अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए।
अरमान नदीम - आज के वक्त में देख रहे हैं की संस्कृति और धर्म को लेकर भी एक अलग विवाद चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है संस्कृत अपनी जगह है जिसका मुझे लगता है धर्म से कोई वास्ता नहीं है । मेरी संस्कृति हो सकती है , लेकिन जरूरी नहीं की वह मेरे धर्म में भी चीज मेंशन हो। जिसे मैं बताने के लिए सिर्फ एक ही एग्जांपल देता हूं कैसे 47 में धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना लेकिन 71 में संस्कृति ही थी जिसे बांग्लादेश को जन्म दिया
डॉ. दीक्षा तिवारी :- जी बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूं और यह जो इन बातों पर झगड़ने की बात करते हैं या फिर बांटने की बात करते हैं एक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है लोग उकसाने की बात करते हैं लेकिन मेरा एक स्टैंड क्लियर रहता है कि ऐज ए हिंदू , ऐज ए ब्राह्मण मुझे गर्व है लेकिन मैं उसके बाद में किसी और चीज के ऊपर या किसी और धर्म पर सवाल नहीं उठाती। और कई लोग मतलब आज की डेट में आप देखेंगे कल दिखाने के लिए या फिर देखने के लिए खुद के धर्म को गाली देते हैं तो मैं वह नहीं करती । एक सामान्य सी चीज है की सामने वाला व्यक्ति मेरी सम्मान करें और मैं उसका सम्मान करूंगी और अगर आप इसे यूं देखेंगे कि तो सांस्कृतिक रूप से तो भारत-पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही है । मान के चलिए आप घर पर रहते हैं तो आप कुछ चीज नहीं करते हैं आप घर पर बैठकर सिगरेट नहीं कर पीते हैं आप ड्रिंक नहीं करेंगे क्योंकि आपके पैरेंट्स वहां मौजूद होते हैं एक नियम बना हुआ है कि वह चीज आप घर पर नहीं करते हैं जैसे इंडियन जिस वक्त इंडिया में होते हैं और वहां के सिटीजन पाकिस्तान में अपने देश में होते हैं तो वह चीज उसे अलग तरीके से अप्लाई करती है तो वह जो निरेटिव पर चलता है तो वह उसका पार्ट बने रहते हैं लेकिन जब आप यूके में देखेंगे मतलब दूसरे देशों
अरमान नदीम - आत्म चिंतन को आप कैसे देखते हैं
डॉ. दीक्षा तिवारी :- मैं पर्सनली तौर पर बहुत ज्यादा सेल्फ एनालिसिस करती हूं पहले मैं यह नहीं किया करती थी। एक बार में अपना रिसर्च का काम कर रही थी और जिस पर मैंने प्रपोज दिया कि मैं इस पर अपना थीसिस लिखना चाहती हूं उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था कि आपको जो मालूम है जो आपको पता है वह आपको क्यों पता है वह आपको कहां से मालूम हुआ उसका सोर्स आफ नॉलेज यानी की उसका सोर्स क्या था, उस नॉलेज का ओरिजिन कहां से हुआ । जो चीज आप तक पहुंची है जहां से वह आ रही है तो क्या आपने कभी सोचा है कि वह कहां से आ रही है वह सोचो यह पूरा फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा पार्ट है तो यह चीज मुझे काफी हिट किया और मैं इसके बारे में काफी सोचना शुरू किया सेल्फ एनालिसिस मेरा बढ़ गया । अगर मेरे दिमाग में किसी कम्युनिटी को लेकर स्टीरियो टाइप्स ख्याल आते हैं या फिर एक स्टोरी को लेकर मेरे दिमाग में पर्टिकुलर निरेटिव बना हुआ है तो कहां से आ रहा है । वह चीज मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी लेकिन मेरे पिता के पास में वह बात कहां से आई उनके उनका सोर्स क्या था इन सब चीजों को जवाब बैठकर सोचते हैं तो वह एक आपका नेचर डेवलप हो जाता है तो और फिर उसके बाद में आप सवाल बहुत करने लग जाते हैं चीजों को लेकर और जाने की जिज्ञासा ही व्यक्ति के विचार को जन्म देती है मुझे लगता है। वही एक टाइम होता है । मुझे लगता है यह चीज हमेशा व्यक्ति को सोचनी चाहिए की जो चीज आपको मालूम है वह आपको कहां से मालूम हुई और जो चीज आपको मालूम है क्या वह वाकई में उसे वह चीज हकीकत से रिलेट भी करती है या नहीं और उस निरेटिव को बनाने वाला कौन है और जिसने इस नेगेटिव को जन्म दिया ।उसकी आईडियोलॉजी क्या थी तो यह सब चीज देखनी सोचनी समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसके बगैर आत्म चिंतन में लगता है अधूरा है यह कुछ बेसिक से बिंदु होते हैं जिसे आपको सोचने समझने की बेहद जरूरी होती है ।
अरमान नदीम - आपका बहुत बहुत आभार ।
Monika Chopra
मोनिका चोपड़ा
सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुंसर मोनिका चोपड़ा से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
सोशल मीडिया माध्यम से आम आदमी की मदद की कोशिश भी की है :- मोनिका
अरमान :- आज के वक्त में सोशल मीडिया को सब अपने-अपने इस्तेमाल के अनुसार देखते हैं और अलग-अलग तरह का इसका प्रयोग है। आप बताइए कि आप अपने पेज के द्वारा किस तरह का काम करते हैं और आपका मोटिव क्या रहता है सोशल मीडिया को लेकर और साथ ही अपने बारे में कुछ बताइए।
मोनिका चोपड़ा :-जी बिल्कुल आपने सही कहा और मैं यह कह सकती हूं कि सब अपने अपने उपयोग के अनुसार इसका लाभ लेते हैं और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है तकरीबन दो साल से मैं सोशल मीडिया पेज पर काम कर रही हूं जिसमें मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं बीकानेर शहर के जो व्यापारी हैं और जो दुकान और अलग-अलग तरह की जगह के बारे में जानकारी है उन्हें लोगों तक पहुंचाने का मेरा मोटिव रहता है। शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई क्योंकि अगर मैं अपने ही शौक की बात करूं तो खाने का मुझे काफी शौक है और स्ट्रीट फूड जिसे हम कहते हैं मैं उसे एक्सप्लोरर किया करती थी और उसी के बाद में मैंने यह महसूस किया कि जो लोग इसी तरह का शौक रखते हैं उन्हें भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस जगह क्या सही दाम में मिल सकता है। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अच्छाइयां और खामियां दोनों हमें देखने को मिलती है तो हमेशा से कोशिश रही कि जब भी किसी चीज को इस्तेमाल करूं तो एक अच्छा रिव्यु अपने दर्शकों तक पहुंचाओ जिससे उन्हें उसे इस्तेमाल करने में ज्यादा परेशानी ना हो और वह फैसला कर सके कि यह उनके लिए सही है या नहीं।
मैंने एमजीएसयू यूनिवर्सिटी, बीकानेर से अंग्रेजी में पीएचडी की है और पिछले दो वर्षों से बीकानेर में एक इंफ्लूएंसर के रूप में कार्य कर रही हूँ। जो एक जुनून के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक विकसित कौशल बन चुका है, जिससे मुझे बीकानेर और उसके बाहर एक सौ से अधिक ब्रांड्स के साथ काम करने का अवसर मिला है।
मुझे भारत सरकार द्वारा आयोजित पहले क्रिएटर्स अवार्ड में आमंत्रित किया गया था, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसके अलावा, मैंने राजस्थान सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रमों जैसे आरटीडीसी जयपुर और राजवीका में भी भाग लिया है।
साहित्य और कविता मेरे दिल के करीब हैं, और मुझे पढ़ने और लिखने का बहुत शौक है। मेरे सबसे यादगार पलों में से एक था जब मैंने अपने स्कूल के दिनों में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साहब से मुलाकात की थी। अपने सफर में, मैंने हमेशा पारंपरिक रास्तों से अलग विकल्प चुने हैं, अक्सर सवालों और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी निरंतरता और कड़ी मेहनत से मैंने हर बार खुद को साबित किया है।
मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं अपने परिवार में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली पहली शख्स हूँ और बीकानेर से राष्ट्रीय क्रिएटर्स मीट में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र डिजिटल क्रिएटर हूँ।
अरमान :- क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि जिस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं या करने वाले थे उसमें वह बात नहीं है लेकिन फिर भी एक दबाव रहा उसे प्रमोट करने का?
मोनिका :- बताना चाहूंगी कि जब भी इस तरह की किसी प्रमोशन की बात होती है या पेड प्रमोशन की बात होती है तो कोशिश यह रहती है कि सबसे पहले तो उस चीज के बारे में जानकारी मिले कि वह वाकई में उस पैरामीटर पर है या नहीं और जो चीज हम लोगों के सामने रख रहे हैं तो कोशिश जैसा मैंने आपको कहा पहले यह रहती है कि उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाए उसके बाद ही उसका प्रमोशन होता है । और जैसा आपने कहा कि दबाव तो मुझे नहीं कभी ऐसा लगा कि मुझ पर किसी चीज का दबाव है और कब अगर कभी भविष्य में इस तरह की की चीज आती भी है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे मना करूं क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना मकसद नहीं होना चाहिए हम सोशल मीडिया के थ्रू भी समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं और उसे बेहतर ढंग से निभाने का जोखिम हमें उठाना पड़ेगा और मैं यही कहना चाहूंगी कि इसी तरह कैसे काम करना चाहिए जिससे समाज को फायदा हो। एक वक्त हो जाता है जब हम प्रोडक्ट्स के या फिर उसे जगह के बारे में एक जानकारी रखते हैं तो पहले से ही कुछ चीजों के बारे में पता होता है कि वह काम की है या नहीं है तो खुद से भी हमें इस चीज का महत्व मालूम होना चाहिए। क्योंकि मेरा जो काम है बाजार में लोगों के लिए तो वह ज्यादातर बीकानेर के शहर के लोगों के लिए ही है और मैं जहां तक भी काम किया है तो वह ऐसी दुकानें हैं, ऐसी चीज हैं जो पहले से एक लंबे वक्त से स्टेबलिस्ट तो जब कभी भी मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू उनका प्रमोशन किया है तो कहीं ना कहीं लोग खुद ही आगे आते हैं और उन्होंने भी अपने रिव्यूज दे दिए कि हम तो इस जगह से काफी वक्त से सामान ले रहे थे और यह वाकई में काफी अच्छा है तो जब इस तरह के रिव्यूज दूसरे नए जो लोग हैं वह देखते हैं तब उन्हें एक विश्वास भी होता है कि हां यह जगह वाकई में विश्वसनीय है और यहां से हम सामान ले सकते हैं।
अरमान :- सभी के फायदे और नुकसान अपनी अपनी जगह पर होते हैं और हम सोशल मीडिया के अक्सर लोगों से नुकसान सुना करते हैं लेकिन आप क्योंकि इससे जुड़े हैं आपकी नजर में इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है?
मोनिका :- आपको बता सकती हूं मेरा खुद का अनुभव इससे जुड़ा हुआ जिसके कारण हम एक कह सकते हैं पुण्य का काम भी किया है और वह सोशल मीडिया का पॉजिटिव ही है कि एक बार तकरीबन साल भर पहले मेरी एक दोस्त ने मुझसे बात करते हुए अपने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची की परेशानी के बारे में बताया जो कि कैंसर से पीड़ित है। और वह बच्ची सिर्फ 16 साल की उम्र की थी और उसका परिवार इतना समर्थ नहीं था कि वह इलाज शुरू करवा सके। हालांकि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। उनका घर दूसरों के घर में काम करके चलता था। मेरी दोस्त से जब मेरी बात हुई तो हमने फैसला किया कि हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ को इसमें मदद करने की कोशिश करेंगे और क्योंकि मैंने उसे वक्त से अपना सोशल मीडिया शुरू कर दिया था तो मैंने एक स्टोरी लगाई और एक रात के अंदर इतना ज्यादा रिस्पांस मिला और लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए आगे आए । और बाहर के भी कुछ जो पेज हैं उनसे संपर्क हुआ और हमने कुछ ही वक्त के अंदर एक लाख से ज्यादा की राशि इकट्ठा की और उस बच्ची इलाज शुरू हुआ । तो मैं यह कह सकती हूं कि मैं अकेले तो यह कभी नहीं कर पाती या एक लाख इतने कम वक्त में किसी और माध्यम से जोड़ना यह भी एक बहुत मुश्किल काम है। मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे इलाज शुरू करवाने के बाद भी वह बच्ची इस दुनिया में नहीं रही । हम उसे नहीं बचा पाए क्योंकि उसका कैंसर आखिरी स्टेज पर था लेकिन जो परिवार है, उसके बाकी भाई बहन है उनकी मदद के लिए बाद में और भी एन जी ओ आगे आए। और आपने जैसा कहा कि फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं यह व्यक्ति के ऊपर है कि वह उसका इस्तेमाल अपने फायदे या समाज की भलाई के लिए करता है या सिर्फ उससे उसका नुकसान हो रहा है तो हमने यह भी किया है। के बाद जब दूसरे न्यूज़पेपर वालों ने भी इस चीज को कर किया तब भी मैं इस चीज का जिक्र किया कि सोशल मीडिया और इन सब चीजों से भी हम काम करते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा इससे लेनी चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों को इस तरीके से भी लाभ पहुंचा सकते हैं अगर आप की रीच थोड़ी बहुत भी है अगर आप कुछ इसमें काम करते हैं। आपको न सिर्फ इश्क का अपने लिए इस्तेमाल बल्कि समाज के लिए भी फायदा पहुंचा ऐसा काम करना चाहिए। सोशल मीडिया को सोशल हेल्प के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अरमान :- कंटेंट क्रिएटर जिन्हें हम कहते हैं सोशल मीडिया के क्या उन्हें पूरी तरीके से इसी पर निर्भर होना चाहिए?
मोनिका:- मेरा मानना है कि आप जो प्राइमरी हैं यानी की फर्स्ट पर्सन जिस जिस जरिए से आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि जब आपसे कोई पहली दफा पूछता है तो आप जवाब देते हैं कि मैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूं, एक्टर हूं ,राइटर हूं या और कोई दूसरा काम जो आप करते हैं लेकिन आपको पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं तो आपको अपना झुकाव पूरा इस पर नहीं करना चाहिए । आपको अपने एकेडमिक से हो या फिर दूसरे दीगर इनकम ऑफ सोर्स उस पर भी वैसा ही ध्यान देना चाहिए जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना वक्त दे रहे हैं । फिर चाहे आपने इसमें अच्छा खासा नाम भी कमा लिया हो तो भी लेकिन एक जो निर्भरता है उसके नजरिए से हम देखें तो पूरा इसके ऊपर झुकाव नहीं होना चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि सोशल मीडिया आज के वक्त में लोगों को बड़ा मुकाम भी दे रहा है। हमने यह भी देखा है कि जो आज की डेट में टीवी एक्टर बॉलीवुड में सोशल मीडिया के जरिए भी गए हैं जो पहले सोशल मीडिया पर काम किया करते थे और उसके बाद मैं बड़े पर्दे पर भी देखा जाता है। देखते हैं कि जो बड़े पर्दे पर काम कर चुके हैं सिंगर राइटर एक्टर और दूसरे कलाकार तो वह सोशल मीडिया की तरफ भी आते हैं तो यह एक साइकिल जैसा अब बन चुका है।
अरमान :- सोशल मीडिया के आने वाले दस सालों को आप कैसे देखते हैं?
मोनिका :- सोशल मीडिया के अगर हम आने वाले वक्त की बात करें तो वह सकारात्मक भी है और नेगेटिव फॉर्म में भी हम उसे देख सकते हैं। नेगेटिव में जैसे हम आज भी देखते ही हैं फेक रिव्यूज स्कैम्स भी हमें सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं। एक छोटी से छोटी चीज का प्रमोशन किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने वक्त की बात करूं जब मैं आज से तकरीबन दो साल पहले इसे ज्वाइन किया तो उस वक्त तक में भी यानी कम टाइम में भी बीकानेर शहर के अंदर सोशल मीडिया के अंदर बाजार का जो प्रभाव है इतना नहीं था। जैसे-जैसे सोशल मीडिया पर क्रिएटर आए बीकानेर से तो मार्केट को भी एक पकड़ मिली तो वह जो अपना व्यापार में भी उन्हें बढ़ोतरी मिली और वह अपना सामान सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी से प्रमोट भी करवा रहे हैं। अगर हम दूसरे माध्यमों की बात करें फिर चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या फिर होर्डिंग लगवाना हो तो वह एक पारंपरिक तरीका हो सकता है लेकिन उन्हें उसे तरीके का रिस्पांस नहीं मिलता था जिस तरीके का रिस्पांस सोशल मीडिया के प्रमोशन से मिला है। क्योंकि जब वह ऑनलाइन मार्केटिंग करवाते हैं तो उसका असर हमें देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है कि इसका मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर है और एक ब्राइट फ्यूचर देखने को मिलता है बाजार के लिए। लगता है यह काम आगे से आगे चलता ही रहेगा जहां तक की काम ईमानदारी से किया जाए तो। समय की मांग की अगर हम बात करें तो उसमें बदलाव भी जरूरी होते हैं जिस तरीके से धीरे-धीरे बदलाव होते हुए हम आज यहां तक पहुंचे हैं तो आने वाले वक्त में भी मुझे लगता है कि बदलाव होंगे और होने भी चाहिए समय के साथ।
अरमान :- वक्त में आपका उद्देश्य क्या है अपने सोशल मीडिया से और आप कहां तक इसे लेकर जाना चाहते?
मोनिका :- उद्देश्य यही है कि मैं बीकानेर के बाजार के लिए काम करूं एक अच्छी ऑडियंस बाजार के लिए बने और अपने श्रोताओं को भी बाजार का एक अच्छा अनुभव करवाना। बड़े-बड़े जो ब्रांड हैं उनके लिए तो हर कोई काम करता है लेकिन जो छोटी दुकानें हैं शहर का जो बाजार है उनके ऊपर इतना खास ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन सही मायने में सबसे ज्यादा जरूरी यही है चाहे वह किसी भी लिहाज से देखा जाए अर्थव्यवस्था के मद्देनजर या फिर आम जनता की जरूरत को पूरा करने वाला एक माध्यम तो जो बाजार सबसे ज्यादा जरूरी है लोग उसे पर सबसे कम ध्यान देते हैं तो मेरी कोशिश यह है कि मैं बीकानेर के छोटे दुकानदारों और बाजार पर अपना पूरा ध्यान बनाए रखूं। दुकान ऐसी भी हम देखने को मिलती है जो अच्छा सामान बेचते हैं उनके क्वालिटी एक स्टैंडर्ड होती है लेकिन आम जनता उन्हें इतना नहीं जानती या फिर उन्हें आसपास के इलाकों तक ही वह सीमित रह जाते हैं तो जब वह उन तक वह चीज पहुंचती है तो जाहिर सी बात है वह अच्छी चीज के लिए पैसा भी खर्च करते हैं और अपने शहर में हो तो वह वहां जाते भी हैं तो इससे दोनों तरफ का फायदा है जो जनता है जो लोग हैं उन्हें एक बढ़िया सामान मिलता है अच्छी किफायती दाम में और जो व्यापारी है उनका तो खैर उससे फायदा है ही।
अरमान :- क्या आप अपनी ऑडियंस तक को अपना काम पहुंच पा रहे हैं?
मोनिका :- बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों से मैं जुड़ी हूं जो लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं वह लगातार मेरा काम देख रहे हैं और उसकी सराहना भी की जा रही है। सब चीज मुझे घर बैठे जन को नहीं मिलता जब मैं बाहर जाती हूं तब भी लोग पहचान जाते हैं और के उन्हें अच्छा भी लगता है और वह अपना फायदा भी बताते हैं कि आपने वह चीज हमें रिकमेंड करी थी और वहां जाकर जब हमने वह चीज ली तो वाकई में हमें काफी फायदा हुआ तो इस तरह की की चीज भी होती है तो अच्छा लगता है और एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि जो हम काम कर रहे हैं वह लोगों के फायदे के लिए है और लोग उसका फायदा ले भी रहे हैं तो और आगे इसी तरह का काम करने की प्रेरणा भी हमें लगातार इन चीजों से मिलती है।
अरमान :- इस तरह का काम करने का विचार कैसे आया दिमाग में?
मोनिका :- दूसरे ब्लॉगर्स है या फिर जो कंटेंट क्रिएटर है उन्हें देखा करते थे जो बाहर दिल्ली मुंबई और जयपुर जैसे दूसरे बड़े शहरों में अपना काम किया करते थे और इसी तरह की चीज अपने सोशल मीडिया पर डाला करते थे जो वहां के जो लोकल बाजार के हैं दुकान हैं और वह अपने रिव्यूज दिया करते थे फिर चाहे वह फूड ब्लॉगिंग हो या फिर दूसरी तरह की दुकानों पर जाकर उनके सामान की चर्चा करना हो तो मुझे वह सब देखने में अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं दिमाग में यह था कि बीकानेर शहर के अंदर ऐसा कोई पेज नहीं है जो बीकानेर की जनता को यह चीज बताएं और क्योंकि हर कोई व्यक्ति जाकर हर जगह नहीं जा सकता और सामान्य चुनने में जो इस तरह के का वक्त लगता है वह हम घर सभी जानते हैं और अच्छा और खराब में तो फिर आज के दौर में हम देख ही रहे हैं किस तरह के किस गेम्स भी होते हैं और बड़े-बड़े लोग नकली सामान भी बाजार में बेचते हैं बड़े स्तर के ऊपर तो इस तरह की की चीज जब मैं सोची तो मुझे लगा कि बीकानेर के अंदर भी ऐसा कोई पेज होना चाहिए और वह शुरू मैंने किया अपने माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से और वहीं से फिर मैंने शुरुआत में फूड ब्लॉगिंग भी की और आज की तारीख में इसी तरह का काम हो रहा है।
मैं अपनी बात में यह भी कहना चाहूंगी कि जैसा कि हमें आज की तारीख में देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया का जो युग हम जिसे कहें हर जगह देखने को मिल रहा है इसका असर और काफी लोग इसकी तरफ जैसा आ रहे हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि जो आपका शुरुआती काम है उसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए चाहे फिर वह पढ़ाई की क्यों ना हो, पढ़ाई जरूरी है इन सब चीजों से पहले और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जब कोई चीज नहीं शुरू करते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप सोशल मीडिया पर आ सकते हैं लेकिन उससे एक तरफ अलग रखकर आप कम कीजिए लेकिन जो आपका एकेडमिक है उसे आपको पहले पूरा करना चाहिए। मैं बार-बार एक चीज दोहराना चाहूंगी कि आप इस साइड में लेकर साथ में काम कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई को ना छोड़े और अगर आप इसमें अपना काम कर रहे हैं तो कोशिश यह करें कि जितना बेहतर हो सकता है अपनी तरफ से वह करें।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार
मोनिका - धन्यवाद
Jitendra Shrivastav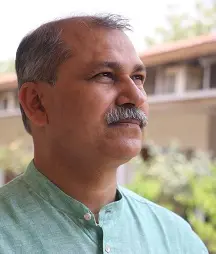
जितेंद्र श्रीवास्तव
वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक और इग्नू के अंतरराष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत।
साहित्य स्टारडम का खेल नहीं है - जितेंद्र श्रीवास्तव
परिचय
जितेन्द्र श्रीवास्तव
देवरिया (उत्तर प्रदेश) में जन्मे और जे एन यू, नई दिल्ली से उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिष्ठित कवि-आलोचक जितेन्द्र श्रीवास्तव इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के मानविकी विद्यापीठ में हिंदी के प्रोफेसर हैं। पूर्व में इग्नू के कुलसचिव और पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा प्रबंध विद्यापीठ के निदेशक रह चुके हैं।इन दिनों इग्नू के अंतरराष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक हैं।
हिन्दी के साथ-साथ भोजपुरी में भी लेखन प्रकाशन। इन दिनों हालचाल, अनभै कथा, असुन्दर सुन्दर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायान्तरण, सूरज को अँगूठा, जितनी हँसी तुम्हारे होंठों पर, काल मृग की पीठ पर, उजास , कवि ने कहा, बेटियाँ, रक्त-सा लाल एक फूल, स्त्रियाँ कहीं भी बचा लेती हैं पुरुषों को (कविता); तेरे खुशबू में भरे ख़त (कहानी) भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना का मानुष-मर्म, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि, रचना का जीवद्रव्य, कहानी का क्षितिज, कविता का घनत्व, आस्था और विवेक (आलोचना); प्रेमचंद कहानी समग्र, प्रेमचंद: स्त्री जीवन की कहानियां, प्रेमचंद: दलित जीवन की कहानियां, प्रेमचंद: दलित एवं स्त्री विषयक विचार, प्रेमचंद: स्वाधीनता की कहानियां, प्रेमचंद : किसान जीवन की कहानियां, प्रेमचंद: हिन्दू - मुस्लिम एकता संबंधी कहानियां, शोर के विरुद्ध सृजन सहित कुछ अन्य पुस्तकों का संपादन। गोदान, रंगभूमि और ध्रुवस्वामिनी जैसी कुछ कालजयी पुस्तकों की पुर्नप्रस्तुति के लिए उनकी संक्षिप्त भूमिकाएँ भी लिखी हैं।
कई कविताओं का अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। लम्बी कविता सोनचिरई की कई नाट्य प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं। कई विश्वविद्यालयों के कविता केन्द्रित पाठ्यक्रमों में कविताएँ शामिल हैं। कविताओं पर देश के कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में दस से अधिक शोधकार्य हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं।
साहित्यिक पत्रिका 'उम्मीद' का संपादन किया है और 'नयी उम्मीद' का संपादन कर रहे हैं।
अब तक कविता के लिए 'भारत भूषण अग्रवाल सम्मान' और आलोचना के लिए 'देवीशंकर अवस्थी सम्मान' सहित हिन्दी अकादमी दिल्ली का 'कृति सम्मान', उ.प्र. हिन्दी संस्थान का 'रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार, उ. प्र. हिन्दी संस्थान का 'विजयदेव नारायण साही पुरस्कार', भारतीय भाषा परिषद्, कोलकाता का 'युवा पुरस्कार', 'डॉ. रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान', 'परम्परा ऋतुराज सम्मान', गोपालकृष्ण रथ स्मृति सम्मान और स्पंदन कृति सम्मान ग्रहण कर चुके हैं
अरमान:- साहित्यिक समाज में आपकी शुरुआत कैसे हुई?
जितेन्द्र श्रीवास्तव:- साहित्य में अब तो काफी वक्त हो चला है लेकिन मेरी पहली रचना 1986 में प्रकाशित हुई लेकिन काफी कम उम्र से ही साहित्य में दिलचस्पी बनने शुरू हो गई थी और 1990 के बाद में निरंतरता आई। क्योंकि 1990 के बाद में जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी उनमें मैंने कविताएं ,कहानियां भेजना शुरू किया और वह वहां लगातार प्रकाशित भी हुई। सिलसिला चल पड़ा लोगों ने काफी पसंद किया। और जब आत्मविश्वास बढ़ा तो फिर संग्रह भी प्रकाशित हुए। और मेरा पहला संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम था "हाल-चाल" और वह प्रकाशित हुआ था इलाहाबाद की एक पत्रिका कथ्य रूप में । कविताओं का वह मेरा पहला संग्रह था। हाल-चाल के बाद अंत्य कथा के नाम से मेरा संग्रह आया। इस तरह से आगे मेरे कविताओं के संग्रह प्रकाशित होते रहे और साहित्य के प्रति मेरा रुझान जिस तरीके से कम उम्र से ही रहा फिर वह बाद में बढ़ता गया। इन सभी के बीच में किताब घर की बहुत प्रसिद्ध श्रृंखला है "कवि ने कहा" प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह है वह प्रकाशित हुआ। अगर मैं अपने कुछ और संग्रहों की बात करूं तो अब तक के हिंदी इतिहास में बेटियों के ऊपर भारत में एकमात्र संग्रह है जो मेरा लिखा हुआ है। इस तरह से कुल मिलाकर आठ संग्रह है कविताओं के और 12 किताबें आलोचना पर लिखी गई है। जब साहित्य में कविताएं और रचनाएं कर रहा था तो समानांतर ही मेरी आलोचना की किताबें भी प्रकाशित हो रही थी तो किताबों में प्रेमचंद और भारतीय समाज की समस्याओं पर आलोचनात्मक काम भी प्रकाशित हुआ है। भारतीय राष्ट्रवाद और प्रेमचंद यह विषय रहे। शब्दों में समय।
अरमान:- मन चंचल होता है और उसमें भी युवाओं का मन कुछ अधिक चंचल होता है तो सवाल यही है कि युवा लेखन को आप कितना स्वतंत्र मानते हैं और जिम्मेदारियां का निर्माण क्या कर पा रहे हैं इसके ऊपर आपके विचार?
जितेन्द्र श्रीवास्तव:- हम हिंदी साहित्य की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि युवा बड़ी संख्या में रचनात्मक काम कर रहे हैं। और काफी अच्छा काम कर रहे हैं काफी अच्छा लिख रहे हैं। जब बहुत सारे लोग कोई काम करते हैं तो उसमें औसत दर्जे का भी कार्य सम्मिलित होता है।
लेकिन हमें उसे चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो बेहतर हो। और अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो काफी बड़ी संख्या है युवाओं की। क्योंकि अगर हम युवा वर्ग की बात करें तो उसमें 20 से 21 से लेकर 40 तक को हम युवा मान सकते हैं। अगर हम इसी वर्ग को लेकर चलें तो कम से कम 200 तो इसमें इतने कमाल के कवि, लेखक आपको मिलेंगे जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। काफी अच्छे कथाकार हैं ,काफी आला दर्जे के रचनाकार हैं, कहानीकार हैं। कुछ नए आलोचक भी हमें देखने को मिलते हैं जिनका दृष्टिकोण वाकई में कमाल है। और क्योंकि अब मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। चमक दमक का दौरा आ चुका है जिसमें हर कोई खुद को आगे दिखाना चाहता है। 1990 के आसपास का जो समय था जब हम लोगों ने या मेरी उम्र के साथी लेखकों ने साहित्य में अपनी शुरुआत की लिखना शुरू किया। वक्त अखबार और पत्र पत्रिकाएं ही छापने का आधार थी। और पत्रिकाओं के अंदर अपनी रचना छपवाना आसान नहीं हुआ करता था। संपादक काफी ठोक बजाकर रचनाओं को छापा करते थे। वह यह देखा करते थे कि इस वक्त क्या यह रचना पक पाई है या नहीं। रचना में चमक है या नहीं। तो एक तरह से अगर मैं बात करूं तो आप उनकी नजर से तराशे जाते थे। कि जब आप अपनी रचनाएं भेजा करते थे तो आपको मार्गदर्शन भी दिया जाता था। उससे आप अपनी कमियों को भी जान पाते थे। लेखक को यह भी पता चल पाता कि क्या पढ़ना चाहिए लिखने से पहले। अगर हम आज के युवाओं की बात करें और जिनमें से ज्यादातर अगर जो साहित्य के विद्यार्थी हैं। अगर सिर्फ हम साहित्य के विद्यार्थियों की बात करें तो भी फिर उन्हें थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन समस्या उनके साथ में आती है जो सीधे तौर पर साहित्य के विद्यार्थी नहीं है लेकिन उनमें प्रतिभा है मगर उन्हें किसी तरह का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा वह कहीं ना कहीं कई बार भटक जाते हैं। और वह कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने की, ब्लॉग पर या अपने द्वारा बनाई वेबसाइट पर। कई बार वह चीज भी वायरल हो जाती है काफी ज्यादा तादात में लोग उनकी चर्चा करने लगते हैं। लेकिन वह उसे चर्चा के अंदर वह बात समझ नहीं पाते हैं कि जो रचना उनकी वायरल हुई है क्या वाकई में उसने हिंदी साहित्य में कोई योगदान दिया है? हो सकता है जो चीज जो रचना वायरल गई है उससे बेहतर काम किया जा सकता था या फिर किया जा चुका हो। संभवत कहीं बार ऐसा हो जाता है कि उनको और उनकी वाहवाही करने वालों को सही तरह की समझ ना हो। नजर में युवाओं को आज की तारीख में इस और ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है जो लोग लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं। जो लंबी पारी खेलना चाहते हैं। उनके लिए लिखना सिर्फ कोई शौक नहीं है प्रतिबद्धता है। वंचितो के प्रति ,राष्ट्र के प्रति ,समाज के प्रति। तात्कालिक चमक है उससे बचने की जरूरत है साहित्य में रातों-रात फेमस होने की इच्छा यह कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान दे जाती है, यह क्रिकेट नहीं है कि एक सिक्सर लगाया और आप फेमस हो गए ,आपका नाम हो गया आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक लंबे वक्त तक अपने आप को इसमें तपाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि साहित्य स्टारडम का खेल नहीं है। यह लंबी पारी का है और इसमें लंबे वक्त तक आपका नाम रहता है ये नेम फेम वाला काम नहीं है जहां पर कम वक्त के अंदर आप आए और अपना नाम बड़ा बनाने की जद्दोजहद में लग जाए और अगर ऐसा किसी के मन में हैं तो वह उसके काम में भी हमें देखने को मिलता है और जब शुरुआत से ही इस तरह की मानसिकता लेकर कोई लेखक चलता है तो वह लंबे वक्त तक टिक भी नहीं पता क्योंकि जो उसकी सोच है वह उसके पर के काम पर हावी हो ही जाती है। और जब पाठकों को आपका काम आपकी रचनाएं पसंद आती है तो जाहिर सी बात है कि उनका प्यार भी आपको मिला है।
अरमान:- आपने अपनी किताबों का जिक्र करते हुए एक बात कही कि प्रेमचंद और भारतीय समाज की समस्याओं पर आपने काम किया ,आलोचनात्मक किताबें भी आपकी प्रकाशित हुई तो आपकी नजर से भारतीय समाज की समस्याओं को कैसे देखा है?
जितेन्द्र श्रीवास्तव:- जी बिल्कुल वह किताब प्रेमचंद के रचनाकर्म पर लिखी गई है । प्रेमचंद ने जो बहुत सारे निबंध लिखे हैं संपादकीय लिखे थे उनको केंद्र में रखते हुए वह किताब लिखी गई और समस्याएं तो अगर हम बात करें तो बहुत सारी है लेकिन उसके अंदर मुख्य रूप से चार मुद्दों को केंद्रित किया गया है कि जो प्रमुख समस्याएं जिन्हें हम कह सकते हैं जिन पर पहले दृश्य हमें देखने को मिलता है और हमें अपनी दृष्टि भी उसमें रखनी होती है। एक तो स्त्री के जीवन को लेकर बात की गई है के भारतीय सामाजिक संरचना में स्त्री की क्या भूमिका है और क्या स्थिति है उसे पर बात की गई है कि किस तरीके से हमें वह भूमिका और परिस्थिति दोनों को समझना होगा तभी हम समस्याओं को भी देख पाएंगे समझ पाएंगे। दूसरी प्रमुख समस्या जो उसके अंदर केंद्रित की गई है जो कि वाकई में एक बड़ी समस्या भी जिसे हम कह सकते हैं किसान जीवन। कोशिश की गई है कि यह दर्शाया जाए और यह महसूस किया जाए कि किसान की क्या परेशानियां है क्या समस्याएं हैं जिनसे उन्हें हर रोज जूझना पड़ता है और जिनका सामना वह करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेमचंद भी किसानों के काफी करीब थे। और वह खुद किसानों के प्रति काफी लगाव महसूस किया करते थे उनके बारे में काफी सोचते थे उनकी समस्याओं के बारे में काफी सोच करते थे विमर्श किया करते थे यह चीज उनकी लेखनी में भी हमें देखने को काफी ज्यादा मिल जाती है और उनके लेखन का बड़ा सा किसानों के ऊपर केंद्रित रहा है किसानों से संबंधित है। जो किताब में भी यही चीज है कि किसानों के जीवन में क्या समस्याएं हैं और उनसे केंद्रित चीज। प्रेमचंद खुद किस तरीके से देखते थे उसका विश्लेषण करने की कोशिश हुई है। और दलित समाज को लेकर ,जो वंचित है उनकी समझ में क्या परेशानियां है जो उन्हें महसूस करनी पड़ती है जो सबसे बड़ी समस्या है छूत अछूत का जो प्रश्न है जो की एक लंबे समय से बरकरार है उसे चीज को लेकर जो प्रेमचंद ने चिंतन किया विचार किया गया है इस चीज को भी विशेष रूप से दर्शाने की कोशिश हुई और हिंदू मुस्लिम एकता प्रेमचंद किस तरीके से देखते थे जोश भाव है जो भाईचारा एकता की जो बात है प्रेमचंद के लेखनी में और उनके विचारों में मुख्य तौर पर यह मुद्दे हैं किताब के अंदर जो कि यह चार मुद्दे किताब है।
अरमान :- भेदभाव वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है फिर हम लोग किसी भी समाज के लिए बात करें लेकिन जब यह चीज साहित्य में हमें देखने को मिलती है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं गुटबाजी हावी हो जाया करती है।
जितेन्द्र श्रीवास्तव:- जी बिल्कुल भेदभाव तो कहीं पर भी नहीं होना चाहिए और रही बात साहित्य की तो साहित्य तो भेदभाव को मिटाने के ऊपर अपना काम करता है और लेखक योगदान देते हैं। रही बात कुछ बाजी की तो यह तो सबसे बड़ी समस्या भी है और गलत है काफी। और जो गुटबाजी करेगा वह व्यापक मनुष्यता की बात कैसे करेगा वह सब के कल्याण की बात कैसे करेगा जो एक क्षेत्र की बात करेगा या फिर अपने अच्छा की बात करेगा वह सब के बारे में तो नहीं सोच सकता तो इस तरह की चीज केवल नुकसान पैदा करती है। साहित्य आपको सीमाओं से मुक्त करता है वह आपको बांधता नहीं है और जो सीमाओं में बंधेगा उसका साहित्य कैसे किसी और को उज्ज्वलित करेगा कैसे किसी और को रास्ता दिखाएगा। साहित्य का काम तो मुक्त करना है। किसी प्रकार की जकड़ बंदी का विरोध होना चाहिए साहित्य में।
अरमान:- एक समस्या और भी है समझ में पिछड़ेपन की एक लेखक की नजर में वह कब खत्म हो सकता है या फिर उसकी कल्पना कहां तक जाती है इसको लेकर?
जितेन्द्र श्रीवास्तव:- अगर आप पीछे पलट कर देखेंगे तो काफी चीज काफी धीरे-धीरे बेहतर हुई है। जब प्रेमचंद लिख रहे थे पिछले शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उसे वक्त तक बहुत बड़ी संख्या नहीं थी स्त्रियों की जो पढ़ लिख रही हूं। बहुत बड़ी संख्या नहीं थी दलित समुदाय से आने वालों की जो नौकरी में हो और अच्छा पढ़ लिख रहे हो। अगर आप आज के वक्त में देखेंगे तो एक बड़ी संख्या है स्त्रियों की जो पढ़ती भी हैं और पढ़ाती lभी हैं एक बड़ी संख्या है दलित समाज से आने वालों की जो एक अच्छी स्थिति में देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद या उनके जैसे लेखक जो उसे वक्त इस तरह की चीजों की मांग किया करते थे तो उनका सपना काफी हद तक साकार हुआ देखने को मिलता है। कह सकते हैं महात्मा गांधी का डॉक्टर अंबेडकर का जो भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने जो सपना स्त्रियों के लिए, दलित समाज के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए देखा था तो वह कहीं ना कहीं धीरे-धीरे धरातल पर आ रहे हैं हमें देखने को मिल रहा है जो बदलाव समाज में हुआ है जो एक समानता की बात भी करता है और उन्हें अधिकार भी देने का काम करता है। और वक्त के साथ आने वाले दिनों में यह और ज्यादा काम होगा। यह समाज जिस समाज में हम हैं यह हजारों साल की संरचना है। वह चीज एक दिन में नहीं बदल सकती है फिर चाहे वह समस्याओं की बात हो सुधार की बात हो या परिवर्तन की बात हो। बदलाव होगा तो वह सामूहिक योगदान से होगा किसी सरकारी योजना से नहीं। हमको आपको सबको एक साथ बदलना है। निश्चित तौर पर पिछड़ापन दूर होगा। और पिछड़ा अपन दोनों तरह का है आर्थिक पिछड़ापन भी है और मानसिक पिछड़ापन भी है दोनों से मुक्ति की जरूरत है।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार।
जितेंद्र श्रीवास्तव - धन्यवाद
Hammad Hasan Rind
हम्माद हसन रिंद
ब्रिटिश लेखक और अनुवादक ,उर्दू, फ़ारसी,अंग्रेजी, सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता हम्माद हसन रिंद से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
एक अनुवादक दो भाषाओं और दो संस्कृतियों के बीच पुल का काम करता है - हम्माद हसन रिंद
हम्माद हसन रिंद
वेल्स(ब्रिटेन )में रहने वाले एक बहुभाषी लेखक और अनुवादक हैं और अंग्रेजी, उर्दू, फ़ारसी, वेल्श और यिडिश सहित कई भाषाओं में काम करते हैं। पहले उपन्यास फोर दरवेश (सेरेन बुक्स, 2021) को ब्रिटिश साइंस फिक्शन एसोसिएशन अवार्ड के लिए चुना गया था। उन्होंने भारतीय कवि नवीन किशोर की नॉटेड ग्रिफ़ का 2022 में उर्दू (ज़ुका बुक्स) में (उलझा ग़म) के रूप में अनुवाद किया और 2024 में फिलिस्तीनी कवि नजवान दरवेश की कविताओं के संग्रह का नोदियादलीफ़र बाख वाई वावर (वाई स्टैम्प) शीर्षक के तहत इस्तिन टाइन के साथ अरबी से वेल्श में सह-अनुवाद किया। हम्माद ने किंग्स्टन विश्वविद्यालय, लंदन से फिल्म निर्माण में एमए किया है।
अरमान:- साहित्य में अनुवाद एक बड़ा जिम्मा है और मुश्किल भी ,आपने यह शुरू कैसे किया ?
हम्माद हसन रिंद:- तकरीबन दस साल से वेल्स में रह रहा हूं लिहाज़ा एक लंबा वक्त गुजर चुका है कि मैं इंग्लैंड में हूं और अगर मैं अपने सफ़र की शुरुआत के बारे मैं बात करूँ तो बचपन से ही पढ़ने का काफ़ी शौक़ रहा और कहीं न कहीं शुरू से ही दिमाग़ में ये बात थी जो मैं पढूं उसे उसकी असल ज़बान में ही पढूं तो इसी के चलते नई ज़बाने सीखने का एक शौक़ रहा और जैसा कि आपने कहा कि ट्रांसलेटर के तौर पर मैंने शुरू किया और क्यों किया उसकी वजह मैंने आपको बताई की क्योंकि मेरे ज़ेहन शुरुआत से ही था कि जब भी मैं कोई एक नई चीज पढ़ूं या फिर समझूं तो उसे उसी की जबान में पढ़ूँ यानी कि मेरा जो पर्सनल थॉट अप्लाई करता है वह यह करता है कि जब किसी के विचार सुनूं तो उसी की असल जबान में और उसे समझने की कोशिश करूं जाहिर तौर पर है कि सभी चीज नहीं सीखी जा सकती और इंसानी दिमाग की कुछ हद है । लेकिन मैंने कईं भाषाए यहां सीखी जैसे फारसी ,उर्दू । यहां आकर मैंने वेल्स सीखी और भी दूसरी जो भाषाएं हैं जिनमें मैं लगातार काम कर रहा हूं और और जो मैंने कहा भाषाएं सीखने का मुझे बचपन से ही शौक लगा था। तुर्की और अरबी भी शामिल है । और अगर यूरोप की भाषाओं की बात करूं तो मुझे फ्रेंच ,इटालियन भी आती है। जब मैं लिखता हूं तो भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसी भाषा में वह साहित्य लिखूं । मेरा पहला नॉवेल पब्लिश हुआ वह अंग्रेजी में था "फोर दरवेश" 2021 में प्रकाशित हुआ । उसे लिखने की जो मेरी इंस्पिरेशन थी कह सकते है जो दास्तांगोई हमारी एक रिवायत है उर्दू फारसी अदब में । पहले तर्जुमा जो मेरा रहा वो यही के शायर नवीन किशोर जो कोलकाता से हैं। वे खुद पब्लिशर है । उनका ज्यादातर इंटरेस्ट है वह तर्जुमा छापने में है उन्होंने ख़ुद भी अनुवाद पर काम किया है।
अरमान :- जैसा की शुरुआत में ही मैंने बात रखी की अनुवादक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर चलता है क्योंकि जो चीज इंसान नहीं जानता उसके लिए आप बहुत बड़ा एक मकाम रखते हैं भाषा के तौर पर। लेकिन अनुवादक के लिहाज़ से आपको सबसे बड़ी चुनौतियां क्या नजर आती है?
हसन :- सवाल आपका काफी दिलचस्प है और सबसे पहले तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा कि यह वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी बात की मैं ताईद करूंगा कि एक अनुवादक जो है वो एक पुल का काम करता है दो संस्कृति दो भाषाओं के बीच में की जो उससे अनजान है वह उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है। अदब से यह वाकई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपका सवाल था की चुनौतियां क्या नज़र आती है तो मैं कह सकता हूँ की चुनौतियां तो इसमें बहुत सारी है लेकिन अगर हम कुछ चुनौतियां की बात करें जो मुख्य तौर पर नजर आती है सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जिस कल्चर से आप तर्जुमा कर रहे हैं तो कुछ हद तक आपको उसके बारे में भी जानना होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम सीधे तौर पर किसी भी चीज का तर्जुमा नहीं कर सकते बिना उसके बारे में समझे हुए कुछ ऐसे टेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं वह मुश्किल हो सकती है उसे समझने के लिए आपको इसकी संस्कृति से रूबरू होना पड़ता है उसके समकक्ष को देखना पड़ेगा कि वह किस परिवेश में लिखा गया है उसकी सोच क्या थी लिखने की और किस तरीके से वह लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। लोगों के दिमाग में एक यह चीज भी है तर्जुमा को लेकर अनुवाद को लेकर के वह एक-एक शब्द का होता है यानी कि एक-एक शब्द का तर्जुमा होता है जैसे मान कर चलिए अंग्रेजी का कोई शब्द है उसका सिर्फ जो हिंदी में मतलब है उसे ही हम लेकर चले लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि तर्जुमा का असल मकसद यह है कि सामने वाले व्यक्ति को उससे रुबरु करवाना और उसका जो भाव है उसे खत्म न होने देना वह सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। कई बार हमें खुद से क्रिएटिविटी भी लगानी पड़ती है उसे ट्रांसलेट करने के लिए जाहिर तौर पर है इससे आप भी वाक़िफ़ होंगे। एक मजा भी आता है और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि हम उसे क्रिएटिविटी के साथ में उसका जो मूल है उसे ना बदलें। की जो चीज आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं वह एक कल्चर में है लेकिन दूसरे कल्चर में दूसरे अदब में नहीं है तो आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप उसे कैसे लोगों तक लेकर आएंगे वह सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है कि जिस कल्चर से जी अदब से सामने वाला इंसान वाकिफ नहीं है उसे उसके हिसाब से आप कैसे समझेंगे। सबसे बड़ी जो चीज आती है बाहर निकाल कर वह आती है क्रिएटिविटी।कई बार लोग यह भी समझते हैं कि जो अनुवादक है जो तर्जुमा करने वाला है वह अदीब से कमतर है यानी कि जो लेखक है वही क्रिएटर है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते है वहाँ मेरी नजर में एक ट्रांसलेटर जब उसका अनुवाद करता है किताब का तो वह भी उसका उतना ही भागीदार है जितना कि लेखक। जब किसी किताब का नई भाषा में तर्जुमा किया जाता है तो मुतर्जिम का भी उसी तरह का दखल रहता है जो एक लेखक का होता है । पूरी चीज अनुवादक की स्किल के ऊपर निर्भर करती है कि वह उस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभा पाता है। चुनौतियों की जैसे आपने जो बात कही एक यह भी चीज मेरी नजर में जो मैं खास ध्यान रखता हूं कि जब भी हम तर्जुमा करें और नई भाषा के अंदर ऐसा नहीं लगना चाहिए पढ़ने वाले को कि वह अनुवाद हो रखा है वह लगना चाहिए कि इस भाषा में वही चीज पहली बार लिखी गई हो।
अरमान :-अगला सवाल एक परिस्थिति से आप समझ सकते हैं मान के चलिए आप अपने कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका आपको अनुवाद करना है लेकिन क्या कभी ऐसा आपको लगा कि पढ़ते पढ़ते जिसका अनुवाद करना चाह रहे थे आपने उसकी आलोचना भी लिखी हो?
हसन:- काफी दिलचस्प सवाल है यह भी आपका। अगर आपके सवाल से थोड़ा मैं अलग होकर कहूं तो खैर मैं काफी रिव्यूज लिखे हैं किताबों के जिन पर मैंने काम किया था।
और आपने सवाल किया कि कभी अनुवाद करते हुए तर्जुमा करते हुए आलोचना की स्थिति बनी तो ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं मैंने कभी ऐसा अलग से उसके क्रिटिक के तौर पर कभी मेने नहीं लिखा लेकिन वाकई में यह अगर सिचुएशन होती तो काफी दिलचस्प थी जैसा आपका सवाल बना। अरमान साहब अगर मैं आपके सवाल को दूसरे एंगल से लेना चाहूं तो मैं उसका जवाब कुछ यू दूंगा क्योंकि एक तर्जुमा करने वाला इंसान किसी भी टेक्स्ट को स्क्रिप्ट को काफी ध्यान से देखता है उसे ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कहा जाता है कि जो सबसे अच्छा पाठक होता है वह अनुवादक होता है। मुझे लगता है यह एक नेचुरल चीज है क्योंकि जब भी आप किसी चीज को गहराई से देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसमें आपका आलोचनात्मक दृष्टिकोण बन जाता है कई बार जैसा मैंने कहा कि किस तरीके से कहानी पेश की गई है आपको उसमें भी कुछ ना कुछ खामियां नजर आएंगे के इसको ऐसा न होकर ऐसा होना चाहिए था।
अरमान:- हमें देखने को मिल सकता है कि आज की जनरेशन की अगर हम बात करूं या जो मेरे हम उम्र हैं मुझे ऐसा लगता है कि वह साहित्य के की जो औपचारिकता है उसे वह दूर होते जा रहे हैं यानी कि जो चीज मूल है जो चीजों को निभाना जरूरी है उनसे वह लोग दूर होते जा रहे हैं। मैं आपको अपने एक अनुभव के साथ में इसका उदाहरण दे सकता हूं कि कहा गया कि कि जब हम किताब प्रकाशित करते हैं तो उसमें इतनी मुश्किल भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ? हम जो टेक्स्ट व्हाट्सएप के अंदर जब हम टेक्स्ट चैट करते हुए इस्तेमाल करते हैं क्या उसमें किताब नहीं लाई जा सकती । कहीं ना कहीं यह सवाल बचकाना हो सकता है लेकिन अभी तालिब होने की नजर से यह गंभीर फिक्र पैदा करता है।
हसन:- ऐसा महसूस किया जाता है कई बार। लेकिन हम अभी भी काफी अच्छे मकाम पर हैं जैसा आपने कहा कि बचकाना सवाल लग सकता है जाहिर तौर पर लग सकता है और है भी। लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान में आज भी अदब को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है तो यह कुछ चीज बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है लेकिन इन्हें संभाला भी जा रहा है । मुझे लगता है की सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें माना जाए तो सोशल मीडिया को हम कह सकते हैं क्योंकि जैसा जो हाल हमें देखने को मिला युवाओं की सोच के अंदर तो वह क्यों हुआ ? क्योंकि जो सोशल मीडिया जिस पर निर्भरता इतनी बढ़ गई थी युवाओं की तो उसका हमें आज भी हमें देखने को मिला क्योंकि लगातार सिर्फ जो कंज्यूम किया गया सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट वह इसी तरह का था तो कहीं ना कहीं जो गंभीरता जैसा आपने कहा वह कम हुई लेकिन अब वापस से जो एक चुके सकते हैं रिकवरी मोड पर हैं हम तो हम संभाल सकते हैं। क्योंकि उसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया जो पढ़ने की आदत थी , पढ़ने की आदत कम हुई क्योंकि किताबें लोगों ने छोड़ दी घरों के अंदर और सोशल मीडिया के दबाव में बहुत ज्यादा आ गए । जबकि होना यह चाहिए था कि लोगों को किताबों की तरफ और ज्यादा जाना चाहिए था । अदब की तरफ जाना चाहिए था , लेकिन युवाओं के साथ ऐसा हुआ नहीं। का सबसे बड़ा आप कारण यह भी देखेंगे कि जो नौजवान है वह बड़े ही सोशल मीडिया के साथ में है लेकिन जो उनसे पहले की जो पीढ़ी है जो मैं कह सकता हूं जो 90 के दशक से थोड़ा पहले या उसे वक्त तक में जिनकी पैदाइश हुई उन्हें उससे पहले का दौर मालूम है वह जानते हैं कि अपने वक्त को और कैसे यूटिलाइज करना है । हम कह सकते हैं वह जो 15 से 25 साल की उम्र के जो नौजवान हैं वह काफी ज्यादा इसमें खराब हो रहे हैं.
अरमान :- आपने बहुत सही बात कही के जो आज का जो नौजवान है वह इसमें काफी परेशान है लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जो नौजवान जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की जिम्मेदारी की तो जिम्मेदारी से दूर हो जाना चाहता है उन्हें काम तो करना है लेकिन मेहनत नहीं करनी है उन्हें सफलता चाहिए लेकिन जो उसके पीछे का काम करने का तरीका है जो औपचारिक था जिसे हम कह सकते हैं वह उसे निभाना नहीं चाहते और साफ-साफ शब्दों में कहूं तो वह सिर्फ ऊपर की मलाई देख रहे हैं मेहनत नहीं।
हसन:- आपने सही फरमाया। कि हम सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे तो बिल्कुल इससे पहले थोड़ा मुश्किल हो जाता था लोगों के बारे में यह जानना कि वह अदब के बारे में क्या रुख अपनाना चाहते हैं वह जो एक बंदिश लगी रहती थी । कैसे अगर हम देखें , हम किसी भी इंसान के साहित्यिक रुझान को समझ सकते हैं कि वह आखिर में क्या चाहता है और उसका क्या रवैया है अदब के लिए। अपने बहुत से सही कहा कि जो काम करने का तरीका है जो सही काम करने का तरीका है उसे लोग पीछे हट रहे हैं जिससे अगर हम शेरो शायरी की हम बात करें तो आज के वक्त में हमें वह सब देखने को मिलता है जिसके अंदर रूल्स जो है उर्दू अदब के और उन्हें नहीं देखे जाते और खुले तौर पर नजर अंदाज किया जाता है तो ऐसी चीज लगातार हमें सोशल मीडिया पर ही देखने को मिल रही है। हम इसे देखें तो यह बहुत ज्यादा आज के दौर में डेमोक्रेटिक हो चुका है क्योंकि पहले अगर हम के वक्त को देखें तो जब आप कुछ लिखना चाहते थे या छापना चाहते थे तो उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती थी। ऐसा नहीं कहूंगा की मेहनत आज नहीं लगती आज भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है अगर आपको उन्हें ट्रेडिशनल तरीके से अपनी किताब को छापना चाहते हैं या फिर अपने काम को आगे पब्लिश करवाना चाहते हैं लेकिन पहले काफी ज्यादा आपको काम करना पड़ता था लेकिन आज के वक्त में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता अगर आप लिखना चाहते हैं , प्रकाशित होना चाहते हैं तो यह काफी ज्यादा आसान हो चुका है सोशल मीडिया के जरिए से लेकिन हर चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी । हमें देखने को खैर लगातार मिले रहे हैं। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वह लोग ज्यादा चीज पसंद कर रहे हैं जो ज्यादा जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए यानि कि जो जल्दी से जल्दी समझ आ जाए उसे वह लोग पढ़ाना चाह रहे हैं लिहाजा बगैर किसी मेहनत के या फिर ज्यादा दिमाग लगाएं। जैसे-जैसे वक्त बदल रहा है काफी चीज नहीं हमें सामने नजर आ रही है।
अरमान:- सोशल मीडिया है या फिर दीगर जो चीज हैं उसे हम एक कह सकते हैं 10% में डाल सकते हैं लेकिन जो 90 फ़ीसदी चीज हैं वह तो वही है जो शुरुआत से चलती आ रही थी वैसी ही है। सकते हैं कि किरदार बदले हैं शक्ल में बदली है लेकिन हरकतें वही है क्योंकि जो चीज हमने अपने बुजुर्गों से सुनी और सीखी इस को ही तो हम कहीं ना कहीं दोहरा रहे हैं मोहब्बत की बात करें यह शेरो ,शायरी ,दोहे हैं यह तो जब से इंसान ने लिखना शुरू किया तब से ही किसी ना किसी रूप में है। आपको नहीं लगता कि कहीं बार इन सब चीजों में कुछ बदलाव नजर आता है ?
हसन:- आपकी बात एकदम सही है इंसान है और काम करने का जो तरीका है और जो हमारा समाज है वह सदियों से एक साथ चला आ रहा है जैसे पहले था ,जो उसकी कहानी है और जो लिखा गया है वह भी तकरीबन एक समान है । उसमें हो सकता है कहानी में नया रुख आ जाए ,कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं किरदार चेंज हो सकते हैं लेकिन कहानी जो है वह एक सी ही है यह तो बात आपकी बिल्कुल सही है। इश्क ,मोहब्बत की बात करें तो पहले का जो वक्त है उसमें भी हम देख सकते हैं जो दो मिलने वाले हैं मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके जो मिलने का जो अंदाज था वह मुख्तलिफ था लेकिन इश्क वही है लेकिन उसका अंदाज है जो उसका तरीका है वह थोड़ा सा बदला होगा उसके इजहार के तरीके मुख्तलिफ हो चुके हैं। मैं आपको अपनी बात कुछ इस तरीके से कह सकता हूं हमारे शायर हैं सैफुद्दीन शेख वह कहते हैं
" सैफ अंदाज़े बयान रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं "
दुनिया में हर बात पहले से कहीं जा चुकी है लेकिन हम जब उसे कहते हैं तो अपने तरीके से थोड़ा अलग बना कर कहते हैं तो यह तो खैर हम सभी इस बात को मानेंगे किस्सा वही है पुराना जो बता रहा है जो इंसान नया है। जैसा कि आपने कहा डिस्टरबेंस वो भी देखने को मिलती है। जिससे आपकी रचनात्मकता व्यक्तित्व को एक नई दिशा मिल सकती है। से कि आप अगर हम बात करें कुदरत आफतों की या फिर हम बात करें उन चीज़ों , परेशानियों इंसानों की वजह से आई हो। हम कह सकते हैं काफी गंभीर किस्म के मसले हैं। लेकिन इन सब के बाद में भी जो आर्ट है अदब है उन्हें अपना एक नया अंदाज मिल जाता है। चाहे अगर बड़ी-बड़ी जंग हमने देखी है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो साहित्य ने एक रुख लिया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह सकता हूं जब नेपोलियन ने रूस पर हमला किया और वह शिकस्त खाकर वापस लौटने लगा। यह देखेंगे कि उसके हमला करने से रूस के अंदर आने से और शिकस्त खाने से वहां के कल्चर में किस तरीके की तब्दीली आई है। लियो टॉल्स्टॉय ने एक बहुत बड़ा नॉवेल लिखा "वॉर एंड पीस" रशियन समाज पर एक बहुत बड़ा नॉवेल है यह और वह शुरू इस तरीके से होता है जब नेपोलियन हमला करने वाला होता है और वो खत्म होता है उसके जाने के बाद इसमें वह इस तरीके से चीज हमें देख लो मिलती है कि वह बहुत बड़ा खतरा था समाज के ऊपर लेकिन उसके ऊपर टॉल्स्टॉय ने लिखा इंसानी तारीख में यह कई बार जरूरी हो जाता है इस तरीके के डिस्टरबेंस होना। इस तरह के डिस्टरबेंस से भी जो अदब है वह अपना रास्ता तलाश ही लेता है इसमें रुकावट दरपेश नहीं होती।
अरमान :- जॉन एलिया अपने अंदाज में कहते हैं
"मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं"
लेकिन आज के वक्त में देखने को मिल रहा है किताबें तो छोड़िए कागज भी कमरों में नजर नहीं आते। कहीं ना कहीं जब हम आम जनता से बात करते हैं तो वह इस मॉर्डनाइजेशन का आधुनिक करण का जो ठीक रहा है वह यूरोपियन कलर के ऊपर मांडने की कोशिश करते हैं लेकिन मुझे ऐसा कि यूरोप के अंदर आज भी पढ़ने वालों की तादाद अच्छी खासी नजर आती है क्योंकि आप खुद वहां आज के वक्त में है क्या फर्क देखते हैं ?
हसन:- यह एक ढंग से देखें तो हो सकता है लेकिन अगर मैं आपको अपनी खुद की बात कहूं तो मेरे घर में किताबें इस कदर हो चुकी है किसी और चीज की जगह नहीं बची है।
आपने कहा यूरोप के अंदर आज भी अच्छी खासी तादात है पढ़ने वालों की तो बिल्कुल सही है और मैं भी लगातार यही चीज देखता हूं यहां पर रहने के बाद में कि जब किसी लंबे सफर पर लोग जाते हैं ट्रेन बसेस के अंदर तो वह किताबें साथ लिया जाते हैं उन्हें नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन अगर हम आम में हिंदुस्तान में देखेंगे तो कभी बहुत कम हमें ऐसे लोग देखने को मिलेंगे की जो साथ में आज भी बस ट्रेन के अंदर किताबें लेकर जाते हैं तो एक हद तक कहा जा सकता है कि मैं थोड़ी कमी आई है और आपने कहा कि यूरोप के ऊपर मांडने की एक कोशिश रहती है तो यह भी गलत है क्योंकि पढ़ रहे हैं लोग और यहां पर पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को यहां पर भी और हिंदुस्तान के अंदर तो खैर एक अपने आप में शुरुआत से ही चल चल रहा है लेकिन वक्त के साथ में कुछ ना कुछ बदलाव तो आए हैं इसका हम कह सकते हैं। तो खैर है ही और जब मैं खुद भी यहां ट्रैवल किया करता था और मेरे साथ वाले भी जिन्हें पढ़ने का शौक था लेकिन यह देखने को बहुत कम मिला करता था कि लोग अपने साथ में ट्रेवल यात्रा के दौरान किताबें ले जाते हैं।
अरमान:- बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और जब मैंने इन्हीं चीजों के ऊपर बातचीत की तो वहां के रहने वालों में यह बताया गया कि वहां कुछ ऐसी चीज भी है जो आमतौर पर हर जगह देखने को नहीं मिलती है जैसे कि कॉर्नर लाइब्रेरीज हैं यानी की गली मोहल्लों के नुक्कड़ के ऊपर आपको बुक शेल्फ देखने को मिलेगी ,ओपन लाइब्रेरी देखने को मिलेगी जिसमें लोग आते हैं अपनी हिसाब से किताबें ले जाते हैं और ईमानदारी के साथ में वापस रख भी जाते हैं तो ऐसी चीज भी वहां रहने वालों से सुनने को मिली।
हसन:- बिल्कुल आपने यह बात सच कही और ऐसा है यहां इंग्लैंड के अंदर भी यह चीज देखने को मिलती है कि बहुत लाइब्रेरीज है पुराने जमाने में जो हुआ करती थी वह आज भी मुकम्मल तौर से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल सही का ईमानदारी से लोग आते हैं अपने हिसाब की किताबें लेते हैं और उसे वापस भी रख जाते हैं तो यह जो सिलसिला है यहां एक लंबे वक्त से चला रहा है जिसमें किसी भी तरह का कोई हम कह सकते हैं दखल किसी दूसरी चीज को हमें देखने को नहीं मिला है यानी कि जैसे वक्त के साथ-साथ कुछ चीज बदल जाती है लेकिन यह उन चीजों में से हैं जो आज तक बरकरार है। जैसे कि जो इंग्लैंड के जो फेमस टेलीफोन बूथ हुआ करते थे तो की जाए तौर पर सभी ने कहीं ना कहीं उनकी तस्वीर देखी होगी लेकिन अब वह हर जगह इतना काम नहीं आते हैं तो उन जगहों पर लाइब्रेरी बना दी गई है किताब में रखते हैं लोग उसके अंदर तो इस तरह से भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह पूरी की पूरी फ्री है यानी कि आपको उसमें एक नया पैसा नहीं देना है अपनी तरफ से सिर्फ ईमानदारी की बात है क्या आप अगर किताब वहां से ले रहे हैं तो उसी हालत में वहां आपको वापस भी रखें। और मैं यह कहूंगा कि जब समिति ने जब यह जानने की कोशिश की कि हमें आगे जाना है थोड़ा कामयाब और ज्यादा होना है तो उन्होंने एक चीज को अपना लिया कि मैटेरियलिज्म उसी को वह आगे भी लेकर चलने लगे यानी कि अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको सिर्फ दो-तीन चीजों में से कुछ चुना होता है यानी की बहुत ही सीमित दायरा बना दिया जाता है । जिस इंसान की जो सच है वह आगे तब्दील नहीं हो पाती है तो यह जो खामियाजा हमें देखने को मिल रहा है वह इन चीजों की वजह से भी है हमारा समाज में कई बार ऐसा लगता है कि बहुत चीज थाम ली गई है उन्हें सीमित कर दिया गया है उसे दायरे से बाहर ही जाने नहीं दिया जाता। जैसे कि अगर हम आमतौर पर भी सुनते आ रहे हैं कि अगर कोई आदमी कामयाब है या फिर उसको यह सुनने के लिए कहा जाता है तो उसके सामने रखा जाता है इन डॉक्टर इंजीनियर यह दो शब्द तो बहुत ही ज्यादा आम हो चुके हैं लेकिन आप यह देखेंगे कि किसी को यह नहीं कहा जाता अदब की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए उसको उसे तरफ बढ़ावा देने के लिए आर्ट कल्चर इन चीजों की तरफ आगे भेजा नहीं जाता जबकि अगर हम प्रोफेशनली भी देखें तो इन सब चीजों में भी काफी स्कोप है ऐसा नहीं है तो यह सिर्फ शौकिया तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं अगर हम इसे दूसरे नजर से देखें तो इसमें भी काफी ज्यादा काम है। मसाला यही आता है कि लोगों का रुझान इसमें काफी कम है।
अरमान:- एक खूबसूरत चीज है आपने कहीं और शुरू में देखा आपने कहा था कि आपको खुद भी लिखना पसंद करते हैं तो ना सिर्फ आपका यह काम तर्जुमा का इसके अलावा जब आप लिखते हैं तो उसका मोटिव क्या रहता है आपकी नजर है?
हसन:- मेरा जो काम है जिस तरह से मैं लिखता पसंद करता हूँ कह सकता हूँ वह काफ़ी मुख्तलिफ रहते हैं। मेरी कोशिश रही रहती है की उनके मोटिव ज्यादातर सोसाइटी के मसलों पर हो लिहाज़ा मुझे पसंद भी है की मैं लिखूं समाज की जो परेशानियां हैं जो चीज हैं उनके ऊपर अपना काम समाज के जो अलग-अलग दौर गुजरे हैं । मैं कभी किसी एक चीज को लेकर मैंने ऐसा नहीं किया । हर तरह का साहित्य मैंने पढ़ा है और मेरी भी कोशिश यह रहती है कि मैं उसी तरीके से अपना काम करूं और मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग भी है कि मेरी कोशिश यह भी रहती है कि मैं उसे ऐतिहासिक रूप से भी देखूं क्योंकि अगर मैं जैसा कि आपको पहले बताया मेरा नॉवेल था उसकी जो इंस्पिरेशन है वह अमीर खुसरो से है लेकिन मैंने उससे लिखा सामाजिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से। इस नॉवेल के अंदर जो मैं कह सकता हूं जो मुख्य चार किरदार हैं वह चारों ही अपने-अपनी कहानी सुनाते हैं अपनी सामाजिक परेशानियों को लेकर।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ।
हसन रिंद - आपका भी बहुत शुक्रिया ।
Pratap Singh Mehta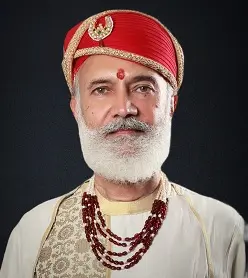
प्रताप सिंह मेहता
प्रताप सिंह मेहता - परिचय
कमांडर प्रताप मेहता भारतीय नौसेना और 1971 के भारत-पाक युद्ध के एक अनुभवी वेटेरन रहे हैं। वे उन्नीसवीं शताब्दी में मेवाड़ राज्य के वरिष्ठ सैन्य कमांडर लक्ष्मीलाल मेहता एवं निष्ठावान प्रधान मंत्री रायपन्नालाल मेहता, सी.आई.ई., के प्रपौत्र हैं। कमांडर मेहता समुद्री विज्ञान में भारतीय नौसेना अकादमी के स्नातक हैं, लेकिन वे हमेशा राजपपूताना के इतिहास के बारे में बहुत भावुक हैं।
इतिहास के प्रति उत्साही होने के नाते, वह अपने पूर्वजों के इतिहास के एक उत्सुक पर्यवेक्षक भी हैं। आज वह एक मोटिवेशनल कोच, ट्रेनर और स्पीकर हैं।
कमांडर प्रताप मेहता की पुस्तक, ‘राजपुताना क्रॉनिकल: पराक्रम और परम्परा - राजपुताना के विस्मृत शासकों और मंत्रियों के शौर्य की ऐतिहासिक गाथा’ (2023), इसी दिशा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।यह उन्हीं की लिखित पुस्तक, ‘Rajputana Chronicles: Guns and Glories - The thousand-year story of the Bachhawat clan’ (2016) का हिंदी अनुवाद है। उनके इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कार्य का प्रकाशन इसी दिशा में उल्लेखनीय है।
राजाओं और राज्यों के बारे में पर्याप्त इतिहास लिखा गया है, लेकिन उनकी इस पुस्तक के माध्यम से हमें समकालीन विस्मृत व अल्प ज्ञात शासकों उनके मंत्रियों के पराक्रम और परम्परा की अनकही ऐतिहासिक गाथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अपने अनुभवों की कटुता के बावजूद उनका जीवन विनम्र भाव से चला है। बच्छावत वंश की उत्पत्ति, अतीत और वर्तमान में, दस शताब्दी से ऊपर राजपपूताना के देलवाड़ा, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर राज्यों के शासकों एवं वहां के प्रशासन से किसी न किसी रूप में निकटस्थ रहा है। जीवन के व्यापक घात-प्रतिघात के बीच उनकी यह कहानी, इतिहास भी है और इतिहास से सीखा गया सबक भी। राजपुताना के इतिहास पर शोधकर्ताओं औरजिज्ञासुओं के लिए तो यह पुस्तक एक अत्यंत संवेदनशील दस्तावेज है
कैप्टन मेहता कहते हैं -
मैं राजस्थान से हूं, उदयपुर में पैदा हुआ और पला-बढ़ा। हालांकि मैं अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान जयपुर और बीकानेर में भी रहा हूं, लेकिन अब मैं 1994 में भारतीय नौसेना से अपनी प्रारंभिक सेवा निवृत्ति के बाद से मुंबई में रहता हूं। मैंने सेंट जेवियर्स जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय और बाद में भारतीय नौसेना अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। मैंने शैल लोढ़ा मेहता से शादी की और मेरे दो बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, प्राची और नकुल, दोनों विवाहित हैं और मीडिया पेशेवरों के रूप में बस गए हैं। नकुल मेहता सुप्रसिद्ध टेलीविजन स्टार और कार्यक्रम संचालक है ।
बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री रहे बच्छराज जी के वंशज नौ सेना के पूर्व कमांडर और इतिहास विज्ञ प्रताप सिंह मेहता से खास बातचीत ।
मैंने अपने पूर्वजों का एक हज़ार साल का इतिहास लिखा है - प्रताप सिंह मेहता ।
अरमान नदीम : आपने भारतीय नौसेना में आपने सेवाएं दी जिसमें आपने 1971 के भारत-पाक युद्ध में भाग लिया और लगातार देश की सेवा की लेकिन भारतीय नौसेना में जाने की सबसे बड़ी प्रेरणा कौनसी रही।
प्रताप सिंह मेहता :- मैं बचपन से ही फौज में जाना चाहता था क्योंकि मेरे पूर्वज भी फौज में कमांडर रहे हैं और रियासत काल में प्रधानमंत्री रहे जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पावर थी जिन्होंने युद्धों में भाग लिए थे । तो बचपन से ही उनकी कहानियां सुनते-सुनते में बड़ा हुआ और वहीं से मुझे फौज में जाने की प्रेरणा मिली। 1970 में नेवी में मेरी जॉइनिंग रही
अरमान :- जब आप नेवी में थे उस दौरान किसी तरह की कठिनाइयां सामने आई?
प्रताप सिंह मेहता :- नेवी के टाइम पीरियड में ऐसी कोई बड़ी कठिनाई नहीं आई मुझे । बहुत इंटरेस्टिंग लगता था । दिक्कत नहीं आई और ट्रेनिंग के दौरान ही 1971 में कराची साइड पोस्टिंग थी । नेवी में स्पेशलाइजेशन किया नेवल एविएशन में । हेलीकॉप्टर के टेक्निकल ऑपरेटर और हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग के लिए मैं 1979 में रशिया भी गया लगभग 15 से 17 महीने वहां रहा । हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग ली और भारत का फर्स्ट मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत पर हेलीकॉप्टर के साथ तैनात था । नेवी में 25 साल नौकरी की और 1994 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। और नेवी के तो कई किस्से है जैसे हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हुए कई बार तो ऐसा लगता था कि बस अब गए जैसे कई बार इंजन में कुछ दिक्कत आ जाया करती कभी कुछ तो कभी कुछ हुआ लेकिन एक अच्छी ट्रेनिंग रही और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट्स ऑफ माइंड और सही वक्त पर सही डिसीजन लिए गए । नेवी का वक्त काफी खूबसूरत रहा आखिरी दिनों में मैं 1991 में मिसाइल बोर्ड का स्क्वाडन
कमांडर भी रहा । मैं आपको बताना चाहूंगा हेलीकॉप्टर स्पेशलाइजेशन का मतलब यह नहीं के शिप में आप नहीं जा सकते हैं नेवी में यह कह सकते हैं कि वह तो आपका बुनियादी पेशा है और स्पेशलाइजेशन नेवल एवियशन जिसमें हेलीकॉप्टर उड़ाना मेरा काम था उसी के साथ मिसाइल बोर्ड का मुझे कमांडर भी बनाया विशाखापट्टनम में वह भी बहुत कामयाब रहा है।
अरमान नदीम :- आपने किताब लिखी पराक्रम और परंपरा यह लिखने की क्या वजह हुई और जरूरत महसूस क्यों हुई ।
प्रताप सिंह मेहता :- यह बहुत ही रोचक सवाल है आपका मैंने इससे पहले एक अंग्रेजी में किताब लिखी थी राजपूताना क्रॉनिकल्स गंस एंड ग्लोरी इसका हिंदी रूपांतरण है पराक्रम और परंपरा । मैंने अपना यह रिसर्च शुरू किया की जैसा कि मैंने आपको बताया मैं बचपन से ही अपने पूर्वजों की कहानी सुनते हुए बड़ा हुआ । और अपने पूर्वजों के ऊपर काम किया जाए ये बात लंबे समय से दिमाग में थी। यह भी आया कि पता लगाया जाए कि हम कहां से थे कैसे थे मुझे इसमें काम करने में इस पर रिसर्च करने में 20 साल से ज्यादा का वक्त लगा 2016 में पहली पुस्तक जो अंग्रेजी में थी उसका प्रकाशन हुआ अगर आप सवाल करें कि मुझे इस किताब में इतना वक्त क्यों लगा तो आपको मैं बताना चाहूँगा की मैंने इसमें यह नहीं लिखा कि किस राजपूताना के शासक ने क्या किया क्या नहीं किया वह आपको आम इतिहास की किताबों में मिल जाएगा राजपूताना में जितने भी किंगडम है उनको लाने वाला कौन था क्योंकि सारे के सारे राजा इतने सक्षम नहीं थे कि वह पूरा प्रशासन संभाल सके सारी चीजों पर नजर रख सके । उनके पास ऐसे विशेष व्यक्ति हुआ करते थे जिन्हें वह अपना प्रधानमंत्री ,सेनापति कमांडर बनाया करते, मंत्री बनाया करते थे इतिहास में उन लोगों को इतनी जगह नहीं दी गई। मेरी रुचि इसमें थी की उन लोगों के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें उजागर किया जाए ।ऑथेंटिक रिसर्च हो, मुझे आपको यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है जब किताब आई इसे लगभग तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसके बाद काफी स्टूडेंट्स ने कॉल किया ,कांटेक्ट किया कुछ हिस्ट्री के प्रोफेसर्स ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि आपकी किताब पढ़ कर एक ऑथेंटिक इनफॉरमेशन हमें मिली और कहा कि हमारे जो पी एच डी के स्टूडेंट हैं हम उन्हें ये किताब रिफरेंस के तौर पर पढ़ने के लिए सजेशन दे रहे हैं। मैंने अपने पूर्वजों का एक हज़ार साल का इतिहास लिखा है इस किताब में।
अरमान नदीम :- आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही के इस तरह की चीजों में वक्त लगता है और एक ऑथेंटिक इनफॉरमेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए लेकिन अफसोस के साथ मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सभी इतिहासकार, सभी लेखक इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने इस तरह की थिअरीज दी जिसके बाद में एक बड़ा विवाद पैदा हुआ और सांप्रदायिक रूप से लोगों के मन में संकट पैदा किया, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा पी एन ओक का उन्हें मैं उन्हें एक फिक्शन राइटर कहना ज्यादा पसंद करूंगा उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि ताजमहल पूर्व में तेजो महालय था ।और उसके बाद में एक बड़ा विवाद पैदा हुआ और आज भी लोगों के मन में इस तरह की की शंकाएं बनी हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे।
प्रताप सिंह मेहता :- जी यह चीज विवाद वाली हैं और आपका कहना सही है ।लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि कौन कितना सही है या कितना गलत है निजी ओपिनियन है आपको एक बात यह भी बताना चाहूंगा इतिहासकार जब कुछ लिखता है तो उसका अपना एक नजरिया होता है , अकबर के साथ जहांगीर के साथ या किसी भी मुगल बादशाह के साथ जो स्टेट पॉइंट्स उनके साथ रहा करते थे तो जब उनके बारे में लिखते तो अपने-अपने नजरिए से उनका वर्णन करते। तो यह विवादित चीज हैं। एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा की , जैसे कोई राजा सुंदर नहीं दिखता लेकिन जब उसका वर्णन होगा तो इस तरीके से किया जाएगा कि उसने क्या पोशाक पहनी है या उसके हाथ में क्या है एक अलग तरीके से उसे बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। आपको वाकया बताना चाहूंगा की बीकानेर के शासक थे राजा राय सिंह और प्रधानमंत्री थे करमचंद बच्छावत, बहुत ही स्टेट फॉरवार्ड और ईमानदार व्यक्ति थे लेकिन राजा राय सिंह बड़े गुस्से वाले थे उनको तारीफ़ बहुत पसंद थी । एक बार किसी से खुश होकर राजा ने अपने दीवान करमचंद जी को कहा कि उन्हें 100000 मुद्राएं दे दी जाए तो उस वक्त बच्छावत जी ने कहा कि महाराज प्रशंसा हुई है अच्छी बात है लेकिन आप कुछ और दे दीजिए गमछा दे दीजिए अंगूठी दे दीजिए , मुद्राएं बहुत भारी रकम है देने के लिए तो राजा जी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं और ऐसा होना चाहिए । क्योंकि करमचंद जी काफी समझदार भी थे तो उन्होंने एक लाख स्वर्ण मुद्राओं की बोरियां या पोटली कहें इस तरीके से बंधवाई की पूरा दरबार भर सा गया और जब उन्हें कहा गया है आप अपने हाथ से ही दे दीजिए और जब राजा जी ने वह दृश्य देखा तो उन्होंने कहा कि यह तो वाकई में बर्बादी होगी तो इस तरह की चीज भी हुआ करती थी।
अरमान नदीम :- एक घटना और हुई थी बच्छावत वंश के साथ बीकानेर राजवंश के द्वारा जो आपने अपनी किताब में भी अंकित की है वह घटना क्या हुई थी ।
प्रताप सिंह मेहता :- करमचंद जी को यह पता चला कि राजा राय सिंह और राजा के कान भरने वालों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया है और यह उन्हें मालूम हो गया कि वह लोग उन्हें जान से मार देना चाहते हैं यह सब घटनाएं शुरू हुई जब बादशाह अकबर ने राजा राय सिंह को बुरहानपुर की तरफ पोस्टिंग की और उन्हें कई साल वहां बुरहानपुर रहना पड़ा राजा की गैर उपस्थिति में करमचंद जी ही बीकानेर का राज्य चलाते थे और बहुत सुचारू रूप से चलाया करते थे ।राजा राय सिंह जी ने करमचंद जी को आदेश दिया कि एक नए किले का निर्माण शुरू करवाया जाए जिसे आज जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। जब नक्शा तैयार हुआ किले का तो उन्होंने कहा कि आप भूमि पूजन के लिए आइए बीकानेर लेकिन उस वक्त राजा राय सिंह ने कहा कि भूमि पूजन भी तुम ही कर लो मुझे आने में विलम्ब हो सकता है। और किले शुरू में नाम पड़ा चिंतामणि दुर्ग । और यही नजदीकियां देखकर जो राजा के करीबी थे उन्हें परेशानी भी हुई और उन्होंने एक अलग तरीके से राजा राय सिंह के कान भरने शुरू किया और उन्हें यह कहा कि यह तो अब बीकानेर राज्य पर कब्जा करना चाहता है । यहा तक कहा कि आपको राज्य से निकाल देना चाहता है और वहीं से राजा राय सिंह ने लोगों की बातों में आना शुरू किया और एक प्लान बनाया कि करमचंद बच्छावत जी को खत्म कर देना है। इस बात की हवा करमचंद जी को भी पड़ गई और उन्होंने काफी आदर के साथ राजा राय सिंह को पत्र लिखा और जब राजा सिंह वापस बीकानेर राज्य पधारे तो उन्होंने कहा कि अब आप मुझे इजाजत दीजिए मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं अब रिटायर्ड होना चाहता हूं । आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं उसके बाद वह अपने ननिहाल मेड़ता साइड चले गए और बाद में उन्होंने अपनी सेवाएं बादशाह अकबर को दी लेकिन जब राजा राय सिंह की मृत्यु नजदीक आई तो उन्होंने अपने पुत्र सूरसिंह को बुलाया और कहा की अब मेरा वक्त नजदीक है लेकिन तुम्हें किसी भी तरीके से करमचंद को वापस बीकानेर बुलाना है और उससे बदला लेना है । राजा की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र सूरसिंह ने गद्दी संभाली और यही दिमाग में रहा कि कैसे भी करके करमचंद से बदला लेना है और जब बादशाह अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठे उस दौरान सुरसिंह दिल्ली पहुंचे जहांगीर को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए और क्योंकि करमचंद जी और उनका परिवार भी उस वक्त दिल्ली में ही थे तो सुरसिंह ने वहां उनसे और उनके परिवार से मुलाकात की और कहा कि आपने हमारे खानदान की काफी सेवा की है बीकानेर राज्य की काफी सेवा की है आप वापस बीकानेर पधारिए हम आपको मंत्री बनायेंगे और सुविधाए देंगे । इस तरह के लालच उन्हें देने शुरू किए ताकि वह वापस से बीकानेर आ जाए । ये बाते सुन कर करमचंद जी ने कहा कि मैं इस बारे में विचार करूंगा लेकिन वह कभी बीकानेर नहीं गए और उन्होंने अपने दोनों लडको को यह साफ तौर पर कहा कि कभी इस के लालच में मत आना और भूल कर भी बीकानेर जाने का विचार अपने दिमाग में मत लाना । सूरसिंह के आंसुओं पर मत जाना यह मगरमच्छ के आंसू हैं इस बहकावे में मत आना उन्होंने आखिर तक अपने बच्चो को यही सलाह दी लेकिन जब करमचंद जी की मृत्यु हुई उसके बाद में बीकानेर से फिर बुलावा आया और कहा कि हम आपको मंत्री बनायेंगे और इस बार इनके पुत्र अपने पिता की बात भूल गए और वह अपने परिवार समेत बीकानेर चले गए । बीकानेर जाने के बाद में उन्हें मंत्री बनाया गया काफी शोहरत मिली और उन्हें भी एक विश्वास होने लगा कि अब सब कुछ सही है और यह पुरानी बातें भूल चुके हैं वह एक हल्के मन से वहां रह सकते हैं । सोचा कि हमें राजा जी का सम्मान करना चाहिए उन्हें अपनी हवेली पर बुलाना चाहिए । हवेली में जब राजा आए तो सब साथ बैठे और फिर उसी रात को 4000 राज्य के सैनिक आए और पूरे चौक को सभी हवेलियों को घेर लिया और जो भी बच्छावत नज़र आया उसे वहां मार दिया बच्चे बुजुर्ग,महिलाएं सभी को मार दिया और जो बच सकते थे इधर-उधर भाग गए अपनी जान बचाकर और उस वक्त महिलाओं ने वहां जल जौहर किया । और जो गर्भवती महिला हुआ करती है उसे जौहर की अनुमति नहीं होती है और उसे एकदम से मारा भी नहीं जाता है । भागचंद जी की पत्नी वह गर्भवती थी । पिता थे भामाशाह,उनके जो सेवक थे वह उसे वहां से निकाल के सबसे पहले तो करणी माता की मंदिर लेकर गए और वहां से फिर वह उदयपुर की तरफ चली गई और उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया । नाम पड़ा भानु मेहता । क्योंकि करमचंद जी को मेहता की उपाधि मिली थी । उदयपुर में रहा करते हैं वह मेहता सरनेम का इस्तेमाल किया करते हैं। क्योंकि बाकी जो बच्छावत है वह सिर्फ बच्छावत ही लगाते है । मेहता की उपाधि है वह केवल करमचंद जी को ही मिली थी जो की बादशाह अकबर ने उन्हें दी थी तो जो उनके जो वंशज है यानी कि डायरेक्ट जो उनके हैं वही मेहता की उपाधि लगाया करते हैं।
अरमान नदीम :- लेखक हो पत्रकार हो या साहित्यकार हो वह विचार परख लेखन से दूर होकर सिर्फ अपने विचारधारा थोप रहे हैं।
प्रताप सिंह मेहता :- विचार परख लेखन से आपका क्या तात्पर्य है?
अरमान नदीम :- विचार परख लेखन से मेरा तात्पर्य है कि न्याय संगत बात होनी चाहिए विचारधारा कुछ भी हो सकती है । न्याय संगत बात तब होगी जब मैं अपनी विचारधारा के विपरीत जाकर भी सही और गलत का फैसला करूं ।
प्रताप सिंह मेहता :- मैं इस बात से सहमत नहीं हूं विचार परख और विचारधारा आपके अनुसार जो सही या गलत बात करे?
अरमान नदीम :- जी नहीं, न्याय संगत अगर हम इसे और सरल बनाकर बात करें तो न्याय संगत बात होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर विचार को अपनी थ्योरी में जगह ने दें सभी की बात सुनी जाए और विवादित मुद्दों को सुलझाने पर काम किया जाए।
प्रताप सिंह मेहता :- विचार परख लेखन,विचारधारा, न्याय संगत जो भी आपने डिफाइन किया ये काम है न्यायाधीश का उसके पास न्याय करने की क्षमता होती है । निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों को सुनते हैं और फिर अपना जजमेंट देते हैं। हर लेखक की अपनी एक विचारधारा होती है सही या गलत वह उसकी एक बात अलग है । लेकिन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए हम कौन होते हैं कहने वाले बहुत सी फिल्में बन रही है जो विचारधारा के विपरीत है कैसे विचारधारा प्रकट करो अगर जिस किसी दूसरे को आघात हो या चोट पहुंचे तो फिर आपको उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए । आज के वक्त में डेमोक्रेसी की भी सभी की अपनी-अपनी डेफिनिशन हैं मुझे लगता है होती रहेगी है क्या अगर आप इसे जितना बचने की कोशिश करोगे तो लोग उतना ही उत्तेजित होंगे। इसका एक ही हल है कि हमें शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए शिक्षा का क्या मतलब जब सिर्फ यही है की डिग्री हासिल कर ली गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। यह नहीं होना चाहिए।
अरमान नदीम :- व्यक्ति में मैच्योरिटी होनी चाहिए परिस्थिति को समझने के लिए ।
प्रताप सिंह मेहता :- इस शब्द को भी डिफाइन करना पड़ेगा यह एक बहुत ही सुंदर शब्द है। जिसका मतलब कुछ नहीं है मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आदमी का रवैया मानवता के हित में हो। किसी देश प्रधान के हित में नहीं यह एक या कम्यूनिटी प्रधान के हित में नहीं हो वह पूरी मानवता के लिए काम करें ।यह रवैया आपको मिलेगा दुनिया की हर आम फोर्सज में के लोग होते हैं । मैच्योरिटी होनी चाहिए तो हर एक व्यक्ति के जहां में दिमाग में इसकी भी अलग-अलग परिभाषा है घर के 10 साल की उम्र वाला अभी मेच्योर है कोई कहेगा 50 साल वाला भी है महत में है अभी। रिस्पांसिबिलिटी आपको अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए l फिर बात आती है पंक्चुअलिटी की समय का पाबंद जिसे कहा जाता है जैसे हमने इस वार्ता के लिए 9:00 बजे का वक्त फिक्स किया और इस वक्त में हमने अपनी बातचीत शुरू की । ना तो हमने 9:00 से पहले एक दूसरे से बात की और ना ही हमने 9:00 बजे के बाद बात शुरू की तो यह आपकी कहे या मेरी यह एक पाबंदी है एक पंक्चुअलिटी है अपने कार्य के प्रति। आज से कम से कम 10 से 15 साल हमें और लगेंगे अगर हमारे यहां नैतिकता, करेक्टर बिल्डिंग की शिक्षा लोगो को दी जाए।
अरमान नदीम - "शब्द संवाद" के लिए अमूल्य समय देने के लिए आपका आभार ।
प्रताप सिंह मेहता - जी आपका भी बहुत आभार ।
Mansoor Hasan
मंसूर हसन
पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी के सदस्य, कोलकाता खिलाफत कमेटी के उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता मंसूर हसन से शब्द संवाद के लिए अरमान नदीम की खास बातचीत ।
1992 में शिव मंदिर हिफ़ाज़त का जिम्मा हमारे कंधों पर रहा :- मंसूर हसन
अरमान:- मौजूदा वक्त में आप सियासत के साथ-साथ अदब से भी जुड़े हैं. मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि उर्दू अदब में आपकी दिलचस्पी कैसे हुईं ?
मंसूर हसन:- दिलचस्पी तो स्कूली वक्त से ही थी और उस वक्त से ही मज़ामीन लिखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां साप्ताहिक अखबार निकला करता था। शुरू में उसमें भी अपने मजमून और कहानी भेजा करते थे तो फिर एक निरंतरता बनी। जब उसमें कलाम शाया हुआ तो हौसला अफजाई भी हुई । लगातार काम होता रहा और जब कोलकाता रहने के लिए आए तो यहां पर भी एक बहुत मशहूर अखबार था "मशरिक़" इसमें भी भेजा कलाम और जब शाया हुए मजमून तो एक जो कंटिन्यूटी थी वह हमेशा के लिए हो गई । और रही बात सियासत में शुरुआत की तो जब कॉलेज में एडमिशन लिया वही से सियासत भी शुरू हो गई और सियासत में आने का मकसद यही था कि आम आदमी की परेशानी दूर हो। कोशिश हमेशा से यही रही की कोई तकलीफ में ना रहे जितना बन पड़े अपनी तरफ से काम किया जाए । साफ सुथरा काम हो ,फसाद दूर करने की कोशिश रहती है और परेशानियों से लोगों को निजात देने की कोशिश रहती है। तो हमेशा से यही मंसूबा रहा सियासत का भी। मजहबी तौर से हो, जाती हो, सबको एक करने की कोशिश हमेशा से बनी रही और मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब भी रहे है क्योंकि जिस तरीके से आज के वक्त में लोग भटक रहे हैं जब बात होती है तो लगता है कि अगर समझाइश हो बेहतर तरीके से तो फसाद से बचा जा सकता है। और इसी से जुड़ा एक वाकया आपको बताऊं 1992 के जो फसाद हुए उसमें हमारे यहां एक मंदिर है शिव मंदिर है उसकी हिफाजत का जिम्मा हमारे कंधों पर रहा इतने भयंकर फसाद में भी उस मंदिर की हिफाजत हमने की और उसमें हम सभी थे ,मेरे बड़े भाई साहब भी मौजूद रहे । हिफाजत की मंदिर की। इसी तरह मैं आपको भाईचारे की एक मिसाल और दूं तो यहां कलकत्ते के अंदर बहुत बड़ी जमात होती है ईद की वहां उसे मैनेज करना और उसी तरीके से दूसरे दीगर काम जैसे ब्लड डोनेशन के कैंप लगवाना तो हर जगह कोशिश रही के काम हो । बड़े से बड़े काम हुए । अगर छोटे काम भी देखे जाए तो जैसे राशन कार्ड के कोई मसले हो गए या फिर कुछ और समस्याएं तो लगातार इन चीजों से जुड़ाव बना रहा ,अभी बना हुआ है तो कहीं ना कहीं से लोगों का जो प्यार है मोहब्बत है वह भी बरकरार है इन्हीं सब चीजों की वजह से।
अरमान:- वाकई आपके काफी शानदार काम है। आपकी सियासत किस तरह की है? आपकी नज़र में क्या मतलब है सियासत का ?
मंसूर हसन:- बिल्कुल जैसा मैंने कहा सियासत में शुरुआत से ही दिलचस्पी थी और उसके ज़रिए काम करने का जुनून था। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत हुई कॉलेज में कांग्रेस ज्वाइन किया। वार्ड में पहले जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। फिर वहां से जब हमने काम शुरू किया तो जिले के अंदर जनरल सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे । लगातार संगठन को मजबूत करने का काम किया और अपनी तरफ से भी लगातार छात्रों के लिए काम जारी रखा। छात्र परिषद के बाद में यूथ कांग्रेस ज्वाइन हुई और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए। फिर एक वक्त आया जब तृणमूल कांग्रेस जाने का विचार बनाया । अभी चार साल पहले तक हम अपने वार्ड के प्रेसिडेंट रहे।
अरमान:- सियासत को आपने किस तरीके से लिया चुनाव शुरुआत से ही दिमाग में था या फिर कोई ऐसी परिस्थितियों बनी जिससे सियासत में मजबूरी में आना पड़ा?
मंसूर हसन:- जैसा मैंने आपको कहा शुरुआत से ही मन बना रहा और जन सेवा का स्टूडेंट लाइफ से ही। मैं आपको बताऊं जब हम छोटे थे जब किसी संगठन से जुड़े हुए भी नहीं थे तब भी चाहे कोई भी रैली आज से पास से गुजरती तो उसमें जुड़ जाया करते थे और वहां लोगों को देखा करते थे।
अरमान:- आप उर्दू अदब से भी जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि अदब को भी फैशन का हिस्सा बनाया जा रहा है । सभी तरह के साहित्य को जैसे हम अगर सोशल मीडिया की बात करें ,फोन से, इंटरनेट से जुड़ी चीज की हम बात करें , उर्दू शायरी के ऊपर के कुछ साउंड इफेक्ट जिस तरीके से लगाकर अपने मन मुताबिक उसे प्रेजेंट करने की कोशिश रहती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूं कि एक बंदा जिसे आज भी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी साउंड इफेक्ट लगाकर कहने को तो हम उसे कह सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा देखा जा रहा है वह सेल्फ प्लेजर वाली चीज साहित्य में जबरदस्ती डाली जा रही है और जो नए एकदम यूथ है वह कहीं ना कहीं उसी को मेंन स्ट्रीम का हिस्सा मान रहे हैं तो उसे एक आदत पर भी असर पड़ता है और नौजवानों की जो मानसिकता है उसे पर भी इसका असर पड़ रहा है।
मंसूर हसन:- बिल्कुल बिल्कुल यह आपने बहुत सही बात कही है और यह मैं भी चीज महसूस कर रहा हूं और मैं उर्दू अकादमी से 2011 से जुड़ा हूं। हमारी कोशिश पूरी रहती है कि उर्दू को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और हमें हालिया वक्त में हिंदी और बंगाली को भी साथ में लेकर चलना है और हम इसमें लगातार काम कर रहे हैं उर्दू के लिए अपनी तरफ से अकादमी भी पूरी शिद्दत से इसमें अपना योगदान दे रही है। हिंदी और बंगाली में उसका जो ट्रांसलेशन है वह बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और उर्दू अकादमी बहुत बेहतरीन काम कर रही है । मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल में वह स्कॉलरशिप भी मुहैया करवाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकादमी अपनी तरफ से कोचिंग भी करवाती है, स्पॉन्सरशिप भी देती है स्टूडेंट को और जो उर्दू के शायर हैं जिन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है तो उन्हें आगे बढ़ने का भी काम इसमें जोड़ा गया है। उनकी किताब पब्लिश करवाई जाती है ।अकादमी जानिब से मुशायरा होता है। और एक चीज आपने बहुत ही सही कही की जो चीज सेल्फ प्लेजर से साहित्य की तरफ बढ़ जाए तो वह बड़ी नुकसानदायक हो जाती है और मैं यह आपको कहना चाहूंगा कि इसके लिए भी काम करना चाहिए और लोगों को असल साहित्य जो वास्तविक अदब है उसे जोड़ना चाहिए। जिससे उनकी सोचने की और तर्क करने की जो ताकत है और जहनी ताकत है उसमें इजाफा होगा। और इसमें अदब में भी लोग जो काबिल हैं आपको यह देखने को मिलेगा वह फाइनेंशली इतने ताकतवर नहीं है तो यह भी एक समस्या हमें देखने को मिलती है। और उसी के लिए उर्दू अकादमी कोशिश कर रही है कि जो अदीब है उन्हें रिकॉग्निशन दी जाए । काबिलियत को देखते हुए आगे लाया जाए। और अगर मैं अकादमी की ही बात अगर कहूं तो हमारी लगातार कोशिश भी रहती है कि नए लोग हैं जो युवा हैं उन्हें अदब से जोड़ा जाए ।तो इस तरीके से अकादमी काम कर रही है लगातार अपने स्तर पर और लोगों को जोड़ा जा रहा है।
अरमान :- आप खुद भी लिखना पसंद करते हैं और काफी खूबसूरत कलाम है आपका। लेकिन मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या संदेश रहता है अपने लेखन के माध्यम से अपने पाठकों के लिए। फिर चाहे मजहबी फसाद से निजात का मामला हो या और कोई सामाजिक परेशानी।
मंसूर हसन:- जो सबसे बड़ी चीज मेरे कलाम में अगर आप देखेंगे तो आपको साफ़ साफ़ नज़र आयेगा की तरबियत का कितना असर होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा मैंने लिखा था स्टूडेंट लीडर के कर्तव्यों पर और उसमें लिखा कि अगर आप स्टूडेंट लीडर हैं तो आप उस वक्त क्लास के अंदर दाखिल हुए जिस वक्त क्लास शुरू भी ना हुई हो यानी कि वक्त से पहले आप क्लास में मौजूद हो जाए। कुछ बच्चे अकड़ के खड़े रहते हैं और बात नहीं मानते तो इस तरह की चीज हमने शुरुआती दौर में लिखी थी। समाजी मसलों पर खूब लिखा खास तौर पर नौजवानों को ध्यान में रखकर ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिल सके ।
अरमान :- आप जैसी शख्सियत जो सही मायने में समाज के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई है फिर चाहे वह सियासत हो या फिर अदब के ज़रिए। अदब के जरिए से और लिहाजा उसे इंसान का नजरिया भी थोड़ा अलग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति का प्रभाव अलग ढंग से हमें देखने को मिलता। लेकिन जब अदब में ही सियासत होने लगे तो आप उसे कैसे देखेंगे। फिर चाहे वह अकादमियों को लेकर कुछ गलतफहमियां हो या फिर और दीगर कुछ मसले। अकादमी वाकई में राज्य सरकारों की गिरफ्त में रहती है या फिर कुछ आजादी है अभी।
मंसूर हसन:- ज्यादातर की अगर बात कही जाये तो गिरफ़्त में रहती है। बात आपकी बिल्कुल सही है और इत्तेफाक रखता हूं। और अगर बंगाल अकादमी की मैं बात करूं तो उसे छूट है ममता बनर्जी के हुकूमत में और मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 18 करोड़ की ग्रांट मिलती है अकादमी को और काफी हाथ खुले हुए हैं और जो पैसा है वह भी जहां पहुंचना चाहिए सही ढंग से वहां पहुंच रहा है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं अदब हो या सियासत वह मौजूदा वक्त में बहुत बदलाव हुए हैं ।
देखेंगे तो बहुत से ऐसे शायर है लेखक हैं जो अपने लिखने में अपने काम में सरकार की हम नवाही करते हैं। और इन चीजों से हम देख रहे हैं समाज में जो आपसी फूट पैदा हो रही है वह बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। और जैसे अगर हम बात करें कई बार जो गलत खबरें हैं फैलाई जाती है तो उनसे भी बड़ी-बड़ी समस्याएं सामने आती है । तो यह कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेदारी है और लिखने वालों को भी इसका महत्व समझना होगा कि उनके शब्द कितने प्रभाव डालते हैं समाज के ऊपर। और लगातार ही हम देख रहे हैं क्या आज के वक्त में जो यह हरकतें हैं जो घटनाएं हैं वह हमें ज्यादा देखने को मिल रही है जो आज से पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी। और यही कारण माने जा सकते हैं जिसकी वजह से अदब में भी सियासत बड़ी है। और काफी फर्क हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि सभी सरकार के लिहाज से काम करना शुरू कर चुके हैं।
अरमान :- आपने कहा कि अदब में सियासत नहीं होनी चाहिए यह बहुत सही बात है और कहा की बंगाल उर्दू अकादमी को आजादी है वह अपने हिसाब से फैसला ले सकती है तो उर्दू अकादमी बंगाल उर्दू के लिए क्या कर रही है?
मंसूर हसन:- बंगाल की उर्दू अकादमी उर्दू को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रही है वह मैं आपको बता सकता हूं जिसका हेड क्वार्टर आज के वक्त में कोलकाता में है हमने दो ब्रांचेस और बनाई है। बंगाल उर्दू अकादमी की कोशिश हमेशा से यही रहती है कि वह बंगाल के कोने - कोने में जाकर प्रोग्राम करें जिससे लोग अकादमी से जुड़े साहित्य अदब से जुड़े उर्दू से जुड़े। और जहां-जहां पर भी लोग उर्दू पढ़ते हैं समझते हैं तो वहां तक इसे पहचाने का जिम्मा उर्दू अकादमी ने उठाया है और वह लगातार एक बेहतर ढंग से अपना काम कर रही है और जो काबिल लोग हैं उनसे भी लगातार संवाद किया जाता है मशवरे लिए जाते हैं कि और किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं।
अरमान :- आपने साहित्य अकादमी के काफी अच्छे काम गिनवाए और आपने कहा कि वह लगातार प्रोग्राम करती है और जो लेखक हैं जो शायर हैं उन्हें जोड़ा जाता है लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता सिर्फ उसे लिखने वाले जो शायर हैं या जिन्हें लोग जानते हैं वही जुड़ रहे हैं आम आवाम जो अदब में दिलचस्पी रखती है उन्हें अकादमी कैसे जोड़ती है?
मंसूर हसन:- जी बिल्कुल आपने सही कहा और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी अकादमी में सिर्फ अदबी लोग ही नहीं जो पहले से जुड़े हुए हैं। हम लगातार नए लोगो को भी जोड़ने का काम कर रहे है जैसा मैंने आपको कहा नए लोगों को भी जोड़ते हैं और जो आम आवाम है उर्दू पढ़ती है ,पढ़ना पसंद करती है उन्हें भी लगातार हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। बात करें तो उसमें सभी लोग हैं फिर चाहे वह पार्टी से जुड़े हुए लोग वह भी इंटेलेक्चुअल जो है वह इंडिविजुअल होकर भी इसे अपना आपको जुड़ा महसूस करते हैं और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम कोने कोने पर जाकर प्रोग्राम करते हैं फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उसमें आम जनता सबसे ज्यादा वहां से जुड़ती है अदबी कार्यक्रमों से। पॉलीटिशियंस खासी दिलचस्पी लेते हैं तो आप इसे सिर्फ अदबी लोगों से जुड़ा नहीं कह सकते इसमें सभी लोग हैं सामान्य से लेकर बड़े से बड़े स्तर तक का व्यक्ति इसे अकादमी से जुड़ा है और उनके प्रोग्राम को अटेंड करता है।
अरमान:- आज के वक्त में आप भी उर्दू अकादमी के एक मजबूत सदस्य हैं तो आपकी नजर में मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी चुनौती अकादमी के लिए क्या पेश आ रही है?
मंसूर हसन:- उर्दू के लिहाज़ से अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी परेशानी कहीं हद तक यह भी नजर आती है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी की तरफ धकेल रहे हैं ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत है। भारी दुनिया के लिए वह बहुत जरूरी हो सकती है लेकिन हमें अपनी जो ज़बाने हैं उन पर भी बच्चों को आगे करना चाहिए उन्हें समझना चाहिए क्योंकि अगर शुरुआती दौर में ही उन्हें उस चीज से महरूम रखा जाएगा तो वह आने वाले वक्त में उसे भुला देंगे। और सिर्फ एक राह पर चल पड़ेंगे। मैं आपको कह सकता हूं कि मेरे खुद के बच्चों ने अंग्रेजी की तालीम हासिल की है लेकिन उन्हें साथ ही साथ उर्दू का भी उसी ढंग से घर में माहौल मिला। उनका शौक भी उर्दू में पैदा हुआ और वह आज उर्दू में लिखना पढ़ना भी जानते हैं। तो यह हम लोगों को ही यह माहौल बनाना होगा चाहे वह उर्दू हो या दूसरी मातृ भाषा उनको वह माहौल देना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बच्चे ही नहीं सीखेंगे तो उर्दू तरक्की कैसे करेगी। फिर क्या होगा वह हमारे एक जमाने तक रहेगी और उसके बाद में खत्म हो जाएगी।
अरमान:- अपनी सियासत की शुरुआत छात्र राजनीति से की स्टूडेंट पॉलिटिक्स से की आज के जो छात्र नेता है उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं या क्या नसीहत देना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि जो मौजूदा वक्त की छात्र राजनीति है उसे बदनाम छात्र नेताओं ने ही किया है।
मंसूर हसन:- जी बिल्कुल आपने यह जो बात की है काफी दूर अंदेशी वाली है और इसमें काफी हद तक हकीकत है क्योंकि जब सियासत में लोग एक तरफ होने लग जाए तो वो सियासत नहीं कहलाती और इसमें छात्र नेता भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका से हट रहे हैं।और मेरी नजर में सियासत वही है जो सभी को साथ में लेकर चले ना किसी एक के तरफ अपना मत दे और किसी के दबाव में आकर काम करें अपने स्वार्थ को बुलाकर समाज सेवा हो इन सब बातो को ध्यान में रख कर जो काम करे वाकई उसे ही असली राजनेता कहा जा सकता है बाकी तो सब अपना अपना मतलब निकाल लेते हैं फिर चाहे वह नेता जो चुनाव लड़ रहा हो छात्र नेता हो या और कोई भी कार्य करता सभी को अपना दायित्व कार्य कर्तव्य समझना होगा और उस पर काम करना होगा। आपने सही कहा कि छात्र नेता उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उन्हें नहीं जाना चाहिए वह एक तरफा हो कर रहे हैं और यह एक समस्या भी है जिसका समाधान जिसे सुधारने का काम हम सभी का है क्योंकि उनकी यह हरकतें मुल्क के लिहाज से सही नहीं है।
अरमान :- बंगाल और अदब का रिश्ता कोई नया नहीं है। लंबे वक्त से वहाँ के लोगो में किताबो के लिए मोहब्बत नज़र आती रही है और आज के वक्त भी वही माहौल है।
मंसूर:- जी बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही है। मैं आपको कह सकता हूँ क्योंकि आज के वक्त मैं जैसा आपने कहा वही माहौल और यहाँ की आवाम में अच्छी किताबे ख़रीदने का जो उत्साह देखने को मिलेगा और कहीं नहीं है क्योंकि बाक़ी जगहों पे लोग समान ख़रीदने के लिए लाइन लगाते है वही बंगाल मैं आपको देखने को मिलेगा किताबों के लिए लोग लंबी लंबी लाइन लगा कर किताबे ख़रीदा करते है। ये कोलकाता के दुर्लभ नज़ारे मुझे नहीं लगता की आपको कहीं और देखने को मिलेंगे।
अरमान:- पश्चिम बंगाल और राजस्थान के रिश्तों को आप कैसे देखते हैं?
मंसूर:- यह सवाल आपका काफी खूबसूरत है क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही लोग चाहे वह बंगाली हो या फिर राजस्थानी अपनी संस्कृति को लेकर काफी ज्यादा भावुक रहते हैं और यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है और राजस्थान और पश्चिम बंगाल का रिश्ता अगर हम एक साहित्यिक नजर से देखें तो भी एक अनूठा रिश्ता है यह बात अलग है कि दोनों में भौगोलिक दूरी है लेकिन राज्यों की जो मानसिक सोच हम कह सकते हैं वह कहीं ना कहीं आपको एक जैसी मिलेगी जैसा कि मैने आपको बताया यहां या फिर राजस्थान दोनों ही जगह पर रहने वाले मूल निवासी अपने-अपने राज्यों की संस्कृति को लेकर काफी ज्यादा भावुक रहते हैं और उनका जो सेवा भाव है वह दिखता है कि वह किस तरीके से अपने समाज और अपने देश के लिए हमेशा समर्पण भाव से काम करते हैं और हमेशा से कोशिश रहती है कि समाज में शांति बनी रहे और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वह तो हमेशा से ही अतिथि देवो भव को सर्वोच्च रखता है । जो संस्कृति हिंदुस्तान की है अतिथियों का स्वागत करने की वह जो सबसे ज्यादा हमें नजर आती है वह राजस्थान के लोगों में है। जैसा की किताबें लेने का जो परंपरा है ,लोग लाइन लगाकर किताबें लिया करते हैं और वही चीज राजस्थान में भी साहित्य के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है और जो योगदान राजस्थान ने दिया वह कम नहीं है तो मुझे लगता है की भौगोलिक दूरी को हमें नहीं देखना चाहिए जो मानसिक एकता है वह हमें करीब लाती है।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार ।
मंसूर हसन - आपका भी बहुत बहुत आभार ।
Himanshi
हिमांशी
दिल्ली में रहने वाली क्विंट की संवाददाता हिमांशी राजनीति, जाति, अपराध और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर रिपोर्ट करती हैं। वह गहन ग्राउंड रिपोर्ट और लॉन्गफॉर्म टेक्स्ट और वीडियो डॉक्यूमेंट्री फीचर में माहिर हैं। पांच साल से अधिक के अनुभव वाली पुरस्कार विजेता पत्रकार हिमांशी अपनी वर्तमान भूमिका में राजनीति, शासन और समाज के बीच के संबंधों की जांच की देखरेख करती हैं। चुनावी बॉन्ड और भारत के चुनाव आयोग के कामकाज पर उनकी जांच को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। हिमांशी की रिपोर्टिंग ने उन्हें दो बार लैंगिक संवेदनशीलता के लिए प्रतिष्ठित लाडली मीडिया अवार्ड दिलाया है, साथ ही उन्हें द रेडइंक अवार्ड, खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड और WAN IFRA अवार्ड जैसे अन्य पुरस्कार भी मिले हैं।
अरमान :- सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने पत्रकारिता को ही क्यों चुना?
हिमांशी:- अरमान अगर मैं आपको अपने स्कूल के बाद के सफर के बारे में बताओ कि किस तरीके से पत्रकारिता में शुरुआत पहले अगर मैं अपने एकेडमिक से शुरू करूं तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूं उसके बाद में कॉलेज जाना था एडमिशन की तैयारी करनी थी लेकिन मैं मेडिकल को आगे जारी नहीं रखना चाहती थी मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वह चीज आपके स्कूल में ही पता लग जाती है जब आप 2 साल पढ़ाते हैं किसी सब्जेक्ट को उसके बाद में आप फैसला कर लेते हैं कि आगे आपको इसके साथ जाना है या नहीं। और व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि वो फील्ड ऐसी है जो उसके लिए नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बता सकती हूं साहित्य में मुझे शुरुआत से दिलचस्पी रही है मैंने अपने कॉलेज के अंदर अंग्रेजी साहित्य ऑनर्स किया है दिल्ली के मोती लाल नेहरू कॉलेज से। और जब मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती थी तो मुझे उसमें दिलचस्पी आई थी फिर चाहे वह शिक्षक हो नॉन फिक्शन हो तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मेरा झुकाव लिटरेचर की तरफ होने लगा। क्योंकि 3 साल की डिग्री थी और मैं आपको बताऊं कि 2 साल तक तो मैं सिर्फ फिगर आउट ही कर रही थी कि मुझे अब आगे क्या करना है। लेकिन इस दौरान मैं कॉलेज का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। और जवाब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर थिएटर करते हैं तो आप स्टेज भी करते हैं स्ट्रीट थिएटर भी करते हैं। और स्ट्रीट थिएटर आते हुए आपका एक सोशल पॉलीटिकल जागरूकता आप में आती है और आपको वह चीज महसूस होने लगती है और आपको यह एहसास होने लगता है कि आसपास किस तरह की परेशानियां समाज में हो रही है। और मुझे उसे वक्त धीरे-धीरे यह एहसास होने लगा कि एक्टिविज्म, आर्ट यह सब चीज मेरे लिए है। और जब मैं अपने बा के फाइनल ईयर में थी तब मुझे यह महसूस हुआ कि आर्ट और एक्टिविज्म इंडिया के अंदर इतना टिकाऊ नहीं है कहने का मतलब यह है कि आपको एक परमानेंट नौकरी नहीं मिल सकती। और एक महिला होने के नाते यह भी जरूरी है क्या आपको एक फाइनेंशली इंडिपेंडेंट मिले। और बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद में अगर किसी एक प्रोफेशन की तरफ मेरा रुझान हुआ और उसे चीज समझ आई तो वह था जर्नलिज्म। और मुझे यह भी चीज का एहसास हुआ कि जर्नलिज्म ही वह एक प्लेटफार्म का लीजिए या फिर वह चीज का सकते हैं जहां यह सब चीज एक साथ आ सकती है जिन्हें मैं पसंद करती हूं। और यहां क्रिएटिविटी आप अपने ख्याल यहां रख सकते हैं सोशल इश्यूज की तरफ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्योंकि आप एक नौकरी भी कर रहे हैं तो फाइनेंशली इंडिपेंडेंट भी आपको इसमें मिलती है तो वह सब चीज जो मैं चाहती थी वह यहां एक साथ हो रही है। और फिर वहीं से मैंने फैसला किया कि पत्रकारिता की जा सकती है। मेरे परिवार में पहले कोई पत्रकारिता से नहीं जुड़ा हुआ तो मुझे इसकी कोई गाइडेंस भी नहीं थी तो जो भी हुआ वह इंटरनेट के थ्रू ही हुआ। और बहुत सारे कॉलेज के मेन एंट्रेंस एग्जाम दिए और आखिर में आईआईएमसी दिल्ली और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई के एंटरेंस एग्जाम्स मैंने क्लियर किया और फिर इन दोनों में से किसी एक को चुनने का मेरे पास में मौका था और क्योंकि दिल्ली के अंदर में पहले पढ़ चुकी थी इसलिए मुझे लगा कि बॉम्बे जाना चाहिए और देखते हैं कि मुंबई में किस तरह का कल्चर है नए शहर को एक्सप्लोर करने का ख्याल भी मन में था। वहां से मैं फिर अपना डिप्लोमा किया और डिप्लोमा पूरा होने के बाद में कुछ टीवी चैनल के साथ में मैंने इंटरशिप की। और जिस वक्त में उन टीवी चैनल के साथ मेंटालिशप कर रही थी तो उसे वक्त ही एक रिलाइजेशन भी होने लगा था कि जो मेंस्ट्रीम मीडिया है आप देखिए यह मैं वक्त बता रही हूं 2018 का और उसे वक्त मिनिस्ट्री मीडिया का डाउनफॉल शुरू हो ही चुका था रिपब्लिक नया-नया आया था टाइम्स नाउ कि अगर हम बात करें तो सब एक साथ ही ऐसा चल रहा था। और यह वह समय था जब आपको यह एहसास होने लगा था कि टीवी न्यूज़ में अब कुछ बचा नहीं है। और मुझे यह लग गया था कि अब मैं में सरिता में फिट नहीं हो सकती हूं हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से वहां स्टोरी कवर की जा रही थी। और एक टीवी चैनल में इंटर्नशिप के दौरान मेरा जो एक दिन था उसे वक्त वह माहौल था कि जब इंडियन एयर फोर्स के फाइटर पायलट अभिनंदन पाकिस्तान से वापस लौट रहे थे और जिस तरह का माहौल न्यूज़ रूम में था किस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां किया जा रहा था मैं आपको यह बता सकती हूं कि उसे वक्त मुझे जर्नलिज्म का इतना आईडिया नहीं था लेकिन फिर भी आपको यह तो एहसास होता ही है कि कुछ तो गलत हो रहा है। और उसे दौरान मुझे यह तो पता लग गया कि टीवी चैनल मेरे लिए नहीं है। और अगर हम न्यूज़ चैनल के बाद में न्यूज़ पेपर की बात करें प्रिंट मीडिया के ऊपर जब हम बात करते हैं उनकी सैलरी किस तरीके से होती है यह हम जानते हैं बड़े-बड़े जो न्यूज़ पेपर से उनका यह कहना होता है कि हमारे साथ काम करना ही आपके लिए रिवॉर्ड है बहुत से लोग यह चीज सपोर्ट कर सकते हैं जिनके पास में फैमिली सपोर्ट रहता है या फिर कोई उनके पास में एक बैकअप है लेकिन प्राइमरी जॉब में आप उसे उसे तरीके से नहीं ले सकते। आपको खुद की तरफ से अगर सरवाइव करना है और वह भी दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में तो आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं प्रिंट मीडिया में अप्लाई नहीं किया करने की कोशिश की हो लेकिन क्योंकि वहां सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको जिस तरीके से सिखाया जाता है आपको लिखना सिखाया जाता है आपकी गलत तरह की ट्रेनिंग होती है। पत्रकारिता की दृष्टिकोण से अगर हम देखें जो चीज आपको प्रिंट में मिल सकती है मुझे लगता है आज भी डिजिटल के पास में वह रिसोर्सेस नहीं है आज भी। लेकिन आखिर मे क्विट को ज्वाइन किया।
अरमान :- मेंस्ट्रीम मीडिया के डाउनफॉल का अपने जिक्र किया और बाकी में यह एक गंभीर विषय है। और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जब भी हम पत्रकारिता के सम्मान की बात करते हैं तो हम उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं लेकिन आज वही स्तंभ लोकतंत्र की नीव हिलाने में लगा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को टाइम पीरियड को एग्जामिन करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
हिमांशी:- बिल्कुल अरमान मेंस्ट्रीम मीडिया की जो हालात आज के वक्त में है वह किसी से छुपी हुई नहीं है हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है और अगर हम बात करें कि यह क्यों हो रहा है या फिर मैं इसे कहूं कि मेरे हिसाब से यह क्यों हो रहा है की कुछ वक्त मुझे अब इसमें हो चुका है तकरीबन 6 साल से मैं पत्रकारिता से जुड़ी हूं और मुझे भी कई चीजों के बारे में एहसास हुआ है। और मेरी नजर में मिनिस्ट्री मीडिया के डाउनफॉल का सिर्फ यह कारण नहीं है कि कोई पार्टिकुलर पार्टी आज पावर में है और वह उन्हें ज्यादा रेगुलेट करना चाहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे पहले जो सरकारी थी उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की थी ऐसा नहीं है कि जो पहले सरकारें थी उस वक्त के जो जनरलिस्ट थे उनके फेवर में काम नहीं किया करते थे और उस वक्त भी सरकारों के लिए लॉबिंग हुआ करती थी। और अगर मिनिस्ट्री मीडिया का सबसे खराब वक्त आज अगर हम इंडिया में देखते हैं स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो वह इसलिए हो सकता है एक कारण सबसे बड़ा यह हो सकता है कि सोशल मीडिया आ चुका है क्योंकि जो मीडिया हाउसेस है वह मुझे लगता है पहले से ही एक्जिस्टेंशल क्राइसिस में है और अब आप यह देखिए कि आप किसके साथ कंपटीशन में है पहले जो है अगर हम देखें इंडियन एक्सप्रेस है हिंदू के साथ में कंपटीशन में था दैनिक भास्कर शायद अमर उजाला के साथ कंपटीशन में था एनडीटीवी टाइम्स नाऊ के साथ कंपटीशन में है। अब आप सभी को मिलकर एक चीज के साथ और कंपटीशन में उतरना है जो की है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के साथ जब आप कंपटीशन में है तो वह जो स्पीड फैक्ट चेकिंग रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है तो यह सब चीज एक साथ आपको देखनी पड़ती है और सोशल मीडिया के साथ आप जब कंपटीशन में है या तो आपको वह चीज चुन्नी पड़ेगी आप वक्त लीजिए और एक-एक चीज को वेरीफाई करके और उसके बाद ही आप उन्हें पब्लिश करें। और आप इनफॉरमेशन निकलेंगे बिना किसी सनसनी के फिर चाहे हमें कुछ काम उसे मिले क्योंकि जब सोशल मीडिया पर वही चीज वायरल होगी फिर चाहे वह फेक न्यूज़ ही क्यों ना हो तो वहां पूरा माहौल बदल जाता है। और जब इन सबकी आप फैक्ट चेक करके एक टाइम लेकर आप अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं न्यूज़ डालते हैं तो उसका नतीजा सिर्फ यही नतीजा होगा की आपको व्यूज उसके मुकाबले में कम मिलेंगे और बहुत सारे लोग वह रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सीधी बात यह है कि सोशल मीडिया के साथ आपको स्पीड बना कर रखनी पड़ेगी। दूसरा तो ऑफिस बात है ही की जो पॉलीटिकल प्रेशर बाकी सरकारों से ज्यादा जो पॉलीटिकल प्रेशर आज के वक्त में है। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है उनका इस्तेमाल करके मीडिया हाउसों पर रेड की गई है एनडीटीवी का आपने पूरा कैसे देखा। यह सब सच्चाई तो डाक्यूमेंट्री है आप इन्हें खुद देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं। और यह कह सकते हैं कि इस वक्त ज्यादा प्रेशर है पहले के मुकाबले। और इन सबके अलावा एक और प्रॉब्लम मुझे नजर आती है जो की इंडियन मीडिया का रिवेन्यू सिस्टम है पैसा कहां से आ रहा है अगर आप सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं सरकारी विज्ञापनों पर अपनी पब्लिकेशन को चलाने के लिए। तो फिर आपको सरकार के लिए ही काम करना होगा। यह तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज हो चुकी है अगर मैं आपको किसी काम के लिए पैसे दे रही हूं तो तो आप फिर मेरे लिए ही काम करेंगे। और एक और चीज जो मैंने अब तक की पत्रकारिता में 6 साल की जो मेरी चटनी रही है उसमें नोटिस किया है वह यह है कि भारतीय मीडिया में ओनरशिप है वह बहुत से मिनिस्ट्री मीडिया में जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर हैं वहां पर डाइवर्सिटी बहुत कम है और उन पदों पर अधिक प्रभुत्व रखते हैं अपर कास्ट अपर क्लास मैन और इस चीज के ऊपर भी अध्ययन हो चुका है यह ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं। इन सब के बाद में आप यह देखेंगे कि जो मीडिया है वह लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगी वह उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी जो लोग वहां रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है यह बहुत सारे कारण मिलकर जो मिनिस्ट्री मीडिया को डाउनफॉल की तरफ धकेल रहे हैं। और यह वाकई में एक बड़ा क्राइसिस का टाइम चल रहा है और न जाने यह कब उसमें से बाहर निकलेगा और सवाल तो यह भी है कि बाहर निकल पाएगा या भी नहीं।
अरमान:- अपने मीडिया हाउसों के रिवेन्यू कलेक्शन की बात की और हाल ही में हमने ए एन आई कैस देखा जो की ए एन आई बनाम युटयुबर्स हो गया इसे आप एग्जामिन करते हुए क्या कहना चाहेंगे?
हिमांशी:- देखिए अगर मैं कहूं कि मैं कंटेंट क्रीटेड नहीं हूं और यह चीज मुझे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती है तो उसके बाद में भी मैं यह कहूंगी कि यह बात सच है कि अगर आप किसी का कंटेंट उसे करते हैं एक रिवेन्यू बात होनी चाहिए शेयरिंग डील होनी चाहिए लेकिन इस केस में जो ए एन आई का बिहेवियर रहा वह धमकाने वाला था आप किसी को थ्रेटेन कर रहे है। तो यह जो पूरा कैसे अगर हम देखें तो मीडिया हाउस ए एन आई की तरफ से बिल्कुल भी एथिकल नहीं था। देखिए गलत नहीं है कि अगर आप अपने कंटेंट के लिए किसी से पैसा लेना चाहते हैं लेकिन आपको एक मॉडल डेवलप्ड करना चाहिए था उन कंटेंट क्रिएटर के साथ। आप उनसे मुंह मांगे दम कैसे मांग सकते हैं आपको उनके साथ में बैठी है एक रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल बनाया उनसे दोनों तरफ बात होनी चाहिए बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जिनसे ए एन आई इन इश्यूज को सॉल्व कर सकता था। लेकिन जो उन्होंने रवैया युटयुबर्स के साथ में दिखाया कि आप बहुत ज्यादा रेवेन्यू उनसे मांग रहे हैं और वह भी बहुत छोटी क्लिप का कुछ चंद सेकेंड्स की जो क्लिप है और उसके बाद मैं अपने स्ट्राइक्स की धमकी देते हैं और उनके चैनल उड़ने की धमकी देते हैं कि आपका चैनल बंद ही करेंगे हम। हम यह भी जानते हैं कि की ए एन आई की किस तरीके से मोनोपोली है पूरी सेक्टर में उन्हें जो एक्सेस मिलता है जिस तरीके का उनके पास में सुविधा है और वह सब आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आपके पास में राइट्स है कि बहुत सारी चीज सिर्फ आपके पास में ही है जो औरों के पास में उपलब्ध नहीं है और वह इसलिए नहीं है कि वह अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने रिपोर्टर से कोई काम करवाया हो या आपकी कोई एक्स्ट्रा मेहनत उसमें है वह इसलिए है क्योंकि आपके पास में राइट से उसे चीज को एक्सेस करने के लिए। और यह कोई गलत चीज नहीं है हम इसका चीज का रिस्पेक्ट करते हैं के आपके पास में एक्सेस है लेकिन इन सब के बाद में आप किसी के साथ में इस तरह का रवैया रखेंगे तो यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और वाकई में बहुत से रास्ते थे इस केस के ऊपर काम करने के लेकिन उन्होंने सबसे खराब रास्ता चुना।
अरमान:- पत्रकारिता के अंदर हम जब इन्वेस्टिगेटिव जनरेशन की बात करते हैं जो सत्ता को पावर में बैठे हुए लोगों को सीधी चुनौती दिया करता था लेकिन आज हम देख रहे हैं वह खुद कहीं चुनौतियों से घिरा हुआ नजर आता है एक तो वह सिक्योरिटी परपज था ही के पत्रकारों को मारने की धमकी और लेकिन आज के वक्त में और किन आधुनिक चुनौतियों से आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म झूंझती हुई नजर आती है?
हिमांशी:- बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आज के समय में हमारी राजनीतिक व्यवस्था वहां पर प्रदर्शित नहीं है और जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है डाटा नहीं है एक्सेस भी नहीं है और बहुत सालों की स्ट्रगल के बाद आरटीआई एक्ट पास हुआ आरटीआई बहुत ही इंर्पोटेंट टूल था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में इसके करीब बहुत सारे पत्रकारों ने जो स्टोरी है वह कर की है जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक स्टोरी रही है अब अपने धीरे-धीरे आईटीआई एक्ट को इतना डाइल्यूट कर दिया है पतला कर दिया है कमजोर कर दिया है कि अब कोई भी इनफॉरमेशन आरटीआई के जरिए से निकल पाना लगभग इंपोसिबल सा हो गया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए जो टूल कई सालों से या यूं कहूं के जिस तरीके का सिस्टम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हुआ था और उन्होंने खुद डेवलप किए थे उन सभी को एक सिस्टमैटिक ढंग से खत्म करने की कोशिश रही है यह तो एक आपका काम करने में ही बधाएं हैं डिफिकल्टी हैं। और इन सबको भी अपने ओवर कम करके कोई रिपोर्ट पब्लिश कर भी दी उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आपके सामने आएगी वह पहले नहीं होता था जिस तरीके से आपके ऊपर डिफामेशन केस होंगे जिस तरह की ट्रोलिंग का सामना आपको सोशल मीडिया पर करना पड़ेगा जिस टाइम पीरियड में हम रह रहे हैं उस हम पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड कह सकते हैं जहां सच-सच नहीं है तथ्य तथ्य नहीं है। और अगर आपने कोई अच्छी रिपोर्ट पब्लिश कर भी दी है आपने वहां एक-एक चीज दर्शी है कि यह एबीसी हमारी समस्याएं हैं फिर भी कुछ एक कोई ग्रुप होगा जो सोशल मीडिया पर रहेगा यह झूठ है यह सब गलत है। और एक ट्रोलिंग का साइकिल भी शुरू होगा। तो आप यह देखिए की 360 डिग्री एक रिपोर्टर पर अटैक होता है जब आप एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जो किसी पावरफुल इंसान खिलाफ होती है या उनसे अकाउंटेबिलिटी की डिमांड उसमें की जाती है और मैं जैसा कहा कि यह सिर्फ सरकार के केस में नहीं है बड़े कॉरपोरेट हाउसों के ऊपर रिपोर्ट करें या दूसरे पॉलिटिशियन के ऊपर रिपोर्ट करें इस चीज के लिए आपको तैयार पड़ता है कि आपके ऊपर लीगल अटैक होगा। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए पब्लिश कर रहे हैं अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके पब्लिकेशन को अलग-अलग तरीके दबाव डाला जाएगा। और यह हमने देखा भी है कि किस तरीके से बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं तो उन्हें किसी और तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी। और यह सब जानते हैं समझते हैं कि यह ऐसा क्यों हो रहा है और यह क्यों हुआ आचनक आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है सुद्दनली आपके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टेड क्यों रेड करने आ रही है और उसके बाद में एक डर का माहौल बनाया जाता है कि आप आगे से इस तरह की रिपोर्ट पर काम ना करें। और कहीं ना कहीं रिपोर्टर के ख्याल में भी यह चीज आएगी कि अब रहने देते हैं। तो हम यह साफ शब्दों में कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना आज के वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको कहा सबसे पहले तो स्टोरी निकाल पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है और उसके बाद में भी आपने वह कर लिया उसके बाद का जो सफर है पब्लिश होने के बाद शायद आप जिस तरह का डर के माहौल का आपको सामना करना पड़ेगा कि पता नहीं क्या हो सकता है मेरे साथ में वह एक अलग तरह की चुनौती होती है। यह तो मैं बड़े शहरों की बात कर रही हूं आप अगर छोटे शहरों में जाएंगे जो पत्रकारिता वहां कर रहे हैं वहां पर एक असल डर का माहौल आता है आपकी जिंदगी के साथ। हमने बस्तर का कैसे देखा। उत्तर प्रदेश की अगर आप हेडलाइंस देखेंगे बहुत सारी जगह पर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। आपने किसी विधायक के खिलाफ रिपोर्ट किया या गांव के प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट क्या आपने सेंड माफिया के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की उसके कुछ वक्त बाद उसे पत्रकार का मर्डर हो जाता है या फिर गायब हो जाता है इनमें से बहुत सी चीज पहले से थी और कुछ अभी हम हाल ही में देख रहे हैं। अरमान :- मीडिया किसी भी केस को किस तरीके से कवरेज देता है यह हम सब जानते हैं फिर चाहे वह क्रिमिनल हो फैमिली केस और एक शब्द भी हमें बहुत सुनने को मिलता है कि अभी तो "मीडिया ट्रायल" चल रहा है और जिससे जाहिर तौर पर आम जनता प्रभावित होती है सवाल यह है क्या कोर्ट भी मीडिया ट्रायल से प्रभावित होता है?
हिमांशी :- मैं इस बात से शत प्रतिशत सहमत हूं कि मीडिया ट्रायल से बहुत सारे केसेस में कोर्ट भी प्रभावित होती है हमने यह चीज सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को काफी वक्त तक जेल में रहना पड़ा अगर यह एक नॉर्मल कैसे होता मीडिया ट्रायल इन पर नहीं चला होता अगर इन सबके खिलाफ पब्लिक सेंटीमेंट इस तरीके से नहीं होता तो उन्हें वो वक्त जेल में नहीं बिताना पड़ता तो हम यह साफ तौर पर देखते हुए कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मीडिया ट्रायल का सिर्फ पब्लिक पर प्रभाव नही पड़ता है और यह हमने हिस्टोरिकल देखा है की मीडिया ट्रायल से कोर्ट भी काफी हद तक इंपैक्ट हुए हैं। और हम इसमें यह नहीं कह सकते कि यह सिर्फ कुछ दिनों का सर्कस चलता है और बाद में सब नॉर्मल हो जाता है के बहुत हद तक असल जिंदगी में भी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं जिसमें निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ता है। और हम यह कह सकते हैं कि मीडिया ट्रायल से कोर्ट प्रभावित होते हैं।
अरमान :- जिस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर बात की आपने भी बताया कि जो पत्रकार हैं उन्हें इतना प्रेशर कई बार होता था कि वह उस रिपोर्ट से अपने आप को पीछे रख लेते थे तो क्या आपके साथ खुद ऐसा कभी कोई अनुभव हुआ है जहां आपको पॉलिटिकल या फिर किसी भी तरह का प्रेशर का सामना करना पड़ा हो रिपोर्टिंग को लेकर?
हिमांशी:- हां फेस की है बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट होती है बहुत सारी ऐसी चीज होती है जहां करने से पहले आप सोचते हैं कि वह आपको करना चाहिए या नहीं इलेक्टरल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं वहां बहुत सारी कवरेज हुई उसमें से बहुत सारी स्टोरी ऐसी थी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उन्हें एकदम से आईडेंटिफाई नहीं करना चाहूंगी लेकिन बहुत सारी स्टोरी ऐसी होती हैं जिसमें बिजनेसमैन के नाम आते हैं और फिर एक बार ख्याल आता है दिमाग में पॉलीटिशियंस का जब नाम आता है रिपोर्ट में या किसी पार्टी की अगर हम बात करें यह बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं पहले इनके बारे में जिन्होंने रिपोर्ट किया है उन पर किस तरह के एक्शंस हुए हैं और फिर यही चीज ख्याल आता है क्या आपको इस रिपोर्ट के साथ में जाना। और वहां पर जो जिससे आप जुड़े हैं जिन एडिटर के साथ आम कम कर रहे हैं उनका सपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी होता है लकिली मेरे एडिटर और जहां मैं काम करती हूं पब्लिकेशन है जो हमेशा साथ देते हैं। मेरे एडिटर कहते हैं कि अगर आपका रिपोर्ट फेक्चुअल है और आपके पास में एविडेंस है फिर डरने की कोई बात नहीं है। और फिर वहां पर आपकी पब्लिकेशन और एडिटर का जो रोल है काफी जरूरी होता है। जब भी मुझे ऐसा लगा कि इस रिपोर्ट पर काम करना चाहिए या नहीं या फिर उसे पब्लिश करना चाहिए या फिर नहीं तो उन्होंने हमेशा से मुझे बैक सपोर्ट के साथ में कहा है कि बिल्कुल आपको इस रिपोर्ट के साथ में जाना चाहिए यह अगर फेक्चुअल है और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ में जाती है तो हम इसे बिल्कुल पब्लिश करेंगे और पूरा साथ आपके साथ रहेगा।
अरमान :- सरकारी विज्ञापनों की आपने चर्चा की और सवाल भी यही बनता है कि जिस तरीके से सरकारी विज्ञापनों का प्रभाव मीडिया हाउसों पर है और एक और उन्हें पाने की लगी हुई हमें देखने को मिलती है इस पर किस हद तक सैंक्शंस लगनी चाहिए आपकी नजर मे?
हिमांशी:- समस्या सबसे बड़ी ही आती है कि अभी जो हमारा रिवेन्यू मॉडल है जिस तरीके से खबरों को भारत में देखा जाता है न्यूज़ के जो कंज्यूमर हैं उनकी एक हैबिट है हमें लगता है न्यूज़ फ्री है। अगर हमारे हाथ में एक न्यूज़ पेपर आता है हम उस न्यूज़पेपर का पैसा देना चाहते हैं ठीक है वह पेपर है वह प्रिंट हुआ है उसकी कीमत है हम उसे न्यूज़पेपर का पैसा देते हैं। न्यूज चैनल की भी अगर हम बात करें तो हम अपनी केबल ऑपरेटर को पैसा देते हैं अगर आप डायरेक्टली सीधे तौर पर न्यूज़ के लिए पैसा आप पार्टिकुलर इस चैनल को देखने के लिए पैसा देंगे शायद लोग ना दे क्योंकि उन्हें लगता है और उन्हें आदत है कि यह फ्री है और अगर हम फिर से डिजिटल की बात करें तो आप इंटरनेट के लिए पैसा देना चाहते हैं जिओ के लिए पैसा देंगे एयरटेल के लिए पैसा देंगे अगर आप शायद एक क्विट मीडिया हाउस के लिए पैसा मांगेंगे तो लोग नहीं देंगे बहुत कम लोग होते हैं जो उसके लिए राज़ी होकर पैसा देते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि सरकारी विज्ञापनों से पैसा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए सरकारी इश्तहार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो हमें साथ में यह भी देखना चाहिए कि अल्टरनेट क्या है इस चीज का और एक अल्टरनेटिव यह होता है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ट आप एक मॉडल तैयार करें लोगों से सीधा पैसा ले और वह मॉडल डेवलप करने के लिए न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबली मीडिया इंड्वार्टी अगर हम देखें तो बहुत पीछे है ऐसे बहुत ही काम मॉडल है जो वास्तव में सक्सेसफुल हुए हैं इसमें। शायद लोग इस वक्त न्यूज़ के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यह हमें तैयार करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं सरकार से जब हम पैसा लेने की बात करते हैं और जो सरकार के सपोर्ट से पैसे से चलने वाला मीडिया हाउस है तो वह रिपोर्टिंग तो वह ना तो आज कर पा रहे हैं ना कल कर पाएंगे और आगे भी शायद नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक स्वतंत्र मीडिया हाउस बनाना है आपको डिपेंड होना पड़ेगा अपने व्यूअरशिप पर उनके पैसों पर कंज्यूमर के पैसे पर। जब तक वह नहीं हो रहा है तब तक कुछ अल्टरनेटिव क्या है कि सरकार का या फिर कमर्शियल ऐड ब्रांड से पैसा लीजिए। अगर हम ब्रांड की बात करें तो वह भी काफी हद तक सहयोग नहीं करना चाहते। क्योंकि एक जेनरेशन ऐसी भी है जो न्यूज़ से दूर रहते हैं वह कहते हैं कि हम पॉलिटिकल इन सब में नहीं होना चाहते। जिनके लिए न्यूज़ काफी बेसिक चीज है जिन्हें उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं है ऐसी भी एक जेनरेशन एक पूरा ग्रुप आफ पीपल है। मान के चलिए कोई शैंपू का ब्रांड है तो वह उसमें एसोसिएट नहीं करना चाहेगा। तो उनके पास में दूसरा रास्ता ही नहीं है बजाय कि वह सरकार के पास जाएं। और अगर हम चाहते हैं कि सरकारी विज्ञापन ना आए तो हमें एक अल्टरनेटिव मॉडल डेवलप करना पड़ेगा।
 Alok Puranik
Alok Puranik
आलोक पुराणिक
—- क्योंकि वह इतने पावरफुल हैं कि वह चुनाव जितवाते हैं और चुनाव हरवाते ? :- पुराणिक
तमाम पाठकों को मेरा आदाब नमस्कार , अपने साप्ताहिक कॉलम “शब्द संवाद”में जिसमें कोशिश है कि एक ऐसी शख़्सियत से बात हो जो अपनी विधा में विशेष योगदान देता है और साथ ही जब हम उनसे बात करे तो कुछ नया सीखने को और समाज को समझने का एक अलग दृष्टिकोण मिले और इसी के चलते आज के कॉलम के ख़ास मेहमान है सुविख्यात वरिष्ठ व्यंग्यकार ,दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर श्री आलोक पुराणिक जी।
30 सितंबर 1966 आगरा में जन्मे आलोक जी अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी रखते हैं तो वे बतौर साहित्यकार ,पत्रकार अर्थशास्त्री लगातार अमर उजाला’, ‘राष्ट्रीय सहारा’, ‘नवभारत टाइम्स’, ‘जागरण’, ‘उदय पत्रिका’, ‘दैनिक नवज्योति’, ‘दैनिक ट्रिब्यून‘, ‘स्वतंत्र वार्ता’, ‘सेंटिनल’, ‘लोकमत समाचार’, समेत कई पत्र-पत्रिकाओं में नियमित व्यंग्य-लेखन। अपने विचार अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में लेखन के माध्यम से व्यक्त करते हैं उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ :- ‘बालम, तू काहे न हुआ एन.आर.आई.’, ‘नेकी कर, अख़बार में डाल’, ‘ह्वाइट हाउस में रामलीला’, ‘छिछोरेबाज़ी का रिजोल्यूशन’। उनसे वार्तालाप करते हुए कही मसलों पर ख़ास चर्चा हुई जैसे पत्रकारिता पर लगातार उठते सवाल अन्य सामाजिक परेशानियाँ, धर्म संस्कृति में अंतर।
प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के अंश
अरमान नदीम:- हिंदी मीडिया पर से आज के युवा बुद्धिजीवियों का विश्वास क्या उठता जा रहा है?
आलोक पुराणिक :- देखिए पत्रकारिता और बुद्धिजीविता का या विचार परख लेखन का रिश्ता प्रश्नों में आज से नहीं बहुत लंबे समय से था लेकिन हाल में दरअसल हुआ यह है कि जो हिंदी के अलग-अलग माध्यम है जैसे कि वह अख़बार है पत्रिकाएं हैं यूट्यूब चैनल है फेसबुक, ट्विटर है अभी इसमें कुछ इस तरह की चीज हो गए कि जो एक संतुलित स्वर हुआ करता था एक ऐसा व्यक्ति ऐसा ज्ञानी जो तमाम पक्षों की बात को गहराई से समझ कर बात लिख रहा है और जिसके स्वर में अतिरेक नहीं है जिसके स्वर में विवेक है वैसे स्वर नदीम साहब बहुत कम हो गए हैं कम क्या हो गए हैं खत्म ही हो गए हैं और अखबार में एक बहुत सीधा इंपैक्ट मुझे दिखाई पड़ता है मार्केट के प्रेशर का वहां विचार की जगह वह कहते हैं कि हम बेच सके आप ऐसा कुछ लाइए आप भी मीडिया के छात्र हैं तो इसे गहराई से देखेंगे कि टेलीविजन ने अखबार के कंटेंट को पूरे तौर पर इनफ्लुएंस कर दिया है और जो टीवी पर आता है वह उसको अखबार महत्व दे ऐसा एक बाज़ारी प्रेशर हो जाता है। जैसे कि अगर वैलेंटाइन डे है उसमें आसपास तमाम टेलीविज़न चैनल में वैलेंटाइन की खबरें दिखाई पड़ती हैं और अखबार में भी देखता हूं उसी तरह का एक कंटेंट देखते हैं के कैसे बनाएंगे मनोज तिवारी अपना वैलेंटाइन डे पहले वैलेंटाइन को याद कर रहे हैं महानायक। इस तरह की चीज हमें देखने को मिलती है क्योंकि मुख्य समस्या अखबार की है, पत्रिका की है ,मूल समस्या विज्ञापन लाना है पैसा बनाना है पैसा आ रहा है टीआरपी आ रही है। अब बहुत गंभीर तरह से चीज देखने को नहीं मिल रही है अखबार में जैसे पहले दिखा जाया करती थी तो मैं इस बात को काफी हद तक मानता हूं कि विचारपरख पत्रकारिता प्रिंट और मैनली प्रिंट की पत्रकारिता से लगभग गायब हो चुकी है ऐसा मुझे लगता है।
अरमान नदीम :- क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जिनके समान अर्थ थे मगर उनके भाव बदल चुके हैं जैसे कि अब मान के चलिए की लोग पत्रकार को तो कुछ अब भी मानते हैं हां की यह बेहतर बात कर सकता है लेकिन एंकर को कहते हैं कि बस यह सूट पहन कर आता है और सामने खड़ा हो जाता है जबकि जर्नलिस्ट और एंकर में फर्क है लेकिन लोग एक ही मानते थे मगर अब फर्क समझ रहे हैं। और कहते है इस सूट वाले को क्या मालूम फटी बनियान वाले का हाल - आप इसे कैसे देखते हैं?
आलोक पुराणिक:- भाई आप तो बात कर रहे हैं मैं व्यंग लिखा था। दिल्ली में एक टीवी चैनल के एंकर का किडनैप हो गया अपहरण हो गया वह अपना सूट टाइप पहन कर आता था उसको पकड़ लिया ले गए वहां जाकर उसने किडनैपर को बताया भाई मुझे तो 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है “हंसते हुए”अरे इससे पैसे लेंगे या इसे पैसे देने पड़ेंगे मैंने व्यंग लिखा भाई यह टीवी इंडस्ट्री के ऐसा जिसके मूल में कमर्शियल कंसंट्रेशन हो उसमें फिर क्या होता है मूल चिंताएं होती है कि भाई धंधा बढ़ाओ। अब धंधा बढ़ाओ तो खबर यह होती है कि रोज रात को 12:00 बजे नींद में नदीम के पास आती है नागिन और अब जब वह सो रहा है तो उसे चुपके से चूम कर चली जाती है। अब यह खबर बड़ी बेहूदा है लेकिन देखी जाएगी और अब होगा कि नदीम की वाइफ लाओ या नागिन का नाटक रूपांतरण करवाओ। कतई बेहूदा बेवकूफ आना चीज हैं लेकिन जनता देख रही है इनको। अब जनता देख रही है तो उनको टीआरपी मिल रही है टीआरपी से विज्ञापन आ रहा है तो अब यह एक ऐसा दुष्कर्म हो गया है भाई। उसमें अब टीवी चैनल वाले भी कहें कि हम क्या करें। एक बहुत सीनियर बहुत बड़े चैनल के जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी तो वह बता रहा था कि भाई साहब एक जमाने में पत्रकार का जिम्मा होता था हर विधा का जानकार होता था। लेकिन अभी एक नागिन वाले को सेट कर रखा है रात को 12:00 भी वाइट दे देता है साधु बाबा को सेट कर रखा है मैंने कहा कि भाई तू पढ़ा लिखा आदमी है। वह कहता है भाई बात ऐसी है उसमें हमें टीआरपी आ रही है तो जब टीआरपी ओरिएंटेड जर्नलिज्म हो जाती है तो एक मात्र क्राइटेरिया रहता है देखा क्या जा रहा है। अभी आप देखेंगे दीवाली के वक्त में हम हैं। तो अब विज्ञापन आते है धनतेरस में धन कैसे कमाए?
अरमान नदीम:- एस्ट्रोलॉजी को लाते हैं।
आलोक पुराणिक:- अरे यह तो हर बड़े चैनल में आपको कंपलसरी मिलेगी। अब क्या कहोगे इसको लोकतंत्र है और लोकतंत्र में गुंडो को इलेक्ट कर रही है जनता तो वह भी जनप्रतिनिधि है।
अरमान नदीम -:आपने गुंडो के प्रतिनिधि की बात करें , कुछ तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि है इसी पर हम बात करें तो जब मीडिया किसी को बनाता है या यू कहे ग्लैमराइज करती है तो सीधा-सीधा इंपैक्ट हम नौजवानों पर देखते हैं। हम देख रहे हैं आज के वक्त में उनके आदर्श वह हैं जो कानून की नजर में गुनहगार है सजा काट रहे हैं या काट चुके हैं लेकिन उन्हें रील पर सोशल मीडिया पर एक एजेंडा के साथ ग्लैमराइज किया जाता है और उससे बस उनकी खामियां छुप जाती है।
आलोक पुराणिक :- देखो सोशल मीडिया ने यूट्यूब इन सब ने एक अलग तरह का बाजार क्रिएट कर दिया है और उसमें कोई भी व्यक्ति लगातार दिखाई दे रहा है सामने आ रहा है तो उसका अपना आभामंडल बन जाता है हालांकि बात है आप खुद इसे डिसाइड कीजिएगा पाकिस्तान हमसे कहीं मामलों में बहुत पीछे है लेकिन कुछ में आगे भी है आप सर्च कीजिएगा पाकिस्तान में डाकू है खास तरह के डाकू हैं वहां उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और उसमें डाकू अपनी शेरो शायरी करते डाकू दिखता है और कैसे मैंने अपहरण किया वगैरा और सब उसको देख रहे हैं भाई।
अरमान :- वीडियो कॉल में तो यहां के भी पीछे नहीं है सर।
आलोक पुराणिक :- हां यही तो, अब हो क्या गया है दरअसल जो दिख रहा है वो बिक रहा है। एक इसका स्टारडम बन गया है कि उस स्टारडम के लिए सत्कर्म जरूरी नहीं है वह काम कीजिए जिसकी विजिबल वैल्यू हो आप कर लीजिए आप स्टार बन जाएंगे। स्टार में अब क्रिमिनल भी यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और सट्टेबाज भी खोल रहे हैं और उसमें जुआरी भी खोल रहे हैं।
अरमान नदीम:- चलो यह तो एक बात है कि दिख रहा है आईटी सेल के जरिए हो रहा है लेकिन लोग इसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं क्या वाकई लोगो की सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है?
आलोक पुराणिक :- सर, ऐसा है कि क्या हमारी जनता को हमारे लोगों को वाकई में एक मानसिक मैच्योरिटी की शिक्षा दी गई या उनके लिए शिक्षित किया गया लोग जैसे हैं वैसे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं एक जमाना था जब मानता था कि शिक्षा में फर्क आता था। लेकिन अब बड़े-बड़े शिक्षा प्राप्त किए लोग भी मार मचाये हुए हैं। तो मुझे लगता है जो एक भौतिक ट्रेनिंग भारत वर्ष के लोगों को होनी चाहिए थी वह हुई नहीं है और इसका असर बहुत दिखाई भी पड़ता है। आप कुछ भी कह दीजिए वह चीड़ जाता है। तमाम तरह के बाबा हैं जिनके बलात्कार के आरोप सिद्ध , साबित हो चुके हैं जिन पर हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं लेकिन उन बाबा के आपको लाखों फॉलोअर मिलेंगे।
अरमान नदीम:- आज की तारीख में उनके फॉलोअर मरने मारने को तैयार बैठे हैं।
आलोक पुराणिक :- क्योंकि वह इतने पावरफुल हैं कि वह चुनाव जितवाते हैं और चुनाव हरवाते हैं। तो अब सवाल यह है कि चुनाव जितवाने हरवाने में इनका हाथ है। समझदार है जो वह कहता कौन इनके चक्कर में पड़े चुपके से पतली गली से निकाल लेता है और अगर आप टीवी देखे तो एक अतिरेक स्वर को ही अट्रैक्शन मिल रही है। एक तार्किक बात करने वाले को नहीं सुना जाएगा। आज सुबह सोच रहा था बुद्धिमता का मार्ग है जो हमेशा मध्य से जाता है भगवान बुद्ध ने ही कहा था।
अरमान:- क्योंकि अगर आप सामने वाले की बात को सुनेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे?
आलोक पुराणिक:- समझना तो उद्देश्य ही नहीं मुझे अगर पापुलैरिटी चाहिए तो मैं एक वह एक्सट्रीम पोजीशन लूं कि जिसमें सुनकर लोग कहें के बड़ी सही बात कर रहे हैं और वही में बैलेंस बात कहूं तो वह कहेंगे कोई मतलब ही नहीं इसकी बातों में फील नहीं आ रही।
अरमान:- और यह बात हर धर्म मजहब के हैं अगर कोई हिंदू इस तरह की बात करता है तो मुसलमान उसको बोलेंगे। मुस्लिम कहता नजर आएगा तो हिंदू पक्ष क्रिटिसाइज करेगा। लेकिन खुद पर सवाल नहीं उठाएंगे यह तो इकबाल साहब कहते हैं “अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है” तो वह बस सामने वाले को देख रहे हैं खुद के किरदार पर तो पर्दा डाले बैठे हैं।
आलोक पुराणिक:- जी, बिल्कुल अब इसमें मीडिया का क्या योगदान है कि मीडिया को चाहिए टीआरपी और वह संतुलित बात से आती नहीं टीआरपी अतिरेक की बात से आती है।
अरमान :- मेरा अगला सवाल भी कुछ इसी के आसपास का ही है कि लोग धर्म और संस्कृति को एक ही मान लेते हैं। मैं इसे आपको इस तरह से बता सकता हूं की धर्म के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में पाकिस्तान तो बना दिया लेकिन वह संस्कृति ही थी जिसने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिया। और आज की तारीख में जब हम धर्म और संस्कृति को आमने-सामने रखते हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं इस पर आपके विचार क्या है?
आलोक पुराणिक:- देखिए इंडोनेशिया में एक बार पाकिस्तान के नेता गए तो वहां उन्होंने तमाम जगह देखा गणपति की फोटो है करेंसी नोट पर भी तो पाकिस्तान के मंत्री ने पूछा आप तो ईमान वाले लोग हैं हिंदुओं के देवी देवता आपके यहां क्या कर रहे हैं ?आपके नोट पर। तो कहां देखे साहब हमने अपना धर्म बदला है हम अपने पूर्वज थोड़ी ना बदलेंगे तो धर्म और संस्कृति में फर्क तो यह है कि गणपति संस्कृति के तौर पर आपके साथ न जाने कब से हैं। धर्म बदलें तो भी कोई दिक्कत नहीं धर्म बदलने के बाद आप एक दूसरे के साथ न्यूनतम सद्भाव तो रखें 1947 में जब देश डिवाइड हो रहा था तब मौलाना आजाद ने एक बहुत बढ़िया स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को आप बहुत लंबे वक्त तक बांध के नहीं रख पाओगे ।क्योंकि उनको दिखाई पड़ गया था कि वह निहायत ही निकम्मे किस्म के लोग हैं इतने पावर हंगरी हैं की नाक से आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता इन लोगों को। और जब उर्दू को थोपा गया पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश पर वहाँ रिवॉल्ट हो गया। धर्म बहुत ही अलग मसला है और एक जो न्यूनतम समझदारी है वह जब अनुपस्थित हो जाती है तो फिर समझना और समझना दोनों ही मुश्किल हो जाता है।
अरमान:- मैं एक चीज आपको यह पूछना चाह रहा हूं की जिन्हें तमगा मिला महान लेखक होने का ,महान कवि होने का क्या वह कुछ हद तक बायस्ड थे? क्या उन्होंने पूरी सच्चाई लिखी?
आलोक पुराणिक :- देखिए, पूरी सच्चाई नदीम साहब एक ऐसा कांसेप्ट है जिनके अलग-अलग मायने हैं इसका पूरी सच्चाई का प्रैक्टिकल अलग है। पॉलिटिकल अलग है बड़े लेखक जिनको हम मानते हैं बड़ा लेखक में कहता हूं। जिसकी रचना हमारे पास 50 साल बाद 100 साल बाद भी दमदार लगे और वह बड़े लेखक क्यों हैं क्योंकि एक वक्त की छन्नी पार करने के बाद भी हमें लगता है कि हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। बात है कि क्या सच्चा क्या झूठ। सच्चा-झूठा भी बहुत सब्जेक्टिव है क्योंकि जो आपको सच्चा लग सकता है मुझे झूठ लग सकता है आपको जो सही लग सकता है मुझे गलत लग सकता है।
अरमान:- तो उन्होंने उसे वक्त की ऑडियंस के हिसाब से लिखा।
आलोक पुराणिक :- हां, जैसे हम एक बड़े लेखक का एग्जामपल लें प्रेमचंद उनकी एक कहानी है कफन उसमें एक स्त्री मर रही है दर्द की अवस्था में है और उसके पति और उसका ससुर निहायत ही गैर जिम्मेदार नालायक किस्म के व्यक्ति हैं और वह मर जाती है और उसके कफन के लिए पैसे से शराब ले आते हैं तो कहानी पढ़ते वक्त आप उन दो कैरेक्टर के प्रति स्त्री के पति और उसके ससुर के प्रति बहुत नाराजगी से भर उठते हैं कितने निकम्मी लोग हैं लेकिन प्रेमचंद आखिर में बताते हैं कि वह इतने गैर जिम्मेदार और लापरवाह क्यों हो गए पहले वह मेहनत करते थे गांव में वह उनको कुछ खास नहीं मिलता था तो उन्होंने कर्मठता के बजाय निकम्मेपन को जीवन में अपनाया तो यह बताता है कि जो समाज के सबसे नीचे तबके के खड़ा मजदूर उसको जो उसका प्रति भाग मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा यह जो कहानी है वह ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं है वह कहानी यह इंसानियत की तरह जटिल है
अरमान :- जैसे हम खुले शब्दों की बात कहें तो मंटो को देखिए
आलोक पुराणिक :- अरे मंटो ,मंटो एक अलग जीनियस है मंटो बड़े हिम्मती लेखक थे उनके जैसा बनना बड़ा मुश्किल है भाई ,मंटो अपने आप में बहुत ही हिम्मती थे उनके जैसे तो मेरे ख्याल से उनके पहले हुए और ना उनके बाद हुआ वैसा होना आसान नहीं है
अरमान :- मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने कहा कि व्यंग्यकार को पत्रकार का दर्जा हासिल है लेकिन एक लेखक , शायर, कवि को वह दर्ज नहीं मिलता
आलोक पुराणिक:- मैं यही बताना चाहूंगा कि जो लेखन की बहुत सारी विधाएं हैं तौर तरीके हैं जैसे कहानीकार है। कहानीकार कहानीकार है पत्रकार नहीं है। कवि कवि है पत्रकार नहीं है लेकिन व्यंग्यकार एक तरह से पत्रकार है और एक तरफ से साहित्यकार है जैसे शरद जोशी जी रोज व्यंग लिखते थे नवभारत टाइम्स में पत्रकार भी माने जाते थे। आप उस वक्त पैदा भी ना हुए हो, मुंबई में एक अखबार निकलता था आफ्टरनून डिस्पैच एंड कोरियर करके इंग्लिश का अखबार था मैंने देखा उसके आखिरी पेज पर एडिटर का एक कॉलम आता था। राउंड एंड अबाउट शायद कॉलम का नाम था। बहराम ठेकेदार नाम था उनका यह मैंने अपनी आंखों से देखा लोग वह अखबार खरीदते और पहले उस कॉलम को पढ़ते थे फिर बाकी के पूरे अखबार को पढ़ते थे। तो व्यंग्यकार का सम्मान अखबार में इस तरह होता। क्योंकि व्यंग्यकार के पास एक छूट होती है की करंट सिचुएशन करंट, विषय पर वह एक व्यंग लिखे और अखबार उसको छापे और एक समर्थ व्यंग्यकार कहीं ना कहीं आधा पत्रकार हो जाता है। व्यंग्यकार की रीच बहुत होती है उसको लोग पढ़ते भी ज्यादा हैं व्यंग्यकार का जिम्मा भी बहुत बड़ा होता है उसे बतौर पत्रकार ,साहित्यकार बतौर कम्युनिकेटर जो कुछ कहे बोले उसे बहुत गंभीरता से कहना और बोलना चाहिए।
अरमान नदीम - आपके अनमोल विचारों से युवा पाठकों को नई दिशा मिलेगी । बातचीत हेतु आपका बहुत धन्यवाद सर ।
आलोक पुराणिक :- धन्यवाद ।
 Ramesh Saini
Ramesh Saini
रमेश सैनी
देश के प्रख्यात साहित्यकार , व्यंग्यकार रमेश सैनी से साहित्य,समाज और व्यंग्य विधा पर कॉलम शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
व्यंग्यकार की भूमिका केवल शोषित के साथ खड़े होने में है। - रमेश सैनी
परिचय
नाम - रमेश सैनी
*जन्म - 3 जून 1949, महाराजपुर (मंडला) म.प्र.।
*शिक्षा - विज्ञान स्नातक, स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान) 1982, मेँ कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा
*प्रकाशन - विगत 55 वर्षों से सारिका, माधुरी, इंडिया टुडे, कादम्बिनी, नवनीत, वागर्थ, कथादेश, कादम्बरी, साक्षात्कार, मायापुरी, नई गुदगुदी, व्यंग्य यात्रा,मरु नवकिरण, आसपास, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, दैनिक भास्कर, युगधर्म, स्वतंत्र मत, दैनिक देशबंधु,नवीन दुनिया,राजस्थान पत्रिका, जनसंदेश, सुबह सबेरे, अनवरत, उत्तर उजाला, जनपक्ष,अमर उजाला, आज, ब्लिट्ज, रविवार, आदि पत्र-पत्रिकाओं में व्यंग्य और कहानियों का प्रकाशन।
प्रसारण - जबलपुर, भोपाल, छतरपुर, लखनऊ, दिल्ली आदि आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्रों से कहानी, कविता ,कहानी और व्यंग्य रचनाएं विभिन्न रचनाओं का प्रसारण तथा व्यंग्य और कहानी पर विमर्श का प्रसारण।
अनुवाद - अनेक रचनाओं का बंगला, पंजाबी, अंग्रेजी और नार्वेरियन भाषा में अनुवाद।
सम्पादन - अंतर्राष्ट्रीय संस्था सर्विस सिविल इन्टरनेशनल (स्विट्जरलेण्ड) जिसकी सौ से अधिक देशों में शाखाएं हैं,भारत शाखा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ‘प्रयास’ का अनेक वर्षों तक संपादन सभी देशों में प्रसारित जिसका संस्था के अनेक, तथा "जाबालि सैनी बंधु "अख़बार का अनेक वर्षों तक सम्पादन।
कृतियाँ - मेरे आसपास, बिन सेटिंग सब सून, पाँच व्यंग्यकार, मेरी प्रतिनिधि व्यंग्य रचनाएँ ,अतृप्त आत्माओं की मुक्ति (व्यंग्य संग्रह), अंतहीन वापिसी (कहानी संग्रह), सब कुछ चलता है, बक्से में कुछ तो है (व्यंग्य उपन्यास) शीघ्र प्रकाश्य।
बक्से में कुछ तो है (व्यंग्य उपन्यास) के अधिकांश अंश व्यंग्य की एक मात्र गंभीर और महत्वपूर्ण पत्रिका 'व्यंग्य यात्रा' में प्रकाशित। इसी के साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में अंश प्रकाशित.
इसी के साथ दूसरा व्यंग्य उपन्यास "सब कुछ चलता है" भी शीघ्र प्रकाशित।
*व्यंग्य आलोचना पर निरंतर कार्य, -व्यंग्य आलोचना पर व्यंग्य की सामाजिक परिवेश में आवश्यकता, व्यंग्य के शास्त्रीय कोण, व्यंग्य का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैयक्तिक प्रभाव इससे संबंधित विषयों पर केंद्रित पचास से अधिक आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित, इसके प्रभाव तथा इससे मुझे आलोचना के क्षेत्र में जाना जाने लगा।
* व्यंग्य आलोचना पर शीघ्र ही आलोचना पर पुस्तक प्रकाश्य.
*'व्यंग्य यात्रा' द्वारा व्यंग्य आलोचना पर आयोजित विभिन्न स्थानों में आयोजित संगोष्ठियों में सहभागिता और व्यंग्य विधा पर केंद्रित अनेक विषयों पर जबलपुर , दिल्ली , डलहौजी (दो बार),श्रीगंगानगर राजस्थान (दो बार) मडगांव (गोव, कुल्लू मनाली (हिमाचल प्रदेश )में, बिलासपुर,दुर्ग (छत्तीसगढ़), शिमला, उज्जैन में वक्तव्य ,शब्दायतन द्वारा गोरखपुर में व्यंग्य केन्द्रित वक्तव्य।
* इसी तरह व्यंग्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की जन्म शती के अवसर पर जबलपुर में दो बड़े और महत्वपूर्ण आयोजन आयोजित करना, जिसमें डाॅं. प्रेम जनमेजय, डाॅं. रमेश तिवारी,डाॅं. सेवाराम त्रिपाठी सहित अनेक विद्वानों की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही । चार सत्रों में हरिशंकर परसाई और व्यंग्य पर विचार विमर्श।इन आयोजनों की स्मृतियां लोगों के हृदय में स्थान बनाए हुए हैं।
* हरिशंकर परसाई जी जन्म शती के अवसर पर परसाई जी पर केंद्रित संस्मरण और उनके साहित्य और लेखों पर केंद्रित समालोचनात्मक आलेख विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित ।
सम्मान/पुरस्कार -
*कादम्बिनी (मासिक पत्रिका) द्वारा
कादम्बिनी सम्मान - 1994,
*म.प्र. युवा रचनाकार सम्मान-सन् -1992
*मध्यप्रदेश साहित्यकार मंच सम्मान सन्1995
*म.प्र. लघु कथा परिषद द्वारा लघुकथा सम्मान सन् 1996
*पाथेय जबलपुर द्वारा "सृजन सम्मान "-सन् 2002
*मध्यप्रदेश लघुकथाकार परिषद द्वारा "यश अर्चन" सम्मान सन्-2002
*हीरालाल गुप्त स्मृति सम्मान।
*मध्यप्रदेश लघु कथाकार परिषद द्वारा अखिल भारतीय स्व. रासबिहारी पाण्डेय स्मृति सम्मान सन् 200
व्यंग्य यात्रा (पत्रिका) द्वारा व्यंग्य यात्रा सम्मान सन्-2015
*शोभना ट्रस्ट दिल्ली द्वारा "व्यंग्यकार सम्मान" सन्-2017
*ज्योतिबा फुले सम्मान भोपाल द्वारा फुले सम्मान सन् 2016
मध्यप्रदेश आंचलिक परिषद् का "अखिल भारतीय स्व. रासबिहारी पाण्डेय स्मृति व्यंग्य सम्मान"सन्-2017
*सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी की स्मृति में "गंगेश्वर उपाध्याय कहानीकार सम्मान" गहमर ( उ.प्र) सन् 2018
*बिलासा कला मंच द्वारा सम्मानित सन् -2018
*हिंदी साहित्य एवं व्यंग्य संस्थान द्वारा सम्मानित सन् 2020
न्यू भूमिका साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा व्यंग्य साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया
*साहित्य संगम संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सम्मानित सन् 2022
*माता कौशल्या ज्योतिष साहित्य संस्कृति शोध पीठ एवं डॉ. माया ठाकुर फाउंडेशन से व्यंग्य विभूषण सम्मान से सम्मानित सन् 2023
* गया प्रसाद खरे स्मृति साहित्य कला एवं खेल संवर्धन मंच द्वारा "शांति गया साहित्य भूषण सम्मान से अलंकृत 8 जून 2024"
बी पी ए फाउंडेशन एवं इंडिया नेटबुक्स द्वारा 'आनंदी देवी अवस्थी साहित्य भूषण सम्मान' से सम्मानित किया किया गया 2024
व्यंग्यधारा द्वारा गत वर्ष हम (रमेश सैनी ) पर 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम हुआ इसमें रमेश सैनी पर केंद्रित उनकी रचनाओं, व्यंग्य आलोचना और कहानियों पर विस्तार से विमर्श का आयोजन जबलपुर में हुआ जिसमें देश के सभी दिशाओं से लगभग 35 सर्व श्री व्यंग्य आलोचक डा.रमेश तिवारी डॉ.सेवाराम त्रिपाठी, अनूप शुक्ल, विनोद साव, कैलाश मण्डलेकर डॉ प्रदीप मिश्र, राजेंद्र चंद्रकांत राय, टीका राम साहू आजाद सहित वरिष्ठ व्यंग्यकार और युवा व्यंग्यकार साहित्यकार सम्मिलित हुए और उन्होंने रमेश सैनी के प्रति अपनी भावना व्यक्त की इसी अवसर पर अनवरत मासिक पत्रिका रमेश सैनी पर केंद्रित विशेषांक "रमेश सैनी एकाग्र "अतिधि संपादक डॉ.रमेश तिवारी का विमोचन हुआ। यह अंक शीघ्र ही पुस्तक रूप में प्रकाशित होकर आ रहा है।
*जयलोक दैनिक, जबलपुर द्वारा रमेश सैनी के 50 वर्ष होने पर हम पर (रमेश सैनी) पर केन्द्रित अंक का प्रकाशन 3/6/1999.
*अंतरराष्ट्रीय संस्था - सर्विस सिविल इंटरनेशनल संस्था (भारत शाखा) शाहदरा दिल्ली में कुष्ठ रोगियों की दो वर्षों तक सेवा सुश्रुषा तथा ,उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।
*1972 उदयपुर (राजस्थान) के आसपास के गाँवों में जल-समस्या तथा समस्याओं पर गहन कार्य।
*1970 में एस सी आई के माध्यम से हरियाणा, बिहार आदि क्षेत्रों में लोककल्याण कार्यों का निर्वहन.
*एस सी आई अंतर्राष्ट्रीय संंस्था की दिल्ली शाखा में तीन वर्षों तक सचिव
*साहित्यिक संस्था - मिलन, मित्र संघ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन (जबलपुर शाखा), म.प्र. लेखक संघ (जबलपुर इकाई), साहित्य संघ, पहल गोष्ठी आदि संस्थाओं में अनेक पदों पर सक्रियता से सहभागिता,विभिन्न
*कहानी मंच में ‘अध्यक्ष’ तथा अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों का संयोजन।
* "व्यंग्य यात्रा" द्वारा आयोजित विभिन्न शहरों जबलपुर, ,डलहौजी, गोवा, बिलासपुर, दुर्ग,(नगपुरा) श्रीगंगानगर, कुल्लू, दिल्ली गोवा,आदि व्यंग्य शिविरों में व्यंग्य आलोचना के विभिन्न विषयों पर आलोचनात्मक वक्तव्य।
रायपुर ( छग ) गोरखपुर ( उप्र ) आदि व्यंग्य आयोजन में व्यंग्य आलोचना पर वक्तव्य.
*विगत वर्षों से व्यंग्य पर केंद्रित संस्था व्यंग्यम का संयोजन.संचालन.
* व्यंग्यम संस्था का विगत छ:वर्षों से संयोजक का दायित्व का निर्वाह करते हुए व्यंग्यम द्वारा निरंतर व्यंग्य पाठ गोष्ठी , व्यंग्यम गोष्ठी में व्यंग्य विधा पर व्यंग विमर्श गोष्ठी का आयोजन तथा व्यंग्य पुस्तकों पर समीक्षा गोष्ठी का आयोजन करना.
* विगत पाँच वर्षों से डॉ.रमेश तिवारी और रमेश सैनी के संयुक्त तत्वावधान में व्यंग्यधारा समूह में व्यंग्य को केंद्र में रखकर व्यंग्य के आलोचना पक्ष में विमर्श का आयोजन करना. अभी तक 175 आन लाइन गोष्ठी का आयोजन। जिसमें एक लेखक की रचनाओं का पाठ और उस पर विमर्श, वरिष्ठ व्यंग्यकारों संतोष खरे, कुंदन सिंह परिहार, श्रीकांत चौधरी एकाग्र पर आयोजन, व्यंग्य को केन्द्र में रखकर व्यंग्य के विभिन्न बिंदुओं सामाजिक, राजनीतिक वैयक्तिक, सामाजिक सरोकारों, वर्तमान व्यंग्य लेखन के स्तर और उसकी गंभीरता,पर हमारे समय के महत्वपूर्ण व्यंग्यकार सहित अनेक विद्वानों व्यंग्यकार आलोचकों लगभग अस्सी गोष्ठियों में विमर्श वार्ताओं के माध्यम से व्यंग्य विधा का संवर्धन करना,इसी के साथ साहित्य और पाठकों के मध्य में प्रचारित प्रसारित करना। व्यंग्य की अनेक पुस्तकें पर समीक्षा गोष्ठी कर चर्चा करना।
*खेल - टेबिल टेनिस में अनेक वर्षों तक जिला स्तर और प्रादेशिक स्तर पर ठीम प्रतिनिधित्व, अनेकानेक विजेता, उपविजेता पुरस्कार/सम्मान अर्जित किया
*विदेश - सर्विस सिविल इन्टरनेशनल द्वारा 1972 में पश्चिम जर्मनी आमंत्रित,
सम्प्रति - रक्षा लेखा विभाग से वरिष्ठ अंकेक्षक पद से सेवा निवृत्त।
**
देश के प्रख्यात साहित्यकार , व्यंग्यकार रमेश सैनी से साहित्य,समाज और व्यंग्य विधा पर दैनिक युगपक्ष के कॉलम शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
व्यंग्यकार की भूमिका केवल शोषित के साथ खड़े होने में है। - रमेश सैनी
अरमान:- साहित्य जगत में रमेश सैनी जी एक बड़ा जाना माना नाम है, लेकिन आपका रुझान साहित्य में किस तरीके से बना और भाषा के प्रति आपके प्रेम के बारे में कुछ बताइए।
रमेश सैनी:- स्कूली वक्त में अपने दादा दादी जी के साथ मंडला जिले के एक कस्बे महाराजपुर में रहा करता था। हमारे आसपास आदिवासियों का इलाका था । आज भी वहॉं आपको यही परिवेश देखने को मिल सकता है। वहॉं पर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था । तकरीबन सातवीं ,आठवीं क्लास की बात होगी । मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं । हमारे एक शिक्षक थे ।नाम था शिवकुमार शर्मा बागी और वे काफी अच्छे कवि थे ,काफी अच्छा लिखते थे और उनका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। उनका टाइम मेनेंजमेंट बहुत बढ़िया था। जो सिलेबस के विषय हैं ,उन्हें तो वह पढ़ाया ही करते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो घटनाएं घटित हो रही हो, देश दुनिया में उसके बारे में भी बच्चों को जागरूक और उनकी जानकारी दिया करते थे। और वह हमेशा अपने पास में किताब रखा करते थे। जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जापान में किस तरह का संघर्ष हुआ होता था। वहॉं की जनता संघर्ष भी युद्ध का सामना कैसे करती थी, उसको भी पढ़ाया करते थे। उसका विवरण उस किताब में हुआ करता था। हमारा जो पढ़ाई का पीरियड 40 मिनट का था। जिसमें वह 30 मिनट हमें पढ़ाई करवाते और आखिर के 10 से 12 मिनट उस किताब में से हमें यह बताते कि किस तरीके से वहॉं के लोगों ने उस युद्ध के वक्त में कैसे संघर्ष किया और सेना की कैसे मदद की। जनता ने किस प्रकार से अपना साहस दिखाया और वे यह दिखाते और समझाते थे कि देश प्रेम क्या होता है। कहते थे कि देश को बचाने की, रक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ सेना की नहीं ,हम आम जनता की भी होती है। उसी के साथ-साथ वह अन्य कवियों के कविता भी पाठ और आलेख पढ़कर सुनाया करते, देश प्रेम की कविताएं हमें सुनाया करते थे तो वहॉं से ही हमें साहित्य के प्रति जो रुझान हुआ वह आज भी है। एक चीज के लिए वे हमें प्रोत्साहित किया करते थे कि पढ़ाई के साथ-साथ कुछ और चीजों में भी अपनी रुचि बढ़ाओ। चित्रकारी या कुछ लिखना शुरू करो । क्योंकि हमारा परिवार इतना समृद्ध परिवार नहीं था की चित्रकारी जैसी चीजों में पैसा जाया जाए करें।हां फिर वहॉं कलम का सहारा लिया यह हमें सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ लगा और लिखने का निर्णय लिया तब वहीं से लिखना शुरू किया। पहिले एक कविता लिखी और उन्हें दिखाई। तब उन्होंने कहा -"अच्छी लिखी है" और ऐसा कहकर मुझे प्रोत्साहन दिया और साथ ही में वह कविता भी उन्होंने अखबार में प्रकाशनार्थ भेज दी और वह जब छपी तो मैं उस वक्त इतना खुश हुआ कि मेरी कविता अखबार में आई है। उस अखबार को दोस्तों और पड़ोसियों को दिखाता फिरता।
अरमान:- इस प्रकार बाद में आपने व्यंग्य विधा पर काम किया है । वाकई वह प्रेरणा का स्रोत है और मुझे सौभाग्य मिला वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रेम जनमेजय जी से वार्ता करने का और उनसे बातचीत के दौरान भी व्यंग्य पर काफी कुछ चर्चा हुई । आपसे सवाल रहेगा कि आपकी नजर में मौजूदा वक्त में व्यंग्य और व्यंग्यकार की क्या भूमिका है ? उस परिवर्तन को आप किस प्रकार से देखते हैं जब आपने शुरुआत की थी।
रमेश सैनी:- आपने प्रेम जनमेजय जी का नाम लिया वह हमारे काफी घनिष्ठ हैं और लंबे वक्त से परिचित हैं । व्यंग्य की भूमिका की अगर बात करें। जब व्यंग्य लिखना शुरू किया गया तो यह सामाजिक परिवर्तन को उजागर करने की और पाखंड को उजागर करने का माध्यम लगा, और जो बदलाव हो रहे थे। समाज के विपरीत जाते थे। जिस प्रकार समाज में दोगलापन बढ़ रहा था उन्हें उजागर करने की जरूरत महसूस हुई।आम जनमानस में शासकीय कामकाज में जो भ्रष्टाचार फैल रहा था। उससे आम जन में असंतोष फैल रहा था। उन सब चीजों को लेकर व्यंग्य सामने आया था। और सही मायने में व्यंग्य की सबसे पहले और बड़ी भूमिका का यही थी कि इन सभी चीजों को उजागर करे और निष्पक्षता से उजागर करना। साहित्य हमेशा से समाज के साथ है, मानव के साथ है, सामाजिकता के साथ है क्योंकि व्यंग्यकार के पास में और कोई विकल्प नहीं है। व्यंग्यकार हमेशा शोषित के साथ खड़ा होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब साहित्यकार , व्यंग्यकार यह कहते हैं लेखक को तटस्थ होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि व्यंग्यकार तटस्थ नहीं हो सकता, और मान कर चलिए अगर व्यंग्यकार तटस्थ हो रहा है तो वह धोखा दे रहा है खुद को भी और सामने वाले को भी। व्यंग्यकार की भूमिका केवल शोषित के साथ खड़े होने में है। कोई और जगह है ही नहीं। कहानी में हो सकती है ,यह दूसरे किसी विधा के लेखन में हो सकती है। लेकिन व्यंग्य में उसकी केवल यही भूमिका है कि वह सामाजिक मूल्यों पर शोषित के साथ खड़ा हो । यह महत्वपूर्ण बात है और व्यंग्य की सबसे बड़ी भूमिका। यह भी है कि उसने अपने आप में कोई विकल्प नहीं रखा। सामाजिक सरोकार के साथ में जुड़ा है। हमेशा से उस कमजोर वर्ग के साथ में जुड़ा है जो अपना प्रतिरोध नहीं कर सकते। प्रतिरोध के लिए शब्द ढूंढता है ,भाषा ढूंढता है उसका उपयोग लेखक कैसे करता है उसी से व्यंग्य होता है और न जाने क्यों आज के समय में इसकी भूमिका अपने आप बदलती जा रही है।अब इसे देखकर चिंता भी होती है क्योंकि आज व्यंग्य लाभ और हानि को देखकर लिखा जा रहा है। आज कल के अधिकांश लेखक इसी तरह से लिख रहे हैं और यह सब देखकर यूं लगता है कि उन्होंने हमसे पहले वाले व्यंग्यकार और उनकी लेखनी को पढ़ा ही नहीं है या फिर परसाई की समकालीन पीढ़ी को भी कम पढ़ा है। आज के लेखकों के दिमाग में एक बात हमेशा रहती है उन्हे लगता है कही हमारा किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। हमें अपने आने वाले लाभ में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए । राजनीतिक विसंगतियों पर अगर हम बात करें। कहीं वह राजनीतिक व्यक्ति हमसे नाराज ना हो जाए। अगर नौकरी कर रहे हैं तो मन में डर बैठ जाता है की नौकरी में किसी तरह की समस्या ना आ जाएं। और यह सब बातें व्यंग्य में बहुत गहराई तक चली गई है लोग डर-डर कर बच बच कर लिख रहे हैं। इसी का यह कारण है कि व्यंग्य की जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह इन चीजों से बड़ी विचलित होती जा रही है। इसके ऊपर अगर मैं आपको बात कहूॅं तो लोग आज व्यंग्य को याद नहीं रख पा रहे हैं उसे भूल जाते हैं। आज हम देखते हैं। हमें परसाई बहुत याद आते हैं उनके समकक्ष या उनसे पहले के व्यंग्यकार याद आते हैं, लेकिन आज के व्यंग्यकार हमें याद नहीं आते, ना नाम ध्यान में आता है। कोई रचना अगर हम पढ़े सवेरे पढ़े और शाम को याद नहीं रहती। वो बात नहीं रही, वो साहस नहीं रहा व्यंग्यकार का। अब वह साहस नहीं रहा व्यंग्यकार की उससे मुठभेड़ की जाए। विसंगतियों से मुठभेड़ कर सके ,उस प्रवृत्तियों से मुठभेड़ कर सके। पहिले जन जन की बात हुआ करती थी ,पर वह नहीं कर पाते। बोलो, जो सिर्फ अपना नुकसान ही देखते हैं यानी कि नफा नुकसान देखकर लिखने वाले ही आज व्यंग्य को भटका रहे हैं। इनका आम पाठक है। वह समझता है कि यही व्यंग्य है। अभी पूरी तरह बदला नहीं है कि न ही यह पूरी तरीके से परिवर्तित हुआ है। आज भी बहुत लोग हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं । महत्वपूर्ण लिख रहे हैं, जोरदार लिख रहे हैं, मतलब कि यह कि ना तो उन्हें सत्ता का डर है, ना किसी के क्रोध का डर है, और ना ही किसी की नाराजगी से उन्हें फर्क पड़ता है । और यही लेखक आज भी व्यंग्य को जिंदा रखे हुए हैं । और पाठक है उन्हें भी इस चीज की समझ है। व्यंग्य की यही चीज दूसरी विद्या वालों को आकर्षित करती है क्योंकि हम इसमें अपने मन की बात कह सकते हैं। एक चीज में यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग नया लिख रहे हैं जिन्होंने अभी 5-10 साल पहले लिखना शुरू किया है उनसे यह आग्रह रहेगा की आप लिखिए लेकिन विरोध का स्वर कम नहीं होना चाहिए साथ ही में आप लिखे भी और पढ़े भी आप पुराने लोगों को पढ़िए। ऐसा नहीं था कि परसाई जी को विरोध का सामना ना करना पड़ा हो उन्होंने भी विरोध का सामना किया। शरद जोशी जी उनको भी बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा और उन जैसे लेखक को अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ा लेकिन उन्होंने इस चीज के बाद में भी लिखना नहीं छोड़ा। लेखनी में जो साहस था उसे कमजोर नहीं होने दिया। लोग कहते हैं कि हमको समाज को बदलने की जरूरत है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम व्यंग्य के माध्यम से समाज को बदलते नहीं है ,उसे जागरुक करते हैं और यही हमारी कोशिश भी रहती है समाज की जो कमजोरियां हैं उन्हें पिन आउट करते हैं। समाज में कमजोरी है, व्यक्ति में कमजोरी है जो संस्था में कमजोरी है जो सत्ता में कमजोरी है उसे कमजोरी की बात करनी होगी उसे जागरूकता के साथ में लोगों के सामने लाना होगा। अपनी बात में मैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहूंगा। परसाई जी की एक रचना है ।उनका एक प्रसंग है जिसमें एक व्यक्ति के दो बेटे होते हैं दोनों पढ़ रहे हैं संध्या वंदन के समय यानी शाम के वक्त में जो व्यक्ति पीता है पिता की इच्छा पीने की होती है और वह अपने छोटे लड़के को सोडा लाने को कहता है कि यह पैसा ले और सोडा लेकर आ जा । इस बात पर वह लड़का मना कर देता है। वह कहता है कि अभी मैं पढ़ रहा हूॅं ,मेरा पूरा पाठ हो जाएगा उसके बाद ही मैं सोडा लाऊंगा।यह बात सुनकर वह अपने बड़े बेटे से कहता है और वह लड़का दौड़ कर चला जाता है तब बाप इस दृश्य को देखकर कहता कि आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं बाप का कहना नहीं मानते। वो कहता है कि बड़ा बेटा अच्छा बेटा है। आप यह देखिए कि वह किस चीज को अच्छा कह रहा है। बेटे का साहस देखिए वह स्थिति के अनुसार अच्छी जो चीज है, उसका चुनाव करता है और फैसला करता है। कहता है कि मैं अभी नहीं जाऊंगा बाद में जाऊंगा अपना पाठ पूरा करने के बाद जाऊंगा। यही व्यंग्य की शक्ति है। अगर हम बात करें कोरोना काल की। कितनी अराजकता फैल गई थी अस्पतालों में और दूसरी चीजों के अंदर जो जरूरत के समान है उसमें किस तरीके से लूटपाट हो रही थी किसी भी प्रकार का भय नहीं था कि हम किस हद तक जाकर लूट मार कर रहे हैं। अनाप शनाप पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लाखों लोगों की जान चली गई। परिस्थितियों भी हुई कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो रही है और सामने वाला ऑक्सीजन मांगने आया है तो बेड पर लेटे हुए व्यक्ति की ऑक्सीजन निकालकर उसे दे दी जाती है जो नया मरीज आया है कि कहीं यह न भाग जाए और जिसकी ऑक्सीजन निकाल जाती है उसकी जान चली जाती है। मुझे इन तीन-चार साल के कालखंड में ऐसी कोई रचना नजर नहीं आती जिसे लम्बे समय तक याद रखा जा सके। इन बारे में कोई चर्चा मुझे देखने को नहीं मिलती।
अरमान :- आपने एक बात वाकई खूबसूरत और सटीक कहीं कि आज का जो व्यंग्यकार है, जो लेखक है ।वह घबराता है फिर चाहे वह राजनीतिक व्यक्ति हो या किसी और परिस्थिति वश और एक चीज यह भी कहना चाहूंगा कि 90 के दशक के बाद जो उभरा है उन्होंने साहित्य को स्टारडम की नजर से देखना शुरू किया । बड़े पर्दे पर अपने आप को देखना चाहता है इसी चीज को देखते हैं और जो युवा लेखक है उसकी परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं। जब आपने लिखना शुरू किया तब आप भी युवा थे वह वक्त और आज का वक्त क्या फर्क देखा हैं ?
रमेश सैनी:- अरमान यह आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। विचारणीय सवाल है । इस मुद्दे पर वाकई बड़ी गंभीरता के साथ में चर्चा करनी चाहिए। मैं आपको बात कहूॅं कि हम लोगों में हमारे जो बुजुर्ग थे व्यंग्य के प्रतिष्ठित नाम में से एक परसाई जी हमारे शहर के है। परसाई जी कहा करते थे की पढ़िए और पढ़ने का मतलब यहां मैं आपको बताऊं अगर हम कहानी लिख रहे हैं, हम व्यंग्य लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं वह कहते थे कि अगर हम व्यंग्य लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ हम व्यंग्य ही पढ़े ,कहानी लिख रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं की पुरानी कहानियां ही पढ़े। आप पढ़िए सबको पढ़िए और उसके साथ आपको समाजशास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। आपको विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। दर्शनशास्त्र भी पढ़ना पड।साथ ही में आपको अर्थशास्त्र की भी समझ होनी चाहिए। साहित्य के अलावा भी आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। जब आप समाजशास्त्र पढ़ोगे तो समाज में हो रहे परिवर्तन को विश्लेषण कर पाते हो। जब आप विज्ञान पढ़ते हो तो वर्तमान में अपनी जीवन शैली को समाज परिवर्तन को वैज्ञानिक दृष्टि से देख पाते हो। उसमें वह वैज्ञानिक दृष्टि उत्पन्न होगी। सब विचारों के साथ में निश्चित ही आपके विचारों और आपकी लेखनी में भी काफी बदलाव आएगा। इतिहास पढ़ोगे तो जो ऐतिहासिक कमजोरी रही होगी जो घटनाएं घटित हुई। फिर चाहे वह स्थानीय इतिहास हो राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो हमें यह भी मालूम होगा कि कहॉं पर हमारी कमजोरी साबित हुई। इस तरह का विस्तृत अध्ययन करके जब व्यक्ति रचना करता है तो एक प्रमाणिकता का असर होगा। इससे आंतरिक संतुष्टि भी होती है कि हम जिस बारे में लिख रहे हैं ,हमें उसकी जानकारी भी है। जब रचना पाठक के पास में जाती है समझ में जाती है। उन्हें भी वह चीज मुकम्मल तौर पर नजर आती है और उसका प्रभाव ही अलग होता है। आप बगैर किसी जानकारी के, बगैर किसी अध्ययन के लिखते हो तो उसका भी लोगों के बीच में प्रभाव तो होता है लेकिन गलत। अपने दौर में पढ़ते थे हम पत्रिकाएं पढ़ते थे हम दूसरी किताबें पढ़ करते थे और पढ़ने के बाद में हम लोग लिखा करते थे और लिखने के बाद खुद उस रचना को तीन-चार बार पढ़ते थे। लगातार पढ़ने से उसमें सुधार किया जाता था उसमें परिवर्तन होता था। लगातार पढ़ते रहना यह हमारी प्रकृति के अंदर आ चुका है। यह हमारे स्वभाव में आ चुका है। और एक वक्त के बाद में यह चीज सोची समझी नहीं जाती है खुद ब खुद होने लगती है। हम आज के युवा की बात करें तो उसके मन में बस यही रहता है कि एक बढ़िया नौकरी हो जाए 15 - 20 लाख का पैकेज हमारे पास में हो । पैकेज से उसकी जीवन शैली बदल सकती है लेकिन समाज में उसका नाम नहीं हो रहा। आज भी जो लोग लिख रहे हैं, तो यह भी देखने को मिलता है कि उसे पाठ के पीछे का जो ज्ञान है, वह उनके पास में नहीं है ऐतिहासिक ज्ञान है वह उनके पास में नहीं है, जो सामाजिक संदर्भ है वह उनके पास में नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह एक हड़बड़ी में लिख रहे हैं। अब तो संसाधन इतनी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। मोबाइल में बोलो और टाइप हो जाता है और रचना एक सेकंड में अखबार के पास पहुॅंच जाती है। यह चीज हमारे वक्त में नहीं हुआ करती थी। हम उसको टाइप करवाते थे ।उसके बाद में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संपादक तक भेजी जाती थी । सप्ताह सप्ताह तक इंतजार किया जाता था। कहॉं से वापस जवाब आता था कि आपकी रचना स्वीकृत हो चुकी है या फिर अस्वीकृत हुईं है। वहॉं नहीं हुआ तो दूसरी जगह भेजते थे। पेशेंस लेवल था, वह आज के वक्त में देखने को नहीं मिलता। वो पेशेंस आज की तकनीक ने खत्म कर दिया है। इसी वजह से लेखन में भी एक हड़बड़ी मच रही है। अगर वह हड़बड़ी कम हो जाए तो बात भी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं की तकनीक बिल्कुल ही खराब है। आप तकनीक का पूरा इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से कीजिए। तकनीक अपनी सुविधा के लिए है। वह हमारी कमजोरी बढ़ाने के लिए नहीं है, कम करने के लिए। साथ ही साथ में जो रचनात्मक कार्य है। उसमें और खास तौर पर लेखन में सावधानी और पेशेंस दोनों बरकरार रखने होंगे। लेखन में ही सबसे ज्यादा हड़बड़ी है। अगर मैं आपको बताऊं संगीत में हड़बड़ी नहीं है, पेंटिंग में हड़बड़ी नहीं है ,संगीत सीख रहे हैं तो उसमें तो रियाज करना ही पड़ेगा आपको। पेंटिंग में हड़बड़ी करोगे तो आप खुद देखोगे कि काम खराब हो रहा है। लेकिन आपको अपनी खराब रचना कविता या लेखन में नजर नहीं आएगी। यही बात है कि इसके पीछे की जानकारी नहीं है। रचनात्मक हो सकते हैं लेकिन सिर्फ अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं और मैं ऐसे कई युवाओं को जानता हूॅं ,जो मुझे प्रेरित करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी विषय आपके दिमाग में आता हो लेखन से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक होना चाहिए। जब जानकारी के साथ आप अपनी रचना लिखेंगे और वह पाठक के सामने आएगी तो वह परिपक्व रचना होगी। उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। और ये कमजोरी आज के युवा में भी है क्योंकि वह जानना ही नहीं चाहता। मन में विचार आया उसे टाइप किया और उसके बाद भेज दिया। यही हड़बड़ी है। छोटा सा फर्क है गंभीरता और अ
गंभीर व्यक्ति में यही चीज सोचने और समझने की है।
अरमान :-- बड़ी सटीक बात कही आपने की पढ़ने काफी कम हो चुका है। युवाओं के अंदर अपने समाजशास्त्र की बात की अर्थशास्त्र पढ़ने की बात की जब हम उनका अध्ययन करते हैं। साहित्य के अलावा सोचने की जो क्षमता है ।उसमें परिवर्तन लाती है। मेने अपने एक आर्टिकल में कहा था कि अकेले और अकेलेपन में बड़ा फर्क होता है । इसे विस्तृत रूप में देखा जाए। अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है लेकिन अकेले पन का शिकार व्यक्ति हजारों में भी खुद को अकेला पाता है जो अवसाद को भी जन्म देता है। और जिस तरीके से अध्ययन में कमी आई है अगर हम युवाओं की बात करें वो जो शिक्षा अपने आने वालों को दे रहा है। इसे आप कैसे देखते है और समाधान क्या नजर आता है?
रमेश सैनी:- परिवेश के अनुसार यह बड़ा ही जरुरी सवाल है। अगर समाचार पत्रों को हम पढ़ते हैं जो खबरें देखने को मिलती है कि बीस साल के युवक ने, चौदह पंद्रह साल के बच्चों ने आत्महत्या कर ली की ।ऐसी बहुत सी घटनाएं हमें सुनने पढ़ने को मिलती है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे नजर आती है वह सबसे चीज यही है कि व्यवहार में कमी हो रही है और लगातार परिवार छोटे होते जा रहे हैं। आस पड़ोस से मिलना जुलना काम हो गया है। बच्चे भी कम हो गए हैं। एक बहुत गंभीर और जरूरी बात भी है ।इसके साथ की जो शिक्षा प्रणाली है। वह पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसका जो प्रभाव है वह समाज के ऊपर काफी ज्यादा पड़ा है, क्योंकि मॉं-बाप चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वह बीस लाख का पैकेज लेकर आएगा और जब उसे बच्चों के सामने बीस लाख के पैकेज की बात करते हैं और जो वह बच्चा दसवीं में इ है उस वक्त से ही उसके दिमाग में यह चीज डाल दी जाती है और दसवीं के बाद में वह कोई सामान्य सब्जेक्ट चुनने की कोशिश भी नहीं करता और अगर उसकी रुचि हो या ना हो वह उसके विपरीत जाकर इंजीनियरिंग यह मेडिकल की तरफ जाता है ।कला का जो विद्यार्थी है। उसकी तरफ उसका रुझान जब है ।तब भी वह उसको नहीं चुनता। और सबसे बड़ी बात यह भी है महाविद्यालय का जो छात्र है। वह भी इस चीज को महसूस करेगा कि यह संस्थाएं इतनी व्यावसायिक हो चुकी है जिस वक्त हम पढ़ा करते थे जो कट ऑफ है या फिर जो व्यवस्था है। वह बनाई जाती थी के एक कट ऑफ होने के बाद ही आप उस विषय में जा सकते हैं। आज क्या हो रहा है कि चालीस परसेंट वाला बच्चा भी इंजीनियरिंग पड़ रहा है। और अगर मॉं-बाप के पास में पैसा है तो पचास परसेंट वाला भी मेडिकल में जा सकता है। कॉलेज की महॅंगी महॅंगी फीस भरी जा रही है। एक व्यवसाय बन चुका है। जब वह बच्चा अपना बैकग्राउंड देखा है कि मां-बाप इतना पैसा लगा रहे हैं। पढ़ाई में फिर चाहे आप मध्यम वर्ग से हो या अमीर परिवार के, तो उसे बच्चों के दिमाग में कला विषय नहीं आएगा और जब अर्थशास्त्र दिमाग में आ जाता है कि मेरे मॉं-बाप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे यही करना चाहिए। दसवीं के बाद में सब कला उस बच्चों के अंदर से बाहर आ जाती है। इतिहास उससे बाहर आ जाता है। उसकी रुचि खत्म हो जाती है। समाजशास्त्र से वह अलग हो जाता है। पढ़ने का इतना दबाव हो जाता है कि वह बाकी दीन दुनिया को छोड़ देता है। एक बार मेडिकल कर लिया जो कोर्स है। उसे पूरा कर लिया तो अब नौकरी की कांपटीशन में जाना है। इन सब घटनाओं के चलते जो जीवन के अनुभव है उनसे वह दूर होता जाता है,और वह चीज कभी उसे अनुभव ही नहीं होती। बच्चा जो कभी साहित्य में अपनी रुचि रखता था वह इस हाल में लगने के बाद में बीस लाख का पैकेज लेने के बाद में सोचे कि मैं अब लिखना शुरू करूं तो भैया अब आप क्या लिख पाओगे । आपको समाज का अनुभव नहीं रहा समाज देखा नहीं, आपने ठीक से अपने समाज को परख नहीं कलाओं को आपने देखा नहीं, इन सब क्या अभाव में आप क्या लिख पाओगे। यह एक बहुत बड़ा संकट है। परसाई जी की एक बहुत ही अच्छी रचना है । किताबों की दुकान दावों की दुकान। वह कहते हैं की किताबों की दुकान बंद हो रही है और दवाओं की दुकान खुल रही है। कि हम आज वह स्थिति देख रहे हैं जहॉं काला को खत्म किया जा रहा है। मैं आपको कह सकता हूॅ कि दस साल बाद कहीं ऐसी स्थिति न जाए ।क्या आपको इतिहास के टीचर मिलना मुश्किल हो जाए। आपको भाषाओं के टीचर मिलना बंद हो जाएंगे आपको समाजशास्त्र के टीचर मिलना बंद हो जाएंगे। हम अपनी पीढ़ी को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि ना तो हम अपने घर का भला कर पा रहे हैं और ना ही समाज का भला कर पा रहे हैं। प्रकृति है वह अपना रास्ता ढूंढ लेती है । जब बाढ़ आती है, तो पानी निकासी का रास्ता देख लेता है वही चीज धन के साथ भी है।
अरमान:- आपने कहा कि लेखन में हड़बड़ी एक चरम पर पहुंच रही है और यह बात सत्य भी है तो क्या आपको इसकी वजह यह नहीं लगती कि उन्होंने आलोचना पढ़ना और लिखना छोड़ दिया है वह उसे केवल एक विलेन के तौर पर देखते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि सब्र खत्म हो रहा है लेखन में ।
रमेश सैनी:- लेखक हड़बड़ी में नाम चाहता है और नाम चमकने के बाद लोग उसे नापसंद करते हैं या फिर आलोचना करते हैं उन्हें तो वह अलग नजर से देखा है और जो जी हजूरी करते हैं। उनकी वह खुशामद करता है। मेरा ऐसा मानना है कि जिसने आपकी आलोचना की है। वही आपका सच्चा मित्र है। आलोचना ही आदमी में सुधार का काम करती है। आलोचना ही लेखक की लेखनी को सुधारता है। आदमी आज के वक्त में आत्ममुग्ध हो चुका है। और इतना आत्ममुग्ध हो चुका है कि वह अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है। मैंने ही सब कुछ लिखा है। मैं ही सबसे बड़ा लेखक हूॅं । और आत्ममुग्ध होने की वजह से ही आलोचना करनी और होनी कम हो रही है । लेखक कहता है कि मेरी इतनी बढ़िया रचना है। इतनी अच्छी रचना है, तो कोई कमी ही नहीं हो सकती। जब कोई इस बारे में बात करता है, तो वह चीज उसे सहन नहीं होती,और इसी तरह आलोचना न सुनने की वजह से व्यंग्य किस तरह से कमजोर हुआ है। आज के वक्त में भी इतनी रचनाएं छपती है। हर रोज मैं खुद भी नई रचनाओं को पढ़ने की इच्छा रखता हूं और मैं यह कह सकता हूॅं। लोग वह कोई यह बात बुरी लग सकती है लेकिन वह समाज पर तो क्या उनकी रचना लेखक पर भी किसी तरह का प्रभाव नहीं डालती है। कहने का मतलब यही है कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे, पुरानी पुस्तक और पुराने लेख तो उस चीज से एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि एक अलग दृष्टि आपमें विकसित हो जाएगी और उसे दृष्टि विकसित होने के बाद में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी रचना की आलोचना करें या ना करें लेकिन आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि और वह दृष्टि आपको समझेगी कि आपकी रचना यहॉं कमजोर है। जब आपको पुरानी रचना पढ़ोगे और खुद की रचना पढ़ोगे तो आपको खुद को भी कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कि मेरी लिखने में कहॉं गलती आ रही है और आप खुद से ही उसमें परिवर्तन करेंगे। अध्ययन और इस तरीके से पढ़ना ही हमें आत्मआलोचना की तरफ ले जाता है। भले ही आप दूसरों से अपने आलोचना ना सुनी। लेकिन जब आप स्वयं की आलोचना करते हैं तो काफी कुछ परिवर्तित होता है। दूसरों की रचना तो छोड़िए हम तो खुद की रचना भी दुबारा नहीं पढ़ते। आप देखिए कि आप रचना लिखकर संपादक को भेज देते हैं। वह अपने हिसाब से कुछ काट छॉंट करके छाप देता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि उसने कहॉं परिवर्तन किया है और क्यों जरूरत पड़ गई। परिवर्तन करने की। आपके पास जैसे ही वह प्रति आई। आपने सोशल मीडिया पर लगा दी। अपने मित्रों को भेज दी। इन सब चीजों पर ध्यान देना और इन सब चीजों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है साहित्यकारों के लिए। मैं यही कहता हूं कि आप अपनी रचना को दोबारा पढ़िए। दूसरों की भी रचनाओं को अच्छे से पढ़ो और आलोचना तो पढ़नी ही चाहिए। फिर चाहे वह आपको खराब लगे या अच्छी लगे। पता है कि किसी मुद्दे पर या रचना पर कोई व्यक्ति आपकी बड़ी गंभीर और तीखी आलोचना करे तो बुरी लग सकती है लेकिन आप उसे वक्त अपने आप में शांत रहिए, चुप रहे और मंथन कीजिए उसका विश्लेषण कीजिए। क्या सही में यह सब है। जिस तरीके की आलोचना की गई। क्या जो वह व्यक्ति कह रहा है, वह सही है और नहीं तो कितना नहीं और अगर हॉं तो कितना हॉं। यह भी देखी कि कहीं वह बायस् होकर तो नहीं लिख रहा। तर्क कीजिए अपनी रचना के साथ उस आलोचना के साथ आपकी दृष्टि भी विकसित होगी।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने हेतु आपका बहुत आभार ।
रमेश सैनी - धन्यवाद
 Eric Chopra
Eric Chopra
एरिक चोपड़ा
संग्रहालयों और स्मारकों में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को डिज़ाइन और संचालित , विरासत संवर्धन से जुड़े प्रख्यात युवा लेखक और इतिहासकार एरिक चोपड़ा से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
आपको हमेशा पीछे देखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए- एरिक चोपड़ा
परिचय
एरिक चोपड़ा, भारतीय इतिहास और कला को समर्पित एक समावेशी मंच, "इतिहासोलॉजी" के संस्थापक हैं। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज, नई दिल्ली से इतिहास की पढ़ाई पूरी की है। लेखक और पॉडकास्टर हैं, जो कला, विरासत, भावनाओं, परलोक के इतिहास पर केंद्रित हैं। उनके काम का एक प्रमुख पहलू इतिहास को सार्वजनिक चर्चा के लिए सुलभ और आकर्षक बनाना है। संग्रहालयों और स्मारकों में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को डिज़ाइन और संचालित करते हैं और "फॉर ओल्ड टाइम्स सेक" पॉडकास्ट और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के "जयपुर बाइट्स" पॉडकास्ट के सह-होस्ट हैं। दिल्ली के स्मारकों और उनके "भूतिया" इतिहास पर उनकी पुस्तक "स्पीकिंग टाइगर" के साथ जल्द ही प्रकाशित होने वाली है।
अरमान: इतिहास पर किया गया आपका शोध वाकई आज प्रेरणा का स्रोत बना है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि इतिहास में आपका रुझान किस तरह से हुआ?
एरिक चोपड़ा: बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं साहित्य का विद्यार्थी बन सकता हूँ क्योंकि मुझे कहानियों का काफी शौक था, पढ़ाई में ज्यादा शौक नहीं था। यह कह सकता हूँ कि मेरी पूरी स्कूल लाइफ इन्हीं सब में रही, फिर चाहे वह पब्लिक इवेंट्स रहे हों, वाद-संवाद, इंग्लिश क्लासेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा, ड्रामा मुझे काफी अच्छे लगते थे—इन सब चीजों में मुझे काफी दिलचस्पी थी, जिन्हें स्कूल में को-करिकुलर और एक्स्ट्रा-करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता है। पढ़ाई में मुझे इतना खास इंटरेस्ट नहीं था।
अगर कभी मैं यह सोचूँ कि यह सब कुछ कैसे शुरू हुआ, एग्जैक्ट वह पॉइंट कौन सा था कि जब मुझे यह पता चला कि इतिहास मेरे लिए है, मैं कह सकता हूँ कि जब मैं 12वीं क्लास में था, सीबीएसई बोर्ड था। मेरे सिलेबस की हिस्ट्री की जो बुक्स थीं, हड़प्पा से लेकर स्वतंत्रता और संविधान तक थीं। ये तीन किताबें लगभग पूरे भारतीय इतिहास का सार था। और मुझे याद है कि जब मैं अपनी बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था, उस वक्त पढ़ते-पढ़ते जब मैं संविधान और भारतीय स्वतंत्रता के चैप्टर तक पहुँचा, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच थी जो उन्होंने कॉन्स्टीट्यूशनल असेंबली में दी थी। उन्होंने अपना एक विज़न दिया था, उन्होंने कहा था कि जब हम अपना संविधान बना रहे हैं, स्वतंत्र भारत का, तो हम अपने इतिहास को भूल नहीं सकते और आप दूसरी जगह के इतिहास को भी नहीं भूल सकते। और इन सब चीजों को देखने-पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि आपको हमेशा पीछे देखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए।
अरमान: आपने अपनी बात में पूर्व प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इतिहास को भूल नहीं सकते। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मौजूदा वक्त में जो असल इतिहास है उसे पढ़ना और ढूंढना कितना मुश्किल हो चुका है और अगर हम सिनेमा की भी बात करते हैं तो उसमें भी इस चीज का कुछ खास ख्याल नहीं रखा जाता, मुझे ऐसा लगता है कि जो फैक्ट्स हैं उन्हें फिक्शन की तरफ धकेला जा रहा है। इसका जो नुकसान है इसे आप कैसे देखते हैं?
एरिक चोपड़ा: एक बात है जो बहुत से इतिहासकारों ने पहले भी कही है और हो सकता है मैं उसे रिपीट ही कर रहा हूँ कि आपका जो इतिहास है, उसे बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारी पावर्स अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगी। फिक्शन और फैक्ट्स से ज्यादा बड़ी बात यह हो जाती है कि आप इतिहास से चाहते क्या हो। और अगर इतिहास ही आपकी जड़ है और जब आप उस जड़ तक जाओगे और अपने हिसाब से उसे जड़ से निकालोगे कहानी, तो आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी। तो यह चीज हमने हर बार, हर टाइम पीरियड पर, ऐसी चीज कि आपको हमेशा पीछे देखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिएथा और वह सब लेकर आप आज एक-दूसरे से लड़ो। और इतिहासकार भी एक-दूसरे से आर्ग्यू करते हैं। क्योंकि इतिहास में सिर्फ तथ्य नहीं होते, इसमें यह होता है कि आप उन तथ्यों की किस तरीके से व्याख्या करते हो। मेरे पास कुछ तथ्य होंगे, आपके पास कुछ तथ्य होंगे, लेकिन मैं जिस तरीके से उसकी व्याख्या करूँगा, जरूरी नहीं है कि सब उस तरीके से ही उस तथ्य की व्याख्या करें।जिसमें मैं एक अपना उदाहरण नहीं देता हूँ कि हमारी दिल्ली के अंदर बहुत से मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ओरल हिस्ट्री चलती है, जिनके अंदर लोगों को लगता है कि वहां भूत और जिन्न हैं, फिरोजशाह कोटला हो, खूनी दरवाजा हो। क्योंकि मेरा काम पब्लिक हिस्ट्री में भी है, हेरिटेज वॉक पर जाता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बताते हैं कि यहां भूत है, यहां जिन्न है। अब मैं उस भूत में मानूँ या न मानूँ, लेकिन वह कहानी है। और अगर वह कहानी एक्ज़िस्ट करती है उनके लिए, तो हम यह जान सकते हैं कि क्या रिलेशन है उनका हिस्ट्री के साथ। यहां फैक्ट यह है कि वह कहानी अस्तित्व में है। वहां तथ्य यह नहीं हो जाता कि भूत है या नहीं। अगर मैं किसी और इतिहासकार से बात करूँ तो हमारा इस मुद्दे पर डिबेट हो सकता है, हमारे विचारों में फर्क हो सकता है। वह कह सकते हैं कि ओरल हिस्ट्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि नहीं, ओरल हिस्ट्री भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इसे एक हेल्दी डिस्कशन कह सकते हैं। मगर आज जो डिस्कशन होते हैं, वह इस तरीके से नहीं होते, उन डिस्कशन का एक अलग मोटिव है।और मैं कहना चाहूँगा सिर्फ इतिहास ही नहीं, हमारे पास में आज के बड़े-बड़े सवाल खड़े हुए हैं। अगर हम अपने म्यूजियम की बात करें, हमारी कलेक्शन्स हैं, इंडिपेंडेंस के बाद कॉलोनियलिज्म के दौरान पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गईं। लेकिन जो मौजूदा वक्त में हमारे पास कलेक्शन्स हैं, आप उनकी म्यूज़िमाइजेशन देखिए, वह हमारी प्रायोरिटी है। आप देखिए हमारे मॉन्यूमेंट्स का हाल। कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो ASI से प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आप यह देखिए कि उनसे किस तरह की मीनिंग जुड़ी हुई है जहाँ जाकर लोग वहां पिलर्स को भी गिरा सकते हैं, उन्हें ध्वस्त भी किया जा सकता है। और जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि तुम क्या पढ़ सकते हो और क्या नहीं पढ़ सकते हो, तो मुझे तो लगता है कि आपको बताना चाहिए कि आप इससे क्या सीख सकते हो और किस तरीके से आपकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकती है। इस तरह की चीजें होनी चाहिए लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मौजूदा वक्त में काफी कुछ चीजें बदली हैं और काफी अनहेल्दी डिस्कशन की तरफ हम इतिहास को ले जा रहे हैं।
अरमान: बिल्कुल आपने सही कहा कि आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए लेकिन सवाल मेरा यह रहेगा कि इतिहासकार किसी ऐतिहासिक घटना पर अपने विचार रखता है तो क्या उसके व्यक्तिगत स्वार्थ भी वहां प्रभावित करते हैं? कि वह खुद उस स्थिति को कैसे देखा है और अगर ऐसा है तो हम इसे किस तरीके से बच सकते हैं।
एरिक चोपड़ा: जब आप किसी भी चीज के बारे में लिखते हो, फिर चाहे वह फिक्शन हो या नॉन-फिक्शन हो, आप अपनी परिस्थितियों से अपने आप को दूर नहीं रख पाते। मान के चलिए आप अगर फिक्शन नॉवेल भी लिख रहे हैं। बानू मुश्ताक जी ने जो किताब लिखी है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उनकी और उन्हें बुकर प्राइज भी मिला है। जब आप उनके जितने भी इंटरव्यूज देखेंगे तो वह अपने इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि मैंने जो भी कहानी लिखी है वह मेरे काफी करीब है, काफी नजदीक है। और इसी तरीके से अगर आप इतिहास में देखते हैं और आपको यह सोचते हैं कि इतिहासकार अपनी परिस्थितियों से दूर जा सकता है, मुझे लगता है वह नामुमकिन है। वह अपने अंदर ही डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते। यह आसान हो जाता है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी की बात करना लेकिन अंत में हम सब इंसान हैं, हमारे अपने बहुत सारे ख्याल हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी जिम्मेदारियां हैं कि आप अपना इरादा देखिए, आपका उद्देश्य क्या है कि आप अपनी परिस्थितियों से हटकर इतिहास में आपको उनकी स्थिति को देखना है। अगर आप उनकी स्थिति को नहीं समझ पाए तो आपका जिसमें आप अपनी कहानी बता रहे हैं मुझे लगता है वह अधूरा रहेगा।
मैं तो हमेशा यही कहता हूँ जब मैं लोगों के साथ में म्यूजियम जाता हूँ कि आप एक चीज पर रुकिए मत, आप सवाल पूछते रहिए। क्योंकि जब आप सवाल पूछते रहेंगे तो आप एक व्यापक समझ की तरफ आगे बढ़ेंगे, पूरी तरीके से उन्हें समझ पाएंगे। मान के चलिए आप किसी चित्र को देख रहे हैं तो आप यह मत सोचिए कि वह कहां से आया, आपको लगातार यह पूछना भी चाहिए कि यह किसने बनाया। अगर यह किसी ने बनाया होगा तो इसके लिए पैसे किसने दिए होंगे। अगर किसी ने पैसे दिए होंगे तो इसके पीछे भी किसी की इच्छा होगी, वह इच्छा किसकी थी। और अगर यह किसी ने बनाए हैं और उस वक्त बहुत बड़े नंबर में बनी होगी तो उस वक्त भी इसकी एक इकोनॉमी रही है, एक बड़ा मार्केट होगा। अब सवाल यह भी होते हैं कि उस मार्केट में कौन एम्प्लॉई थे, इसके खरीदार कौन थे, फिर सवाल आता है कि ये लोग रहते कहां थे। आप एक सवाल से इतनी सवालों तक पहुँच सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको अपनी परिस्थिति और जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं उनकी परिस्थिति दोनों को साथ में रखना ही पड़ेगा।
अरमान: अपनी बात में कहा कि हमें लगातार सवाल करने चाहिए और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, कोई 100-200 साल पहले तक हम सीमित नहीं रहे। जब हम उसका अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हम चुनाव करते हैं कि यह जो कालखंड है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उसमें भी हम कई बार पार्टिकुलर पर्सनैलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि यह हमारे को पढ़ना और उनके बारे में जानना काफी जरूरी है। मेरा सवाल यह है कि हम उन्हें महत्वपूर्ण किस आधार पर बनाते हैं? क्या वक्त के अनुसार वह कालखंड और वह पर्सनैलिटीज बदलेंगी? हमारी नजर में जो ऐतिहासिक तथ्य महत्वपूर्ण हैं, क्या 50 साल बाद, 100 साल बाद भी वह उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे या उसमें परिवर्तन आएगा?
एरिक चोपड़ा: एक आपने बहुत ही सही बात कही कि हर टाइम के हिसाब से आपका इतिहास पर आपका ओपिनियन है, जो इंपॉर्टेंट फिगर पॉप आउट कर रहे हैं बाहर निकल रहे हैं उनका कितना ज्यादा प्रभाव था। आर्ट हिस्टोरियन हैं ई.एच. गोंब्रिच जो कि इतिहास के बारे में लिखा करते थे और जो इतिहास में आर्ट हुआ उसके बारे में लिखा करते थे। उन्होंने एक बेहद ही लोकप्रिय किताब लिखी थी जिसका नाम है "स्टोरी ऑफ आर्ट"। और इस किताब में आपको यह देखने को मिलेगा जितने भी आर्टिस्ट हैं वह सभी पुरुष हैं। तो फिर क्या इतिहास में महिलाएं नहीं थीं, फीमेल आर्टिस्ट नहीं थीं? और अब जाकर कुछ साल पहले एक हिस्टोरियन हैं केटी हेसल, उन्होंने अब एक बुक लिखी है "स्टोरी ऑफ आर्ट विदाउट मैन"। और इस किताब में वही पीरियड, वही आइडिया, वही सब कुछ इस टाइम के हिसाब से लेकिन उन्होंने इस किताब में रखा है सिर्फ महिलाओं के बारे में, वुमेन आर्टिस्ट जो हुईं उस टाइम ऑफ पीरियड में।बात यही है कि आपका जो इतिहास है उसमें सब कुछ है लेकिन आप वहीं पर यह फैसला करते हैं, चुनाव करते हैं कि आपको कौन सी कहानी आगे लानी है। और यहां हमें फैसला करना होगा इन सब चीजों को एक साथ लाने का और यह मेरी भी इच्छा थी कि जब मैं इतिहास पढ़ना शुरू किया था और काम करना शुरू किया था तो मैं यह देखा था कि ऐसी कौन सी कहानी है जो हम आगे नहीं ला पा रहे हैं? ऐसे कौन से किस्से हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज हम नहीं सुन रहे हैं? अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं और कहते हैं कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था तो हम यह क्यों नहीं पूछते कि वहां पर वह ड्रेनेज स्कीम किसने की? सारी बातें करते हैं और यही सवाल फिर से उठकर आते हैं और जब हम हड़प्पा को गहराई से पढ़ते हैं तो ऊपरी तौर पर भी हम कहते हैं कि काफी अच्छे घर थे, टू फ्लोर्स हाउस अरेंजमेंट थी, बाथरूम थे, बहुत ही वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। लेकिन यह सब बना कौन रहा था? यह सवाल क्यों नहीं होता है? इन सब की देखभाल कौन करता था? यह भी तो हमारे सवाल आने चाहिए।
हिस्टोरियोग्राफी जो है वह आपका एक प्रक्रिया है जिसकी मदद से आप इतिहास लिखते हो और वह हिस्ट्री से अलग है क्योंकि जो इतिहास में हुआ है वह हिस्टोरियोग्राफी चूज करती है अपने हिसाब से। और मैं यह कह सकता हूँ कि बहुत वक्त तक हिस्टोरियोग्राफी एक लेंस के द्वारा ऑपरेट की गई, ज्यादातर कहानियां सिर्फ उन लोगों की थीं जो कि जहां इतिहासकारों को लगा कि वह महत्वपूर्ण हैं यानी कि जो अपर सेक्शन के थे। और निःसंदेह वह काफी महत्वपूर्ण थे क्योंकि एक लंबे वक्त तक उन्होंने हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल शुरुआत से लेकर सब कुछ संभाला। मुझे कोई एक जगह नहीं हुई, आप इजिप्ट देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, जहां कहीं भी हम देखते हैं वहां हमें यह देखने को मिलता है। वह जो किंगशिप थी वह महत्वपूर्ण है लेकिन हम यह भूल गए कि उनकी वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़े थे। और वह सवाल अब हम कर रहे हैं, अब हमें और महिलाओं की आवाज सुनाई है, हमें LGBTQ कम्युनिटी की आवाज सुनी है, जो कि सब इतिहास में दर्ज हैं।
अरमान: हम इतिहास पढ़ते हैं और अगर मैं कहूँ एक-एक लाइन में हमें एक क्वेश्चन मार्क मिलता है, जैसा आपने कहा भी कि सवाल करते रहना चाहिए। और मैं कहूँगा कि एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज इतिहास में यह होती है कि "अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर क्या होता या फिर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता?" मेरा सवाल यह बनता है कि इस इमेजिनेशन की तरफ व्यक्ति को जाना चाहिए या फिर जो फैक्ट्स हैं उन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए?
एरिक चोपड़ा: अरमान, आप यह जो बात कह रहे हैं इस चीज को कहते हैं काउंटरफैक्चुअल हिस्ट्री। बेसिकली यह एक मेथड है जिसमें आप एक क्वेश्चन पूछते हो, जैसा कि आपने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता? देखिए, जिज्ञासा जो है वह बेहद ही महत्वपूर्ण तत्व है हम सब में और जिज्ञासा का होना वाकई में बहुत जरूरी है। और यहां भी वही बात फिर से आ जाती है कि उद्देश्य क्या है? इस तरह के सवाल पूछने में कुछ गलत नहीं है। यह एक बहुत ही रोचक तरीका हो सकता है कि आप इतिहास के बारे में किस तरीके से बात करते हो, आपकी चर्चा किस मुद्दे पर आधारित हो सकती है। आप एक वाइड डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हम किन परिस्थिति में होते।परेशानी यहां तब आती है जब लोग एक चीज को भूल जाते हैं, जैसे कि एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है जिसमें एक तितली अपने पंखों को किसी दूसरे समय पर फड़फड़ाए और उस वक्त न करे जिस वक्त उसे वाकई में करना था। बाद में हम इसे एक डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। यह एक समझने का तरीका है जिसमें आप कह सकते हो कि बहुत छोटी सी चीज भी एक बहुत बड़े इंसिडेंट को शुरू कर सकती है। हम यह भूल जाते हैं कि काउंटरफैक्चुअल हिस्ट्री यह नहीं होता कि ये राजा बन गया और वह वह बनता तो हमारा राज्य कितना परिवर्तित होता। और मान के चलिए अगर ऐसा हो भी जाता, आपका जो मनपसंद ऐतिहासिक शख्सियत उस पद पर पहुँच जाती जो बने थे वह नहीं बनते और जो आपकी इमेजिनेशन में बन रहा है, उनकी परिस्थितियाँ भी तो उन्हें इनफ्लुएंस करेंगी। मान लिया वह बहुत ही डाइवर्स थे, सब कुछ चीज थी तो क्या आपको उसमें डिप्लोमेसी नहीं चाहिए? बहुत सी चीजों पर खुद को ध्यान रखना होता है, ज्ञान चाहिए होता है, आपकी जो सेना है उसकी आपको ताकतवर तरीके से देखभाल करनी होती है। और इस तरीके से आप लगातार सवाल वहां भी करते जाएंगे, आपको यह पता चलेगा कि एक चीज दूसरी चीज को ऐसे प्रभावित करती है कि आप इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि आज उनका इनफ्लुएंस क्या होता। डोमिनो इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, एक डोमिनो गिरने पर आगे के सारे डोमिनो गिरते हैं। अगर इतिहास में कुछ भी परिवर्तन हुआ होता तो आज बहुत चीजों पर उसका प्रभाव होता। मतलब की बहुत छोटी सी चीज बहुत बड़ी और व्यापक घटनाओं का कारण बन सकती है।काउंटरफैक्चुअल हिस्ट्री में एक मेथड है और जिस तरीके से यहां लोग सवाल पूछते हैं वह उससे काफी अलग है। वह सवाल करते हुए परिस्थितियों को भुला देते हैं और वहां सिर्फ वह यही सवाल करते हैं कि अगर यह न हुआ होता तो यह क्या होता और जिसका सवाल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। यहां पर अच्छे और बुरे की बात है ही नहीं। अगर आप लोगों को उनकी परिस्थितियों से हटा दोगे तो आप जवाब दे ही नहीं।
अरमान :- जब हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं और मुगल पोट्रेट्स को हम देखते हैं उन सभी ने अपने आप को जनता के सामने भगवान के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाने की कोशिश की और यहां हम सिर्फ भारतीय समाज की बात नहीं कर सकते हमने जहां पर भी देखा कि किंगशिप मौजूद थी उन सभी ने इस तरह की चीज को अपनाया सवाल यह है क्या यह सिर्फ जनता से जुड़ाव का एक तरीका था या इसके और भी राजनीतिक पहलू हो सकते हैं?
एरिक :- आपने जो बात कही और डिवाइन किंशिप की है जब हम बात करते हैं तो यह बहुत ही पुराना कांसेप्ट है और अपने खुद ने भी कहा कि हम इसे विश्व स्तर पर देखते हैं अगर हम बात करते हैं प्राचीन इजिप्ट की वहां पर भी एक डिवाइन कैरेक्टर था हमेशा से। जब हम मुगल पेंटिंग्स की बात करते हैं तो जो डिवाइन लाइट उनमें नजर आती है तो हम कह सकते हैं कि जो डिवाइन किंगशिप का कॉन्सेप्ट बाद ही जटिल है जैसा कि आपने कहा कि जनता से जुड़ने की बात यह बिल्कुल सच है कि ऐसा होता था एक यह भी इसका कारण है और एक मिथ मेकिंग भी होती है यह चीज हमें उसे वक्त हर कलर में देखने को मिली और यह जितनी भी फ्रेंडशिप की हम बात करें जिनमें डिवाइन किंशिप हमें देखने को मिलती है राजा रानियां खुद को भगवान से जुड़ पाए थे वह एक खुद की वैलिडेशन बनाए रखने के लिए भी होता था। और जब हम प्रशस्तियों को देखते हैं यानी कि वह पत्र या कविताएं जिम राजा रानियां की प्रशंसा की जा रही हो और जिसमे भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत बार उन्हें एक रिलिजियस पावर से कंपेयर किया जाता है। अगर हम मुगल की बात करें अबुल फजल ने जब लिखा फिर चाहे उन्होंने जो लिखा अकबरनामा उन सभी में आपको एक दिव्य संबंध देखने को मिलेगा एक एक डिवाइन रिलेशन आपको उसमें महसूस होगा तुम मिथ मेकिंग के अंदर वह भी इंवॉल्वड थे। और यह चीज इतनी ऐतिहासिक घटनाओं में शामिल थी कि उसे वक्त जितनी भी पावर्स हुई उन सभी ने इसका इस्तेमाल किया उसे हम सिर्फ जनता से जुड़ाव का ही नहीं हम कह सकते हैं कि वह एक हिस्टोरिकल फेनोमेना था। और वह चीज चलती रही क्योंकि आपको अपनी दगी को वह ताकत देनी थी और वह यह दर्शाता था कि आपके पास में ऐसी ताकत है कि जो सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि दूसरी दुनिया तक में भी महसूस की जा सकती है वह हर दुनिया में। और जिन पर आपका अधिकार है वह भी यह चीज महसूस करते हैं कि यहां तो सिर्फ उनकी बॉडी है लेकिन जो इनकी पवित्र आत्मा है वह पूरे विश्व में राज कर रही है।
अरमान - कॉलम शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने हेतु आपका बहुत आभार ।
एरिक - आपका भी बहुत आभार
 Anirudh Kanisetti
Anirudh Kanisetti
अनिरुद्ध कनीसेट्टी
साहित्य अकादेमी के युवा पुरस्कार से समादृत युवा इतिहासकार, कथाकार अनिरुद्ध कनीसेट्टी से कॉलम शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
हमें इतिहास की अधिक व्यापक और मानवीय समझ रखने की आवश्यकता है। ताकि हम अपने लिए यह आकलन कर सकें कि ऐतिहासिक कहानियों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कैसे तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। - अनिरुद्ध कनीसेट्टी
परिचय - अनिरुद्ध कनीसेट्टी
अनिरुद्ध कनीसेट्टी एक पुरस्कार विजेता लेखक, इतिहासकार और कहानीकार हैं जिन्हें भूले-बिसरे इतिहास को उजागर करने का जुनून है। 29 अक्टूबर 1994 को विशाखापत्तनम में जन्मे, उन्होंने बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका असली जुनून उन्हें इतिहास की ओर ले गया। मुख्य रूप से अंग्रेजी में लिखते हुए, अनिरुद्ध का काम कथा और गैर-कथा दोनों क्षेत्रों में फैला है, जो विद्वानों के शोध को आकर्षक कथाओं के साथ जोड़ता है। उनकी पहली पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन: सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्य टू द चोलस 500 साल के मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास की पड़ताल करती है, जिसमें क्षेत्र के खोए हुए राजवंशों की कहानियों को उजागर करने के लिए कला, वास्तुकला, साहित्य और पुरालेख का उपयोग किया गया है। इस पुस्तक को व्यापक प्रशंसा मिली है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार (2023) और टाटा लिटरेचर बेस्ट नॉनफिक्शन बुक ऑफ द ईयर अवार्ड (2022) अपनी किताब के अलावा, अनिरुद्ध का काम डिजिटल दुनिया में भी फैला हुआ है। वह द प्रिंट के लिए साप्ताहिक "थिंकिंग मेडिवल" कॉलम लिखते हैं और लोकप्रिय पॉडकास्ट - "इकोज़ ऑफ़ इंडिया", "युद्ध" और "द अल्टर ऑफ़ टाइम" होस्ट करते हैं, जो सभी अपनी समृद्ध और मनमोहक कहानियों से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। उनका काम द हिंदू, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और लाइवमिंट जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हो चुका है, और उन्हें द वीक के 40 अंडर 40 सबसे होनहार रचनाकारों में से एक माना गया है। अपने लेखन और शोध के माध्यम से, अनिरुद्ध ऐतिहासिक गैर-काल्पनिक साहित्य में एक जाना-माना नाम बन गए हैं और भारत के मध्यकालीन इतिहास को समझने के तरीके को नया रूप दे रहे हैं।
अरमान:- दक्षिण भारत के इतिहास पर आपने बड़ी गहराई से काम किया है और आपकी कहीं किताबें भी दक्षिण भारत इतिहास l प्रकाशित हुई मैं यही जानना चाहूंगा इतिहास में आपकी रूचि किस तरह हुई? और आप अपने सफर को शुरु से लेकर अब तक किस तरह दिखते।
अनिरुद्ध: - अगर मैं बात करूं किस तरीके से इतिहास में मेरी रुचि हुई ,मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था । मेरे पास काफी वक्त था और मैं हिस्टोरिकल वीडियो गेम्स खेलना पसंद करता था और इस वक्त से मेरे अंदर एक बड़ी दिलचस्पी इतिहास को लेकर हुई। और हम देख सकते हैं कि ज्यादातर हिस्टोरिकल वीडियो गेम्स यूरोपियन द्वारा में बनाए जाते हैं। और जब आप इन गेम्स को खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में यूरोप की हिस्ट्री पढ़ने की भी इच्छा जागरुक होती है। और आपको बड़ी ही आसानी से विद्वानों द्वारा लिखी यूरोपियन हिस्ट्री पर किताबें मिल जाएगी जिसे आप पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन जब हम भारतीय इतिहास पर बात करते हैं तो वह इतना आसान नहीं होता। यह उतना तकनीकी नहीं होता है। हालांकि, भारत में निश्चित रूप से महान शिक्षाविद हैं, लेकिन वे अक्सर आम पाठकों के बजाय वह अन्य शिक्षाविदों के लिए लिखते हैं। । तो मुझे लगा कि इन विद्वानों के काम को पढ़ने और उनका विश्लेषण करने, उनके बारे में इस तरह से बात करने का जुनून है और फिर ऐसा काम किया जाये जो आम आदमी के लिए सुलभ हो।
अरमान:- चोल साम्राज्य पर क्योंकि आपका काफ़ी काम भी देखने को मिलता है आपके विचार में, चोल साम्राज्य के वक्त कला, संस्कृति, साहित्य में किस तरह का विकास हुआ?
अनिरुद्ध: - मेरे विचार से चोल साम्राज्य भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य के समग्र विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा उदाहरण निश्चित रूप से नटराज है। वह आज हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक हैं, जब जी-20 सम्मेलन हुआ था भारत मंडपम में नटराज की एक विशाल प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। लेकिन वास्तव में वो एक चोल रानी ही थीं जिन्होंने सबसे पहले शिव के इस विशेष रूप में नृत्य को संरक्षण दिया और लोकप्रिय बनाया। चोलों ने दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला को भी बदल दिया। तो अगर आप दक्षिण भारत जाते हैं, तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में हमेशा कई प्रवेश द्वार होते हैं। उनमें कई आंगन होते हैं। ये सभी चोल काल के विकास के परिणाम हैं। और साहित्य के संदर्भ में भी, विशेष रूप से तमिल साहित्य के संदर्भ में, आज भी कई तमिल मंदिरों में लोग अभी भी गीत गाते हैं। वे अभी भी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो चोल काल के दौरान लोकप्रिय हुई थीं। लेकिन यह सिर्फ राजवंश की कहानी नहीं है। हम अक्सर केवल राजाओं के बारे में सोचते हैं। हमारे मन में राजाओं के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत सम्मान है। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि हम बड़े पैमाने पर बाकी समाज को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। और चोल काल की अद्भुत बात यह है कि बहुत से लोगों ने मंदिरों को दान दिया था जो मंदिर की दीवारों पर शिलालेखों में संरक्षित हैं। तो हमारे पास तमिल समाज के एक व्यापक दायरे की समझ है। हम कुछ हद तक आम आदमी के दृष्टिकोण को भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सदियों से आम आदमी कैसे बदलता है। तो अपनी किताब में, मैं वास्तव में इस बात पर जोर देता हूँ कि इतिहास केवल राजाओं और रानियों की कहानी नहीं है, बल्कि वास्तव में उस समय के सभी लोगों की कहानी है।
अरमान :- अपने को बहुत सही बात कही कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है और खासकर की आज के वक्त में ऐसा लगता है कि जो फैक्ट्स हैं उन्हें फिक्शन की तरफ धकेला जा रहा है इस का आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे?
अनिरुद्ध: - मुझे लगता है कि इतिहास के बारे में बहुत जिज्ञासा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन, दुर्भाग्य से, इस जिज्ञासा के कारण, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, खासकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग। जो जानते हैं कि तथ्यों पर आधारित न होकर भावनाओं पर आधारित एक कहानी को कैसे गढ़ा जाए। वे जानते हैं कि लोगों की भावनाओं को कैसे अपील करें ताकि उन्हें एक विशेष तरीके से महसूस कराया जा सके और खासकर पिछले एक दशक में यह राजनीतिक रूप से बहुत लाभदायक हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका समाधान शैक्षणिक कार्य को तथ्यों को, सबूतों को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है, बल्कि लोगों को यह सीखने में भी मदद करना है कि इतिहास के बारे में कैसे सोचें। जैसे, आप आलोचनात्मक रूप से कैसे सोचते हैं? ऐतिहासिक कहानियों का निर्माण कैसे होता है? आप अपने स्वयं के निष्कर्षों पर कैसे पहुँच सकते हैं, अपना स्वयं का शोध कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि यह भारतीय नागरिकों के हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है, संविधान में यह है कि हमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें ऐतिहासिक स्वभाव विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। हमें इतिहास की एक अधिक व्यापक और मानवीय समझ रखने की आवश्यकता है। ताकि हम अपने लिए यह आकलन कर सकें कि ऐतिहासिक कहानियों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कैसे तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है।
अरमान :- वर्तमान समय में इतिहास के अध्ययन और शिक्षण में आपको क्या प्रमुख चुनौतियाँ दिखती हैं?
अनिरुद्ध:- अरमान, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों के लिए गलत ऐतिहासिक जानकारी तक पहुँचना बहुत आसान चुका है । गलत सूचना फैलाने में सेकंड लगते हैं, लेकिन उस सूचना का खंडन करने और सच्चाई को सामने लाने में दिन, हफ्ते, महीने लगते हैं। और तब भी, यह हमेशा उन सभी तक नहीं पहुँच पाती जहाँ इसे पहुँचना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने निश्चित रूप से पूछा है कि भारतीय इतिहास के सिलेबस को बदला जाना चाहिए, कुछ साम्राज्य को हटा दिया जाना चाहिए, कुछ साम्राज्य को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे छात्रों को कई चीजें सीखनी होती हैं। हम उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे अपना पूरा स्कूल जीवन केवल पूरे देश के व्यापक इतिहास का अध्ययन करने में बिता दें। सबसे व्यावहारिक समाधान यह है कि पाठ्य पुस्तकों में सब कुछ भरने की कोशिश करने के बजाय, हमें यह समझना होगा कि शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है। यह स्कूल से शुरू नहीं होती, स्कूल से खत्म नहीं होती। हमें छात्रों को आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। हमें उन्हें सिखाना होगा कि इतिहास कैसे लिखा जाते हैं, और हमें उन्हें वे कौशल प्रदान करने होंगे कि यदि उनमें जिज्ञासा है, तो वे भारत के किसी भी हिस्से के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और मुझे लगता है कि वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों की धार्मिक राजनीति में उलझने के बजाय जो अब बहुत पहले चले गए हैं, हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत में हर समुदाय, हर क्षेत्र, हर भाषा ने हमारे देश के आज के रूप में एक विशेष योगदान दिया है। तो भारतीयों के रूप में इन सब से अवगत होना हमारा मौलिक कर्तव्य है।
अरमान :- जब हम इतिहास पर बात करते हैं तो सबके अपनी-अपनी सोच हो सकती है राजनीतिक और कुछ धर्म के हिसाब से भी सोचते हैं आपके लिए इतिहास का क्या मतलब है और आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं?
अनिरुद्ध:- इतिहास इस बात की कहानी है कि हमारी दुनिया आज जैसी है क्यों है। यह आप और मेरे जैसे लोगों की कहानी है, ऐसे लोग जिनमें प्रतिभा और रचनात्मकता की वही क्षमता है, लेकिन घृणा और लालच और हमारी प्रकृति के सभी नकारात्मक और सकारात्मक चरम सीमाओं की वही संभावनाएं भी हैं, जितने सक्षम हम हैं अतीत के लोग भी सक्षम थे। मेरे लिए इतिहास की अद्भुत बात यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अक्सर ऐसा लगता है कि एक ही कहानी अलग-अलग संस्कृतियों और अलग-अलग भाषाओं में सुनाई जा रही है। यह ताक़त की कहानी है। यह वास्तव में मानवता की कहानी है। अगर हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो न्यायपूर्ण हो, जो एक समान समाज हो, जो हमारे सभी नागरिकों के लिए एक मानवीय समाज हो, तो यह इतिहास को चुनिंदा रूप से देखकर, कुछ समुदायों को मार कर नहीं होगा। यह एक व्यापक मूल्यांकन से आएगा। यह हमारे पूर्वजों की खामियों को समझने से आएगा, उनकी प्रतिभाओं के साथ-साथ उनकी खामियों को समझने से आएगा, और फिर एक समाज के रूप में मिलकर उन असमानताओं, उन अन्यायों को ठीक करने के लिए काम करना होगा जो कई शताब्दियों तक हुए। जब तक हम एक-दूसरे को दोष देने के इस तरीके में फंसे रहेंगे, सोशल मीडिया पर धकेले जा रहे किसी भी राजनीतिक कथानक में उलझे रहेंगे, तब तक हम उन्हीं चक्रों में फंसे रहेंगे, और हमारे लिए वास्तव में एक ऐसा भारत बनाना मुश्किल होगा जो सभी भारतीयों के लिए सबसे अच्छा करे।
अरमान:- एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा जिसे हम ऐतिहासिक रूप से भी लगातार देखते हो आ रहे हैं जिसमें हम न सिर्फ दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि विश्व स्तर पर देखा गया है राजाओं ने शासको ने अपने आप को भगवान के अवतार के रूप में जनता के सामने खुद को प्रस्तुत किया क्या वह सिर्फ जनता से जुड़ाव की वजह से था या इसके और भी राजनीतिक कारण थे?
अनिरुद्ध:- सभ्यता की शुरुआत से ही, यहां तक कि अगर आप मिस्र को देखें, अगर आप मेसोपोटामिया को देखें। वहां भी, चीजें वैसी ही देखने को मिलती है । वे खुद को देवता होने का दावा कर रहे थे। वे देवताओं के करीब होने का दावा कर रहे थे। और यह वर्तमान तक जारी है जहां दुनिया भर में बहुत कम अपवादों के साथ। ज्यादातर देशों में, राजनेताओं को यह दिखाना बहुत, बहुत लाभदायक लगता है कि वे धर्मात्मा हैं, यह दिखाना कि वे किसी न किसी तरह से दिव्य रूप से पसंदीदा हैं। भारत इससे कोई अपवाद नहीं है, चाहे वह अतीत में हो या वर्तमान में। बहुत अच्छा। शक्ति की प्रकृति यह है कि धार्मिक और राजनीतिक शक्ति बहुत आसानी से आपस में जुड़ सकती है। लेकिन और एक बार जब वे आपस में जुड़ जाते हैं, तो यह कुछ, खासकर गलत व्यक्तियों के हाथों में, बहुत बार दुरुपयोग हो सकता है। तो समाधान मेरा मतलब है कम से कम मेरे विचार में मुझे लगता है कि, इसका समाधान वही है जो मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से कह रहा हूं कि हमें इतिहास को समझने की आवश्यकता है यह हमें शक्ति की प्रकृति को समझने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हालांकि वेशभूषा बदल सकती है, अभिनेता बदल सकते हैं, नाटक, शक्ति का नाटक हमेशा वही रहता है चाहे वह कोई भी पीढ़ी हो। और एक लोकतंत्र के नागरिकों के रूप में शक्ति की आलोचना करना हमारा कर्तव्य है।
अरमान:- क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास पर बड़ी गहराई से आपका काम है रीजनल हिस्ट्री पर जब काम करते हैं तो उस वक्त आपको किस तरह की अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
अनिरुद्ध:- जब चोल साम्राज्य की बात आती है, तो यह एक इतिहासकार के रूप में एक बहुत ही दिलचस्प और संतोषजनक कार्य है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था तमिल मंदिरों में समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा बड़ी संख्या में शिलालेख बनाए गए थे, जो हमें सदियों से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुए, इसका एक बहुत विस्तृत चित्र प्रदान करता है। यह भारत के सभी हिस्सों के लिए ऐसा नहीं है, दुर्भाग्य से. हमारे पास उतने प्राथमिक स्रोत नहीं हैं, यानी उन समय के लोगों द्वारा बनाए गए साहित्य या शिलालेख। वे या तो गायब हो गए हैं या वे नष्ट हो गए हैं या वे विभिन्न संघर्षों में नष्ट हो गए थे। तो मेरे विचार में, मुझे लगता है कि भारत के लिए बड़े पैमाने पर पुरातात्विक उत्खनन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज पुरातात्विक उत्खनन राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थानों पर बहुत केंद्रित होते हैं। लेकिन अगर आप बाकी दुनिया को देखें तो बहुत बार पुरातत्व ने उन कहानियों को सही करने में मदद की है जो प्राथमिक स्रोतों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। इसने इसे जटिल बनाने में मदद की है। इसने अनमोल कलाकृतियाँ पाई हैं जिन्हें संग्रहालयों में रखा जा सकता है और लोगों में गर्व की भावना पैदा करने में मदद मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि भारत को वास्तव में यही चाहिए। हमें उद्देश्यपूर्ण और आलोचनात्मक पुरातत्व की आवश्यकता है। हमें उन महान खोए हुए शहरों को खोजना होगा जिनके बारे में साहित्य में बात की गई है। हमें अपने पास मौजूद स्मारकों को बेहतर ढंग से संरक्षित करना होगा। क्योंकि हम इसे कैसे कहें? अभी भारत में, हमें नहीं पता कि हम कितना नहीं जानते। इतिहास का एक विशाल हिस्सा है जिसे खोजा जाना बाकी है, जिसके बारे में बात की जानी बाकी है, जिसे हमारी बातचीत में प्रवेश करना बाकी है। और जब हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर व्यस्त हैं और एक-दूसरे के साथ ये अनावश्यक झगड़े कर रहे हैं। यह वास्तविक इतिहास, जो स्मारक बचे हुए हैं, बस उपेक्षित हो रहे हैं और टूट रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक ऐसे देश के लिए जो अपने अतीत का सम्मान करता है और जिसका इतना समृद्ध और विविध अतीत है, मुझे लगता है कि यह एक वास्तविक त्रासदी है।
अरमान:- आपने बड़ी गंभीर और जरूरी बात कही बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी चर्चाओं में आना अभी बाकी है लेकिन जो हमारे समक्ष हैं हम यह भी देखते हैं कि उन्हें किस तरीके से बदला जाता है जब हम ताजमहल की चर्चाओं में देखते हैं उसे तेजो महालय कह दिया जाता है। और भी इस तरह के फिक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फैक्ट्स को फिक्शन की तरफ धकेला जा रहा है। जब इस तरह की चीज लगातार आती है उसे आप कैसे देखते हैं और हम इनसे किस तरीके से बच सकते हैं? खासकर इतिहास के वो गंभीर छात्र।
अनिरुद्ध:- महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि इतिहास के गंभीर छात्रों को किताबों से जानकारी लेनी चाहिए। उन्हें विद्वानों से जानकारी लेनी चाहिए, आदर्श रूप से। राजनेताओं या सोशल मीडिया पर लोगों से नहीं। मैं पूरी तरह से समझता हूं और मैं लोगों को अतीत के बारे में जिज्ञासा रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। लेकिन अगर किसी बिंदु पर वह जिज्ञासा अन्य समुदायों के प्रति घृणा की भावना में बदल रही है, तो वह कम से कम मेरे अनुसार कुछ चेतन होने की जरूरत है । क्योंकि मेरे सभी अध्ययनों में और जितने वर्षों से मैं इतिहास का अध्ययन कर रहा हूं, और आप किसी भी इतिहासकार से यह पूछ सकते हैं, एक बात जो इतिहास के गंभीर छात्र को सिखाता है वह यह है कि यह मनुष्यों की कहानी है। मनुष्य दोषपूर्ण होते हैं। मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होते। जैसे हमारी दुनिया में, बहुत सी चीजें हैं जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें भी हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, अतीत के साथ भी ऐसा ही है। यदि कोई अतीत की एक ऐसी तस्वीर चुन रहा है जो सभी पूर्वग्रहों की पुष्टि करती है और किसी को भी चुनौती नहीं देती है। तो स्वचालित रूप से वह एक सच्चा इतिहास नहीं है। यह एक सरलीकृत कहानी है जिसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बेचा जा रहा है। मैं इतिहास के सभी छात्रों को इतिहास को आपको चुनौती देने की अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, इतिहास को आपको सोचने के लिए प्रेरित करने की अनुमति दें, और इतिहास को आपको अपने साथी मनुष्य की समझ विकसित करने में मदद करने की अनुमति दें।
अरमान:- एक सवाल मैं आपसे चोल साम्राज्य पर और पूछना चाहूँगा किस तरह का उनका अंतरराष्ट्रीय संबंध देखने को मिलता है बाक़ी राज्यो से उनका व्यापार संबंध कैसा देखने को मिलता है?
अनिरुद्ध:- अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यापारियों द्वारा संचालित किया जाता था जो सामूहिक समूहों में संगठित थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण समूह को पांच सौ कहा जाता था। यह एक व्यापारी निकाय था, जो एक हजार साल के बेहतर हिस्से तक अस्तित्व में था जो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी लंबा है। उनकी पहुंच और उनका प्रभाव उत्तरी कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। और हम यह भी जानते हैं कि इंडोनेशिया में उनकी बस्तियां थीं। और तेरहवीं शताब्दी में, उन्होंने चीन में एक मंदिर भी बनाया था। तो यह वास्तव में एक उल्लेखनीय समूह है। और यही मैं पहले कह रहा था कि, जाधव, जब भी हम राजाओं को इतिहास के मुख्य नायक के रूप में सोचते हैं, तो हम इन बहुत अधिक दिलचस्प लोगों को नहीं देख पाते। लेकिन एक बार जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि समाज विविध है, कि सभी सामाजिक समूहों की अपनी प्रेरणाएं, प्रोत्साहन हैं, तो हम इस व्यापार की एक बहुत समृद्ध तस्वीर देखना शुरू करते हैं। और हम जानते हैं कि तमिल व्यापारियों ने न केवल जीवन की सभी दैनिक आवश्यकताओं में व्यापार किया, बल्कि उस समय दुनिया के कुछ बेहतरीन विलासिता के सामानों में भी व्यापार किया। तो चंदन, कस्तूरी, कपूर, लोबान, जो अरब से लेकर सुमात्रा, इंडोनेशिया तक दूर से आते थे। ये सभी सामान भारतीय शहरों में उपलब्ध थे। यह ऐसे व्यापारियों के कारण ही था कि भारत वैश्विक व्यापार के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बन गया।
अरमान :- शुरू मैं जैसा आपने कहा की बहुत बड़ा भाग है जिसे भारतीय राष्ट्रीय इतिहास अक्सर नज़रंदाज़ किया जाता है आपके हिसाब से वो कौनसे दक्षिण भारतीय इतिहास के प्रमुख पहलु है जिन्हे अनदेखा किया जाता है?
अनिरुद्ध:- मैं यह देखकर बहुत खुश हूं कि चोलों के बारे में एक बार फिर बात हो रही है। उनके बारे में जिज्ञासा है। लेकिन विशेष रूप से दक्कन क्षेत्र में भी कई, राष्ट्रकूट जैसे राजवंश हैं, जिन्होंने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था जिन्हें अरब यात्रियों द्वारा अब्बासी खलीफा, चीन के सम्राट, रोम के सम्राट के बराबर माना जाता था। उन्हें उनके समकालीनों द्वारा इतना शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन आज, वे हमारी ऐतिहासिक कल्पना में बहुत कम भूमिका निभाते हैं। लेकिन यह केवल राष्ट्रकूटों के लिए ही नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे स्थानों में भी कई अन्य राजवंश हैं, उदाहरण के लिए परमार। अगर आप झारखंड को देखें आप छत्तीसगढ़ को देखें, कलचुरी राजवंश या यहां तक कि ओडिशा के राजवंशों को देखें, खासकर, वे वैश्विक व्यापार में बहुत, बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने कुछ मंदिर चोल मंदिरों जितने बड़े बनाए, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, उदाहरण के लिए, ओडिशा के सोमवंशी राजवंश के बारे में। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था, जैसे, हर क्षेत्र ने भारत को वैसा बनाने में अपना योगदान दिया है जैसा वह है। हम यह नहीं कह सकते कि एक भाषा, एक समूह, एक धर्म ने ही सब किया है भारतीयता की पूरी अभिव्यक्ति है। हम प्रागैतिहासिक काल से ही हमेशा से एक विविध देश रहे हैं। और यही वह है जो सभी ऐतिहासिक साक्ष्य दर्शाते हैं।
अरमान - कॉलम शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार ।
अनिरुद्ध - धन्यवाद ।
 Madhav Kaushik
Madhav Kaushik
माधव कौशिक
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष प्रख्यात साहित्यकार माधव कौशिक से अरमान नदीम की खास बातचीत ।
मेरी पीढ़ी के पास साधना थी ,साधन नहीं थे आज की पीढ़ी के पास साधन तो बहुत है, साधना नहीं है - माधव कौशिक
परिचय - माधव कौशिक
- पद: वर्तमान में वह साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं.
- जन्म स्थान: हरियाणा के भिवानी शहर में, 1955 में जन्मे.
- साहित्यिक योगदान:
- छात्र अवस्था से ही कविताएँ और नाटक लिखना शुरू कर दिया था.
- 30 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें ग़ज़ल संग्रह, कविता संग्रह, आलोचना, बाल साहित्य, और अनुवाद शामिल हैं.
- उनके कुछ कार्यों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है.
- उन्होंने पुरस्कार विजेता टेलीफिल्म "हरि भरी हरियाली धरती" के लिए पटकथा भी लिखी है.
- पूर्व पद:
- पहले चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं.
- राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं.
- पुरस्कार:
- विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि सुब्रमण्यम भारती राष्ट्रीय पुरस्कार.
- उन्हें शिरोमणि साहित्यकार सम्मान, महाकवि सूरदास सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का सुब्रमण्यम भारती राष्ट्रीय पुरस्कार, और हरियाणा साहित्य अकादमी का आजीवन साहित्य साधना सम्मान भी मिला है.
- हाल ही में, उन्हें रूसी केंद्र विज्ञान और संस्कृति, नई दिल्ली द्वारा प्रतिष्ठित "दास्तोयेवस्की स्टार अवार्ड" से सम्मानित किया गया है.
- साहित्यिक संगठन में अनुभव: इनके पास साहित्यिक संगठन का व्यापक अनुभव है.
- दृष्टि: सभी 24 भारतीय भाषाओं में लेखन की गुणवत्ता में सुधार और उसे बनाए रखने, भाषाओं को जोड़ने और अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक मंचों पर भारतीय साहित्य की प्रतिष्ठा स्थापित करने पर बल देते हैं.
- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य: उन्हें साहित्य और संस्कृति में उनकी विशेषज्ञता के लिए राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष द्वारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य भी नियुक्त किया गया था.
अरमान :- मौजूदा वक्त में आप साहित्य अकादमी के अध्यक्ष लेकिन मैं यही जानना चाहूंगा कि साहित्य के प्रति आपका प्यार किस तरीके से उरुजगी पर आया और यह शुरुआत कैसे हुई?
माधव कौशिक:- अरमान, दरअसल मेरा यह मानना है कोई भी लेखक है वह परिवार और परिवेश की उपज होता है वही पहला वातावरण उसे आगे बढ़ाने मे मदद करता है और यह सच भी है । और अगर मैं आपको अपने शुरू के दिनों के बारे मे बताऊं मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ वहाँ पढ़ने लिखने का माहौल था। मेरे पिता श्री एक अध्यापक थे और वे उर्दू और फारसी के बड़े विद्वान थे। इसी वजह से जब आंख खुली और होश संभाला तो आसपास सिर्फ किताबें ही किताबें थी । मैंने बचपन से ही पत्र, पत्रिकाओं को अपने आस पास देखा और इसी वजह से बचपन से ही पढ़ने का शौक रहा । मेरे लिए उस माहौल का बड़ा योगदान रहा और एक प्रोत्साहन मिला। और दूसरी बात यह कि हमारे घर में भी पढ़े-लिखे लोगों का आना-जाना लगा रहता था। उर्दू हिंदी के बड़े लेखक शायरों का घर आना रहता था। शायर, अदीब आया करते थे । एक तरीके से इसी साहित्यिक माहौल में बड़ा हुआ मैं। और दूसरी एक चीज की जब कॉलेज में बी ए तक पहुंचा वहाँ मैंने देखा और महसूस किया की हिंदी के सारे क्लासिक पहले ही पढ़ लिए थे क्योंकि जैसा मैंने बताया की पढ़ने का शौक छोटी उम्र में ही हो गया था और हमारे घर में इतना प्रभाव था इन सबका कि घर में ही अच्छी खासी एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमे उस वक्त का अच्छा समृद्ध साहित्य मौजूद था । और मैं कह सकता हूं कि यह ईश्वर की कृपा ही थी मुझ पर और मेरी खुशनसीबी है कि जो मेरा पेशन था वहीं मेरी नौकरी भी उसी तरह की हुई। जिसने शुरुआती दिनों में मैंने अंकुर और सुगंधा दो साहित्यिक पत्रिकाएं उनका संपादन किया और फिर 2001 में मैं चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का सचिव हो गया। 20-25 साल तक रिटायरमेंट के बाद भी वॉइस अध्यक्ष रहा और 2007 से लेकर अब तक साहित्य अकादमी दिल्ली में हूं। पहले हिंदी परामर्श मंडल का सदस्य रहा ,कन्वीनर रहा फिर 2018 में वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। 2023 में मैं अध्यक्ष चुना गया। पूरा जीवन मेरा कह सकते हैं की साहित्यिक माहौल में ही बीता। ईश्वर की कृपा रही एक सुविधाजनक स्थिति रही मेरे लिए कि जिन चीजों से मैं प्रेम करता हूं, जिन्हें पसंद करता हूं वही सब चीजों के साथ में काम कर रहा हूं। कि मुझे और बड़े लेखकों का सानिध्य भी मिला समर्थन भी मिला और उनका प्रेम भी मिला।
अरमान:- मौजूदा वक्त को अगर हम देखते हैं तो लोग एकांत को काफी पसंद करने लगे हैं अगर हम सोशल मीडिया भी देखते हैं तो उसमें अपना वक्त देना ज्यादा पसंद करते हैं । आपके विचार में हम सामाजिक संवाद किस तरीके से बढ़ा सकते हैं?
माधव कौशिक:- देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। लेकिन आज हमने उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया जैसा होना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया और इसके एडिक्ट हो गए । टेक्नोलॉजी को अगर आप अपना मास्टर बना लेंगे तो फिर तो वह आपके कंधे पर बेताल की तरह बैठ जाएगी। लेकिन अगर आप उसे एक उपकरण की तरह सहायक की तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसी वो है और जिसका इस्तेमाल उसी तरीके से होना चाहिए तो वह आपको उसी ढंग से ही सुविधा देगी जैसा आप चाहते है । मैं अक्सर युवा लेखकों से जब भी संवाद करता हूं मैं यही बात कहता हूं हमारे मोबाइल में दुनिया की सभी भाषाओं का, सभी जबानों का साहित्य है। दुनिया की सभी लाइब्रेरीज इसमें है सारे म्यूजियम आपको इसमें मिल जाएंगे । अनुवाद इसमें है, दुनिया भर की ऑडियो बुक्स इसमें है अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम जिन गांवों में पैदा हुए क्योंकि वहां तो कोई किताब ही नहीं थी ना कोई दुकान थी। गांव में तो इस तरह की चीजों की आपको सुविधा नहीं थी लेकिन आज सभी के पास है मोबाइल फोन। अगर किसी को इसका इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता उसमें जुनून नहीं है फिर वह तो गलत है । अब तो आप जैसे बोलोगे वैसा लिखा भी जाता है इसमें मैं पूरे देश भर में जाता हूं बहुत सारे जो नए पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वह इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करते हैं । ऐसा तो नहीं कह सकते कि सभी खराब ढंग से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। था तो ही एक वरदान की तरह ही लेकिन अगर आप इससे फेसबुक पर घटिया चीज देखेंगे तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। हिंदी में आपको उदाहरण दूं तो कविता कोश करके एक वेबसाइट है उस वेबसाइट में आपको शुरू से लेकर अब तक लाखों किताबें ,लाखों लेखक के बारे में जानकारी मिल जाएगी और यह सिर्फ हिंदी में नहीं यह तो हर भाषा में आपको यह सब चीज मिल जाएगी। हाथों हाथ अनुवाद होने लगा है अब तो। अगर टेक्नोलॉजी को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह साहित्य के लिए भी संवर्धन में होगी। और आप जब इस पर लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो इसकी कोई सीमा तो है नहीं यह पूरे विश्व में आपको पहुंचा सकती है। पहले आपको इंतजार करना पड़ता था वह इंतजार खत्म हो चुका है सारे रिसाले आपको इसमें मिल जाएंगे, सभी अखबार आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप में जुनून होना चाहिए। पढ़ने लिखने की भावना होनी चाहिए। सीखने की ललक होनी चाहिए।
अरमान:- आपने अपनी बात में युवा लेखकों के साथ संवाद का जिक्र किया आपकी नजरों के सामने से न जाने कितनी ही रचनाएं कितनी ही किताबें निकली है। आपकी नजर में मौजूदा युवा लेखन की क्या स्थिति नजर आती है आपको?
माधव कौशिक:- मेरे हिसाब से युवा लेखन इस समय हिंदुस्तान की हर भाषा का बड़ा ऊर्जावान है क्योंकि उनके पास में बदलते दौर की संवेदना भी है और सोच भी है । मेरी पीढ़ी के आदमी के पास जो कथ्य था वह तो पुराना कथ्य था अभी जो समाज में बदलाव आए हैं वह उसे पूरी तरीके से जी रहे हैं और लिख रहे हैं दिक्कत सिर्फ यह है और यह बात में रेखांकित करना चाहूंगा मेरी पीढ़ी के पास साधना थी, साधन नहीं थे आज की पीढ़ी के पास साधन तो बहुत है, साधना नहीं है। भाषा के प्रति लापरवाही है जल्दबाजी में भी हैं और उन्हें लगता है कि एक ही रात में कालजई रचना आए और हम महान हो जाएं। यह जो ललक है इससे साधना में थोड़ी कमी आती है। जितने उनके पास में साधन है अगर उसके साथ में उनके साधना भी जुड़ जाए तो नई पीढ़ी कमाल कर देगी। नई पीढ़ी बहुत अच्छा लिख रही है इसमें कोई दो राय नहीं है। हम साहित्य अकादमी की तरफ से युवा पुरस्कार भी देते हैं। युवाओं की नई किताबें भी आती है। कई बार हमारे पीढ़ी के लोग बड़े दुखी होते हैं कि उनसे निर्णय नहीं हो पता इतनी नई चीज आ रही है और एक चीज और नई भाषा और नए कथ्य की जो नई पीढ़ी है उसने नई तरह की विधाओं का भी आविष्कार किया। आपको लगेगा कई बार कहानी पढ़ते हुए संस्मरण का भी तत्व बीच में आया यानी कि एक विधा दूसरी विद्या के साथ जुड़ी हुई है। विधाओं की आवा जाई बहुत अच्छी हुई है। नई विधाएं भी बनी है एक तरह से साहित्य को रिच करने का यही सही तरीका है। इसमें सभी चीज सम्मिलित हैं आत्मकथाएं भी है अब तो छोटे-छोटे पीस भी आने लगे हैं तो यह काफी चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं और जब इनमें परिपक्वता आ जाएगी क्योंकि नई विधाओं को थोड़ा पकाने में भी समय लगता है। ग़ालिब साहब का मिसरा है ना एक "आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक" कुछ समय के साथ में वह चीज अच्छी भी हो जाएगी पक भी जाएगी।
अरमान:- आपने अपनी बात में कहा कि हमारी पीढ़ी के पास में साधना थी और आज की पीढ़ी के पास में साधन है । कहीं ना कहीं भाषा के प्रति साधना है पकड़ है मौजूदा वक्त में थोड़ी कम देखने को मिलती है । हम सब जानते हैं साहित्य समाज में बदलाव का एक बड़ा माध्यम है और यह सवाल स्थापित लेखक के लिए भी है और नौजवान साहित्यकारों के लिए भी है । क्या वह वाकई सामाजिक मूल्यों पर ध्यान दे रहें हैं क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं लेखक को तटस्थ होना चाहिए या फिर कुछ हद तक लेखक पक्षपाती हो जाता है?
माधव कौशिक:- आपने यह बहुत बढ़िया सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया दो तरह का लेखन है दुनिया में इस वक्त एक लेखन है टिकाऊ और एक लेखन है बिकाऊ जो बिकाऊ लेखक है वह बेस्ट सेलर तो हो जाता है उसकी बहुत सारी किताबें बिक जाती है। मार्केटिंग का भी दौर है लेकिन वह टिकता नहीं है और जो टिकाऊ लेखन होता है वह हमेशा समाज के आम आदमी का प्रवक्ता होता है। वह किसी और के लिए नहीं सच्चाई के लिए लिखता है। उसे यह परवाह नहीं होती है कि कैसे देख कर कोई ताली बजाएगा या नहीं। और जो बेस्ट सेलिंग की क्लास में आते हैं जो बिकाऊ होते हैं वहां कुछ ऐसा होता है कि लोग सिर्फ फायदा उठाने का सोचते हैं खास तौर पर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसने बिकाऊ लेखन को बहुत ज्यादा हवा भी दी है लेकिन उसका इतना ज्यादा अर्थ और इतना ज्यादा महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वह चार दिन रहता है और फिर गायब भी हो जाता है । और उनका पता भी नहीं चलता आखिर में तो वही साहित्य बचता है भाई जिसमें मानवीय मूल्य होते हैं जिसमें दृष्टि होती है और जो समाज में बदलाव है और वह जो बदलाव है आपको दृष्टि संपन्नता देता है । और वह आपको नजर नहीं आता बदलाव होता तो है जैसे टेक्नोलॉजी सबको एक रात में बदल देती है वह एक रात में नहीं बदलता। वह एक रात में तो नहीं बदलते लेकिन इंसानियत को जिंदा रखने के लिए सबसे कारगर वही ठहरता है "पत्थरों के देवता होते हैं, पत्थरों पर नहीं" समय पर जो छाप छोड़ता है वह वही लेखन छोड़ता है। आप देखो हमारे पास हजारों साल का कलाम है ,हजारों साल की कविताएं हैं, हमारा भक्ति काव्य भी है, सूफी काव्य भी है। हिंदुस्तान की जो असली संस्कृति है वह बड़ी मिली जुली है वह बुनी हुई एक रस्सी की तरह से है उसमें एक-एक रेशा ऐसे मिला हुआ है अगर उन रेशों को कोई बिखरने की कोशिश करता है तो वह मूर्ख है जो समाज का नुकसान कर रहा है। बेस्ट सेलिंग तो वह हो जाती है जो बनी हुई रस्सी के रेशों को बिखेरने की कोशिश करते हैं।
अरमान :- आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से टिकाऊ और बिकाऊ का उदाहरण दिया. और जो बिकाऊ लेखन के अगर हम बात करें तो वह कहीं ना कहीं हमें गुटबाजी की तरह भी ले जाता है आपकी नजर में गुटबाजी साहित्य को किस हद तक नुकसान पहुंचा रही?
माधव कौशिक:- सुनिए, लोगों को ऐसा लगता है कि यह चीज नुकसान पहुंचाती है। एक दरिया बह रहा है उस दरिया में कोई व्यक्ति डंडे से या लाठी से मारता है तो उस दरिया के पानी में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं अलबत्ता कुछ छींटे उड़ के किसी के कपड़ों पर जरूर लग सकते हैं । जो साहित्य, अदब है यह तो एक दरिया की तरह बहने वाली चीज इन गुटबाजियों का कोई अर्थ नहीं है और इनका कोई असर भी नहीं है। वह कुछ लोगों के अहम को संतुष्ट करने का साधन हो सकता है बाकी किसी भी तरह का कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकते । और हिंदुस्तान में तो मैंने देखा है और जो टेक्नोलॉजी आई है और नई पीढ़ी के बच्चों में नए लेखकों में चाहे जितनी मर्जी उनमें साधना की कमी हो जल्दबाजी भी कर रहे हैं लेकिन उनमें गुटबाजी नहीं है। यह एक बहुत बड़ी बात है मैंने नए लेखकों को बहुत ज्यादा इन चक्करों में पड़ते हुए नहीं देखा। ये आज से 10 - 20 साल पहले तक था। संकट मेरी पीढ़ी के सामने था । बहुत सारे लेखक जनवादी हो गए थे कुछ धनवादी हो गए थे । न जाने और कितनी गुटबाजियां हो गई थी। कह सकते हैं कि उनके कुछ सिद्धांत कम थे व्यक्तिगत में वह ज्यादातर सामंती मानसिकता के लोग ज्यादा थे। अब यह चीज नई टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दी है। पहले पत्रिका का जो संपादक होता था उसका एक गुट होता था। अब उन संपादकों की कोई परवाह नहीं करता ।अब जिसे जो लिखना होता है वह सोशल मीडिया पर भी डाल देता है। इतने ई पब्लिकेशन शुरू हो चुके हैं अभिव्यक्ति का माध्यम है और इतने माध्यम हो चुके हैं अब किसी का सामंतवाद नहीं चल सकता साहित्य में । मेरी नजर में अब गुटबाजी उस अंदाज़ में नहीं है जो पहले हुआ करती थी।
अरमान :- आपकी नजर में साहित्य आलोचना है वह क्या है? क्या साहित्यिक आलोचना में व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा सकती है?
माधव कौशिक:- साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज है रचना। जब तक आलोचना का वर्चस्व रहा गुटबाजी रही। और जिस तरह की आलोचना हुआ करती थी अब वैसे आलोचक भी नहीं रहे। पहले जो आलोचना हुआ करती थी ,आलोचक होते थे उनके फ्रेम बने हुए थे एक मार्क्सवादी फ्रेम था वह अलग-अलग उनके हिसाब से आलोचना कर्म करते थे । और वह सारे फ्रेम टूट चुके हैं कह सकते हैं कि एक तरह से जो आलोचक का आतंक था वह समाप्त हो गया । पहले आलोचक को खुश करने के लिए उसकी नजरों में चढ़ने के लिए लिखते थे अब किसी को परवाह ही नहीं है क्योंकि आलोचना का मतलब हमारे यहां कुछ गलत भी दिया गया है । आलोचक का काम ही होता है कि जो कृति है उसके अंदर कुछ आम पाठक को बातें नजर नहीं आती वह उसको दिखाएगा सामने लाकर अब इतना कोई मेहनत ही नहीं करता अब यह सब चीज बदल गई है ।आलोचना के भी पैरामीटर बदल गए हैं मेरा यह मानना है कि कोई आलोचक कृति के माध्यम से ही गुजर कर आलोचना कर सकता है। और बहुत सारे लेखकों का मूल्यांकन भी नहीं हुआ । किसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि वह किसी फ्रेम में नहीं है अब वह स्थिति नहीं है क्योंकि साहित्यिक आलोचना अर्थ भी बदल गए हैं उसके पैरामीटर भी बदल गए हैं । अब जो राजनीतिक गुटबाजी की, राजनीतिक सिद्धांतों पे ना कोई आलोचना कर सकता है और ना कोई उसका अर्थ है।
अरमान:- आपने पत्रिकाओं के संपादकों की बात की , पूरी स्थिति आपको कैसी नज़र आती है आज के वक्त में?
माधव कौशिक:- मैं प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया का मेंबर रहा हूं। और इस लिए मैं यह कह सकता हूं कि बदलती हुई स्थिति और बदलती हुई टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे संस्थाओं के चरित्र को भी बदला है। और अगर हम कहे की इस टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बिगाड़ ही दिया है तो ये भी सही बात नहीं है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज नई भी दी है। फिर कहूंगा की ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो गया है। और जो दृष्टि संपन्न व्यक्ति है वह तो हमेशा से अच्छा काम ही करेगा इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी अपनी शख्सियत है जिसके अपने विचार फिर चाहे वह पत्रकारिता में हो साहित्य में हो वह अच्छा काम ही करेगा खराब आदमी कहीं पर भी हो वह खराब काम ही करेगा।
अरमान :- मौजूदा वक्त में साहित्य अकादमी क्या ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जो कम प्रकाशित साहित्यिक भाषाओं को में फ्रेम में लाने का काम किया जाए?
माधव कौशिक:- साहित्य अकादमी के नवाचारो पर अगर मैं बात करूँ तो जी बिल्कुल यह हमने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है पहले तो केवल जो 24 भाषाओं के लिए ही जो साहित्य अकादमी में हुआ करता था जिस मान्यता प्राप्त है उसी में काम करते थे लेकिन अब हमने उन भाषा उन बोलियां को भी ले लिया है जिनकी खुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं है उनमें भी एक इनाम देते हैं भाषा सम्मान के नाम से और इसी के साथ ही साहित्य अकादमी ने आदिवासी लेखन और एलजीबीटी लेखन भी हमने अपने दायरे में शामिल किया है। हम लगता इन सबको साथ लेकर आयोजन कर रहे है बड़े-बड़े। इस मामले में हमने यह नई चीज की शुरुआत की है। और मेरा ऐसा मानना है की कहीं पर भी अभिव्यक्ति किसी भी वर्ग द्वारा फिर चाहे वह हास्य का लेखन है हम उसको भी उतना ही सम्मान देते हैं और यह भाषा सम्मान उसी का नतीजा है की। और हमारी यही कोशिश रहती है की सभी वर्गों को समान आधार पर आपनी बात कहना का मौका मिले कोई भी किसी भी आधार से वंचित न रहे और हमने आकाशवाणी के साथ भी अनुबंध किया है। नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक सेंटर है जिसे हम निकोल कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट को में भाषाओं का अजायबघर घर कहता हूं । कह सकता हूं कि साहित्य अकादमी की जो योजनाएं हैं उनमें से सबसे बड़ी योजनाओं में से यह है। और जो मौखिक परंपराएं हैं उन्हें भी हम केंद्र में लेकर आए। पुरस्कृत भी हम उसी आधार पर करते हैं बोलियां में और अच्छा एक दूसरा काम हमने और शुरू किया है आने वाले दिनों में ई पब्लिकेशन भी हमारी योजना में शामिल है। कोशिश है कि जो गांव-गांव में लिखने वाले हैं उनके साथ फिर राब्ता बनाने के लिए आयोजन करते हैं और जो उसे ग्रामीण परिवेश में लिखने वाले हैं उनकी रचनाओं को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं।
अरमान - कॉलम शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने हेतु आपका बहुत बहुत आभार ।
माधव कौशिक - आपका भी बहुत आभार ।
 Dr. Mamta Pant
Dr. Mamta Pant
डॉक्टर ममता पंत
प्रतिष्ठित साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर ममता पंत से कॉलम शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
मेरे लिए आलोचना करते समय व्यक्ति मायने नहीं रखता, बल्कि उसकी रचना मायने रखती है - ममता पंत
परिचय
डॉ. ममता पंत एक प्रतिष्ठित हिंदी शिक्षिका, साहित्यकार, शोधार्थी और समर्पित अकादमिक व्यक्तित्व हैं, जिनका शिक्षण, लेखन और सामाजिक चेतना से भरपूर योगदान बहुआयामी है। उत्तराखंड की साहित्यिक परंपरा में उन्होंने न केवल रचनात्मक लेखन को सशक्त किया है, बल्कि प्रशासनिक व शिक्षणीय जिम्मेदारियों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में वे सुभाष चंद्र बोस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अल्मोड़ा के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व वे कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस.एस.जे. परिसर, अल्मोड़ा में भी अध्यापन कर चुकी हैं। उनके पास 15 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की गरिमामयी सूची है, जिनमें ‘डॉटर ऑफ उत्तराखंड अवार्ड’, ‘राष्ट्रीय भाषा सेवा रत्न सम्मान’, ‘अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मान’, ‘फिजी मातृभाषा सम्मान’ और ‘पर्यावरण योद्धा सम्मान’ जैसे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल हैं।
साथ ही, इनके तीस से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोधपत्र/लेख प्रकाशित हैं। उनके लेखन का विषय क्षेत्र नारी विमर्श, दलित साहित्य, उत्तराखंडी समाज, मीडिया अध्ययन, पर्यावरण चेतना और साहित्यिक समालोचना जैसे विविध और समसामयिक मुद्दों को समेटे हुए है। डॉ. ममता पंत विभिन्न अकादमिक समितियों की सक्रिय सदस्य रही हैं—जैसे प्रवेश समिति, पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा मूल्यांकन समिति, महिला उत्पीड़न निवारण समिति, IQAC, NAAC मूल्यांकन आदि। महिला सुरक्षा, सामाजिक समरसता और पर्यावरण सरोकारों की मुखर पक्षधर रही हैं।
अरमान: आपकी साहित्य में शुरुआत किस तरीके से हुई ? और आपका अकादमिक्स वाकई प्रेरणा का स्रोत है।
ममता: मैं शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी। मेरा जन्म संयुक्त परिवार में हुआ था, जहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि लड़कियों को आगे पढ़ाने में परिवार हिचकिचाता था, क्योंकि हमारा एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार था। लेकिन मैं थोड़ी विद्रोही प्रवृत्ति की थी और गलत चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैंने हमेशा पढ़ाई जारी रखने का सोचा और पापा से बात की। पापा ने मेरा साथ दिया और कहा कि अगर मैं अच्छे नंबरों से पास होती रहूँ, तो मेरी पढ़ाई जारी रखेंगे। इंटर तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बी.ए. में कुछ दिक्कतें आने लगीं, क्योंकि जो विषय मैं लेना चाहती थी, उनमें प्रैक्टिकल थे और कॉलेज रोज़ जाना पड़ता था। पापा तो ठीक थे, लेकिन माँ डरती थीं। मम्मी खुद एक टीचर होने के बावजूद पारिवारिक दबाव के कारण डरती थीं। इसलिए मुझे अपने विषय बदलने पड़े। रेगुलर कॉलेज जाने के बावजूद भी मेरी पढ़ाई प्राइवेट जैसी हो गई थी। मैंने घर की जिम्मेदारियाँ, बहनों, भाई और अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ निभाते हुए स्नातक की पढ़ाई पूरी की। जब मैं इंटर में पढ़ती थी, तो मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। मना करते-करते मैंने जैसे-तैसे बी.ए. पास किया, लेकिन जैसे ही मैंने एम.ए. में एडमिशन लिया, फिर से पारिवारिक दबाव बढ़ने लगा। ताऊजी और बड़े पापा जैसे संयुक्त परिवार के सदस्यों ने कहा कि लड़की को इतना क्यों पढ़ाना है? मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होती थी, फिर भी यह दबाव था। एम.ए. के दौरान फिर से रिश्ते आए, तो पापा ने कहा कि मम्मी बहुत जिद कर रही हैं। मैंने पापा से कहा, "आप बहनों की शादी करवा दीजिए, पर मुझे तो पढ़ना है।" तो मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पापा का सपना था कि मैं एम.ए. टॉप करूँ और मैंने एम.ए. प्रीवियस में टॉप किया और उसके लिए मुझे पुरस्कृत भी किया गया। एम.ए. फाइनल में भी मैंने टॉप किया । पापा ने यह भी कहा था कि अगर मैं एम.ए. में अच्छा करूँगी, तो वह मुझे नेट करने के लिए बाहर भेज देंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है। मैंने सोचा कि अगर मैं नेट क्वालीफाई करके प्रवक्ता बन जाती हूँ, तो मेरे लिए सिविल सर्विसेज के रास्ते भी खुल जाएँगे। मैं टॉप तो कर गई, लेकिन मुझे नेट की कोचिंग के लिए नहीं भेजा गया। मम्मी के दबाव में मेरी शादी हो गई। बहुत जोर-जबरदस्ती के साथ, कि "बड़ी बहन हो, शादी तो करनी ही है ।" मैंने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी, हालाँकि मैं PCS का पहला एग्जाम नहीं दे पाई। शादी के एक साल के अंदर मेरा बेटा हुआ। उसके बाद दो-तीन साल तक मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ाया, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी । पापा और मम्मी को भी धीरे-धीरे महसूस हुआ कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मेरे डॉक्टर भी पापा से नाराज होते थे कि उन्होंने बेटी का भविष्य बर्बाद कर दिया है । इसी दौरान मैंने पी.एच.डी. में रजिस्ट्रेशन करवाया। यह मेरे लिए एक नया उद्देश्य था, क्योंकि मैं डिप्रेशन की स्थिति से उबर रही थी। पी.एच.डी. में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मुझे सौभाग्य से बहुत अच्छे निर्देशक मिले, जिनका व्यवहार पिता जैसा था। उनकी पत्नी भी हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती थीं । पी.एच.डी. की थीसिस मैंने सिर्फ साढ़े पाँच महीने में पूरी कर दी। यह एक जुनून था। मैंने दिन-रात मेहनत करके थीसिस लिखी और तुरंत ही मेरा वाइवा हुआ। मेरी थीसिस पर बहुत अच्छी रिपोर्ट थी और लोग बहुत खुश थे। मनोहर श्याम जोशी पर यह मेरी पहली पी.एच.डी. थी, जो कुमाऊँ विश्वविद्यालय से हुई थी। उस समय राष्ट्रीय स्तर पर मनोहर श्याम जोशी को उत्तर-आधुनिक उपन्यासकार के रूप में प्रचारित किया जा रहा था । इसके बाद गुरुजी ने मुझसे पूछा कि अब क्या करोगी? मैंने कहा, "अब क्या करूँगी? बच्चा भी है, उसे पढ़ाना है।" उन्होंने मुझे बी.एड. करने की सलाह दी। मैं बी.एड. नहीं करना चाहती थी, लेकिन गुरुजी के कहने पर मैंने बी.एड. भी किया । आज मुझे लगता है कि गुरुजी ने क्यों कहा था। बी.एड. के दौरान मैंने टीचिंग की बारीकियां सीखीं और मुझे रोल मॉडल टीचर मिले, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बी.एड. के एग्जाम चल ही रहे थे कि कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पोस्ट निकली। मैंने आवेदन किया और मेरा चयन हो गया । इस तरह मैं कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एसएसजी प्रिसल, अल्मोड़ा में पढ़ाने आ गई। मेरा टीचिंग कार्य शुरू हुआ और इसी दौरान 2010 में परमानेंट फैकल्टी की पोस्ट आई। लेकिन यूनिवर्सिटी की कुछ राजनीति के कारण 2010 में मुझे एन.एफ.एस. कर दिया गया, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्टुअल पद पर बनी रही। फिर 2013 में भर्तियाँ दोबारा हुईं । उस समय भटनागर सर कुलपति बनकर दिल्ली से आए थे। उनका विजन बहुत बड़ा था। उस समय हम दो कॉन्ट्रैक्टुअल फैकल्टी का चयन परमानेंट पद पर हुआ। बाकी सभी कॉन्ट्रैक्टुअल फैकल्टी को बाहर कर दिया गया और बाहर से नई फैकल्टी लाई गई, कोई जापान से, कोई अमेरिका से। 2013 में हम लोगों को "भटनागर ब्रांड" कहा जाता था। मेरा चयन परमानेंट पद पर हो गया । इसके बाद मैंने हिंदी अध्यापन लगातार जारी रखा। मेरा सिविल सर्विसेज का सपना तो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं और उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। इसके बाद मैंने एन.सी.सी. के लिए भी अप्लाई किया, तीन इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरते हुए मैं पास हुई। मैं तीन महीने ग्वालियर ट्रेनिंग के लिए गई, जहाँ से मैं लेफ्टिनेंट बनकर लौटी। आज मेरे एन.सी.सी. के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं।
अरमान - लेखन के विषय में बताइए ।
ममता - मेरा लेखन तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। मैं नौवीं-दसवीं क्लास से ही कविताएँ लिखती थी। एम.ए. के दौरान मेरी टीचर डॉ. प्रभा पंत मैम ने मेरी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने कहा कि मेरी कविताएँ समसामयिक परिवेश पर बहुत सटीक होती हैं और मुझे अपना लेखन जारी रखना चाहिए । मैं अपनी कविताओं को कभी संकलित नहीं कर पाई। वह कभी डायरी में, कभी कॉपियों में ही रह गईं। लेकिन कैंपस में आने के बाद मैंने अपनी पहली कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था 'पीड़ा पातक पानी'। कुमाऊँनी में इसका अर्थ होता है, अरबी के पत्तों में चमकती हुई पानी की बूँद, जो जरा सी हलचल से गिर जाती है। मैंने इसे स्त्री के जीवन के प्रतीक के रूप में लिया । इस कहानी का प्रसारण आकाशवाणी अल्मोड़ा से हुआ। हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष ने इसे रेडियो पर सुना और मुझे बुलाया। उन्होंने मेरी कहानी की बहुत तारीफ की और कहा कि यह हमारे परिवेश का जीवंत चित्रण है। उन्होंने मुझसे एक कहानी संग्रह तैयार करने को कहा और कहा कि उसकी भूमिका वह लिखेंगे। लेकिन समय के अभाव और अन्य परेशानियों के कारण मैं उनके रहते यह संग्रह नहीं लिख पाई। मैंने अपनी कहानियों का संग्रह 'तिमूर' नाम से छपवाया। कई लोगों ने इसकी तारीफ की। मुझसे पूछा गया कि मैं यह कैसे कर लेती हूँ। मैंने कहा कि मेरी कहानी तो स्वतः मुझे लिखवाती हैं, क्योंकि मैं जो सोचकर लिखती हूँ, वह कहानी नहीं बनती, बल्कि कहानी अपने आप कोई और ही मोड़ लेकर अपने अंतिम पायदान पर पहुँचती है। इसी बीच जयपुर साहित्य संगीत में एक विज्ञापन निकला था, जिसमें कहानी संग्रह और कविता संग्रह पुरस्कार हेतु भेजे जाने थे। मैंने अपनी पाँच प्रतियाँ भेजीं और बाद में मुझे पता चला कि मेरे कहानी संग्रह 'तिमूर' को जयपुर सम्मान के लिए पुरस्कृत किया गया है। यह मेरी पहली क्रिएटिव राइटिंग थी। इसके अलावा, मेरे रिसर्च पेपर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपे हैं। कई साहित्यकार मेरे आलोचना कर्म की भी सराहना करते हैं। उनका कहना है कि मैं जिस तरीके से आलोचना करती हूँ, वह आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। मेरे लेखन की शुरुआत इसी तरीके से हुई। मुझे बहुत लोगों का प्रोत्साहन मिलता रहा, लेकिन पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक परेशानियाँ भी थीं। फिर भी, मैं इन सब से विचलित नहीं हुई और लगातार कार्य करती रही। आज मैं जिस भी स्तर पर हूँ, वह मेरे आत्मविश्वास का परिणाम है।
अरमान - नशा मुक्ति अभियान से ज़मीनी स्तर पर क्या बदलाव महसूस हुआ ।
ममता: देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी काम तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक आप उसे अंतःप्रेरित होकर न करें। कागज पर काम करना अलग बात है और अंतरात्मा की प्रेरणा से काम करना अलग। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो सफलता निश्चित ही मिलती है। मैं इस समय महिला समिति की अध्यक्ष हूँ और नशा मुक्ति अभियान की सदस्य भी हूँ। एन.सी.सी. में भी होने के कारण हम आए दिन कुछ ऐसे काम करते रहते हैं, जिससे हमें जिले स्तर पर पहचान मिलती है और समर्थन भी मिलता है। आज की तारीख में युवा नशे की गिरफ्त में हैं। हमारी रिसर्च में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जैसे, लोग फ्लूइड, बाम और विक्स से भी नशा कर रहे हैं। हमने कई लोगों की काउंसलिंग करवाई है। हमारे कैंपस में कई संवाद कार्यक्रम और काउंसलर सेशन हो चुके हैं, जिसमें हमारे साइकोलॉजी विभाग ने बहुत मदद की है। इस काउंसलिंग के दौरान कुछ कारण सामने आए। इनमें से एक कारण अभिभावक भी हैं। आजकल पति-पत्नी दोनों सर्विस क्लास हैं और एकल परिवार बढ़ गए हैं। अगर दादा-दादी नहीं हैं, तो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। सुबह बच्चा स्कूल चला जाता है और शाम को घर आता है, तो माँ-बाप उसे समय नहीं दे पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा बाहर क्या कर रहा है। हमें खुद भी प्रेरणा लेनी होगी कि हम अपने बच्चों का रखरखाव और पालन-पोषण कैसे करें। घर के संस्कार काम आते हैं, लेकिन आजकल बच्चा घर पर बहुत कम समय बिताता है। वह ट्यूशन में या बाहर रहता है। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे माध्यमों में ज्ञान का भंडार है, लेकिन दिशा भटकाने के भी कई रास्ते हैं। हमें यह नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है। इसलिए हमें अंतःप्रेरित होकर काम करना चाहिए, न कि केवल वाहवाही लूटने के लिए। मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ, जिससे कोई दिशा मिल सके। एन.सी.सी. में भी हम ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं। मेरी पूरी गर्ल्स वाहिनी है। मेरी एक बच्ची वाई.पी. के तहत कजाकिस्तान तक गई है। उसने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल लेकर आई। उसे मुख्यमंत्री से लेकर गवर्नर तक के अवॉर्ड मिले हैं। मैं अपने एन.सी.सी. के बच्चों से कहती हूँ कि जो बच्चे कैंपस के पास पेड़ों के बीच बैठकर नशा कर रहे होते हैं, उन्हें जागरूक करो। बच्चे कभी-कभी सफलता पाते हैं और कभी-कभी उन्हें सुनना भी पड़ता है। मैं दो साल पहले जिला स्तर के बोर्ड में भी थी। हम अप्रत्यक्ष रूप से बताते थे कि नशा कहाँ होता है। वहाँ धर-पकड़ भी होती थी और उनकी काउंसलिंग भी की जाती थी। आज काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से सफल हो गए हैं, क्योंकि इसमें घर-परिवार का बहुत महत्व है।अगर हम किसी को बताते हैं कि आपका बच्चा यह सब कर रहा है, तो वे विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि हम उनके बच्चे को बदनाम कर रहे हैं। अगर कोई शिकायत करता है और बच्चा गलत कदम उठा लेता है, तो यह भी एक चुनौती है। मुझे लगता है कि सरकार तो योजनाएँ बनाती है, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारना हम जैसे लोगों का काम है। अगर हम यह कहते हैं कि सरकार साथ नहीं देती, तो मुझे लगता है कि हम अपने काम से विमुख होकर यह सब बातें करते हैं।
अरमान - महिला सुरक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगी।
ममता: कानून तो बन गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है, महिला का स्वयं जिम्मेदार होना। मेरे पास जो भी केस आए, उनमें मुझे यह लगा कि पीड़िता में एक डर होता है। पहला डर अपने परिवार से, कि वह उसका समर्थन करेगा या नहीं। दूसरा डर समाज से और तीसरा उस संस्थान से, जहाँ वह काम करती है। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर के डर को दूर करना होगा। कानून और सरकारी योजनाएँ भी हमारा साथ तभी देती हैं, जब हम बिना डरे अपनी बात रख पाते हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब स्त्री की बात आती है, तो मुझे लगता है कि हम आज भी बहुत पीछे हैं। हमारा यह संकरा आसमान अभी भी विस्तार मांग रहा है। सरकारी प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन कभी-कभी कानून या सरकार में बैठे लोग भी इन चीजों को अनदेखा कर देते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि कई मामलों में दबाव के कारण ऐसा होता है। मेरे पास जो केस आते हैं, उनमें कई लोगों ने अंडर इंफ्लुएंस की बात की। मुझे फोन भी आए कि "मैम, इसे जरा वैसे देखिएगा।" लेकिन मेरा जो मन कहता है कि यह गलत है, वह सही है, मैं उसी के साथ खड़ी रहती हूँ। अगर कोई शिकायत हमारे पास आती है, तो हम सबसे पहले पीड़ित को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर बात सही लगती है, तो हम संबंधित विभाग में एक मीटिंग रखते हैं और खुलकर बात करते हैं। हम वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी करवाकर आगे की कार्रवाई के लिए कुलपति महोदय को भेज देते हैं। जब बात पुलिस तक जाती है, तो कई बार पुलिस एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं करती। इसका कारण भी दबाव ही होता है। हम भी अपने दायरे में रहकर कोशिश करते हैं। हमारे साथ विधि विशेषज्ञ और एन.जी.ओ. से जुड़े लोग भी होते हैं, जिनकी मदद से हम पीड़ितों की मदद करते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई महिला वाकई पीड़ित है, तो उसकी एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए और पूरी जाँच-पड़ताल भी। दूसरा, समझौते की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आज समझौता हो जाता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि कल दूसरी पीड़िता नहीं आएगी? महिलाएँ डर के मारे नहीं बता पातीं। उन्हें डर होता है कि उन्हें अपने एच.ओ.डी. का डर है या फिर उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगा। जब तक एक महिला अपने अंदर के डर को दूर करके आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए मुझे अंतःकरण की आवश्यकता लगती है और परिवार का सहयोग भी बहुत जरूरी है। मुझे यह समझ नहीं आता कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, तो वह बदनाम कैसे हो जाएगी? परिवार उसका समर्थन क्यों नहीं करता? इसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया।
अरमान - अवसाद और शिक्षा का क्या संबंध है ।
ममता: देखिए, शिक्षा के माध्यम से हम अवसाद को काबू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे काउंसलिंग सेशन जरूरी लगते हैं। अगर शिक्षा में एक काउंसलर को जोड़ा जाए, तो बहुत फर्क पड़ सकता है।जहाँ मेरा बेटा पढ़ता था, वहाँ की प्रिंसिपल बहुत दूरदर्शी थीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अवसाद केवल बालिगों में होता है, यह बच्चों में भी शुरू हो जाता है। अगर मैं अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रही हूँ, तो वह धीरे-धीरे अवसादग्रस्त हो जाता है। वह आक्रामक होना शुरू कर देता है और पढ़ाई को लेकर दबाव महसूस करता है।जब मैंने प्रिंसिपल मैम से इस बारे में बात की, तो उन्होंने एक काउंसलर रखा। इसके बाद बच्चों में बहुत फर्क आया। बच्चे अपने खेलने के समय में भी स्वेच्छा से काउंसलर मैडम के पास बैठकर अपनी समस्याएँ बताते थे।मुझे लगता है कि शिक्षा में एक काउंसलर की भूमिका बहुत जरूरी है, और इसे नर्सरी से ही शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नर्सरी का बच्चा अवसादग्रस्त नहीं होता। अगर कोई बच्चा ड्राइंग पसंद करता है और हम उसे बार-बार पढ़ाई करने को कहते हैं, तो उसका स्वाभाविक विकास बाधित हो जाता है। जब प्राकृतिक विकास बाधित होगा, तो निश्चित ही अवसाद की स्थिति आएगी। एन.सी.सी. के बच्चों से भी जब मैंने बात की, तो ज्यादातर बच्चे अपने बचपन की बातें बताते थे, कि उन्हें घर पर भी डांट मिलती थी। तो मुझे लगता है कि मानसिक विकास वहीं से अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में काउंसलिंग का एक पीरियड होना बहुत जरूरी है, जिसमें बच्चा खुलकर अपनी बात कह सके। काउंसलर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए भी, क्योंकि हम भी अवसादग्रस्त हो सकते हैं। हर कार्यालय में, हर क्षेत्र में एक काउंसलर होना चाहिए, जो इस अवसाद को दूर करने में मदद करे।
अरमान - आलोचनात्मक लेखन: व्यक्तिगत नहीं, रचना पर आधारित आप क्या कहना चाहेंगी ।
ममता: बिल्कुल भी नहीं। आलोचना हमेशा रचना को देखकर की जानी चाहिए, न कि व्यक्ति को देखकर। मैं आपका प्रश्न समझ गई। मेरे लिए आलोचना करते समय व्यक्ति मायने नहीं रखता, बल्कि उसकी रचना मायने रखती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रचना का नीर-क्षीर विवेक करूँ। मैं उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू ढूँढती हूँ। जहाँ तारीफ करने लायक होता है, वहाँ मैं तारीफ करती हूँ, लेकिन जहाँ लेखन संबंधी त्रुटियाँ होती हैं, वहाँ मैं वह भी लिखती हूँ। आलोचना हमेशा तटस्थ होकर करनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप किसी को जानते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा लिखें और किसी को नहीं जानते हैं, तो कुछ भी लिख दें। संपूर्ण तो कोई नहीं होता, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आलोचना के मापदंडों के आधार पर ही किसी कृति की आलोचना करें।
अरमान - लेखन का मुख्य मुद्दा क्या रहता है ।
ममता: वैसे तो मेरा लेखन समसामयिक परिदृश्य, स्त्री लेखन और थर्ड जेंडर जैसे मुद्दों पर है। एक स्त्री होने के नाते मेरे जीवन के अनुभव तो मेरे लेखन में स्वाभाविक रूप से आते ही हैं। मेरा रचना कर्म समाज के ऐसे परिदृश्य उजागर करने की कोशिश करता है, जो छिपे हुए हैं।
अरमान - थर्ड जेंडर और नारीवाद को आप कैसे देखते हैं ।
ममता: नारीवाद केवल पुरुषों का विरोध करके नहीं हो सकता। मैं इस बात की घोर विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि इस जगत में जितनी स्त्री की भूमिका है, उतनी ही पुरुष की भी है। हाँ, मैं पितृसत्तात्मकता के खिलाफ हूँ, जहाँ नारी की आकांक्षाओं और इच्छाओं का दमन किया गया। आपने कहा कि नारीवाद में सिर्फ जन्मजात महिलाओं की जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। थर्ड जेंडर में भी अगर कोई स्त्री है, जिसकी सारी भूमिकाएँ नारी जैसी हैं, तो उसे हम किनारे क्यों कर दें? मुझे लगता है कि नारीवाद से संबंधित सभी सामाजिक विमर्शों में थर्ड जेंडर का योगदान होना चाहिए। मेरी समझ में यह नहीं आता कि अगर कोई विकलांग पैदा हो जाता है, तो हम उसे समाज से अलग नहीं करते, लेकिन एक थर्ड जेंडर को परिवार ही अपने से अलग कर देता है। ऐसा क्यों? यह आज तक मैं समझ नहीं पाई। थर्ड जेंडर को भी हमारी तरह जीने का अधिकार है। क्यों उनको परिवार से अलग करके एक अंधेरी कोठरी में धकेल दिया जाता है? यह मेरे लिए बहुत कष्टदायक है। जब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, तो क्या वे समाज के अंग नहीं हैं? इतिहास उठाकर देखें, तो थर्ड जेंडर की हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजा-महाराजाओं के समय से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैंने उनके बारे में जितना अध्ययन किया है, मुझे लगता है कि वे किसी भी काम को बहुत ईमानदारी और वफादारी से करते हैं। तो क्यों हम उनको अलग करके उनकी खूबियों का उपयोग राष्ट्रीय हित में नहीं करते? मुझे लगता है कि उनकी जो खूबी है, उसे राष्ट्रीय हित में इस्तेमाल करना चाहिए।
अरमान - नई शिक्षा नीति और बेरोजगारी पर आपके विचार जानना चाहूंगा ।
ममता: यह बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा नीति को प्राइमरी लेवल से ही सुधारने की जरूरत है। जो पुरानी पद्धति थी, जिसमें साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ था, वह बेहतर थी। आज जो बिना फेल किए पास करने की बात है, उसने पूरा विकास अवरुद्ध कर दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, बी.ए. लेवल के बच्चों को यह पता नहीं है कि अलंकार क्या है, समास क्या है। मुझे लगता है कि हमारी पुरानी नीति तो होनी ही चाहिए, साथ ही नई शिक्षा नीति के इनोवेशन को भी जोड़ा जाना चाहिए। वैज्ञानिकता भी तभी कारगर होगी, जब हमारी जड़ मजबूत होगी। हमने एक पेड़ तो लगा दिया, लेकिन उसे जरूरी खाद-पानी नहीं दिया। वह एक दिन सूख जाएगा। आज तक के बच्चों को बिना पढ़े पास कर दिया जाता है। मेरी बहन इंटर कॉलेज में लेक्चरर है। वह बताती है कि अगर वह बच्चे पर दबाव डालती हैं, तो बच्चे कहते हैं, "मैडम, आर.टी.ई. का अधिनियम आपको पता है ना? आठ तक तो पास करना है।" हमें अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति में नवीनता का उन्मेष करना चाहिए। साथ ही, चीन, जापान और फ्रांस की तरह हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। हमारे यहाँ आज भी हिंदी दूसरे दर्जे पर है। अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हुए सारे विषय हिंदी में पढ़ाना अनिवार्य कर दें, तो मुझे लगता है कि हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में नंबर एक पर आ जाएगा। बेरोजगारी की बात करें, तो हम सरकार का ही मुंह क्यों देखते हैं? आज गाँव में कई लोग अपना उद्योग खोलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना में क्या है? आपके अंदर के निजी कौशल को ही तो बढ़ावा दिया जाता है। हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में अल्पाना की कारीगरी की जाती है, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी है। उससे नेम प्लेट और घर की सजावट की चीजें बन रही हैं और अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। मुझे लगता है कि कर्मठता बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कर्मठता है, तो आप अपने निजी उद्योग-धंधों को भी विकसित कर सकते हैं। समाज की जो यह मानसिकता है कि सरकारी नौकरी ही जरूरी है, इसे हमें ही तोड़ना होगा। कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे लगता है कि आधुनिक पीढ़ी इस सोच को नहीं मानती। कुछ समय बाद यह चीजें भी खत्म हो जाएँगी। जैसे जातिगत भेदभाव धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, वैसे ही यह भी खत्म हो जाएगा।
अरमान - कॉलम शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने हेतु आपका बहुत बहुत आभार ।
ममता - धन्यवाद