List of interviews Back
|
गुरमेहर कौर |
उर्ना बोस |
वन्दना यादव |
श्री चिंतन उपाध्याय |
डॉक्टर सीमा जैन |
|
प्रेम जनमेजय |
डॉक्टर संजुक्ता दासगुप्ता |
राजा हसन |
श्रेया गुप्ता |
Sarju Katkar सरजू काटकर |
| Darshan Darshi दर्शन दर्शी |
Dr.Ravindra Mangal डॉ. रविन्द्र मंगल |
Gaur Haridas गौर हरिदास |
N Kiran Kumar एन किरण कुमार |
Ustad Amin Sabri उस्ताद अमीन साबरी |
We offer a 30-day return policy for all products. Items must be in their original condition, unused, and include the receipt or proof of purchase. Refunds are processed within 5-7 business days of receiving the returned item.
Gurmehar
Kaur 
गुरमेहर कौर
युवा लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता गुरमेहर कौर से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
रचनात्मक साहित्य समाज में आमूल चूल परिवर्तन की ताकत रखता है - गुरमेहर
परिचय
गुरमेहर कौर युवा भारतीय एक्टिविस्ट और लेखिका हैं। लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक करने के बाद, इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविले कॉलेज से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। छोटी उम्र और विषम परिस्थितियों में जो उपलब्धियां हासिल की है वो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादाई है ।
अरमान :- गुरमेहर कौर नाम से आज हर कोई परिचित है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके लेखन की शुरुआत किस तरह से हुई ?
गुरमेहर:- अगर मैं आपको अपने लेखन के बारे में बताऊं तो मैं कह सकती हूं कि मैंने लिखना कम उम्र में शुरू कर दिया था और मुझे याद आता है जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी उस वक्त मेरी मैथ्स कुछ ज्यादा खास नहीं थी इसलिए अतिरिक्त क्लास हुआ करती थी तो मेरे टीचर्स मुझे निबंध लिखने के लिए कह देते थे । और उस वक्त में चार-चार घंटे एक ही विषय पर लिखा करती थी और इस तरह से जैसे-जैसे वक्त आगे हुआ तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैं लिख सकती हूं और मेरे विचार लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकती हूं । और यह विचार भी पुख़्ता होने लगा कि बड़े होने के बाद में भी मुझे राइटिंग ही करनी है । और इसी दौरान जब मेरा लगातार इंटरेस्ट राइटिंग में बन रहा था तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि इंडिया की बहुत बड़ी लेखिका हैं उनका नाम है अरुंधति रॉय उनकी किताब में आपको लाकर देती हूं ,उनकी किताब आप पढ़ो क्योंकि वह मौजूदा वक्त में बहुत अच्छी लेखिका है। तो आप उनसे सीखिए और जब बचपन से ही मैंने अरुंधति रॉय की किताबें पढ़नी शुरू कर दी थी । लगभग मेरी उम्र रही होगी तेरह से चौदह साल जिस वक्त मैंने पहली बार उन्हें पढ़ा था । और एक किताब पढ़ने के बाद जब मैं बार-बार और दूसरी किताबें भी मैंने उनकी किताबें पढ़नी शुरू की तो मैं यह कह सकती हूं कि उन्हीं की किताबों के थ्रू मेरा रुझान एक्टिविज्म की तरफ भी काफी हुआ । और जितना मैंने उन्हें पढ़ा और एक्टिविज्म को मैंने समझा और इतना इंटरेस्ट आ गया कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था और उस दौरान और भी कई संगठन एक्टिव हुए थे। और उसके बाद में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आई लगातार ही जब किताबें पढ़ी ,लोगों को पढ़ा और उन्नीस साल की उम्र तक मेरा पॉलीटिकल आईडियोलॉजी को अगर हम कह दें तो लेफ्ट की तरफ मेरा रुझान काफी हो गया था । और जब एक इंसिडेंट हुआ था एबीवीपी ने अटैक किया था तो उस दौरान मैंने कैंपेन चलाया था स्टूडेंट अगेंस्ट एबीवीपी जिससे मोमेंट पर काफी ज्यादा अटेंशन लोगों की हुई थी। और जो पूरा राइट विंग का इकोसिस्टम है उन्होंने पूरा मेरे खिलाफ काम करना शुरू किया और सवाल उठाए और यही चीज थी मैंने उसके बाद में लिखना शुरू किया ।
अरमान :- अगर मैं राज्य सरकारों की साहित्य अकादमियों पर बात करूं तो यह जग जाहिर है कि उन पर किस तरह का पॉलीटिकल कंट्रोल रहता है। क्या आपको लगता है यह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस साहित्य अकादमी से हटना चाहिए?
गुरमेहर:- बिल्कुल हटना चाहिए इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है फिर चाहे वह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या किसी भी तरह का दबाव जैसा कि आपने कहा क्योंकि उससे लिटरेचर का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि साहित्य का काम यह नहीं है कि वह किसी सरकार का नैरेटिव लोगों के सामने रखे और उसको बनाए रखने में अपना योगदान दे । किसी सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा करे। लिटरेचर का असल काम यह है कि हमारे रोजमर्रा में जो डे टु डे कहानी होती है उसे बताया जाए, एक खूबसूरत तरीके से उसे लोगों के सामने, पढ़ने वालों के सामने पेश किया जाए लिटरेचर की क्राफ्ट और केंद्रीय स्ट्रक्चर में उस चीज को बताया जाए हमारी कहानी, जो हमारी चीज हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज होना बहुत जरूरी है की साहित्य जैसी जो कला है, जो टैलेंट है ,आर्ट है और उसे किसी भी प्रकार के प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल ना किया जाए। रचनात्मक साहित्य समाज में आमूल चूल परिवर्तन की ताकत रखता है । और यह बड़ी जिम्मेदारी साहित्य अकादमियों की भी बनती है कि वह किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा में शामिल ना हो । साहित्य अकादेमी दिल्ली जरूर अपने विधान के कारण अपवाद है वरना राज्यों की साहित्य अकादमियां पूरी तरह राजनीति से प्रभावित है । राज्य अकादमियों में नियुक्तियां भी राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर होती है । आप समझ सकते है कि जब अकादमियों में नियुक्तियां राजनीतिक आधार पर होगी तो साहित्य की क्या दशा होगी ।
अरमान :- अगर मैं आपसे नई बात पर सवाल करता हूं ,यह किसी और भी महिला से सवाल करूं अगर मैं राइट विंग की महिला से बात करता हूं या सेंट्रल से सवाल करूंगा मुझे हर बार एक अलग पहलू मिलेगा और उसकी परिभाषा भी सबकी अलग-अलग है मैं जानना चाहूंगा आपकी नजर में नारीवाद क्या है और अगर आप उसे अपने शब्दों में परिभाषित करें तो वह कैसी होंगी ?
गुरमेहर:- देखिए जो मेरे लिए नारीवाद है बहुत जरूरी है कि इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म हो। ऐसी फेमिनिज्म ना हो जो किसी भी ग्रुप को एक्सक्लूड ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरनेट पर हम जब फेमिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं और जो बहुत ही ज्यादा कुछ चीज प्रचलित है फेमस हो रही है या फिर जो पॉपुलर नरेटिव्स हैं। और अगर हम देखते हैं वेस्ट में अभी नई-नई जे.के रॉलिंग स्टाइल की फेमिनिज्म चली है कि हम महिलाओं के हित में बात कर रहे हैं तो हम एंटी ट्रांस बात करेंगे तो हमने देखा कि इस तरह की फेमिनिज्म भी चली है। लेकिन जो मुझे लगता है मैं जिस तरह की फेमिनिज्म को मानती हूं जो मुझे सही लगती है वो इंटरसेक्शनल होनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ अपर कास्ट या फिर बॉर्न फीमेल की बात ना करें । आप यह भी देखिए कि क्या आपकी फेमिनिज्म की डेफिनेशन में दलित महिलाएं, बहुजन महिलाएं शामिल है, ट्रांसजेंडर उनमें शामिल है क्या आप उनके बारे में भी इस समानता के साथ में बात करती हैं क्या उनके अधिकारों की भी उसमें बात होती है। मेरी नजर में तो यही असली नारीवाद है जिसमें सभी महिलाओं के हित हो, सभी महिलाओं का ख्याल रखा जाए। जब हम पितृ सत्ता के खिलाफ बात करते हैं इस तरह से हम समानता के साथ में बात करें मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जब हम इन सब बातों के ऊपर अपनी बात रखते हैं और यह जब जिस तरह का विरोध करते हैं तो एक ख्याल यह भी रखना चाहिए सिर्फ अपर कास्ट विमेंस उन्हीं का नैरेटिव आगे ना बढ़ाएं सभी के साथ समान व्यवहार रखा जाए । और मैं फिर कहना चाहूंगी कि फिर चाहे वह दलित हो ,ट्रांसजेंडर महिलाएं हो सभी का इसमें ध्यान रखना चाहिए। उन सभी महिलाओं की बात भी इसमें सामान्य के साथ में रखी जाए जितना की एक अपर कास्ट महिला के हित की बात की जाती है। जितना एक बॉर्न फीमेल को स्पेस होता है उतना ही बाकियों को भी मिलना चाहिए। मेरे लिए तो असल नारीवाद यही है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है।
अरमान :- बिल्कुल आपने सही बात की हम समानता की बात करते हैं एकता की बात करते हैं लेकिन आज के वक्त में अगर हम देखें तो उदार हो जाने को भी गाली बना दिया गया है इसे आप कैसे देखते हैं?
गुरमेहर:- बिल्कुल लिबरल्स को तो काफी लोग डिफेंस करते हैं और अगर हम राइट विंग की बात करें तो वह एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं लिब्रांडू। लेकिन अगर हम बहुत ही लेफ्ट की तरफ भी देखें तब भी वह वहां भी इसी तरह की चीज हमें देखने को मिलती है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लिबरलिज्म को कुछ खास आईडियोलॉजी की नजर से मैंने नहीं देखी । भारत में आईडियोलॉजी लिबरल लेफ्ट राइट इतना नहीं चलता । मुझे लगता है यह एकेडमिक साइंस में या फिर ऑनलाइन ट्विटर के पर वहां मुझे लगता है कि इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है कि मैं लिबरल हूं, मैं मार्क्सवादी हूं और वह लोग इस लेंस से दुनिया को देखते हैं और मुझे लगता ही बहुत छोटी स्पेस है। यह आप भी जानते हैं अगर उन स्पेस से अगर हम हट के देखें क्योंकि पॉलिटिक्स में काफी काम करती हूं जो कि मेरा डे टू डे का काम है ,मेरी दिनचर्या है उसमें मैं काफी स्थानीय संगठनों से बात करती हूं कि वह किस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं ,उन पर मैं बात करती हूं, उन पर चर्चा की जाती है, उनसे बात की जाए कुछ पॉलिसीज के ऊपर वह क्या चाहते हैं इन सब चीजों में मेरा काम बहुत ज्यादा रहता है। और वहां मैंने एक ही चीज लगातार देखी है। वह लोग इन सब चीजों को इतना महत्व नहीं देते। अगर हम अपनी कॉलोनी , देखें अगर हम अपने गांव को देखें, अपने आसपास की जगह को देखें तो वह लोग ज्यादातर कास्ट के लेंस से इन सब चीजों को देखना पसंद करते हैं । लोग धर्म के आधार पर देखते हैं। आईडियोलॉजिकल लेंस इतना डोमिनेट नहीं करता। अगर उदाहरण के लिए हमें कहूं कि पंजाब को लीजिए अब पंजाब के अंदर कोई लिबरल है या नहीं हमें यह नहीं पता लोगों का ऐसा मानना है कि लिबरल या लेफ्ट हो जाने का मतलब स्टेट के अगेंस्ट जो स्टेट के ऑपरेसिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके अगेंस्ट बोले। अमृतपाल मेहरों करके एक लीडर हैं उन्होंने एक यंग लड़की का मर्डर किया है और अपने तर्क में यह कहा है कि वह सिखईस्म की मर्यादा से बाहर जा रही थी तो इसका मर्डर जस्टिफाई है। तो जितनी भी माइनॉरिटी हैं फिर चाहे वह सिख हो या अन्य उन्हें वह काफी ऑपरेस्ड करती हैं। और पंजाब में क्या हो रहा है कि लिबरल और लेफ्ट की जो एकेडमिक्स है वह एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं । अगर हम जैसे मान के चलिए एक छोटी टिक टोकर का मर्डर हुआ सिख एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा हम कह सकते हैं तो अगर इस चीज को हम विरोध करेंगे तो ऐसा लगेगा स्टेट के साथ हैं दूसरे पक्ष में अगर चले गए तो ऐसा लगेगा कि हम सिख और माइनॉरिटी के हित में बात नहीं कर रहे और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से चुनना पड़ता है और इसी वजह से इनका स्टैंड इतना क्लियर नहीं है।
अरमान :- वह जो एक वक्त था जब वह पूरा राइट विंग और मीडिया एक मशीनरी के साथ में संगठित होकर आपके खिलाफ खड़े थे और उसे स्थिति में भी अपने अपने आप को संभाले रखा वह मनुष्य थी आपकी क्या थी क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है।
गुरमेहर:- अंग्रेजी में एक कहावत है सिंक ओर स्विम अगर आपको एक तालाब में फेंक दिया जाए तो आपके पास में क्या रास्ते बचते हैं वही मुझे लगता है मेरे साथ भी हुआ। तो यह सब देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे पास में और कोई दूसरा रास्ता बचा हुआ है । जब आपके ऊपर इतनी ताकतवर तरीके से हमले होते हैं अब उसे आपको लगातार किया जाता है पूरे एक सिस्टमैटिक ढंग के साथ में एसॉल्ट डेथ मारने करने की धमकियां रेप थ्रेड और उसे वक्त सिर्फ आप उन्नीस साल के हैं आप उसे वक्त भी एक टीनेजर ही हैं आपने उसे वक्त इतनी ज्यादा दुनिया देखी भी नहीं है। और यह सब चीज लगातार देखने के बाद मुझे एहसास हुआ और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास में कोई और विकल्प मुझे दिखा नहीं और मैंने यह ठाना की अगर इन्होंने मुझे इस तरीके से अटैक करना शुरू ही कर दिया है तो अब मैं भी अपनी पूरी ताकत के साथ में इनका सामना करूंगी । और अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी जीनी है तो मैं इस तरह तो जी नहीं सकती हूं । मैं यह देखकर नहीं जी सकती की यह मुझे एंटी नेशनल बोल रहे हैं । जो मुझे इन्होंने शब्द बोले हैं तो उसके बाद में फिर जो जब मुझे लगा कि मेरे पास में प्लेटफार्म था उसे कैंपेन के बाद में और उसके बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो एक नॉरेटिव है उसे रिक्लेम करना है उनके हाथों से और इस तरह की परिस्थितियों में अक्सर यही होता है कि लोगों के पास में रास्ते नहीं होते हैं । या तो आप उसे खत्म कर दीजिए या फिर आप सरवाइव कीजिए और मैने सरवाइव करने का फैसला किया।
अरमान :- अगर हम युवा राजनेता की बात करें जिस तरीके से लगातार युवाओं का राजनीति में भागीदारी हम देखते हैं और जो एक दृश्य हमें दिखाया जाता है क्या वाकई में वह इतने स्वतंत्र है जैसा हमें दिखाने की कोशिश होती है?
गुरमेहर:- यह चीज डिपेंड करती है कि वह किस पार्टी से आ रहे हैं अगर आप कहेंगे कि बीजेपी से कि वह बहुत स्वतंत्र हैं तो उसका आप क्या जवाब बन सकता है । यह फैसला युवाओं को करना है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में युवा राजनीति में आ रहे हैं अब यह देखिए कि वह कौन सा संगठन ज्वाइन करते हैं यह चीज उन पर डिपेंड करती है और मैं यह कह सकती हूं कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मैं काम करती हूं और यह चीज भी अच्छी है कि हम लोग यह सोचते हैं कि जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं कि वह सिर्फ आईडियोलॉजिकल बेस के ऊपर आते हैं । ऐसा नहीं है मुझे लगता है कि राजनीति काफी ज्यादा उनके रीजंस होते हैं बहुत अलग-अलग मोटिव होते हैं । और मुझे लगता है यह कोई मोरली खराब बात हो ऐसा भी नहीं। वह किसी भी पार्टी से हो किसी भी मोटिवेशन से हूं मैं बहुत खुश यूथ को एक्टिव होना चाहिए पॉलिटिक्स में मोरालिटी के गेम में नहीं अगर आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूं।
अरमान :- सोशल मीडिया नॉरेटिव जिस तरीके से किए जा रहे हैं और उसमें भी अगर हम ए की बात करते हैं डायरेक्ट हमारे को अगर हम उसमें जोड़ें और इन सब के साथ में जो एक डबल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है सोशल मीडिया पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि युवाओं को गुमराह करने का एक रास्ता ही है कि जो रियल इश्यूज है उनसे अलग रखा जाए और उन्हें मिस गाइड करने का ही एक तरीका बन चुका है। और जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड अप करने का काम मीडिया करती है
गुरमेहर:- और मुझे तो लगता है यह सिर्फ एक नैरेटिव नहीं और यह इस तरीके से भटका रहे हैं कि यूथ को एक जोंबी सा बना दिया जाए उन्हें किसी चीज का फर्क ही ना पड़े और आज हम देख भी रहे हैं कि उन्हें किसी चीज से फर्क पड़ता भी नहीं है आसपास लोग हैं उनसे पूछिए कि गजा में इतनी बड़ी जंग चल रही है इतना वक्त हो चुका है इतने हजारों लोग मर रहे हैं बच्चे लगातार मार रहे हैं क्या उन्हें वाकई में इस बात से फर्क पड़ता है उनसे पूछे उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर सोशल मीडिया पर भी इस तरह के विजुअल आते हैं तो कुछ देर उसको देखते हैं फिर अगर उसको स्वीप कर देंगे तो किसी और की फोटो आ जाएगी किसी डॉग की वीडियो आ जाएगी किसी क्यूट पप्पी की वीडियो आ जाएगी तो इस परिस्थिति में आप देखेंगे भी तो क्या किया आपका माइंड ही जोंबी सा बन गया है आपके दिमाग में रहता ही नहीं है कि हम किसी से पूछे किसी से सवाल करें की हो क्या रहा है हमारी आंखों के सामने आप इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं।
गुलमेहर कौर - धन्यवाद
Urna Bose 
उर्नाबोस
पोएट्री सिर्फ हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है वह हमारे जीवन का भी हिस्सा है। - उर्ना बोस
देश की प्रतिष्ठित अंग्रेजी साहित्यकार और सामाजिक विषयों पर गहरी पकड़ रखने वाली उर्ना बोस से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
परिचय
उर्ना बोस प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवयित्री, संपादक और समीक्षक हैं। लगातार छह वर्ष से उनकी कविताएँ विश्व स्तर पर वायरल हो रही हैं। उन्होंने तेलंगाना कविता मंच से ‘द एनचैंटिंग एडिटर अवार्ड, 2019’ और ‘महिला सशक्त - शानदार रचनात्मक प्रभावशाली - स्त्री शक्ति प्रेरणा पुरस्कार, 2020’ जीता। फिर प्रतिष्ठित ‘निसिम इंटरनेशनल प्राइज़ फ़ॉर पोएट्री, 2021’, उसके बाद ‘पैनोरमा इंटरनेशनल लिटरेचर अवार्ड, 2024’ मिला। ‘डिफरेंट ट्रुथ्स’ की उप संपादक के रूप में, वह अपना समय ‘पोएट 2 पोएट’ कॉलम को भी समर्पित करती हैं - एक गहन प्रेमपूर्ण श्रम जिसमें वह गहराई से निवेश करती हैं। उर्ना के अव्यवस्था-तोड़ने वाले, प्रतिष्ठित विज्ञापन अभियान और ब्रांड कार्य ने उद्योग श्रेणियों में प्रतिष्ठित और अत्यधिक सम्मानित भारतीय और वैश्विक रचनात्मकता पुरस्कार जीते हैं, और कुछ आज उद्योग के केस स्टडी भी हैं।
अरमान :- अंग्रेजी साहित्य में मौजूदा वक्त में आप एक बड़ा नाम है तो सबसे पहला सवाल यही है कि आपका साहित्य में रुझान कैसे हुआ
उर्ना बॉस:- अगर मैं आपको अपनी जर्नी शुरू से बताऊं तो जो शब्दों के साथ में लगाव है और उनसे जो प्रेम है वह काफी कम उम्र से खुद महसूस करने लगी थी. आप कह सकते हैं कि जब मेरी उम्र पांच या छह साल रही होगी उस वक्त से शब्दों के साथ मेरा जो प्रेम है वह मुझे महसूस होने लगा था। और स्कूली वक्त में जब काम दिया जाता था तो मुझे जो सबसे पसंद आता था वह लिखता ही होता यानी कि जब होमवर्क के लिए लेख, राइटिंग या पोयम्स दी जाती थी तो वह मुझे काफी ज्यादा पसंद थी । और मुझे उसमें मजा भी आता था तो कम उम्र से ही लिखने का और पढ़ने का मुझे शौक हो गया था। और जब क्लास में पोएट्री पढ़ाई जाती तो वह मुझे काफी पसंद आई थी खासकर की मेरा जो रुझान है वह अंग्रेजी साहित्य की तरफ ज्यादा होने लगा। अगर हम अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली में भी अंग्रेजी अन्य भारतीय भाषाओं के साथ मान्यता प्राप्त है । अब उसे कॉलोनियल लैंग्वेज नहीं माना जाता, एक वक्त था जब हम कह सकते थे कि विदेशी लोगों के साथ इसे लाया गया लेकिन एक लंबे वक्त के साथ यह भाषा भी यहां के रंग-ढंग में बस गई । और साहित्य अकादमी ने भी इसकी पुष्टि की । शब्दों के साथ जो मेरा रिश्ता बचपन से ही महसूस किया वह आज तक महसूस होता है कि जब मैं अपनी लाइफ में कोई भी काम क्यों ना करूं तो जुड़ाव हमेशा शब्दों के साथ ही रहता है। पोएट्री का मेरे जीवन में इतना प्रभाव रहा कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई उसके बाद में और ज्यादा मुझे इसके बारे में समझ आई क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है सीधा सिंपल आपकी जीवन शैली होती है तो उस वक्त आपको शायरी की जो महत्व है शायद समझ नहीं आती लेकिन जब ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ होती है तो उसका महत्व और उसका जो मूल रस है उसे आप अपने आप को जोड़ते हैं। और उसके बाद में यह चीज का एहसास होता है की पोएट्री सिर्फ हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है वह हमारे जीवन का भी हिस्सा है। और जब इसे गहराई से पढ़ना शुरू किया तो यह एहसास हुआ कि यह आपके अंदर तक उतरती है लेखक ने इसे किसी भी जगह बैठकर लिखा हो अपनी स्थिति के अनुसार लिखा हो लेकिन यह आपको खुद के साथ जोड़ती है और आप खुद को इससे जुड़ा महसूस करते हैं फिर चाहे वह एक सौ साल पहले ही क्यों ना लिखी हुई हो। वह कविता जो लेखक ने सौ साल पहले लिखी थी वह मुझे आज मदद कर रही है यही असली लेखन की लेखक अपनी स्थिति और अपने वक्त की स्थिति को लिखना है लेकिन वह आने वाले सौ सालों तक भी महफूज रहती है और पाठक को अपने से जोड़े रखती है। और इसी एहसास की वजह से मेरा रिश्ता जो शब्दों के साथ बचपन से ही था वह आगे चलते-चलते साहित्य में इस तरह बन गया कि मैं इसे हमेशा अपने से जुड़ा महसूस करती हूं।
अरमान :- आपने बहुत खूबसूरत बातें कहीं जिसमें जो भाषा से आपका प्रेम है वह आपने दर्शाया फिर वह कोई भी भाषा हो सकती है सभी साहित्य सृजन के मार्ग है लेकिन जब भाषा विवाद आप देखते हैं तो उस वक्त लेखक के रूप में आपको क्या महसूस होता है?
उर्ना बॉस:- आपका जो यह सवाल है काफी जटिल है और उतना ही जटिल इसका जवाब भी अगर इस मुद्दे के ऊपर में अपनी सोच बताऊं क्योंकि भारत में जितने भी लेखक हैं साहित्य से जुड़े हुए लोग वह लगातार ऐसी चीजों को बड़ी गंभीरता के साथ में देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि इनका नुकसान भी हमारे समाज को कितना हो सकता है ।और इसी समस्या के बीच में रहकर हम लिख भी रहे हैं जैसा कि मैं आपको कहा यह बड़ा ही जटिल मुद्दा है तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी पूर्ण रूप कोई जवाब हो ना हो इसका भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन जहां तक मेरी समझ जाती है मैं कह सकती हूं कि हमारा जो देश है वह काफी खूबसूरत और डायवर्स है क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं सभी के अपने साहित्य हैं कोस कोस में बदले पानी चार कोस में बानी ऐसा हमारा देश है। अगर हम हिंदी की भी बात करें तो कुछ इलाकों के बाद में आप जब जाएंगे तो उसमें भी आपको कुछ फर्क नजर आएगा अगर आप राजस्थान में हिंदी बोलेंगे उसमें आपको कुछ शब्दों में फर्क महसूस होगा वही उत्तर प्रदेश के व्यक्ति से जब बात करेंगे या महाराष्ट्र के व्यक्ति से तो इस तरह हमारा देश खूबसूरती का एक गुलदस्ता है। आपकी एक मातृभाषा है आपके विद्यालय में भाषा है और एक आपकी तीसरी भाषा भी है आप यह देखिए की ना सिर्फ लेखक जो कि साहित्य से जुड़ा व्यक्ति है एक आम इंसान आम नागरिक भी अपने दिन में तीन से चार भाषाओं का उपयोग करता है और वह समझता भी है। सच है कि हम हर भाषा को समझ भी नहीं सकते हमारी भी कुछ सीमाएं हैं , इंसान है तो हर चीज को ना तो हम समझ सकते हैं लेकिन हर भाषा को सम्मान तो हम दे सकते हैं फिर चाहे आप उसे समझा ते हो या फिर ना समझते हो लेकिन सम्मान अगर हम देते हैं तो इसमें हमें कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए। आपको उदाहरण दूंगी मेरे साहित्य अकादमी के अनुभव से कि जब वहां हम गए तो पूरे देश से वहां लेखक आए और उन्होंने अपनी अपनी रचनाओं का वाचन किया और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब वह अपनी शैली में बात करते हैं तो कुछ चीज या कुछ शब्द समझ नहीं आते हैं लेकिन साहित्य और भाषा का जो रिदम है वह आपके दिल तक जब जाता है तो वह खुद वह खुद आपको उसकी समझ होने लगती है। और यही खूबसूरती है विविधता में एकता की और मुझे लगता है कि इससे एक जश्न के माहौल के साथ हमें देखना चाहिए और मैं जहां तक देखा और समझा है मैं फिर से यही कहूंगी की भाषा हमें कोई समझ आए या ना आए लेकिन हमें उसका सम्मान जरूर करना चाहिए।
अरमान:- बात सच है कि सभी भाषाओं को सपना सम्मान देना चाहिए और अगर मैं बात करूं लेखन के सब्र की तो उसमें काफी कमी देखने को मिलती है यानी कि जो लोग बाहर से साहित्यिक जगत को देखकर आते हैं उसके बाद में उनमें सब्र खत्म हो जाता है कि जल्दी छापना और आगे बढ़ाने की हो इसे आप कैसे देखते हैं?
उर्ना:- यह आपने बिल्कुल सही बात की और मैं इससे सहमत भी हूं और यह मैं कहना चाहूंगी कि हर दौर के अपने-अपने कुछ फीचर्स और परेशानियां होती है मौजूदा वक्त में जो टेक्नोलॉजी है अगर हम उसे देखते हैं तो वह बहुत ही अच्छी और उपयोगी चीज है लेकिन वह भी अपने साथ में बहुत सी खामियां लेकर आती है इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि हर चीज उंगलियों पर मिलनी शुरू हो चुकी है अगर कोई सामान भी चाहिए तो बाहर जाने की जरूरत है मैं महसूस नहीं है हम घर बैठे वेबसाइट से खाने की चीज या और दीगर हमारे जो सामान है उन्हें हम आर्डर करके मंगा सकते हैं और पेमेंट भी ऑनलाइन ही कर देते हैं पहले जो चिट्ठी लिखी जाती थी अब ईमेल ने उसकी जगह ले ली है वहां तक कि अगर हम मनोरंजन की बात करें तो फिल्म देखने के लिए जो पहले टिकट लेते हुए लाइनों में लगा वह भी अब नहीं होता हम घर बैठे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं आप यह देखिएगा कि वह चीज भी तो खत्म हुई है यानी कि मनोरंजन के लिए भी जिस तरीके की मेहनत एक जो हमें करनी पड़ती थी वह जो उसके बाद की खुशी हमें मिलती थी वह अब खत्म हो चुकी है यह जो आदत हमें वहां से पड़ी तो वह हमें साहित्य में भी कई बार महसूस हुई की हर चीज जब इतनी ही आसान हो गई है तो हम दूसरी चीजों में भी वैसी ही मांग करने लग गए हैं। और यह कहीं ना कहीं समझ में लोग नहीं पा रहे हैं कि हर चीज में वह आसानी जो आप चाहते हैं काम नहीं करती। दिसंबर महीने के अंदर बैठकर में बारिश की तो ख्वाहिश नहीं कर सकती हूं । मानसून का अपना एक वक्त है प्रकृति ने जो समय निर्धारित किया है उसे हिसाब से ही चीज होगी। मुझे लगता है कि इस वक्त को महत्व और सम्मान देने की जरूरत है जो लोगों ने कुछ कम किया है। और इसी के चलते में बात करूं तो लोगों ने जो नए लेखक हैं वह रिजेक्शंस फेस ही नहीं कर पा रहे हैं और मैं यह कहूंगी कि बहुत बार यह जरूरी हो जाता है कि आपको रिजेक्शन भी मिले यही चीज हमें सिखाती है और साहित्य तो समाज के प्रति अपना एक अलग दायित्व पर अदा करता है और उसके अंदर अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी-जल्दी सब कुछ कर लेना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेखक के रूप में समाज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और यह काम आप जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं। और यही वह चीज है जो आपने कहीं की जो पेशेंस लेवल में गिरावट आई है और इसका जो रीजन है वह कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ही है जिसे काफी ज्यादा लोगों को आलसी बना दिया है वह जल्दी-जल्दी सब कुछ काम करना चाहते हैं मेहनत करेंगे उसमें भी वह यह चाहते हैं कि सिर्फ सफलता हासिल हो रिजेक्शन और दूसरी चीजों पर उनका कभी ध्यान ही नहीं जाता जबकि सफलता हमें सब कुछ नहीं बता सकती हमें हार भी देखनी पड़ेगी रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ेगा। और अगर आज के स्टूडेंट लाइफ को भी अगर हम देखें तो वह भी काफी ज्यादा आसान हुई है सब कुछ आपको फोन पर मिल जाता है ज्यादा मेहनत इसमें भी करने की जरूरत नहीं है अगर मैं अपने ही वक्त की बात करूं तो अगर किसी मुश्किल विषय के ऊपर हमें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो पहले 4 से 5 किताबों को हमें पढ़ना होता था उसके बाद में हम आपस में डिस्कशन करते थे फिर जाकर कहीं हमारी रिपोर्ट तैयार होती और हम उसे सबमिट करने आज अगर आप देखेंगे तो जो टॉपिक आपको चाहिए उसे सिर्फ एक लाइन में लिखने की देर है लिखने की भी नहीं सिर्फ आप उन चीजों को बोल देंगे और आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ जाएगी।
अरमान :- आत्म चिंतन और आत्मा आलोचना को आप किस तरीके से देखते हैं?
उर्ना:- अरमान जी अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं तो बहुत ज्यादा सेफ क्रिटिक हो के जैसे आप कुछ भी लिखें आप उसे बार-बार देखे रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है । अगर मैं इस साक्षात्कार का ही उदाहरण लूं जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो दो महीने बाद भी मेरे दिमाग में यह चीज आनी चाहिए कि मैं किस विषय पर अपनी बात कही थी और वह चीज किस तरीके से प्रभाव डालेगी मुझ पर और जो उसे पढ़ेंगे उन पर तो इस तरह की चीज दिमाग में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कहूंगी की ना सिर्फ जो व्यक्ति लिखता है या साहित्य से जुड़ा है वह हम सभी के लिए यह सब जरूरी है एक आम व्यक्ति एक आम विद्यार्थी भी यह चीज महसूस करे और अपने पिछले किए गए कामों को वह ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। खुद के अंदर झांक कर देखना बहुत बड़ी चीज होती है। मेरी नजर में बहुत ज्यादा जरूरी भी है विकास के लिए। मेरा यह मानना है कि अगर हम दोबारा उस चीज को नहीं देख रहे हैं हम अपने आप में झांक कर नहीं देख रहे हैं तो हमारे किए गए काम जाया चले जाएंगे। अब आप आत्म चिंतन और आत्म आलोचना प्रतिशत के आधार पर देखें तो यह तो व्यक्ति से व्यक्ति पर आधारित है सब में अलग-अलग चीज आपको देखने को मिलेगी हमारी पांचो उंगलियां भी एक सी नहीं होती है। लेकिन काम या ज्यादा की बात नहीं होती होना चाहिए बात असल में यही कही जाए कि इन सब चीजों का मूल्यांकन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और लेखक के रूप में तो यह बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है कि हम क्या लिख रहे हैं । हमारे लिखने का तरीका क्या है हम क्या बोलना चाहते हैं हमारे जो शब्दों का प्रयोग है वह किस तरीके से किया जाए। मैं कहूंगी इन सभी का मिश्रण होकर व्यक्ति को सेल्फ क्रिटिक होना चाहिए। इस चीज से हर चीज में फर्क आपको देखने को मिलेगा एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा नात शरीफ लेखन में बल्कि जो आपसी रिश्ते हैं दोस्ती है वह भी बेहतर होकर सामने नजर आती है।
अरमान :- जब हम लिखते हैं कई चीजों के समाधान देने की भी कोशिश करते हैं और उसमें बहुत सी चीजों का विवरण दिया जाता है लेकिन यह सवाल मैं आपसे यूं पूछूंगा एक ऐसे शख्स के नजरिए से जिसका साहित्य से सीधा कोई रिश्ता ना हो। क्योंकि उपदेश देना काफी आसान हो जाता है क्या लेखक खुद भी उन चीजों को अपने जीवन में उतरता है आप अपने विचारों में इसे कैसे देखते हैं?
उर्ना:- आपके इस सवाल का जवाब मैं दो हिस्सों में देना चाहूंगी। पहली बात तो यही है कि हर व्यक्ति को साहित्य प्रभावित करता है अगर मैं पढ़ भी नहीं सकती हूं लिखना भी मुझे ना आए लेकिन साहित्य मुझ पर प्रभाव डालेगा। जब व्यक्ति पैदा होता है और उसके बाद में जो इसकी शुरुआती ज़रूरतें क्या होती है खाना और सुरक्षा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी मांग किस प्रकार से आपके सामने आती है ,वह कहता है कि मुझे कहानी सुनाओ ,लोरी सुना कर उसे सुलाया जाता है कहानी से उसका मनोरंजन किया जाता है। दुनिया में हर जगह आपको यही चीज देखने को मिलेगी । हर व्यक्ति साहित्य से प्रभावित होता आपको नजर आएगा। उस चीज में आपका साक्षर होना जरूरी नहीं है । अगर मैं अपनी भारतीय संस्कृति की बात करूं तो इतना लिखना भी नहीं होता था लेकिन हम अपनी बातों के माध्यम से और जो कहावत जिसे हम कहते हैं वहां से आपने विचारो को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक पहुंच जाते हैं। इसमें क्या-क्या चीज आ जाती है कि कहानी हम बताएंगे कि उस वक्त किस तरीके से चीजों को इस्तेमाल किया जाता था लोरी जो है वह बहुत सी चीज ऐसी है जो कभी लिखी नहीं गई लेकिन घर परिवार में जो गांव के अंदर है वह बरसों से वैसे ही चली आ रही है। साहित्य इस प्रकार से हर व्यक्ति को प्रभावित करता है यही तो चीज है कि जो छोटा बच्चा है दो साल का, ढाई साल का उसे आप कैसे समझाएंगे कि वह दार्शनिक बातें हैं तो आपकी समझेगा नहीं वह कहानी है काल्पनिक चीजों को आप जब इस्तेमाल करते हैं वह चीज उसे पर ज्यादा प्रभाव डालती है । और वह बेहतर ढंग से उसे चीजों को समझ पाता है तो जब आप खुद से क्रिएशन भी करते हैं तो वह भी कहीं ना कहीं आप पर साहित्य का प्रभाव दर्शाता है। और जब छोटी उम्र से ही वह बच्चा इस तरीके की चीजों में पला ,बड़ा हो रहा है फिर वह बाद में जब खुद समझने जैसा होता है तब वह यह चीज महसूस करता है कि साहित्य क्या चीज है और उसके बाद में वह अपने रुचि के अनुसार उस पर काम भी करता है। यह बात सच भी है कि साहित्य को लोग अलग-अलग नजरियों से देखते हैं । अपनी-अपनी जो सभ्यता है, उनकी जो संस्कृति है उसके माध्यम से जिन चीजों को वह समझते हैं फिर वह साहित्य का दर्पण जब उनके सामने आता है तो वह उसे तरीके से भी चीजों को समझते हैं। जैसा कि मैं भारतीय संस्कृति की बात की तो यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी संस्कृति इतनी ज्यादा खूबसूरत है और जो मौखिक रूप से साहित्य को शुरुआत से समझ रहे हैं अगर आप गांव की बात करें या फिर जो इतना सिर्फ गांव की अगर हम बुजुर्गों के पास में बैठते हैं तो वह हमें पुरानी पुरानी कहानी सुनाते हैं जो हमने कभी-कभी लिखी हुई नहीं देखी है हमने कभी उन्हें पढ़ा नहीं है लेकिन हमने उनसे वह चीज सुनते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इसे कहीं पढ़ा है या अपने इन्हें कहां से सुना तो वह कहते हैं कि यह तो हमें हमारे पिताजी ने हमारी दादी जी ने हमें यह सुनाया करते थे । तो यह जो चीज चलती आ रही है यही तो प्रभाव है साहित्य का। जैसा कि मैंने कहा कि इसके दूसरे भाग की में बात करो अपने सवाल की तो आपने जो सवाल किया था वह काफी जटिल है लेखक के सजेशन के ऊपर क्या वह खुद भी अपने जीवन में उसे उतारता है। इसके जवाब में मैं यह कह सकती हूं की सबसे पहले तो कि हमारे सामने बहुत सारी लेयर्स कहीं बार आ जाती है और लेखक जब अपने अवेयरनेस के हिसाब से किसी भी सवाल का हो या परेशानी का जवाब या सलाह मशवरा देने की कोशिश करता है तो यह भी चीज उसके ऊपर प्रभावी रूप से हमें देखने को नजर आती है। लेखक कोई भी बात जब करता है फिर चाहे वह कहीं अपने काव्य पाठ में बात कर रहा हो या फिर लेखनी के अंदर वह अपनी जागरूकता के अनुसार बात करने की कोशिश करता है यानी कि जो चीज उसने अपने आसपास महसूस की है वह उन्हीं को अपने रिफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करता है। और हम यह भी जानते हैं और समझते हैं कि जिस लेखक को हम पढ़ रहे हैं वह वास्तविक जीवन में खुद कैसा है इसे हम नहीं जानते एक पाठक अपने लेखक को उसकी लेखनी से ही पहचानता है।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार ।
उर्ना बोस - आपका भी बहुत बहुत आभार ।
Vandana Yadav
वन्दना यादव 
पांच विषयों में एम ए मां और सात विषयों में एम ए पिता की बेटी होने पर अत्यंत गर्व है । - वंदना यादव
सुप्रसिद्ध साहित्यकार, मोटिवेशनल स्पीकर और समाज सेविका वन्दना यादव से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
परिचय : वन्दना यादव
लेखिका, मोटिवेशनल स्पीकर और समाज सेविका वन्दना यादव का जन्म 1 जुलाई 1972 को बीकानेर,राजस्थान में हुआ। मूलत: महेंद्रगढ़, हरियाणा की रहने वाली वन्दना यादव का वर्तमान निवास स्थान दिल्ली है।
वन्दना यादव का सैनिकों की पत्नियों पर लिखित ‘ कितने मोर्चे’ उपन्यास, “सेपरेट फैमिली क्वाटर्स” पर अब तक का पहला हिन्दी उपन्यास है। इसके अतिरिक्त लेखिका का भारतीय संस्कृति को समर्पित ‘शुद्धि’ उपन्यास, भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है।
‘अब मंजिल मेरी है’ मोटिवेशनल पुस्तक के लिए भारतीय सेना के प्रथम “सीडीएस” ‘जनरल विपिन रावत’ ने शुभकामनाएं दी थीं।
सैनिक की पत्नी के दृष्टिकोण से लिखा यात्रा-वृतांत ‘सिक्किम: स्वर्ग एक और भी है।‘ के अतिरिक्त बाल साहित्य में भी वन्दना यादव ने काम किया है।
‘सब्जियों वाले गमले’ (बाल कहानी की पुस्तक) को नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया (NBT) ने प्रकाशित किया है। यह पुस्तक एन बीटी की बेस्ट सेलर बुक्स की लिस्ट में शामिल है। इस पुस्तक की अब तक चार लाख से अधिक प्रतियां पाठकों द्वारा ख़रीदी जा चुकी हैं। अनेक राज्यों के सरकारी शिक्षण प्रोजेक्ट्स में इसे लिया जा रहा है। उड़िया भाषा में इसका अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है तथा अनेक राज्यों की बुलबुल प्रोजेक्ट में पुस्तक को शामिल किया गया है।
साहित्यकार वन्दना यादव के ‘कुछ कह देते’ कविता संग्रह को हरियाणा साहित्य अकादमी, अनुदान योजना के तहत प्रकाशित किया गया है।इसके अतिरिक्त वन्दना की अलग-अलग विधाओं में पन्द्रह पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आपने आधा दर्जन से अधिक पुस्तकों का संपादन भी किया है। आकाशवाणी पर रचना पाठ एवं समाचार -पत्र , पत्रिकाओं में मानसिक स्वास्थ्य , महिला अधिकारों और अन्य सम सामयिक विषयों पर वन्दना लगातार लिखती हैं। लंदन से ऑनलाइन प्रकाशित होने वाली पत्रिका “पुरवाई” में एक वर्ष से अधिक समय तक “मन के दस्तावेज़”कॉलम प्रकाशित हुआ है।
अरमान:- आपका एकेडमिक्स कैरियर बेहद शानदार है और आज के वक्त में आप वंदना यादव साहित्य समाज में एक जाना पहचाना नाम है । मैं यह जानना चाहूंगा कि आपकी साहित्य में रुचि किस तरह हुई ?
वंदना यादव: - मेरे माता-पिता दोनों ही हाईली एजुकेटेड थे. मेरी माता जी बीकानेर से है। और मेरे नाना जी के चाय के बागान थे। और मेरी नानी जी का मानना था की लड़कियां सिर्फ चूल्हे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए और इसी का नतीजा था कि मेरे माता-पिता ने भी मुझे और मेरी बहन को खूब पढ़ाया। मेरे पिताजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हैं और हम गांव में रहते थे वह हरियाणा का इतना पिछड़ा हुआ इलाका था। आप यह सोचिए कि जब 93 में मेरी शादी हुई थी जब तक हमारे गांव में पानी नहीं आता था । हम पानी खींच के लाया करते थे कुएं से। मेरा बचपन इस तरह निकला कि राजस्थान के सीमावर्ती गांव भी देखें और दोनों संस्कृतियों को काफी नजदीक से देखा। और मैं यह कह सकती हूं भले से माता-पिता दोनों अलग-अलग संस्कृति से थे लेकिन वह दोनों पढ़े लिखे थे। मेरी माता जी ने पांच सब्जेक्ट में एम ए किया है और अपनी जनरेशन की हाईली क्वालिफाइड लेडी है वे। और मेरे पिता ने भी सात सब्जेक्ट में एम ए किया हुआ है। और टेलीविजन तो हमारे घर के अंदर बहुत बाद में आया हमारे घर में उसकी बजाय लाइब्रेरी थी। और इस तरह की दिनचर्या थी कि अगर आप खाली बैठे हैं तो आपको पढ़ना है। और अखबार में भी वह कहते थे कि आप संपादकीय आलेख पढ़िए। और लाइब्रेरी में अलग-अलग तरह की किताबें थी । साहित्य को समझने वाला वह माहौल था जहां मैंने अपनी समझ के साथियों से पहले प्रेमचंद को ,महादेवी वर्मा को , रविंद्र नाथ टैगोर को पढ़ लिया था। उसे वक्त इतना समझ नहीं आता था लेकिन फिर भी उनकी लिखी हुई रचनाओं को मैंने पढ़ा। और क्योंकि घर से यही सीख थी कि तुम पढ़ लो बाकी बातें खुद ब खुद समझ आने लग जाएगी।
अरमान :- आपने काफी काम मोटिवेशन पर कर रखा है और सवाल ये है की परेशानियां लोगों की एक सी हो सकती है लेकिन उनके समाधान जरूरी नहीं की एक ही हो ऐसी कौन से की - पॉइंट्स है जो सभी स्वीकार कर सकते हैं?
वंदना:- सबसे पहली बात तो यह की सफलता के मायने सभी के लिए अलग है। कुछ साल पहले खबर आई थी कि महिला मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना चाहती है साथ ही खबर यूं भी आई की महिला दरगाह जाना की इच्छा रखती है उनके लिए सफलता हो सकती है। वह जो प्रतिबंध उन पर लगे हैं उन्हें लांघना उनके लिए सफलता हो सकती है। बच्चों के लिए सफलता हो सकती है कि मैं अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आऊं या फिर अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। एक ग्रहणी के लिए सफलता यह हो सकती है कि मैं इतना अच्छा भोजन बनाऊं और सेवा अपने परिवार की यूं करूं कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। हर एक के लिए सफलता के मायने अलग हैं। मेरे लिए सफलता के मायने अलग हो सकते हैं मैं काफी फ्रंट पर काम करती हूं अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं तो मान कर चलिए कि वह बच्चा जो घोर निराशा से गुजर रहा है उसे मैं कुछ उजाले की किरण दूं मेरे लिए वह सफलता है। एक जो अपने सबसे बड़ी बात यह पूछी कि ऐसी कौन सी बात है जो सभी के लिए कहती हूं मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि हर एक तस्वीर के दो पहलू होते हैं और आप पहले पकड़ लीजिए पहले सकारात्मक है। ओवरथिंक करके जरूर से ज्यादा उसे चीज को सोचते रहेंगे तो उसके बहुत से डाइमेंशन निकलेंगे। बहुत आसानी से नकारात्मक हो सकते हैं बीते हुए कल में जो भी खराब अनुभव रहे उन्हें आप छोड़ दीजिए उन्हें आप मत पकड़ के रखिए। सकारात्मक वातावरण को पकड़ के रखिए आपका पूरा आभामंडल परिवर्तित हो जाएगा। इस बात से सहमत होते हैं सभी लोग।
अरमान :- और अगर हम युवाओं की परेशानियों का आकलन करते हैं तो मैं फिर कहूंगा कि सबकी अलग-अलग परेशानियां हो सकती और आपने भी कहा कि सफलता के मायने सबके अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन एक चीज उभर कर सामने आती है वह अवसाद की समस्या है खासकर की युवा वर्ग में। यह समस्या आपकी मोटिवेशनल स्पीच में और लेखन में कितनी जगह और महत्व रखती है?
वंदना:- अवसाद आज की युवाओं को और महिलाओं को तो सदियों से है क्योंकि उन्हें तो एक लंबे वक्त से एक सिर्फ घेरे में बंद कर रख दिया गया था। एक बात है कि जब तक आप किसी को कुछ करने के लिए विवश नहीं करेंगे जब तक व्यक्ति अपने मन का कर रहा है वह अवसाद में नहीं आएगा लेकिन जब एक अलग तरह का प्रेशर रहता है फिर मान के चलिए पेरेंट्स की तरफ से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वह जो नहीं बन पाए वह अपनी औलाद को बनाना चाहते हैं। अगर आप भी यह मानते हैं कि एक इंसान के रूप में हम अलग पैदा हुए हैं हर एक व्यक्ति का जन्म अलग हुआ है और उसकी मृत्यु भी अलग से होगी और जब वह अलग ही पैदा हुआ है तो आप उसे अपनी कार्बन कॉपी क्यों बनना चाहते हैं। यह अपनी अपेक्षाओं की तस्वीर उसमें क्यों देखना चाहते हैं। जो बच्चा बनना चाहता है या उसमें जो क्वालिटीज हैं उसे पर आप उसे काम क्यों नहीं करने देते । इंप्रूव करने में उसका सहयोग कीजिए ना। जैसा कि आपको बताया कि मैं हरियाणा और राजस्थान की साझा संस्कृति को समझती हूं और उसमें पली बढ़ी हूं और वह इतना प्रगतिशील क्षेत्र नहीं था। और मेरी मम्मी को उस वक्त महसूस हुआ कि हम दोनों बहनों को कत्थक मैं कुछ दिलचस्पी है। उसमें उन्होंने हमें सहयोग दिया और मैंने कत्थक सीखा और मैंने स्टेज परफॉर्मेंस भी दे रखी है। और उसके बाद घर में प्रैक्टिस चलती रही लेकिन जब शादी हुई और एक फौजी के घर में मेरा जाना हुआ तो वहां मैं उसे जारी नहीं रख पाई। कहने का मतलब यह है कि यह पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वह अपने बच्चों को समझें और उनके जो पसंद ना पसंद है उन पर ध्यान देते हुए उनका आकलन करें और एक ऐसा वातावरण बनाएं के बच्चे खुलकर अपनी बात कह सके और अपने इच्छा के अनुसार वर्ग चुन सके। अवसाद एक गंभीर समस्या है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता और अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण लगता है कि मुझ में है मेरे दोस्त में है मेरे बेटे में है या मेरे मां-बाप में है तो इस पर बात करनी चाहिए यह कोई शर्म की बात नहीं है। कोई भी हमारे शरीर में समस्या होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसका इलाज हो जाता है यह आप इस तरह लीजिए। मैं कहना चाहूंगी कि यह टैबू नहीं है इसे पागलपन से जोड़ना सही नहीं है यह बीमारी है जिसका इलाज संभव है। हम लोग प्रकृति की देन है प्रकृति के साथ समय बताइए पेड़ पौधों के साथ समय बताइए जब यह महसूस होकर कोई काम नहीं है आपके पास तो आधा घंटा शांत मन के साथ में प्रकृति में बिताए।
अरमान :- आपने बहुत अच्छी बात कही कि यह एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अवसाद आखिर में होता क्या है?
वंदना:- क्योंकि अगर हम इसमें कुछ लक्षणों की बात करें जो सामान्यत सभी में आपको महसूस होंगे कि कुछ करने का मन नहीं करना और विटामिन की जिस तरीके से इसमें कमी आती है वह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है जिसमें तुरंत मेडिकल जांच करवानी भी आवश्यक होती है । इसमें मेडिकल का भी एक बड़ा रोल है। अगर हम बच्चों के लिए बात करें तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर माता-पिता में कुछ कह दिया तो उसके मूड खराब होने से वह डिप्रेशन हो गई। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और उसे अवसाद नाम दे दिया जाए तो यह सब भी नहीं होना चाहिए इस पर अध्ययन की जरूरत है और हर एक को इसे समझने की भी आवश्यकता है। मूड स्विंग्स को अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन समझता है तो यह भी एक परेशानी की बात है। और इस पर काम करने की भी जरूरत महसूस होती है। मैं अपनी बात एक बार फिर दोहराते हुए कहूंगी कि यह बीमारी है लेकिन इतनी भयंकर बीमारी नहीं की जिसका इलाज संभव नहीं। मैं आपको कह सकती हूं कि क्योंकि मैं कथाकार हूं लेखक हूं मैंने सेना परिवेश में बहुत काम किया मैं टीचर भी रही हूं और स्कूलों में भी पढ़ाया है ,आर्मी की इंस्टीट्यूशंस है और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम महिलाओं की तरक्की पर भी काम करते हैं तो यह सब चीज लगातार हमारे सामने आती भी है। वहां अलग-अलग समस्याएं भी हमारे सामने आती है पहले में काउंसलर से खुद जाकर बात किया करती थी किस तरह की परेशानी है हम पहले अपॉइंटमेंट लिया करते थे फिर उन महिलाओं को उनके पास में भेजा करते हैं कहीं बार उन महिलाओं के साथ उनके परिवार भी जाया करता था और कई बार अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई केस है कि परिवार की वजह से ऐसा हो रहा है और उसमें मैं खुद भी साथ उनके जाया करती। यह चीज डॉक्टर भी साफ करते हैं कि मूड खराब हो जाना मूड स्विंग्स होना अलग बात है और डिप्रेशन बिल्कुल ही एक अलग चीज।
अरमान :- एक चीज आपने यह भी कहीं की काफी समस्याओं की वजह ओवरथिंक करना भी हो सकता है आज का जो परिवेश है इसकी आपको वजह क्या नजर आती है क्योंकि अगर हम पहले के लेखन भी देखें तो उनमें इन चीजों का जिक्र इतना नहीं किया जाता था? 1920 से लेकर 1980 के लेखन को अगर हम ध्यान से देखें बात सीधे स्पष्ट रूप से बताई और समझाई जाती थी ।
वंदना यादव :- इस सवाल का जवाब में अपने जीवन के अनुभव से दूंगी जैसा कि आपको बताया कि मैं अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग क्षेत्र के लोगों से, वर्ग के लोगों से लगातार संवाद करती हूं और उससे मुझे इस मुद्दे पर एक ही बात समझ आती है कि अकेलापन है मुझे लगता है कि अकेलेपन की वजह से ही हम ओवरथिंक करते हैं ज्यादा चीजों को सोचते हैं उसको बार-बार अपने ध्यान में घूमते हैं हम बहुत ज्यादा एंबिशियस भी हो गए हैं। ओवरथिंक कहां से शुरू होती है गहन चिंतन तो ठीक है लेकिन बेवजह की चीजों के ऊपर अपना दिमाग लगाना और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना वह ओवरथिंक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे पानी के डेम के पास में काफी कचरा धीरे-धीरे जमने लगता है क्योंकि उस बांध के बाहर जो पानी गिर रहा है वह एक दीवार के पास में बह रहा है और जो पानी गिरेगा इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो जो पत्ते हैं जो लकड़ी है और जो अनावश्यक दूसरी कोई चीज हैं वह धीरे-धीरे वही एकत्रित होने लग जाती है अगर हम इसे इकट्ठा करते रहेंगे तो पूरा का पूरा जो बांध क्षेत्र है वह इन्हीं सबसे भर जाएगा और इसी वजह से वहां लगातार सफाई होती रहती है बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है उस कचरे को हटाने के लिए यही असल में हमारे अगर संदर्भ में बात करूं तो ओवरथिंक है बेवजह की चीजों के ऊपर अपना वक्त अगर हम जाया करते हैं और उन्हें बार-बार घूमते रहते हैं अपने दिमाग में तो उसी से वह ओवरथिंक होता है और हमारी उर्जा भी व्यर्थ होती है। हम सभी मनुष्यों को एक निर्धारित समय मिला है इस दुनिया पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए और उससे मुझे लगता है इन सब चीजों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए इतना सब कुछ सुंदर हमारे आसपास होता है हमें उन पर ध्यान देना चाहिए चिंतन होना चाहिए विचार करना चाहिए चीजों पर गहन चिंतन होना चाहिए लेकिन इन सब अनावश्यक चीजों पर ओवर थिंक करना बिल्कुल सही नहीं है। और एक की भी चीज में कहना चाहूंगी कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो व्यक्ति कभी अकेला रही नहीं सकता था कोई ना कोई घर का बड़ा छोटा उसके साथ में होता था सब एक दूसरे की समस्याओं को सुना करते थे समझा करते थे तो वह जो अकेलापन जो सबसे बड़ी समस्या बनकर आज हमारे समक्ष आ रहा है। वह तो पहले कभी था ही नहीं। मान के चलिए कि अगर कोई खाली भी बैठा है तो उसे काम दिया जाता था संवाद होता था। आज अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली है और भी अगर हमेशा आगे बढ़कर बात करें तो जो युवा है नौकरी के लिए अकेले रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जिंदगी में किसी और का दखल तब तक नहीं है जब तक आप नहीं चाहेंगे। अगर ऐसी स्थिति में आप नकारात्मक विचारों से घिर गए मेरा यकीन मानिए जब तक आप मदद नहीं मांगेंगे तब तक तो उसमें आपका जो प्राइवेट एरिया है उसमें कोई घुस नहीं सकता लेकिन ऐसा संयुक्त परिवारों में नहीं होता था। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो मैं आपको इस पर कहना चाहूंगी कि मैं फोन तब उठाती हूं जब मुझे लगता है कि उसे अटेंड करना चाहिए क्योंकि फोन मेरे लिए है मैं फोन के लिए नहीं हूं । हर उस व्यक्ति को समझना है कि मैं किसके लिए हूं और कौन मेरे लिए है। देखिए आप परिवार के लिए हैं रिश्ते आपके लिए हैं भाई बंधु सब आपके लिए हैं और आप उनके लिए सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक इस फेहरिस्त में नहीं आते कि आप अपना पूरा जीवन उन पर व्यतीत कर दें उनका निर्माण इसलिए नहीं किया गया। अगर आज हम बात करें तो मैं देखती हूं कि जब हम कहीं जाते हैं ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो ,बस अड्डे हो वहां पर सभी लोग अपने फोन निकाल लेते हैं , ईयरफोन लगाकर गेम्स खेलते हैं लेकिन कोई आपस में संवाद नहीं करता। यानी कि एक तो हो जाता है कि हम जब मिलते हैं या अपनी सीट के पास वाले व्यक्ति से बात करते हैं हो सकता है कि लोग इतने खुले ना हो लेकिन अपने साथ वालों से भी वह बात नहीं करते वह फोन चलाते हैं।
अरमान नदीम :- आपकी एक किताब है कितने मोर्चे शीर्षक उसका काफी शानदार है और सवाल भी एक बनता है कि एक लेखक अपने आप को कितने मोर्चों पर खड़ा पाता है ?
वंदना यादव:- सैनिक जितने भी हैं वह बॉर्डर्स पर हैं उनके पास एक मोर्चा है कि कोई आतंकवादी कोई विदेशी सरहद पार करके हमारे देश में ना घुस जाए । वहां वो उस मोर्चे पर हमारी सुरक्षा करते हैं और जो सैनिक वहां बॉर्डर पर रहते हैं उनकी पत्नियों जब यहां सिविल में रहती हैं उनके समक्ष अनेक मोर्चे रहते हैं और यह किताब भी नॉवेल मैं इसी थीम को लेकर लिखा था कि उस महिला के मोर्चे क्या है कि बच्चों को पढ़ाना है, घर का काम करना है, मां-बाप की सास ससुर की सेवा करनी है, और अपना खुद का ध्यान रखना है और वहां उसे बॉर्डर पर खड़े पति को यह बात नहीं बतानी है कि हमें यहां किस तरह की परेशानी हो रही है या हम किन समस्याओं को अपने सामने खड़ा पाते हैं । क्योंकि जब उस सैनिक को अपने घर की परेशानियों सुननी को मिलती है तो वह वहां खड़ा अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता। और यही जो शीर्षक है कितने मोर्चे मैं आपका सवाल भी समझती हूं और यही रेखांकित करते हैं कि एक लेखक के कितने मोर्चे हैं। और मैंने कहा कि बहुत रिसर्च के बाद किताब लिखी जाती है । मैं इतिहास की छात्रा रही हूं , पॉलिटिक्स पढ़ी है ,हिंदी मेरा विषय रहा है लेकिन उसके बाद भी जब मुझे कुछ पढ़ना होता है या कुछ लिखना होता है तो मैं उसके पीछे बहुत रिसर्च करती हूं क्योंकि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी किताब में जानी नहीं चाहिए । क्योंकि जो व्यक्तिगत जीवन में मैं क्या करती हूं वह मेरे शौक हो सकते हैं या जो मैं नहीं कर पा रही हूं वह मेरी मजबूरी हो सकती है जिसे मैं पसंद करती हूं उसमें मेरी रुचि हो सकती है परंतु अगर मैं किताब लिख रही हूं तो मेरी यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो उस किताब को खरीदेगा तो वह पैसा देगा कि अगर किसी की मेहनत का पैसा मेरी किताब लग रहा है तो यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सार्थकता होनी चाहिए । और दूसरी बात यह कि वह उसे पढ़ेगा या नहीं वह अपना उस पर वक्त देगा हम कहते ही हैं कि समय से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं है और सबसे ज्यादा जरूरी के वह अपना समय दे रहा है अपना पैसा दे रहा है उसे पर अपनी उर्जा दे रहा है और पढ़ने के बाद में उस पर वह अपना चिंतन करेगा कि लेखक ने यह क्या लिखा है क्यों लिखा है। वह अपने जीवन से लेखनी की तुलना करेगा अगर कोई व्यक्ति इतनी सारी चीज आपकी पुस्तक पर खर्च कर रहा है तो आपकी पुस्तक अनेक मोर्चा पर खड़ी होनी चाहिए। फिर चाहे वह रिसर्च के लेवल पर हो या वैचारिक स्तर पर हो।
अरमान :- किसी भी रचना का पहला आवरण उसका शीर्षक होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि शीर्षक पढ़ लेने से ही रचना समझ आ जाती है साथ ही लेखक के भी मन में यह रहता है कि मैं अपने शीर्षक को इस तरह रखूं कि वह पाठक के दिल दिमाग पर छा जाए आपकी एक किताब है जिसका शीर्षक है "आई डोंट लाइक यू" मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा ,मैंने इसका इंडेक्स देखा लेकिन यह जो शीर्षक है यह क्या वजह लेकर चलता है इसके बारे में आप बताइए?
वंदना यादव:- बहुत ही अच्छा सवाल है यह आपका और मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस चीज के ऊपर एक ऑनलाइन चर्चा भी हुई थी और काफी अच्छा लग रहा है मुझे इस पर बात करते हुए क्योंकि जैसे ही यह किताब आई और जब यह शीर्षक सबके सामने रखा गया तब मेरी सहेली का एक मैसेज आया तो उसने लिखा सुनो आई लाइक यू उस चीज को देखकर हम काफी देर तक हंसते रहे क्योंकि वह जानती थी कि इसका शीर्षक ऐसा क्यों रखा गया है किताब का और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका शीर्षक कैसा क्यों है । इस किताब में मैंने अपना जीवन लिखा है मैंने तीन तरह का जीवन जिया है। एक जो हरियाणा का बहुत पिछड़े गांव से मैंने वह जीवन जिया उसके बाद में सीमावर्ती गांव हैं वहां मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। और मम्मी चूरू में नौकरी किया करते थे तो वह एक शहरी जीवन भी देखा और इन सब अनुभव को मैंने इस किताब में लिखने की कोशिश की ।और एक ऐसा बच्चा मेरी शादी के कई सालों बाद मेरे जन्म में आया जब मेरी बेटियां शिखा और शिवानी हॉस्टल में थी। उस वक्त में मैं और मेरे पति काफी खाली महसूस किया करते थे । हमारे पड़ोस में एक बच्चा आया जिसकी मां ब्रिटिश नागरिक हैं और उसके पिता भारतीय सेवा के अधिकारी तो वह बच्चा बड़ी ही सहजता के साथ में इंग्लिश बोला करता था की इतनी सहजता से जितनी सहजता से हम सोच भी नहीं सकते कि भारतीय मूल का बच्चा अंग्रेजी बोलता हो। बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग था क्योंकि घर में मम्मी पापा डांटा करते थे । बच्चा अपनी एनर्जी मांग रहा था और हम दोनों इतने खाली थे कि हमें उस बच्चे का होना अच्छा लगता था । हमारे घर इस लालच में आता था कि हम उसे हाथों हाथ रखते हैं । खाने का बड़ा चोर था खाना नहीं खाता था तब उसकी मम्मी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसे खाना खिला दिया करूं और जब मैं उसे कहती थी की दही खा लो और जब मैं उसके पीछे भागती थी कि तुम्हें खाना पड़ेगा तब वह मुझे कहता था "आई डोंट लाइक यू" उसके मन में यह रहता था कि दो-तीन घटे जो यहां उसे बिताने के लिए मिल रहे हैं खाना खाने में वह वक्त खराब हो जाएगा। एक बार मेरे हस्बैंड कर्नल साहब ने यह सुन लिया तो उन्होंने उससे पूछा अंग्रेजी में व्हाट हैपेंड वह कहता है यू नो शी does not like me यानी कि कुछ देर पहले उसने मुझे कहा था आई डोंट लाइक यू और जब हस्बैंड साहब ने उससे बात की तो बात ही पलट दी। एक कमाल का ही कांबिनेशन था कि जब कोई और उससे पूछता था तो वह उन्हें कहता था मुझे पर्सनली कहता था कि आई डोंट लाइक यू। तब किताब बन रही थी तो इससे मासूम शीर्षक कोई हो ही नहीं सकता था।
अरमान नदीम - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने हेतु आपका बहुत आभार ।
वन्दना यादव - धन्यवाद
Chintan Upadhayay 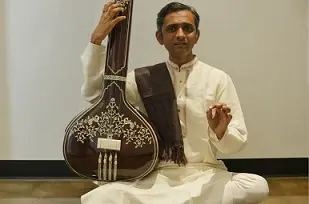
चिंतन उपाध्याय
गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित भारत के सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक चिंतन उपाध्याय जी से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते , हम सिर्फ उनसे सीखते हैं - चिंतन उपाध्याय
परिचय
श्री चिंतन उपाध्याय
जन्म गुजरात के भावनगर शहर के सांस्कृतिक माहौल में हुआ था। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने माता-पिता से मिली, जो संगीत के विद्वान शिक्षक थे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के एक प्रसिद्ध शिष्य स्वर्गीय श्री लक्ष्मी पति शुक्ला जी और भावनगर में स्वर्गीय पंडित रसिकलाल अंधारिया के शिष्य श्री अश्विन अंधारिया से प्रशिक्षण प्राप्त किया।
यह यात्रा तब शुरू हुई, जब चिंतन जी ने बृहद गुजरात संगीत समिति द्वारा आयोजित संगीत अलंकार परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और संगीत में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए ललित कला केंद्र, पुणे विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और भारत सरकार से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त की; पुणे के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक डॉ. विकास कशालकर और पंडित विजय कोपरकर के मार्गदर्शन में पाठ्यक्रम पूरा किया। । 2013 में आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी-कोलकाता में शिक्षक बन गए और पंडित उदय भवालकरजी से अपनी तालीम हासिल की। चिंतन जी को 2014 में ध्रुपद अध्ययन के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। उन्हें ध्रुपद गायक के रूप में आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा 'बी हाई ग्रेड' आवंटित किया गया है। चिंतन जी को सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए "युवा गौरव पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है। उन्होंने पारंपरिक ध्रुपद प्रारूप को बदले बिना कला के कई रूपों के साथ प्रयोग किया है और अपने अनुभव की सीमाओं को समृद्ध किया है। इन प्रदर्शनों में ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, आधुनिक नृत्य, थिएटर शो और कई पश्चिमी संगीतकारों के साथ संगीत का आदान-प्रदान जैसे नृत्य शामिल हैं। कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए ध्रुपद गाया है और यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म “पृथ्वीराज चौहान” में भी, एक दरबारी संगीतकार के रूप में काम किया हैं। भारत में आपने एनसीपीए-मुंबई में ‘प्रोमिसिंग आर्ट’ श्रृंखला के लिए, रजा फाउंडेशन दिल्ली के लिए “आराधिका” राष्ट्रीय सम्मेलन स्पिकमैक सूरत के लिए, दादर माटुंगा सांस्कृतिक केंद्र-मुंबई, आईसीसीआर ‘क्षितिज श्रृंखला’ के लिए, बाजा गाजा 2012-पुणे, स्वर्गीय उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब की याद में ‘बरसी’, होशियारपुर, पंजाब में उस्ताद अल्लारखा संगीत सम्मेलन, वाई.बी. 'रंग स्वर' के लिए चौहान हॉल, काला तट संगीत फ़ेस वैल उडुपी, गुजरात राज्य संगीत नाटक द्वारा 'आदित्यराम जी शास्त्री संगीत महोत्सव' अकादमी, जूनागढ़ में, देवनंदन उभेकर फेस वैल बैंगलोर,
वीणा फाउंडेशन और गंधर्व महाविद्यालय के लिए युवा ध्रुपद फेस वल, पुणे, उपनगरीय संगीत मंडल - मुंबई, में अपनी कला का प्रदर्शन किया है ।
स्वामी विवेकानन्द जी के जन्म स्थान एवं निवास स्थान कोलकाता में, श्री आनंद मयी माँ आश्रम-कोलकाता, मल्हार फ़ेस वल पुणे, घराना सम्मेलन नालासोपारा, मुंबई,
काला तट संगीत उत्सव 2015, उडुपी,
लातूर, तालेगांव, अहमदनगर, नैनीताल, धारवाड़, द्वारका, वडोदरा आदि। चिंतन जी पिछले कुछ समय में कनाडा, अमेरिका, यूके, जर्मनी, वियना में कॉन्सर्ट किए हैं
वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर पढ़ाया और कार्यशालाएँ आयोजित कीं जिनमें से कुछ प्रमुख थी: मल्हार ग्रुप - टोरंटो, शिवानंद सेंटर - वालमोरिन और मॉन्ट्रियल, कनाडा, द लाहासिंडा क्रिएव स्टूडियो - मॉन्ट्रियल, स्वरसाधना - टोरंटो, 'धारणा' बर्लिन - जर्मनी, 'अलंकार संगीत सोसायटी' - वियना, पुर योग - ड्रमंडविले, - कनाडा सितार संगीत सोसायटी - लीसेस्टर - यूके, कॉथम चर्च, ब्रिस्टल, - यूके, ध्रुपद संगीत सोसायटी - ओकलैंड्स कॉलेज - लंदन, द एपरी स्टूडियो - लंदन, आदि। चिंतन जी ने प्राचीन संगीत को सिखाने के लिए "एलेम्बिक ध्रुपद फाउंडेशन" के बैनर तले वडोदरा में ध्रुपद संगीत के लिए एक नया केंद्र शुरू किया है। चिंतन जी पंडित उदय भवालकरजी के मार्गदर्शन में बंगाल परम्परा संगीतालय, ढाका, बांग्लादेश में जूनियर गुरु - ट्यूटर के रूप में भी पढ़ा रहे थे। चिंतन कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, वियना, जर्मनी, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, कतर, ढाका आदि देशों के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से पढ़ाते रहे हैं। चिंतन जी ने भारत में विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं भी आयोजित कीं, जिनमें शामिल हैं: ‘महागामी’ नृत्य गुरुकुल - औरंगाबाद, हार्मनी स्कूल ऑफ म्यूजिक - मुंबई, एफटीआई - फिल्म और टेलीविजन संस्थान - पुणे, सूरत में राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए गहन कार्यशाला उत्कृष्टता केंद्र - भावनगर, गुजरात, एम.एस. विश्वविद्यालय, संगीत विभाग, वडोदरा, वल्लभ विद्या नगर, गुजरात।
अरमान :- संगीत के प्रति आपका प्रेम और लगाव किसी से छुपा नहीं है लेकिन शुरुआती दिनों में आपने इसे कैसे शुरू किया इसके बारे में आप बताइए
चिंतन:- सबसे पहले तो नमस्कार अरमान जी और अगर मैं अपने शुरुआती दिनों की बात करूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि मैंने जो कुछ भी सीखा है अपने जीवन में वह गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखा है और अगर मैं गुरु की बात करूं तो वह एक बहुत ही महान इंसान होता है जीवन में अगर आप समंदर से एक बाल्टी पानी लेते हैं तो आप वापस समंदर को क्या दे सकते हैं। हम गुरु को कुछ दे नहीं सकते सिर्फ उनसे सीख सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं अपने जरिए लोगों तक कोई संदेश पहुंचा सकूं तो वह भी मेरी गुरु सेवा है। और मैं फिर अपने अगर शुरुआती दिनों की बात कहूं तो मेरा जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ। भावनगर के राज्य चित्रकार श्री सोमालाल जी के घर जो उनकी तपोभूमि थी वहां मेरा जन्म हुआ। और मेरे पिताजी भी साहित्यकार संगीतकार चित्रकार और फिलॉस्फर हैं उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला और इसी वजह से मुझे घर में बचपन से ही यह सब संस्कार मिले थे। और जब मैं छोटा था तो घर में संगीत की कक्षाएं चलती थी तो बचपन से ही में इन सब चीजों के परिवेश में पला और बड़ा हुआ। मेरे पिताजी के जो गुरुजी थे उनका नाम पंडित लक्ष्मण पति शुक्ला जी जो की पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य थे। पिताजी सुनने के काफी शौकीन थे तो उस वजह से मुझे बचपन से ही बड़े गुलाम अली खां साहब, आमिर खां साहब, पंडित ओमकानंद ठाकुर जी जैसे बड़े-बड़े कलाकारों को सुनने का मौका मिला । बड़े-बड़े विद्वानों से सीखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ।
अरमान :- जिन महान कलाकारों के अपने नाम लिए और जो वातावरण आपने बताया वह वाकई काफी सुखद और सुंदर है और मैं आपसे यह जानना चाहूंगा जब आपने इन सब से सीखा और प्रस्तुति देनी शुरू की तो क्या आपके मन में ऐसी चीज रहती है कि किसी तरह का कोई संदेश अपनी प्रस्तुति में अपने श्रोताओं को दूं?
चिंतन:- बिल्कुल बिल्कुल यह विचार मेरे मन में पिछले काफी वर्षों से है जो अपने सवाल किया और जो "ख्याल" है मैं उसे काफी वक्त से सीख रहा हूं। यूथ फेस्टिवल के दौरान में बाहर जाया करता था जैसे गोवा, नागपुर, ग्वालियर, जयपुर , पुणे जाने का सौभाग्य मिला जहा पर मेरे गुरुजी पंडित उदय भावल्कर जी जमाने के बहुत बड़े ध्रुपद गायक है , विद्वान है और गुरु शिष्य परंपरा में उनके घर पर मैं आठ साल तक रहा। उनसे सीखते हुए मुझे आज 22 साल हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ़ पुणे में ललित कला केंद्र वहां एडमिशन हुआ था । ख्याल संगीत में मैं वहां से मास्टर्स हूं । और इसी कालखंड में सिखाते सिखाते ध्रुपद से इतना मोह हो गया कि मैंने निश्चय किया । मुझे याद है कि जब मैं 22 साल का था। जिससे मैं बचपन से गा रहा था और थोड़ा कंफर्टेबल था गाने के अंदर ख्याल गायन और उसके बाद में मैंने यह फैसला किया कि जीवन में कुछ भी हो जाए मैं ध्रुपद नहीं छोडूंगा और इसे गाऊंगा। और जैसा कि आपका सवाल था की प्रस्तुति के दौरान संदेश का तो यह विचार मुझे आया कि जब कलाकार अपने कला की प्रस्तुति मंच पर देता है । संदेश के बारे में मुझे कभी-कभी लगता है कि ईमानदारी रखनी चाहिए । जाने अनजाने में कलाकार कुछ ऐसे संदेश दे देता है जिसे सुनने वालों की बेचैनी बढ़ जाती है लेकिन होना ऐसा चाहिए कि यह तो कला जगत है बहुत ही खुला मैदान है तो कह तो नहीं सकते कि यह ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं खुद के लिए ऐसा प्रयास करता हूं। और उस्ताद जी डागर साहब ऐसा कहते थे कि मंच से ऐसी प्रस्तुति दो के ताली बजनी ही नहीं चाहिए हाल में सन्नाटा हो जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि यही कोशिश रहनी चाहिए कि आप ऐसा गाए ऐसा बजाएं और जो आपकी गायन वादन है वह पूजा हो जाए । और उस पूजा में जो आपने ऊर्जा प्रार्थना की वह वहां साक्षात प्रकट हो जाए और वहां सब को आशीर्वाद मिले की सब मंत्रमुग्ध हो कर मौन होकर घर जाएं । यह हमारे संगीत की महानता है और ऐसा मैंने दृश्य खुद देखा है एक दो बार गुरु जी के कार्यक्रम में ऐसा हुआ और एक दो बार मेरे खुद के कार्यक्रम में भी मुझे ऐसा अनुभव हुआ और दूसरे बहुत से कलाकारों के प्रोग्राम में भी देखा भी है और पढ़ा भी है। ढोंडू ताई कुलकर्णी के जीवन पर एक किताब लिखी हुई है यह किस्सा ऐसा आता है कि कलाकार है जो गायन प्रस्तुति करता है कार्यक्रम के बाद में कोई उनको आकर बताता है क्या आपने इतना सुंदर गया कि ऐसा लग रहा था कि आपने एक ईंट रखी और उसके ऊपर दूसरी ईंट रखी और एक इतनी सुंदर इमारत खड़ी कर दी ज्यादा तालियां बजी के मानो ऐसा लग रहा था के एक-एक ताली से एक-एक इंट टूट कर नीचे गिर रही हो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई । ये एक भावना होनी चाहिए कलाकार की कि यह कोई दिखावे की चीज नहीं है मानो कि हम घर में दीया जलाते हैं ,आरती करते हैं, पूजा करते हैं तो वहां हम यह उम्मीद अपेक्षा नहीं रखते हैं कोई आकर ताली बजाएगा और उसकी सराहना करे कि तुमने कितना अच्छा गाया है तो हम उसे तरीके की उम्मीद ही ना रखें। कई बार तो मुझे बुरा भी लगता है , यह तो मैं अपनी प्रार्थना कर रहा हूं इसमें तारीफ़ वाली क्या बात है। मुझे लगता है किन चीजों में जागरूक रहना भी काफी जरूरी है हम क्या कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं हम इस जहां में क्यों आए हैं तुम मेरी भी यह बहुत ज्यादा कोशिश रहती है कि मैं इस चीजों में सतर्क रहूं, जागरूक रहूं और कभी भटकू नहीं। जो सबसे बड़ा प्रयास है वह यह रहता है फिर चाहे मैं सीख रहा हूं उस वक्त या रियाज कर रहा हूं, कंसर्ट में हूं तो कभी यह नहीं होना चाहिए मेरे साथ में कि मैं अपने कौशल का दिखावा करने में लग जाऊं। यह जो चीज है मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। हमारे ध्रुपद में कहते हैं कि आलाप की जो भाषा है वह बहुत बड़ा सुंदर विषय है कि ऐसा लगने लगता है कि अमृत के साथ बातचीत शुरू हो गई हो। और अगर आप सही अलाप लगाए और उसे सुने और गाने के कौशल में लगे तो ऐसा लगता है कि आप एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और वहां से उसका जवाब आ रहा है मेरे गुरुजी यह समझाते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से आप एक प्रश्न पूछते हैं और उसके उत्तर में दूसरा फ्रेज आता है । दो फ्रेज के बीच का जो साइलेंस होता है। उसके अंदर से हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका जो संभावित उत्तर है वह क्या होना चाहिए। उसके आपकी सोच से परे हो जाता है गाना बजाना। पूरे डूब जाते हैं तभी आप इसकी असल भाषा के साथ जुड़ सकते हैं । और कई बार तो वैसा भी नहीं हो पता जैसा आप सोचते हैं। यही प्रयास रहता है जिससे मैं आपको मैसेज वाली बात भी बताई कि किस तरीके से संदेश होना चाहिए तो यह मेरा खुद का स्वयं का प्रयास रहता है और वाकई में आपकी यह जो बात थी वह काफी सुंदर थी के कलाकार का प्रयास रहना चाहिए किसी तरह का संदेश देने का अपनी कला के माध्यम से तो मेरा भी यही मानना है।
अरमान:- आपने बहुत ही सुंदर बात की और गुरुजी के आपने जिस तरीके से विचार रखे उन्हे उनके व्यक्ति वाकई में मंत्रमुग्ध हो जाए। और आपने बताया कि जिस तरीके से बचपन से ही संगीत का वातावरण आपके आसपास रहा जिससे आपकी स्वाभाविक रूप से दिनचर्या पर प्रभाव रहा आपकी दिनचर्या क्या होती है ?
चिंतन:- बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब शुरुआत होती है तो वह संगीत के साथ ही होती है सुबह पांच बजे से स्वर साधना शुरू हो जाती है अभी मौजूदा वक्त में बड़ौदा में मैं सिखाता हूं जिसके अंदर विदेश के मेरे कुछ विद्यार्थी भी आते हैं । जैसा मैंने अपने गुरुजी से सीखा वैसा ही मेरी प्रयास रहता है कि मैं भी वैसा सीखने की कोशिश करूं और जब शुरुआत होती है स्वर साधना की तो एक स्वर के ऊपर आधा घंटा चालीस मिनट से ऊपर भी रुकते हैं। जिस प्राकर हम सवेरे प्राणायाम करते हैं इस प्रकार से तो पूरी सांस भर के स्वर साधना करते हैं और एक-एक स्वर के ऊपर आधा घंटा रुकते हैं। हम दो घंटे के अंदर तीन-चार स्वर गाते हैं। जो यह हमारा सुबह का 5:00 से 7:00 का स्वर साधना का कार्यक्रम रहता है । यह पूरा आपकी सोच को बदल देता है और उसके बाद जो बाकी का दिन होता है वह जिस प्रकार की शांति देता है वह किसी और चीज से नहीं मिल पाती क्योंकि सवेरे सवेरे इस तरह का योग और स्वर साधना दोनों यह एक साथ हो जाना यह वाकई में अपना आप में शरीर की शुद्धि का एक रास्ता है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी हमारे पास में आते हैं और वह पहले से कहीं उन्होंने कुछ सीख रखा है ध्रुपद के अलावा तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यह क्या हो रहा है अभी तो मैं पंचम के ऊपर था और यह अचानक से क्या हो गया तो कई बार उन्हें थोड़ा अलग-अलग लगता है इसे समझने में वक्त भी लगता है तो इस प्रकार से भी हमें नई-नई चीज़ सीखने को मिलती रहती है और जो विद्यार्थी आते हैं उन्हें भी हम अपने तरीके से इस चीज को समझने की कोशिश में रहते हैं। तो यह इस चीज की पहचान है कि आप उसे टाइटल से परे होने की जो आपकी प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद में भूल जाते हैं कि यह पंचम था मध्य था या कौन सा था। यह होना चाहिए इस तरह से जब हम अभ्यास करते हैं तो यह होना एक अच्छी निशानी कहलाता है। मेरा नाम चिंतन है लेकिन जो मेरी अंतरात्मा है जो मेरे अंदर के भाव हैं। मेरा जो व्यक्तित्व है वह ज्यादा इंपोर्टेंट है ना मेरे नाम से। मैं क्या काम करता हूं मेरा कर्तव्य क्या है मेरा कर्म क्या है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि मेरा नाम। प्रकार से जो सारेगामा है उस पार जाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। उसकी प्रक्रिया है जो आपको गुरु मुख से सीखने को मिलती है। तो सबसे पहले के जो दो घंटे हैं उसमें हम यह करते हैं और उसके बाद में जो प्राचीन संगीत है उसके कभी कुछ सूर सरगम गाते हैं कुछ राग कुछ आलाप। पूरे संगीत के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें तो कानों का जो केंद्र है वह इसमें बहुत ज्यादा महत्व रखता है उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो वहां पर भी यह न सोचे कि आप कौन सा राग गाएंगे। जो आपको इशारा मिलता है वही आपकी प्रस्तुति होनी चाहिए। पर ऐसा भी होता है कि आप सोचते कुछ हैं कि मैं इस राज के साथ शुरुआत करूंगा और यहां उसे खत्म करूंगा ग्रीन रूम के अंदर आप जब अभ्यास करते हैं या काम करते हैं तो अब आप सोचते हैं कि अब इस राग के ऊपर काम करूंगा लेकिन जब अपनी प्रस्तुति देते हैं तो आपको दूसरे राज की आज्ञा होती है तो इस प्रकार से भी संगीत अपना प्रस्तुत होता है। इसका भी संस्करण है वह सवेरे रियाज़ से ही होता है। प्रकार से आप सुनते हैं और वही तानपुरा आपके कानों पर बार-बार पड़ता है तो जैसे-जैसे कान में आपको वह तानपुरा बज रहा है लेकिन आधे घंटे बाद में आपको कुछ और ही सुनाई देने लग जाता है तो यह जब गायन में अपनी प्रस्तुति देते हैं तो कई बार ऐसा लगता है अभी तो यही बज रहा था लेकिन यह कुछ देर बाद में आपको कुछ दूसरे राग दूसरी चीजों की आज्ञा होती है तो आप उस तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपका संस्करण अब गहराई में जा रहा है आपके कान खुलने लगे हैं अभी यह अमृत का जो दरवाजा है हम इसे वह मानते हैं कि अब वह आपके लिए खुल रहा है क्या आप उसे भाषा के अंदर संगीत में बात कर रहे हैं की जिससे आप अमृत की भाषा से अपने आप को जोड़ सकते हैं कि अब आप उसे दरवाजे को खटखटा रहे हैं और धीरे-धीरे वह दरवाजा आपके सामने खुल रहा है। और आलाप की जो भाषा है वह हमारे संस्कृत में बहुत बड़ा विषय है इतना महत्वपूर्ण बड़ा विषय इसलिए है क्योंकि बंदिश है उसमें तो आपको साहित्य दिया जाता है जो साहित्य का भाव है वह आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसी प्रकार से आप अपने गायन में उसका भाव प्रकट करते हैं लेकिन अगर मैं कहूं राग भैरव है तो उसका खुद का भाव क्या है तो मेरा यह खुद का मानना ऐसा है कि हम उसे बांध नहीं सकते हैं। वह जो रस है उसे हमें टटोलना है उसमे एक प्रार्थना का आवाहन रहता है के अंदर कोई शब्द नहीं है साहित्य से जुड़ा हुआ आप उसे कैसे देखते हैं और उसे किस तरीके से महसूस करते हैं मैं आपको कोई रस नहीं दिया जाता है क्या आप उसमें विचार करें जिस क्षण में आप इसका अभ्यास कर रहे हैं और उसी क्षण में जो रस आपके सामने आता है आप उसी का अभ्यास करते हैं और इस राग में वह रस है आपके लिए। आपने सुबह अभ्यास किया है गया है और जब शाम को आप उसे दोहराएंगे तो उसमें आपको अलग ही रस की प्राप्ति होगी। इसकी बहुत बड़ी देन है भारतीय संगीत में।
अरमान:- एक सवाल ऐसा है जो रूप बदल बदल कर सामने आता है । वही मैं आपसे भी जाना ना चाहूंगा कि आपकी नजर में संगीत क्या है?
चिंतन:- मैं ध्रुपद संगीत के बारे में कहना चाहूंगा कि उसे शुरू करने के बाद वह एक ऐसी भाषा है जो आपके अंतर जगत से आपको बात करने के लिए माध्यम प्रदान करती है। यूं समझिए कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो कोशिश यह रहती है कि हम अपने अच्छे-अच्छे जो पहलू हैं वह उनके सामने प्रस्तुत करें और हर व्यक्ति की कोशिश रहती है कि जो बुराई है हमारे अंदर उसे हम छुपाई रखें और उसे व्यक्ति के सामने सिर्फ अपनी जो अच्छी बातें हैं उन्हें सामने रखें। फिर जैसे बार-बार उनसे मुलाकात होने लग जाए फिर जब वह दोस्त बन जाता है व्यक्ति तो वहां खामियां भी नजर आती है और जो दूसरी आदतें हैं उनका भी पता चलता है। जब आप लोग साथ में रहने लग जाएंगे दो-चार महीने जब साथ में वक्त बिताएंगे तो सब कुछ एक दूसरे के बारे में जानना हो जाता है। वजह से साथ में रहते हुए वैसी बातें हैं वह आदतें भी सामने आ जाती है जो आपने उसे वक्त अपने स्वभाव के अंदर उन्हें दिखाने की कोशिश नहीं की थी और जिन्हें छुपाने की कोशिश रही थी। तो उसी प्रकार से ऐसी जो छुपी हुई बातें हैं जो आपको खुद को भी एहसास नहीं होता है अंदर यह है और उसे भी पकड़ पकड़ के वह बाहर निकलता है एक तरीके से हम कह सकते हैं उसकी शुद्धि करना यह जो प्रक्रिया है केवल मेरी नजर में संगीत के माध्यम से आ सकती है। और संगीत का मतलब सिर्फ यह नहीं कि जब हम गाते हैं तभी मन को शांति मिलती है या फिर जैसा मैंने आपको कहा कि एक शुद्ध की प्रक्रिया शुरू होती है अगर आप इसे मन से सुनेंगे तब भी यह चीज होती है कई बार जब लोग सुनते हैं तो उन्हें बहुत खुशी भी मिलती है और वह मन के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। और जो कलाकार खुद गाता है और बजाता है उसको तो खैर एक अलग तरह की फीलिंग का अनुभव होता ही है। के वह पूरे शरीर से और ब्रीदिंग सिस्टम से वह चीज पूरी जुड़ जाती है। आज की तारीख में मैं खुद भी सीख रहा हूं तो मुझे बहुत युवा लोग मिलते हैं जो मेरे शिष्य हैं यही कोई उम्र 20 - 22 साल है और वह जब यह चीज सीखना शुरू करते हैं तो वह कुछ ही वक्त में मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि हमें इससे पहले को बेचैनी हुआ करती थी एंजायटी की समस्या हमारे यहां बहुत ज्यादा थी लेकिन जैसे ही हमने ध्रुपद शुरू किया तो मन काफी ज्यादा शांत रहने लगा और जो एक मैंने शब्द इस्तेमाल किया शुद्ध वह उन्हें अनुभव हुआ तो इस प्रकार से जब लोग सिखाते हैं और इस अभ्यास करते हैं तो न सिर्फ एक शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं और यह चीज है भी साबित के यह संगीत आज के वक्त में जो आज के नौजवानों की जो समस्याएं हैं उनके लिए यह दवाई के लिए भी उपयोगी है उसका काम न सिर्फ लोगों को संगीत से जोड़ना बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर करना है। कि आज भी हम देख रहे हैं ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनकी कोई दवाई नहीं है तो उनका इलाज संगीत है। वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है किसी के हृदय के अंदर स्थान पाना और वह चीज केवल संगीत के माध्यम से कला के माध्यम से ही संभव है। किसी के हृदय में स्थान पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप किसी को मना सकते हैं जबरदस्ती काम करवा सकते हैं पैसे देकर उन्हें किसी चीज का लालच देकर अपना काम करवा सकते हैं लेकिन इसे भी हृदय तक उनके नहीं पहुंच सकते क्योंकि वह लालच था और अगर वाकई में हृदय के अंदर स्थान पाना यह केवल मेरी नजर में संगीत के माध्यम से ही संभव है। और सामने वाले व्यक्ति की आंखों में पानी आ जाता है आप संगीत की प्रस्तुति कर रहे हैं और आपके सामने वाला आपको देखकर भावुक हो जाए यही तो असली जुड़ाव है। वाकई में बहुत ही अद्भुत और कमाल का माध्यम है संगीत की जब आप प्रस्तुति करते हैं तो आप अपने गुरु से भी जुड़ते हैं जिसे आपने सीखा है और आप अपनी ऑडियंस से भी जुड़ते हैं जो वह मन का दिल का जो जुड़ाव है वह महसूस होता है। और यह एक माध्यम है आप खुद एक सेतु बन जाते हैं जब आप अपने ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं प्रस्तुति देते हैं तो आप खुद एक सेतु बन जाते हैं अपने गुरु के जो शिक्षा है उन्हें आप अपने माध्यम से अपने ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं। जो शांति , मित्रता सद्भाव का जो संदेश है वह आपके माध्यम से लोगों के सीधा दिल तक उतरता है। सदियों से एक परंपरा बनी हुई है और एक माध्यम बनता है उसका आप भी अनुसरण करते हैं। और जो चीज आप तक भी पहुंची है आपके गुरु के द्वारा यानी कि आपके गुरु ने आप तक पहुंचा जो कि उन्होंने अपने गुरु से सीखा था और फिर उसे चीज को अब दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह सोचना भी मन को कितना सुख पहुंचना है यही तो असली संस्कृति है यही तो असली संस्कार है। और उसे चीज के पास जो वातावरण में सकारात्मक बदलाव आता है वह भुलाए ना भूले ऐसी चीज होती है। उसे चीज को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं किसी को बात नहीं सकते आपका वह अपना होता है यह चीज केवल अनुभव से ही संभव है।
अरमान :- संगीत को अपने जिया है और काफी नजदीक से आप इसके पहलुओं के बारे में जानते हैं तुम्हें इसके बारे में आपसे और जानते हुए यह सवाल करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से और बदलाव ला सकता है शास्त्रीय संगीत?
चिंतन :- संगीत में कहूंगा तो उसमें हमारी एक लंबे वक्त से शुरू से परंपरा रही है यज्ञ करने की , किसी राज्य के राजा को पुत्र नहीं हो रहा तो पुत्र प्राप्ति के दिए भी यज्ञ का आयोजन होता था। या फिर किसी की खेत के अंदर फसल नहीं हो रही है उपजाऊ जो जमीन है वह खराब हो रही है तो उसके लिए भी यज्ञ हुआ करते थे और कुछ अगर बड़े स्तर पर होता है कोई बड़ी चीज है तो महायज्ञ तो यह परंपरा हमारे यहां शुरू से रही। वह उसे वक्त क्या होता था वह जो एक ऊर्जा है उसे आमंत्रित किया जाता था यज्ञ के माध्यम से और यह बिलीव है कि वह ऊर्जा आएगी और आपको वह प्रसाद देगी फिर चाहे वह पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हो या फिर खेत के लिए। आपका जो इंटेंशन है वह फुलफिल होता है उसे यही चीज हम राग के अंदर भी समझ सकते हैं आप राग से उस ऊर्जा को न्योता देते हैं और वहां से वह ऊर्जा आपको आशीर्वाद देती है। लोक संगीत के माध्यम से राज के माध्यम से उसे चीज से अपने आप को जोड़ सकते हैं उसे ऊर्जा से अपने आप को जुड़ा महसूस कर सकते हैं जो कि यह कैसे माहौल से पैदा होती है जिससे आपकी जो चिंताएं हैं जिससे आप इसे रोज-रोज प्रोफाइल कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी चेहरे पर लगती है हम घर जाकर स्नान कर लेते हैं तो शरीर साफ हो जाता है लेकिन हमारी जो अंतर आत्मा में शुद्ध की आवश्यकता महसूस होती है वह हम कैसे करें उसका मध्य संगीत कला साहित्य है।
अरमान :- जो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा वह जाहिर तौर पर वही व्यक्ति बता सकता है जो एक लंबे वक्त से कला से उस विद्या से जुदा हो। क्या आपको मौजूदा वक्त में लग रहा है कि वक्त के साथ-साथ संगीत और उसके कलाकारों में किसी तरह का कुछ परिवर्तन आ रहा है फिर चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक आपकी नजर में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिले हैं?
चिंतन :- अगर मैं आपको अपने ही अनुभव से बताऊं तो जब बी कॉम करने के बाद एम बी ए और सी ए फाउंडेशन शुरू किया था और उसके बाद में मैं पुणे चला गया था। और उसके बाद में मैं अपने गुरु जी के साथ में रहना शुरू कर दिया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इनकम क्या होगी क्या मैं कुछ काम पाऊंगा या नहीं क्या संगीत के माध्यम से मैं कमा लूंगा या फिर कोई और काम करूंगा तो कभी भी इस तरह की चीज मेरे दिमाग में उन दिनों में नहीं आई इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैं संगीत को पूरी तरीके से अपने आप से जोड़ लिया था और मैं खुद को उसमें पूरी तरीके से डूबा देना चाहता था । उसे वक्त बिलकुल भी यह मन में नहीं था कि मैं इससे पैसे कमाऊं या फिर किसी तरह की कोई शोहरत हासिल करने की कोशिश करूं। और आज की तारीख में भी जब मैं कहूं कि मुझे सिखाते हुए इतने साल हो गए हैं तो अब भी ऐसा कोई ख्याल मन में नहीं आता है। मुझे मन ही मन से यह खुशी भी थी और मैं काफी अपना को समृद्ध महसूस कर रहा था संगीत में पूरी तरीके से डूब कर कि अब एक लंबा वक्त हो चुका है और मैं खुद भी अब सिखाता हूं तो ऐसा लगता है कि वह पेशेंस का ठहराव आज देखने को नहीं मिल पाता है जो अभी सीखना जिन्होंने शुरू किया है वह मंच की तलाश में रहते हैं उन्हें लगता है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी प्रस्तुति देनी शुरू करें और वह कहीं ना कहीं उसे होड़ में लग जाते हैं सीखने की बजाय वह दिखने की होड़ में लग जाते हैं। मैं अलग-अलग जगह पर ट्रैवल भी करता हूं दूसरे देशों में भी मैंने प्रस्तुति दी है और अपने गुरु जी के साथ में मैं जाता रहता हूं तो मुझे यह महसूस हुआ है खासकर की इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर की आज की जो पीढ़ी है वह एक लंबे समय तक अपने गुरु जी के साथ में नहीं रह पा रही है यह चीज उनमें मुझे एक कमी नजर आती है सबसे बड़ी। जैसा कि मैंने कहा कि वह सीखने से पहले तो दिखाना चाहते हैं तो जो आर्थिक व्यवस्था है वह उसकी तरफ देख रहे हैं कि हम इसे कैसे पैसा बना सकते हैं या फिर कैसे अपना नाम इसमें बना सकते हैं। और अफसोस के साथ कह रहा हूं कि वह विद्या ग्रहण करने की जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उससे वह दूर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ी उम्र के हैं या फिर जो थोड़ा कुछ सीख चुके हैं छोटी उम्र के 20-22 साल के सीखना आते हैं उनके दिमाग में भी यही चीज रहती है उन्हें वह जो पवित्रता है वह कहीं नजर नहीं आती है सिवाय इसकी शोहरत के। मुझे लगता है कि अगर आप इन चीजों को देखें तो इसमें आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है अगर आप कोई काम भी शुरू करते हैं कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं तो भी तो उसमें रिस्क है कि आप क्या 100% उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे और यह तो बिजनेस तो नहीं है यह तो कला है। यह एक बहुत ही लंबी यात्रा है यह स्टारडम का खेल नहीं है इसमें भक्ति और श्रद्धा इसकी काफी ज्यादा जरूरत है काफी ज्यादा आवश्यकता है।
अरमान :- बहुत खूबसूरत बात कि उद्देश्य केवल इस वक्त सीखने का होना चाहिए लोग दिखाने में लग जाते हैं । जैसे-जैसे जल्दी से जल्दी अपना नाम कैसे बढ़ाए साहित्य अकादमियों के द्वारा या और किसी संस्थान के द्वारा यह चीज हमें हर जगह देखने को मिलती है जो वाकई में पवित्रता को खंडित करने का काम करती है क्योंकि यह वह माध्यम है जो व्यक्ति को व्यक्ति के मन मस्तिष्क से जोड़ता है और मस्तिष्क ऐसा जो केवल शांति की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है जो समाज के सुधार के लिए काम कर रहा है ना केवल स्वार्थ के लिए।
चिंतन:- कला, साहित्य मैं संगीत की बात करूं जब वह व्यक्ति अपना जो नाद है उसमें जो गोपनीयता है भाव वह भी धीरे-धीरे बाहर आने लगता है उसको पता होना हो कि वह क्या दर्शा रहा है लेकिन जो उसे सुन रहा है वह व्यक्ति कहीं ना कहीं समझ जाता है कि इसकी मंशा क्या है। प्रगति ही की बात है तो अगर आप जितना ईमानदार रहेंगे आप इसमें उतना ही नाम कमाएंगे उतनी ही प्रगति करेंगे अगर आप ईमानदारी को ही एक किनारे कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे बल्कि आप जैसा आपने बहुत खूबसूरत बात की पवित्रता को खंडित करने वाली चीज हो जाती है । क्या आप जिस काल से जुड़े हैं आप उसे खराब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि कुछ चीज जो होती है छुपाए नहीं छुपती और मैंने शुरुआत में ही जैसा कहा कि संगीत वह माध्यम है व्यक्ति के सीधा मन तक पहुंचता है तो आप जितना चाहे उतना बाहर बाहर से दिखा देंगे । मैं तो साधना कर रहा हूं या फिर मेरा वह भाव नहीं है लेकिन जो आपके अंदर से ध्वनि निकलेगी वह दुनिया को बताएगी क्या आपका असली उद्देश्य क्या है संगीत कला के लिए।
अरमान :- शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार ।
चिंतन - धन्यवाद
Dr.Seema Jain
डॉक्टर सीमा जैन
सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाली डॉक्टर सीमा जैन , सहायक आचार्य समाजशास्त्र (महाराजा गंगा सिंह विश्विद्यालय बीकानेर) राज्य महासचिव अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, राजस्थान से शब्द संवाद के लिए अरमान नदीम की खास बातचीत ।
आज सबसे बड़ी जरूरत हिन्दू मुस्लिम एकता और भाईचारा कायम रखते हुए एकजुट देश के जरिए आतंकवाद और पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों को ध्वस्त करने की है । - डॉक्टर सीमा जैन
अरमान:- आप राजनीतिक , शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों में एक साथ सक्रिय हैं यह सब कैसे शुरू हुआ ?
सीमा जैन:- अगर मैं अपने शुरुआती समय की बात करूं और अपने एकेडमिक्स की बात करूं तो मैं काफी सामान्य परिवार से बिलॉन्ग करती हूं मेरे पिता ड्राइवर थे उन्होंने मेहनत मजदूरी के साथ में पढ़ाया लिखाया और एक चीज हमेशा उन्होंने सिखाई की कभी भी गलत चीज को बर्दाश्त ना करें । उनका कहना था कि मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब तुम मजबूती के साथ आगे बढ़ोगे चाहे वह पढ़ाई हो सामाजिक क्षेत्र हो या और कोई भी काम और अकादमिक करियर की अगर बात है तो वह तमाम आर्थिक तंगियों के बाद में गुजरते हुए यहां पहुंची हूं । और एक लंबा वक्त हो चुका है मुझे टीचिंग लाइन में और इसमें यह एक चीज महसूस की है कि लोगों का मानना है कि आर्ट फील्ड में जो पढ़ाई होती है सबसे सस्ती पढ़ाई मानी जाती है लेकिन फिर भी आर्थिक चुनौतियां खूब झेली है इसमें इसीलिए शिक्षा का महत्व बहुत ही अच्छी तरह से समझती हूं कि शिक्षा हासिल करना एक निचले तबके के विद्यार्थी के लिए कितना मुश्किल होता है और कितना जरूरी भी होता है । उन तमाम चुनौतियों को पार करके शैक्षणिक योग्यता हासिल की है और अपने कॉलेज टाइम कि बात करूं उस वक्त एक रुझान सभी में यह रहता था कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ जाए और व्यक्तिगत रूप से भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और गतिविधियों से मेरा जुड़ाव काफी कम उम्र से ही रहा है तो खेल के टूर्नामेंट काफी ज्वाइन किए और इतनी रुचि होने की वजह से जब मैं बी ए सेकंड ईयर में थी तो उस वक्त यूनियन के चुनाव हुए स्टूडेंट यूनियन के जो चुनाव हुआ करते थे उस वक्त व्यवस्था यह हुआ करती कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव किया करते थे अब इसमें थोड़ी प्रक्रिया में बदलाव आया है । सबसे पहले जब मैं खेल यूनियन की सचिव बनी बी ए सेकंड ईयर में और उसे समय ढाई सौ रुपए जमानत राशि जमा करवानी पड़ती थी और वह भी मेरे पास में नहीं थी वह भी मेरी दोस्त ने जमा करवाई कि नहीं तुझे चुनाव लड़ना है, और ताकत के साथ अपना प्रचार करना है वहां से मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का सफर शुरू हुआ । और ठीक अगले साल ही छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और वहां पर भी इलेक्शन कैंपेनिंग में मिलकर फंड जमा किया और खुद से उन्होंने 10-10 रुपए जोड़े उसमें । आज तो हम देखते हैं कि छात्र संघ के चुनाव बहुत महंगे हो चुके हैं। क्योंकि घर वालों ने तो उस वक्त साफ कह दिया था कि तुम्हें पढ़ा ही रहे हैं उतना काफी है चुनाव के लिए पैसा देना हमारे बस का नहीं । इसी कारण मैं हमेशा से अपने दोस्तों का आज भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने उस वक्त मेरा जिस तरीके से हौसला बढ़ाया उस वजह से मैं राजनीति में उस वक्त कामयाब भी हुई। जो मेरी पहली पारी राजनीति की रही छात्र राजनीति की रही वह मेरी दोस्तों ने दस रुपए चंदा इकट्ठा करके शुरू करवाई और इसी का नतीजा रहा कि साल 2003 में छात्र संघ अध्यक्ष रही श्री जैन कन्या कॉलेज में तो वहां इतना कोई ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं था । गर्ल्स कॉलेज थी प्राइवेट कॉलेज थी। लेकिन जैसे ही पीजी में एडमिशन लिया 2003 में डूंगर कॉलेज में। और मैं कह सकती हूं कि एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान ही फिर चाहे वह कोई भी संगठन हो एबीवीपी, एनएसयूआई, एस एफ आई सभी संगठनों की यह कोशिश रही कि मुझे अपने साथ शामिल किया जाए। सभी की कोशिश रहती थी तब बात करने की कोशिश में थे अपने साथ है लेने की जद्दोजहद की लेकिन मुझे अपने पिताजी की उस वक्त की बात आज भी याद है वह बताते हैं और वह हमें हमेशा से यह समझाते रहे कि बेटा देखो, समझो, परखो और उसके बाद फैसला करो। छात्र संगठन है तो सब अपने-अपने अलग-अलग विचारधाराओं को साथ में लेकर चलते हैं और इस फैसले को लेने से पहले मैंने सभी का थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ा और जहां तक मुझे समझ आई एस एफ आई ही क्योंकि वह संगठन शिक्षा और संघर्ष का नारा देती है और उसके साथ में उनका नारा है लड़ो लड़ाई पढ़ने को तो यह चीज मुझे भी महसूस हुई कि मैं तो पढ़ने के लिए लड़ तो रही थी । पहले से ही तमाम हालात से जूझ रही थी। नारा है कि लड़ो लड़ाई पढ़ने को पढ़ो समाज बदलने को। जो सोशल चेंज की बात जो वो करते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण रहा एस एफ आई ज्वाइन करने का और वहां से मेरा जो सफर है सक्रिय राजनीति का वह और ज्यादा ताकतवर हुआ। और उसके बाद में जो विश्वविद्यालय का पहला आंदोलन है जो की 2003 के नजदीक में और उसके आसपास उसका पहला सेशन 2003 में ही रहा तो उसमें हमने जोर शोर से अपनी आवाज उठाई । वह सेशन शुरू हुआ और फिर उसके बाद में जो फीस बढ़ाई गई थी विद्यार्थियों की उस पर हमने अपना आंदोलन शुरू किया ,आंदोलन ऐतिहासिक रहा। लगभग दो साल तक हमने आंदोलन किया । लेकिन लोग यह कहा करते थे कि एक संगठन के आ जाने से क्या होगा तुम्हारी आवाज कौन सुनेगा नया विश्वविद्यालय है फीस तो बढ़ाएगा लेकिन हमने हार नहीं मानी और आखिर हर छात्रों को विश्वविद्यालय ने फीस लौटाई और हमारा आंदोलन सफल हुआ और आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय को अस्तित्व में देख रहे हैं और आज मैं खुद यहां लॉ फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूं।
अरमान :- आपकी खुद की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई और आपने बताया कि किस तरीके से मौजूदा वक्त के चुनाव महंगे हुए हैं। आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं?
सीमा जैन:- बिल्कुल आपने सही मैं आपसे सहमत हूं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है मौजूदा वक्त में जो मोबाइल की ट्रेडिंग बढ़ी है विद्यार्थी जो तमाम संगठन से जुड़े हैं वह मोबाइल पर ही क्रांति करना चाहते हैं। वह सिर्फ उसी में उलझे रहते हैं और आधारभूत मुद्दे होते हैं उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता है सिवाय इसके की एक इकट्ठा भीड़ की जाए और उसके साथ में रियल स्टेटस अपडेट किया जाए । इससे आगे उनके जो उद्देश्य हैं वह नजर ही नहीं आते हैं उन्होंने केवल सोशल मीडिया को ही अपना सर्वोच्च मान लिया है। और इसी से हमें यह महसूस होता है कि विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं वह छात्र नेता उठाना ही भूल चुके हैं क्योंकि वह दूसरी चीजों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने को वह समस्या नजर ही नहीं आती जो रोजाना आम बच्चे देख रहे हैं महसूस कर रहे हैं फिर चाहे वह फैकल्टी के साथ में अनुबंध और इसी से हमें यह महसूस होता है कि विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं वह छात्र नेता उठाना ही भूल चुके हैं । उठाते भी हैं तो सांकेतिक रूप से उस पर बात करते हैं एक आध प्रदर्शन किया कुछ लोगों को इकट्ठा किया और फिर वही पुरानी आदत उनमें की उसकी रील और फोटो स्टेटस पर अपना अपडेट करना। और क्योंकि यह बात हम कह सकते हैं क्योंकि हमने शुरुआत ही छात्र राजनीति से की है तो उसे वक्त ऐसा लगता था कि आने वाले वक्त में जो छात्र राजनीति होगी वह और ज्यादा गंभीर होगी और सक्रिय रूप से होगी बिना किसी भेदभाव के होगी । विद्यार्थियों के हित में काम किया जाएगा और जो लोग उनका शोषण कर रहे हैं ऊपर लगाम लगेगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो नई राजनीति हम देख रहे हैं वह यही है और अगर हम विद्यार्थियों की बात करें विद्यार्थियों के परेशानियों की बात करें जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 के बाद में उसके अंतर्गत बहुत बड़े-बड़े बदलाव किए जाएंगे जो कि छात्र हित में नहीं है मौजूदा विद्यार्थी वर्ग इन खतरों को भांप नहीं रहा है। कंफर्ट और लग्जरी जोन में काम कर रहा है केवल चुनाव लड़ना और सिर्फ चुनाव लड़कर या जीत कर खुद को छात्र संघ अध्यक्ष बनाकर छात्र नेता बन जाना यह कहना यह बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि अगर छात्र हित में काम नहीं किया गया तो वह नेता नहीं कहलाया जा सकता। मेरा मानना यह है कि केवल प्रचार प्रसार करने में वह व्यस्त हो चुके हैं और इसी के इर्द गर्द छात्र राजनीति चल रही है। आज हम देखते हैं कि छात्र नेताओं के द्वारा बड़े-बड़े आंदोलन होना ही बंद हो चुके। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो आंदोलन चाहे दस दिन चले या पचास दिन हम सड़कों पर रहते थे तभी प्रशासन पर दबाव बनता है और वह छात्र हित में फैसला लेते हैं। लेकिन बड़े आंदोलन तो छोड़िए जो कैंपस के भीतर अगर हम सेफ एनवायरमेंट हो जिम्मेदारी जो छात्र नेताओं की भी होनी चाहिए वह भी हमें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि वह तो खुद आउटर स्टूडेंट के साथ में आते हैं तो कैंपस के भीतर की जो समस्याएं हैं या फिर जो और छात्र हित में कार्य होने चाहिए वह उन पर कहां ध्यान दे पाएंगे। और साथ ही सेफ एनवायरमेंट की जिम्मेदारी तो छात्र नेताओं की होनी ही चाहिए और जो कमजोर वर्ग से जो विद्यार्थी आते हैं उनको आगे बढ़ाने और उनकी मदद करने को भी छात्र नेताओं को आगे आना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो छात्र नेता है वह आकर्षित हो रहे हैं धर्म की राजनीति , जात की राजनीति में उनका इंवॉल्वमेंट ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है और अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो उनका तो कोई धर्म ,जाति से मतलब नहीं होना चाहिए उन्हें केवल अपने छात्र हितों के ऊपर कार्य करना चाहिए और अगर समाज में कोई बड़ी परेशानी है तो उसे पर भी उन्हें जिम्मेदारी के साथ में अपनी आवाज उठानी चाहिए ना कि इस तरह की राजनीति में अपना नाम बनाना चाहिए। हम आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में यह चीज देखते हैं और महसूस करते हैं कि जो एक वक्त में भाईचारा और एकता की बात की जाती थी और सब एक साथ मिलकर समस्याओं का निवारण करते थे वह धीरे-धीरे देखने को हमें कम मिल रहा है।
अरमान:- लेकिन विद्यार्थियों की मांगों की बात करते हैं तो वह हमें नजर आती है जो की काफी मूलभूत चीज होती है यानी की मूलभूत सुविधाओं की मांग हमें ज्यादातर देखने को मिलती है तो क्या प्रशासन का जो रवैया है या कार्य शैली इस तरह नजर नहीं आती कि थोड़े से बदलाव को हम विकास समझ बैठे हैं यह जो स्थिति है इसे आप क्या कहेंगे?
सीमा जैन:- आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और हमें यह भी देखना होगा कि जिस तरह की मांग होगी जिस तरह की आवाज होगी जिस तरह का सुर होगा वैसी ही परिपूर्ति होती है संसाधनों की मैं आपको स्पष्ट रूप से यह बात कहना चाहती हूं मारवाड़ी में कहावत है जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां भी दूध नहीं पिलाती। यह चीज मैं खुलकर कह सकती हूं भले ही मैं उस प्रशासन से जुड़ी हूं आज लेकिन जब तक विद्यार्थी अपने मुद्दों पर सतर्क नहीं होगा पैनी नजर नहीं बनाएंगे तो उसे चीज का निवारण नहीं हो पाएगा क्योंकि यह भी चीज है और इसमें कोई दोहरा नहीं है कि कोई भी विश्वविद्यालय या विद्यालय है वह छात्रों की वजह से ही चलते हैं और वहां पर विद्यार्थियों की बात को निश्चित रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए और विद्यार्थियों को खुद अपनी बात प्राथमिकता के साथ में उठानी भी चाहिए प्रशासन को भी इसका संज्ञान लेकर समस्या का निवारण करना चाहिए।
अरमान :- अगर हम बात करें और जब हम सेंट्रल लिस्ट लोगों को सुनते हैं या फिर राइट विंग या और किसी भी विचारधारा के लोग जो साम्यवाद पर सवाल उठाते हैं और तर्क भी देते हैं कि लेनिन के बाद साम्यवाद जब हम विश्व स्तर पर देखते हैं रिश्ता है वह हमें तानाशाही के साथ नज़र आता है। क्या संबंध है तानाशाही और साम्यवाद का इसे आप कैसे देखते हैं?
सीमा जैन:- जी बिल्कुल भी नहीं ऐसी यह बात सही नहीं है साम्यवाद में तानाशाही की रत्ती भर भी जगह नहीं है। आपने जो बात कही सेंट्रललिस्ट यह यह बात केंद्रीयता की साम्यवाद करता है जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ने की बात होती है, मान सम्मान की बात होती है और जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए काम किया जाता है जब भगत सिंह को फांसी का हुक्म हुआ जब अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की अपनी नियति साफ कर दी उसके बाद में जब उन्हें बुलाया गया तो उस आखिरी वक्त में भी वह किताब जो पढ़ रहे थे वह लेनिन की थी और उन्होंने कहा की एक क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी से मिलन हो रहा है। तो इस तरह की सोच और काम साम्यवाद में है जहां राई बराबर भी तानाशाही की जगह नहीं है। कम्युनिस्ट विचारधारा तो मजदूर वर्ग को किस वर्ग को विद्यार्थियों को मेहनतकश तबके को साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। हर किसी को समानता की नजर से देखने वाली विचारधारा है फिर चाहे वह चाहे कोई भी हो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता चाहे किसी भी जाति धर्म का हो।
अरमान:- हाल फिलहाल में देश में हुई घटनाओं का आप कैसे मूल्यांकन करते हैं?
सीमा जैन:- पहलगाम में जो हुआ इतना दर्दनाक है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता । बर्बर तरीके से की गई हत्याएं आहत करती है। कितने परिवार उजड़ गए, वहां तक पहुंचने के लिए कई सुरक्षा चरणों को पार करना पड़ता है अब से पहले जो वहां गए हैं और जिन्होंने मुझे अपना अनुभव साझा किया है वह बताते हैं वहां पहुंचना ही काफी मुश्किल है सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद रहती है और कड़े इंतजामत होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही सुरक्षा में चूक है और केन्द्र सरकार ने इस चूक को माना भी है । और ऊपर से आतंकियों ने जो षड्यंत्र रचा देश को तोड़ने का, नफरत फैलाने का, आपस में लड़ाने का यह सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने वहां धर्म पूछ कर मासूमों को मारा। जो षड्यंत्र उनका था वह कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल भी रहा है जिस तरह से तनाव हुआ देश में। यही तो उनका असल उद्देश्य था कि देश में भाईचारा खत्म हो जाए उसी की चपेट में हम लोग आने लगे। और इसको आग भड़काने का जो काम हमारे देश में कट्टरपंथी ताकतें हैं वह लगातार कर रही है । और यहां देश में कट्टरपंथी आतंकवाद से लड़ने के बजाय देश को हिन्दू मुसलमान में उलझा कर भटकाने का काम कर रहे हैं । जबकि आज सबसे बड़ी जरूरत हिन्दू मुस्लिम एकता और भाईचारा कायम रखते हुए एकजुट देश के जरिए आतंकवाद और पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों को ध्वस्त करने की है । मुसलमानों का योगदान देश की आज़ादी की लड़ाई में रहा है । दोनों तरफ से हमें सतर्क होने की जरूरत है। वर्तमान समय में हमें आतंकवाद के खिलाफ एक साथ होकर मोर्चा खोलना चाहिए और इसमें सरकार जो एक्शन ले हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये नहीं सोच रहे हैं देश की एकता अखंडता को बनाए रखने की कोशिश में नहीं लगे हैं । कुछ लोग नफरत को और बढ़ाने का काम कर रहे है। और लगातार देश के अलग-अलग स्थानों से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। नफरत की राजनीति का ही असर है। और यह बेहद चिंतनीय विषय है कि जब हमारे देश में इतना बड़ा हमला हुआ है उसे हमले के ऊपर विचार विमर्श और उस पर एक्शन लेने की बजाय अपने देश के लोगों पर ही एक्शन ले रहे हैं।
अरमान:- जो घटना पहलगाम में हुई उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वह कम है जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से वह हमला हुआ वहां इंसानियत को जिस तरीके से बे आबरू किया गया वह वाकई सभी को शर्मसार कर देने वाला है और जिस तरीके से जो षड्यंत्र रचा हिंदुस्तान की एकता और भाईचारे को खंडित करने की जो कोशिश रही यही आतंकवादियों का असली मकसद था जिसके नतीजे हम देख में देख रहे है। पहलगाम घटना के बाद में जो देश में हो रहा है वह काम घातक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोगों का ब्रेनवाश किया गया है वह तो अब सुनने को ही कुछ तैयार नहीं।
सीमा जैन:- बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों का ब्रेनवाश किया गया है और मैं बात यह कहना चाहूंगी कि कम्युनिस्ट बनना आसान नहीं है उसके लिए गहन अध्ययन करना पड़ता है उसके बाद आप कह सकते हैं कि हम कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हैं लेकिन मूर्ख बनने के लिए आपको किसी अध्ययन की जरूरत नहीं है मूर्ख बनने के लिए आपको फेसबुक और व्हाट्सएप का ज्ञान काफी है जो भी झूठ फैलाया जा रहा है आईटी सेल के द्वारा उसे आसानी से मान लिया जाए और मूर्ख तैयार हो जाते हैं। यह जो समाज में हिंसा का दौर चल रहा है नफरतों का दौर चल रहा है उसके खिलाफ निश्चित रूप से प्रगतिशील मानसिकता के लोग वह भी इस बात को देखें कि यह जो कचरा और यह जो नफरत फैलाई जा रही है वह सिर्फ यही है क्योंकि जो सैलानी वहां से आ रहे हैं अगर आप उनसे बात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे उन्होंने से ज्यादातर ने यह कहा कि कश्मीर के जो लोग थे वहां के जो मुसलमान थे उन्होंने हमारी मदद की । वहां खुद एक कश्मीरी लोकल शहीद हो गया लोगों की सैलानियों की जान बचाने के लिए। और तमाम कश्मीरियों ने अपनी ऑटो रिक्शा फ्री कर दी वहां की सेवाएं मुफ्त में देना शुरू कर दिया। होटल वालों ने किराया नहीं लिया लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने को क्या मिलता है अडानी की जो एयरलाइंस है उसने यहां इस परिस्थिति में अवसर देखा और अपनी फ्लाइट की टिकटों की कीमतें कितनी ज्यादा कर दी । होना तो यह चाहिए था कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द वहां से मुफ्त में निकालना चाहिए लेकिन व्यवस्था ने अपना अवसर देखा और वहां से भी कमाई करना शुरू किया। लेकिन कश्मीर के जो मुसलमान हैं जिनके खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाया गया वहां पर बचाने के लिए जो मदद की गई वह वहां के कश्मीरी ही थे। लेकिन किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया जो मंसूबा जो षड्यंत्र पाकिस्तानियों का और आतंकवादियों का था वह पूरे देश में फैलाया और आपसी भाईचारे को खंडित करने का काम किया गया। पहलगाम हमला हुआ उसे हम भूल नहीं हैं बड़ा ही दर्दनाक हमला था हम उसको आज भी याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। यह जो आतंकी हमला हुआ इसमें पूरी सुनियोजित तरीके से धर्म पूछ कर मारा गया तो यह तो सीधा-सीधा उनका मंसूबा दर्शाता है कि वह पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे चाहते थे और जो तनाव उन्होंने बनाने की कोशिश की वह सफल होते नजर आ रहे हैं लेकिन मेरी अपील यही रहेगी कि हम उन आतंकवादियों के मंसूबों को धराशाई करें और आपसी भाईचारे को और एकता को बनाए रखें। मैं जनवादी महिला समिति से जुड़ी हूं कितनी महिलाओं के फोन कॉल्स मेरे पास में आए हैं मुस्लिम महिलाएं भी है उसमें काफी वह कहते हैं अब हम क्या करें पड़ोस में जो घर हैं वह हमें घृणा की नजर से देखते हैं । ऐसी चीज है मैंने खुद ऑब्जर्व की है। बहुत ही खतरनाक समय है और इसमें सभी को अपना सहयोग और योगदान देना चाहिए आपसी एकता को बनाए रखने के लिए और उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए।
अरमान:- और इन सब घटनाओं को लेकर पत्रकारिता के ऊपर भी सवाल उठता है जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का उसके जब प्राइम टाइम को हम देखते हैं तो किस तरह की हेडलाइंस हमें देखने को मिलती है यह भी एक चिंतनीय विषय है इस मुद्दे के पर मिडिया के रवैया को आप कैसे देखते हैं ?
सीमा जैन:- मीडिया की भूमिका है वह बहुत ही सकारात्मक होनी चाहिए लेकिन यह बहुत ही दुखद है लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है जो मजबूत स्तंभ माना जाता है वह जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। और मैं बेहद स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी कि आज का मीडिया पैड मीडिया हो चुका है। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में ब्याह शादी होती है तो जो आजकल इवेंट मैनेजर होते हैं उनको निर्देश दिए जाते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। और उन्हें साथ में निर्देश मिलते हैं कि कार्यक्रम शुरू होने से लेकर विदाई तक हर एक चीज को बेहतर ढंग से कवरेज करना है। वही काम और भूमिका आज की मीडिया निभा रही है सरकार बने जब से लेकर दोबारा चुनाव पूर्ण नहीं हो जाते तब तक आपको हमें सुरक्षित रखना है और तुम्हें इन्हीं चीजों का कवरेज करना है और जनता के जो मुद्दे हैं और जो असल चीज जिन्हें न्यूज़ में जगह मिलनी चाहिए उन्हें हटाना है तो इस तरह के जब निर्देश और उनका पालन मीडिया करने लगे तो हम क्या कह सकते हैं। मीडिया का जो प्रचार है जनता के बीच में जिस प्रकार होगा। जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो वह इस तरह का माहौल बना देते हैं सनसनी कैसे खबर बन जाती है और ना कुछ चीजों को वह इतना बड़ा बना देते हैं और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीजों को दो लाइनों में समेट देते हैं और कहीं बाहर तो उसे जगह तक नहीं मिलती है। हिंदू और मुस्लिम डिबेट के जरिए जो माहौल बनाया जाता है यह भी एक बड़ा कारण है देश में नफरत का। और जो काम करना चाहते हैं और जो इमानदारी से अपनी रिपोर्टिंग करते हैं पत्रकारिता करते हैं उन्हें निकालने के लिए उनके चैनल तक खरीद लिए जाते हैं ईमानदार पत्रकार जो सरकार से सीधा सवाल करते हैं उन्हें आज यूट्यूब के जरिए अपनी बात रखनी पड़ती है लेकिन वह आज भी वैसे लोग हैं जो बेबाकी से अपना काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों की हमें जरूरत है देश को जरूरत है पत्रकारिता को जरूरत है।
अरमान:- और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि लोगों ने सेंट्रल लिस्ट होना छोड़ दिया है यानी कि वह दोनों पक्षों को सुनना ही नहीं चाहते हैं वह एक तरफ बस हो जाना चाहते हैं।
सीमा जैन:- हमारी जो विचारधारा है उसमें तो हम जनवादी केंद्रीयता की ही बात करते हैं। उसी से संबंधित अपने सवाल किया है और अपनी बात रखी है की जो केंद्रीय कारण जो है वह आज नहीं रहा है देश के स्तर के जो मुद्दे हैं उसे पर लोगों ने बात करना विचार विमर्श करना छोड़ दिया है और उनका एक यही मंसूबा रहता है कि जो आसानी से काम हो जाए उसमें वह अपना वक्त देते हैं। भीड़ के सहयोग में जिस तरीके से आ जाते हैं यह भी देखने वाली चीज है जबकि अगर हम बात करें तो इसके खिलाफ कानून भी बने हैं पिछली सरकारों में मोब लिंचिंग के लिए। लेकिन जब भीड़ के द्वारा किसी काम को अंजाम दिया जाता है तो उसके लिए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए व्यवस्था हमें ज्यादा देखने को मिलती नहीं। तो जो जनवादी केंद्रीयता है वह तो खत्म ही हो गई है। जयपुर की घटना का जिक्र किया जिसमें जो माहौल खराब किया एक चुने हुए विधायक ने तो एक यह भी चीज सोचनी चाहिए कि क्या आपको सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों ने वोट किया है क्या बाकियों ने आपको वोट नहीं दिया और अगर ना भी दिया हो उसके बाद में भी आप चुनने के बाद में उन सभी के विधायक हैं आप सभी धर्म समाज अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी वर्गों के विधायक हैं तो इस तरह का माहौल तैयार करना यह उचित नहीं है और जनप्रतिनिधियों को इस चीज को समझना चाहिए और जनता को भी इसका मूल्यांकन करना चाहिए। जिन लोगों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया आज उनको गिराने का काम कौन कर रहा है ।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने हेतु आपका बहुत आभार
सीमा जैन - धन्यवाद ।
Prem Janmejai 
प्रेम जनमेजय
व्यंग्य विधा के विश्वविद्यालय कहे जाने वाले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यंग्यकार प्रेम जनमेजय से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
मेरा मानना है कि विरोध विसंगत समय में आपको नपुंसक होने से बचाता है। - प्रेम जनमेजय
प्रेम जनमेजय
जन्म:18 मार्च , 1949 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
वर्तमान दौर की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य विधा के संवर्धन एवं सृजन के क्षेत्र में प्रेम जनमेजय का विशिष्ट स्थान है। कोई इन्हे व्यंग्य का विश्वविद्यालय कहता है तो कोई व्यंग्य का एक्टिविस्ट। प्रेम जनमेजय के व्यंग्य -लेखन को हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण रचनाकारों एवं आलोचकों ने सराहा है । व्यंग्य को एक गंभीर कर्म तथा सुशिक्षित मस्तिष्क के प्रयोजन की विधा मानने वाले प्रेम जनमेजय ने पिछले लगभग दो दशक से 'व्यंग्य यात्रा 'के सम्पादन द्वारा व्यंग्य विमर्श का एक सुदृढ़ मंच तैयार किया है। हिंदी व्यंग्य का विश्वविद्यालय कहे जाने वाले प्रेम जनमेजय की चर्चा के बिना हिंदी व्यंग्य पर बातचीत अधूरी है। हिंदी व्यंग्य नाटक की रेतीली जमीन को इन्होंने अपने तीन व्यंग्य नाटकों द्वारा उर्वर किया है। अनेक पत्रिकाओं ने इन पर एकाग्र प्रकाशित किए हैं। मुम्बई, गुजरात, चेन्नई केंद्रिय विश्वविद्यालय आदि विश्विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएँ सम्मिलित हुई हैं।बर्दमान विश्विद्यालय, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा,उच्च शिक्षा विभाग मद्रास,पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, जीवाजी विश्विद्यालय ग्वालियर आदि में शोध हो चुके हैं/हो रहे हैं। प्रेम जनमेजय की व्यंग्य रचनाओं के अनूदित संकलन मराठी, पंजाबी, राजस्थानी और अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग चार वर्ष तक ‘यूनिवर्सिटी आफ वेस्ट इंडीज’ में अतिथि आचार्य के रूप में कार्य करते हुए प्रेम जनमेजय ने त्रिनिदाद में सांस्कृतिक और भाषाई स्तर पर भी महत्वपूर्ण कार्य किए। भोपाल में आयोजित दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन के , ‘विदेशो में हिंदी’ सत्र की अध्यक्षता करने के साथ मॉरिशस में आयोजित ग्यारहवें वे विश्व हिंदी सम्मेलन के प्रवासी भारतीय वाले सत्र में बीज वक्तव्य दिया था। इसके अतिरिक्त लंदन में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, यू के, न्यूयार्क आदि में आयोजित संगोष्ठियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रेम जनमेजय ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की महत्वपूर्ण पत्रिका ‘ गगनांचल ’ के संपादन के अतिरिक्त ‘हरि गंधा’ ‘ व्यंग्य विविधा’ जैसी अनेक पत्रिकाओं के अतिथि संपादक की भूमिका निभाई है। पिछले बीस वर्ष से, प्रेम जनमेजय के संपादन में निरंतर प्रकाशित हो रही‘ व्यंग्य यात्रा ’ को अनेक साहित्यिक पत्रकारिता सम्म्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे-- माधवराव सप्रे साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान पं0 बृजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान 2013, हिंदुस्तान प्रचार सभा मुंबई का साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान, ‘स्पंदन सम्मान’ , साहित्य मंडल श्रीनाथद्वारा सम्मान आदि। प्रेम जनमेजय का पहला संकलन ‘राजधानी में गंवार’ बहुत चर्चित रहा।
प्रकाशित कृतियों की संख्या : 54 लेखन की विधा: व्यंग्य, नाटक, संस्मरण ,प्रवासी साहित्य , बाल - साहित्य, नव -साक्षरों के लिए, संपादन
व्यंग्य संकलन: राजधानी में गंवार, बेशर्ममेव जयते, हंसो हंसो यार हंसो, भ्रष्टाचार के सैनिक आदि
व्यंग्य नाटक: तीन व्यंग्य नाटक व्यंग्य , क्यूं चुप तेरी महफल में है ।
संस्मरण: इर्दम गिर्दम अहं स्मरामि, स्मृतियन के घाट पर जनमेजय चंदन घिसें , दिल्ली विश्वविद्यालय का स्मृति राग साक्षात्कार : समय के पदचिन्हों से साक्षात्कार
कहानी: तीसरी प्रेमिका
कविता: मेरी नादान काव्याभिव्यक्तियां
आलोचना : आजादी के बाद का हिंदी गद्य व्यंग्य, प्रसाद के नाटको में हास्य व्यंग्य, हिंदी का राष्ट्र : राष्ट्र की हिंदी, श्रीलाल शुक्ल आदि
बाल साहित्य - शहद की चोरी , अगर ऐसा होता ,नल्लू राम
संपादन धर्मवीर भारती :धर्मयुग के झरोखे से,नरेंद्र कोहली एक मूल्यांकन , बींसवीं शताब्दी उत्कृष्ट साहित्य, हिंदी व्यंग्य की धार्मिक पुस्तक: परसाई, शरद जोशी: हिंदी व्यंग्य का नाविक आदि
सम्मान:
प्रेम जनमेजय व्यंग्य विधा को केंद्रित लगभग सभी सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। मुख्य हैं -- हरिशंकर परसाई स्मृति सम्मान, शरद जोशी सम्मान, व्यंग्यश्री सम्मान, माध्यम ’ पं0 श्रीनारायण चतुर्वेदी सम्मान शिखर अट्टहास -सम्मान, कमला गोइन्का व्यंग्यभूषण सम्मान, दुष्यंत कमार अलकरण ‘नई धारा’ 2015 रचना सम्मान आदि
अरमान :- हिंदी साहित्य में जब भी व्यंग्य पर बात की जाए तो आपके नाम के बगैर चर्चा ना तो शुरू हो सकती है ना खत्म इसीलिए यह जानना भी रोचक होगा कि आपकी साहित्यिक शुरुआत किस तरीके से हुई ?
प्रेम जनमेजय:- मेरा जन्म इलाहाबाद का है। और इलाहाबाद को साहित्य की राजधानी माना जाता था और यह कहा जाता कि अगर जन्म आपका इलाहाबाद में हुआ है तो यह जन्मजात लेखक है इसे वहां के मिट्टी के संस्कार मिले। क्योंकि महादेवी वर्मा जी के साथ ही मेरा संयोग और एक जगह लिखा भी क्या अब यह मान लेंगे की महादेवी वर्मा ने कहा कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे और मेरे पिताजी सुबह मुझे घूमते हुए कहते कि तुम्हें निराला जैसा बनना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बचपन काफी स्वाभाविक रहा लेखन उस वक्त कहीं नहीं था। और जब पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली में हुआ उसके बाद अंग्रेजी मीडियम में मेरा दाखिला हुआ। उस वक्त यह माना जाता था कि अगर अच्छी शिक्षा पानी है तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना होगा। और उसे वक्त मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि पांचवी क्लास तक मैं अंग्रेजी पढ़ी नहीं थी मैं हिंदी मीडियम से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। हमारे वक्त में आठवीं कक्षा के जो नंबर आते थे उसके आधार पर यह तय किया जाता था कि आप किस विषय में जाएंगे उसे वक्त अच्छे नंबर आने का यही एक विकल्प था कि आप विज्ञान लेंगे। दसवीं, ग्यारवीं तक यही चलता रहा। उन दोनों मेरे एक मित्र थे अखिलेश उन्हें लिखने का काफी शौक था। तो उन दिनों मैं भी यह कहानी लिखी और एक पत्रिका में भेज दी। और रिजल्ट आने के बाद कॉलेज की जब तलाश हुई और हमारे यहां यह माना जाता था कि अच्छा कॉलेज वही है जो पास में है। मैं साइंस का विद्यार्थी था और मुझे मैथ्स काफी अच्छी लगती थी तो उस वक्त मैथ्स ओनर ले ली। इत्तेफ़ाक हुआ कि उन दिनों वह कहानी छप कर आ गई। मेरे नजदीकी दोस्तों में किसी को कहानी साहित्य से कुछ खास लगाव नहीं था। तो मेरे मित्र अखिलेश ने कहा कि तुम अपनी रचना अपने यहां के हिंदी के टीचर को दिखाओ। और उस वक्त हमारे हिंदी के महेंद्र कुमार जी अध्यक्ष थे तो मैंने पूछा कि वह कहां मिलेंगे तो एक जगह बताई की हिंदी के सभी लोग उस जगह बैठे हैं । और मैं गया उनको दिखाने के लिए और वहां कैलाश वाजपेई जी थे नरेंद्र कोहली थे। तो उन्होंने कहा कि यह देखो नरेंद्र कहानी लिखी है इसने भी और उन दिनों में नरेंद्र कोहली काफी चर्चित चेहरा थे। और फिर उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू की तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो और मैंने जवाब कहा कि सर मैं क्लास में आता हूं सामने क्लास होती है मैं रोज क्लास में जाता हूं। उन्होने कहा हिंदी ऑनर्स की क्लास तो ऊपर होती है तब मैंने उन्हें बताया कि मैं हिंदी ऑनर्स से नहीं हूं मैथ्स ऑनर्स से हूं। और फिर उन्होंने वहां से मुझ पर एक जादू सा डालना शुरू किया और कहा कि तुम भी हिंदी ऑनर्स ले लो। और यह कहा कि तुम्हारी कहानी अभी कच्ची है भाषा की दृष्टि से। और उस वक्त 1966 में एक बड़ा आंदोलन देश में था हिंदी के लिए। और पिताजी का भी यही मानना था कि मैं एक बार कैसे भी ग्रेजुएट हो जाऊं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आकर सरकारी घर मिल जाए। फिर उसके बाद में मैंने भी सोचा कि जीवन में काफी चुनौतियां ली है और इसे भी इसी तरीके से लेते हुए मैंने अपना विषय बदल दिया। और एक कहानी से मेरी धारा बदल गई कि विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य में आ गया । और पहले वर्ष में जो परीक्षाएं हुई क्योंकि मुझे हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं थी तो मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ। यही सब कुछ सोच रहा था तब नरेंद्र कुमार मेरे पास में आए और पूछने लगे क्या हुआ रिजल्ट अच्छा नहीं गया तुम्हारा। फिर मैंने उन्हें बताया कि आप देख लीजिए कि अब मुझे लगता है कि मेरा कैरियर इसमें खराब हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा की चिंता मत करो अब जिम्मेदारी हमारी भी हैं। और यही उनकी सोच भी थी और जिस लगन के साथ उन्होंने मुझे पढ़ाया और अपना वक्त दिया तो सेकंड ईयर में यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए तब मेरे 56% आए। फाइनल ईयर में मेरे 65% बने और लड़कों में पूरी यूनिवर्सिटी में मैं अकेला था जिसके फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा नंबर हो। क्योंकि आपने लेखन की बात की और मैं कविताओं की बात करूं तो हमारे सरकारी स्कूल के डॉक्टर बत्रा हुआ करते थे अंग्रेजी के वह हमें पढ़ाया करते उस वक्त उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी मैं अंग्रेजी में उस एक कविता लिखी थी। पढ़ने का शौक रहा ,कबीर को जब पढ़ा और प्रसाद इन दोनों से मैं काफी प्रभावित हुआ जबकि इन दोनों का लेखन बिल्कुल विपरीत है। और व्यंग्य में जिस प्रकार से मेरी रुचि जागृत हुई वह वजह कबीर को मानता हूं। कबीर के कारण ही व्यंग्य शुरू किया और मेरा झुकाव व्यंग्य की तरफ हुआ। और जब प्रसाद के नाटकों को भी पढ़ा । व्यंग्य की तरफ झुकाव बढ़ता रहा। और कविताएं भी लगातार लिखी गीत भी लिखा। मेरी मूल विद्या व्यंग्य रही और आज भी है लेकिन मैंने यह समझा कि आपको कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए मतलब की साहित्य की अन्य विधाओं का सृजन होना चाहिए। व्यक्ति की अपनी एक मुख्य विद्या होती है लेकिन अगर हम उदाहरण भी लें परसाई, शरद जोशी, श्री लाल शुक्ला सभी ने अपना आरंभ कविता से किया। और यह भी एक युवावस्था की ही बात है कि युवावस्था जो होती है तितलियों के पीछे भागने की होती है और रंग बिरंगी तितलियां फिर कविताएं लिखवा देती हैं। एक जगह मैंने कहा भी था की परसाई के कारण जबलपुर व्यंग्य की मातृभूमि है। और मेरी मातृभाषा जो है वह व्यंग्य है।
अरमान :- पाठक की रुचि की बात करें तो उन्हें व्यंग्य पढ़ने में काफी आनंद आता है क्योंकि व्यंग्य अपने आप में काफी कुछ समेट लेता है आपकी नजर में साहित्य की विधा व्यंग्य क्या है?
प्रेम जनमेजय:- आपने एक चीज साहित्यिक विधा कहा अगर हम इस पर बात करें तो हम यह कह सकते हैं कर्ण को राजा बना दिया गया था लेकिन उसको उस तरीके से राजा माना नहीं जाता था। और जबकि अगर हम व्यंग्य की बात करें तो इसमें वह सारी चीज हैं जो एक विधा के अंदर होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही रचनाकार लिखने लगता है और उसको लगने लगता है कि इसके कारण मुझे कहीं ना कहीं सीमित कर दिया जा रहा है मुझे व्यंग्यकार माना जा रहा है, साहित्यकार माना नहीं जा रहा। मैं परसाई का उदाहरण देना चाहूंगा आप इसमें श्री लाल जी का भी उदाहरण ले सकते हैं परसाई को अगर आप पढ़े तो आप यह महसूस करेंगे कि उनका आरंभिक लेखन तो आप यह देखेंगे कि परसाई विद्या के लिए ही लड़ रहे हैं। दूसरी चीज के लिए लड़ रहे हैं की हास्य और व्यंग में जमीन आसमान का अंतर है उनका यह मानना है कि हर व्यंग में हास्य की कोई आवश्यकता नहीं है। और वह कहते हैं कि शिष्य हास्य कि मुझे उसे वक्त ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे कान में तेजाब डाल दिया। इसलिए वह व्यंग्य को उससे अलग करते हैं और वह व्यंग्य की ताकत को पहचानते हैं। कहीं जगह वह कहते हैं कि व्यंग्य को शुद्र माना जाता था वह ब्राह्मण हो गया है , ब्राह्मण नहीं है वह क्षत्रिय है लड़ता है। फिर वह प्रगतिशील हो जाते हैं और आप यह भी मानेंगे कि जो प्रगतिशील पत्रिकाएं हैं उन्होंने कभी नहीं माना की व्यंग्य कोई विधा है। और उन लोगों में कोई भी नहीं मानता तब परसाई ने कहना शुरू किया की व्यंग्य विधा नहीं स्पिरिट है। इस तरह से इसकी परिभाषाएं बनी की व्यंग्य अग्रिम पंक्ति में खड़ा योद्धा है। इसी तरीके से व्यंग्य अपना एक स्वरूप ग्रहण कर रहा है तो यह चीज होती है की शुरुआत में कहा जाता है कि व्यंग्य विधा है और बाद में रहते हैं की व्यंग्य विधा नहीं यह कैसे हो सकता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा की व्यंग्य की अपनी अलग पहचान है और लोग उस पर बात नहीं करते व्यंग्य का पाठक वर्ग अलग होता है व्यंग्य में कथानक अलग होता है व्यंग्य की भाषा अलग होती है उसका शास्त्र आलोचना शास्त्र अलग होता है । व्यंग्यकार का उद्देश्य अलग होता है। और मैं एक बात और परसाई की लूंगा उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध को लेकर सामान्यत किसी भी समकालीन रचनाकार के विषय में प्राप्त और प्रगत भाषा से किया जा सकता है लेकिन हिंदी में शायद मुक्तिबोध ऐसे कवि इनके बारे में चर्चा करते वक्त प्राप्त भाषा काम नहीं चलता। इसका मतलब यह है कि जो चीज अलग है अब मुक्तिबोध दूसरों से क्यों लगे कि उनके लिए आप प्राप्त भाषा से काम नहीं चला सकते प्रगत भाषा से भी काम नहीं चला सकते इसीलिए व्यंग्य को भी आप प्राप्त भाषा से नहीं समझ सकते । व्यंग्य के लिए एक अलग भाषा एक पूरे अलग ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो रचना है जिसे ना तो मैं कहानी कह पा रहा हूं और ना ही मैं उसे निबंध कह पा रहा हूं वह मुझे अलग तरीके से ले जा रही है और सबसे बड़ी बात होती है व्यंग्य में जो हस्तक्षेप बीच-बीच में जिस तरीके से रचनाकार हस्तक्षेप करता है मुझे लगता है व्यंग्य का एक अलग स्वरूप है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे आलोचक हुए नित्यानंद तिवारी उनसे भी मेरी इस बारे में बात हुई वह एक सवाल करते हैं क्या हरिशंकर परसाई ने यह संभावना नहीं की कहानी और निबंध एक हो सकते हैं एक दूसरे से मिले-जुले हो सकते हैं। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं वह परसाई की रचनाओं में व्यंग्य का विधान है इसकी संरचना व्यंग्य की संरचना है और हमारा आने वाला यथार्थ अगर पूरी तरीके से समझना है तो व्यंग्य के विधान के बिना नहीं समझ सकते। और मैं एक जगह अपनी बात कहते हुए कहा था कि यह व्यंग्य का संक्रमण काल है क्योंकि व्यंग्य अपनी पहचान 21वीं सदी में धीरे-धीरे बना रहा है। बीते कुछ समय पहले मुझे मॉरीशस में बुलाया गया जो विश्व हिंदी सचिवालय है उन्होंने न्योता दिया कि आपको व्यंग्य को लेकर कार्यशाला करनी है मैंने सोचा कि यहां ही कोई व्यंग्य की कार्यशाला नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां महात्मा गांधी संस्थान के जो छात्र है वह व्यंग्य की समझ रखते हैं। जो चीज मैंने कभी भारत में नहीं कि उस विषय के साथ में मॉरीशस में अपनी बात रखी और अपनी बात में मैंने बताया व्यंग्य की अवधारणा क्या है व्यंग्य का स्वरूप क्या होता है। उसकी परंपरा क्या होती है, व्यंग्य की भाषा क्या होती है ,व्यंग्य का उद्देश्य क्या होता है ? इन विषयों के ऊपर मैंने वहां 50-50 मिनट के वक्तव्य भी दिए। और उसके बाद में उन्होंने मुझसे सवाल किया ऐसा नहीं रहा कि वह सिर्फ बैठे और सुनते रहे। और हमारे यहां इस तरीके के प्रयत्न नहीं हो रहे हैं। आजकल हम यहां अपने आप को व्यंग्यकार समझ लेते हैं कि अखबार में छपने तक यानी कि वह व्यंग्यात्मक रचना नहीं है वह व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हैं। देखिए तीन चीज हैं रचना में व्यंग्य और एक होती है व्यंग्य रचना यानी कि व्यंग को रचना के रूप में लेकर आना। फिर तीसरे पर आती है व्यंग्यात्मक टिप्पणियां मेरा ऐसा मानना है कि अधिकांश स्तंभ लेखन जो है वह व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। मौजूदा वक्त में भी अगर हम देखें तो लोग बिना राजनीति को समझे व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। किस तरह की चीज किसी भी विद्या के लिए बहुत खतरनाक है।
अरमान:- आपने व्यंग्य विधा में एक-एक चीज को खंगालते हुए स्पष्ट रूप से उसका विवरण दिया और एक चीज आपने बताई के कई बार व्यंग्यकार अपने आप को सीमित महसूस करने लगता है। मैं एक बार आलोक पुराणिक जी से बात कर रहा था तो वह कहते हैं कि व्यंग्यकार को पत्रकार का दर्जा हासिल है एक कवि कवि हो सकता है वह पत्रकार नहीं हो सकता लेकिन जो व्यंग्यकार है वह पत्रकार हो जाता है।
प्रेम जनमेजय:- बात यह है कि जो परसाई, शरद जोशी उस समय के जो तत्कालीन स्तंभ लेखक थे उनकी दृष्टि से यह कह सकते हैं कि उन्होंने स्तंभ लेखन किया और पत्रकार की भूमिका भी निभाई और मेरा मानना यह है कि जब आप कहीं पर चीजों को सीमित कर देते हैं अगर आप उस समय का लेखन पढ़ें हैं उस समय काफी ज्यादा राजनीतिक संदर्भ भी इस्तेमाल हैं जो आज प्रहारक नहीं है दूसरी तरफ जो परसाई और शरद जोशी जैसे लेखक हैं जिन्होंने स्तंभ लेखन किया और अगर आप श्रीनाथ शुक्ला को देखें और इसी तरह से रवींद्रनाथ त्यागी को देखें। अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना ही की श्री लालजी ने जोशी और परसाई की आप उस वक्त यह देखेंगे कि हमारे समय में जो भ्रष्टाचार में नैतिकता इतनी भी नहीं मिलती चारों तरफ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है किसी भी तरह के नैतिक मूल्य नहीं मिलते हैं । आप स्वयं जानते हैं साहित्य का भूगोल इसके मुकाबले में कहीं ज्यादा जटिल है। व्यंग्य का एक स्वरूप और भी है पांच से छह पन्नों का एक व्यंग्य हो सकता है कहीं जगह कुछ शब्दों का व्यंग्य छपता है और इसका उद्देश्य क्या होता है माहौल, मजाक, कटाक्ष और इस क्षेत्र में ढाई तीन दर्जन नाम ऐसे हैं जो बहुत चर्चित हैं और बहुत छपते हैं अच्छा भी लिखा है उन लोगों ने बहुत सारा लिखा है कुछ ने 20-20 किताबें भी लिखी है मगर मैं देखता हूं लेखक का अपना रवैया क्या है उसका दृष्टिकोण क्या है व्यंग्य तो सामाजिक आलोचना है कुछ भी खाने लिखने से पहले अपना स्टैंड साफ करें और इन सब से मैं बहुत उत्साह जनक की स्थिति नहीं पता स्तंभ लेखन की। क्योंकि अधिकांश व्यंग्य लेखन से प्राण गायब है । मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहूंगा एक अखबार से मुझे कॉल आता है और वह मुझे कहते हैं कि हम व्यंग्य का स्तंभ शुरू कर रहे हैं और मुझसे कहा गया कि आप लिखिएगा हमारे लिए तब मैंने उनसे कहा था कि मैं स्तंभ लेखन नहीं करता तब मैंने कहा कि मैं व्यंग्य रचना के रूप में आपको दूंगा और उन्होंने कहा हां बिल्कुल हम भी वही चाहते हैं। और इसमें मैंने जितनी भी चीज़ लिखी है सारी की सारी व्यंग्य रचना के रूप में लिखी है और अगर उसमें कहीं तात्कालिक संदर्भ भी लिए हैं । और यह तकरीबन तीन साल तक चला था। मैंने यह चीज समझी और मुझे यह एहसास होने लगा कि मेरा लेखन सिर्फ तीन सौ - चार सौ शब्दों में सीमित नहीं होना चाहिए । मैं उसे रचना के रूप में नहीं ले पाऊंगा मेरा यह मानना है कि मैं खुद को इन सब चीजों से थोड़ा अलग रखता हूं। आप अपनी जो बात कहना चाहते हैं कहते हैं प्रासंगिकता ऐसी प्रासंगिकता होनी चाहिए जो बाद में भी आपके सामने आए परसाई की प्रासंगिकता प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं । जो लोग अपना दिमाग नहीं बदल सकते वह कुछ नहीं बदल सकते। आज का उदाहरण लेते हैं जो मोबाइल फोन इंटरनेट है क्या वह पर सही के समय था नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जीवन मूल्य होते हैं ,शाश्वत होते हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। एक आपको उदाहरण देता हूं बात कही गई कि स्त्रियों के बाल ही उनके आभूषण होते हैं भूख बहुत लगती है हैं ,धनहीन एवं अनेक तरह की ममता दुखी रहती है , पुत्र माता-पिता को तभी सम्मान देता है जब तक उन्हें विवाह पुराण जब तक उन्हें अपनी स्त्री का मुंह नहीं दिख जाता, ससुराल उसे प्यारी लगती है सभी पारिवारिक संबंध शत्रु हो जाते हैं बहुत झूठ बोलते हंसी दिल्लगी करने वाले को गुडी आदमी समझा जाता है"सब सुनकर आपको लगेगा कि मैं आज के समय की बात कर रहा हूं यह बात सच है कि आज ऐसा हो रहा है के ससुराल में लड़के को पैसा अच्छा लगता है लेकिन यह सब लिखा है छह सौ साल पहले और यह तुलसीदास ने कहा है अबला कच भूषन भूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा॥ सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता। मति थोरि कठोरि न कोमलता॥ ये तुलसी का लिखा हुआ है और आज भी प्रासंगिक है। 1995 और आज के भारत में आज जमीन आसमान का अंतर है उसे वक्त 2G की शुरुआत हुई थी और आज 5G का समय और उसके बाद में सोशल मीडिया में प्लेटफार्म शुरू हुआ। और परसाई का निधन इन सबसे पहले हो गया था यानी कि उनके निधन तक सोशल मीडिया नहीं था। अब तो ए आई का जमाना है और मैंने ए आई प्लेटफॉर्म पर कहा कि मुझे परसाई की तरह व्यंग्य लिखना है विशेष शिक्षा की विसंगतियां उसने निकाल कर दे दिया ।आज के लिए सब पढ़ना ,लिखना कितना सरल हो गया है । अगर उस नजरिए से देखा जाए। तो यह चुनौतियों का समय है कि नहीं। उस चीज में आपको लेखक का चिंतन नहीं मिलेगा मैं आपको एक रचना कोई बात रहेगी और दूसरी रचना में एक अलग बात महसूस होगी। श्री लाल जी ने कहा था दृष्टिकोण होना चाहिए उनके समय शरद जोशी की अलग दृष्टि थी लेकिन इन सब चीजों में आपको किसी भी तरह दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। परसाई अपनी दृष्टि के कारण प्रगतिशील होने के कारण आपातकाल का समर्थन करते है। और शरद जोशी को अगर आप देखेंगे तो उनकी दृष्टि है सत्ता विरोध की। वह कांग्रेस का भी विरोध करते हैं बाद में जो जनता सरकार बनती है उसका भी विरोध करते हैं। और इस कथन में मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। और परसाई के समर्थन में उनका एक प्रगतिशील खेमा है और परसाई मेरी पाठशाला है मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और उस पाठशाला में उन्होने मुझे सिखाया है कि तुम विरोध भी कर सकते हो। मैंने उनसे सीधे सवाल भी किए हैं और 1975 के बाद में मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया था तब मैंने उनसे पूछा था क्या परिस्थितियों व्यक्ति को विवश नहीं करती है जो उसके मन में है वह उसे वैसा नही लिखता है तब उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रेम तुम मुझे सीधा आपातकाल में मेरी भूमिका की बात क्यों नहीं करते यानी कि इसमें उन्होंने मुझे डांट कर अलग नहीं किया उन्होंने शालीनता से उस चीज का जवाब दिया। और इसी वजह से मैं परसाई को पसंद करता हूं मैं युवा लेखक था और मैं हाथ मसलते हुए उनसे कहा कि आपने इतना लिख दिया है अब हम क्या लिखेंगे उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि नहीं प्रेम हमने अपने पिता को नंगा नहीं देखा है तो कहने का मतलब उनका इस कथन से था कि हमारे यहां वह साहस नहीं था तुम्हारी पीढ़ी में वह साहस है। वह कहीं पर भी इस तरह का घमंड नहीं पालते हैं कि जो मैंने लिख दिया वही सब कुछ लिख दिया। परसाई का दृष्टिकोण अलग है उन्हें उसे दृष्टि से देखना चाहिए और शरद जोशी का अपना एक अलग दृष्टिकोण है। श्री लाल जी का अलग दृष्टिकोण है । उनसे जब पूछा जाता है कि आप कहां खड़े हैं तो कहते हैं कि ना तो मैं दाएं और बाएं खड़ा हूं पटरी के उसे तरफ जो वंचित खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूं। उनका विचार है। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं शरद जोशी और परसाई से अपने विचार ग्रहण किए हैं। कबीर में साहस था उन्होंने लिखा कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय। ता चढि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय। और उसी तरह ब्राह्मण को भी कहा जो तूं ब्राह्मण , ब्राह्मणी का जाया आन बाट काहे नहीं आया। यह साहस था उन्हों में लेकिन आज हमारे सामने बहुत खतरे हैं। और एक बार विश्वनाथ त्रिपाठी जी से व्यंग्य यात्रा के दौरान जो मैंने इंटरव्यू लेते हुए पूछा क्या परसाई आज के वक्त होते इस तरह से विरोध करके लिख सकते थे। क्योंकि मेरा मानना है विरोध विसंगत समय में आपको नपुंसक होने से बचाता है। और जो व्यंग्य है उसका एकमात्र हथियार विरोध है। अगर उसमें विरोध नहीं है तो वह व्यंग्य नहीं है। और इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि शायद नहीं या लेखक के रूप में कोई और मध्यम ढूंढ लेते। तो आप यह देखिए कि समय के अनुसार चीज बदलती रहती है। लेकिन व्यंग्य तभी व्यंग्य रहेगा जब उसमें विरोध हो। एक बार नामवर जी से बात हो रही थी तब उन्होंने कहा था व्यंग्य के ऊपर जो बिंदी है ये डंक है यह ना हो व्यज्ञ हो जाएगा। जब तक व्यंग्य में डंक नहीं होगा तब तक वह व्यंग्य नहीं होगा यानी कि उसमें वह डंक होना बहुत जरूरी है इसमें वह उसे मार की बहुत जरूरत है व्यंग्य कोई प्रेम गीत नहीं है। आप बताइए क्या किसी भी व्यंग्यकार ने प्रेम गीत लिखा है। व्यंग्यकार प्रेम गीत लिख ही नहीं सकते। व्यंग्य तो सीधा विरोध प्रकट करता है। व्यंग्य सुशिक्षित मस्तिष्क की विधा है सुशिक्षित का मतलब यह नहीं की पी एचडी की जाए। व्यंग्य कि अगर आपको परख नहीं है फिर वह आपके ऊपर से निकल जाएगा आप उसकी पकड़ नहीं कर पाएंगे यह मैं कहता हूं अगर व्यंग्य के पाठक को उसकी पकड़ नहीं होगी तो वह सपाट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हू हास्य व्यंग्य को इससे अलग क्यों किया जाता है हमारे जीवन में हास्य कब आया यह तो आदिमानव के समय से है जो चीज मिल जाती थी खुश हो जाता था हंसता था । चोट लग जाती तो रोने लगता था। जब आदिमानव धीरे-धीरे आगे बढ़ा बुद्धि उसके अंदर थी पर ज्ञान नहीं था। मैं कहता हूं व्यंग सभ्य मानव की भौतिकता का उद्घोष है। सभ्य मानव के जीवन में व्यंग्य था आदिमानव के जीवन में व्यंग्य नहीं था।
अरमान:- पाठक के सोचने की क्षमता व्यंग्यकार की लेखनी पर किस तरीके से प्रभाव डालती है ?
प्रेम जनमेजय:- बिल्कुल पाठक लेखक के ध्यान में रहता है मुख्यतः दो चीजों से लेखक प्रभावित होता है समय से और पाठक से। अगर मैं कविता लिख रहा हूं तो मेरे ध्यान में मेरे मन में यह हमेशा से रहेगा कि इस कविता का पाठक कौन है। अगर मैं प्रेम गीत लिख रहा हूं तो मेरे ध्यान में यह रहेगा कि किस तरीके से मौजूद प्रेम गीत चल रहे हैं। ग़ज़ल आती है ,हिंदी में गाने आएंगे तो यह समझ आने लगता है कि भाई पाठक उसे चीज को चाह रहा है वह मांग पाठक की है। यही चीज व्यंग्य के साथ भी है। हर आदमी के मन में जो आजादी के बाद मोह भंग हुआ है उसमें गुस्सा था और इसी गुस्से के वजह से व्यंग्यकार अपना व्यंग्य सामने लेकर आता है। और आप देखिए जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तब लोगों को क्या लगता था कि भाई अब आजाद हो चुके हैं हम और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन क्या सब कुछ ठीक हुआ? आदमी को लगने लगा कि मैं तो दो रोटी के लिए मरता जा रहा हूं और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दो की चार चार की आठ और , आठ की सोलह कर रहे हैं. पहले एक राजा हुआ करता था अब संसद में इतने राजा हुआ करते हैं। मैं इन सबको नेता कहा करता था लेकिन अब यह सारे के सारे सत्ता कर्मी है। सभी लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं कोई भी नेता नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह वाकई में देश प्रेम के लिए कुछ कार्य हो रहे हैं तो यह हमारा बुलावा है यह सब वोटो की राजनीति की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो मोह भंग की बात कही कमलेश्वर वह कहते हैं उनका व्यंग्य संग्रह है उसके उन्होंने भूमिका लिखी है और बाकायदा यह कहा है की किस तरह से जब मैं इलाहाबाद से यहां पर आया कि उस वक्त मेरी चीजों को देखने की समझने की उस वक्त विसंगतियां थी अपने समय को समझने की सबसे बढ़िया जो दृष्टि है व्यंग है। आज के वक्त आप बताइए कि क्या माहौल है मैं कहता हूं कि आज बाजार के कारण हर एक चीज प्रोडक्ट बन चुकी है सभी चीजों को बेचा और खरीदा जाने लगा है। और मैं कहता हूं कि आज के वक्त में न्याय भी प्रोडक्ट बन चुका है क्या आपके पास में इतनी हिम्मत है की सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस लड़ सकें क्या न्याय मिलेगा। जो अपने आप को हमारा जन सेवक कहते अगर उनके ऊपर कुछ आ जाए उनके पास वकीलों की भरमार है रात को कार्रवाई होकर कोर्ट भी खुलवा सकते हैं। यही तो एक तरह का प्रोडक्ट हो गया हर एक चीज को उद्योग से जोड़ा जा रहा है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि पत्रकारिता भी व्यापार हो रही है क्या दिखेगा कौन कितना लिखेगा सब पहले से तय है। जो एक वक्त में पत्रकारिता मिशन हुआ करता था आज क्या हाल है। बहुत सी जगह पर जो संपादक है वह संपादक नहीं रह गया है वह एक मैनेजमेंट है। मैं इसको यही कहूंगा कि हमारे वक्त के मौजूदा वक्त के हर एक वक्त का जो रचनाकार है उसे वह पर्दाफाश करना चाहिए। चीज में और कहना चाहूंगा कि वंचित के ऊपर कभी भी व्यंग नहीं करना चाहिए मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूं कि हमारे मिलने वाले थोड़ा गुस्से में थे मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि मैं जब आ रहा था तो ₹10 किराया हुआ थोड़ा सा आगे छोड़ने के लिए कहा तो ₹15 हो गए सब के सब भ्रष्टाचारी हो गए हैं तो मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह गलती तुम्हारी है कि पहले तुमने जगह तय नहीं की और मैंने कहा कि अगर वह भ्रष्टाचार कर भी रहा है तो आखिर कितना कर रहा है कि थोड़ी बहुत उसके घर में खुशहाली हो जाए। हो सकता है कि वंचित भी थोड़ी बहुत बेईमानी करें लेकिन वह आखिर कहां तक करेगा एक सब्जी वाला जो है वह थोड़ी ऊपर नीचे करेगा। ऐसा क्यों करेगा कि अगर उसके दो लड़के हैं एक को दूध मिल रहा है तो वह चाहेगा कि दूसरे को भी दूध मिले। जो आदमी संपन्न है वह भ्रष्टाचार किसके लिए करता है वह अपनी अय्याशी के लिए करता है।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने हेतु आपका बहुत आभार ।
प्रेम जनमेजय - धन्यवाद
Dr.Sanjyukta Dasgupta
विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षिका रही वरिष्ठ साहित्यकार और कलकत्ता विश्विद्यालय की पूर्व डीन डॉक्टर संजुक्ता दासगुप्ता से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
परिचय
डॉक्टर संजुक्ता दासगुप्ता
डॉ. संजुक्ता दासगुप्ता, प्रोफेसर और पूर्व प्रमुख अंग्रेजी विभाग और पूर्व डीन, कला संकाय, कलकत्ता विश्वविद्यालय फुलब्राइट पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप (यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, चैपल हिल) और फुलब्राइट स्कॉलर इन रेजिडेंस (स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, ओस्वेगो) ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल फेलोशिप, जेंडर स्टडीज फेलोशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ट्रांसलेटर फेलोशिप, बीसीएलटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, नॉर्विच, आदि प्राप्त कर चुकी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के निमंत्रण के अलावा दासगुप्ता ने यूएसए, यूके, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया और व्याख्यान दिए हैं। उन्होंने जूरी सदस्य और कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया 2018 में, पोलैंड के क्राको में जगियेलोनियन विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। वह सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, कोलकाता में अंग्रेजी विभाग की मानद विजिटिंग प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कोलकाता के साहित्य भाषा और संचार में उत्कृष्टता केंद्र (CELLCS) के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष हैं। इंटरकल्चरल पोएट्री एंड परफॉर्मेंस लाइब्रेरी, कोलकाता की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष हैं। अक्टूबर 2024 में उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफ़ोर्ड सेंटर फ़ॉर हिंदू स्टडीज़ (OCHS), ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में टैगोर के लेखन पर दो व्याख्यान दिए। संजुक्ता दासगुप्ता को 2019 में IWSFF महिला अचीवर्स अवार्ड, 2020 में WEI कमला दास कविता पुरस्कार, 2022 में ETHOS साहित्य पुरस्कार, 2024 में मुक्तधारा टैगोर सम्मान मिला। उन्हें 2024 में गवर्नर स्क्रॉल ऑफ़ ऑनर और CLRC नेशनल लाइफ़टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। दासगुप्ता कवयित्री, लघु कथाकार, आलोचक और अनुवादक हैं और 27 प्रकाशित पुस्तकें हैं: हक्सले और हेमिंग्वे के उपन्यास: वास्तविकता के दो धरातल में एक अध्ययन, प्रतिक्रियाएँ: चयनित निबंध, स्नैपशॉट (कविता), दुविधा (कविता), पहली भाषा (कविता), अधिक प्रकाश (कविता) उनकी कहानियाँ (अनुवाद), मणिमहेश(अनुवाद), द इंडियन फैमिली इन ट्रांजिशन (सह-संपादित SAGE)। मीडिया, जेंडर और भारत में लोकप्रिय संस्कृति: परिवर्तन और निरंतरता पर नज़र (सह-लेखक, SAGE, 2012), टैगोर: एट होम इन द वर्ल्ड (सह-संपादक SAGE 2013), रैडिकल रवींद्रनाथ: टैगोर के उपन्यास और फिल्मों में राष्ट्र, परिवार और जेंडर। (सह-लेखक, ओरिएंट ब्लैकस्वान 2013), स्वदेश- टैगोर के देशभक्ति गीत (अनुवाद, विश्व भारती प्रकाशन प्रभाग, 2013), गाली और अन्य लघु कथाएँ (दासगुप्ता बुक कंपनी, 2013) टैगोर की ओर निबंधों का संग्रह (संपादन परिचय के साथ - विश्व भारती प्रकाशन, 2014), गोलपो संकलन: अनुवादित समकालीन बंगाली लघु कथाएँ (साहित्य अकादमी नई दिल्ली 2016, दूसरा संस्करण 2018), लक्ष्मी अनबाउंड (कविता) 2017. ऑस्ट्रेलियाई महिला लेखन के लिए जगह का दावा (सह-संपादित) प्रकाशक: पान मैकमिलन, यूएसए), 2017, सीता की बहनें (कविता) हवाकाल 2019। इन मेमोरियम: स्वर्ण और पलटाका में टैगोर की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद (साहित्य अकादमी), 2020, वह: भारतीय महिला लेखकों की लघु कथाएँ (संपादित। साहित्य अकादमी 2021), अनबाउंड नई और चुनिंदा कविताएँ एड जयदीप सारंगी, संघिता सान्याल (ऑथरप्रेस 2021), यह घर से शुरू होती है और अन्य लघु कहानियाँ (विरासत, 2022), भारतीय लोक कथाएँ (साहित्य अकादमी, 2022 में संपादित), अदम्य द्रौपदी (कविता), हवाकाल, 2022, विविधता: चयनित समीक्षाएँ, पत्र, लेख और साक्षात्कार (2000-2022) ऑथरप्रेस, 2023, एकलव्य बोलता है (2023)। वह फैमिलीज ए जर्नल ऑफ रिप्रेजेंटेशन्स (2000-2012) की प्रबंध संपादक थीं।
अरमान:- आज की तारीख में साहित्य में आप एक जाना माना नाम है लेकिन आपकी लेखनी की शुरुआत किस तरह हुई?
डॉ. संजुक्ता दासगुप्ता:- अगर साहित्यिक सफर की बात की जाए तो अब तो उसे काफी वक्त बीत चुका है लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो यह सब शुरू हुआ मेरे स्कूली वक्त से मिडिल स्कूल ,हाई स्कूल के बीच में । उस वक्त कुछ कविताएं ,कहानियां पढ़ना शुरू की और जो स्कूल के सिलेबस की जब किताबें पढ़ी जाती और उसमें कुछ कहानी होती तब भी एक उसमें दिलचस्पी बनती थी और खासकर लघु कथाओं ने मुझे काफी प्रेरित किया और लिखना भी शुरू किया । ज्यादातर लेखन अंग्रेजी में है क्योंकि बचपन से ही स्कूल हार्डकोर इंग्लिश मीडियम रहा और स्कूल में दूसरी भाषाओं के साहित्य पर कुछ खास चर्चा नहीं हुआ करती थी । वह वक्त था 1970 का। इस वजह से जो मेरी लिखने की शैली रही वह अंग्रेजी की रही। और घर की बात करें तो मैं बंगाली बोला करती और हिंदी में बोल लेती हूं जितना हम आपस में बात करके एक दूसरे को समझ सके। इस दौरान जब मैं स्कूल में थी तो मैं अपने डैडी को कहा कि मैं राइटर बनना चाहती हूं। और मेरे माता-पिता दोनों ही टीचिंग लाइन से जुड़े थे पापा कॉलेज में और मम्मी स्कूल टीचर थी और उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली में आपको सबसे पहले जॉब की सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए ना कि अपने दूसरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और उनकी सलाह मुझे हमेशा से यही रही की सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ काम के बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही यह कहा कि नौकरी लगने के साथ में तुम कर सकती हो यानी कि दिन में अगर आप काम करते हैं नौकरी करते हैं तो रात में यह आपका शौक जो है उसे आप निभा सकते हैं। और जब इन सब के बाद में मेरी स्कूल पूरी हुई और मैं कॉलेज आई और पढ़ाई की ऑनर्स में और कोलकाता यूनिवर्सिटी में जब मेरा दाखिला हुआ और वहां से मैं पीएचडी भी की। और उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली रिसर्च करने की भी तो इस तरीके से एकेडमिक्स चला रहा और उसके साथ-साथ ही साहित्य सृजन भी बरकरार रहा। लेकिन जो मेरी शायरी थी उसमें मुझे इस तरीके की चीज महसूस हुआ करती कि यह बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है और इसे शेयर करने का कोई मतलब इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा था। जब एक वक्त पर मुझे यह रिलाइजेशन हुआ कि मैं सिर्फ अपने आपके लिए नहीं लिख रही हूं मैं सोसाइटी के लिए लिख रही हूं मैं समाज के प्रति अपना एक दायित्व दे रही हूं तो उसके बाद में मैंने इसे सुचारु रूप से और ज्यादा करने का प्रयास किया। और एक फ्रेज है अंग्रेजी में जिसे हम जनरल स्टडीज में इस्तेमाल करते हैं "द पर्सनल इस द पॉलिटिकल" व्यक्तिगत जो है वह भी राजनीति है तो आइडेंटिटी के बारे में हर चीज में राजनीति हो सकती है यह एक फ्रेज है। जैसे कि जो टॉपिक्स जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया जो विषय थे इक्वलिटी अनइक्वलिटी तो इनके ऊपर मैंने लिखना और पढ़ना बहुत ज्यादा किया। और मुझे लगा कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ योगदान दूं तो मुझे काफी खुशी होगी। और मैं इसके बारे में काफी पढ़ाया भी है । अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं मैं जनरल स्टडीज पढ़ती थी एचडी गाइडेंस के अंदर तो उसके बाद में कहीं ना कहीं यह मेरा मुख्य विषय बन गया। और मेरी लेखनी के अंदर यह चीज साफ नजर आती है। 2023 के अंत में और 24 की शुरुआत के मध्य मेरी कविताओं की एक किताब प्रकाशित हुई "एकलव्य" उसके बाद से मैं कास्ट की तरफ शिफ्ट हुई और हमारे देश में कास्ट बड़ा मुद्दा है। और अगर मैं बात करूं एक और विषय पर अगर हम महिलाओं की बात करें तो उसे तो हर जगह से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है फिर चाहे वह लोवर कास्ट हो या आप पर हर जगह उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है फिर चाहे वह हम घर की बात करें या बाहरी सामाजिक जीवन में। हम तो यह कह ही सकते हैं ना कि नारी जो है वह सभी क्लास से नीचे हो जाती है। वह एक अलग परेशानी हमारे को देखने को मिलती रही है या जैसे कास्ट की जो मैंने बात की या फिर रिलिजियस बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन लेकिन जो महिलाओं का उत्पीड़न है वह आपको हर जाति समाज वर्ग में आपको देखने को मिलेगा इसलिए मैंने कहा की नारी कहीं ना कहीं सारी क्लास से नीचे आ जाती है। इस तरह कि चीज देखते हैं यह समस्याएं हमारे इर्द-गिर्द नजर आती है तो यूं लगता है कि हमने विकास कहां किया हम तो और ज्यादा पीछे जाए जा रहे हैं। वह डेवलपमेंट फिर हमें सिर्फ फ्लाईओवर में नजर आता है। मैं अपने और लेखन की बात करूं तो मैं ज्यादातर क्रिएटिव राइटिंग करती हूं उसमें कोशिश रहती है कि एसथेटिक को डाला जाए राइटिंग में मैं थोड़ा क्राफ्ट भी डालती हूं। उस नजर से आर्ट भी है और क्राफ्ट भी है।
अरमान :- बहुत सही बात कही महिलाओं के उत्पीड़न के ऊपर हर जगह उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन हम यह देखते हैं जो अच्छी-अच्छी बातें उनके लिए कही जाती है वह सिर्फ किताबों में और ऊंचे मंचों से की जाती है लेकिन क्या ग्राउंड लेवल पर छोटे स्तर के ऊपर उनके लिए वाकई में काम हो रहा है और लोगों की मानसिकता में फर्क आ रहा है? क्योंकि फिर वह किसी भी धर्म से क्यों ना हो ।
डॉ. संजुक्ता दासगुप्ता:- यह वाकई बहुत गंभीर होता है और मेरी लघु कथाओं की दूसरी किताब उसमें मैं इस चीज का जिक्र किया है कि जो समस्याएं हैं उनकी शुरुआत घर से ही होती है। कि पहले सबसे पहले जो जेंडर इक्वलिटी की बात है वह आपके घर से होनी चाहिए। घर में तो आपके ऊपर कैमरे ,पत्रकारों के माइक नहीं लगे हुए हैं ना तो आसानी से आप उसे वक्त क्या करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। हम हिंदी में कहीं पितृसत्तात्मक समाज में हम हैं मेरी नजर में पितृसत्ता ने हमारा गला घोंट के रखा है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है यहां मर्द भी खुश नहीं है उन्हें भी एक अलग तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है हम अक्सर सुना करते हैं कि अगर तुम मर्द हो तो तुम अपने इमोशनल जो बातें हैं उसे खुले तौर पर नहीं करना मर्द हो तो तुम रो नहीं सकते अपने दिल की बात जो तुम्हारी है वह खुले तो और पर नहीं कर सकते और उन्हें बांधा जाता है उनको मजबूर किया जाता है कुछ चीज करने के लिए और यह एक व्यवस्था से बन चुकी है। हर जगह महसूस होगा अगर आप सिनेमा देखेंगे तो फिल्मों के अंदर भी मर्दों के जो भाषा इस्तेमाल होती है वह इतनी वायलेट की जाती है जिससे यह एहसास दिलाया जाए कि वह कितने हार्डकोर हो सकते हैं लेकिन क्या हर जगह सभी एक जैसे होते हैं क्या सभी लोग सभी मर्द इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वर्बल के साथ-साथ में फिजिकल बैलेंस को भी प्रमोट किया जाता है। और इस व्यवस्था ने हमारे दिमागों पर बहुत गहरा और बहुत ही ज्यादा ताकतवर पकड़ बना रखी है हम इसे ना तो एक बार में खत्म कर सकते हैं और ना ही लोगों को एक बड़े पैमाने पर इसे समझा सकते हैं यह जिस तरीके से शुरू हुआ इस तरीके से इसे समझने की जरूरत है यानी कि ग्राउंड लेवल से घर के स्तर से जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो वह अपना स्तर बढ़ाती भी है और जड़े भी मजबूत करती है। और यह विचारों के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभाव देता है और लोगों के विचारों को गुलाम करने की कोशिश इसमें हमेशा से रही है और अगर आपके विचार आजाद नहीं है तो व्यक्ति कभी आजाद नहीं हो सकता। और इस व्यवस्था से औरत तो परेशान है ही जैसा मैंने आपको बताया मर्द भी उतने ही पीड़ित है। यही चीज मैं अपनी कविताओं में और लघु कथाओं में मुखर होकर और खुले तौर पर दर्शाने की कोशिश हमेशा से करती हूं और करती रहूंगी। मैंने एक कहानी लिखी थी जिसमें मैंने यह दर्शाया की मर्द को घर में भी एक मिनट का स्पेस नहीं मिल पाता अगर वह बाथरूम में ज्यादा वक्त लगा दे तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वह कहीं अंदर सुसाइड ना कर ले। और उसे कहानी में यह भी चीज हुई कि जब वह अपने घर के अंदर अपना दुख परेशानियां नहीं शेयर कर पता है तो एक लड़के से ही उसका इमोशनल कनेक्शन होता है तो जब इस तरह की चीज हम समझ में देखते हैं और खुद उन चीजों से गुजरते हैं तब महसूस होता है कि हम किस तरह के गंभीर परेशानी को नजरअंदाज कर रहे थे और जब यह चीज समझ आती है तो फिर काफी देर हो जाती है और उसके बाद में जो परिणाम हमें देखने को मिलते हैं फिर हम कहते हैं बैक स्टेप नहीं ले सकते।
अरमान :- बड़े ही गंभीर मुद्दे को अपने काफी सरलता से बताने की कोशिश की हो रही है वाकई में समझने वाली चीज भी है क्योंकि समाज का दोगलापन हमें हर जगह देखने को मिलता है और जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ एकदम बड़े स्तर पर तो हमने वहां पर भी देखा हम यह भी देखते हैं फिर चाहे वह महिलाओं हो लोवर कास्ट जो डार्क जोक्स की सबसे बड़ी संख्या हमें देखने को मिलती है वह सोशल मीडिया से होती है शुरू और उसके बाद में उसे आम जीवन में भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
डॉ. संजुक्ता दासगुप्ता:- सही बात कही आपने और जो चीज हम मीडिया के अंदर देखते हैं या एडवर्टाइजमेंट होती है न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वह सिर्फ 30% को टारगेट करने का उनका लक्ष्य रहता है बाकी 70% से उन्हें कोई मतलब नहीं है उनके लिए मीडिया के अंदर कुछ भी नहीं है। वाकई में जो हमारे 70 परसेंट ऑर्डिनरी लोग हैं वह मीडिया के अंदर उनकी समस्याएं नजर ही नहीं आती है जो एडवर्टाइजमेंट कि अगर हम बात करें उसके अंदर कभी भी आपको उसे वर्ग के लिए जगह देखने को नहीं मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट में आपको एकदम फेयर लवली देखने को मिलेगा एकदम फेयर लवली स्किन हो जाएगी क्या वाकई में हम जब सड़कों पर उतरते हैं तो हमें हर जगह व्हाइट स्किन ही नजर आती है अगर मैं अपने देश की अपने समाज की बात करूं तो। स्किन कांप्लेक्शन है वह कहां से फिर चीज नजर आती है वह इन्हीं एडवर्टाइजमेंट से ही तो हमें देखने को मिलता है। इंडियन की स्किन टोन ही पूरी चेंज कर दी है एडवर्टाइजमेंट ने और मीडिया ने। उन्होंने व्हाइट भी किया है और माइंड वॉश भी किया है। और यह अलग-अलग तरह की इनकी स्ट्रैटेजिस है अपने सामान को बेचने की अगर बहुत ही कोई महंगा प्रोडक्ट है तो उसका विज्ञापन अंग्रेजी में फिर कुछ कम है तो हिंदी में बात की जाएगी और उसके बाद में एकदम रीजनल लैंग्वेज के ऊपर आ जाते हैं। उसमें भी क्लास आ जाता है।
अरमान:- आपकी रचनाएं प्रेरणा का स्रोत है और प्रेरणा ली जाती है उन लोगों से जो वाकई में काबिल हो और यह सवाल अगला आपसे मैं यूं करुंगा क्योंकि आप भी डिपार्टमेंट हेड रही किस तरह का रिलेशन होना चाहिए स्टूडेंट और प्रोफेसर में? आपका कैसा रिलेशंस था स्टूडेंट के साथ।
डॉ. संजुक्ता दासगुप्ता:- एक शिक्षक का मतलब यूं है कि वह आपका फ्रेंड होगा फिलॉसफर होगा और गाइड होगा। आप इन तीनों को देखोगे तो यह बिल्कुल सिनोनिम्स नहीं है मैने उनके मतलब अलग बनते हैं। फ्रेंड हो जाने का मतलब यह है कि वह आपसे अपनी हर एक बात कह सकेंगे आपसे अपने परेशानियां दिक्कतें जो यूनिवर्सिटी कैंपस में उन्हें परेशानी आती है और जो पढ़ाई से संबंधित जो मसले हैं उन्हें वह एकदम बेझिझक होकर आपसे पूछे बिना किसी डर के और बिना किसी दूसरी कन्फ्यूजन के उनके दिल की क्या बात है वह किस तरह की सोच रखते हैं यह सब कुछ खुलकर एक बात की जाए तब दोनों तरफ से एक समान सम्मान जब होता है उस वक्त हम बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाते हैं और देख पाते हैं और उनका समाधान भी करने की कोशिश करते हैं। और फिर मैंने कहा दार्शनिक फिलॉस्फर कि हम बात करते हैं तो वहां फिर वह यह चीज आ जाती है कि वह सिलेबस से बहुत ज्यादा ऊपर और अलग हो जाता है यानी कि वह खुद को भी देखें और अपने स्टूडेंट को भी एक दिल की गहराई से समझाएं और दुनिया जो चीज हैं वह उसे समझ सिर्फ मकसद यह नहीं रहे की सिलेबस पूरा करना है। जब हम दुनिया से रिलेट करते हैं दुनिया की चीजों के बारे में बात करते हैं तो वह एक पल का काम करता है जो आइडेंटिटी के साथ में जो रिश्ता है हम उसकी बात करते हैं यानी की दुनिया और आइडेंटिटी के बीच का जो पुल है वह बन जाता है। आप किस तरीके से किस आसानी के साथ में उन्हें दुनिया की जो बातें हैं और सामाजिक समस्याओं से समाधान के तरीके आपने किस तरीके से बताते हैं यह भी एक बड़ा काम हो जाता है। और जब गाइडेंस कि हम बात करते हैं तो वह उनके करियर से लेकर उनके इंटरनल तक चला जाता है यानी की वह बॉर्डर्स वह चीज है जाती है कि आप सिर्फ अपनी किताब की लाइन उनके सामने ना दोहराए जो गाइडेंस है वह आप उन्हें वह दे जो उनके लिए बेहतर से बेहतर साबित हो। यानी कि जब दिमाग बगैर किसी डर के साथ में काम करता है तभी उसकी प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ज्ञान के अंदर एक स्वतंत्रता होनी चाहिए ।
अरमान:- आपने कही भ्रमण किया है और एक रचनात्मक व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह सिर्फ वहां की खूबसूरती नहीं वहां की सामाजिक स्थिति को भी महसूस करता है आपने जब भ्रमण किया तो आपके विचारों में किस प्रकार से बदलाव आए?
डॉ. संजुक्ता दासगुप्ता:- बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम यात्रा करते हैं फिजिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो हम चीजों को देखते हैं और उन्हें अपने कमरे में कैद करने के अंदर लग जाते हैं लेकिन जब हम विचारों के साथ भ्रमण करते हैं यानी की रचनात्मक दृष्टिकोण से भी उन चीजों को देखते हैं तो समझने का जो तरीका है वह बहुत ज्यादा अलग हो जाता है । हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं जब वह बाहर जाते हैं मैं अमेरिका गई तो वहां मैं पढ़ाया भी है और रिसर्च भी काफी किया है वहां जाने के बाद और कुछ वक्त बिताने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि जो अमेरिकन सोसाइटी और जो वहां की पॉलिटिक्स हम यहां से देखते हैं वह धरातल पर काफी अलग है। मैं एक बार आपको टैगोर साहब की बात भी कहूं क्योंकि उनका जो ट्रैवल राइटिंग है वह बहुत ज्यादा है उन्होंने जितना लिखा है भ्रमण के ऊपर और इन चीजों को जिस दृष्टिकोण से उन्होंने परखा है वह वाकई में कला साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी लिखने में आपको हर चीज मिलेगी भूगोल से लेकर इतिहास साहित्य कला और मानव विकास। रूस जापान ईरान में गए वह वहां सब जगह उन्होंने वह चीज जब देखी तो लिखा भी। उन्होंने वह लिखा कि उन्होंने वहां के लोगों से क्या सीखा और मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस करती हूं कि मैं जितने भी देश में गई तो मैं वहां के लोगों से वहां की संस्कृति से वहां के वातावरण व्यवहार से काफी कुछ सीखा है और समझने को भी मिला है कि जब हम दूर बैठे कहीं से किसी के बारे में सुनते हैं और नजदीक से जब उस स्थिति के अंदर उतरते हैं तो उनमें कितना ज्यादा फर्क नजर आता है।
अरमान:- एक सवाल जो हमेशा से एक आम व्यक्ति के मन में आता है जो साहित्य से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है और यह सवाल एक आलोचक के रूप में मेरा भी रहेगा क्या लेखक की लेखनी तभी सार्थक मानी जाए जब उसका कलम उसके हाथों में अवार्ड थमा दें? क्योंकि मैं ऐसे कई लखको को जानता हूं जो इस तरह की सोच रखते हैं।
डॉ. संजुक्ता दासगुप्ता:- बिल्कुल भी आपकी बात सच है क्योंकि बहुत सालों की सोच यही है और जो इंटरनेट का लेखक है ना अभी तो यह इंटरनेट से सर्टिफिकेट भी चाहते हैं प्राइसेस भी क्रिएट कर रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं पॉइंट यह बन जाता है कि फेसबुक पर कुछ डालना लेकिन यह अभी तक यह चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि फेसबुक के बाहर दुनिया जो है वह असली दुनिया है असली दुनिया का इन्हें सम्मान नहीं चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर जो ग्लोरी है वह इन्हें संतुष्ट करती है। कि यह कोशिश इनकी रहती है कि फेसबुक पर मुझे और कैसे लाइक्स मिलेंगे इंटरमीडिएट में कैसे रिकॉग्निशन और यह भी एक सच कहना है कि सब लोग ऐसे नहीं है कुछ ऐसे आ जाते हैं और हमेशा से यह एक चीज बनी रही है क्या हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता है लेकिन सभी इस प्रकार के नहीं होते हैं लोग सही तरीके से काम भी करना चाहते हैं और अपना जो योगदान उसे ईमानदारी के साथ में निभाना चाहते हैं जिन्हें चमक धमक से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें केवल अपना लेखन अपना काम करना है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ यह भी कहना है की मेजोरिटी का सोच ऐसा बन गया है।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने हेतु आपका बहुत आभार ।
डॉक्टर संजुक्ता दासगुप्ता - आपका भी बहुत आभार
Raja Hasan 
राजा हसन
हम सबको उम्मीद है कि एक दिन राजस्थानी भाषा को मान्यता जरूर मिलेगी। - राजा हसन
फिल्मफेयर ओटीटी पुरस्कार प्राप्त सुप्रसिद्ध युवा गायक कलाकार राजा हसन से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत
परिचय
राजा हसन एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और निर्माता हैं, जो मूल रूप से बीकानेर, राजस्थान से हैं, जिन्होंने रियलिटी टीवी शो सा रे गा मा पा चैलेंज 2007 में भाग लेने के बाद प्रसिद्धि प्राप्त की, जहाँ वे उपविजेता रहे। उन्होंने हिंदी, तेलुगु, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में काम किया है।
शुरुआती करियर:
राजा हसन का संगीत कैरियर सा रे गा मा पा चैलेंज 2007 के बाद आगे बढ़ा।
पार्श्व गायन:
राजा हसन ने बचना ऐ हसीनों, 99, तेरी संग: ए किडल्ट लव स्टोरी, माधोलाल कीप वॉकिंग, तीस मार खान, नो वन किल्ड जेसिका, चलो दिल्ली, शंघाई, इश्क, पूला रंगाडू, बूनो हांश, चिन्नादाना नी कोसम और प्यार का पंचनामा 2 सहित कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गायन किया है।
संगीत निर्देशन:
उन्होंने राजस्थानी फिल्म मरूधर म्हारो घर, और ये है इंडिया सहित कई फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया है।
अन्य उल्लेखनीय प्रस्तुतियाँ:
हसन गायन प्रतियोगिता शो "वॉयस ऑफ शेखावाटी" में जज भी रह चुके हैं और कई अन्य टीवी शो में भी दिखाई दिए हैं।
संगीत वंशावली:
पिता, रफ़ीक सागर और दादा, अल्लाह रक्खा खान भी गायक और संगीतकार रहें हैं, और वे गायन में अपने पिता को गुरु मानते हैं।
पुरस्कार:
राजा हसन ने सर्वश्रेष्ठ मूल साउंडट्रैक (2024) के लिए फ़िल्मफ़ेयर ओटीटी पुरस्कार और 12वें मिर्ची संगीत पुरस्कारों में पुरस्कार जैसे पुरस्कार जीते हैं।
अरमान :- बॉलीवुड के सामने बीकानेर ने आपको प्रतिनिधि के रूप में देखा है लेकिन यह जानना काफी रोचक होगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई?
राजा हसन:- अगर मैं आपको अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताऊं कि किस तरीके से मेरी संगीत, गायन में दिलचस्पी बनी तो मुझे याद आता है कि जब मैं काफी छोटा था तो यहां चौक में जागरण हुआ करते थे तो बचपन से ही वह सब मेरे कानों में पड़े और अगर यूं भी मैं आपको बताऊं तो फादर साहब का पहले से संगीत में बड़ा नाम रहा है मरहूम रफीक सागर साहब। क्योंकि परिवार में शुरुआत से ही संगीत का वातावरण माहौल मिला तो कम उम्र से ही खुद ब खुद इसकी तरफ रुझान बनने लगा।मैं काफी कम उम्र से ही गाना गाने लगा था। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरा म्यूजिक में टेस्ट था वह कुछ अलग था क्योंकि जैसा कि आपको बताया की मोहल्ले में जागरण हुआ करते थे तो वह तो एक शुरुआती कदम था। जब हम नेक्स्ट जेनरेशन की बात करते हैं तो कुछ परिवर्तन आने वाजिब भी है तो इसी हिसाब से हमने भी कुछ अलग तरीके से शुरुआत की और आर्केस्ट्रा के साथ गाना शुरू किया। और इसी के साथ-साथ हमने खुद का भी ग्रुप बनाया और उसमें भी हम प्रोग्राम किया करते थे। और उस ग्रुप के अंदर बीकानेर के तमाम कलाकार शामिल होते थे जो संगीत से, गायन से जुड़े थे । तो सब एक साथ होकर प्रोग्राम किया करते थे जैसे कि हमारे बीकानेर की संस्कृति है। और धीरे-धीरे फिर टीवी शोज में भी जाना शुरू हुआ और वह दौर था नए-नए सिंगर का नए-नए एल्बम शुरू हो रहे थे तो इसी वजह से मेरा फोकस नए तरह के गानों पर ज्यादा होने लगा। और लोगों का प्यार जब उन गानों की तरफ देखने को मिला तो एक प्रेरणा भी मिली कि इन चीजों में इस तरह से भी काम किया जा सकता है। लोग इसे पसंद करते हैं ,सुनना पसंद करते हैं और इसी तरीके से मैंने अपना जो रुझान है वह नए गानों की तरफ शिफ्ट किया। और इसी के साथ इन्हीं दिनों के अंदर में मुंबई आया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में और वह भी एक अलग ही संघर्ष के दिन थे । मुंबई में काम करना शुरू किया लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ नए गाने ही गाए और पूरी तरीके से शास्त्रीय संगीत ग़ज़ल को छोड़ दिया । अगर मैं आपको बताऊं ,जब मैं मुंबई नया-नया आया था तो क्लब्स वगैरा में ग़ज़ल गाया करता था और इस दौरान मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया सारेगामा और उसके बाद में तो सब कुछ एक तरीके से बदल ही गया।
अरमान:- जैसा कि आपने कहा कि फादर साहब भी गायन में थे और बीकानेर के तमाम कलाकारों के साथ में आपका राब्ता है और इससे पहले भी बीकानेर के संगीतकारों ने बॉलीवुड को काफी कुछ दिया है जैसे गुलाम मोहम्मद साहब जिन्होंने पाक़ीज़ा फिल्म में संगीत दिया।
राजा हसन:- बिल्कुल बिल्कुल बीकानेर के बहुत बड़े-बड़े कलाकार मुझे हर फील्ड में देखने को मिलते हैं । ऐसा नहीं है कि सिर्फ गायन में हर क्षेत्र के अंदर बीकानेर के कलाकारों ने ,हमारे लोगों ने बीकानेर का नाम पूरे भारत में रोशन किया है । जैसे अपने भरत जी का नाम सुना होगा। गुलाम मोहम्मद साहब ने संगीत में मील का पत्थर स्थापित किया । स्वर्गीय संदीप आचार्य का नाम हर कोई बीकानेर में जानता है और भी अगर हम बात करें तो शमसुद्दीन खान साहब ,अलाउद्दीन सिराजुद्दीन साहब हैं तो बीकानेर के दिग्गज कलाकारों की फेहरिस्त बहुत लंबी है । यह वह लोग हैं जो पहले से अपना नाम ,अपना काम दुनिया के आगे स्थापित कर चुके हैं। और इन्हें तो हर कोई जानता है लेकिन जब मैं मुंबई गया तो मुझे वहां ऐसे भी और बीकानेर के साथ ही मिले जो लगातार अपना काम कर रहे हैं और इसी फील्ड में संगीत में साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। और लेखन से अलग होकर भी अगर हम बात करें तो एडिटिंग फील्ड में फिल्म मेकिंग के अंदर एक बड़ा काम बीकानेर के लोगों ने वहां किया है। तो मैं अगर सीधे-सीधे तौर पर कहूं तो हमारी फील्ड में जितने भी काम है उसमें बीकानेर के लोगों का योगदान मुझे वहां देखने को मिला। बहुत से कलाकार हैं जो वहां पर नाटक प्रस्तुति भी देते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मैं भी उनमें से शामिल होकर बीकानेर का नाम आगे कर रहा हूं । इसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता रहूं और मैं तो बिल्कुल अदना सा हूं उन सभी के सामने उन लोगों ने तो पहले ही बीकानेर का नाम इतना ऊंचा कर रखा है।
अरमान:- बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं और आज आप भी बीकानेर को देश दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको बीकानेर और बॉलीवुड का रिश्ता अब कैसा नजर आता है?
राजा हसन:- बिल्कुल अपनी तरफ से हम काम कर रहे हैं लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बीकानेर में आज भी बहुत सी ऐसी चीज हैं जो करनी बाकी है जिन पर बहुत सारा काम करना है और क्योंकि हम बॉलीवुड से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अगर मैं बात करते हुए यही कहूं कि अगर हम बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से बीकानेर को देखें जो एक विस्तृत रूप है जो एक विस्तार होता है । वह मुझे लगता है अब तक मिल नहीं पाया है बीकानेर को जो मिलना चाहिए था ,क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मैंने आपको बड़े-बड़े नाम बताएं बीकानेर से जो बॉलीवुड में गए या फिर दूसरे क्षेत्र में बाहर जाकर जिन्होंने पूरे देश में अपना कला के माध्यम से योगदान दिया तो वह कलाकार बैठे हैं मुंबई में दूसरे शहरों में जो बहुत पहले ही अपना लोहा मनवा चुके हैं । तो ऐसे बहुत से लोग हैं कहने का मतलब यह है की सबसे बड़ी बात है कि वह रिकॉग्निशन बीकानेर शहर को मेरी नजर में अब तक नहीं मिल पाई है। तो मैं ऐसे आपको और भी नाम गिनवा सकता हूं और आप खुद भी उनसे वाकिफ है नाम जानते हैं लेकिन बात यह है कि वह सारी चीज जो वहां हो चुकी है वह बीकानेर शहर में प्रैक्टिकल तौर पर हमें आज भी देखने को नहीं मिलती है।
अरमान:- बहुत ही मार्मिक बात कही आपने लेकिन वह चीज प्रैक्टिकल में आए इसके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा ?
राजा हसन:- बिल्कुल यह चीज से जैसा कि आपको बताई की प्रैक्टिकल में चीज आना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल में चीज तभी आती है कि जब हम उसे बैठकर खुद करते हैं और मेरा सुझाव मैं नहीं कहूंगा मेरा प्रयास जो वह यह रहेगा कि मैं बीकानेर शहर के अंदर एक इंस्टिट्यूट बनाना चाहूंगा ताकि जो नए चेहरे हैं ,नए बच्चे हैं नई ऊर्जा है वह जो आगे काम करना चाहते हैं उन्हें पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिले और उन लोगों के लिए एक नया रास्ता खोले उनकी पोटेंशियल खराब ना हो । उनका जो योगदान है वह जो काम दे सकते हैं जो वह बीकानेरी नहीं पूरे समाज के लिए हमारे शहर के लिए जो चीज कर सकते हैं वह खराब ना हो और उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आगे का एक रोड मैप मिले। और मेरा यह सपना है कि वह जो इंस्टिट्यूट होगा वह पूरा एक रास्ता आपको बॉलीवुड तक ले जाएगा और म्यूजिक इंडस्ट्री से एक अच्छा रिलेशन बन जाए ।जैसा कि आपने अपना सवाल भी किया था कि बीकानेर और बॉलीवुड का रिश्ता आप कैसे देखते हैं तो रिश्ता तो खैर बहुत ही अच्छा है और लगातार पहले भी कलाकारों ने बॉलीवुड में अपना नाम दिया है ,काम किया है लेकिन जो रिश्ता एक अटूट रिश्ता जो है उसे एक धार मिले । मुझे लगता है कि इस चीज के लिए एक प्रॉपर इंस्टिट्यूट होना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है जिसके दूरगामी प्रभाव ज्यादा होंगे।
अरमान:- अपने बॉलीवुड में प्लेबैक भी किया है और लाइव शो भी किए हैं सीधा सवाल अगर मैं आपसे यही पूछूं की लाइव शो और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या नजर आता है और जो एक नया बच्चा है, नया संगीतकार है जो आपको देखकर आगे बढ़ रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वह खुद लाइव शो और स्टूडियो रिकॉर्डिंग में दोनों में तालमेल कैसे बनाएं?
राजा हसन:- काफी अच्छा सवाल है यह आपका मैं कहना चाहूंगा कि जो एक बना हुआ कपड़ा होता है और बगैर सिला हुआ कपड़ा होता तो कपड़ा ही है यह चीज आप वैसे समझ सकते हैं उसमें ज्यादा फर्क तो है नहीं लेकिन लाइव में और स्टूडियो की सिंगिंग में उसमें आपकी थोड़ी कॉन्शसनेस थोड़ी बढ़ जाती है स्टूडियो की सिंगिंग में क्योंकि वह एक बार ही रिकॉर्ड होता है और हमेशा के लिए रहता है और लाइव शो के अंदर आप देखिए कि आप जितना चाहे उसमें बदलाव कर सकते हैं फिर आपके गाने का तरीका हो गया हाव-भाव हो गए तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि स्टूडियो सिंगिंग जो है वह थोड़ी मुश्किल है लाइव शो के मुकाबले में।
अरमान :- लाइव परफॉर्मेंस के लिए सबसे जरूरी चीज आपको क्या लगती है जो की एक सिंगर को अपने ध्यान में रखनी चाहिए?
राजा हसन:- लाइव शो के बारे में तो मैं सबसे बड़ी चीज जो है यही कह सकता हूं कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और गंभीर होना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस के लिए आप अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ऑडियंस को राज़ी किस तरीके से रख सकते हैं यही सबसे बड़ी चीज होती है। बाकी सब चीज तो खैर होती ही है कि आप अपने हाव-भाव किस तरीके से बना सकते हैं और ऑडियंस का मूड उसे वक्त क्या है आपको यह भी पहले जानना होगा और यही बात है कि आपको उन्हें राजी रखना है और अपने परफॉर्मेंस के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क रहकर काम करना है और जो अपडेट्स लगातार होती है उनका खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है आपको पहले से नहीं मालूम कि अब अगला क्या होने वाला है तो जो माहौल के साथ में काम हो रहा है उसी को देखते हुए आपको अपना काम करना है।
अरमान :- अगर हम शास्त्रीय संगीत की बात करें और आपने भी कहा कि शुरू में आप ग़ज़ल भी गाया करते थे लेकिन आज बॉलीवुड के गानों में मुझे लगता है यह चीज थोड़ी कम सी होती जा रही है आपकी नजर में शास्त्रीय संगीत का क्या महत्व है?
राजा हसन:- बिल्कुल आपने बात सही कही और मैं यह आपको बात कहना चाहूंगा कि सो सोनार की एक लोहार की शास्त्रीय संगीत जो है वह हमारा बेस है अगर आपने शास्त्रीय संगीत को हटा दिया अगर वह नहीं होगा तो जो म्यूजिक है वह नहीं बन पाएगा । तो यह तो बहुत कह सकते हैं साफ बात है और यही हकीकत है कि जो लोक संगीत है, और शास्त्रीय संगीत है वही अव्वल दर्जे का गायन है बाकी वह तो सब कमर्शियल एंगल है तो जो चीज है कि गायन में भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और कमर्शियली किसी ने अगर कुछ कर दिया तो कर दिया लेकिन वह क्लासिकल से हटकर काम नहीं कर सकता। और मैं तो यही कहना चाहूंगा और यही बात मैं दिल से कह सकता हूं कि जो बात आपने भी कहीं की क्लासिकल संगीत को कम किया जा रहा है यह गलत है और जो महत्व है वह तो सबसे बड़ा क्लासिकल संगीत का ही रहेगा । और वह बरकरार रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और कोई व्यक्ति जब क्लासिकल परफॉर्मेंस करता है तो इसका वर्चस्व और जो प्रभाव है उसे भी अगर हम देखें तो वह ज्यादा माना जाता है।
अरमान:- बिल्कुल काफी खरी बात कही आपने और बीकानेर ही नहीं बॉलीवुड के अंदर जो आपकी इमेज है वह एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति की इमेज है जिसमें हमने यह भी देखा कि जब राजस्थानी भाषा के आंदोलन पर गीत बनाए जा रहे थे तब हमने आपको भी सुना। तो हमने यह भी देखा कि जो लेखक हैं, कला से जुड़े हुए लोग हैं वह लगातार राजस्थानी भाषा की मान्यता की मांग करते रहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता का जुड़ाव अब तक हमें इतना खास देखने को नहीं मिलता है इसके आपको क्या कारण नजर आते हैं?
राजा हसन:- मौजूदा वक्त अगर हम बात कहें तो आज का जो दौर है वह सोशल मीडिया का है और यह वक्त की मांग होती है, हर वक्त में अलग-अलग समस्याएं भी होती है और उनका निवारण करने का तरीका भी अलग होता है और अपने जैसा बात कही की जनता का जुड़ाव हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है और यह कहीं ना कहीं सच भी है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें आज के वक्त में जनता को इस चीज से जोड़ना है तो उसका तरीका भी कुछ अलग होना चाहिए । और अगर जनता डिजिटल तरीके से ज्यादा जुड़ती है तो हमें फिर उसे पर भी काम करना चाहिए और इसके लिए जो सोशल मीडिया है आज के वक्त में हमारे पास में एक बहुत बड़ा माध्यम बनकर आया है। और इसके ऊपर भी हम लगातार अपना काम कर सकते हैं अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए और बिल्कुल अपने गाने की बात कही तो आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मैं न सिर्फ गाना बल्कि पूरी फिल्म बना दी है इसके ऊपर। मैंने फिल्म बनाई है मरुधर म्हारो घर वह पूरी जो फिल्म है वह भाषा के ऊपर ही केंद्रित है। तो इसी तरीके के जो प्रयास हैं मुझे लगता है कि जिससे जनता और ज्यादा गहराई से और तेजी से इस आंदोलन के साथ जुड़ सकती है और हम सबको उम्मीद है कि एक दिन राजस्थानी भाषा को मान्यता जरूर मिलेगी।
अरमान :- जब मैं इंटरव्यू के दौरान शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए बड़े लोगों से बात की तो उनका कहना है कि आज के नौजवानों में संगीत के प्रति कोई ईमानदारी नहीं रही वह सिर्फ इसको एक कमाई का साधन मानते हैं इसके पर आपके क्या विचार हैं?
राजा हसन:- इसके ऊपर अगर मैं बात कहूं तो मैं यह कह सकता हूं कि यह तो एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा यह कहना है कि किसी की रोजी-रोटी के बारे में तो हम बोल नहीं सकते तो अगर किसी को बचपन से ही पैसे कमाने हैं तो वह जूते पोलिश करके भी कमा लेता है और अगर गायन से पैसे कमाने हैं और इसी को अपना इनकम सोर्स बनाना चाहता है । तो मुझे लगता है इसमें तो कोई बुरी बात है नहीं लेकिन इसके अंदर भी अगर हम दोनों पहलुओं को लेकर बात रखें और समझ कर इस पर चर्चा करें तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क आता है और वह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यह आता है कि कौन कितना जानता है और अगर हम इसे समझने के लिए कहे तो यह पढ़ाई लिखाई जैसा ही है मान के चलिए कि सर्दी जुखाम है और एक आम आदमी कहता है कि यह यह दवाई है फलां दवाई है इसे ले लो या कोई घरेलू नुस्खे हैं उसका वह अपनी तरफ से सुझाव देता है लेकिन दूसरी तरफ एक डॉक्टर जो है वह मेडिकल प्रूव्ड व्यक्ति है वह आपको बताता है ,अपने प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसे चीज में काफी फर्क है तो अगर आपको एक आम सुझाव देना है या एक डॉक्टर बनकर उसे बीमारी का इलाज करना है तो इसमें बड़ा फर्क आ जाता है और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी एक बड़ा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा पूरे प्रक्रिया के ऊपर से गुजरना पड़ेगा उसके बगैर आप डॉक्टर नहीं बन सकते आप डॉक्टर तो क्या कहीं पर क्लीनिक में नहीं खोल सकते तो यही बात है कि संगीत में भी कौन कितना जानता है वह अपने अनुभव से अपने काम से अपनी लगन से कितना सीखना है यह सबसे बड़ी बात हो जाती है और उसके बाद में वह किस तरीके से कमाता है यह भी एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। और यह चीज नौजवानों को समझने बहुत जरूरी भी और जैसा कि आपने कहा कि वह जो वरिष्ठ लोगों ने जैसा सुझाव था सम्मानित लोग हैं वह हमारे और यह बात सच भी है कि आज थोड़ा हमें इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और इसीलिए मैंने आपको बताया कि मेरा जो विचार है मेरा जो काम है वह इंस्टीट्यूट की तरफ है उसमें यह सब चीज शामिल है कि उन्हें संगीत के बारे में जानकारी देना और एक प्रॉपर रास्ता बना कर देना जिसमें वह कहीं और भटके ना। और यह सबसे बड़ा कारण है कि एक म्यूजिकल यूनिवर्सिटी होना कितना जरूरी बन गया है कि लोगों को संगीत के बारे में जानकारी हो उन्हें असल इसका मतलब मालूम हो कि संगीत की परिभाषा क्या है और उन्हें यह भी समझ आए कि सिर्फ संगीत में अगर आप आ रहे हैं और आपका उद्देश्य कमाना है तो यह भी सच है कि संगीत कमाने के लिए नहीं है संगीत लोगों को राजी करने के लिए है लोगों को खुश करने के लिए है कमाई तो इसके साथ-साथ फिर हो ही जाती है।
अरमान :- काफी अच्छी बात कही आपने और इसे एक ही भी बड़ा सवाल आ जाता है कि एक संगीतकार की समाज के प्रति आज क्या भूमिका है?
राजा हसन:- देखिए संगीतकार को बहुत सी चीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखती होती है और पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखनी होती है और अगर कोई संगीतकार ऐसा है जो इसी पर आधारित कि मुझे तो सिर्फ देश भक्ति ही संगीत पर काम करना है तो यह उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कोई संगीतकार ऐसा होता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ कमर्शियल गाने ही बनाने हैं ताकि मेरे गाने ज्यादा से ज्यादा सुने जाएं और हिट हो और जैसे कमाई हो सके यह दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर सही है। अब यहां हम किसे गलत बोलेंगे और मैं अगर आपका सवाल पर जाऊं जैसा आपने सवाल किया कि एक संगीतकार के समाज के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए तो यह दोनों उदाहरण मैंने आपको दिए यह दोनों ही गलत नहीं है लेकिन एक चीज जो है जो भी संगीत आए उस संगीत का ऐसा प्रभाव पड़े कि लोग उससे कुछ सीखें कुछ नया कुछ प्रभावित हो और उसे अपने बच्चों को वह प्रेरणा दे सके ना कि उसे संगीत से कोई गलत परंपरा शुरू हो।
अरमान :- आपने कही मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी और मेरा सवाल आपसे यह रहेगा कि मौजूदा वक्त में म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए आपको सबसे बड़ी चुनौतियां क्या नजर आती है?
राजा हसन:- सबसे बड़ी चुनौती के में आपके सामने बात करूं तो मुझे लगता है कि मौजूदा वक्त में म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती एक ही है जैसा कि मैंने बात रखी भी की एक बड़ा प्लेटफार्म सोशल मीडिया भी है और वह काफी चीजों में हमें फायदा भी देता है और लोगों से जुड़ने का एक बड़ा प्लेटफार्म है और सोशल मीडिया पर सब लोग एक दूसरे से अपडेट रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहना भी चाहते हैं जो की एक बड़ी अच्छी बात भी है और हमने काफी मुद्दों पर सोशल मीडिया के फायदे भी देखे हैं और जो सबसे बड़ी चुनौती जो अगर हम देखें और पहले की अगर पहले की बात करूं तो जैसे रफी साहब , लता मंगेशकर जी ,किशोर कुमार साहब थे अब वैसे प्लेबैक सिंगर हमें देखने को नहीं मिलते हैं और मुझे लगता है कि अब लगातार कम होती जा रही है वह संख्या सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि वह स्तर जो है वह क्यों गिरता जा रहा है उसे बरकरार रखना और बरकरार रखते हुए बढ़ाना मेरी नजर में अभी म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौती है । और यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम भी है कि ऐसे प्लेबैक सिंगर और लोगों के सामने उन्हें इंट्रोड्यूस करवा जिन्हें जनता सुनना पसंद करें जिन्हें जनता प्यार दे और वह एक जो स्टैंडर्ड है वह बरकरार भी रहना चाहिए। और कई बार हमें सोशल मीडिया से भी ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जो काफी अच्छा गाते हैं । तो यह तालमेल बरकरार रहे एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे मेरा यह कहना है।
अरमान नदीम -शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने हेतु आपका बहुत आभार ।
राजा हसन - बहुत आभार ।
Shreya Gupta 
श्रेया गुप्ता
इतिहासकारों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को सही जानकारी दे - श्रेया गुप्ता
ऑक्सफोर्ड में एशमोलियन संग्रहालय के साथ कार्य कर रही युवा इतिहासकार श्रेया गुप्ता से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।
परिचय: एक्सेटर विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष पीएचडी छात्रा हैं. ऑक्सफ़ोर्ड में एशमोलियन संग्रहालय के साथ काम कर रही हैं। वह संग्रहालय संग्रह के साथ काम करते हुए औपनिवेशिक भारत में सिक्के एकत्र करने के इतिहास पर भी शोध कर रही हैं। पीएचडी से पहले उन्होंने भारत में संग्रहालय क्षेत्र में भी उपलब्धि मूलक काम किया है ।
अरमान :- एक किताब तब ही सफल हो पाती है जब उसे एक अच्छा पाठक मिलता है और आपने काफी किताबें पढ़ी । ज्यादा हिस्ट्री पर आपका काम है। इतिहास में आपकी दिलचस्पी कैसे बनी और जो किताबें आपने पढ़ी उनको लेकर इतिहासकारों के लिए किस तरीके से नजरिया बने, बदले, बिगड़े ?
श्रेया:- इतिहास में अगर दिलचस्पी की बात करूं तो बचपन से ही रुचि रही फिर चाहे वह स्कूल टाइम की अगर बात करें जब सब्जेक्ट चुनने की बारी आती है तब भी इतिहास की तरफ रुझान सबसे पहले रहा। और इस वक्त से किताबों के प्रति और ज्यादा रुचि बड़ी उन्हें पढ़ना अच्छा लगने लगा क्योंकि जो ऐतिहासिक किताबों में जानकारी मिली वह काफी रोचक रही उसे वक्त तक के लिए और और आगे उसके बाद में भी जानने की जिज्ञासा बनी फिर चाहे वह फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो नक्सली मूवमेंट जो हुआ और इस तरह की और घटनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा और पूरी तरीके से जानकारी हासिल करने की रुचि बनी फिर दूसरी जो किताबें थी जो ऑथर्स ने लिखी ऐतिहासिक घटनाओं पर उन्हें पढ़ा था के किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया यह चीज को गहराई से समझने की कोशिश रही। और ऐतिहासिक मसलों मे भारत बल्कि विश्व स्तर की जो घटनाएं थी जो बड़ी घटनाएं उन पर खास नजर बनाए रखी और जिसमें शुरुआती अगर टाइम पीरियड्स की बात की जाए तो वह प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय पर विश्व युद्ध की घटनाओं के बारे में और जो समस्या आज तक हमें देखने को मिल रही है इजराइल और फिलिस्तीन की उसकी क्या जड़ें रही उन पर भी खास जोर दिया गया और स्विस कैनाल का जो मसाला हुआ और क्यों उसकी वजह से चीजें बदली और वहां से लेकर जो कोल्ड वॉर जहां फिर उसपर का विघटन हुआ वह पूरा घटनाक्रम विस्तार से और गहराई से समझने का प्रयास रहा। विश्व स्तर के ऊपर हम इतनी सारी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं जिनका असर आपके खुद के जीवन पर भी कहीं ना कहीं होने लगता है तो उनमें दिलचस्पी आना लाजमी भी है और उन्हें पढ़ना ना सिर्फ पसंद की बात बल्कि यह भी था कि क्या सच घटनाएं लोगों के सामने पेश की जा रही है या उन्हें मेनू प्लेट किया जाता है या अपनी तरफ से भी बनाने की कोशिश रहती है। स्कूल के बाद ग्रेजुएट होने की बारी आई तभी इतिहास पर ही मेरा जोर रहा और उसे वक्त स्टीफन को चुना। यूनिवर्सिटी में आने के बाद सोचने का जो नजरिया है वह थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तब तक दिमाग में सिर्फ यह रहता है कि हमें पास कैसे होना है मार्क्स लाने हैं और उसकी जो मेकिंग प्रोसेस है उसके ऊपर कभी इतना दिलचस्पी नहीं रहती है लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद में मैंने यह सोचना शुरू किया के इतिहास बनता है कैसे है यह जो घटनाएं हुई उनके पीछे की क्या वजह थी तो जब इस तरह की की सो जाने लग जाए तो इंसान खुद के ऊपर भी कहीं ना कहीं काम करने लगता है क्योंकि आपका उद्देश्य केवल उसे याद करना नहीं है उसे समझना है उसके परिणाम क्या हुए और वह क्यों हुआ उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। जिस तरीके से हम कई बार सिर्फ सिलेबस के ऊपर बंध जाया करते थे यानी कि हमने एक चीज पढ़ी और जो किताब में लिखा है जो हमारे सिलेबस की किताब में हैं हमने उसे याद कर लिया और बात खत्म लेकिन एक वक्त यह भी होता है कि हम उसमें अरगुमेंट करते हैं हम उसके विकल्प देखते हैं कि बाकी इतिहासकारों ने अपने-अपने वक्त में इस घटना को किस नजरिए से देखा है। और निष्कर्ष के रूप में यही चीज निकलती है आपको खुद को चुनना पड़ेगा कि आप किन के तरफ ज्यादा अपने आप को सही समझते हैं और सही समझने से मतलब यह है कि आप किन्हे देख रहे हैं। और आप उनसे सहमत क्यों हैं जिन्हें आप पढ़ रहे हैं उसका भी आपके पास में वजह होनी चाहिए और जिसे आप सहमत नहीं है उनके लिए भी आपके पास में वजह होनी चाहिए वजह सिर्फ यह ना हो कि आपको उनकी वह बात पसंद नहीं आई उसके कुछ कारण होने चाहिए कि आप जिस इतिहासकार की बात काम पर अपना समर्थन दे रहे हैं उसकी वजह क्या है। और इस चीज की वजह से आपका आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी बढ़ता है। शुरुआती वक्त के अंदर दिल्ली में पढ़ाई करने का सबसे बड़ा जो फायदा में कह सकती हूं वह यह रहा कि जिस इसके बारे में हम पढ़ रहे थे उसे हम जाकर देख भी सकते थे यानी कि अगर हम लाल किला कुतुब मीनार यह जो बड़े स्मारक है उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उन्हें देख भी सकते थे। स्नातक होने के बाद में भी मेरा जो लगाव है इतिहास के प्रति और ज्यादा बड़ा और मेरी इच्छा थी कि और ज्यादा पढ़ो इसीलिए मैंने अपने मास्टर्स के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन) यहां का भी अनुभव मेरा काफी शानदार रहा क्योंकि जो तरीका है वह कुछ थोड़ा बदला की जो यहां यह सिखाया जा रहा था कि आप खुद कैसे इतिहासकार बनते हैं क्या आपको किस तरीके से लिखना चाहिए घटनाओं को देखकर समझ कर। और जो बाकी हम सब्जेक्ट पढ़ा करते थे तो यहां पर उसके बाद में छोटा थिसिस देखना होता था तकरीबन 20000 शब्दों का जिसमें मैंने जो अपना टॉपिक चुना वह था अकबर और जहांगीर क्या जो रिलेशनशिप था आपस में जो रिबेलियंस हुए जहांगीर ने अकबर के खिलाफ जो किया तो उस पर मैंने अपनी तरफ से लिखा था। जो उनके रिश्तों में उतार-चढ़ाव थे। और उसमें मेरे कुछ खास चीजों में ध्यान यह रहा कि जो इमारतें थी और जो सिक्के थे उसे वक्त के तो उन्हें किस तरीके से डिफरेंटशिएट किया जा रहे थे पेंटिंग्स हुई उनके हिसाब से समझने की कोशिश की दोनों के रिलेशनशिप कैसा थी।
अरमान :- इतिहासकारों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से कई बार उनमें कुछ भी होने लग जाती है जैसा आपने कहा कि यह फिर व्यक्ति के ऊपर है कि वह किसको मानता है और किसे गलत समझता है और उसका भी वह कारण दे लेकिन वाकई इतिहासकारों का जो रोल है वह क्या होना चाहिए?
श्रेया:- यह चीज मैं समझी और जब मैं वापस भारत आई उसके बाद में मैं कहीं ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किया। इंडियन कल्चर पोर्टल और वहां पर आपको काफी रेयर किताबें महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलेंगे और एक क्षेत्र था हिस्टोरिकल सिटीज जिसके ऊपर में काम किया करती थी। इसमें हमारा काम था कि जो भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक और ऐतिहासिक शहर है उनके ऊपर हम कम करें उन्हें मार्ग किया जाए जैसे कि दिल्ली ,लखनऊ, जयपुर ,वाराणसी ,कोलकाता, भोपाल इस तरह की जो मुख्य प्रमुख शहर है उनके ऊपर कम करें जैसे वहां के स्मारक और कल्चरल प्रोग्राम। इसमें हमारी कोशिश यह भी रहती थी कि हम जो प्रमुख घटनाएं हुई है उनके बारे में जानकारी दें जो टाइम पीरियड है उसके डिफरेंट डिफरेंट प्वाइंट्स क्या रहे वहां की वीडियोग्राफी और जो जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे गहराई से दिखाने की कोशिश रहती थी। उसे वक्त मेरी दिलचस्पी म्यूजियम के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। यह मेरा मानना है कि भारत में लोगों को उनके इतिहास के बारे में जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है और जैसा की इतिहासकारों का भी इसमें जो काम है वह बड़ा है क्योंकि फेक न्यूज़ का जो चालान जिस तरीके से हम देख रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा है। मिस इनफॉरमेशन जिस तरीके से स्प्रेड किया जा रहा है उसमें इतिहासकारों का भी एक जिम्मा है कि वह उसे चीज को समझाएं कि क्या चीज किस तरीके से हुई थी और इसे किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा। व्हाट्सएप की बात करें तो जो फॉरवर्ड से किस तरीके के क्लेम आते हैं। और यह इतिहासकारों का काम है कि वह लोगों को सही जानकारी दें। सबसे जो स्ट्रांग जो इनिशिएटिव मुझे लगते हैं समझाने के वह हैं म्यूजियम, ब्लॉक हो गए मीडिया के ऊपर भी हम सही जानकारी दे सकते हैं अगर गलत इनफॉरमेशन इस तरीके से स्प्रेड की जा सकती है तो हम ऑथेंटिक जानकारी क्यों नहीं दे सकते। मैंने आपको कहा कि म्यूजियम में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा तो मास्टर्स के बाद पीएचडी भी मैंने इसी में शुरू कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक म्यूजियम के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में कोलैबोरेटेड पीएचडी का और अभी मैं उसके आखिरी साल में हूं। म्यूजियम है वह ऑक्सफोर्ड के अंदर है जिसमें मेरी रिसर्च इस बात में है कि कुछ लोग कॉलोनियल ऑफिशल्स थे , इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर थे। भारत आए कॉलोनियल रूल के दौरान। उसे वक्त वह भारत के इतिहास से काफी आकर्षित हुए। उन्होंने सिक्कों का कलेक्शन शुरू किया। और उन्हें पढ़ना और समझने की उन्होंने कोशिश की। इन्हीं चीजों की वजह से वह काफी कुछ समझ पाए। कौन सा रोलर असिएंट इंडिया के अंदर किसके बाद में आया किसकी सत्ता कितने वक्त तक स्थापित रही और कब किसे पराजित किया गया। फ्री रिसर्च है वह उन लोगों के ऊपर ही है कि उनका जो इंटरेस्ट है वह इतना कैसे बना और किस तरीके से उन्होंने काम किया होगा तो यह चीज मेरे रिसर्च फॉर्म में। क्योंकि वह ब्रिटेन से आए थे और जो कि हिंदुस्तान पर रूल कर रहा था तो उसे वक्त उनकी सोच कैसी थी तो यह भी जानना काफी दिलचस्प रहता है। साथी में उनके बारे में भी पता लगाना जिन्होंने इनके साथ में काम किया था इन सिक्कों को पढ़ने में उन्हें समझाने में। क्या उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट रहस्य या फिर वह साथ में काम कर रहे थे और जो इंडियन से उनका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है तो यह सब मेरे रिसर्च के अंदर में पता लगाने की कोशिश में।
अरमान :- साहित्य हो ,इतिहास, कला यह सब रुचि के काम है जिन्हें इसमें दिलचस्पी है वह इतने बेहतरीन तरीके से देखा है और इसके प्रति अपना योगदान देने की कोशिश करता है। हमें देखने को मिलता है कि हमें अपना इतिहास पढ़ना ही क्यों जरूरी है । कई बार चाहे वह फिर मजाक में ही कि हम उनकी तारीख से जानकर क्या करेंगे कि जो आज से 500 साल पहले खत्म हुए तो आप जो इतिहास के विद्यालय हैं किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को और जो जनरेशन है उन्हें इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है?
श्रेया:- जी यह चीज है एक लंबे वक्त से सामने आती है और रही बात इतिहास क्यों जाने ना जरूरी है तुम मुझे लगता है कि जो आज के वक्त में जो घटना घटित हो रही है हम कहीं ना कहीं उसके ओरिजिन उसके मूल तक जा सकते हैं अपने इतिहास को पढ़कर समझकर। जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें हर चीज के बारे में जानकारी मिलती है फिर चाहे वह रिलेशन हो खानपान की चीज क्या रहने का जोड़ा गया तरीका है तो हम इन सब के बारे में इतिहास में जानकारी ले सकते हैं। और यह चीज जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो असर है वह हमें अपने मौजूदा वक्त में भी देखने को मिलता है जिसमें हम समझ सकते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है वह मेरी नजर में काफी ज्यादा बढ़ती है। और इतिहास हमें बताता है कि किसी भी घटना के या कोई चीज के एक या दो पहलू नहीं होते हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन सभी पहलुओं को देखना समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इन चीजों के ऊपर गहन अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है सहनशीलता आपकी बढ़ जाती है और जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और वह कुछ चीज कहता है तो आप यह भी देख पाते हैं कि उसके कहने के पीछे उसके क्या-क्या सरकमस्टेंसस रहे होंगे। और इससे आप किसी भी इंसान को एक नजरिए से नहीं देखे यह नहीं देखा जाता कि हम अलग हैं और वह अलग हैं हम यह भी देख सकते हैं कि क्या-क्या समानताएं हमारे बीच में आती है।
अरमान :- ऐसा टाइम पीरियड आपकी नजर में कौन सा है जिसके अंदर किस अल्पसंख्यक और महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर रही थी? जिन्होंने न सिर्फ सीमा विस्तार बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर भी उसे तरीके से तवज्जोह दी जिस तरीके से बाकी अपनी सेना को ताकतवर करने में लगा रहे थे।
श्रेया:- देखिए कोई भी जो शासन हो वह सबसे पहले जो काम करता है वह अपने इंटरेस्ट को देखते हुए काम करता है और यह आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्यादातर जो राजा या बादशाह सम्राट हुए उन्होंने सीमा वृद्धि के ऊपर ज्यादा जोर रखा । ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे भी कालखंड हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफी ज्यादा आंतरिक मसलों पर भी ध्यान दिया जैसे कि अगर हम बात करें मुगल काल की। और बात अगर की जाए उनके काम की तो उन्होंने काफी ज्यादा काम किया कला संस्कृति को बढ़ावा देने के ऊपर काफी ज्यादा अनुवाद उसे वक्त हुए अकबर के काल में रामायण, महाभारत का अनुवाद हुआ। जहांगीर के वक्त में जब क्रिश्चियन आए तो वह अपने साथ में यीशु और मेरी के चित्र भी लाया करते थे तो उसे वक्त मुगल काल के अंदर उन्होंने उसे मुगल डिजाइन के अंदर बनाया और स्टोरी उनकी वही रही लेकिन जो कल थी और जो तरीका था वह बिल्कुल अलग हो गया। उन्होने उस कहानी को उसे चित्र को मुगल फ्लेवर दे दिया। चीज भी हमें यह बताती है कि आप किस तरीके से अलग-अलग चीजों से इन्फ्लुएंस ले सकते हैं। प्रॉब्लम भी आती है कि हमारे पास में इतनी ज्यादा सोर्स नहीं रहते आम जनता के बारे में बात करने की के उसे वक्त उनकी क्या कंडीशन थी चाहे वह फिर आपने कहा महिलाएं या फिर अल्पसंख्यकों की भी अगर हम बात करें तो वह जो सोर्स है हमें इतना ज्यादा कहीं पर पुख्ता तौर पर किसी भी कालखंड के ऊपर नहीं मिलता। अगर हम मुगल पीरियड की ही बात करें तो जो रिसर्च हमें सामने देखने को मिली है। रूबीलाल प्रोफेसर है जिन्होंने उसे वक्त महिलाओं के ऊपर जो कंडीशन थी काम किया। उन्होंने बताया है कि जो मुगल परिवार था जिसमें महिलाएं उनकी माताएं बहने जो उनकी सीनियर मेंबर्स थे फैमिली के उनके पास में काफी इनफ्लुएंस था। खुद के जो पैसे हैं वह कंट्रोल किया करते थे इस वक्त अपने दौर में काफी चैरिटी भी की अपने पैसों से। उन महिलाओं ने खुद से अपनी हज यात्रा ऑर्गेनाइज की। इस तरह के जो मुद्दे हैं और जो लोग देखना और समझना चाहते हैं तो उन पर अब धीरे-धीरे काम शुरू हो रहा है और हम देख पा रहे हैं कि हमें उसे वक्त के लोगों के बारे में जानकारी फीमेल रही है जैसा कि आपका सवाल था। इतिहास की अगर हम बात करें तो यह वह लिखते हैं या उनके द्वारा लिखा जाता है जो जीत जाते हैं यानी की जिनकी हार हुई उनकी कंडीशन असल में कैसी हुई थी वह हमें पूरी तरीके से कई बार देखने को नहीं मिल पाती है। अगर आपको महिलाओं की और अल्पसंख्यक की जो कंडीशन है जो और जानी है तो हमें इसे और अलग नजरिए से और अलग ढंग से ढूंढने की भी जरूरत पड़ती है।
अरमान :- हां बिल्कुल आपने जो बात कही इतिहासकारों से सहमत हो ना हो कोई बात है लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है फिर चाहे वह इतिहासकार किसी भी सोच का हो वह सिर्फ अपनी बात को एक तरीके से थोप रहा है क्या कोई ऐसा सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड आपको महसूस होता है?
श्रेया:- मेरी नजर में इतिहासकारों से ज्यादा बड़ा जो इशू है वह आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर हो रहा है फिर चाहे आप एक्स,फेसबुक ले लीजिए ,वेबसाइट ले लीजिए तो यह जो चीज हैं यह ज्यादा कई बार परेशानी खड़ी कर देती है। क्योंकि यहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल एक विचारधारा से प्रभावित होकर चीज फैलाने का गलत खबरों को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि एक जो मोमेंट अभी चल रहा है कि हर दूसरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक आज के जमाने में है वह यह सब चीज हैं जिस तरीके से गलत खबरों को तूल देकर उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है और जो सच है उसे एक अलग मोड़ देकर लोगों के सामने पेश किया जाता है तो जब पहली बार कोई व्यक्ति सब चीजों को देखा है तो वह समझ ही नहीं पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि वह बार-बार एक ही एक ही चीज को देख रहा है। जो मिस इनफॉरमेशन है और जो गलत खबरें हैं इसे संभाल कर रहना सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में नजर आता है। जो ऐतिहासिक घटनाओं को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं उसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। यह हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब भी हम इस तरह की कोई खबर पड़े और लगने लगे कि यह सच नहीं है या फिर इसे बड़ा-चढ़कर पेश किया गया है तो हम न सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप पर निर्भर होकर या तो खुद की रिसर्च करें या फिर किताबें पढ़ें और उसे पता लगे कि असल में क्या हुआ था और इस घटना को किस तरीके से पेश किया जा रहा है। अभी देखना जरूरी होता है कि वह जो चीज आप पढ़ रहे हैं वह कहां से आ रही है वह लिखा किसने है क्या वह वाकई में एक विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति है संगठन है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई उद्देश्य ही इस तरह के की चीजों को स्प्रेड करना है। इन सब चीजों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है।
अरमान :- अपने बात सही की के हमें वह सोर्स देखना चाहिए कि वह किसने लिखा है और वह क्या वाकई में उसे विचारधारा से प्रेरित होकर लिखा गया क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब एक झूठ लंबे वक्त तक टिक जाए और उसका खानदान ना हो तो उसे भी ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में प्रेषित पेश किया जाने लग जाता है जैसे उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं जो कुछ वक्त पहले तक ताजमहल का विवाद काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और उसमें जो अरगुमेंट थी वह थी पीएन ओक की एक किताब खुद एक इतिहासकार थे नहीं थे इसमें भी एक अलग बहस हो जाती है लेकिन जब इस तरह की की चीजों को ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में प्रेजेंट किया जाता है आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो एक फेक न्यूज़ एक लंबे वक्त तक टिक गई हम उसे भी एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करने लग जाते हैं।
श्रेया:- बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही थी कि यह बिल्कुल गलत है और यह सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वह यहां पर इतिहासकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन चीजों का खंडन करें। वह आगे आए और यह कह के जो चीज फैलाई जा रही है उसका भी एविडेंस दिन की यह गलत क्यों है और जो उसकी सही घटना है और जो सही चीज है उसका भी हम पूरे तरीके से पक्ष लेते हुए अपने एविडेंस डे के असल में जो चीज है वह क्या थी। यह हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है क्या हम भी उसे चीज के विरोध में अपने एविडेंस प्रेजेंट करें और लोगों को एक ऑथेंटिक इनफॉरमेशन प्रोवाइड करें। बड़ी जिम्मेदारी निकाल कर आती है कि हम लोगों से बात करते रहे जो गलत जानकारी फिर चाहे वह लोगों के दिमाग में बैठ ही क्यों ना गई हो हमारी कोशिश से रहनी चाहिए कि हम उन तक सही इनफॉरमेशन पहुंचाएं फिर वह किताब हो सकती है सोशल मीडिया के ऊपर हम अपना अलग तरीके से कम कर सकते हैं जिस तरीके से फेक न्यूज स्प्रेड की जाती है हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हम सच्ची खबर जो वाकई में जो घटना हुई है उसके बारे में अपनी जानकारी दें और जो ब्लॉक्स होते हैं ऑथेंटिक ब्लॉक को शेयर किया जाए तो यह सब चीज बड़ी जिम्मेदारी का काम निकाल कर आता है और इतिहास कारों का भी एक जिस तरीके से कई बार जो गुट बन जाता है वह इसे भी नुकसान देता है।
अरमान :- अगर हम दो साम्राज्यों की बात करें जिसमें जो मुगल काल है और दिल्ली सल्तनत का काल है यह अपने-अपने वक्त में काफी महत्वपूर्ण रहे और एक लंबे वक्त तक इन्होंने शासन किया जब दिल्ली सल्तनत से मुगल काल पर शिफ्ट होते हैं तो उस वक्त कौन से बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं? बाकी के दूसरे शासक रहे उनके साथ में रिलेशंस कैसे बिल्डअप हुए या बिगड़े उसे पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है
श्रेया:- जब दिल्ली सल्तनत से मुगल शिफ्ट हुए तो उसे वक्त भी काफी ऐसी डायनेस्टी थी जो अपने-अपने एरियाज पर रूल कर रही थी फिर चाहे वह छोटे-छोटे ही पार्ट्स में भी हम मगर बात करें या फिर राजपूताना थे तो वह भी एक अलग तरीके से रूल कर रहे थे तो काफी ज्यादा सबसे पहली बात तो यह है कि एरिया था जो खुद भी रूल कर रहा था या फिर हम जैसे साउथ इंडिया में दक्कन सल्तनत की बात करें तो वह भी उसे टाइम तक खुद से रूल थी। जब मुग़ल में शुरुआत आए तो उन्होंने काफी ज्यादा युद्ध लड़े जंग हुई । उन्हें यह चीज भी कहीं ना कहीं रिलाइज हो रही थी कि अगर उन्हें वाकई में हिंदुस्तान के ऊपर एक लंबे वक्त तक शासन करना है और अपना प्रभाव जमाए रखना है प्रभाव ऐसा के जिसमें जो आम जनता है उन्हें वह एक्सेप्ट करें शासन के रूप में। वह भी किस तरीके से जिस तरीके से वह बाकी राजाओं को सम्मान दिया करते हैं। यह चीज महसूस की कि हमें जो अपने ट्रेडीशंस है वह यहां के लोगों के साथ में जोड़ने होंगे। उन्हें वैसा ही सम्मान दें जैसा कि हम उनसे चाहते हैं। चलते उन्होंने राजपूत राजाओं के साथ में काफी संधियां हुई और मेट्रोमोनियल रिलेशन भी बिल्ड अप हुए। कि अगर आप और भी चीजों के ऊपर ध्यान देना सिर्फ शादी या फिर युद्ध के ऊपर जो संध्या हुई बल्कि जो स्मारक बने उनमें भी उनकी एक साझेदारी हमें देखने को मिलती है अगर हम यहां जयपुर में सिटी पैलेस की बात करें तो वहां पर आपको मुगल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा क्योंकि जयपुर का उसे वक्त मुगल से काफी अच्छा रिलेशन बना रहा था। उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाइयां साथ में भी लड़ी। जब बाद में उदयपुर के साथ में उनके संबंध सुधारे तब भी वहां भी हमें देखने को मिलता है कि मुगल आर्किटेक्चर की आपको झलक उनके महलों में देखने को मिल जाएगी। मैं नहीं कह सकती कि यह एकदम से हुआ उन्हें वक्त लगा यह चीज रिलाइज करने में और इसे स्टेबल करने के अंदर। ऐसा नहीं था कि आते ही उन्होंने रिलेशन सुधारने पर काम किया जाहिर सी बात है जब भी अगर आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपको थोड़ा पहले वक्त मिलता है आप वहां समझते हैं कि किस तरह के लोग हैं और वहां किस ढंग से हम अपना काम कर सकते हैं। वह तो प्रचलन ही ऐसा था कि आप तो पहले युद्ध लड़ते हैं और उसके बाद में वहां पर शासन किया जाता है। जब वह थोड़े स्टेबल हुए और उनका प्रभाव बढ़ा इंडिया के अंदर तब उन्होंने दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि अगर हम बात करें अकबर का जो टाइम पीरियड था उसमें उनके जो कछवाहा डायनेस्टी के जनरल उन्होंने काफी मंदिर भी बनवा जैसे वाराणसी, ब्रज इलाकों के अंदर निर्माण थे वह सब अकबर के सहयोग से हुए। सब चीज भी हमें देखने को मिलती है मुगल टाइम पीरियड में।
अरमान :- ऐतिहासिक इमारतों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं की सरकार ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है जो पुरानी बिल्डिंग है या फिर जो बड़े गेट बनाए गए हैं या फिर वक्त के साथ में उन पर ध्यान न देने की वजह से वह खुद ही गिर जाते हैं तो जिस तरीके से उन्हें नजर अंदाज किया जा रहा है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे और हम किस तरीके से उन्हें बचा सकते हैं? अगर मैं आपको इसका उदाहरण दूं बीकानेर शहर से आता हूं और वहां जो परकोटा है जो शहर की दीवार कही जाते थे उन दीवारों को ही लोगों ने अपना घर बना लिया है उसके अंदर उन्होंने अपने घर की दीवारें जोड़ ली है और जो कहीं हिस्से हैं उन्हें तोड़ दिए गए हैं लेकिन किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया हमें उन चीजों के ऊपर देखने को नहीं मिलती है।
श्रेया:- वाकई में बहुत गंभीर मसला है और यह हम देखते हैं कि किस तरीके से प्यासी की इमारत को कई बार लगता है नजरअंदाज किया जा रहा है यह बिल्कुल सही कहा आपने जो संरक्षण का काम है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ़ इंडिया के पास में है। लेकिन उन इमारत को संरक्षण देता है जो बहुत ज्यादा पुरानी है बहुत ज्यादा प्राचीन है जैसा कि आपने उदाहरण दिया पर परकोटे का तो कुछ शहर हैं जिनके ऊपर भी वह काम है जैसे जयपुर के अंदर अगर हम परकोटे की बात करें तो उनका संरक्षण है और उनके ऊपर सरकार भी ध्यान देती है लेकिन जैसा आपने बीकानेर का उदाहरण दिया तो ऐसी जगह पर वह ध्यान नहीं दे पाते या नहीं देते। हम यह भी देख सकते हैं कि इतनी क्षमता नहीं है कि वह हर एक छोटी-छोटी चीज का ध्यान रख सके तो यह जिम्मेदारी वहां के लोकल्स की भी बन जाती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बनती है कि वह उनको कैसे प्रिजर्व करते हैं और उनका बचाव फिर चाहे वह नेचुरल डिजास्टर की बात हो या फिर ऑक्यूपेशन की बात की जाए उनको वह किस तरीके से संरक्षण कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एएसआई को इससे पूरी तरीके से हट जाना चाहिए उन्हें और ज्यादा फंड की अगर है सरकार से लेकर तुम उन्हें भी वह बड़ी जिम्मेदारी है कि वह उन चीजों के ऊपर भी अपना नजर रखे। वह ऐसे ऑफिसर्स लगा पाए जो की ग्राउंड लेवल पर छोटे-छोटे जगह पर भी उन चीजों को प्रेशर रखें जैसे आपने बात अपनी कही के लोग उन पर अपने घर बना लेते हैं और उन पर कब्जा करने लग जाते हैं तो इन सब चीजों से बचाव की काफी ज्यादा जरूरत है। साथ ही में इतिहास की और ऐतिहासिक इमारत की जो अवेयरनेस है वह पूरे देश के अंदर बढ़ाने काफी ज्यादा जरूरी है तभी हम सही महीने में उनकी सुरक्षा कर पाएंगे वरना सिर्फ मशीनरी को उनके संरक्षण में डाला जाए उसे कुछ नहीं होगा जब तक की लोग अपने मन से उनके प्रति काम ना करें।
अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार ।
श्रेया - आपका भी बहुत आभार ।
Sarju Katkar 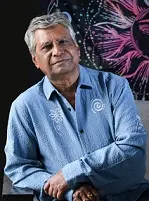
सरजू काटकर
मेरा लेखन मानवता को समर्पित है , मैंने उन्नीस साल की उम्र में साहिर लुधियानवी साहब का इंटरव्यू लिया था - सरजू काटकर
अरमान:- बात आपकी साहित्य में रुचि से करें ?
सरजू काटकर :- मैं एक कन्नड़ लेखक हूं । मातृभाषा मेरी मराठी है लेकिन मेरी जो शिक्षा है, पढ़ना लिखना वह सभी कन्नड़ भाषा में ही हुआ है। मैंने एम ए किया, पी एच डी किया उसके बाद पत्रकार बना और पत्रकारिता मैंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से शुरू की। और आपको बताऊं कि मेरी मातृभाषा मराठी है और जिसमें मैंने सब कुछ सीखा वह कन्नड़ भाषा, जो मैंने अखबार में लेखन शुरू किया वह अंग्रेजी । आपको बताऊं मेरी बीवी गुजराती है तो इस तरह चार भाषाओं का संगम आपको मेरे घर में मिलेगा । हम लोग चार भाषाएं बोल पढ़ लिख सकते हैं। जब मेरी उम्र काफी कम थी, मैं सातवीं क्लास में था उस वक्त से ही साहित्य में रुचि जगी । हमारे स्कूल में प्राइमरी तक अखबार निकला करता था हाथ से लिखा हुआ प्रिंट नहीं होता था । उस वक्त अखबार का एडिटर मुझे बनाया गया था।
लेखन की अगर मैं बात करूं तो मैं कविता लिखता हूं, उपन्यास लिखता हूं ,स्टोरी लिखता हूं, आर्टिकल लिखता हूं , ड्रामा लिखता हूं, अनुवाद करता हूं। इंग्लिश में अनुवाद किया , हिंदी से अनुवाद किया है। मराठी से अनुवाद किया है। 20 किताबें ऐसी है जो अनुवादित हैं , कन्नड़ में। आपको बताने की कोशिश करूं तो मेरी 80 किताबें हैं जिसमें से 6 उपन्यास है । आपको सुनकर हैरानी होगी कि यह जो 6 किताबें हैं इन सभी पर फिल्में बन चुकी है। और इन सभी उपन्यासों को अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और मिला भी स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक। एक फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। कर्नाटक में कर्नाटक साहित्य अकादमी है, मैं नौ साल तक लगातार मेंबर रहा। सरकार ने मुझे अपॉइंट किया। साहित्य अकादेमी दिल्ली में बड़े भाई साहब मधु आचार्य जी के साथ काम करने का मौका मिला। मेरा लेखन मानवता को समर्पित है । मैं यह कह सकता हूं कि गरीबों , पिछड़ा वर्ग और उनकी परेशानियों पर मेरा लेखन केंद्रित रहा । और हमेशा कोशिश यही रही कि उनकी जो परेशानियां है तकलीफें हैं उन्हें समाज के सामने उजागर किया जाए जिससे जो कमियां हैं वह भी सामने आएगी जो गलतियां हैं वह भी सामने आएगी और सभी एक दूसरे को देखकर समझ कर सामाजिक मूल्यों को मानकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जनहित के विरोध में मैं आज तक कभी नहीं लिखा और ना मैं जाता हूं और न कभी जाऊंगा। जब पत्रकारिता की तरफ जा रहा था और मैं आपको कहना चाहूंगा हमारे जो एडिटर थे वह समाजवादी थे वह राम मनोहर लोहिया के शिष्य थे। वह हमसे सवाल किया करते थे कि तुम किसके लिए लिखना चाहते हो तुम टाटा के लिए लिखना चाहते हो या बिरला के बारे में लिखना चाहते हो। मैं लिखना चाहता हूं समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के बारे में। आखरी कोने पर व्यक्ति है उसके बारे में लिखना चाहिए। इसका कोई नहीं है उसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता, ऐसा भी नहीं है लेकिन अगर तुम उस पर ध्यान ही नहीं दोगे उस पर लिखोगे ही नहीं तो लोग कैसे अपनी सामाजिक समस्याओं को समझ पाएंगे। तो अपने लेखन का केंद्र बिंदु उसे बनाओ।
अरमान -: कहा चार भाषाओं को जानते हैं ,पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा इन चारों भाषाओं के पाठकों को लेकर। इन चारों भाषाओं के साहित्य के जो पाठक हैं उनके जो विचार हैं या फिर मैं यूं कहूं उनकी जो मांग रहती है अपने लेखन से उन्हें आप कैसे डिफरेंटशिएट करेंगे या उन्हें आप कैसे संतुष्ट करेंगे क्योंकि अगर हम देखें सभी की अलग-अलग सोच है सभी अपने-अपने विचारों में अलग बुद्धिमत्ता को जन्म देते हैं तो यह जो फर्क नजर आता है या फिर मैं यह कहूं कि जो अलग मांग होती है लेखक से क्योंकि आप चारों भाषाओं को समझ सकते हैं जान सकते हैं तो सबसे बड़ा फर्क आपको क्या नजर आता है चारों भाषाओं के पाठकों में ना कि लेखक में ।
सरजू काटकर :- मैंने साहित्य अकादेमी के कन्नड़ भाषा के कन्वीनर के रूप में मैं काम किया और मैं कह सकता हूं 24 भाषाएं हैं 24 भाषाओं के अलग-अलग लेखक हैं जो इस काम को कर रहे थे जो सरकार से मान्यता प्राप्त है और वहां सिर्फ इन चार भाषाओं उन सभी से बात संवाद करने का मौका मुझे। एक बात कह सकता हूं जो पाठक के हृदय में बसा हुआ है फिर वह कहीं का भी पाठक हो चाहे वह कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का आप उन्हें अच्छा साहित्य अगर दे दीजिए अभी पाठक बेहतर साहित्य का स्वागत करते हैं। कन्नड़ में भी है बंगाली में भी है गुजरात में भी है सभी जगह है।
अरमान - अगर अच्छा साहित्य है तो वह दूसरा व्यक्ति भी से पढ़ना चाहेगा अगर कन्नड़ में कुछ लिखा हुआ है तो राजस्थान का व्यक्ति भी उसे पढ़ना पसंद करेगा। अनुवाद माध्यम से बिल्कुल सही कहा आपने।
सरजू काटकर :- अमेरिका का दौरा किया, मैं इंग्लैंड जाकर आया वहां के रीडर जो पाठक हैं उनसे जब संवाद हुआ वहां से भी कहीं ना कहीं यही बात आती थी कि आपका लेखन क्या मानवता के हित में है क्या आप मानवता को अपना लेखन समर्पित करते हैं या नहीं समिति। आपका लेखन क्या सामाजिक मूल्यों पर खरा उतरता है क्या वह उसे मदद करता है एक व्यक्ति को अपने सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए। अगर आपको अपने लेखन के बारे में एक बार फिर बताओ तो मैंने कभी बड़े सेठ साहूकारों के बारे में नहीं लिखा मैंने पिछड़े वर्ग जो एकदम आंखें छोर पर जो खड़ा व्यक्ति है उसके समस्याओं को जागृत करने की कोशिश रही। मैं आपको अगर बात बताऊं अपनी माता जी की तो वह अक्सर मुझे कहानी सुनाया करती थी वह कहती थी और कहीं ना कहीं आपको यह हर भाषा में रूपांतरण इसका मिल जाएगा तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार राजा की बेटी गायब हो जाती है मतलब एक राक्षस उसे उठाकर ले जाता है तो सेनापति का लड़का है वह कहता है कि मैं जाता हूं जंगल में और बचा के लाता हूं तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला दिखती है तो वह उसे लात मार कर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह उसे लात मारता है तो वह वहां पत्थर की मूरत में बदल जाता है। एक और मंत्री का लड़का कहता है कि इस बार मुझे मौका मिलना चाहिए , वह जाता है तो फिर वह बुजुर्ग औरत आती है उससे भीख मांगती है लेकिन वह फिर से से लात मारने की कोशिश करता है तो वह भी वहां पत्थर की मूर्ति बन जाता है। उसी राज्य का एक गरीब परिवार से लड़का कहता है कि मैं जाकर उसे बचा कर लाता हूं और वह खुद के लिए रोटी लेकर जाता है और फिर वही होता है बुजुर्ग महिला है उससे भीख मांगती है लेकिन इस बात क्या होता है वह अपनी रोटी दे देता है। महिला काफी खुश होती है और उससे कहती है कि मैं इसी ही तरह किसी का इंतजार कर रही थी और वह उसको बताती है कि तू जिससे लड़ने जा रहा है वह राक्षस बहुत खतरनाक है और तेरे पास कुछ है भी नहीं तो वह उसे कुछ पत्थर देती है। तो फिर इस तरीके से राजकुमारी को ले आता है। कहानी का जो मूल उद्देश्य बताना है कि जो गरीब व्यक्ति होगा वह हमेशा विनम्र होगा।
अरमान -: जैसा कि आपने बताया कि अपने पत्रकारिता भी की अंग्रेजी अखबार के लिए तो सवाल कर यही है क्या फर्क नजर आता है किसी तरह की क्षेत्रीयता को अगर हम देखें या फिर हिंदी और अंग्रेजी के जो पाठक हैं चाहे फिर वह न्यूज़ ही क्यों ना देखते हो क्या उसमें भी किसी तरह का कोई फर्क नजर आता है।
सरजू काटकर :- जब से सोशल मीडिया फ्रेम में आया है तब से कहीं ना कहीं कुछ चीज बदली है। और अगर हम कोरोना काल की बात करें तो उस वक्त तो सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा प्रभावी रूप से सामने हमें नजर आया। इसमें प्रिंट मीडिया तो बिल्कुल ही उसे वक्त बंद हुई थी लेकिन जो डिजिटल मीडिया जो सोशल मीडिया है वह बहुत ज्यादा अग्रसर होकर सामने आई अपने सवाल किया हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेजी अखबार पत्रिका में तो जब हम हिंदी पत्रकारिता को देखेंगे तो इसके साथ-साथ जो मराठी है गुजराती है इस पूरे क्षेत्र को भी एक साथ लिया जाए और दूसरे तरफ अंग्रेजी को रखा जाए। ना कहीं यह सारी भाषाओं को अगर हम देखें तो यह जान जनता के लिए जो पत्रकारिता है यह वह है और अंग्रेजी जो पत्र कहता है अंग्रेजी जो अखबार है वह ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो शासन प्रशासन से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए ज्यादा मान्य रखती है। और मैं एक बात को यह इस तरीके से भी समझाना चाहूंगा इंडियन एक्सप्रेस का उदाहरण लेते हुए , जब अंग्रेजी में अपने कुछ आर्टिकल या फिर न्यूज़ देंगे तो वह एक अलग फ्रेम में होगा लेकिन वही जब स्टेट लेवल में उनकी लोकल लैंग्वेज में उसे प्रकाशित करना होगा तो उसमें फर्क नजर आएगा । अंग्रेजी अखबार का जो प्रभाव मैंने देखा है वह ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जैसे एक मंत्री जी हैं उन्होंने अखबार देखा कन्नड़ का तो उसमें जो न्यूज़ आई थी वह उनके अंग्रेजी अखबार में नहीं आई थी तो वह यह कहते हैं कि अंग्रेजी अखबार में नहीं आई तो मैं कैसे मानूं। जो राज्य चला रहे हैं जो शासन प्रशासन के अंदर हैं उनके ऊपर अंग्रेजी अखबार का प्रभाव शुरू से ही हमें देखने को मिला है। तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं हर चीज का व्यवसायीकरण हुआ लेकिन जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो आजादी से पूर्व इसका उद्देश्य था आजादी दिलाना उसमें सहयोग करना लोगों तक जन संपर्क का एक माध्यम लेकिन जब आजादी मिली। उस वक्त इन अखबारों के कर्मचारियों में या मालिक में और यहां जो पत्रकार थे उनमें यह बिल्कुल था ही नहीं पैसा कमाना है या सैलरी के बारे में वह नहीं सोचा करते थे। और स्वतंत्रता मिलने के बाद जब इंडस्ट्रियलिस्ट इस क्षेत्र में आए तो वहां से बदलाव शुरू हुआ। हां से उन्होंने पत्रकारिता में निवेश करना शुरू किया और जब कहीं निवेश होता है तो जाहिर सी बात है मुनाफे की तरफ जाया जाता है और मुनाफे को ध्यान में रखा जाता है। हर जगह जिस तरीके से हम समझते हैं वही पत्रकारिता में भी हो रही है जो निवेश हुआ तो मुनाफे की होड़ तो लगेगी।
अरमान - सुनने में या फिर यह कहेंगे लगातार कहा जा रहा है कि गिरावट आ रही है पढ़ने वालों में जो एक रुझान था एक वक्त में पाठकों में वह रुझान कम देखने को मिल रहा है आपका इसमें क्या मानना है।
सरजू काटकर :- मैं बताना चाहूंगा मैं एक पत्रकार भी हूं और लेखक भी। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जब मेरी किताबें आई और उसके कहीं ना कहीं एडिशंस भी मैं निकले तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर किसी चीज के सीरीज निकल रही है तो उसे लोग पढ़ नहीं रहे या फिर ऑडियंस में गिरावट है तो मुझे नहीं लगता ऐसा सच में है। न सिर्फ मैं अपनी बात करूं मैं अगर कन्नड़ लेखन की ही आपको बात बताऊं तो जैसे दूसरे जो लेखक से वह अपनी किताबों के नोवेल्स के 10-10 एडिशन भी निकाल देते हैं तो ऐसा नहीं है की गिरावट है और लोग पढ़ रहे हैं पढ़ना पसंद करते हैं और शुरू से लेकर आज भी मुझे इसमें फर्क नजर नहीं आता मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि लोग सोशल मीडिया पर भी ई बुक्स भी पढ़ा करते हैं। रीडर और पाठक में गिरावट आई है तो इतना एडिशन भला कैसे आ सकते हैं। तो वही है कि हमें पाठकों तक पहुंचना जरूरी है हमें अपने पाठकों को समझना जरूरी है उन तक उनका साहित्य पहुंचना जरूरी है। किसी व्यक्ति को एक अच्छी किताब मिले तो वह उसे पड़ेगा वह चाहेगा उसे और समझना उसके बारे में उसके कैरेक्टर्स तक और उसे देखना लेकिन वही अगर मैं अखबार की बात करूं। जब पत्रकारिता में आया। इस वक्त में पूरे कर्नाटक में दो ही अखबार चला करते थे। लोकल अखबार जो कन्नड़ भाषा में छपते थे। आज मैं अगर आपको बताऊं तो स्टेट लेवल में 10 से ज्यादा अखबार हुए। अभी हर जिले में उनके अपने-अपने एडिशन हैं तो जिस तरीके से विस्तार हुआ है तो हम उसमें यह कैसे कह सकते हैं कि पाठकों में गिरावट आई है। जब हमने यहां बेलगाम में इंडियन एक्सप्रेस हमारे अध्यक्ष ने हमसे यही पूछा था। का सवाल था कि कितना सरकुलेशन तुम दोगे। उनको एक संख्या बताइए अपनी तरफ से तो वह हंसते हुए कहते हैं कि अगर इसमें से एक भी काम हुआ तो तेरी नौकरी गई। हम उसे वक्त बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे और हमने नए लोगों को जोड़ा हमने नए पाठकों को अखबार से जोड़ा और हम अपने काम में सफल हुए। आपको फिर एक बार कहना चाहूंगा कि मैं इस बात में नहीं मानूंगा कि पाठकों में गिरावट आई है।
अरमान - लेखन में आपकी सबसे प्रिय विद्या कौन सी है आपको कहानी लिखना ज्यादा पसंद है उपन्यास या फिर कविताएं सबसे ज्यादा आपकी दिलचस्पी किसमें है?
सरजू काटकर :- कर्नाटक में कवि के रूप में प्रसिद्ध हूं। मैं आपको कहना चाहूंगा बताना चाहूंगा कि मेरे घर का जो नाम है वह काव्य ही है। तो फिर उसके बाद में मैं कहानी लिखना शुरू किया नाटक लिखना शुरू किया ऐसा नहीं है कि मैं कविता को छोड़ दिया लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से थी। आज के टाइम में मैं ज्यादातर आर्टिकल्स भी लिखता हूं। मैंने आपको बताया कि अनुवाद भी किए हैं। मेरा जो पी एचडी का थीसिस का विषय है कन्नड़ और मराठी दलित साहित्य। पूरा एक तरीके से आप शोध कार्य देखिए कि जो दलित हैं वह कनाडा के जो दलित हैं उनके ऊपर और मराठी दलित है उन पर जो काम है वह इसमें सम्मिलित है। मां से पूछेंगे क्या आपको कब की कौन सी बेटी पसंद है तो वह कहेगी कि मुझे तो सभी पसंद है सभी एक बराबर है। अगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं नाटक लिखता हूं तो मैं पूरी तरीके से सिर्फ एक नाटककार की भूमिका ही समझता हूं। काव्य लिख रहा हूं तुम्हें पूरी तरीके से अपना आपको उसमें रुझान करता हूं। यही कहूंगा कि मुझे इन सभी से प्यार है और मैं किसी एक का नाम इसमें से नहीं ले सकता सब मेरे लिए बराबर है सभी विधाओं ने मुझे प्यार दिया और मैं भी यही कोशिश करता हूं कि मैं सभी को बराबर सम्मान और प्यार के दर्जे में रखो।
अरमान:- मेरा अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि हमें कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में गुटबाजी की समस्या देखने को मिल सकती है चीज जब हमें साहित्य लेखन समाज में देखने को मिलती है तो उसका जो असर है वह आम जनता पर समाज पर आप कैसे देखते हैं?
सरजू काटकर :- यह सवाल कई बार अलग-अलग तरीकों से सामने आता है आपको कहना चाहूंगा कि मैं गुटबाजी में नहीं मानता हूं। होता यूं है कि जब एक विचार रखने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनके जो सिद्धांत हैं जिन्हें वह मानते हैं और उन सिद्धांतों का वह प्रचार करने लगे तो उसमें एक तरीके से क्या गलत हम कह सकते हैं। स्वतंत्रता मिलने के उत्तर भारत में प्रोग्रेसिव लिटरेचर हमें देखने को मिलता है। साहिल लुधियानवी प्रोग्रेसिव लिटरेचर को मानते थे। इस तरह की की चीज होती है जब बहुत सारे चाय लेख को या दूसरे क्षेत्र में भी एक विचार वाले जब एक साथ हो जाते हैं तो वह जाहिर सी बात है वह अपने सिद्धांत है उनका प्रचार करेंगे तो उसे आप इस तरीके से मत देखिए कि वह गुटबाजी कर रहे हैं इसका शाब्दिक अर्थ कहीं ना कहीं वह हो सकता है लेकिन हम जब इसे बेहतर तरीके से समझेंगे तो मुझे लगता है इसमें फर्क नजर आएगा। की एक से विचार रखने वालों का संगठन ग्रुप का सकते हैं अपने सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा मैं कॉलेज में था। मेरे जो आदर्श थे शायरी में वह साहिर लुधियानवी थे। मैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए उन्हें देखने के लिए मुंबई गया। उसे वक्त मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। उनसे मिलने के लिए गया उनसे वक्त लिया उन्होंने कहा कि मेरे कोई कविता या ऐसा कुछ याद है आता है तो मैंने उस वक्त उन्हें वह सुनाई उनकी गंगा जमुना के अंदर में कविता थी तो वह मैंने पढ़कर उन्हें सुनाई थी और वह उसे वक्त काफी खुश हुए थे सुनकर। बाद में मुझे अपना इंटरव्यू दिया था।
अरमान:- आपको इतना वक्त हो गया है साहित्य से जुड़े हुए और जैसा कि मुझे याद है आपने कहा था कि कहीं सिक्स्थ क्लास से ही कनेक्शन आपका हो चुका था तो इस लेखन के सफर में कोई ऐसा समय कल आपको ध्यान आता है कि उसे वक्त आपको ऐसा लगे कि मुझे यह संदेश में पाठकों तक पहुंचना चाहिए और उसे विषय संदेश के लिए ही आपने कुछ लंबे वक्त तक लिखा हो?
सरजू काटकर :- जैसा कि हम बात कर ही रहे थे और शुरू में मैंने आपको कहा कि मेरा जो लेखन रहा हमेशा से ही वह गरीबों को पिछड़ों को समर्पित राहत और मेरा हमेशा से ही उद्देश्य रहा कोई एक समय काल में नहीं बता सकता मैं हमेशा से ही इसी चीज में रहकर जो व्यक्ति समाज के आखिरी छोर पर खड़ा है उसके लिए मैं लिखूं उसकी आवाज बनने की कोशिश करूं। और देश के अंदर जो नफरत की भावना पनप रही है उसे अपनी तरफ से काम किया जाए यही मेरा उद्देश्य रहा हमेशा सही लेखन के माध्यम से। मेरा मानना यही है कि अगर ईश्वर ने हमें कुछ दे रखा है तो हम समाज के लिए उसे उपयोगी बनाएं ना कि सिर्फ खुद के बारे में सोचें। चाहे मेरी किसी भी कहानी को उठा लीजिए किसी भी उपन्यास को पढ़ लीजिए। लेखन आपको मानवता के लिए ही समर्पित मिलेगा। मेरा जो लेखन का केंद्र बिंदु हमेशा से मनुष्य ही रहा मानवता, मानव अधिकार यहीं कहीं ना कहीं मेरे लेखन साहित्य का केंद्र बना रहा। मेरा मानना है कि मनुष्य से बड़ा कोई भी नहीं। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भगवान को जब धरती पर प्रकट होना था तो उन्होंने किसका रूप लिया वह इंसानी रूप में आए यानी। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है।
अरमान - शब्द संवाद के लिए आपने समय दिया ,बहुत आभार
सरजू काटकर - बहुत धन्यवाद
परिचय - श्री सरजू काटकर
कविता
बेन्की बेरू: विवेकानन्द प्रकाशन, नवलगुंड, 1973. हसीदा नेला: वाई उगधवानी प्रकाशन, धारवाड़, 1976. सूर्या : साहित्य प्रकाशन, पाशापुर, 1982. घोषणापत्र: पैंथर प्रकाशन, हुबली, 1988, विश्व कन्नड़ सम्मेलन के उत्सव को चिह्नित करने के लिए पुनः प्रकाशित 2011. एकांतदा मनुष्य: वी ऐशाका प्रकाशन, बेंगलुरु, 1993. पेगासस 7. गज़ल: वी आइशाका प्रकाशन, बेंगलुरु, 1996: वी आइशाका प्रकाशन, बेंगलुरु, 1999. हाइकु: परमशंकर प्रकाशन, शिगली- गडग,
1999. आवा: लोहिया प्रकाशन, बेलारी, 2001. नेविले नेवेलु: अन्वेषेणे प्रकाशन, बेंगलुरु, 2003. गांधी से गोधरा: लोहिया प्रकाशन, बेल्लारी, 2007. बेली सैल्मन: रूपा प्रकाशन, मैसूरु, 2008. उतखानाना: (चयनित कविताएँ) बेलाडिंगलु प्रकाशन,
काव्य अनुवाद
1. मराठी दलित काव्य (मूल: मराठी): लोहिया प्रकाशन, बेल्लारी,
1999
2. अटल बिहारी वाजपेयी कविथेगलु (मूल: हिंदी): विमोचन
प्रकाशन, अथानी, 1999, दूसरा संस्करण। वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2018
कहानियों का संग्रह
1. अथिथा: रूपा प्रकाशन, मैसूरु, 2008
कहानियों का संग्रह (अनुवाद)
1. सआदत हसन मंटो कथेगाकु: रूपा प्रकाशन,
मैसूर, 2008, दूसरा संस्करण: अजब प्रकाशन, कोल्हापुर, 2020
पेशे पर आधारित कहानियाँ
1. साक्षी: लोहिया प्रकाशन, बेलारी, 2002
2. वृथंथा: रूपा प्रकाशन, मैसूरु, 2008
3. हेललागाडा कथेगलु: बेलाडिंगलु प्रकाशन, बेलगावी, 2010
उपन्यास
1. देवराय: विमोचन प्रकाशन, अथानी, 2002, दूसरा संस्करण। 2022
2. 22 जुलाई, 1947: वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2015, दूसरा संस्करण। 2023
3. बाजीराव मस्तानी: वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2016
4.सावित्रीबाई फुले: वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2017, दूसरा संस्करण 2018,
5. गौरीपुर: वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2018
6. डांगे: वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2021
उपन्यास अनुवाद
1. ओन्दुरिनल्ली ओब्बा राजनिद्दा: (मूल: मराठी: माधवी देसाई)
रूपा प्रकाशन, मैसूरु, 2008
उपन्यास
1. देवराय: ('इंगले मार्ग' मूवी, 2013)
2. 22 जुलाई 1947 : (फिल्म 2015)
3. बाजीराव मस्तानी: (फिल्म 2016)
4.सावित्रीबाई फुले : (फिल्म 2018)
5. गौरीपुर: ('दंतपुराण' मूवी 2020)
पी एच. डी थीसिस
1. कन्नड़ मराठी दलित साहित्य: एक तुलनात्मक अध्ययन: विमोचन
प्रकाशन, अथानी, 1996 दूसरा संस्करण; रूपा प्रकाशन, मैसूरु,
2010
टीआरए वेलौगे
1. मुक्कम पोस्ट लंदन: श्रुति प्रकाशन, बेलगावी, 2003
नाटक
1. अम्बे: कलारंगा प्रकाशन, बेलगावी, 2003
नाटक (अनुवाद)
1. चिन्ना: (मूल: मराठी: वी अमन तावड़े) पारस प्रकाशन, बेलगावी,
2005
2. देहभाना: (मूल: मराठी: अभिराम भड़कमाकर) सुंदर
प्रकाशन, धारवाड़, 2010
3. मूरनेय मंत्र: (मूल: हिंदी: वाई ओगेश त्रिपति) वाई अजी प्रकाशन,
होसपेट, 2018
तर्कसंगत/दार्शनिक कार्य
1. कोरेगांव: कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी, 2001
दूसरा संस्करण: स्वदेशी परिषद
भारत के लोग, बेंगलुरु, 2020
2. बसव मट्टू: लिंगायत अध्ययन अकादमी, बेलगावी, 2003
मैसूरु, 2018
3. पत्रिके मट्टू साहित्य: अन्वेषेणे प्रकाशन, बेंगलुरु, 2003
4. कुवेम्पु कविशैला मट्टू शेक्सपियरन ऊरु: पारस प्रकाशन,
बेलगावी, 2006
5. शिवाजी मूल कन्नड़ नेला: लोहिया प्रकाशन, बल्लारी। मार्च 2006,
लोकप्रिय संस्करण: अजब प्रकाशन,
कोल्हापुर, 2020
6. आषाढ़स्य प्रथम दिवसे: रूपा प्रकाशन, मैसूरु, 2008
7. इथ्यादि इथ्यादि: रूपा प्रकाशन, मैसूरु, 2008
8. सिनेमा सिनेमा: रूपा प्रकाशन, मैसूरु, 2008
9. शरण संस्कृति: श्री करणजी मठ प्रकाशन, बेलगावी, 2009
तर्कसंगत/दार्शनिक कार्य (अनुवाद)
1. सुप्रसिद्ध भासनगागु (मराठी मूल: डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर),
वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, अप्रैल 2014, दूसरा संस्करण: जून 2014, तीसरा
संस्करण: 2019,
2. नानू हिंदू आगी हुतिद्दीन, आदारे हिंदू आगी सयालारे (मराठी)
मूल: डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर), वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2018
3. मुतिसीकोल्लडवरन्नु नवेके मुतबाबेकु? (मराठी मूल: डॉ.
बाबासाहेब अम्बेडकर), वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2018
4. मराठी कलबुर्गी (मूल मराठी लेख): लिंगायत अध्ययन संस्थान,
जगद्गुरु टोंटादार्य संस्थान मठ, गडग, 2018
ऐतिहासिक वर्णनात्मक रचनाएँ
1. छत्रपति शिवाजी- महान मराठा: वाई अजी प्रकाशन, होसपेट,
2024
2. वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा: वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2024
आत्मकथात्मक कथाएँ
1. नानू पाटिल पुत्तप्पा भाग-1: लोहिया प्रकाशन, बल्लारी, 2011, दूसरा
संस्करण: 2014
2. नानू पाटिल पुत्तप्पा भाग-2: लोहिया प्रकाशन, बल्लारी, 2014
आत्मकथात्मक अनुवाद
1. वाल्मिकी: (मूल मराठी: डॉ. भीमराव गस्ती), सृष्टि प्रकाशन,
बेंगलुरु, 2008, दूसरा संस्करण: 2021, लोकप्रिय संस्करण: अजब प्रकाशन,
कोल्हापुर, 2020
2. आवा: निन्ना अरियाली हयांग?: (मूल मराठी: डॉ. उत्तम कांबले),
रूपा प्रकाशन, मैसूर, 2008, दूसरा संस्करण: अजब प्रकाशन,
कोल्हापुर, 2020
3. चंपा लिमये नेनापुगाडु: (मूल मराठी: चंपा लिमये), लोहिया
प्रकाशन, बल्लारी, 2010, दूसरा संस्करण: अजब प्रकाशन, कोल्हापुर,
2020
4. मधु लिमये आत्मकथे: (मूल मराठी: मधु लिमये), लोहिया
प्रकाशन, बल्लारी, 2010
5. नानू हीगे रूपुगोंडे: (मूल मराठी: भालचंद्र मुनगेकर),
साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2013
जीवनी संबंधी आख्यान
1. कुसुमाग्रज: कर्नाटक साहित्य अकादमी, बेंगलुरु, 2004
2. कर्नाटकादा आत्मगौरव पाटिल पुतप्पा: बैंगलोर विश्वविद्यालय, 2006
4. डॉ. पाटील पूतप्पा: लिंगायत अध्ययन संस्थान, गडग, 2014
5. परमेश्वरप्पा बागीगर: लिंगायत अध्ययन संस्थान, गडग, 2016
6. भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: बेलगावी जिला
प्रशासन, बेलगावी, 2022
7. आदर्श राजकरणी एस.आर. बोम्मई: कन्नड़ साहित्य परिषद, बेंगलुरु,
2023
8. दलित सूर्या डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2023
संपादित कार्य
1. विक्षिप्त: (युवा कवियों की कविताएँ) विवेकानन्द प्रकाशन, नवलगुंड,
1973
2. स्नेहा सम्पदा: (डॉ. तेजस्वी कट्टीमनी अभिनंदन वी ओलूम) सीवीजी
प्रकाशन, बेंगलुरु, 2007
3. कन्नड़ बंदय साहित्य: साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2011
4. कन्नडवे सत्य कन्नडवे नित्य: रूपा प्रकाशन, मैसूरु, 2008
5. कर्नाटक संस्कृति: बेलाडिंगलु प्रकाशन, बेलगावी, 2009
6. बेलगावी संस्कृति: बेलाडिंगलु प्रकाशन, बेलगावी, 2011
7. लिंगायत संस्कृति: (डॉ. टोंटाडा सिद्धलिंग स्वामीजी सत्कार वी ओलूम)
बेलाडिंगलु प्रकाशन, बेलागवी, 2017
8. सव्यसाची: (प्रो. ए.आर. पाटिल अभिनंदन वी ओल्यूम) 2018
9. कंबर काव्य करण: वाई अजी प्रकाशन, होसपेट, 2019
10. मेघमित्रा: (क्षेत्रीय आयुक्त पी. ए. मेघन्नवर अभिनंदन
वी ओलूम) 2021
11.मैत्री: (राहुल कांबले अभिनंदन वी ओलूम), 2023
डॉ. पर साहित्य सरजू कटकर
1. एकांत लोकांतगला नादुवे
संपादित: डॉ. गुरुपाद मारीगुड्डी और विजयकुमार कटगिहल्लीमथ,
अनिमिषा प्रकाशन, बागलकोट, 2009
2. काव्यकार्तिक डॉ. सरजू काटकर
प्रकाश गिरीमल्लनवर,
जिला कन्नड़ साहित्य परिषद, बेलगावी, 2013
पुरस्कार
1. कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, बेंगलुरु (2007)
2. कर्नाटक साहित्य अकादमी मानद पुरस्कार, बेंगलुरु (2003)
3. कर्नाटक अनुवाद साहित्य अकादमी मानद पुरस्कार, बेंगलुरु (2008)
4. कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु द्वारा जगजीवन राम पुरस्कार (2006)
5. आनंदकंद साहित्य पुरस्कार, धारवाड़ (2006)
6. सिरिगन्नाडा साहित्य पुरस्कार, बेलगावी (2008)
7. कर्नाटक विद्यावर्धक संघ पुरस्कार, धारवाड़ (1976)
8. संगति साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुणे (1994)
9. नारायणराव वेड साहित्य प्रतिष्ठान पुरस्कार, बागलकोट (1995)
10.कर्नाटक संघ का जी.एस. शिवरुद्रप्पा काव्य पुरस्कार, शिवमोग्गा (1999)
12. लिंगराज साहित्य पुरस्कार, अथानी (2001)
13. जर्नलिस्ट्स फोरम मीडिया अवार्ड, बेंगलुरु (2001)
14.विश्व कन्नड़ सम्मेलन पुरस्कार, अमेरिका (2000)
15. गोरुरु साहित्य पुरस्कार, बेंगलुरु (2000)
16.सर एम. विश्वेश्वरैया दशकीय सर्वश्रेष्ठ अनुवाद साहित्य पुरस्कार,
बेंगलुरु (2002)
17.एम.के. प्रचार अभिमन्यु पुरस्कार, बेलगावी (2002)
18.काव्यानंद साहित्य पुरस्कार, बेंगलुरु (2002)
19.नागनूरु मठ प्रतिभा पुरस्कार, बेलगावी (2002)
20.जिला मराठी पत्रकार संघ सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार, बेलगावी
(2002)
21.मुंबई कर्नाटक संघ का वी अरदराजा आद्या पुरस्कार, मुंबई (2003)
22.हलाकट्टी श्री पुरस्कार, महालिंगपुर (2004)
23.डॉ. नल्लूर प्रसाद साहित्य-सांस्कृतिक पुरस्कार, बेंगलुरु (2004)
24.विश्वनाथ वारमबली प्रतिष्ठान पुरस्कार, हावेरी (2004)
16
25.डॉ. एस.एस. कोटिन आलोचना पुरस्कार, मुदालगी (2004)
26.हवनूर प्रतिष्ठान पुरस्कार, हावेरी (2003)
27. करावली सांस्कृतिक फाउंडेशन सुवर्णा कन्नडिगा पुरस्कार, कासरगोड (2006)
28. हुबली-धारवाड़ महानगर सभा राज्योत्सव पुरस्कार, हुबली (1986)
29.यू. के. मेयर्स रिकग्निशन अवार्ड, लंदन (2000)
30.यू. के. कन्नड़ बालागा सम्मान, लंदन (2000)
31. विश्व मिलेनियम कन्नड़ सम्मेलन ह्यूस्टन (यूएसए) विशेष
मान्यता पुरस्कार, ह्यूस्टन (2000)
32. आईएमईआर उत्कृष्टता पुरस्कार, बेलगाम (2001)
33. लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा पुरस्कार, बेलगाम (2001)
34. श्री गणेश महोत्सव मानद पुरस्कार, बेलगावी (2006)
35. वीर रानी कित्तूर चेन्नम्मा पुरस्कार, बेलगावी (2007)
36. कर्नाटक मीडिया अकादमी मानद पुरस्कार, बेंगलुरु (2002)
37. गा. गो. राजाध्यक्ष पत्रकार पुरस्कार, बेलगावी (1
39.जायंट्स इंटरनेशनल अवार्ड (कर्नाटक-गोवा यूनिट), बेलगावी (2008)
40.'अम्मा' साहित्य पुरस्कार, सेदाम (2008)
41.एच. के. वी. ईरन्नागौड़ा पत्रकार पुरस्कार, मैसूर (2010)
42.शराना उरीलिंगपेड्डी पुरस्कार, भालकी (2010)
44.समाज भूषणा, पुणे (2012)
45.रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मानद डॉक्टरेट की उपाधि,
बेलगावी (2013)
46.कर्नाटक सरकार का प्रतिष्ठित 'संशोधक कुंडंगारा पुरस्कार'
(2013)
47.आठवें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन, बेलगावी जिले के अध्यक्ष (2013)
48.कन्नड़ साहित्य परिषद, बेंगलुरु द्वारा कुवेम्पु सिरिगन्नदा पुरस्कार ( 2015)
49.श्री करणजी मठ मानद पुरस्कार, बेलगावी (2013)
50.अज़ूर प्रतिष्ठान सर्वोत्तम पुस्तक पुरस्कार, हारुगेरी (2004)
51.दलित साहित्य परिषद पुरस्कार, गडग (2009)
52.बेलगावी जिला साहित्य प्रतिष्ठान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पुरस्कार (2017)
53.सिरीगन्नादा राष्ट्रीय प्रतिष्ठान बेलगावी 'सिरीगन्नादा सम्मान' (2013)
54.परिमाला पुरस्कार, पास्चपुर (2016)
55.बसव विचार प्रसारक पुरस्कार, लातूर (2009)
56.श्री आर गुंडुराव पुरस्कार, हुबली (2013)
57.अखिल भारत शरण साहित्य परिषद बेंगलुरु शकुंतला जयदेव
शरण पुरस्कार (2017)
58.बेलगावी जिला साहित्य प्रतिष्ठान 'सिरीगन्नादा पुरस्कार' (2016)
59.जगन्नाथराव टंकसाली प्रतिष्ठान मुधोल सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार (2015)
60.शिवराम कारंत प्रतिष्ठान मूडबिद्री शिवराम कारंत पुरस्कार (2019)
61.सिरीगन्नादा राज्योत्सव पुरस्कार, बेलगावी (2018)
62.राजश्री छत्रपति शाहू महाराज पुरस्कार, धारवाड़ (2016)
63.अप्पा पुरस्कार, चामाकेरी (2019)
64.लोक विश्वास प्रतिष्ठान गोवा सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार (2018)
65.'इंगले मार्गा' के लिए कर्नाटक सरकार का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सरोकार वाली फिल्म का पुरस्कार
(2008)
66.फिल्म 'इंगले मार्गा' के गीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार
, गोवा( 2015)
67. 22 जुलाई, 1947 को उपन्यास आधारित सिनेमा की पटकथा कर्नाटक को प्राप्त हुई
सरकार का सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार, 2015
68.फिल्म 'सावित्रीबाई फुले' के लिए राज्य पुरस्कार 2018
69.बेंगलुरु इंटरनेशनल में 'सावित्रीबाई फुले' के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार
फिल्म फेस्टिवल, 2019
70.पुस्तक के लिए कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से पुरस्कार
'मराठी कलबुर्गी,
' 2018
71.डॉ. बसवराज कट्टीमनी ट्रस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड, 2020
72.बसवश्री पुरस्कार, कालाबुरागी, 2022
73.अप्पा पुरस्कार, बेलगावी, 2022
74.के. एस. नरसिम्हास्वामी ट्रस्ट अवार्ड, मांड्या, 2023
75.साधक रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023
76.कर्नाटक नाडा पोशक पुरस्कार, मुद्राडी (उडुपी), 2023
न्यूज़ 18 चैनल, बेंगलुरु, 2024 द्वारा 'श्रेष्ठ कन्नडिगा' पुरस्कार
78.कर्नाटक सरकार का प्रतिष्ठित टीएसआर पत्रकार पुरस्कार, बेंगलुरु,
2024
डॉ। वी एरियस समितियों पर सरजू कटकर
1. 2. 3. 4. सदस्य, कर्नाटक राज्य पाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तक समिति, बेंगलुरु (1986)
सदस्य, कुवेम्पु शताब्दी हाई-पावर कमेटी, बेंगलुरु (2003)
सदस्य, पम्पा पुरस्कार चयन समिति, बेंगलुरु (2003, 2008)
सदस्य, अतीमब्बे साहित्य पुरस्कार चयन समिति, बेंगलुरु (2003)
5. सदस्य, कर्नाटक साहित्य अकादमी, बेंगलुरु (1988-91, 1992-95,
1995-98)
6. संयोजक, साहित्य संवाद, बेलगावी (1988 से)
7. जिला संयोजक, बंदया साहित्य संगठन, बेलगावी (लगभग 15 वर्ष तक)।
साल)
8. अध्यक्ष, प्रेस क्लब, बेलगावी (1980-82)
9. सदस्य, टेलीफोनिक सलाहकार समिति (दो पद)
10. सचिव, कर्नाटक संघ, बेलगावी (1980-85)
11. जूरी, कन्नड़ फिल्म चयन समिति, बेंगलुरु (2004)
12.सदस्य, टीएसआर पत्रकार पुरस्कार चयन समिति, बेंगलुरु (2009)
13.सदस्य, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार चयन समिति, नई दिल्ली
(2006, 2008)
14.सदस्य, अकादमिक परिषद, लिंगराज कॉलेज, बेलगावी (2007)
15.सदस्य, पुस्तक चयन समिति, कन्नड़ पुस्तक प्राधिकरण, बेंगलुरु
(2004)
16. संपादक, विद्यार्थी भारती (कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ का प्रकाशन)
(1974-76)
17.संपादकीय बोर्ड सदस्य, अन्वेषाणे-साहित्यिक पत्रिका, बेंगलुरु (1990)
18.सदस्य, कवि चयन समिति, विश्व कन्नड़ सम्मेलन, बेलगावी
(2011)
19.अध्यक्ष, कवि चयन समिति, गदिनाडु सम्मेलन, बेलगावी
(2006)
20.सदस्य, सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन गृह चयन समिति, कन्नड़ पुस्तक
प्राधिकरण, बेंगलुरु (2006)
21.सदस्य, सीमा विकास प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु
(2009)
22.सदस्य, डॉ. बेटागेरी कृष्णशर्मा मेमोरियल ट्रस्ट, कर्नाटक
सरकार, बेंगलुरु (2011 से)
23.सदस्य, कर्नाटक मीडिया अकादमी (2011-2014)
24.सदस्य, सलाहकार बोर्ड, प्रसारंगा, रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय,
बेलगावी
25. सिंडिकेट सदस्य, रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय, बेलगावी
26. सिंडिकेट सदस्य, कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी
27.सदस्य, केंद्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्ली (2018- 2022)
28.सदस्य, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार चयन समिति, बेंगलुरु
(2015, 2017, 2018)
29.अध्यक्ष, बेलगावी पब्लिक लाइब्रेरी गा. गो. राज्याध्यक्ष पत्रकार पुरस्कार
समिति (कन्नड़) (2000 से)
30.सदस्य, लिंगायत वी ईरशैव पृथक धर्म आयोग (न्यायमूर्ति)
नागमोहन दास आयोग, 2018)
31.सदस्य, रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगावी प्रतीक चयन
समिति, बेलगावी (2011) सदस्य, छत्रपति शाहू महाराज अध्ययन केंद्र सलाहकार समिति, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (2019)
Darshan Darshi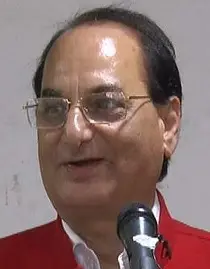
दर्शन दर्शी
जम्मू कश्मीर सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे, साहित्य अकादेमी दिल्ली से पुरस्कृत बहुभाषी साहित्यकार श्री दर्शन दर्शी से अरमान नदीम की खास बातचीत ।
लेखक को खुद आलोचक बनकर अपनी लेखनी को देखना चाहिए - दर्शन दर्शी
अरमान नदीम :- साहित्य में शुरुआत कैसे हुई ,कैसे रुचि हुई आपकी ?
दर्शन दर्शी :- अरमान जी ,यह प्रश्न साहित्यकारों से अक्सर पूछा ही जाता है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म जम्मू से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर गांव में हुआ। इत्तेफाक से हमारा गांव जम्मू कश्मीर का सबसे पढ़ा लिखा गांव माना जाता है। अदबी माहौल भी शुरू से ही मिला। और हमारे स्कूल में काफी मैगजीन और न्यूजपेपर मंगवाए जाते थे। गांव में काफी वक्त लगता था पोस्ट डाक के माध्यम से। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं तो शुरुआत से ही मेरी रुचि पढ़ने लिखने में काफी रही । और मेरा शुमार जहीन बच्चों में किया जाता था। मेरा काफी वक्त लाइब्रेरी में ही बीतता था । वहां मैंने हिंदी ,अंग्रेजी, उर्दू सभी तरह के लेखकों के बारे में पढ़ा उनकी रचनाओं को मैंने पढ़ा तो वहां से कहीं ना कहीं रूचि जागी। साहित्य पढ़ने का मुझ पर काफी प्रभाव रहा जिस वजह से मैं लिख सका और लिखना शुरू किया। गांव में एक नाटक क्लब था जिसमें हर साल रामलीला के अलावा और दूसरे नाटक भी हुआ करते थे। साहित्य से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम या एक सोर्स जिसे कहूं वह नाटक क्लब था मेरे लिए।
अरमान नदीम :- साहित्यकार का जो ताल्लुक बनता है अपने पाठकों के साथ और उसका यह रिश्ता ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने पाठकों के साथ जो रिश्ता है उसे कैसे बयां करते हैं?
दर्शन दर्शी :- मैं आपको बताऊं जब कविता की शुरुआत कुछ इस तरीके से ही हुई थी कि मित्रों दोस्तों और सब लोगों को मुत्तासिर करने की कोशिश लेकिन जब धीरे-धीरे कोशिश की कलम को गंभीर रूप से पकड़ने की तो जो एक संवाद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा मैं मूलरूप से अपने आप को एक डोंगरी लेखक के रूप में ही मानता हूं। और जब डोगरी साहित्य में पठन-पाठन लेखन जब शुरू हुआ तो मुझे उसे वक्त काफी सराहना मिली। उससे लेखन को बड़ा प्रोत्साहन मिला। और जो मेरे श्रोता है ,मेरे पाठक हैं उनसे मैं लगातार ही संवाद किया करता था। वह मेरा अपना एक तरीका था। क्योंकि सबसे बड़ा कारण था कि अगर मेरे पाठक मेरे श्रोता मेरे लेखन को पसंद करते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह उसे क्यों पसंद करते हैं । ऐसा उन्हें उसमें क्या मिला जिसे वह इतना चाहने लगे। कौन सा वह हिस्सा पसंद करते हैं। किसी से मुझे यह भी मालूम रहता कि मुझे कौन सा लेखन ज्यादा करना चाहिए कौन सी विधा में मुझे ज्यादा लिखनी चाहिए । किस तरह के श्रोता कौन से पाठक मेरे पास ज्यादा हैं। लोगों को ज्यादा क्या पसंद है जो लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। वह चीज कौन सी है इससे यह मालूम पड़ता है। और कविताएं और खास करके डोगरी ग़ज़ल उस पर मैंने काफी काम किया है। डोगरी ग़ज़ल जिस पर मैंने काम किया उसे काफी सराहना मिली। आज भी मिलती रही है तो इस तरीके से मैं अपना काम करता हूं। फिर धीरे-धीरे किताबें प्रकाशित हुई और धीरे-धीरे पढ़ाई जाने भी लगी स्कूल कॉलेज में।
अरमान नदीम :- ऐसा लग सकता है पाठक समझ नहीं पाता है कि लेखक उसे क्या समझाना चाहता है और इसके चलते कई बार वह लेखक की आलोचना करने लगता है । मैं यह जानना चाहूंगा जब किसी लेखक की आलोचना होती है तो आप उसे कैसे देखते हैं । मेरी नजर में तो आलोचना लेखक की सबसे बड़ी रचना होती है।
दर्शन दर्शी :- मैं आलोचना को दो तरह तरह से लेने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि लेखक को अपनी आलोचना आप करनी चाहिए। जैसे मैं अंग्रेजी साहित्य बहुत पढ़ता हूं, उर्दू और हिंदी पढ़ता रहता हूं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है खासकर कि अंग्रेजी साहित्य में देखने को मिलते हैं। साहित्यकार अपनी कृति से संतुष्ट न होकर उसे काफी वक्त तक रख देगा। और दो साल बाद उसे दोबारा देखेगा। खुद लगेगा कि यह इस हाल में नहीं छपना चाहिए था। बहुत पढ़ने की जरूरत है। काफी बदलाव की जरूरत नजर आती है। यह तरीका है जिस तरीके से उसे सुधार कर फिर पब्लिश करेगा। मेरे यहां कुछ ऐसी भाषाएं हैं जैसे डोगरी क्षेत्रफल के हिसाब से कहिए या रीजन के हिसाब से कहिए पढ़ने लिखने वालों के हिसाब से कहिए तो हम उसे थोड़ी छोटी भाषा कह सकते हैं। उसके लेखन का दायरा सीमित है ,छोटा है। मैं यह कह सकता हूं लेखन में हमारे यहां तुरंत लिखना और तुरंत छापने का जो मोह है वह बहुत अधिक पाया जाता है । तो आलोचना यह है कि लेखक को खुद आलोचक बनकर अपनी लेखनी को देखना चाहिए। दूसरी आलोचना है आलोचक की और इसमें भी यह बात है कि जो आलोचक है वह आपकी रचना की आलोचना किस तरीके से कर रहा है क्या वाकई में वह पढ़ कर उसका आकलन करके, उसकी आलोचना कर रहा है या फिर किसी व्यक्तिगत कारण के साथ में वह अपनी राय बना रहा है । यह भी समझने और देखने वाली बात होती है। कि वह आपका मित्र नहीं है वह आपसे किसी बात को लेकर नाराज है तो वह आलोचना आलोचना नहीं मानी जा सकती। क्योंकि यहां वह आपके लेखन को नहीं वह आपके व्यक्तिगत रूप से समस्या समझता है। वाकई जो आलोचना होती है लेखन की जिसे वाकई में पढ़कर आकलन किया जाता है उसका तो स्वागत सभी लेखकों को करना चाहिए। क्योंकि वह भी एक सीखने का तरीका है।
अरमान नदीम :- आपने कहा कि हो सकता है व्यक्ति नाराज हो इस वजह से आलोचना कर सकता है। अगर वह किसी चीज से नाराज होकर व्यक्तिगत रूप से आलोचना कर रहा है तो वह आलोचना कैसी, मैं तो उसे हसद कहूंगा और हसद और आलोचना में तो काफी फर्क है।
दर्शन दर्शी :- मैंने जैसे शुरू में ही कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस भाषा में लिख रहे हैं । किस माहौल में आपका लेखन हो रहा है, पढ़ा जा रहा है । अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है हिंदी में कुछ लिखा गया है या उर्दू में लिखा गया है लेखक को यह तो जरूरी नहीं आलोचक उसे व्यक्तिगत तौर पर जानता हो। इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से तो पहचानता ही नहीं है इसलिए उसे पहचानता ही उसके लेखन के जरिए है। मैंने कहा जब क्षेत्र या भाषा छोटी होती है तो वहां ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं । जहां लेखक और आलोचक एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते भी हो। यह बात तो आप भी मानेंगे कि एक लेखक को उसके निजी जीवन से और उसकी लेखनी से दो हिस्सों में बांटना बहुत मुश्किल है। इसी तरह आलोचक की कलम को ,दिमाग को ,उसके व्यवहार को निजी ताल्लुकात से पूरी तरह जुदा करना भी मुश्किल है।
अरमान नदीम :- मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा आपने कहा के लेखक में आत्म आलोचना होनी चाहिए । अपनी रचना लिखकर कुछ वक्त के लिए रख देनी चाहिए जब पढ़ेगा तो उसे लग सकता है इसे छापना नहीं चाहिए था । यह किसी काम की नहीं है या वह समाज के दायरे को पूरा नहीं करती आपको ऐसा नहीं लगता वह समय की मांग होती है। मैं आज के सामाजिक मुद्दों पर या राजनीतिक घटनाओं के ऊपर कुछ लिख रहा हूं तो वह दो साल बाद भी उतन ही प्रासंगिक रहेगा ।
दर्शन दर्शी :- इसमें एक तो वह साहित्य है समय की घटना से उसे वक्त के माहौल से प्रभावित होकर लिखा गया हो। वह साहित्य है जो सही मायने में हम क्लासिकल लिटरेचर कहते हैं अंग्रेजी में। समय के लिए उतना ही उपयुक्त है। तरीके से खाना हम बनाते हैं तो उसे अच्छे से परोसने वाली हमारी नियत रहती है। हम साहित्य की बात करें जिसे आप क्लासिकल में रख सकते हैं। लेखक समझता है कि क्लासिकल रचना से अपने पाठकों तक पहुंचा। और जो दूसरा साहित्य है जो समय की मांग है जो आपने कहा जो किसी घटना को लेकर रची हुई कविता हो तो वह जाहिर सी बात है वह इंतजार नहीं करती वह समय पर ही प्रकाशित होनी चाहिए। क्योंकि उसकी जो उपयोगिता है जो उसकी जो अहमियत है इस वक्त के लिए बनी है। ना कि बहुत देर तक उसे रखा जाए।
अरमान नदीम :- आपने एक बात और कही कि लेखक को बांटा नहीं जा सकता उसके मूल से कई बार ऐसा लगता है कि जो लेखक है वह अपने मूल से भटक रहा है। ऐसा कहें कि वह सिर्फ अपनी विचारधारा ही थोप रहे हैं ।
दर्शन दर्शी :- मैं मानता हूं एक अच्छे लेखक होने के लिए आपको पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। समाज को कैसे देखते हैं समाज आपको कैसे देखता है । समाज के लिए कितने उपयुक्त हैं, समाज आपको कितनी इज्जत देता है । एक बार को आप अपने लेखन को हटा दीजिए। आम आदमी एक आम सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति अपना आपको समझ कर देखिए कि आप समाज को कैसे देखते हैं और समाज आपको कैसे देखता है। एक चरित्र है एक इमेज है। लेखक के रूप में आप बिल्कुल ही एक अलग तरीके की इमेज बना रहे हैं क्या। फिर आप उसमें एक अलग तरह के विचारों को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए मैं यह कह सकता हूं कि उसका श्रोताओं पर पाठकों पर कोई खास असर नहीं होने वाला। जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना जेनुइन होना वह चीज जब खो देता है कोई व्यक्ति तो उसे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो वह अपने पाठकों को प्रभावित नहीं कर पाएगा वह भले ही लिखता रहे । लेखन जो है उसका ज्यादा वक्त तक मकबूल नहीं रह सकता।
अरमान नदीम :- क्षेत्रीयता की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ इसका इस्तेमाल करती है अपने वोट बैंक के लिए क्योंकि हम उदाहरण के लिए लेते हैं भाषा को व्यक्ति सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से लगाव रखता है तो वह अपने संस्कृति अपनी भाषा से रखता है लेकिन हम यह देखते हैं कि कहीं ऐसी आज भी भाषाएं हैं जिनकी मान्यता के लिए लंबे वक्त से आंदोलन चल रहे है लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जाता जैसे कि मैं राजस्थान से हूं ,मैं राजस्थानी की बात करूं तो एक लंबा दौर हम देख रहे हैं जब यहां मान्यता के लिए आंदोलन चल रहा है और आज भी चलते आ रहे हैं लेकिन सरकारें उन्हें वह सम्मान वह मान्यता क्यों नहीं देती है।
दर्शन दर्शी :- देखिए हम भी बहुत लंबे संघर्ष से गुजरे हैं। आपको मालूम ही होगा कि डोगरी 2003 में ही आठवीं शेड्यूल में शामिल किया गया । कश्मीरी को तो शुरू से ही मान्यता थी। और साहित्य अकादमी की अगर हम बात करें तो डोगरी को बहुत पहले से वह स्थान प्राप्त है। और बहुत सारी हमारी भाषाएं ऐसी है जो उसे स्थान को मांग रही। आपने अभी कहा राजस्थानी को भी मान्यता नहीं है। मेरा यह मानना है कि जो सियासी निजाम है जो सियासत करते हैं उन्हें भाषाओं के साथ कुछ खास लगाव नहीं है। उनका प्रेम कहीं और है जो साफ नजर आता है। अगर भाषा संस्कृति इन सभी के प्रति वाकई में सरकारों का आदर सम्मान होता तो मुझे नहीं लगता की भाषाओं की इस तरीके से दुर्गति होती । दुनिया में आप देखिए की कई भाषाएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पर भी पहुंची। भाषाओं की बात कर रहा हूं जिन भाषाओं पर सरकारें ज्यादा गहन चिंतन नहीं करती है। कुछ भाषाएं ऐसी भी है जिनके लिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करती भी हैं। किसी भी भाषा का नाम नहीं लूंगा। होता यह है कि एक बड़ी भाषा और छोटी भाषा इस तरह के शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। वही बात होती है कि एक बड़ी मछली जो है छोटी मछली को तालाब में निकालना शुरू कर देती है। और होता यह है कि जो बड़ी भाषाएं हैं वह विस्तार के लिए छोटी भाषाओं को इस तरीके से प्रभावित करना शुरू कर देती है। छोटा भाषाओं पर लोग यह मान लेते हैं नौकरी के लिए या फिर दीगर मसलों पर वही भाषा उपयोगी है। दूसरी भाषाओं को सिखना पढ़ना इतना काम नहीं देता।
अरमान नदीम :- एक कहावत काफी लंबे वक्त से हम सुनते आते हैं किताबें सब जानती है। जिस पर मैंने अपने एक आर्टिकल में विस्तार से बात भी की है मैंने लिखा था किताबें सच में सब कुछ जानती है लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो तारीख़ में हुए महान लेखकों को अपने हाथ रोकने पर मजबूर कर दिए । ऐसा नहीं था कि उन्हें वह जवाब मालूम ना थे । अगर वह जवाब दे देते तो यह समाज उन्हें महान का तमगा नहीं देता । तो सवाल यह है क्या एक बैरियर रहा है लेखन के बीच में बंधन जिसे हम कहते है ।
दर्शन दर्शी :- जी आपका यह सवाल बहुत ही खूबसूरत है । इस बारे में सोचता रहता हूं। कहीं ना कहीं यह वही बात आ गई जो मैंने शुरुआत में कही थी कि निजी जीवन में लेखक कैसा है निजी जीवन में उसके विचारधारा और लिखने में उसके विचार धारा। सबसे बड़ी बात क्या लेखक वाकई में सत्य को सामने रख रहा है । अपनी लेखनी के माध्यम से चाहता है या फिर किसी विशेष उद्देश्य के साथ लेखन कर रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही वह लेखक जिन्हें समाज ने महान कहा अगर वह सत्य के उस रूप को सामने ला देते तो उन्हें महान लेखक ना कहा जाता। मुझे लगता है अगर वह सच को सामने लाते तो सबसे पहले तो सत्य की जीत होती। लोगों को भूल भुलैया से निकाल कर सही रूप का दर्शन करवाते ही करवाते अपने लिए भी एक बहुत उपलब्धि मूलक कार्य करके जाते । कर्म करना है फल की चिंता नहीं। अगर कर्म करना है फल की चिंता के बगैर तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना होगा फल पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे साहित्यकार ऐसे इतिहासकार जिन्होंने फल को ध्यान रखकर कार्य किया है। उनके काम की कभी सरहाना नहीं की जा सकती।
अरमान नदीम :- अपने एक आर्टिकल "आईने के अरमान" में इस बात का जिक्र किया है। जिस तरीके से कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है अब इस आईने को क्या चाहिए जवाब आता है महान का तमगा अब ये कहां से मिले साहित्य अकादमी से। ये इतना आसान थोड़ी है क्यों नही है जिसके लिए हमने अपने शब्द घुमा दिए क्या उसका एक बार नंबर नहीं घुमा सकते ?
दर्शन दर्शी :- आपने वाकई बहुत खूबसूरत लिखा है। सही बात तो यही है मगर देखेंगे तो ऐसे लोग भी हुए हैं और हैं जो लेखन को लेखन की नजर से ही देखते हैं। मगर हमारे समाज में शुरू से पूरे भारतीय समाज में ,भारतीय संस्कृति और पूरे भारतीय भाषाओं पर भी लागू होगा। हम आमतौर पर प्रशंसा के बड़े भूखे रहे हैं। प्रशंसा का भूखा आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को केंद्र में रख के बात करने की कोशिश करता है। सिर्फ अपने आप को केंद्र में रखेगा । आपको लगता है वह वाकई में अपने लेखन के साथ न्याय करेगा।
अरमान नदीम - बहुत तेज खूबसूरत बात कही की कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो साहित्य को साहित्य की नजर से ही देखते हैं लेकिन मुझे लगता है हम इसे इंसानी फितरत ही कह सकते हैं कि सफेद बोर्ड पर काला धब्बा ही नजर आता है। मैं कहना चाहूंगा मेरी खुशकिस्मती रही कि श्री मधु आचार्य जी जैसे व्यक्तित्व से साक्षात्कार कर सका और वही मणिपुर से किरण जी वह ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हम यह बात कह सकते हैं जो वाकई में साहित्य को अपनी लेखनी को उसके साथ न्याय करते हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आज के हालात है वह कहीं ना कहीं समाज को खोखलेपन की तरफ धकेलने का काम कर रहें है।
दर्शन दर्शी :- आपने बिल्कुल सही कहा और मैं यह कह सकता हूं कि संस्थाओं को जिस तरीके से काम करना चाहिए वह उस तरीके से या उस निष्पक्षता के साथ में काम नहीं कर पा रही है। सरकारें भी उसे तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए । यहां तक कहना चाहूंगा कि जो संपादक हैं ,आलोचक वह भी उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जो सही तरीका होना चाहिए। लेखक थी उसे तरीके से लेखन नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए।
अरमान नदीम - जैसा की मैंने कहा कि जब शब्द संवाद में ही किरण कुमार जी से बात हो रही थी तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि कई लोग उनके पास में आए और ऑफर देने की बात तक उन्होंने कही। उन्हें कमरे से बाहर तक निकाल दिया था और जो ऑफर लेकर आए वह काफी नमी और बड़े लेखक माने जाते हैं। ऐसे भी अनुभव हुए।
दर्शन दर्शी :- काफी हद तक कुछ संस्थाएं ऐसी है जिनके अवार्ड जो दिए जाते मैं कह सकता हूं ऊपर वाले की मेहरबानी से ज्यादा सवाल नहीं उठाते हैं जिसमे साहित्य अकादेमी है लेकिन जैसा कि आपने बताया किरण कुमार जी का जो अनुभव रहा ऐसा होता है। हमारे कई साथियों का तजुर्बा हो सकता है लेखक अपने आप को बहुत ही नीचे स्तर तक रख के मांगने की प्रक्रिया से जाते हुए नहीं बच रहे। तो बचपन से यही पढ़ा है कि प्रशंसा मांगने की चीज नहीं है। अवार्ड और रिवॉर्ड मांगने की चीज नहीं है।
अरमान नदीम - शब्द संवाद हेतु आपने कीमती समय दिया ,बहुत आभार ।
दर्शन दर्शी - धन्यवाद ।
परिचय
श्री दर्शन दर्शी
श्री दर्शन दर्शी, जम्मू-कश्मीर सरकार के पूर्व सिविल सेवक डी.के.वैद का उपनाम है। वे एक प्रमुख डोगरी लेखक हैं, जो एक लोकप्रिय डोगरी कवि होने के अलावा अपनी मातृभाषा डोगरी में कथा, निबंध, साहित्यिक आलोचना भी लिखते हैं। वे डोगरी से अंग्रेजी में और इसके विपरीत अनुवाद भी करते हैं। उन्हें कई सरकारी और गैर-सरकारी साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करने के अलावा, उनके कविता संग्रह, "कोरे काकल, कोरियन तालिअन" के लिए 2006 में साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया था। वे साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड/जीसी में रहे हैं और वर्तमान में जेएंडके कला, संस्कृति और भाषा अकादमी की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और कुछ क्षेत्रीय साहित्यिक संगठनों के मुख्य संरक्षक हैं। वे एक लोकप्रिय प्रेरक वक्ता भी हैं। , आप अक्सर छात्रों को जीवन कोच के रूप में (अंग्रेजी और डोगरी में) व्याख्यान देते हैं। आप अंग्रेजी भाषा में कविता, कथा और व्यक्तिगत निबंध भी लिखते हैं।
Gaur Haridas
गौर हरिदास
साहित्य मेरी व्यक्तिगत विफलताओं की भरपाई, स्वप्न वास्तविकता के बीच रह गए एक शून्य स्थान की पूर्ति है ।- गौर हरिदास
साहित्य अकादेमी दिल्ली से दो बार सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त उड़िया भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार गौर हरिदास से "शब्द संवाद " के लिए खास बातचीत ।
गौर हरिदास जी ने उपन्यास , लघु कथाएं , कविताएं , लेख आलेख , हिंदी और अंग्रेजी में कई किताबों की रचना की और यह कहना ज़्यादा मुनासिब होगा की इन्होंने साहित्य को असल में जिया है । गौरहरि दास जी ने वार्ता के दौरान बताया की जब वह आश्रम में रहा करते थे तो उन्होंने दो बार आत्महत्या करने की कोशिश की। एक व्यक्ति जिसने एक वक्त में खुद को खत्म करने का प्रयास किया हो और वह साहित्य के शिखर तक पहुंचे यह वाकई सोचने वाली बात है। गौरहरि दास जी एक तरफा बात नहीं करते पब्लिक प्लेटफॉर्म में लोग लिखते बोलते वक्त कुछ हद तक हिप्पोक्रेट हो सकते हैं लेकिन जब इसी के चलते मैंने हिपोक्रेसी के ऊपर सवाल किया तो उन्होंने अपना जवाब दिया और कहा की कई मामलो में भारतीय कुछ ज़्यादा हिप्पोक्रेट हो जाते है । गौरहरि दास ना सिर्फ एक वरिष्ठ साहित्यकार बल्कि समाज सुधारक भी हैं। आप सभी लेखकों के लिए यह बात नहीं कह सकते । हो सकता है की उनके पास एक अवार्ड की लंबी लिस्ट हो लेकिन वाकई उनकी लेखनी समाज के लिए कुछ सुधार करें यह जरूरी नहीं है क्योंकि आज के लेखकों ने साहित्य को व्यापार बना दिया है और मैं इस विधा से जुड़ा हूं और मैं इससे खिलवाड़ करने वालों के प्रति मैं उदार नहीं हो सकता। लेकिन गौरहरि दास जी कुछ अलग नज़र आते है क्योंकि जिस कठिनाई से दास जी निकले और अपने लेखन को शुरू किया वही उनके साहित्य में देखने को मिलती है। हरिदास जी कहते है की मेरी सोच आम धारा से कुछ अलग है। मैं लिखित परिचय या पुरस्कारों की फेहरिस्त में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखता, हां एक बार के लिए कह सकते हैं जैसे अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग होता है रिकॉनाइजेशन के लिए लेकिन मेरी राय में एक कलाकार का वास्तविक परिचय उसकी कला की प्रस्तुति ही सकती है वही सही और सच्चा परिचय होता है ।
मैं अपनी बात में विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य आशावादी जी का क्योंकि जिस तरह का स्नेह “शब्द संवाद” को प्रदान किया है वाकई इससे उनकी साहित्य के प्रति सच्ची निष्ठा और लगाव नज़र आता है । जहां आज की तारीख में लोग बड़ी ही बेईमानी के साथ साहित्य का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं वहीं मधु जी जैसे व्यक्ति भी नजर आते हैं जो साहित्य को सर्वोच्च रखने की कोशिश में अपना सर्वोच्च देने का प्रयास करते है। सही मायने में अपनी लेखनी के साथ न्याय करते हैं। जिनकी कथनी और करनी में फर्क नजर नहीं आता। उनका काम उनकी कथनी से ज़्यादा ही है। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर भी मधु जी पहली फ़ेहरिस्त में नज़र आते है।
मैं “शब्द संवाद” के जरिए संवाद कर रहा हूँ तब मेरी उम्र 19 साल है और संवाद के दौरान गौरहरि दास जी ने मुझे बताया कि जब उन्होंने अपनी पहली रचना लिखी उस वक्त वह दसवीं क्लास में थे । इस हिसाब से अगर बताना चाहूं तो उनका साहित्यिक अनुभव मेरी उम्र से भी दोगुना है लेकिन संवाद के दौरान कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं उनकी किसी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं या फिर वह सम्प्रेषण में असहज महसूस कर रहे हैं शायद यही एक लेखक की पहचान है की उसका पाठक उसका श्रोता उसे पढ़े सुने और समझे । और एक बात मैं समझ गया की लालच रखने वाले लोग हो सकते हैं लेकिन उन्हें काबू करने वाले भी मौजूद है। अहम पदों पर रहने के बाद भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्यभार पूरा करने वाले गौरहरि दास जी भीड़ से अलग व्यक्तित्व है। मैं ये भी जानकारी के साथ बता दूँ की गौरहरि दास जी को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तरफ़ से साहित्य की सर्वोच्च संस्था साहित्य अकादेमी से दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है: एक रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में और दूसरा अनुवाद के क्षेत्र में। 1959 में ओडिशा के भद्रक जिले के मंटेई नदी के पास एक सुदूर भारतीय गाँव, संधागरा में जन्मे, उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। एक मठ में पले-बढ़े वास्तविक जीवन के अनुभवों ने एक लेखक के रूप में उनके कौशल को निखारा और उन्हें करुणा और हास्य से भरपूर संवेदनशीलता प्रदान की, जो उनके रचनात्मक अस्तित्व को उसका विशिष्ट चरित्र प्रदान करती है। अब तक इनकी 75 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें निबंध, उपन्यास, लघु-कथाएँ, बच्चों के लिए उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, कविता और लघुकथाएँ शामिल हैं। उनकी कई प्रमुख कृतियों का हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी रचनाओं पर विभिन्न भाषाओं में टेलीविजन धारावाहिक और मंच-नाटक बनाए गए हैं और विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सहित विभिन्न संगठनों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। वे एक शिक्षाविद हैं जिन्होंने दो मास्टर डिग्री प्राप्त की हैं, एक भाषा और साहित्य में और दूसरी पत्रकारिता और जनसंचार में। डॉ. दास के पास व्यापक अनुभव है क्योंकि वे साहित्य अकादमी और अन्य सांस्कृतिक संस्थानों की सामान्य परिषद और कार्यकारी बोर्ड से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वे ओडिशा के अग्रणी साहित्य समूह, सताब्दीरा कलाकार के अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी कनिका चक्रधर बेहरा स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा, वे विभिन्न क्षमताओं में 37 वर्षों से अधिक समय से ओडिशा के सबसे बड़े मीडिया हाउस संवाद समूह के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मास मीडिया के तीनों क्षेत्रों: प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन में काम किया है और समृद्ध अनुभव अर्जित किया है। एक कुशल आयोजक के रूप में, उन्होंने सैकड़ों प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव, प्रदर्शनियां, सेमिनार आयोजित किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने भारतीय लेखकों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में कई देशों का दौरा किया है और फ्रैंकफर्ट, जर्मनी और पेरिस, फ्रांस में आयोजित विश्व पुस्तक मेलों में भाग लिया है। और इन सब उपलब्धियों के बाद भी जब आप उनसे बात करते है तो वो वही सहज सरल व्यक्तित्व से आपसे मिलते है बात करते है जो उन्हें गौरहरि दास बनाता है । एक नाम गौरहरि दास नहीं एक रचनात्मक अभिव्यक्ति गौरहरि दास। और मैंने ये क्यो कहा की इनसे हुई वार्ता “शब्द संवाद” को चरितार्थ करती है क्योंकि मेरे शब्द संवाद का उपदेश केवल साक्षात्कार नहीं है बल्कि इससे मेरे पाठकों को कुछ नया सीखने को मिले ,कुछ नई जानकारी मिले और एक के बाद एक साक्षात्कार से मिलती प्रतिक्रिया से ये पता चलता है कि मैं अपने उद्देश्य की तरफ सफल कदम बढ़ा रहा हूँ।
प्रधानाचार्य: संबाद स्कूल ऑफ मीडिया एंड कल्चर , भुवनेश्वर 2006 से निदेशक, (समाचार), कनक टीवी संपादक (फीचर्स), संबाद (सबसे बड़ा ओडिया दैनिक) और संपादक: कथा, (फिक्शन मासिक) 1985 से
फेलोशिप: सरकार की वरिष्ठ फैलोशिप। भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय - 2011 साहित्य अकादमी, नई दिल्ली में रेजीडेंसी में लेखक - 2010 शैक्षणिक योग्यता: एम.ए., पीएच.डी., एम.जे.एम.सी. (उत्कल विश्वविद्यालय)
साहित्य अकादमी, नई दिल्ली की कार्यकारी समिति के सदस्य 2013-2017 साहित्य अकादमी, नई दिल्ली में ओडिया सलाहकार बोर्ड के सदस्य, 2008-2012 क्षेत्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य, 2012-2016 भुवनेश्वर के सतबदीर कलाकार के अध्यक्ष - 2014 से महाबोधि सोसाइटी, भारत के सदस्य इंटैक के सदस्य स्वतंत्रता सेनानी चक्रधर बेहरा स्मारक समिति के अध्यक्ष , यात्रा किए गए देश: यूएसए, स्वीडन, चीन, जर्मनी, यूके, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, वेटिकन सिटी, स्विटजरलैंड, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस। नियमित स्तंभकार: पिछले 35 वर्षों से जीवनारा जलछबी (जीवन के प्रतिबिंब), ओडिशा डायरी और राजधानी राजनीति (राजनीति के मामले) शीर्षक से नियमित स्तंभों के अलावा संवाद के संपादकीय भी लिखते रहे हैं।
प्रकाशित पुस्तकें
पुनराब्रुत्ती (द रिपीटिशन)-1996 घर (द होम)- 2000 कागजाडांगा (द पेपर बोट) -2002 अहिल्यारा बहघारा (अहिल्या की शादी) - 2004 (मथुरा का रेखाचित्र)- 2007
12. मथुरारा मनचित्र (द नेल एंड अदर स्टोरीज़) - 2009 13. कांता ओ अन्यन्या गल्पा 14. आकाश दिने नीला थिला
(वंस द स्काई वाज़ ब्लू) - 2010 15. अनलेउता ओ अन्यन्या गल्पा (वह व्यक्ति जो वापस नहीं लौट सकता और
अन्य कहानियाँ)- 2015 16. बाघा ओ अन्यन्या गल्पा
(द टाइगर एंड अदर स्टोरीज़) - 2019, उपन्यास, छाया सौधरा अबेशा - 1996, निजा संगे निजारा लधेई - 1999, इथु अरम्भा - 2005 , अपानंका अजनाधिना - 2010, केते रंगारा जीबाना - 2013 , सारांश - 2021, बिदंबिता अभिसार - 2022, लघु कथाएँ, जुआरा भट्टा (हाई टाइड लो टाइड) - 1981 अखाड़ा घर (रिहर्सल रूम) - 1989, (एक सपने के लिए रात कहाँ है) - 1991, भारतवर्ष-1994, माटी कंधेई (मिट्टी की गुड़िया) - 1995, माया - 1998, शेषा बाजी (द लास्ट बैट) - 1997, चयनित कहानियाँ, पिचिला पचीश -2007, श्रेष्ठ गल्पा - 2016, बिदेशा ओ अन्यन्या गल्पा - 2019, कहानियों का सर्वग्राही संग्रह, गौरहरि कथा समग्र- प्रथम खंड - 2021, गौरहरि कथा समग्र- द्वितीय खंड - 2021, गौरहरि कथा समग्र - तृतीय खंड - 2021, उपन्यासों का सर्वग्राही संग्रह, पंच पर्व - 2019, विगनेट्स का सर्वग्राही संग्रह, जिबनारा जलाछाबी, वॉल्यूम। 1 - 2014, जिबनारा जलाछाबी, वॉल्यूम। 2 - 2022, लघुचित्र :- जीवनरा जलछाबी - 1994 चिन्हा चौहदी - 1996 भिन्न भूमिका- 1998 परिचिता परिधि - 2001 असमार्थ ईश्वर - 2007 हतालेखा चिथी- 2012 ईश्वरंका ठिकाना - 2019 खेलें, अपराध - 2003, अमा घर नक्सा - 2021, कविता, पौनशारा पांडुलिपि - 2010, इरसामा ओ अन्यन्या कबिता - 2022
समकालीन उड़िया साहित्य में गौरहरि दास-
भारतीय आधुनिक कहानी का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। चाहे हिन्दी साहित्य के मुंशी प्रेमचंद हो अथवा उड़िया के फकीर मोहन सेनापति ये सभी उन्नीसवीं सदी के लेखक रहे हैं । उनके समय में कहानी के प्रमुख स्वर थे - समाज संस्कार,विधवा विवाह, अस्पृश्यता निवारण, शोषक - शोषित वर्ग के सम्बन्ध, सामंतवादी प्रथा इत्यादि । इसके बाद स्वाधीनता संग्राम के लिए आह्वान चला। फिर 1947 में भारत की स्वाधीनता के बाद कहानी का कैनवास ही बदल गया। 1948 से जो अध्याय शुरू हुआ था, वह स्वाधीन भारत की आशा और मोहभंग की कहानी थी। इस समय की कहानियों में राजनैतिक स्वार्थ, खंडित मूल्यबोध । कभी यूनियन कार्बाइड भोपाल विस्फोट की जैसी दुर्घटना के बाद भारत श्मशान जैसा बन गया था। नदी बांध योजना के लिए विस्थापन इतना भी सहज साध्य नहीं हुआ। शोषित जनजातियों के स्वार्थ की रक्षा हेतु असंख्य जन आंदोलन का सूत्रपात हुआ। साहित्य में दलित विमर्श पर बल मिलने लगा । पूँजीवाद और उपभोक्तावाद का जयगान होने लगा। उदारवादी अर्थनीति में एक साधारण नागरिक या तो एक वोटर बना या फिर एक उपभोक्ता। भारत में यह घटना संगठित होने तक यूरोप में नीत्शे ने घोषणा कर ली थी-‘ईश्वर मृत हैं' । इलियट के 'वेस्टलैंड' (बंजर भूमि) ने जीवन की अर्थहीनता को बहुत ही स्पष्ट रूप में उपस्थापित कर दिया था। तब भारतीय ग्राम्य जीवन शहरांचल की ओर उन्मुख हो चला था । संयुक्त परिवार टूट रहा था। भारतीय समाज से पाप-पुण्य, आदर्श अनादर्श आदि के व्यवधान बढ़ने लगे थे। नारी अपनी पहचान खोजने लगी थी। दलित, शोषित जनता ढूँढ रहे थे अपनी राजनैतिक अस्मिता और अधिकार।
इसी पृष्ठभूमि पर उड़िया कथा साहित्य केंद्रित था। गोपीनाथ मोहंती, मनोज दास, सुरेंद्र मोहंती, अखिल मोहन पट्टनायक, शांतनु कुमार आचार्य, चंद्रशेखर रथ, वीणापाणि मोहंती, प्रतिभा राय, देवराज लेंका, विभूति पट्टनायक के जैसे मूर्धन्य
साहित्यकारों के बाद रवि पट्टनायक, जगदीश मोहंती, ऋषिकेश पंडा, तरुणकांति मिश्र,यशोधारा मिश्र के जैसे अनेक कथाकार कहानी रचना के क्षेत्र में आ चूके थे। उड़िया कहानी की धारा कभी पाश्चात्य परीक्षा- निरीक्ष की और तो कभी पारंपरिक कथा-धर्म की ओर आगे बढ़ रही थी। इसी समय उड़िया कहानी के क्षेत्र में एक तरुण गोष्ठी का आगमन होता है, जिन्होंने उभय पाश्चात्य और पारंपरिक कथा - धर्म के बीच समन्वय की स्थापना की, जिनकी पाठकों ने सराहना की। इसी युवा पीढ़ी के कथाकारों के पास थे नए प्रसंग और नई कथन शैली ,स्ष्टता और सादगी ही उनकी एक अलग पहचान है, जो उन्हें पूरे भीड़ में से स्वतंत्र दर्शाता है। गुणात्मक दृष्टि से उनकी कथाओं का कैनवास जिस तरह विस्तृत और वैविध्यपूर्ण रहे हैं, परिमाणात्मक दृष्टि से उनकी कृतियां उसी प्रकार असंख्य और उल्लेखनीय हैं। उनके समसामयिक साहित्यकारों के बीच वे एक ऐसी हस्ती हैं, जो साहित्य के प्राय सभी विधाओं में अपनी प्रतिष्ठा ज़ाहिर की है और उल्लेखनीय स्वीकृति भी प्राप्त की है। कहानी के लिए वे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने के साथ साथ उपन्यास के लिए भी उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की तरुण नाट्यकार प्रोत्साहन प्राप्त है। कविता, निबंध, पर्यटन कहानी, स्मृतिचित्र, व्यंग्य और अनुवाद आदि विधाओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान सराहनीय हैं। गौरहरि दास जी की पहली कहानी, ज्वार भाटा 80 के दशक की प्रथमार्द्ध में प्रकाशित होती है। तब वे रेवेंसा कॉलेज के छात्र थे।
और भीरु पदपात धीरे दृढ़ और दृप्त हो उठा। बाद में एक के बाद एक कहानी संकलन प्रकाशित होने लगी, जैसे कि - 'आखड़ा घर', 'भारत वर्ष', 'घर' तथा 'कांटा और अन्यान्यगल्प’, सफल संकलन आदि। उसी समय से समानांतर रूप से वे लिखते रहे उनका नियमित स्तम्भ ‘जीवन की जल छवि', जो अद्भुत रूप से लोकप्रिय हो उठा है। यह स्तम्भ समसामयिक समकालीन ओडिशा का विश्वस्त शब्दचित्र माना जाता है। गौरहरि जी के जैसे अन्य किसी के स्मृतिचित्र अथवा कहानी में उड़ीसा के ग्रामीण जीवन को इतने सादगी और स्पष्टतापूर्वक खोज पाना सहज नहीं हो पाता है। गांव के चित्र और चरित्रों को चित्रण करने में उनका योगदान स्वतंत्र रहा है। “साहित्य मेरे लिए मनोरंजन का प्रसंग नहीं है, व्यवस्था पर ये मेरा हस्तक्षेप है” - कमलेश्वर जी की इसी मत से सहमत होते हुए कथाकार गौरहरि दास जी कहते हैं,
“साहित्य मेरी व्यक्तिगत विफलताओं की भरपाई, स्वप्न , वास्तविकता के बीच रह गए एक शून्य स्थान की पूर्ति है”।एक मुग्ध पाठक के दृष्टि से गौरहरि जी के सृजन कर्म में जीवन जिज्ञासा का उत्ताल तरंग, जीवन यात्रा का ज्वलन, स्वानुभूति की विभूति, अनासक्ति की उदासीनता और संभावना का आशान्वित आह्वान को पाठक महसूस करता है। धरातल की वास्तविकता तथा कल्पना के अपूर्व महोत्सव को साहित्य के पन्नो पर उदभाषित करने वाले वे एक उदारपंथी कथाकार हैं। पिछले चार दशकों से जीवन के इसी नित्य प्रवाहमान धारा के साथ अन्तरंग उनकी साहित्यिक आत्मा मानो जैसे एक अमृतकलश बन गई है। अनकही व्यथा और आघातों को उपहार के रूप में ग्रहण कर जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लक्ष्य से उन्होंने असंख्य कथा साहित्य को भेंट दी है।
अरमान नदीम :- भारतीय साहित्य में आप एक जाना माना नाम है । जानना चाहूंगा कि साहित्य को लेकर आपकी रुचि किस तरीके से बनी हालाँकि आपके परिचय में आपने कुछ इसके बारे में बताया है और मैं आपका परिचय जब पढ़ा तो वाकई में एक प्रेरणा का स्रोत है वो इसे हम सिर्फ़ आपका जीवन परिचय नहीं कह सकते। वो प्रेरणा का स्रोत है
गौरहरि दास :- जी जब मैं छोटा था तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे गांव में उस दौरान बिजली नहीं हुआ करती थी बिजली नहीं आई थी लेकिन मेरे पिताजी के पास एक अलमारी थी जिसमे में किताबें भरी रहती थी तो वो मैं पढ़ा करता था । कटक शहर जो की ओल्ड कैपिटल थी उड़ीसा की वहाँ गाँव के एक सज्जन काम किया करते थे । उड़ीसा का सबसे पुराना अखबार है "समाज" और उस अखबार के दफ्तर में वो काम किया करते थे और उनके पिताजी हमारे गांव के थे और मेरा काम यह था कि स्कूल की छुट्टी के वक्त एक कॉपी अखबार की उन तक पहुँचाना । कई बार ऐसा हुआ करता कि रास्ते में चलते-चलते मैं अखबार खोलकर पढ़ लिया करता था और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह भी चीज रहती थी कि अखबार के अंदर मॉस्को ,अमेरिका ,लंदन और बाकी बड़ी-बड़ी जगह के बारे में बात होती है थी लेकिन इसमें मेरे शहर की मेरे गांव की बात नहीं होती थी और मैं यही सोचता था कि इन्हें हमारे गांव के बारे में भी तो लिखना चाहिए ना उस वक्त में यह सोचा करता है कि इतनी जरूरी चीज होती है मेरे गांव में कैसे हम मछली पकड़ कर लाया करते हैं नदी से और इसी के चलते मैंने एक चीज यह की दो पन्ने मैंने फाड़े और उसमें अपने गांव के बारे में लिखना शुरू किया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस वक्त मेरे दो ग्राहक हुआ करते थे मेरी माता जी और मेरे पिताजी वह मेरे अखबार के सब्सक्राइबर थे। और आगे जैसे-जैसे उम्र बड़ी और जब मैं 8 वर्ष का हुआ तो मुझे एक मठ में छोड़ दिया गया था की मेरे माता-पिता की कोई संतान नहीं थी और उस वक्त उन्होंने ये मन्नत की पहली संतान होगी तो उसे मठ में समर्पित कर दिया जाएगा। जब मैं पैदा तो मुझे 8 वर्ष की उम्र में आश्रम में भेज दिया गया। क्योंकि अब मेरी उम्र इतनी कम थी और जब माता-पिता ने मुझे मठ में छोड़ा तो मैं काफी अकेला महसूस करता था और मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि अपने घर परिवार से इतनी दूर अकेला रहूं । बचपन से ही मेरा शौक अखबार, किताबें पढ़ने का था और एक्सरसाइज मुझसे नहीं हुआ करती थी। ऐसे ही चलते-चलते मैं दसवीं कक्षा तक पहुंचा और हमारे यहां एक पत्रिका निकलती थी कल्याणी तो मैंने अपनी रचना भेज दी कहानी छाप भी गई और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस वक्त मेरे स्कूल के किसी स्टूडेंट तो छोड़िए मेरे स्कूल में से किसी टीचर की भी कहानी या रचना अखबार में नहीं छपी थी। उस दौरान जब मैं आश्रम में रहा करता था तो मैं अपने सभी चीजों को बहुत याद करता और मेरे पास एक ही जरिया था कि मैं अपना लिखना जारी रखूं ताकि मैं उन सब चीजों को एक बैलेंस कर सकूं उन दिनों में सिर्फ किताबें और लेखन ही मेरी साथी बनी था मेरे साहित्य में रुचि का और साहित्य लेखन की शुरुआत इस तरह हुई।
अरमान नदीम :- जब आप आश्रम में थे तो आपको अकेलापन महसूस हुआ करता था तो अकेलेपन से डिप्रेशन जैसा कुछ महसूस हुआ ?
गौरहरि दास :- बिल्कुल कह सकता हूं और मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि मैं दो बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की। उस दौरान मैंने अपने आप से सवाल किया कि मेरे माता-पिता ने मुझे यहां क्यों छोड़ दिया मेरी क्या गलती थी दोस्त तो अपने गांव में है मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यहां छोड़ दिया गया हो बात है कि थोड़ा बहुत शरारती था मैं लेकिन उसकी सजा यह तो नहीं हो सकती कि मुझे आश्रम में अकेला छोड़ दिया जाए मेरा दोस्त बना तो वह मुझे कहता है कि जब तक तुम यहां बगावत नहीं करोगे यह लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले जैसे की बगैर स्नान किए तुम मूर्ति को जाकर छू या फिर आंगन में ड्राई फिश जो है उसे बिखर दो कुछ ऐसा करो कि यह लोग तुम्हें खुद ही यहां से निकाल दे । मैंने यह चीज करने की कोशिश भी की और इसमें मैं कुछ हद तक सफल भी रहा यह खबर पिताजी तक भी पहुंची और जब आए तो पंडित जी जो आश्रम के थे वह डांटे थे और कहते थे यह हरकतें करता है ,शरारत करता है तो जितना गुस्सा होते थे मैं मन ही मन में खुश होता था कि हां अब काम मेरा बन सकता है पिताजी ने पंडित जी से बात की और वह वापस से सब कुछ समझ कर खुद काम चले गए और मुझे वहीं छोड़ गए एक बार फिर से तो यह चीज भी मुझे डिप्रेशन की तरफ और ज्यादा धकेलती रही तो उसके बाद में मैंने एक चीज सोच ली कि अगर मैं घर नहीं जा सकता और यहां भी भी नहीं रह सकता तो मैं अपना आपको खत्म कर लूंगा लेकिन वह भी नहीं हो सका और मैंने अपना विचार फिर बदल दिया । क्योंकि मैं आपको एक यह भी बात बताना चाहूंगा कि मैं काफी गरीब परिवेश से था और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी काम में बचा है जो मैंने ना किया हो। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया अखबार देना और दफ्तर में चाय देना तो इस तरह की की चीज में शुरुआती दिनों में किया करता था लेकिन बाद में मैंने पढ़ाई अपनी नहीं छोड़ी चीजों के बाद भी मैं इस तरह के काम किया करता था लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया पी एच डी की तो लगातार सभी चीज में देखी लेकिन पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ा।
अरमान नदीम :- जी बिल्कुल आपकी बात से मैं काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और हमें अपने परेशानियों के साथ समझौता न करके उन्हें समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए हो रही बात अवसाद के सवाल की तो मैं यह सवाल अक्सर किया करता हूं क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज का युवा अवसाद को एक इतना हल्के में लेता है और हर चीज में इसे या डिप्रेशन से जोड़ लेता है छोटी से छोटी समस्या में भी और मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि अगर वाकई में किसी कोई समस्या से वह ग्रसित है तो वह किस तरीके से दूर हो सकता है।
गौरहरि दास :- जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे पहले समझने की जरूरत है और उस व्यक्ति की काउंसलिंग करने की जरूरत है और यह जानने की जरूरत है क्या वाकई में वह अवसर से ग्रसित है या नहीं सबसे बड़ी बात है कि उसे व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वह फिर वही कोशिश करता है आत्महत्या करने की या खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश है । वह उस दौरान करता है ,वह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टाइम होता है व्यक्ति के लिए जैसा कि मैं आपको बताया मैंने कोशिश की खुद ने आत्महत्या करने की लेकिन वह अगर नहीं हो सकता तो मैं अपने मन को समझाया की भगवान की यही इच्छा है कि मैं ऐसा ना करूं । मेरे दोस्त ने मुझे यह चीज समझाई की अभी तुम स्कूल में हो स्कूल पास कर जाओगे तो तुम कॉलेज चले जाओगे और तो यह सब चीज तुम यही छोड़ जाओगे तो मैंने सोचा यह कुछ वक्त तक के लिए है और उसके बाद में मुझे एक अच्छी जगह मिल जाएगी। यही सोचा कि मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए । बाकी इन सब चीजों को एक नजर अंदाज कर देना चाहिए और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बनी अपने डिप्रेशन से उभरने के लिए यही सोचता हूं कि उसे व्यक्ति उसे बच्चों को उसके माता-पिता और उसके दोस्तों का अगर साथ मिलता है उसे दौरान तो वह काफी सहयोग होता है उसे व्यक्ति के लिए लेकिन इसे की भी है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ इस कंपेयर ना करें कि अगर उसके साथ ही हुआ है तुझे वही चीज करने पर उसे व्यक्ति के साथ भी होगा क्योंकि सबके अलग-अलग मानसिकता होती है अलग-अलग हालात होते हैं तो अलग-अलग स्थिति के अनुसार अलग-अलग फैसला लेना जरूरी है।
अरमान नदीम :- समाज के दोगलेपन को आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरह कैसे मंचों पर या ग्रुप डिस्कशन में हम बातचीत करते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी उन्हें सम्मान मिलना चाहिए रंगभेद के ऊपर हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं की बिल्कुल गलत है जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए लेकिन जब सोशल मीडिया का में उदाहरण देते हुए आपको कहूँगा की जिस तरीके से डार्क मिंस आते हैं और चाहे अलग-अलग कम्युनिटी को टारगेट करते हैं तो यह जब चीज होती है तो इसे आप कैसे देखते हैं।
गौरहरि दास :- इंसान हमेशा से ही इसी प्रवृत्ति में रहा है । इंसान की तीन भूमिका होती है तीन तरह की चीज आती है पर्सनल सोशल और प्रोफेशनल हर एक व्यक्ति की अलग-अलग पर्सनालिटी हो सकती है अगर हम इसे समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दूं इसरो का अगर वह रॉकेट लॉन्च करेंगे तो इन चीजों में अंधविश्वास कहे या कुछ कहिए उसमें विश्वास नहीं करता है लेकिन वह जब रॉकेट लॉन्च करेंगे तो वह अपने हिसाब से उसकी पूजा अर्चना करेंगे और पूजा करेंगे तो जबकि वह सिस्टम पूरा कंप्यूटराइज है लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस के लिए यह सब किया जाता है। लेकिन हम इसे देखें तो समझ में बदलाव भी आया है इंटर कास्ट मैरिज इतनी नहीं हुआ करती थी यहां तक कि अगर हम बात करें तो दूसरे राज्यों में भी शादियां नहीं हुआ करती थी । लेकिन अगर हम देखते हैं तो जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वह अपनी इच्छा अनुसार शादी भी करते हैं या दूसरे राज्यों में इंटर कास्ट में जिस भी होती है तो कई चीजों में अगर हम देखें तो बदलाव भी आ रहा है और मैं यह कहूंगा कि आप सही हैं हिपोक्रिसी है मानवता के अंदर और दोगलापन है यह हमें देखने को मिलता है और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि दूसरे देशों के मुताबिक मुकाबले में भारतीय ज्यादा हिप्पोक्रेट हैं।
अरमान नदीम :- एक चीज में थोड़ी हटकर आपसे पूछना चाहूंगा की कई बार लेखक जो है खुद को साहित्य से ऊपर बताने की कोशिश करने लगते हैं या उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि साहित्य ने उन्हें चुनाव हो तो जब इस तरह के एरोगेंट स्टेटमेंट आप देखते हैं तो आप इसे एक क्रिटिक के रूप में देखेंगे या इसका समर्थन करेंगे या फिर इसे सिर्फ छोड़ देंगे?
गौरहरि दास :- जिसके पास भी पांव है वह चल सकता है लेकिन जिसके पास हाथ है वह लिख सके यह जरूरी तो नहीं, वही बात है कि अगर मैं आपको हजार अवार्ड की ऑफर दूं कई चीजों का आपको लालच दूं लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते तो आप उससे नहीं कर पाएंगे पैशन की बात है। अगर मुझ में यह पैशन है लिखने का तो मैं कहीं परेशानियां हो या कैसे भी हाल हो मैं लिखूंगा क्योंकि यह आंतरिक मामला है कि आपने कहा लोग कहते हैं कि साहित्य ने हमें चुना है तो ऐसा नहीं हो सकता । ऐसा नहीं कहना चाहिए के पास से अलग-अलग तरह के अपनी रुचि होती है कोई फोटोग्राफी करता है कोई गाता है कोई पेंटिंग बनाता है तो कोई लिखता है अहंकार सही नहीं है और इस तरह के कि अगर कोई बयान है तो मैं समर्थन नहीं करूंगा और यह चीज तो लगातार सीखने की है अगर आप इसमें तालीम हासिल नहीं करेंगे अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे नहीं तो आप इसके ऊपर काम भी नहीं कर सकते मेहनत और बुद्धिमत्ता दोनों ही आपको एक साथ लेकर चलानी होगी दृष्टिकोण सभी के पास में होता है ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई व्यक्ति नहीं लिखता है तो उसका अपना विचार नहीं है लेकिन जो चुनता है वही लिखता है ऐसा नहीं कह सकते कि साहित्य ने आपको चुना है अपने साहित्य को चुना।
अरमान नदीम :- क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि सोचने की क्षमता सीमित हो रही है या फिर जो चीज मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वह कहीं ना कहीं रुक रही है ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ ?
गौरहरि दास :- नहीं मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। हमेशा अपना संपूर्ण देने का प्रयास किया मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी सोच और अपने भाव को शब्द दूं और अपनी तरफ से उसे संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करूँ।
अरमान नदीम - शब्द संवाद के लिए कीमती समय देने के लिए आपका बहुत। आभार ।
गौर हरिदास - धन्यवाद ।
Dr.Ravindra Mangal
डॉ. रविन्द्र मंगल
मैंने बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से काफी कुछ सीखा है । - डॉ. रविन्द्र मंगल
महाराजा गंगा सिंह विश्विद्यालय में स्कूल ऑफ लॉ के निदेशक , बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ. रविन्द्र मंगल से खास बातचीत ।
परिचय
डॉ. रविन्द्र मंगल अपनी धर्म पत्नी की स्मृति में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन "संतोष मंगल सेवा संस्था" चला रहे है। पीटीईटी में सह-समन्वयक के रूप में काम किया। पूर्व अध्यक्ष (कुलपति) आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बीकानेर,
सेवानिवृत्त प्राचार्य, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज, नोखा, पूर्व निदेशक, अनुसंधान, एमजीएस यूनिवर्सिटी, बीकानेर, पूर्व विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, वर्तमान में निदेशक, स्कूल ऑफ लॉ, एमजीएस यूनिवर्सिटी, बीकानेर का कार्यभार संभाल रहे हैं । राजस्थान सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में प्रथम शिक्षक सम्मान, 2018 के प्राप्तकर्ता,5-7 अगस्त 2017 को जयपुर में भारत में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय “शैक्षणिक महोत्सव” में कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधित्व किया।
एडुहैक 4 और एडुहैक 5 में कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधित्व किया । , बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में “बीकानेर इंटर-डिसिप्लिनरी रिसर्च कंसोर्टियम (BIRC)” और “कलाम लर्निंग सेंटर” के संस्थापक सदस्य। वर्तमान में इको-फ्रेंडली कंपोजिट विकसित करने के लिए अंतःविषय अनुसंधान और भौतिकी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और समाज में विशेष रूप से समाज के वंचित वर्ग के बीच “करके सीखना” के माध्यम से वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहे हैं। * शैक्षणिक कैरियर एम.एस.सी. (भौतिकी) - 1984 I एम. फिल. (भौतिकी)- 1996 I . यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान। पी एच. डी.- 2002 । 1984 और 1985 में दो बार 90 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ गेट पास किया और आईआईटी, दिल्ली में एम.टेक (1984 में एप्लाइड ऑप्टिक्स) में प्रवेश लिया, बीच में ही छोड़ दिया।
* अनुसंधान रुचि: संघनित पदार्थ भौतिकी
* प्रकाशन: i. पुस्तकें – 09
ii. अनुसंधान प्रकाशन – 16
* सेमिनार में भाग लिया: i. अंतर्राष्ट्रीय – 04
ii. राष्ट्रीय – 07
* पुरस्कार/सम्मान: i. स्नातकोत्तर स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति धारक।
ii. एम.फिल. में विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक विजेता।
iii. एम.एससी. में विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान।
iv. बी.एससी. में कॉलेज में स्वर्ण पदक विजेता।
v. अध्यक्ष बीओएस, एमजीएसयू, बीकानेर जनवरी, 2004 से जुलाई 2022
vi. सदस्य अकादमिक परिषद एमजीएसयू, जनवरी, 2004 से जुलाई 2022
vii. अतिथि सम्मानीय, अध्यक्ष एवं सदस्य आयोजन समिति दिसंबर-2005, दिसंबर 2012, फरवरी 2013, अक्टूबर 2015 और नवंबर 2017 में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सेमिनार।
viii. प्रतिनियुक्ति पर निदेशक अनुसंधान जुलाई 2021 से जुलाई 2022
अरमान नदीम :- जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई या फिर मैं यूं कहूं जब पहली बार आपको सुना तो आपने अपने बारे में बताते हुए कहा था कि आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो यह भी अपने आप में एक रोचक बात हो जाती है की साइंस बैकग्राउंड से आप विधि विभाग के डायरेक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। ये सफ़र कैसा रहा?
डॉ. रविन्द्र मंगल :- जी बिल्कुल मेरा बैकग्राउंड साइंस से है लेकिन मुझे शुरू से ही पढ़ना अच्छा लगता था अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी हो ये एक ललक रहती। और लंबे वक्त तक मैंने बच्चो को पढ़ाया है और पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से काफी कुछ सीखा और सबसे ज्यादा मुझे जानने की यह रहती थी कि बच्चों की आखिर समस्याएं क्या होती है । जब मेरी कॉलेज में पोस्टिंग हुई तो यहां पर बच्चों का शुरू से ही पढ़ने में बहुत ज्यादा रुझान था और मेरी पोस्टिंग डूंगर कॉलेज में 1989 में हुई और 2020 तक मैं आपको कह सकता हूं कि मेरी जो क्लास थी उसकी स्ट्रैंथ बहुत ही ज्यादा अच्छी रहा करती थी। मैंने यह जाना कि बच्चों के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है विशेष रूप से फिजिक्स में मेरा ज़ोर इसी में रहता था कि मैं सेलेबस के साथ-साथ उनके जो फंडामेंटल कांसेप्ट है उन्हें भी क्लियर करूं ना की सिर्फ़ सेलेबस पूरा करा कर फ्री होने का लक्ष्य रखू। बच्चों को 11th और 12th में ही आ जानी चाहिए थी वह कॉलेज में उन्हें पढ़ना पड़ता था इसी कारण से जब इस तरह से मैं उनसे कनेक्ट करता उनसे समझाता तो बच्चों से मेरा एक अलग लगाव रहता और बच्चे भी मुझे काफी पसंद करते थे और मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा था कि सभी फ्रैंक होकर मुझ से हर तरह के सवाल कर लिया करते थे। इस तरह शिक्षण का 40 वर्ष का अनुभव रहा । 1984 से 2022 तक मैंने पढ़ाया ही पढ़ाया और इसी बीच मुझे राजस्थान बोर्ड में भी लिखने का मौका मिला वहां पर भी मैंने नवाचार करने की कोशिश की । मैंने आपको बताया जो फंडामेंटल कांसेप्ट क्लियर नहीं थे उन पर मैंने ज़ोर दिया जैसे हम सिर्फ थ्योरिकल सोचते थे और प्रैक्टिकल ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ करती थी इसलिए मैंने काफी चीज उसमें लिखी और अपनी तरफ से उसे बेहतर बनाने का प्रयास किया कॉलेज के सेलेबस में मैं आठ किताबों का सह संपादक रह चुका हूं । बीएससी फर्स्ट से थर्ड ईयर तक की इसी दौरान मैंने 9 विद्यार्थियों को पी एच डी करवाई खास कर फाइबर रेनफ़ोर्स इसमें ये की हम राजस्थान के फ्लोरा को कैसे इस्तेमाल कर सकते है जिसमे हमारा ज़ोर रहता है की प्लास्टिक की समस्या का हल निकले । और फिजिक्स की बात करे तो मैंने छोटी से छोटी क्लास से लेकर एम फिल तक करवाई है। लॉ डिपार्टमेंट से कैसे जुड़ना हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट बल्कि दूसरी चीजों से भी मैं लगातार जुड़ा हुआ था। और आपका पता ही होगा डूंगर कॉलेज राजस्थान का एक मात्र ऐसा कॉलेज बना जिसे लगातर ए ग्रेड मिला सबसे पहले 2006, 2012, 2021 तो ऐसा संभव इसी वजह से हुआ क्योंकि हम लगातार नवाचार किया करते थे। इसी बीच डूंगर मैं हमने कलाम लर्निंग सेंटर भी खोला। और लॉ डिपार्टमेंट से कैसे जुड़ना हुआ तो पहले मैं विश्वविद्यालय में डेपुटेशन पर आया जैसा कि मैंने आपको कहा मेरा लीगल पॉइंट में अनुभव बहुत था तो यहां के कुलपति महोदय ने मेरी चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठित की वहां से धीरे-धीरे मुझे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के विधि विभाग का विभाग अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
अरमान नदीम :- आपने कहा राजस्थान में डूंगर कॉलेज एकमात्र ऐसा कॉलेज बना जिसे तीन बार ग्रेड ए मिला लेकिन हमने यह दृश्य भी देखा कि नेक की रैंकिंग के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय को डिफाल्टर घोषित किया गया इसे आप कैसे देखेंगे?
डॉ. रविन्द्र मंगल :- डिफाल्टर को आप अगर समझेंगे तो इसे डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया था । विश्विद्यालय को नेक रैंकिंग में ग्रेड कम मिले थे।
अरमान नदीम :- रैंकिंग में ग्रेड कम होने के क्या कारण थे?
डॉ. रविन्द्र मंगल :- नेक असल में जिस तरीके से देखता है उनका सबसे बड़ा आयाम होता है फैकल्टी को लेकर वह सेंसिटिव बहुत होते हैं यह सबसे बड़ा कारण था कि टाइम पे फैकल्टी का ना भरा जाना रैंकिंग को गिरा गया और रिसर्च को लेकर भी यहां इतना कुछ खास काम नहीं हुआ करता था लेकिन जब नेक की रैंकिंग में हमें गिरावट मिली तो उसके बाद में यहां रिसर्च पर भी काम हुआ और मैं कहना चाहूंगा डिफाल्टर अपन इसे नहीं कहे ग्रेड कम मिला यह सच है।
अरमान नदीम :- मौजूदा वक्त में आप विधि विभाग के विभागाध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट को लेकर आपका क्या विजन है कि आने वाले वक्त में आप इसे किस मुकाम पर देखना चाहते हैं?
डॉ. रविन्द्र मंगल :- डिपार्टमेंट को लेकर मेरा विजन अगर मैं बताऊं तो सबसे जो मेरी प्रायोरिटी है वह यहां की जो छोटी-मोटी जो परेशानियां हैं उन्हें सुलझाना है जो कमियां चल रही है, बिल्डिंग में भी और जब भी मैं ऑफिस में जाता हूं तो इन चीजों को पहले उठता हूं और फैकल्टी से स्टाफ से बात करता हूं तो कोशिश रहती है कि पहले इनका समाधान किया जाए । बच्चों की जो क्लासेस हैं वह बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल रही है यहां की फैकल्टी अच्छा काम दे रही है हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि यहां जो फैकल्टी हो वह परमानेंट आए इसी के लिए हमारे कुलपति महोदय वह काम कर रहे हैं। परमानेंट फैकल्टी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा , बहुत जल्द आपके यहां परमानेंट फैकल्टी नज़र आएगी।
अरमान नदीम :- मैं खुद महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं, लिहाज़ा मैं जानता हूँ और कहना चाहता हूँ की फैकल्टी से कभी कोई शिकायत नहीं रही जिनमें डॉ सीमा जैन जी ,राहुल यादव जी ,वर्षा पवार जी, मोनिका पवार जी, अनीता कुमावत जी, डॉ. दुर्गा चौधरी जी, उपासना शर्मा जी , डॉ. प्रदीप कछवाहा जी , बीरेन्द्र सिंह जी, सुमन चौधरी जी ,डॉ. अल्पना शर्मा जी , डॉ. ललित पुरोहित जी , विशाल सोलंकी जी , गणेश प्रसाद जी, डॉ. अमित व्यास जी सभी का मैं आदर ,सम्मान करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ जब भी कोई समस्या आई है तो उन सभी ने ना सिर्फ़ डिपार्टमेंट फैकल्टी के तोर पर बल्कि व्यक्तिगत तौर से भी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की है। विशेषकर सीमा मेम की बात की जाए तो जिस तरह वो डिपार्टमेंट के प्रोग्राम या कोई भी जिम्मेदारी हो उसे निभाती है कबीले तारीफ़ है। लेकिन साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा विश्वविद्यालय के प्रशासन स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर कुछ कमी महसूस होती है। आप कैसे देखते हैं?
डॉ. रविन्द्र मंगल :- प्रशासन बहुत पॉजिटिव है जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने सितंबर में यहाँ ज्वाइन किया था और इस दौरान मुझे लंबे विदेश दौरे पर जाना पड़ा था। नवंबर में यहां आया तो फैकल्टी के साथ मीटिंग की और बीसीआई रेगुलेशन को जब हमने ध्यान से देखा उस पर चिंतन हुआ तो उन पर हमने चर्चा की ,विश्वविद्यालय स्तर पे लगातार संपर्क में रहते हैं और मीटिंग चलती है रजिस्ट्रार साहब को कई चीजों को लेकर बड़े प्रोजेक्ट पर बात हुई। और उन्हें चिन्हित किया कि क्या-क्या हमारे डिपार्टमेंट में समस्याएं हैं और किस तरीके से उसका निवारण होना चाहिए आपको। मैं आपको बता सकता हूं कि प्रशासन पूरा एक्टिव है और जब हम बात कर रहे हैं तो मैं पूरे डिपार्टमेंट का ना कह कर मैं पूरे विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं मेरी एक ख्वाहिश है कि जैसे कि हमारे विधि विभाग में एलएलबी का भी कोर्स चल रहा है ,आईआईएम भी है बी ए एलएलबी है जिसमें आप खुद छात्र हैं मैं यह चाहता हूं कि आने वाले वक्त में मैंने आपको जैसा बताया कि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं तो मैं यह चाहता हूं कि बच्चों को विज्ञान के बारे में भी कुछ जागरूक किया जाए उनको उसके बारे में कुछ नॉलेज दी जाए क्योंकि आपका क्षेत्र ऐसा है कि आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा सभी चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा तो एक जो नॉलेज गेम करने वाली जो चीज है वह हम इसमें देखते हैं क्योंकि एक लॉयर को सभी क्षेत्रों को में अपना काम देना पड़ता है काम करना पड़ता है पहले अगर आप वकील बनते हैं तो आपको उसे तरीके से काम करना पड़ेगा और जब आप जज बन जाएंगे तो आप देखिए आपको क्या-क्या काम करना पड़ेगा तो जब नई-नई चीज में विद्यार्थी को सीखना है तो उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है और यही रचनात्मक कार्य में आप खुद भी इसे देखते होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा क्या-क्या नई-नई चीज देखनी सीखनी पड़ेगी तो यह चीज भी हम इसमें देख रहे हैं कोशिश रहेगी कि बाकी चीजों के साथ-साथ एक छोटा सा सेंटर यहां साइंस का भी खोला जाए डेवलप करवाना चाहूंगा जो कि आप लोगों के द्वारा ही बनाया जाए विद्यार्थियों के द्वारा ही बनाया जाए।
अरमान नदीम:- आपने विश्वविद्यालय के प्रशासन की तारीफ की लेकिन सर में एक छोटी सी घटना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ,आज से तकरीबन तीन महीने पहले दीपावली से कुछ दिन पहले अपने डिपार्टमेंट के बॉयज वॉशरूम के जो वाटर टैप है उसकी फिटिंग वहां से हटा ली गई , और जब उसकी शिकायत वहां के हेड तक पहुंचाई गई तो पहले तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और जब मैं खुद गया अपने 2 एल एल बी के साथी हर्षवर्धन सिंह सिद्धू और हिमांशु शर्मा के साथ और जब वहां बात की गई तो उन्होंने शुरू में हमे कहा लगा दी जाएगी और फिर कुछ देर के बाद एक अलग तरीके से बहस करते हुए हमे कहते है की ये जो आप माँग कर रहे हो उसे रिटन में दीजिए और उन लोगों को पकड़िए जो हमें सबकी क्लेरिफेकेशन की रिपोर्ट देते हैं यानी कि वह हमसे ही अरगुमेंट कर रहे हैं जबकि सर मैं कहना यह चाहूंगा कि इन सब चीजों की तो मांग होनी ही नहीं चाहिए यह तो सबसे बेसिक चीज़े हैं और जब इस तरह की चीजों पर हमें अरगुमेंट करना पड़ता है तो सोचने पर हम मजबूर होते है क्या हम सच में एक विश्वविद्यालय में है? हमने प्रशासन को ऐसे भी देखा है हमने। इस पे आप क्या कहेंगे?
डॉ. रविन्द्र मंगल :- देखिए इस तरह का जिस किसी ने भी स्टेटमेंट दिया है यह गलत है और इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको बता सकता हूं ये घटना जैसे ही मेरे संज्ञान में आई वेसे ही इस पर एक्शन लिया । और जब मैं वापस आया अपने विदेश दौरे से यह उस वक्त की बात है और उस वक्त भी लीकेज की प्रॉब्लम थी डिपार्टमेंट के वॉशरूम में जब पता किया गया कि इसका क्या कारण था और फिटिंग क्यों नहीं है तो यह मालूम हुआ कि जो नल हैं वो चोरी हुए थे। और मैं आपको कहूँगा ऐसी बात भी नहीं है कि काम नहीं करते या फिर उस पर सुनवाई नहीं होती है। आपने कहा जिससे भी आपकी बात हुई है इस स्टेटमेंट की मैं आलोचना करता हूं। जिस वक्त यहां सफाई हो रही थी गर्ल्स वॉशरूम के साइड में तो मैंने वहां से ही दो बच्चियों को बुलाया और कहा कि यह आपकी भी जिम्मेवारी है कि अगर आपको कुछ गलत लगता है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है तो आप शिकायत कीजिए उस पर बात होगी और क्योंकि यह आपका डिपार्टमेंट है आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इसे साफ सही रखने की । और जो जिस तरीके से तोड़फोड़ अगर कोई करता है या फिर जो चोरी होती है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। यह भी बात कहीं की आप बताइए कि क्या काम सच में हो रहा है तभी मैं इसकी वेरिफिकेशन के लिए साइन करूंगा वरना मैं यह साइन यहां से करके नहीं भेजूंगा आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि वाकई में आपके डिपार्टमेंट में आपके सुविधा पूर्वक कार्य हो रहा है या फिर नहीं। इस बात को मैं भी समझता हूं जानता हूं कि बच्चों की जो शिकायतें होती है वह बहुत छोटी-छोटी होती है लेकिन वह बड़ी जरूरी भी होती है वह गैर जरूरी चीजों में कभी बात नहीं करते है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि मेरे चालिस साल के अनुभव में मैंने कभी भी बच्चों को गलत चीज की मांग करते हुए नहीं देखा वह जब भी मांग करेंगे तो जेनुइन चीज पर ही अपनी बात रखेंगे । बाय चांस ऐसी कोई चीज हो जाए कि वह जेनुइन बात नहीं है तो अगर हम उन्हें समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह चीज पॉसिबल नहीं है या फिर यह इस दायरे में नहीं है तो बच्चा समझता भी है ऐसी बात भी नहीं है कि वह उस पर अडिग रहता है। एक बात कहूंगा कि अगर काम नहीं भी हो रहा है तो हम सब साथ में मिलकर भी काम करें तो समस्या का निवारण सकता होता है क्योंकि संख्या बल में लॉ डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा है यही कहूंगा कि हम सब साथ में मिलकर लॉ डिपार्टमेंट को नंबर एक डिपार्टमेंट बनायेंगे ।
अरमान नदीम :- अपने बातचीत के दौरान कहा कि प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान होना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए लेकिन एक सवाल यह भी है कि विद्यार्थी दोनों चीजों को बैलेंस किस तरीके से कर सकता है कि वो ज़हनी तौर पर भी ताकतवर हो और ग फील्ड पर भी उसकी पकड़ मजबूत हो यह किस तरीके से बैलेंस होगा क्योंकि कहीं होते हैं जिन्हें थ्योरिकल नॉलेज ज्यादा अच्छी होती है लेकिन फील्ड पर जो काम किया जाता है उन पर एक अलग तरीके की चीज की ट्रेनिंग की जरूरत होती है
डॉ. रविन्द्र मंगल :- अगर मैं विज्ञान के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूं तो बच्चा विज्ञान में प्रैक्टिकल अच्छा कब कर पाएगा जब उसकी थ्योरी अच्छी होगी बिना थ्योरी के तो प्रेक्टिकल कर ही नहीं पाएगा सबसे पहले तो थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है थ्योरी में असल में हो क्या रहा है जैसे कि बता दिया कि भाई इस तरीके से मोटर चलती है या यहां से लाइट आ गई यह तार जोड़ने पर यह होता है वह कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन तो वहां हो रहा है लेकिन बच्चे को समझ कब आएगा जब वह प्रयोगशाला में उसको देखेगा जब वह कम असल में होते हुए देखेगा कि किस तरीके से कौन सी चीज को कहां कनेक्ट करके एनर्जी मिलती है लाइट आती है तो वह चीज होनी भी जरूरी है सब कुछ चीज़ अपनी आंखों के आगे होते हुए देखेगा तब वह उसे थ्योरी को रिकॉग्नाइज करेगा कि हां मैंने इसे पढ़ा था कि यह इस तरीके से चीज होती है और अब मैसेज सामने देख रहा हूं तो वह जब चीज होगी तो उसे बेहतर समझा पड़ेगी चीज सीखना है बच्चा आपको यह भी कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को लेकर यहां हमारे हिंदुस्तान में कमी है और हमारा प्रयास ही है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच को डेवलप किया जाए न सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को बराबर मिली पर मैं आपको यह कह दूं कि मैं एक दिन आपके लोग के बच्चों के साथ ही ऐसा कुछ प्रयोग करने वाला हूं । एक पूरा प्रैक्टिकल फील्ड पर आपको चीज समझने की कोशिश की जाएगी अपन मिलकर ही करेंगे । बता दूं कि उसमें कहीं साइंस नहीं आएगी वहां आपकी ही चीज होगी आपका ही सिलेबस होगा विधि विभाग से ही जुड़े हुई बातों पर हम चर्चा करेंगे और उसे प्रैक्टिकल होते हुए देखेंगे इसमें आपको समझ पड़ेगी विज्ञान की और खेल-खेल में ही आपको लगेगा कि हम विज्ञान को भी समझ रहे हैं देख रहे हैं।
अरमान नदीम :- अभी मौजूदा वक्त में आप यहां लॉ डिपार्टमेंट के हेड हैं कभी कुछ ऐसा सोचा है कि मेरे आने से पहले यह चीज नहीं थी और अभी इस चीज को लेकर यहां समस्या है लेकिन जब मैं जाऊंगा तब यहां ऐसा नहीं होगा। आप अपने पीछे डिपार्टमेंट को किस तरीके से छोड़ा हुआ देखना चाहते हैं?
डॉ. रविन्द्र मंगल :- अपनी वार्ता के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया की हमारी पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर बातचीत चल रही है उम्मीद करता हूं आने वाले छह महीने में जो बदलाव होगा वो आप खुद महसूस करेंगे। डिपार्टमेंट में जो डेवलपमेंट होगा वह दिखेगा ।और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि विकास की गति धीमी होती है धीरे धीरे ही हम बदलाव की तरफ़ आगे बढ़ेंगे काफी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को लेकर मेरे दिमाग में है कई चीज़े हुई है काफी कुछ करना बाकी है। मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है असल मैं बार-बार चीजों को दोहराता रहता हूं जो अथॉरिटीज हैं उनसे कनेक्ट रहता हूं ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधा मिले ये कोशिश है । और सबसे बड़ी जो चीज हमारे दिमाग में है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अलग-अलग क्षेत्र में भी नॉलेज दी जाए न सिर्फ वह किसी एक कोर्स तक सीमित रहे। इस बारे में हम कुछ काम करेंगे। यह भी कहना चाहूंगा कि हमें प्रशासन से लगातार काम लेना है और प्रशासन का रवैया डिपार्टमेंट को लेकर अच्छा रहा है हमेशा से ही और एक बात यह भी है की मां बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है तो मजाक से हटके हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझ नी है और सब मिलके काम करेंगे।
अरमान नदीम - शब्द संवाद के लिए बातचीत करने पर आपका बहुत आभार ।
डॉ रविन्द्र मंगल - धन्यवाद
N Kiran Kumar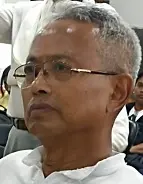
एन किरण कुमार
साहित्य समाज की धड़कन है - एन किरण कुमार
मणिपुरी एवं अंग्रेजी के वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार एन किरण कुमार से शब्द संवाद के लिए अरमान नदीम की खास बातचीत ।
एन. किरण कुमार सिंह जी का जन्म मणिपुर के इंफाल में हुआ था और उन्होंने खुद को एक प्रसिद्ध कवि, गीतकार, अनुवादक और स्वतंत्र लेखक के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने मणिपुर के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में सहायक अभियंता के रूप में कार्य किया, फरवरी 2017 में सेवानिवृत्त हुए। ऑल इंडिया रेडियो, इंफाल और दूरदर्शन केंद्र, इंफाल से जुड़े बेहतरीन गीतकारों में से एक के रूप में जाने जाते हैं, वे मणिपुरी और अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं। सिंह ने कविता के दो प्रशंसित संकलन लिखे हैं: ई ईशेई शेरेंग (स्वयं गीत और कविता) और मेई एशिंग नुंगशिट (अग्नि, जल और वायु)। अनुवादक के रूप में उनका योगदान उल्लेखनीय है, जिसमें ऐनी फ्रैंक की द डायरी ऑफ़ ए यंग गर्ल, सरला बेन मजूमदार की महात्मा गांधी पिक्चर एंड स्टोरी, अमरीक सिंह पाहवा की मणिपुर ऑफ़ माई ड्रीम्स और श्रीमद राजचंद्रजी की आत्मसिद्धि शास्त्र का मणिपुरी में अनुवाद शामिल है। साहित्य समुदाय के भीतर उनका नेतृत्व साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के मणिपुरी भाषा सलाहकार बोर्ड के संयोजक के रूप में उनकी सेवा और मणिपुर राज्य कला अकादमी (2018-2022) की सामान्य परिषद के सदस्य के रूप में उनकी भूमिका से प्रतिष्ठित है। उन्होंने अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक लगातार दो कार्यकालों के लिए मणिपुरी लिटरेरी सोसाइटी, इम्फाल के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वर्तमान में, वे भाषा विकास और कार्यान्वयन निदेशालय, मणिपुर के भाषा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं।
अरमान नदीम :- नमस्कार सर , सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा की आपसे मुझे अपना सानिध्य प्रदान किया। मैं कहना चाहूँगा की आपका साहित्य समाज के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है और एक बार उर्दू के मशहूर अफसानानिगार साअदत हसन मंटो ने कहा था की मेरे शब्द समाज के लिए आईना है। मेरा मानना है की साहित्य समाज का आईना है।
किरण कुमार सिंह :- अरमान आपने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है और यह बात सच भी है लेकिन मैं इससे बढ़कर एक बात और कहना चाहूंगा कि साहित्य समाज की धड़कन है मैं ऐसा मानता हूं। आप जितना भी चाहे इसे नहीं रोक सकते। अगर किसी शरीर में धड़कन नहीं तो वो मुर्दा है।
अरमान नदीम :- बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने की साहित्य समाज की धड़कन है। और धड़कन के बिना शरीर नहीं वो मुर्दा है।तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस धड़कन को अपने पहली बार कब महसूस किया ,साहित्य में पहला कदम कैसे पड़ा आपका।
किरण कुमार सिंह :- साहित्य की शुरुआत यह बहुत लंबी कहानी है असल में मेरे दादाजी के जो भाई थे वह लेखक भी थे और गायन में उनका कौशल बहुत था और मैं आपको कहूं की वो बड़े कलाकार थे साथ ही राजनेता भी थे। मणिपुर में सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट शुरू हुआ था वो उस वक्त से राजनीति में थे। जब मेरी प्राथमिक शिक्षा चल रही थी तो उस वक्त मैं उनके साथ वक्त बिताता था क्योंकि वह शुरुआत से ही लिखते थे और दूसरी भाषाओं से अनुवाद भी किया करते थे। जैसे की बंगाली से मणिपुरी में। उस वक्त मेरी उम्र रही होगी 4- 5 साल और मैं समझता हूं कि मेरी साहित्य में शुरूआत वहीं से हुई क्योंकि जब वह अनुवाद किया करते थे बंगाली से तो मैं उनके पास बैठा करता था और उन्हें सुना करता था, पढ़ा करता था। भगवान की दया ही कहूंगा कि जब मैं बहुत छोटा था उस उम्र से ही मैं मणिपुरी भाषा को एकदम अच्छे से पढ़ और लिख सकता था । महाभारत को मैं बहुत कम उम्र में पढ़ लिया करता था। उस वक्त मेरी उम्र यही कुछ चार साल थी और वहीं से मेरे भीतर साहित्य के प्रति रुचि जागृति और मैं दिल से यह कह सकता हूं कि साहित्य के प्रति मेरा पहला कदम वही था। और मेरी ग्रैंड मदर जो की सिंगर थी मणिपुरी में वहां से मेरे भीतर संगीत के प्रति भी प्रेम बड़ा तो मैं कह सकता हूं साहित्य और संगीत दोनों ही मैं बचपन से ही अनुभव किए हैं। लेकिन साहित्य की मुख्य धारा में मैं बहुत-बहुत बाद में आया आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी गा सकता हूं क्योंकि मेरा जो परिवार है वह संगीत साहित्य रंगमंच कला से जुड़ा हुआ है। Modern music club हमारे गांव में उसे वक्त एक क्लब हुआ करता था जिसका नाम था मॉडर्न म्यूजिक क्लब तो जब मैं वहां से जुड़ा हूं उनसे तो गीत भी लिखना शुरू किए । कोई गीत लिखा तो उसको कंपोज भी किया करता था । तो यह सब चीज भी मैं उन दिनों में उसे आंदोलन ही शुरू की। अरे क्लब का वार्षिक उत्सव भी होता है तो उसके अंदर में गाता भी हूं।
अरमान नदीम :- साहित्य से जुड़े लोगों का हमेशा से प्रयास रहता है कि वह विवादों से दूर रहें और उनका अगर कोई ऐसा है तो उसका समाधान भी करें लेकिन एक चीज शुरू से अब तक चली आ रही है और उसका समाधान नजर भी नहीं दिखता । भाषा विवाद को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है।
किरणकुमार सिंह :- सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं कहीं भाषाओं में लिख सकता हूं बोल सकता हूं काम कर सकता हूं दूसरी भाषाओं का अनुवाद भी करता हूं।
अरमान नदीम :- सर यह बात सच है और मैं यह कहना चाहूंगा कि यह इंसानी फितरत है आप चाहे हिंदी भाषा हो या दूसरी भाषा का व्यक्ति हो वह कोशिश करता है की हम सिर्फ खुद को श्रेष्ठ दिखाएं बाकी जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं । आप और हम लिख सकते हैं लेकिन हम किसी गायन वाले को यह नहीं कह सकते कि भाई तुम लिख नहीं सकते इसलिए तुम्हारी कला का हम सम्मान नहीं करेंगे । व्यक्ति गायन में कुशल है और वह मुझे कहे कि मैं तुम्हारे लेखन को नहीं मानता तो यह इस तरह की चीज करना मेरी नजर में बेवकूफी है और जब अगर हम कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो हमारा विशेष जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के के विवादों को सुलझाने का काम करें।
किरणकुमार सिंह :- अरमान जी, मैं आपकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूं इस तरह की सोच और इस तरह की की बातें नहीं होनी चाहिए समाज में जैसे कि मैं आपको कहा कि मैं कईं भाषाओं में काम कर सकता हूं । हिंदी इंग्लिश मणिपुरी लेकिन अगर मुझे कोई यह कहे की हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को चुनो तो मैं हिंदी को चुनूंगा। मैं आपको यह कहना चाहूंगा की अंग्रेजी काफी अच्छी है, रचनाएं हैं काफी किताबें हैं जिन्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद भी करता हूं मुझे उनमें से भी प्रेरणा मिलती है आपको कहना चाहूंगा की हिंदी से मुझे प्रेम है । बताना चाहूंगा कि मैं उर्दू भी थोड़ी-थोड़ी समझता हूं । कई किताबें उर्दू की है ज्यादा समझता नहीं हूं लेकिन मुझे उर्दू अच्छी लगती है और मेरे पास काफी किताबें हैं उर्दू की। चंद्रभान ख्याल साहब वह मेरे काफी अच्छे दोस्त मैं कई बार उनसे कॉल करके पूछता हूं की इस शब्द का क्या मतलब होता है , इसे क्या कहते हैं तो इस तरह की की चीज में करता हूं क्योंकि हिंदी और उर्दू में कई चीज समान है । जब मैं हिंदी और उर्दू दोनों को देखता हूं या उनकी रचनाएं पढ़ता हूं तो मुझे एक अलग तरह की प्रेरणा मिलती है । कई बार जैसे मैं उर्दू पढ़ता हूं या हिंदी करता हूं तो जो मैं उसको सोचता हूं और जो मैं अपने ख्याल में उसका ट्रांसलेशन करता हूं और जब उसे हिंदी के या उर्दू के शब्दकोश से मैं तुलना करता हूं तो मैं यह पता हूं कि वह जो मैंने सोचा है उसका असल अनुवाद से कहीं अलग है यानी की एक नई चीज मुझे मिल जाती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यह जो भाषा विवाद है यह इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए हमें नई-नई चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए दूसरी भाषाओं से भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह की लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए मेरे विचारों में। मैं कहना चाहूंगा चाहे कोई भी भाषा हो हिंदी इंग्लिश उर्दू तेलुगु मणिपुरी उनके जो शब्द है वह ऊर्जा के स्रोत हैं और वह ऊर्जा क्या है आपके मन में आपके दिमाग में जो ख्याल है वह ऊर्जा है। इसमें आपकी खुशी आपका दुख आपकी चिंता आपके जो भाव हैं वह प्रकट होते हैं इसे।
अरमान नदीम :- बिल्कुल आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही और हम तो लेखनी और साहित्य से ही जुड़े हैं तो मैं आपसे आगे यही पूछना चाहूंगा कि आप जब लिखते हैं या फिर मैं यूं कहूं सीधे-सीधे क्या आप अपनी लेखनी को या साहित्य को सफल कब मानते हैं।
किरणकुमार सिंह :- मौजूदा वक्त में मैं अपनी साहित्यिक रचनाओं में ज्यादातर गीत और कविताएं लिख रहा हूं और अपने सवाल किया की लेखनी को सफल कब माना जाए तो मेरी नजर में तो जब आपकी ऑडियंस जब जनता उसे स्वीकार करें वही सही मायने में साहित्य सफल होना है । यह एक मेरा पर्सपेक्टिव है की मैं इसे इस प्रकार से सफल मानता हूं। और मैं आपको एक किस्सा सुनना चाहूंगा । छोटा सा किस्सा है की जब एक बार कविता सुना रहा था वह पहली बार ही था कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी कोई रचना सुन रहा था और कविता पढ़ने पढ़ने लोगों ने जो उसे इतना प्यार दिया वह मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। और जब मैं अपनी रचना सुन कर मंच से नीचे उतर रहा था तो वहां संगीतकारों का जमघट बन गया और सभी मुझे गले लगा कर यह कहने वालों की बहुत ही खूबसूरत रचना आपने प्रस्तुत की तो जब इस तरह की चीज होती है तो लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लिखने को सफलता की ओर ले जा रहे हैं।
अरमान नदीम :- बहुत ही सत्य वचन हैं आपके और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि पब्लिक की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और यह बात सच भी है और सभी लोगों के इसकी परिभाषा अपनी-अपनी हो सकती है। मौजूदा वक्त में मणिपुर के जो हालात हैं उसे पर आप कुछ अपनी राय देना चाहेंगे कि यह कब सब सामान्य स्थिति में आएंगे।
किरण कुमार सिंह :- मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है रत्नभूमि, लेकिन पिछले कुछ दशकों से भारत के इस सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र की चमक लगातार हिंसा और घृणा का केंद्र रही है। ऐसा माना जाता है कि राज्य में सांप्रदायिक दुर्भावनाओं के कारण वर्तमान अशांति की स्थिति है और यह क्षेत्र समुदायों के बीच जातीय संघर्षों का शिकार हो गया है। इसके कारण मैतेई और कुकी समुदायों के बीच अशांति की वर्तमान स्थिति पैदा हो गई है।
मणिपुर के प्रमुख समुदाय जिनमें मैतेई, नागा, कुकी और मैतेई पंगल शामिल हैं, प्राचीन काल से आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं; और समुदायों के बीच दरार पैदा करने वाले कई मुद्दों में से एक मणिपुर में एक अलग कुकी होमलैंड बनाने का विचार था, जो लगभग तीन दशक पहले सामने आया था। यह विचार अंततः मणिपुर के वर्तमान भूभाग के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा करने वाले कुकी की एक विशिष्ट अलग प्रशासनिक इकाई की वर्तमान मांग में तब्दील हो गया। किसी समूह द्वारा स्वायत्तता की मांग कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह मुख्य रूप से संसाधनों पर विशेष अधिकार और नियंत्रण प्राप्त करने के बारे में है, जिसे मुख्य रूप से साझा किया जाना चाहिए, लेकिन अन्यथा राजनीतिक शक्ति वाले समुदाय द्वारा इसका आनंद लिया जाना चाहिए।
होमलैंड स्थापित करने के लिए कुकी लोगों की कार्यप्रणाली बल के माध्यम से भूमि खरीदना या अधिग्रहण करना था, जिसे वे अपनी वैध संपत्ति मानते हैं। इसके लिए भारी मात्रा में धन और बाहुबल की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण अंततः हेरोइन के लिए अफीम की खेती की जाने लगी। यहाँ, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि म्यांमार से विस्थापित कुकी-चिन आबादी, जो स्वभाव से खानाबदोश है और व्यापार में अनुभवी है, ने मणिपुर में कुकी समुदाय को संगठित किया और एक विशाल ड्रग और हथियार कार्टेल स्थापित करने में मदद की, जिसके जाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच चुके हैं।
कुकी होमलैंड की खोज की आक्रामक प्रकृति ने 1992 में नागा-कुकी संघर्ष को भड़का दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसमें कुकी समुदाय को बड़ी क्षति हुई। मणिपुर के पहाड़ी जिलों में राज्य के आरक्षित वन क्षेत्र में विस्थापितों, कुकी आबादी के पीड़ितों को बसाने की सरकार की दोषपूर्ण योजना तब विफल हो गई जब भारत-म्यांमार सीमा पार से शरणार्थियों और अप्रवासियों ने आरक्षित क्षेत्रों का पूरा नियंत्रण और लाभ उठाते हुए उन कई पहाड़ियों में अफीम की खेती शुरू कर दी, जिन पर वे कब्जा कर रहे थे। इसने मणिपुर के सामने मौजूद गोल्डन ट्राइंगल की भयावहता और खतरों की आग में घी डालने का काम किया है। यह माना जाता है कि ऑपरेशन के निलंबन के तहत कुकी उग्रवादियों ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते का पूरी तरह उल्लंघन और अवहेलना करते हुए इन स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई। हेरोइन का ऐसा अवैध उत्पादन और व्यापार 10-12 साल पहले चरम पर था, जब क्षेत्र और भारत के विभिन्न हिस्सों के हजारों युवा इसके शिकार हुए।
मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल में नशीली दवाओं के खिलाफ एक नाटकीय युद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें अफीम के बागानों को नष्ट करना इसका एक प्रमुख हिस्सा था। स्थानीय लोगों के सहयोग से सरकार ने कड़ी बाधाओं के बावजूद अफीम की खेती को नष्ट करने में बड़ी तेज़ी से कामयाबी हासिल की। यह तो बताना ही होगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स, जिनमें ज़्यादातर हेरोइन होती है, की खेप से यह स्पष्ट था कि ड्रग माफिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और राज्य सरकार के खिलाफ़ उनकी तरफ़ से किसी भी समय अचानक प्रतिक्रिया की आशंका थी। ड्रग्स के खिलाफ़ युद्ध अभियान के परिणामस्वरूप, राज्य के कई हिस्सों में आरक्षित वन क्षेत्रों से अतिक्रमणकारियों को व्यापक पैमाने पर बेदखल किया गया। अतिक्रमणकारियों, मुख्य रूप से कुकी, को बेदखली अभियान का सामना करना पड़ा और इससे राज्य सरकार के खिलाफ़ उनकी पहले से मौजूद दुश्मनी और भी बढ़ गई। यह भी उल्लेखनीय है कि कुकी समूहों की गतिविधियों के बाद एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने एक दशक से भी ज़्यादा समय से चले आ रहे त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग कर लिया। यह भी सवाल उठता है कि सीएसओ या कुकी समुदाय के नेताओं ने अवैध सीमा पार आप्रवासियों के प्रवेश, आरक्षित वन क्षेत्रों में उनके अनियंत्रित अतिक्रमण या राज्य में अफीम की व्यापक खेती के खिलाफ एक शब्द भी क्यों नहीं कहा, वह भी इतने वर्षों से।
ताबूत में आखिरी कील मणिपुर उच्च न्यायालय का गलत समय पर दिया गया फैसला था, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह मेइती लोगों की मांग के संबंध में चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले की उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। मणिपुर के आदिवासी लोगों की एक बड़ी चिंता यह थी की मणिपुर के प्रमुख समुदाय मेइती को अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है, तो वे पहाड़ियों पर जमीन हासिल करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, जो अब तक भारतीय संविधान के मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम 1960 के तहत संरक्षित है। इसके अलावा राज्य के आदिवासी आम तौर पर मेइती लोगों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों और प्रवेश की लगभग सभी प्रविष्टियों में आरक्षित सीटों को हासिल करने में उनके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, मणिपुर (ATSUM) ने अवसर का लाभ उठाते हुए मणिपुर के पहाड़ी जिलों में मेइती लोगों को एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने के खिलाफ तथाकथित एकजुटता जन रैलियों का आयोजन किया। इसने कुकी लोगों को राज्य सरकार के खिलाफ पूरी तरह से उकसाने और विशेष रूप से मुख्यमंत्री को निशाना बनाने के लिए और भी प्रोत्साहित किया । 27 अप्रैल, 2023 को कुकीज ने अपने गुस्से का इजहार तब किया जब उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे और उसके उद्घाटन की पूर्व संध्या पर चुराचनपुर में अपना एक ओपन-जिम जला दिया। इसके बाद अगले ही दिन चुराचांदपुर में एक सरकारी वन कार्यालय को जला दिया गया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कुकी कैंप में युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी, जिसके लिए पहले से ही तैयारियां चल रही थीं। तथ्य यह है कि राज्य प्रशासन मूकदर्शक बना रहा और 3 मई, 2023 को चुराचनपुर के कुकीज की "शांति रैली" के दौरान सांप्रदायिक झड़प होने तक कानून और व्यवस्था को लेकर उनका सबसे अज्ञानी व्यवहार रहा, जो पड़ोसी जिले की ओर बढ़ रहे थे, जहां मैतेई लोगों ने जवाबी उपाय के रूप में सड़क नाकाबंदी कर दी, जो राज्य के बुद्धिजीवियों के पतन और प्रमुख कानून और व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए उनकी अक्षम, कमजोर तैयारी के स्पष्ट संकेत हैं। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि कुकी लोगों ने हजारों की संख्या में लोगों के साथ "शांति रैली" निकाली, जिनमें से कुछ अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, जबकि उसी समय भारत के उपराष्ट्रपति मणिपुर विश्वविद्यालय में शिक्षाविदों और छात्रों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कोई भी यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि ऐसी स्थिति की अनुमति कैसे दी जा सकती है या यह जाने-अनजाने में शीर्ष अधिकारियों की ओर से चूक थी।
यदि युद्ध की रेखा धार्मिक विचारधाराओं पर भी खींची गई थी, तो दोनों समुदायों द्वारा धार्मिक स्थलों में आगजनी और तोड़फोड़ भी ध्यान आकर्षित करती है। क्या धार्मिक समूहों का चल रहे अशांति से कोई लेना-देना है ।
फिलहाल, ये प्रश्न दूर की कौड़ी और महज अटकलें हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि अदृश्य विदेशी हाथ हमेशा "युद्ध के मास्टर" रहे हैं और मासूम, नासमझ लोग उनकी कठपुतली रहे हैं। अब समय आ गया है कि तात्कालिक और प्रत्यक्ष से आगे बढ़कर दूरस्थ कारण पर ध्यान केन्द्रित किया जाए तथा शांति और समृद्धि के लिए दीर्घकालिक समाधान पर चिंतन किया जाए।
अरमान नदीम :- साहित्यकार सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाता है और अपनी कलम को एक रिमोट के साथ जोड़ लेता है उसे आप कैसे देखते हैं और मैं मेरी उम्र कोई ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन मैं यह देख रहा हूं लोग जल्दी-जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और उसे चक्कर में वह कितने चक्र में आते हैं यह भी हमको देखने को मिल रहा है। और व्यक्तिगत रूप से हमें परेशानी ऊबी होती है क्योंकि इससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वह साहित्य का है साहित्यकार तो अपना विस्तार कर रहे हैं लेकिन साहित्य संकुचित होता जा रहा है।
किरणकुमार सिंह :- अरमान जी आपने बहुत सही बात कही और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए और पॉलिटिकल अप्रोच साहित्य के अंदर नहीं होनी चाहिए लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा साथी मैं यह भी कहूंगा कि साहित्य में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए बता रहा था की जब 2018 के अंदर मधु जी और मैं एक साथ ही साहित्य अकादमी में जनरल काउंसिल में थे उससे पहले मैंने बहुत सुना था की लोग अवार्ड के लिए किस तरीके से अप्रोच करते हैं या फिर ऑफर्स देते हैं लेकिन वह मेरे साथ पहली बार ही हुआ था कि कुछ आए मेरे पास में इस तरह की की फरियाद लेकर मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा बड़े लेखक माने जाते हैं अवार्ड धारी हैं अभी आपने जैसा कहा ना की बहुत जल्दी-जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी भी कुछ ऐसी ही ख्वाहिशें थी एक सुबह मेरे पास में आए दो-तीन लेखक और मुझे तरह-तरह के ऑफर्स देने लगे मुझे उसे वक्त इतना गुस्सा आया उनकी बातें सुनकर मैं चिल्लाकर उन्हें वहां से भगाया । घर के सभी लोग बाहर आ गए एकदम अचानक से माहौल बदल गया की क्या हो गया क्या हो गया । लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं हुआ मैंने उन्हें बस वहां से भेज दिया उन लोगों को ऐसा पहले भी हुआ होगा मेरे टेन्योर में भी लोग आए मेरे बाद भी हो सकता है ऐसे कहीं चीज हुई होगी लेकिन जब मैं था तो मैं ऐसी किसी भी चीज को ना तो किया ना होने दिया। कुछ तरह की चीज होती है, और लॉबी है बना रखी है उनमें भी लोग अपनी-अपनी से रखते हैं तो हमें अपनी तरफ से तो कोशिश ही रखनी चाहिए की साहित्य को इन सबसे छोटा रखें और लोगों का विश्वास बना रहे और उनका जो स्वार्थ है वह लोगों के विश्वास के बीच में ना सके। इसी के प्रयास में मैं आपको बताऊं की एडवाइजरी कमेटी होती है । मैंने उन्हें चेतावनी दी इस तरह की ना तो चीज होनी चाहिए और ना ही तरह के व्यक्ति सामने आने चाहिए। मैंने उन्हें कहा की मैं यह बात सुनी है कि तुम लोग अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हो क्योंकि मैं भी कमेटी का मेंबर हूं और इस तरह की क्या चीज ना तो मैं करूंगा ना होने दूंगा।
अरमान नदीम :- जी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जिस तरीके से लोगों के जहन में नेताओं की छवि बनी हुई है अगर वह किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में हवाला कांड में उनका नाम आता है तो अचंभा नहीं होता लेकिन अगर एक साहित्यकार, लेखक का नाम कुछ इन चीजों से जुड़े तो शंका बनती है ।और इसी के चलते मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था कलम से हल्की नोट होती है और हल्की-हल्की नोट आपकी जो जेब भारी कर रही है उनसे अब आपका कलम नहीं उठने वाला तो इस तरह की चीज हैं सर और मैं यह जानना चाहता हूं कि हम किस तरीके से इन सब को रोकने का प्रयास कर सकते हैं।
किरण कुमार सिंह :- बहुत ही अच्छा फ्रेज है हल्के हल्के नोटों से जेब भारी करना बहुत शानदार लिखा अरमान आपने बिल्कुल सही भी है। और अगर हम कुछ हटके लिखते हैं तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है सिस्टम के खिलाफ अगर हम काम कर रहे हैं लिख रहे हैं तो।
अरमान नदीम :- आपने सही कहा लोगों को स्ट्रगल करना पड़ सकता है लेकिन सर मेरा लक्ष्य कभी ये नहीं रहा कि मैं लोगों के गुड लिस्ट में आऊ और मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है की क्या मैं आपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक निर्वहन कर पा रहा हूँ या नहीं । और मैं यह कोशिश करता रहता हूं की मैं मेरे लेखन से अगर किसी एक को भी जागरूक कर पाऊ तो मैं अपने लेखन को सार्थक समझता हूँ। मैं समझता हूं कि वह मेरे लेखन की सफलता है क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है हम देख रहे है। किसी एक का नाम नहीं ले सकते उसी तरीके साहित्य में जिस तरीके से लोगों ने इसे बदनाम करने का काम किया है और यहां करप्शन चल रहा है वह जागरूकता के साथ सामने लाना जरूरी है।
किरण कुमार सिंह :- मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं शुरुआत में हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था साहित्य समाज का आईना है और मैंने कहा कि यह समाज की धड़कन है। एक बात और मैं आपको कहूंगा कि लोग इसे रोक नहीं सकते समाज की धड़कन है आप इसे कैसे रोकेंगे। साहित्य तो समाज के अंदर रुकावट पैदा करने वाली चीजों को उजागर करता है अगर इसमें अगर इस तरह के के लोग हैं तो ज्यादा वह हैं जो समाज को बेहतर राह दिखाना चाहते हैं हर चीज ऊर्जा है ख्याल ऊर्जा है इमोशन भाव जिसे हम कहते हैं ऊर्जा है और यह सब चीज बाहर कैसे आती है शब्दों के माध्यम से।
अरमान - शब्द संवाद के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
एन किरण कुमार - आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ।
Ustad Amin Sabri
उस्ताद अमीन साबरी
बॉलीवुड में मेरा सबसे करीबी दोस्त आमिर खान है - उस्ताद अमीन साबरी
अरमान नदीम :- उस्ताद अमीन साबरी साहब आज की तारीख में आपको पूरी दुनिया साबरी ब्रदर्स के नाम से जानती है और मानती भी है लेकिन कम लोग होंगे जो आपके माज़ी से वाकिफ है, आग़ाज़ कैसे हुआ ?
अमीन साबरी :- हम लोग मेंडू के हैं। नवाब के दरबार में हमारे बुजुर्ग मुलाज़मत करते थे . तो उस वक्त यह काम हमारे आबा ओ अजदाद किया करते थे। और वहाँ से मथुरा जाते थे वहां हमारी पेशकश हुआ करती थी बांके बिहारी जी में . तकरीबन 200 साल पहले उस वक्त के जयपुर महाराजा साहब मथुरा गए और उन्हें हमारे बुजुर्गों का गाना बहुत पसंद आया उस वक्त उनको राजा साहब अपने साथ जयपुर ले आए . बाकायदा कहा गया कि मैं इन्हें गुणीजन खाने में रखूंगा और छः रुपए महीना तनख्वाह दूंगा । हमारे परदादा के वालिद साहब उन्होंने शुरुआत की। फिर महाराज से कहा की हमारे पास यहां रहने के लिए कोई जगह नहीं है , जयपुर में ही हवेली दी गई हमें । उस वक्त हवेली में हमारे वालिद ने ,दादा साहब ने रियाज़ किया और मेरे दादा तबला बजाने के साथ गाया भी करते थे। और फिर मेरे वालिद ने भी इसमें बहुत इजाफा किया। डागर बंधु , उस्ताद रहीमुद्दीन खान ,अशरफ उद्दीन खान ,बाबर भाई , फरियाद भाई उनसे गाना सीखा । वहीं से ध्रुपद की शुरुआत हुई। हमारे वालिद क्लासिकल भी जानते थे जब हमारे दादा साहब का इंतकाल हुआ तो हमारे वालिद ने कव्वाली शुरू की और उन्होंने इतना नाम किया ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ,दूसरे देशों में अमेरिका, फ्रांस , इंग्लैंड में उनके प्रोग्राम हुआ करते थे । लगातार दो दफा गोल्ड मेडल जीता 2001 ,2002 में
अरमान नदीम :- जी बिल्कुल यह कहते सुनते गर्व का एहसास होता है की पूरी दुनिया हमारे कलाकारों को मानती है। अमीन साहब बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई?
अमीन साबरी:- हमें काम करने का मौका मिला फिल्म हिना , परदेश , दिल आशिकाना , लव के लिए कुछ भी करेगा में । शुरुआत हिना से हुई और फिल्म हिना के बाद हमारी एक फ़िल्म थी "उफ़ ये मोहब्बत" । आप जानते हैं जॉन अब्राहम जो आज बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड में उनको हमारे एल्बम से प्रमोट किया गया था जिसका नाम था “रब्बा यार से मिला दे” और अवार्ड की फेहरिस्त की बात करें तो अब्बा को राष्ट्रपति अवार्ड मिला था संगीत नाटक अकादमी से । प्रणब मुखर्जी साहब उस वक्त राष्ट्रपति थे। और मैं कहना चाहूंगा कि लोग हमारे नाम का गलत इस्तेमाल भी करते हैं जबकि उन्हें संगीत की रत्ती भर भी समझ नहीं है लेकिन इस सब के बाद भी लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई । जब भी इलाके में कोई खुराफात हुआ करती थी तो इलाके के एस पी साहब आते और कहते साबरी साहब कोई मोहब्बत का तराना सुनाइए भाईचारा फैलाइए -
“हाथों में गीता रखेंगे सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का अमन की एक अज़ान रखेंगे काबा भी होगा काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे” लेकिन आज का आलम अलग है लेकिन साबरी बंधु का यह कहना है - इधर मंदिर ,इधर मस्जिद, उधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा सभी में नजर आता है ईश्वर अल्लाह का जलवा ।
तो हमारे तो यही रहा है अरमान साहब की हमने हमेशा एकता और भाईचारे के लिए काम किया है लेकिन फिर भी क्या वजह है कि लोग हमें नजरअंदाज करते हैं
“दिल ने तेरी गली से किनारा नहीं किया जालिम ने एक काम हमारा नहीं किया और दुनिया की बात छोड़िए दुनिया तो गैर है तुमने भी कुछ ख्याल हमारा नहीं किया”
"कि हम ग़ज़ल में तेरा चर्चा नहीं होने देते तेरी यादों को भी रुसवा नहीं होने देते कुछ तो हम नहीं चाहते शोहरत अपनी कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते। "
और आज के वक्त में हमारा पांच लोगों का ग्रुप है उस्ताद अमीन साबरी ,तनवीर साबरी ,समीर साबरी ,शब्बीर साबरी ,मतीन साबरी।
अरमान नदीम :- जी बिल्कुल हम देख रहे हैं कि आपका नाम इस्तेमाल किया जाता है और पीछे सिर्फ साबरी नाम लगाकर लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश रहती है और जैसे नुसरत साहब भी एक जाना माना नाम है दुनिया में उनसे मुलाकात का मौका मिला ?
अमीन सबरी :- जब मैं परदेश का गाना कर रहा था। तो उस वक्त नुसरत भाई आए जो मुझसे तकरीबन 6 ,7 साल बड़े थे । वह मेरे भाई बड़े जैसे थे तो उनसे मेरी मुलाकात सुभाष घई जी ने करवाई कहा खान साहब यह अमीन साबरी जयपुरी । तो वो इतने खुश हुए बोले अमीन भाई आपका मैंने बहुत नाम सुना है। मेरे वालिद को पाकिस्तान में सैयद जयपुरी के नाम से जाना जाता था और पाकिस्तान के हैं गुलाम फरीद साबरी जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध कव्वाली "भर दो झोली" गाई थी वो जयपुर आए , सब से मिले हमारी बुआ की शादी में भी शिरकत की थी । में तो वहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान में जो भी आर्टिस्ट बाहर से आए उनको इज्जत मिली शोहरत पाई, पैसा कमाया ,ले गए इसलिए मेरा हमारा हिंदुस्तान सबसे प्यारा न्यारा है। मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है भाई साहब ना तो ऐसा देश कहीं है ना यहां जैसे लोग ना ऐसे प्यार करने वाले जो सब मिलजुल कर त्यौहार बनाते हैं । ईद हो दिवाली हो और अगर अल्लाह फिर जन्म दे तो बार-बार हिंदुस्तान में ही जन्म लेना चाहूंगा क्योंकि ऐसा देश पूरी दुनिया में नहीं है । सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ।
अरमान नदीम :- बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने अमीन साहब । अब अगर हम हाल के वक्त की बात करें जो देखा जा सकता है सब कुछ बदल छा गया है नए लोग आ चुके हैं और क्लासिकल शैली को छोड़ते जा रहे हैं और वेस्टर्नाइज्म को बढ़ावा देने वाले लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है ?
अमीन साबरी:- मुझे अफसोस है इस बात का कि हम तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के संगीत को फैला रहे हैं और कुछ लोग वेस्टर्न संगीत ला रहे हैं ,गुमराह कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन सोचेगी यही हिंदुस्तानी म्यूजिक है । रैप सॉन्ग जिसे कहते हैं तो यह गाना थोड़ी है जिसमें ना तो किसी की राग का पता चल रहा है तो कुछ अच्छे लिरिक्स तो हो और ना ही म्यूजिक अच्छा ।
अरमान नदीम :- जी सही फरमाया आपने पहले के गाने सीधा दिल को छूते थे लेकिन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है सब अपने क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है ।
अमीन साबरी:- जी बिल्कुल पहले गाना था सुनने का सुनते थे लोग लगता था कि जैसे रफी साहब को, किशोर साहब को, लताजी को अब देखना अब देखो फलाना आर्टिस्ट चाहे कितना ही बेसुरा हो लेकिन यार कपड़े अच्छे पहने हैं पहले सुनने का था अब देखने का काम है अब बोल देख गाने के बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया क्या लिरिक्स है भाई जिगर है माचिस है क्या है किसी ने लिखा है बदतमीज दिल लेकिन हम तो मानते हैं दिल तो घर है ईश्वर का अल्लाह का ईश्वर बसता है दिल में तो वह बदतमीज कैसे हो गया मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे हिंदुस्तान का म्यूजिक कुछ लोग बिगड़ने पर लगे हैं बजे उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करने के के देखिए हिंदुस्तान का असली म्यूजिक यह है जब लता जी रफी साहब गया करते थे भजन गया करते थे तो कितना सुख चैन मिलता था जैसे आप सुनिए सुख में सब साथी दुख में ना कोई तो यह बोल है मेरे राम मेरे राम और
अरमान नदीम :- और एक नया ट्रेंड आया है सूफियाना बनाने का गजल के टोन, अल्फाज को उठाकर मन मुताबिक बनाकर उसे भी सूफिया कलाम कह दिया जाता है।
अमीन साबरी:- नहीं नहीं सूफिया नहीं कहा जा सकता उनको अपने कालम में सिर्फ अल्लाह ईश्वर का नाम डाल देने से वह सुफियाना नहीं हो जाता । सूफी साहित्य को पढ़ना पड़ता है अदब की जानकारी होनी जरूरी है और जो सूफी होता है ना वह फिर चाहे पीर हो फकीर हो अच्छा गुरु हो संत हो सुफियान होने का मतलब है वह ईश्वर से लौ लगाता है । उसे इंसान से तलब करने की जरूरत नहीं होती
अरमान नदीम :- जी, सही बात है लेकिन कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि इसमें भी मजहब के नजरिए से देखना शुरू कर दिया गया है। हद तो यह है कि हम हर चीज में कहा जाता है कि इस्लामीकरण किया जा रहा है मतलब कि सिर्फ इस्लाम से जोड़ा जाता है कि पीर फकीर कुछ शब्द दिमाग में इस तरह भर दिए गए हैं उर्दू बोलने वाले है तो उनको कहते हैं इस्लामी करण हो रहा है ऐसी बचकानी और दिल तोड़ देने वाले बयान हमें सुनने को मिलते हैं आज के दौर में।
अमीन साबरी:- “यह अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूते में कई ताज़ पड़े रहते हैं” वह अगर नजर भर के देख ले ना तो किसी को तो वह वाले नारे हो जाए और आपने सही कहा कि सूफियाना कलाम का मजहब से ताल्लुक यूं नहीं है वह एक प्रेम भाव है जो सभी के लिए है उसे किसी एक मजहब से जोड़कर देखना सही नहीं है
अरमान नदीम :- क्योंकि कला साहित्य संस्कृति संगीत ऐसी चीज हैं जो इंसान के सीधे दिल को छूती है । लेकिन अब क्या कह सकते हैं कि इसमें भी सियासत की जाती है आप देखेंगे अवार्ड है तो वह कोशिश यह रहती है कि अपने पसंदीदा को दिलाए और उसमें सिफारिश चलती है।
अमीन साबरी:- बस यही है नाच ना जानू आंगन टेढ़ा। अब उनसे कोई पूछे उनको कुछ आता नहीं है लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं बस लेकिन लोगों को भी समझ में आता है ।ऐसा नहीं है कि लोग इनकी बदमाशी को समझ नहीं रहे हैं ।
अरमान नदीम :- बॉलीवुड में सबसे करीबी दोस्त कौन है आपका?
अमीन साबरी:- मेरा सबसे करीबी दोस्त बॉलीवुड में आमिर खान है। फिर जॉन इब्राहिम, चंकी पांडे सब से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है । ट्विंकल खन्ना की पहली सालगिरह थी तो एक प्रोग्राम हुआ था उनके यहां उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी । ट्विंकल खन्ना से भी बातचीत बहुत है। दत्त साहब नरगिस जी के घर बहुत प्रोग्राम हुए। और सलीम साहब के यहां बहुत आना-जाना रहता था। सलमान खान बॉलीवुड में आए नहीं थे तब से हमारी बातचीत है ।
अरमान नदीम - बेहद शुक्रिया साबरी साहब"शब्द संवाद" के लिए वक़्त देने के
अमीन साबरी - शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी ।
